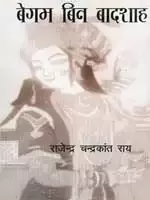|
कहानी संग्रह >> बेगम बिन बादशाह बेगम बिन बादशाहराजेन्द्र चन्द्रकांत राय
|
322 पाठक हैं |
||||||
समाज से बहिष्कृत पात्रों का चित्रण
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राजेन्द्र चन्द्रकांत राय तीन दशक से कहानियाँ लिख रहे हैं। विभिन्न समयों
में उनकी कहानियाँ प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई हैं। उन
पर चर्चा, विवाद भी हुए हैं, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई भी संगृहीत
किताब इसके पूर्व नहीं आ सकी है। यानी ‘बेगम बिन बादशाह’ उनका
पहला कहानी संग्रह होगा। राजेन्द्र चन्द्रकांत राय ने पिछली अवधि में कई
कहानियों को रद्द किया, कई का पुनर्लेखन किया और संग्रह में समाविष्ट
कहानियों के अलावा इस बीच कई लम्बी कहानियाँ लिखीं, जो दूसरे संग्रह में
आएँगी और एक भिन्न एवं बदली हुई दुनिया में पाठकों को ले जा सकेंगी।
चन्द्रकांत राय की रुचियाँ, आग्रह और विशेषज्ञता में वनस्पतियो,
पशु-पक्षियों, पर्यावरण और उसके बीच लुटते हुए मनुष्य तथा सभ्यता का दर्द
और विस्थापन है। उसके पास एक शैलीकार का आवेग और वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि
है-इसी से उनके गद्य की बुनावट हुई है। यह कहानी संग्रह उनकी गुमनामी और
परिस्थिति को किंचित् तोड़ सकेगा अन्यथा आठवें दशक के कहानीकारों की सूची
में अब तक वे प्रमुखता से हो सकते थे।
‘बेगम बिन बादशाह’ की कहानियों में मामूली, अदने, वंचित इंसानों का प्रवेश और चयन है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। ये नाचीज पात्र मनहूस, दब्बू और पराजित नहीं हैं, वे बिना किसी अतिरेक स्वाभाविक रूप से संघर्षशील हैं, जीवनमय हैं और भरोसे को खंडित नहीं करते। उनकी कहानियों में ऐसे पात्रों का वातावरण हमेशा बना रहता है, जो समाज से बहिष्कृत हैं, समाज के सीमांतों पर ठेल दिये गये हैं, पर इसके बावजूद वे हाहाकार नहीं करते, मुठभेड़ करते हैं। वे भटककर विलीन नहीं हो जाते। चरित्र की जगह पात्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि चंद्रकांत राय के चरित्र जीवन-संग्राम में अभिनय कर रहे हैं। इसी को मैं कहानी मानता हूँ। उनकी कहानियों में असंतुलित उम्मीद या रोशनी भी नहीं है। तर्क और विश्वास है। केवल व्यंग्य और वीरता का सहारा उन्होंने नहीं लिया है। स्वतंत्रता के बाद जो अवसाद हिन्दी कहानी में पनपा था, यहाँ उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चन्द्रकांत राय की कहानियाँ इस प्रकार वैयक्तिक कला की उपज नहीं हैं, वे विचार के साथ आते हैं, विचार स्थूल रूप से प्रकट नहीं हैं, किस्से-कहानी-जीवन में विलीन रहते हैं। इस तरह पाठक उनके बारे में अपनी राय तय कर सकते हैं।
‘बेगम बिन बादशाह’ की कहानियों में मामूली, अदने, वंचित इंसानों का प्रवेश और चयन है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। ये नाचीज पात्र मनहूस, दब्बू और पराजित नहीं हैं, वे बिना किसी अतिरेक स्वाभाविक रूप से संघर्षशील हैं, जीवनमय हैं और भरोसे को खंडित नहीं करते। उनकी कहानियों में ऐसे पात्रों का वातावरण हमेशा बना रहता है, जो समाज से बहिष्कृत हैं, समाज के सीमांतों पर ठेल दिये गये हैं, पर इसके बावजूद वे हाहाकार नहीं करते, मुठभेड़ करते हैं। वे भटककर विलीन नहीं हो जाते। चरित्र की जगह पात्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि चंद्रकांत राय के चरित्र जीवन-संग्राम में अभिनय कर रहे हैं। इसी को मैं कहानी मानता हूँ। उनकी कहानियों में असंतुलित उम्मीद या रोशनी भी नहीं है। तर्क और विश्वास है। केवल व्यंग्य और वीरता का सहारा उन्होंने नहीं लिया है। स्वतंत्रता के बाद जो अवसाद हिन्दी कहानी में पनपा था, यहाँ उससे आपको मुक्ति मिलेगी। चन्द्रकांत राय की कहानियाँ इस प्रकार वैयक्तिक कला की उपज नहीं हैं, वे विचार के साथ आते हैं, विचार स्थूल रूप से प्रकट नहीं हैं, किस्से-कहानी-जीवन में विलीन रहते हैं। इस तरह पाठक उनके बारे में अपनी राय तय कर सकते हैं।
बेगम बिन बादशाह
लंबे निर्वासन के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद् में पुनः शामिल किया
गया था। शपथ लेने के दूसरे सप्ताह ही वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के
जनसंपर्क दौरे पर निकल पड़े थे। बगुले के पंखों जैसी सफेदी लिए धोती और
कुर्ते में सजा, देवपुरुष सा अनुपम व्यक्तित्व, गृहमंत्री पद की आभा से और
तीखा बन गया था। लंबी सुघड़ काठीवाली उनकी यूनानी देह सदैव ही सद्यःस्नात
लगा करती है। यात्रा की थकन और श्रम की शिकन आज तक उन पर अपना एक निशान तक
न छोड़ पाई है, गोया उनके प्रभामंडल के दायरे में उनका प्रवेश ही वर्जित
हो। मानव आकृति में किसी कुशल संगतराश के सधे हाथों से खचित प्रस्तर
प्रतिमा ही हैं वे। जो भी सामने आता है, मोहाविष्ट, मंत्रमुग्ध और तरल
होने लगता है।
ठेठ देहाती इलाका है उनका निर्वाचन क्षेत्र। ग्रामीण मतदाता उनके राजसी वैभव को देखकर किलके पड़ रहे थे। अनगिनत सरकारी जीपें, समर्थकों की कारें, व्यापारियों-सेठों के वाहन, पार्टी कार्यकर्ताओं से लदी फदी जीपें....। कुल मिलाकर वाहनों का एक लंबा काफिला जिस गाँव की धूल धूसरित सड़क से गुजरता पाजामे, धोतियाँ, बंजियाँ, बीड़ियाँ और पगडंडियाँ उछाह से मुग्ध-मुग्ध हो जातीं। गाँवों के मुहानों के आम्र-पत्तों के द्वार, बंदनवार और रंगीन कागजी झंडियों, पार्टी-ध्वजों से स्वागत का आयोजन उन्हें भी भीतर तक आह्लादित किए जा रहा है। भीड़ की भीड़ आती। एक दूसरे पर गिरती पड़ती। रोली का तिलक दप-दप करते भाल पर लगता। फूलमालाओं में आदर भरी श्रद्धा भी पिरोई गई होती। भक्ति में डूबकर पाँव छूने की होड़ जारी है। सुदर्शन मुख की धवलता, रोली में रँगकर यों हो गई है जैसे दही में सेंदुर घुल रहा हो।
दिन-भर में ऐसी ही छोटी-बड़ी पचीस-तीस स्वागत-सभाएँ उन्होंने संबोधित की हैं। उन्होंने सधे और सहज लहजे में अपने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन का श्रेय मतदाताओं को दिया। मतदादा गद्गद हो उठे। उनकी आँखों में आँसू डबडबा आए। गले रुँध गए।
साँझ के करीब-करीब काफिला जंगल से घिरे डाकबँगले में आ टिका। बारिश हुई है। घनघोर। जंगली बरसात ने शाम को अपने गीलेपन में लपेट लिया है, दूर-दूर तक नीली धुआँती पहाड़ियों से घिरा सौ-पचास घरों वाला निरा देहात पानी में भीगकर, तालाब में डुबकी लगाकर निकला-निकला-सा लग रहा है। थकन की एक बारीक शिकन, अपूर्व दुस्साहस से उनके चेहरे पर चुपके से आकर लेट गई थी, गो कि वे उसे निंदियाने से लगातार टाले जा रहे हैं।
डाकबँगले के सामने वाले बरामदे में उन्होंने आरामकुर्सी डलवा ली थी। उसी पर बैठ झिम-झिम बरसते पानी में झिलमिलाती बजरी पर नजरें गड़ाए वे अतीत में उतरते जा रहे हैं।
सरकारी अफसर और दोयम दर्जे के नेतागण डाकबँगले के पिछवाड़े चाय-नाश्चे और आपसी स्वार्थचर्चा में लिप्त हो गए हैं। नीला अँधेरा क्रमशः गहरा हो रहा है, जबकि पेड़ों से टपकता हुआ पानी उसे घोल देने को कमर कसे हुए है।
किसानों का एक झुंड उनसे मिलने को आतुर हो रहा है, किंतु डाकबँगले के द्वार पर खड़ा पुलिस अफसर नहीं चाहता कि ‘साहब’ डिस्टर्ब हों। उनकी निगाहों ने बात पकड़ ली और किसानों को आने देने का संकेत किया।
वे सब ओला-पीड़ित थे। उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। वे दुखी थे-बरसात और आँसुओं से भीगे हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। कलेक्टर से, जो पहले ही पीछे आकर खड़े हो गए थे, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मदद के बारे में जाना और राहत राशि तुरंत देने की हिदायतें दीं। किसान लौट गए। वे फिर गीली शाम और भीगी पहाड़ी पीने लगे।
कौन जानता है कि आज के वैभव का किला, कल की तकलीफों और संघर्षों की बुनियाद पर खड़ा है। जितने कड़वे-मीठे दिनों से जूझकर वे यहाँ तक पहुँचे हैं, वे आज भी, अब भी अंदर कहीं जीवित हैं। चीटियों की लंबी कतार से असह्य वे दिन। भीड़ से घिरे वे मुस्कुराते रहते हैं, अंदर कोई अपना नहीं होता। लोगों की भीड़ आती है और अपनी तकलीफों के लंबे बयानों के एवज में उनसे राहत और सांत्वाना के ढेर ले जाती है।
आठ साल के इस अरसे ने और टीसें दी हैं-प्रांत में उनकी वट राजनीति के आश्रय में असंख्य अमरबेलें छितरा गई थीं, पर उनके मंत्रिपरिषद से हटते ही परजीवी अमरबेलों ने अपने ही मातृवृक्ष के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूँककर अपनी नपुसंकता के पोस्टर लगाए थे और सत्ता का छाता पाने चल दी थीं।
सूखे दिन उन पर तो कोई सूखी छाया न डाल सके, पर उन दिनों के मुट्ठी भर साथियों ने दसियों बार भाँति-भाँति से जताया था कि वे उनके बुरे दिनों के साथी हैं। इस तरह वे सब अपनी कीमत के प्रति खुद ही आश्वस्त हो लिया करते थे।
लंबी राजनीतिक जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आया, जो उनके भीतर के दर्द को सहला जाता। अकेलेपन को थपती दे जाता।
कोई तो ऐसा होता, जो माँगने नहीं, देने आता। सुकून का एक कतरा उनकी भी हथेली पर होता। अखबारों, बयानों और गॉसिप कॉलमों में राजनीति का जो चेहरा उकेरा जा रहा था, उसे देखकर वे मजे से मुस्कुराया करते हैं। लोग बाहर-बाहर गोते लगाकर निर्णय दे देते हैं कि राजनीतिज्ञ ऐश्वर्य भ्रष्टाचार और काले समुद्र के पैदाइशी तैराक होते हैं। किसने कोशिश की है कि इस नकली संसार के पीछे छिपी असली दुनिया की कशिश देख सकें।
कितनी ही बार उनका मन राजनीति से विरक्त भी हुआ। सारा छद्म एक झटके से तोड़कर दूर खड़े हो जाने की ललक ने कई दफा सिर उठाया, किंतु देश प्रदेश में फैले उनके असंख्य अनुयायियों ने ऐसा करने से सायास रोक दिया। वे कहने लगे, "हमारी राजनीति, हमारा भविष्य आप हैं। हम आपके नाम से जाने जाते हैं। आपने ही राजनीति छोड़ दी, तो हम किसके पीछे खड़े होंगे ? कौन हमें स्वीकारेगा ? हम चौपट हो जाएँगे। अनाथ हो जाएँगे। अकाल मृत्यु हो जाएगी हमारी।"
उन्हें दिखाई देता कि एक पूरी भीड़ आत्महत्या कर रही है और वे अपने ही फैसले को बेदर्दी से कुचल डालते।
विरक्ति ही नहीं, मोह भी तो उन्हें इसी राजनीति से है। जिस संसार के वे आदी हो गए हैं। उससे कट जाना तो उनके वश में नहीं है। वे शक्ति और वैभव, प्रशंसक और भक्तों के बिना एक छूँछी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते।
झिलमिलाती बारिश में गीली छिपकलियों सी लटों से, छतरी होने के बावजूद जल-बूँद टपकाती हुई, वह बड़ी-बड़ी आँखों वाली लड़की, अपना शरीर गीले वस्त्रों से चिपकाए हुए एकदम सामने न आ खड़ी होती तो अभी और न जाने कितनी देर तक वे वहीं खोये रहते। "गृहमंत्री महोदय को शेफाली नमस्कार करती है...."
नाटकीय लहजे और बेतकल्लुफ भाषा ने उन्हें चौंका दिया। उनकी अपार महिमा को लाँघकर, इस तरह पेश आने वाली यह बेहूदी लड़की, लड़की भी क्यों, तरुणाई को स्पर्श कर पीछे छोड़ने को तैयार-सी प्रौढ़ा भला कौन है ?
उनकी पलकें जल्दी-जल्दी उठीं-गिरीं। वह बोली, "पहचान न पाए होंगे हमें, महामहिम...!"
शंकित स्वरावलि ने कहा, "पहचान पा रहा हूँ, जरा ठहरो, आप...." भीगी पहाड़ियों के शिखरों-सी वह विमुग्धा खिलखिला पड़ी, "बस...बस...यह जो "आप आप" कहने लगे हैं न, हम समझ गए कि याद न आएगा आपको। हम हैं आपकी बाल-सखी, सहपाठिन और स्कूली ड्रामों की नायिका शेफाली...!"
अपनी छतरी बंद कर, लटों और साड़ी के छोर से पानी निचोड़कर वह करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई। चौकीदार तौलिया दे गया। शेफाली ने दाएँ हाथ में उसे अटका भर लिया।
वे बोले, "खूब बड़ी हो गई हो, देखता हूँ, तुम्हारी सदा बहने वाली नाक भी अब नहीं बहती...।" वे हँस दिए, "पर इस जंगल में कैसे आ पहुँची ?"
शेफाली ने अभिनयपूर्वक ही कहा, "सब आप ही की कृपा है महामान्य !"
"मेरी कृपा...मेरी कैसे...? मैं तो स्कूल के दिनों के बाद से तुम्हें अब देख रहा हूँ, मैंने क्या किया ?"
वह हँसी, "श्रीमान जी, न आप इस जंगल में स्कूल खुलने का आदेश कराते और न हम मास्टरनी बनकर यहाँ आते।"
"ओह..."
उन्होंने रहस्य की थाह पा ली, बोले, "पर हम तो कई बार यहाँ से निकले हैं। आ जातीं या चिट्ठी ही लिख देतीं, तो तबादला हो जाता।"
शैफाली के चेहरे से चंचलता गायब हो गई। एक चिंतनपूर्ण मुख वहाँ उपजा, "न, कभी नहीं। आज भी हम तबादला कराने नहीं आए। आपने अपने पिछले इलाके की तरक्की के लिए ही तो स्कूल खुलवाया है न। हमें सौभाग्य मिला है कि आपके उद्देश्यों को पूरा करने में एक अंश हमारा भी हो, तो उसे क्यों छोड़ दूँ ? पाँव सालों से हैं यहाँ पर, आपके सपने को पूरा करने में जुटी रहकर ही अपने को धन्य मान रही हूँ।"
वे अवाक् देखते रह गए, क्या कहते ? यह तो पहली बार घटा था कि कोई उनके सपनों से जुड़ने जंगल में जीवन जगाए बैठा था। पानीदार आँखें और तरल हो गईं।
वह बोली, "घर चलिएगा...! माँ ने कहा था, आएँ तो लेती आना। माँ की चाय...आ...आप कितनी तारीफ के साथ पिया करते थे, याद हैं न...?"
‘‘कहाँ है तुम्हारा घर ?’’
वह खिल गई, "वह पहाड़ी है न सामने, उसके पार, पर कार थोड़ेई जाएगी वहाँ।"
"चलो, जरूर चलेंगे। माँ के हाथों बनी तीखी-तुर्श चाय कब से नहीं पी।"
फिर उन्होंने पुलिस के अफसर से कुछ कहा। कलेक्टर को कुछ समझाया और काले अंघेरे में पैदल चल दिए।
पानी हलके-हलके गिर रहा था पगडंडी की गीली मिट्टी ने उनकी कोल्हापुरी चप्पलों और धोती के किनारों को रँग दिया। दोनों ओर की फूलदार झाड़ियों ने कपड़े गीले किए। शेफाली उनकी हालत देखकर खिलखिलाती रही और दौड़ती हुई आगे-आगे भागती रही। माँ ने बलाएँ लीं बैठने को मोढ़ा दिया। उन्हें भरोसा न था कि इत्ता बड़ा आदमी यों पैदल ही चला
आएगा। माँने बूढ़ें हाथों से वही, पुराने स्वाद वाली चाय पिलाई। वे तारीफों के गुलदस्ते देना नहीं भूले। बतियाते गए। पीते गए। पूछते रहे, "यहाँ अकेले डर तो नहीं लगता ? तबीयत घबरा तो नहीं जाती ? मन विचलित तो नहीं हो जाता कभी ?"
वे न जाने किससे पूछते रहे। शेफाली को लगा, वे कभी उससे और कभी खुद से ही सवाल करने लगते हैं।
शेफाली उन्हें पहुँचाने भी आई। जब पहाड़ी से वे गुजर रहे थे तो एक बड़ी चट्टान पर अकड़कर बैठते हुए शैफाली ने कहा, "आप इस तरह नाटकों के बादशाह बना करते थे।"
वे मुस्कुराए।
वह उठ खड़ी हुई, "अब आप सचमुच के बादशाह हैं, चक्रवर्ती, वे चुप-चुप चलते रहे। आगे-आगे शेफाली और पीछे-पीछे वे धोती कमर के पास अंगुलियों में फँसाए।
वह सीधे, कहीं दूर देखती हुई बोली, "अगली बार जब बादशाह आएँ, तो बेगम को भी जरूर-जरूर साथ लाएँ...।"
वह चलती रही, पर जवाब न आया, उसने रुककर देखा।
वे चलते-चलते करीब आए, "शेफाली, तुम्हारे बादशाह के पास आज तक कोई बेगम नहीं है...।"
वे आगे निकल गए।
वे पहाड़ी की ढलान उतरते जा रहे थे। उनका प्रोफाइल किसी यूनानी योद्धा की तरह दीख रहा था।
ठेठ देहाती इलाका है उनका निर्वाचन क्षेत्र। ग्रामीण मतदाता उनके राजसी वैभव को देखकर किलके पड़ रहे थे। अनगिनत सरकारी जीपें, समर्थकों की कारें, व्यापारियों-सेठों के वाहन, पार्टी कार्यकर्ताओं से लदी फदी जीपें....। कुल मिलाकर वाहनों का एक लंबा काफिला जिस गाँव की धूल धूसरित सड़क से गुजरता पाजामे, धोतियाँ, बंजियाँ, बीड़ियाँ और पगडंडियाँ उछाह से मुग्ध-मुग्ध हो जातीं। गाँवों के मुहानों के आम्र-पत्तों के द्वार, बंदनवार और रंगीन कागजी झंडियों, पार्टी-ध्वजों से स्वागत का आयोजन उन्हें भी भीतर तक आह्लादित किए जा रहा है। भीड़ की भीड़ आती। एक दूसरे पर गिरती पड़ती। रोली का तिलक दप-दप करते भाल पर लगता। फूलमालाओं में आदर भरी श्रद्धा भी पिरोई गई होती। भक्ति में डूबकर पाँव छूने की होड़ जारी है। सुदर्शन मुख की धवलता, रोली में रँगकर यों हो गई है जैसे दही में सेंदुर घुल रहा हो।
दिन-भर में ऐसी ही छोटी-बड़ी पचीस-तीस स्वागत-सभाएँ उन्होंने संबोधित की हैं। उन्होंने सधे और सहज लहजे में अपने दीर्घकालीन राजनीतिक जीवन का श्रेय मतदाताओं को दिया। मतदादा गद्गद हो उठे। उनकी आँखों में आँसू डबडबा आए। गले रुँध गए।
साँझ के करीब-करीब काफिला जंगल से घिरे डाकबँगले में आ टिका। बारिश हुई है। घनघोर। जंगली बरसात ने शाम को अपने गीलेपन में लपेट लिया है, दूर-दूर तक नीली धुआँती पहाड़ियों से घिरा सौ-पचास घरों वाला निरा देहात पानी में भीगकर, तालाब में डुबकी लगाकर निकला-निकला-सा लग रहा है। थकन की एक बारीक शिकन, अपूर्व दुस्साहस से उनके चेहरे पर चुपके से आकर लेट गई थी, गो कि वे उसे निंदियाने से लगातार टाले जा रहे हैं।
डाकबँगले के सामने वाले बरामदे में उन्होंने आरामकुर्सी डलवा ली थी। उसी पर बैठ झिम-झिम बरसते पानी में झिलमिलाती बजरी पर नजरें गड़ाए वे अतीत में उतरते जा रहे हैं।
सरकारी अफसर और दोयम दर्जे के नेतागण डाकबँगले के पिछवाड़े चाय-नाश्चे और आपसी स्वार्थचर्चा में लिप्त हो गए हैं। नीला अँधेरा क्रमशः गहरा हो रहा है, जबकि पेड़ों से टपकता हुआ पानी उसे घोल देने को कमर कसे हुए है।
किसानों का एक झुंड उनसे मिलने को आतुर हो रहा है, किंतु डाकबँगले के द्वार पर खड़ा पुलिस अफसर नहीं चाहता कि ‘साहब’ डिस्टर्ब हों। उनकी निगाहों ने बात पकड़ ली और किसानों को आने देने का संकेत किया।
वे सब ओला-पीड़ित थे। उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं। वे दुखी थे-बरसात और आँसुओं से भीगे हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। कलेक्टर से, जो पहले ही पीछे आकर खड़े हो गए थे, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही मदद के बारे में जाना और राहत राशि तुरंत देने की हिदायतें दीं। किसान लौट गए। वे फिर गीली शाम और भीगी पहाड़ी पीने लगे।
कौन जानता है कि आज के वैभव का किला, कल की तकलीफों और संघर्षों की बुनियाद पर खड़ा है। जितने कड़वे-मीठे दिनों से जूझकर वे यहाँ तक पहुँचे हैं, वे आज भी, अब भी अंदर कहीं जीवित हैं। चीटियों की लंबी कतार से असह्य वे दिन। भीड़ से घिरे वे मुस्कुराते रहते हैं, अंदर कोई अपना नहीं होता। लोगों की भीड़ आती है और अपनी तकलीफों के लंबे बयानों के एवज में उनसे राहत और सांत्वाना के ढेर ले जाती है।
आठ साल के इस अरसे ने और टीसें दी हैं-प्रांत में उनकी वट राजनीति के आश्रय में असंख्य अमरबेलें छितरा गई थीं, पर उनके मंत्रिपरिषद से हटते ही परजीवी अमरबेलों ने अपने ही मातृवृक्ष के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूँककर अपनी नपुसंकता के पोस्टर लगाए थे और सत्ता का छाता पाने चल दी थीं।
सूखे दिन उन पर तो कोई सूखी छाया न डाल सके, पर उन दिनों के मुट्ठी भर साथियों ने दसियों बार भाँति-भाँति से जताया था कि वे उनके बुरे दिनों के साथी हैं। इस तरह वे सब अपनी कीमत के प्रति खुद ही आश्वस्त हो लिया करते थे।
लंबी राजनीतिक जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आया, जो उनके भीतर के दर्द को सहला जाता। अकेलेपन को थपती दे जाता।
कोई तो ऐसा होता, जो माँगने नहीं, देने आता। सुकून का एक कतरा उनकी भी हथेली पर होता। अखबारों, बयानों और गॉसिप कॉलमों में राजनीति का जो चेहरा उकेरा जा रहा था, उसे देखकर वे मजे से मुस्कुराया करते हैं। लोग बाहर-बाहर गोते लगाकर निर्णय दे देते हैं कि राजनीतिज्ञ ऐश्वर्य भ्रष्टाचार और काले समुद्र के पैदाइशी तैराक होते हैं। किसने कोशिश की है कि इस नकली संसार के पीछे छिपी असली दुनिया की कशिश देख सकें।
कितनी ही बार उनका मन राजनीति से विरक्त भी हुआ। सारा छद्म एक झटके से तोड़कर दूर खड़े हो जाने की ललक ने कई दफा सिर उठाया, किंतु देश प्रदेश में फैले उनके असंख्य अनुयायियों ने ऐसा करने से सायास रोक दिया। वे कहने लगे, "हमारी राजनीति, हमारा भविष्य आप हैं। हम आपके नाम से जाने जाते हैं। आपने ही राजनीति छोड़ दी, तो हम किसके पीछे खड़े होंगे ? कौन हमें स्वीकारेगा ? हम चौपट हो जाएँगे। अनाथ हो जाएँगे। अकाल मृत्यु हो जाएगी हमारी।"
उन्हें दिखाई देता कि एक पूरी भीड़ आत्महत्या कर रही है और वे अपने ही फैसले को बेदर्दी से कुचल डालते।
विरक्ति ही नहीं, मोह भी तो उन्हें इसी राजनीति से है। जिस संसार के वे आदी हो गए हैं। उससे कट जाना तो उनके वश में नहीं है। वे शक्ति और वैभव, प्रशंसक और भक्तों के बिना एक छूँछी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते।
झिलमिलाती बारिश में गीली छिपकलियों सी लटों से, छतरी होने के बावजूद जल-बूँद टपकाती हुई, वह बड़ी-बड़ी आँखों वाली लड़की, अपना शरीर गीले वस्त्रों से चिपकाए हुए एकदम सामने न आ खड़ी होती तो अभी और न जाने कितनी देर तक वे वहीं खोये रहते। "गृहमंत्री महोदय को शेफाली नमस्कार करती है...."
नाटकीय लहजे और बेतकल्लुफ भाषा ने उन्हें चौंका दिया। उनकी अपार महिमा को लाँघकर, इस तरह पेश आने वाली यह बेहूदी लड़की, लड़की भी क्यों, तरुणाई को स्पर्श कर पीछे छोड़ने को तैयार-सी प्रौढ़ा भला कौन है ?
उनकी पलकें जल्दी-जल्दी उठीं-गिरीं। वह बोली, "पहचान न पाए होंगे हमें, महामहिम...!"
शंकित स्वरावलि ने कहा, "पहचान पा रहा हूँ, जरा ठहरो, आप...." भीगी पहाड़ियों के शिखरों-सी वह विमुग्धा खिलखिला पड़ी, "बस...बस...यह जो "आप आप" कहने लगे हैं न, हम समझ गए कि याद न आएगा आपको। हम हैं आपकी बाल-सखी, सहपाठिन और स्कूली ड्रामों की नायिका शेफाली...!"
अपनी छतरी बंद कर, लटों और साड़ी के छोर से पानी निचोड़कर वह करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई। चौकीदार तौलिया दे गया। शेफाली ने दाएँ हाथ में उसे अटका भर लिया।
वे बोले, "खूब बड़ी हो गई हो, देखता हूँ, तुम्हारी सदा बहने वाली नाक भी अब नहीं बहती...।" वे हँस दिए, "पर इस जंगल में कैसे आ पहुँची ?"
शेफाली ने अभिनयपूर्वक ही कहा, "सब आप ही की कृपा है महामान्य !"
"मेरी कृपा...मेरी कैसे...? मैं तो स्कूल के दिनों के बाद से तुम्हें अब देख रहा हूँ, मैंने क्या किया ?"
वह हँसी, "श्रीमान जी, न आप इस जंगल में स्कूल खुलने का आदेश कराते और न हम मास्टरनी बनकर यहाँ आते।"
"ओह..."
उन्होंने रहस्य की थाह पा ली, बोले, "पर हम तो कई बार यहाँ से निकले हैं। आ जातीं या चिट्ठी ही लिख देतीं, तो तबादला हो जाता।"
शैफाली के चेहरे से चंचलता गायब हो गई। एक चिंतनपूर्ण मुख वहाँ उपजा, "न, कभी नहीं। आज भी हम तबादला कराने नहीं आए। आपने अपने पिछले इलाके की तरक्की के लिए ही तो स्कूल खुलवाया है न। हमें सौभाग्य मिला है कि आपके उद्देश्यों को पूरा करने में एक अंश हमारा भी हो, तो उसे क्यों छोड़ दूँ ? पाँव सालों से हैं यहाँ पर, आपके सपने को पूरा करने में जुटी रहकर ही अपने को धन्य मान रही हूँ।"
वे अवाक् देखते रह गए, क्या कहते ? यह तो पहली बार घटा था कि कोई उनके सपनों से जुड़ने जंगल में जीवन जगाए बैठा था। पानीदार आँखें और तरल हो गईं।
वह बोली, "घर चलिएगा...! माँ ने कहा था, आएँ तो लेती आना। माँ की चाय...आ...आप कितनी तारीफ के साथ पिया करते थे, याद हैं न...?"
‘‘कहाँ है तुम्हारा घर ?’’
वह खिल गई, "वह पहाड़ी है न सामने, उसके पार, पर कार थोड़ेई जाएगी वहाँ।"
"चलो, जरूर चलेंगे। माँ के हाथों बनी तीखी-तुर्श चाय कब से नहीं पी।"
फिर उन्होंने पुलिस के अफसर से कुछ कहा। कलेक्टर को कुछ समझाया और काले अंघेरे में पैदल चल दिए।
पानी हलके-हलके गिर रहा था पगडंडी की गीली मिट्टी ने उनकी कोल्हापुरी चप्पलों और धोती के किनारों को रँग दिया। दोनों ओर की फूलदार झाड़ियों ने कपड़े गीले किए। शेफाली उनकी हालत देखकर खिलखिलाती रही और दौड़ती हुई आगे-आगे भागती रही। माँ ने बलाएँ लीं बैठने को मोढ़ा दिया। उन्हें भरोसा न था कि इत्ता बड़ा आदमी यों पैदल ही चला
आएगा। माँने बूढ़ें हाथों से वही, पुराने स्वाद वाली चाय पिलाई। वे तारीफों के गुलदस्ते देना नहीं भूले। बतियाते गए। पीते गए। पूछते रहे, "यहाँ अकेले डर तो नहीं लगता ? तबीयत घबरा तो नहीं जाती ? मन विचलित तो नहीं हो जाता कभी ?"
वे न जाने किससे पूछते रहे। शेफाली को लगा, वे कभी उससे और कभी खुद से ही सवाल करने लगते हैं।
शेफाली उन्हें पहुँचाने भी आई। जब पहाड़ी से वे गुजर रहे थे तो एक बड़ी चट्टान पर अकड़कर बैठते हुए शैफाली ने कहा, "आप इस तरह नाटकों के बादशाह बना करते थे।"
वे मुस्कुराए।
वह उठ खड़ी हुई, "अब आप सचमुच के बादशाह हैं, चक्रवर्ती, वे चुप-चुप चलते रहे। आगे-आगे शेफाली और पीछे-पीछे वे धोती कमर के पास अंगुलियों में फँसाए।
वह सीधे, कहीं दूर देखती हुई बोली, "अगली बार जब बादशाह आएँ, तो बेगम को भी जरूर-जरूर साथ लाएँ...।"
वह चलती रही, पर जवाब न आया, उसने रुककर देखा।
वे चलते-चलते करीब आए, "शेफाली, तुम्हारे बादशाह के पास आज तक कोई बेगम नहीं है...।"
वे आगे निकल गए।
वे पहाड़ी की ढलान उतरते जा रहे थे। उनका प्रोफाइल किसी यूनानी योद्धा की तरह दीख रहा था।
प्रतिनायक
रह-रहकर हो रहा था यह। पूरी झुग्गी थर्रा जाती और फिर देर तक यह थर्राहट
बनी रहती। ठहर-ठहरकर काली रात झिमझिमाने लगती। गुस्से की तरह एक तेज बौछार
आती और फूस के ऊपर रखे जर्जर कवेलुओं पर बजने लगी। बरसात उनकी दुश्मन थी।
अकसर वे सोचते कि क्या जरूरी था कि तीन-तीन मौसम हों। सिर्फ ठंड और गर्मी
भी तो हो सकते थे। गर्मियों के खिसकते हुए दिनों में वे बरसात की आहटें
सुनते और जानबूझकर उस तरफ से बेपरवाह होने या उसका खयाल न आने देने की
कोशिश करते। हमेशा की तरह कोशिशें फालतू चली जातीं।
मौसम का पहला पानी जिस दिन बरसता, उनके चेहरे जर्द हो जाते। पक्के मकानों और भरे पेटवाले जब फुहारों का आनंद लेते या मिट्टी की सौंधी महक नथुनों में भर रहे होते, तब वे बरसात को कोस रहे होते। पर शुरू-शुरू में पानी लगातार नहीं गिरता और काम मिलता रहता, इसलिए पानी में भीगने का मन टीकाराम का भी हो जाता। वह जानते-बूझते भीगता हुआ घर आता। पर दरवाजे के पहले ही संकोच उसे अपने पंजों में दबोच लेता। संकोच के नाखूनों से डर रिसने लगता और अपराध की तीखी गंध उसे झिंझोड़ने लगती।
गुजरे हुए हर पिछले साल की असफलता के बावजूद रमुलिया, अगले साल भर प्रयत्न करती रहती कि बरसात के दिनों के लिए अनाज जोड़-बचाकर रखा जाए। इसके लिए उसने टीकाराम से तीन-चार बड़े-बड़े मटके भी माँगवा लिए थे, पर उनमें से एक भी, कभी पूरा नहीं भरा। रोज बनाई जाने वाली रोटियों में से एक मुट्ठी आटा वह मटके में, बिला नागा डालती रहती और उसी हफ्ते ‘अटका’ पड़ जाने पर वह आटा एक ही दिन की रोटियों में उठ जाता।
टीकाराम की आदत पड़ गई थी कि वह रमुलिया को आटा बचाने की ताकीदें करता रहता। रमुलिया को इस आदत पर गुस्सा आता। पर वह दबाए रखती। ताकीदों और कोशिशों के बावजूद बचत संभव नहीं हो पाती और बरसात के शुरुआती दौर में ही काम के लाले पड़ जाते तो उनमें कहा-सुनी भी हो जाती। टीकाराम देहरी पर बैठा-बैठा बड़बड़ाता रहता कि वह साल भर चिल्लाता रहता है, पर रमुलिया ध्यान नहीं देती, इसी से मुसीबत आती है। उनमें दो एक दिन का अबोला भी रहता, फिर अप्रयास ही टूट जाता।
लगातार पानी गिरने का पाँचवाँ दिन था। पानी ने तार न तोड़ा था। झिमिर-झिमिर पानी उन्हें बहुत बेहूदा लग रहा था। बच्चे की नाक बह रही हो जैसे। दूर से आती ढोलक की थाप पर ‘आल्हा’ का राग उन्हें कोंच रहा था। खास तौर पर टीकाराम बुरी तरह बेचैन था। वह भीतर-भीतर कसमसा रहा था। उसका जी कर रहा था कि ढोलक में हँसिया घोंप दे और आल्हा की चिंदी-चिंदी करके चूल्हे में झोंके दे।
रमुलिया प्रायः खामोश रहने वाली औरत थी। वह चूल्हा जलाती और किफायत से रोटियाँ सेंकती। चूल्हे के गिर्द बैठे हुए वे एक ही टुकड़े को देर तक चबाते रहते। एक खेल की तरह ! टीकाराम निवाले को इस गाल से उस गाल की तरफ लुढ़का रहा था। एक अभ्यास हो गया उसे, बल्कि इसमें उसे मजा आने लगा था। खाने की बजाय खेल में उसकी रुचि बढ़ गई थी। उसने रमुलिया को भी इस खेल के प्रति उकसाया था पर वह चोंचलेबाजी में नहीं पड़ी।
रमलिया भी गुस्से में रहती। सीली लकड़ियों और मुन्ना पर उसे गुस्सा आता। वह झींकती, बर्राती किसी तरह पाँच-छह रोटियाँ सेंक लेती। दो-दो वे दोनों खाते और मुन्ना के लिए एक होती। एक रख दी जाती कि मुन्ना माँगता रहता है। टीकाराम रमलिया की तरफ से निराश होकर मुन्ना को खेल तकनीक समझाने लगा था। उसे बहुत उम्मीद थी कि मुन्ना खेल को जल्दी सीख लेगा। मुन्ना उसे प्रतिभावान लगता था।
बरसात रुकती नहीं, लकड़ियाँ जलती नहीं और मुन्ना दिन भर रोटियाँ माँगता रहता। रमुलिया रोटी के टुकड़े पकड़ाती रहती। रोटी खत्म हो जाती पर मुन्ना की भूख खत्म नहीं होती।
बरसात में बेलदारी का काम लगभग बंद हो जाता है। छपाई-पलस्तर का काम कहीं-कहीं होता भी है, तो मिस्त्री से जान-पहचान होने पर ही काम मिलता है। सफेद, प्लास्टिक की पारदर्शी बरसाती ओढ़कर टीकाराम रोज काम झूँढ़ने निकलता है, पर घंटे-दो घंटे में निराश होकर लौट आने के सिवा और कोई चारा नहीं होता।
रमुलिया ने उसे बता दिया था कि आज ‘कंसरा झाड़ के‘ रोटी ‘पई’ गई है। टीकाराम ने टनटनाते कनस्तर को देखा और खामोश रहा।
ऐसी ‘लगसर’ बारिश शहरों में कहाँ होती है, पर इस साल हो रही थी। बादल रह-रहकर गुस्सैल कुत्ते की तरह गुर्राते और छींटे पड़ने लगते। हवा के झोंके लहराते और फुहरियाँ डोलतीं। रोज वर्षा न थी, पर खुला भी न था। कमरा आधा गीला हो चुका था और शेष आधे में शीत फैल गई थी।
कोने में बैठा टीकाराम गिरते पानी को उजड़ी आँखों से देखता रहा। शनिवार था, इसलिए काम मिलने की कोई उम्मीद न थी। शनिवार लेबर पेमेंट का दिन होता है। उधार मिलने की आशा थी। शरबती लाल का काम इस हफ्ते लगा हुआ था। गाँव घर का है, बीसेक रुपया उधार दे सकता है। पर अभी पूरा दिन पड़ा था, रात आठ के पहले मिलने का सवाल ही न था।
मुन्ना नाक बहा रहा था।
खेल रहा था।
खेलने से जल्दी ही ऊब जाता तो रोटी माँगने लगता। नमक-पड़ी बिर्रा की रोटियाँ उसकी ब्रेड थीं। बिस्कुट थीं। खाना थीं। यहाँ तक कि वे मिठाई भी थीं। घर का जैसा वातावरण होता, वैसा रूप बदल लेती थीं वे।
दोपहर तक मुन्ने का नाश्ता, भोजन मिठाई बिस्कुट सब चला। फिर ठप्प। रमुलिया और टीकाराम ने आधी-आधी रोटी सुबह खाकर बे -दूध की गिलास भर चाय मुँह में उड़ेल ली थी और कोनों से फट गई चटाई पर पड़े थे।
मुन्ना ने कहा, "रोटी दे बाई !"
टीकाराम ने उसे किस्सा सुनाया, थोड़ी देर वह रमा रहा, फिर ऊब गया। उसने कहा, "रोटी देना..." टीकाराम ने रमुलिया को देखा। रमुलिया मुन्ना के साथ अटकन-चटकन-दही चटाकन खेलने लगी। वह फिर ऊब गया। उसने ऊपर को नाक सुड़की और रोटी की माँग जरा और जोर देकर की।
टीकाराम ने उसे गोद में उठा लिया, बोला-"लगता है, सोएगा...।" वह रीं-रीं करता रहा। आँखें झपझपाता रहा, फिर रोने लगा और बाप से शिकायत की-"बाई रोटी नईं देती...।"
मुन्ना गोद से फिसल गया और रमुलिया पर लद गया-"बाई रोटी दे...ए बाई...रोटी दे ना...., दे दे बाई...।" रमुलिया गुस्साकर झटके से पलटी। वह गिर पड़ा। रमुलिया ने उसे झिंझोड़ डाला-"ले मोंही खा लै कुलच्छी..." मुन्ना सहम गया। बुक्का फाड़े देखता रहा कि उससे क्या अपराध हुआ है ?
टीकाराम ने उसे उठा लिया। रमुलिया पर वह नाराज हुआ। कंधे पर चिपकाकर वही कोठरी में टहलता रहा। दो कदम इधर कोठरी, दो कदम उधर कोठरी। बजते फूस के संगीत रमुलिया के गुस्से और टीकाराम के प्रेम ने उसे सुला दिया।
नींद रोटी भूल गई।
टीकाराम ने उसे चटाई पर सुलाकर खुद से कहा, संझा के सरबती कुंधाई जइहों...।"
उत्तर कहीं से नहीं आया। रमुलिया की पीठ, कूल्हे और पैर की फटीस हुई एड़ियाँ खामोश रहीं।
पानी थमा नहीं था, पर धीमी फुहारें हवा के झोंकों के कारण दिख रही थीं। एक उदास और गझिन माहौल बाहर जमा हुआ। था। सूनेपन की चादर तनी हुई थी। चुप्पी में अपना अस्तित्व ढहता हुआ प्रतीत होता रहा टीकाराम को। उसे लगा, दुनिया भर के सारे बच्चे, भूख के बावजूद सहमकर सो गए हैं और सोए हुए बच्चों, गुमसुम पड़ी माँओं, बेचैन बापों से लोहा लेती बारिश धीरे-धीरे थक रही है। इस बीच टीकाराम ने अपनी किस्मत के बारे में सोचा। रोटी, मेहनत और बारिश के दरम्यान अकसर किस्मत आती रही है। वह किस्मत पर सोचना नहीं चाहता था, पर वह जोर जबरदस्ती से सिर पर सवार होती रही है।
मुन्ना पलटा।
टीकाराम का ध्यान उधर गया। उसने झक्क से आँखें खोल दीं।
टीकाराम जल्दी से बोला, "निन्नी हो गई मुन्ना का...?" वह फिर रोटी न माँग बैठे इसलिए अतिरिक्त लाड़ से उसने कहा, "आज तो सनीचर है...मुन्ना फिलम देखेगा...बढ़ियाँ...बढ़ियाँ...ढिसुंम...ढिसुंम है ना...।"
मौसम का पहला पानी जिस दिन बरसता, उनके चेहरे जर्द हो जाते। पक्के मकानों और भरे पेटवाले जब फुहारों का आनंद लेते या मिट्टी की सौंधी महक नथुनों में भर रहे होते, तब वे बरसात को कोस रहे होते। पर शुरू-शुरू में पानी लगातार नहीं गिरता और काम मिलता रहता, इसलिए पानी में भीगने का मन टीकाराम का भी हो जाता। वह जानते-बूझते भीगता हुआ घर आता। पर दरवाजे के पहले ही संकोच उसे अपने पंजों में दबोच लेता। संकोच के नाखूनों से डर रिसने लगता और अपराध की तीखी गंध उसे झिंझोड़ने लगती।
गुजरे हुए हर पिछले साल की असफलता के बावजूद रमुलिया, अगले साल भर प्रयत्न करती रहती कि बरसात के दिनों के लिए अनाज जोड़-बचाकर रखा जाए। इसके लिए उसने टीकाराम से तीन-चार बड़े-बड़े मटके भी माँगवा लिए थे, पर उनमें से एक भी, कभी पूरा नहीं भरा। रोज बनाई जाने वाली रोटियों में से एक मुट्ठी आटा वह मटके में, बिला नागा डालती रहती और उसी हफ्ते ‘अटका’ पड़ जाने पर वह आटा एक ही दिन की रोटियों में उठ जाता।
टीकाराम की आदत पड़ गई थी कि वह रमुलिया को आटा बचाने की ताकीदें करता रहता। रमुलिया को इस आदत पर गुस्सा आता। पर वह दबाए रखती। ताकीदों और कोशिशों के बावजूद बचत संभव नहीं हो पाती और बरसात के शुरुआती दौर में ही काम के लाले पड़ जाते तो उनमें कहा-सुनी भी हो जाती। टीकाराम देहरी पर बैठा-बैठा बड़बड़ाता रहता कि वह साल भर चिल्लाता रहता है, पर रमुलिया ध्यान नहीं देती, इसी से मुसीबत आती है। उनमें दो एक दिन का अबोला भी रहता, फिर अप्रयास ही टूट जाता।
लगातार पानी गिरने का पाँचवाँ दिन था। पानी ने तार न तोड़ा था। झिमिर-झिमिर पानी उन्हें बहुत बेहूदा लग रहा था। बच्चे की नाक बह रही हो जैसे। दूर से आती ढोलक की थाप पर ‘आल्हा’ का राग उन्हें कोंच रहा था। खास तौर पर टीकाराम बुरी तरह बेचैन था। वह भीतर-भीतर कसमसा रहा था। उसका जी कर रहा था कि ढोलक में हँसिया घोंप दे और आल्हा की चिंदी-चिंदी करके चूल्हे में झोंके दे।
रमुलिया प्रायः खामोश रहने वाली औरत थी। वह चूल्हा जलाती और किफायत से रोटियाँ सेंकती। चूल्हे के गिर्द बैठे हुए वे एक ही टुकड़े को देर तक चबाते रहते। एक खेल की तरह ! टीकाराम निवाले को इस गाल से उस गाल की तरफ लुढ़का रहा था। एक अभ्यास हो गया उसे, बल्कि इसमें उसे मजा आने लगा था। खाने की बजाय खेल में उसकी रुचि बढ़ गई थी। उसने रमुलिया को भी इस खेल के प्रति उकसाया था पर वह चोंचलेबाजी में नहीं पड़ी।
रमलिया भी गुस्से में रहती। सीली लकड़ियों और मुन्ना पर उसे गुस्सा आता। वह झींकती, बर्राती किसी तरह पाँच-छह रोटियाँ सेंक लेती। दो-दो वे दोनों खाते और मुन्ना के लिए एक होती। एक रख दी जाती कि मुन्ना माँगता रहता है। टीकाराम रमलिया की तरफ से निराश होकर मुन्ना को खेल तकनीक समझाने लगा था। उसे बहुत उम्मीद थी कि मुन्ना खेल को जल्दी सीख लेगा। मुन्ना उसे प्रतिभावान लगता था।
बरसात रुकती नहीं, लकड़ियाँ जलती नहीं और मुन्ना दिन भर रोटियाँ माँगता रहता। रमुलिया रोटी के टुकड़े पकड़ाती रहती। रोटी खत्म हो जाती पर मुन्ना की भूख खत्म नहीं होती।
बरसात में बेलदारी का काम लगभग बंद हो जाता है। छपाई-पलस्तर का काम कहीं-कहीं होता भी है, तो मिस्त्री से जान-पहचान होने पर ही काम मिलता है। सफेद, प्लास्टिक की पारदर्शी बरसाती ओढ़कर टीकाराम रोज काम झूँढ़ने निकलता है, पर घंटे-दो घंटे में निराश होकर लौट आने के सिवा और कोई चारा नहीं होता।
रमुलिया ने उसे बता दिया था कि आज ‘कंसरा झाड़ के‘ रोटी ‘पई’ गई है। टीकाराम ने टनटनाते कनस्तर को देखा और खामोश रहा।
ऐसी ‘लगसर’ बारिश शहरों में कहाँ होती है, पर इस साल हो रही थी। बादल रह-रहकर गुस्सैल कुत्ते की तरह गुर्राते और छींटे पड़ने लगते। हवा के झोंके लहराते और फुहरियाँ डोलतीं। रोज वर्षा न थी, पर खुला भी न था। कमरा आधा गीला हो चुका था और शेष आधे में शीत फैल गई थी।
कोने में बैठा टीकाराम गिरते पानी को उजड़ी आँखों से देखता रहा। शनिवार था, इसलिए काम मिलने की कोई उम्मीद न थी। शनिवार लेबर पेमेंट का दिन होता है। उधार मिलने की आशा थी। शरबती लाल का काम इस हफ्ते लगा हुआ था। गाँव घर का है, बीसेक रुपया उधार दे सकता है। पर अभी पूरा दिन पड़ा था, रात आठ के पहले मिलने का सवाल ही न था।
मुन्ना नाक बहा रहा था।
खेल रहा था।
खेलने से जल्दी ही ऊब जाता तो रोटी माँगने लगता। नमक-पड़ी बिर्रा की रोटियाँ उसकी ब्रेड थीं। बिस्कुट थीं। खाना थीं। यहाँ तक कि वे मिठाई भी थीं। घर का जैसा वातावरण होता, वैसा रूप बदल लेती थीं वे।
दोपहर तक मुन्ने का नाश्ता, भोजन मिठाई बिस्कुट सब चला। फिर ठप्प। रमुलिया और टीकाराम ने आधी-आधी रोटी सुबह खाकर बे -दूध की गिलास भर चाय मुँह में उड़ेल ली थी और कोनों से फट गई चटाई पर पड़े थे।
मुन्ना ने कहा, "रोटी दे बाई !"
टीकाराम ने उसे किस्सा सुनाया, थोड़ी देर वह रमा रहा, फिर ऊब गया। उसने कहा, "रोटी देना..." टीकाराम ने रमुलिया को देखा। रमुलिया मुन्ना के साथ अटकन-चटकन-दही चटाकन खेलने लगी। वह फिर ऊब गया। उसने ऊपर को नाक सुड़की और रोटी की माँग जरा और जोर देकर की।
टीकाराम ने उसे गोद में उठा लिया, बोला-"लगता है, सोएगा...।" वह रीं-रीं करता रहा। आँखें झपझपाता रहा, फिर रोने लगा और बाप से शिकायत की-"बाई रोटी नईं देती...।"
मुन्ना गोद से फिसल गया और रमुलिया पर लद गया-"बाई रोटी दे...ए बाई...रोटी दे ना...., दे दे बाई...।" रमुलिया गुस्साकर झटके से पलटी। वह गिर पड़ा। रमुलिया ने उसे झिंझोड़ डाला-"ले मोंही खा लै कुलच्छी..." मुन्ना सहम गया। बुक्का फाड़े देखता रहा कि उससे क्या अपराध हुआ है ?
टीकाराम ने उसे उठा लिया। रमुलिया पर वह नाराज हुआ। कंधे पर चिपकाकर वही कोठरी में टहलता रहा। दो कदम इधर कोठरी, दो कदम उधर कोठरी। बजते फूस के संगीत रमुलिया के गुस्से और टीकाराम के प्रेम ने उसे सुला दिया।
नींद रोटी भूल गई।
टीकाराम ने उसे चटाई पर सुलाकर खुद से कहा, संझा के सरबती कुंधाई जइहों...।"
उत्तर कहीं से नहीं आया। रमुलिया की पीठ, कूल्हे और पैर की फटीस हुई एड़ियाँ खामोश रहीं।
पानी थमा नहीं था, पर धीमी फुहारें हवा के झोंकों के कारण दिख रही थीं। एक उदास और गझिन माहौल बाहर जमा हुआ। था। सूनेपन की चादर तनी हुई थी। चुप्पी में अपना अस्तित्व ढहता हुआ प्रतीत होता रहा टीकाराम को। उसे लगा, दुनिया भर के सारे बच्चे, भूख के बावजूद सहमकर सो गए हैं और सोए हुए बच्चों, गुमसुम पड़ी माँओं, बेचैन बापों से लोहा लेती बारिश धीरे-धीरे थक रही है। इस बीच टीकाराम ने अपनी किस्मत के बारे में सोचा। रोटी, मेहनत और बारिश के दरम्यान अकसर किस्मत आती रही है। वह किस्मत पर सोचना नहीं चाहता था, पर वह जोर जबरदस्ती से सिर पर सवार होती रही है।
मुन्ना पलटा।
टीकाराम का ध्यान उधर गया। उसने झक्क से आँखें खोल दीं।
टीकाराम जल्दी से बोला, "निन्नी हो गई मुन्ना का...?" वह फिर रोटी न माँग बैठे इसलिए अतिरिक्त लाड़ से उसने कहा, "आज तो सनीचर है...मुन्ना फिलम देखेगा...बढ़ियाँ...बढ़ियाँ...ढिसुंम...ढिसुंम है ना...।"
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book