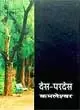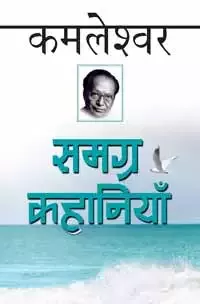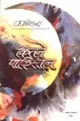|
कहानी संग्रह >> स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानियाँ स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानियाँकमलेश्वर
|
398 पाठक हैं |
||||||
आजादी के बाद के समाज की संपूर्ण छवि
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
स्वाधीनता के पश्चात लिखी गई हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियों का संचयन है। ये
कहानियाँ स्वातंत्र्योत्तर काल की हिन्दी कहानी के विभिन्न रचनात्मक
पक्षों और बदलावों की साक्षी रही हैं, और अपने दौर में सर्वाधिक चर्चित
रही हैं और सराही गईं। यहाँ हिन्दी के मानसिक उद्वेलन, चिंताओं, सरोकारों
के साथ-साथ हिन्दी कहानी के स्वातंत्र्योत्तर विकास क्रम भी दिखते हैं। यह
संकलन आजादी के बाद के समाज की संपूर्ण छवि प्रस्तुत करता है। इन कहानियों
में अपने समय की दारुण परिस्थितियों से सख्ती के साथ निपटने की रचनात्मक
तैयार दिखती है।
गत दो-तीन दशकों में भारत में जिस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक स्खलन और परिवर्तन दिखायी दिये हैं, तथा नई विश्व-व्यवस्था की परिकल्पना और साम्प्रदायिक उभारों ने हमारी जीवन शैली को जिस तरह हिलाया है, उनके ताजा और मौलिक अनुभव इन कहानियों में व्यक्त हुए हैं। दलित चेतना और स्त्री चेतना से भी बीते दिनों हिन्दी कहानी समृद्ध हुई है। यह संकलन उस प्रसंग में भी अपना बयान प्रस्तुत करता है। हिन्दी कहानी की विशाल दुनिया को एक संकलन में समेटना असंभव है। पर इतना तय है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी कहानी के जितने रंग मुखर हुए, उसकी झाँकी यहाँ अवश्य है।
गत दो-तीन दशकों में भारत में जिस प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक स्खलन और परिवर्तन दिखायी दिये हैं, तथा नई विश्व-व्यवस्था की परिकल्पना और साम्प्रदायिक उभारों ने हमारी जीवन शैली को जिस तरह हिलाया है, उनके ताजा और मौलिक अनुभव इन कहानियों में व्यक्त हुए हैं। दलित चेतना और स्त्री चेतना से भी बीते दिनों हिन्दी कहानी समृद्ध हुई है। यह संकलन उस प्रसंग में भी अपना बयान प्रस्तुत करता है। हिन्दी कहानी की विशाल दुनिया को एक संकलन में समेटना असंभव है। पर इतना तय है कि स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी कहानी के जितने रंग मुखर हुए, उसकी झाँकी यहाँ अवश्य है।
संपादकीय वक्तव्य
हिन्दी कहानी रचनात्मक विप्लव की कहानी भी है
कहा जाना चाहिए चाहिए कि कहानी की जरूरत उसी समय सिद्ध हो गई थी जब हिन्दी
के आचार्यगण खड़ी बोली को साहित्य की मुख भाषा के रूप में विकसित स्थापित
करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ की कड़ी में हिन्दी भाषा के उन्नयन और
गद्य-विधाओं के सूत्रपात ने जिस भाषाई जनतांत्रिक का निर्वाह करते हुए
साहित्य रचना की नींव रखी, उसका ध्वन्यार्थ आज की रचनाओं में भी अनुगूंजित
है। उत्तर भारतेन्दु युग जिस रचनात्मकता के संक्रमण का दौर था, उसमें भले
ही किसी एक कालजयी रचना का जन्म न हो सका, किन्तु रचना का उन्मेष हो चुका
था। देवकीनंदन खत्री और गोपालराम गहमरी इत्यादि ने तिलिस्मी ताने-बाने का
गल्प तैयार कर कथा-सृजन की अच्छी वृत्तांतमूलक जमीन तैयार कर दी थी। साथ
ही इनकी रचनाओं ने हिन्दी का एक बहुत बड़ा पाठकवर्ग भी तैयार कर दिया था।
उस समय तक उत्तर भारत में सरकारी स्तर पर फारसी भाषा नहीं थी। तत्कालीन
कथा-लेखन की जुबान खत्री-गहमरी के भाषाई तिलिस्म के इर्द-गिर्द बनती दिखाई
देने लगी थी। परन्तु बीसवीं सदी का हिन्दी कहानी का कथ्य दूसरे ही आस्वाद
पर विकसित हुआ। कहानी में जमीन और समय के यथार्थ से जुड़ने की
कोशिश
आरंभ से ही दिखाई देने लगी। हालांकि भारतेन्दु युग की कविताओं, नाटकों,
निबंधों ने साहित्य को तिलिस्मी वायवीयता और अतिरसिकप्रियता से मुक्ति
पहले ही दिला दी थी। उसका परिवर्द्धित विस्फोट द्विवेदी युग के साहित्य
में दिखाई देता है।
इसी तरह हिन्दी भाषा के तीन प्रमुख उन्नायकों- माधवराव सप्रे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जब इसी दौर में हिन्दी की आरंभिक कहानियां लिखीं तो उन्होंने भी जैसे वायवीय रसिकता के प्रतिमानों के परित्याग पर अपनी-अपनी मुहरें लगा दीं। हिन्दी साहित्य और विशेषत: कथा साहित्य के इतिहास में वह एक क्रांतिकारी शुरूआत थी। साहित्य के काल्पनिक, पौराणिक और रोमांटिक कथानकों को खारिज कर देशज भूमि पर स्थापित करने वाली यथार्थ-विवरण की यह युगांतकारी घोषणा थी।
दरअसल हिन्दी की प्रथम कहानी की जब भी चर्चा की जाती है तो उपर्युक्त तीनों आचार्यों की लिखी कहानियों का नाम जरूर लिया जाता है। माधवराव सप्रे की कहानी ‘टोकरी भर मिट्टी’ हिन्दी की प्रथम कहानी मान ली गई है। इसी कालवधि में रामचन्द्र शुक्ल की कहानी ‘ग्यारह वर्ष का समय’ प्रकाश में आई। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी केवल महावीर प्रसाद नाम से ‘स्वर्ग की झलक’ शीर्षक कहानी लिखी। हालांकि इस कहानी के संबंध में थोड़ा संदेह शेष रह जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी पर अपना पूरा नाम क्यों नहीं दिया ? और फिर यह तथ्य भी सामने है कि यह ‘महावीर प्रसाद’ के नाम पर छपी इकलौती कहानी है। परन्तु शोध के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि कि उस काल में महावीर प्रसाद नाम का कोई अन्य साहित्यकार उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह मान लेना मुनासिब होगा कि यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखी होगी। तत्पश्चात कहानीकारों में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने ‘उसने कहा था’ जैसी कालजयी कहानी सन् 1915 में लिखकर भाषाई आंचलिकता, समय, यथार्थ और संवेगों की रचना का महाद्वार खोल दिया। खुदज इसका शीर्षक ही भाषा की आम-फहम होती प्रकृति का द्योतक है। गुलेरी जी के साथ ही प्रेमचन्द ने ग्रामीण यथार्थ की सबसे महत्वपूर्ण दिशा का रचनात्मक अन्वेषण किया, जिसने कालिदास और गुरुदेव टैगोर के बाद पहली बार भारतीय अनुभव को विश्व-मानस के अनुभव का जरूरी अंश बना दिया। भारत की आध्यात्मिक धरोहर और मुक्ति कामना को संप्रेषित करने वाले योगिराज अरविंग घोष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजनीतिक मुक्ति के साहित्यिक प्रणेता सुब्रह्मण्यम भारती और महात्मा गाँधी जैसे संघर्षशील सिद्धांतकारी मौजूद थे, पर ‘भारतीय सामाजिक यथार्थ’ के, एक मात्र प्रस्तुतकर्ता प्रेमचन्द ही थे।
और यह लगभग विरोधाभासी आश्चर्य है कि इसी दौर में कविता की मुख्यधारा पौराणिक आख्यानवाद और रूमानी छायावाद के छंद विधान में आबद्ध थी, परन्तु कहानी ने वृत्तांत का काल्पनिक छंद विधान त्याग कर ठोस सामाजिक यथार्थ को आत्मसात् कर लिया था। कहानी किस्सागोई से निकलकर, मनोरंजन और रसिकता से मुक्त होकर कथन के लिए सीमांतों तक पहुंची थी और मानवीय अनुभव की समांतर दुनिया का निर्माण कर रही थी। हिन्दी कहानी के इस दौर में प्रेमचन्द्र के अतिरिक्त शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, सुदर्शन, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा जैसे कथा शिल्पी शामिल थे। सन् 1916 में प्रेमचन्द ने अपनी प्रख्यात कहानी ‘पंच परमेश्वर’ लिखकर हिन्दी कहानी का मिजाज और वैचारिक आधारभूमि ही बदल दी थी।
इसी दौर के साथ और कुछ बाद में आती हैं वृंदावन लाल वर्मा, पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, रांगेय राघव, इलाचन्द्र जोशी, भगवती चरण वर्मा आदि की कहानियां। भले ही इस दौर के सभी कथाकारों ने अलग-अलग भावभूमि की कहानियाँ लिखी हों, किन्तु इनका विस्तृत कोलाज मुकम्मिल तौर पर यथार्थवाद और मानवतावादी है। इस दौर तक आते-आते हिन्दी कहानी का अनुभव फलक बहुत विस्तृत हो गया है। सामाजिक विद्रूपता से लेकर मनोजगत की संघटनाओं और ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों तक पर इस दौर में बेमिसाल कहानियां लिखी गईं।
आजादी मिलने के बाद हिन्दी की कथा रचना ने दूसरी महत्वपूर्ण करवट ली या कि उसे लेनी पड़ी। क्योंकि आजादी से पहले जिस समाज की परिकल्पना की गई थी वैसे समाज के निर्माण में संदेह दिखने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध, विभाजन की त्रासदी, और समानता के सपनों के बिखरते परिदृश्य ने देश की जनता का मोहभंग कर दिया था। फलस्वरूप कहानीकार की नई पीढ़ी ने अपनी-अपनी संवेदनाओं की नई जमीनें तलाशीं। अपने-अपने भाषाई और सामाजिक यथार्थ के अनुरूप नए रचना बोध की खोज की। एकाध कहानियां तो सभी पत्रिकाओं में छपती थीं परन्तु कथा-रचना के इस नए बोध का समवेत सर्जनात्मक विस्फोट कहानी विधा को समर्पित ‘कहानी’ नामक पत्रिका में हुआ, जिसके यशस्वी संपादक प्रेमचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय थे। इसकी पहचान अमरकान्त की डिप्टी कलक्टरी, मार्कण्डेय की ‘हंसा जाई अकेला’ कमलेश्वर की ‘राजा निरंबसिया’, राजेन्द्र यादव की ‘जहां लक्ष्मी कैद है’, शेखर जोशी की ‘कोसी का घटवार’, भीष्म साहनी की ‘चीफ की दावत’, उषा प्रियंवदा की ‘वापसी’, मोहन राकेश की ‘मलबे का मालिक’, निर्मल वर्मा की ‘परिंदे’ रांगेय राघव की ‘गदल’ कृष्णा सोबती की ‘बादलों के घेरे’ विष्णु प्रभाकर की ‘धरती अब भी घूम रही है’ आदि में मौजूद है। विभाजन की त्रासदी और तीखे मोहभंग के यथार्थ ने इस दौर में बहुआयामी अभिव्यक्ति पाई।
पांचवे दशक के आते-आते इस प्रवृत्ति ने हिन्दी कहानी में ‘अनुभव की प्रमाणिकता’ ने सहज और स्वाभाविक विस्तार पा लिया। बाद में इस अनुभव और रचना विस्तार को ‘नई कहानी’ का नाम दिया गया। जो कि एक आदोलन बना और जिसने हिन्दी कहानी के सरोकारों को, और स्वरूप को बदल कर उसके विकास क्रम का सार्थक रचना-मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि सन् उन्नीस सौ पचास के आस-पास से ही कहानियों के कथ्य और ट्रीटमेंट की शैली में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। किन्तु इसका नामकरण सन् उन्नीस सौ पचपन में हो सका। इसकी नव्यता को पहचानकर इसे ‘नई कहानी’ की संज्ञा से अभिहित करने का काम प्रगतिशील धारा के कवि दुष्यंत कुमार ने ‘कल्पना’ पत्रिका के जनवरी 1955 के अंक में किया। कहानी के नए सरोकारों और प्रयोगधर्मिता को लेकर डॉ. धर्मवीर भारती ने ‘धर्मयुग’ में कहानी के बदले हुए स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहानीकारों-मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव का त्रिकोण स्थापित कर दिया। इसे कथालोचना में कुछ विचलन भी पैदा हुआ परन्तु सन् 1954 के ‘कहानी विशेषांक’ ने नई कहानी की वैचारिक भूमि पहले ही स्थापित कर दी थी। अमरकांत की कहानी ‘डिप्टी कलक्टरी’ और कमलेश्वर की कहानी ‘राजा निरबंसिया’ लिखी जा चुकी थीं। इसी क्रम में मोहन राकेश का कहानी संग्रह ‘नए बादल’ सन् 1956 में आया। इसी दौर में निर्मल वर्मा की कहानी ‘परिंदे’ और भुवनेश्वर की कहानी ‘भेडिये’ और उषा प्रियंवदा की कहानी ‘वापसी’ पर चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं। इन्हीं कहानियों को नई कहानी की प्रारंभिक कहानियों में गिना जाता है। इनके अलावा ‘कहानी’ और ‘नई कहानियां’ पत्रिकाओं ने इस आंदोलन की अधिकारिक रूप से घोषित पत्रिका थी।
दरअसल नए कहानीकारों ने यह महसूस किया कि वैचारिक स्तर पर यह मूल्यों के विघटन का दौर है। इस दौर में संदेह, अविश्वास, मोगभंग, भय और आशंका के व्यापार ने आदर्शवाद की सुखद कल्पनाओं को हाशिये पर डाल दिया था। इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, व्यक्तिवाद, साहित्यवाद, क्षणवाद, यथास्थितिवाद और इतिहासहीनता या फ्रॉयडवाद को नाकाफी समझ जाने लगा। और संबंधों के नए समीकरणों के बीच व्यवस्था के अंतर्विरोधी को सामने लाया गया। नई कहानी ने संयुक्त परिवार के ह्नास, नौकरी पेशा व शहरीकृत महत्वाकांक्षी नए मध्यवर्ग का उदय, शहरीकरण और पूंजी के बढ़ते वर्चस्व और बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमता को खास तौर से रेखांकित किया। शहरीकरण और पारिवारिक विघटन के कथ्य भी सामने आए। नए कहानीकारों के तर्क के मुताबिक आजादी के बाद जिस प्रकार शहरी मध्यवर्ग की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई, उसी प्रकार उसकी समस्याओं का घनत्व भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। इन स्थितियों के प्रमाणिक स्वर उस दौर की कहानियों में मौजूद हैं। इस बीच आंचलिक कहानियों ने भाषाई देशजता और ग्रामीण यथार्थ की नई जमीन तोड़ी। मार्कण्डेय, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, विद्यासागर नौटियाल, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, विजयदान देखा आदि की कहानियों में आंचलिक यथार्थ का सघन, विद्रूपमय, और करुणापूरित संसार सामने आया। ऐसा नहीं कि इसमें उल्लास नहीं था, पर उल्लास के साथ-साथ ग्राम समाज की पीड़ा, परिवर्तनहीनता और बिडंबनाएं भी बड़ी शिद्दत से सामने आईं।
आंचलिकता के बाद के दौर की कहानियों का भी यह प्रिय विषय बना रहा। आज भी आंचलिक कहानियों काल यह कथा संसार नई प्रतीतियों, अपने दलित और दमित वर्गों के संत्रास और बदले हुए, अपराधग्रस्त समय का अन्वेषण कर रही हैं।
नई कहानी का कथ्य-विस्तार सचमुच चमत्कृत करता है। यह निश्चय ही उस कसौटी की देन थी जो स्वयं कथाकारों ने तैयार की थी और जिसे समीक्षा की शब्दावली में ‘अनुभव की प्रामाणिकता’ कहा गया। बाद में उसका विकृत रूप ‘भोगा हुआ यथार्थ’ भी प्रचलित हुआ।
और यह आकस्मिक नहीं था कि हिन्दी कहानी की परिधि में वह सब कुछ साकार हुआ जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज और देशकाल उस संक्रांति काल में आक्रांत और आहत था। यह एक महाजाति के दैहिक, भौतिक, पराभूत परलौकिक, वैचारिक संवेदना के बदलते प्रतिमानों, संबंधों के विघटन, नए संबंधों के निर्धारण, मूल्यों के विचलन और न्याय-अन्याय के प्रश्नों से जूझता हुआ संक्रमण काल था, जिसे नई कहानी ने समकालीन मनुष्य के संदर्भ में रचनात्मक दक्षता और गहरे मानवीय सरोकारों के साथ प्रस्तुत किया था। जन-मानस की सोच और सौंदर्य को बदला था। इसने साहित्य की परिपाटीबद्ध यथास्थिति को खारिज किया था। विधागत और परिभाषागत नए पैमानों और प्रतिमानों का संधान किया था। शास्त्रसम्मत कहानी के ढांचे को तोड़कर उसे समकालीन समय के लिए संभव और विशाल पाठक वर्ग के लिए मित्रवत दस्तावेजों के रूप में अनिवार्य बनाया था। गंभीर साहित्य के लेखक और जागरूक पाठकवर्ग के वैचारिक संबंधों की परस्परिकता का यह स्वर्णकाल था। भाषाई स्तर पर नई कहानी ने जातीय, जनजातीय, देशज और आंचलिक इलाकों की अस्मिता और उपस्थिति को पहचाना और आत्मसात किया था। इंद्रधनुषी-विप्लव कभी उपस्थित नहीं हुआ था।
इसी तरह हिन्दी भाषा के तीन प्रमुख उन्नायकों- माधवराव सप्रे, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जब इसी दौर में हिन्दी की आरंभिक कहानियां लिखीं तो उन्होंने भी जैसे वायवीय रसिकता के प्रतिमानों के परित्याग पर अपनी-अपनी मुहरें लगा दीं। हिन्दी साहित्य और विशेषत: कथा साहित्य के इतिहास में वह एक क्रांतिकारी शुरूआत थी। साहित्य के काल्पनिक, पौराणिक और रोमांटिक कथानकों को खारिज कर देशज भूमि पर स्थापित करने वाली यथार्थ-विवरण की यह युगांतकारी घोषणा थी।
दरअसल हिन्दी की प्रथम कहानी की जब भी चर्चा की जाती है तो उपर्युक्त तीनों आचार्यों की लिखी कहानियों का नाम जरूर लिया जाता है। माधवराव सप्रे की कहानी ‘टोकरी भर मिट्टी’ हिन्दी की प्रथम कहानी मान ली गई है। इसी कालवधि में रामचन्द्र शुक्ल की कहानी ‘ग्यारह वर्ष का समय’ प्रकाश में आई। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी केवल महावीर प्रसाद नाम से ‘स्वर्ग की झलक’ शीर्षक कहानी लिखी। हालांकि इस कहानी के संबंध में थोड़ा संदेह शेष रह जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी पर अपना पूरा नाम क्यों नहीं दिया ? और फिर यह तथ्य भी सामने है कि यह ‘महावीर प्रसाद’ के नाम पर छपी इकलौती कहानी है। परन्तु शोध के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि कि उस काल में महावीर प्रसाद नाम का कोई अन्य साहित्यकार उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह मान लेना मुनासिब होगा कि यह कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखी होगी। तत्पश्चात कहानीकारों में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने ‘उसने कहा था’ जैसी कालजयी कहानी सन् 1915 में लिखकर भाषाई आंचलिकता, समय, यथार्थ और संवेगों की रचना का महाद्वार खोल दिया। खुदज इसका शीर्षक ही भाषा की आम-फहम होती प्रकृति का द्योतक है। गुलेरी जी के साथ ही प्रेमचन्द ने ग्रामीण यथार्थ की सबसे महत्वपूर्ण दिशा का रचनात्मक अन्वेषण किया, जिसने कालिदास और गुरुदेव टैगोर के बाद पहली बार भारतीय अनुभव को विश्व-मानस के अनुभव का जरूरी अंश बना दिया। भारत की आध्यात्मिक धरोहर और मुक्ति कामना को संप्रेषित करने वाले योगिराज अरविंग घोष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजनीतिक मुक्ति के साहित्यिक प्रणेता सुब्रह्मण्यम भारती और महात्मा गाँधी जैसे संघर्षशील सिद्धांतकारी मौजूद थे, पर ‘भारतीय सामाजिक यथार्थ’ के, एक मात्र प्रस्तुतकर्ता प्रेमचन्द ही थे।
और यह लगभग विरोधाभासी आश्चर्य है कि इसी दौर में कविता की मुख्यधारा पौराणिक आख्यानवाद और रूमानी छायावाद के छंद विधान में आबद्ध थी, परन्तु कहानी ने वृत्तांत का काल्पनिक छंद विधान त्याग कर ठोस सामाजिक यथार्थ को आत्मसात् कर लिया था। कहानी किस्सागोई से निकलकर, मनोरंजन और रसिकता से मुक्त होकर कथन के लिए सीमांतों तक पहुंची थी और मानवीय अनुभव की समांतर दुनिया का निर्माण कर रही थी। हिन्दी कहानी के इस दौर में प्रेमचन्द्र के अतिरिक्त शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, सुदर्शन, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा जैसे कथा शिल्पी शामिल थे। सन् 1916 में प्रेमचन्द ने अपनी प्रख्यात कहानी ‘पंच परमेश्वर’ लिखकर हिन्दी कहानी का मिजाज और वैचारिक आधारभूमि ही बदल दी थी।
इसी दौर के साथ और कुछ बाद में आती हैं वृंदावन लाल वर्मा, पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, रांगेय राघव, इलाचन्द्र जोशी, भगवती चरण वर्मा आदि की कहानियां। भले ही इस दौर के सभी कथाकारों ने अलग-अलग भावभूमि की कहानियाँ लिखी हों, किन्तु इनका विस्तृत कोलाज मुकम्मिल तौर पर यथार्थवाद और मानवतावादी है। इस दौर तक आते-आते हिन्दी कहानी का अनुभव फलक बहुत विस्तृत हो गया है। सामाजिक विद्रूपता से लेकर मनोजगत की संघटनाओं और ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों तक पर इस दौर में बेमिसाल कहानियां लिखी गईं।
आजादी मिलने के बाद हिन्दी की कथा रचना ने दूसरी महत्वपूर्ण करवट ली या कि उसे लेनी पड़ी। क्योंकि आजादी से पहले जिस समाज की परिकल्पना की गई थी वैसे समाज के निर्माण में संदेह दिखने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध, विभाजन की त्रासदी, और समानता के सपनों के बिखरते परिदृश्य ने देश की जनता का मोहभंग कर दिया था। फलस्वरूप कहानीकार की नई पीढ़ी ने अपनी-अपनी संवेदनाओं की नई जमीनें तलाशीं। अपने-अपने भाषाई और सामाजिक यथार्थ के अनुरूप नए रचना बोध की खोज की। एकाध कहानियां तो सभी पत्रिकाओं में छपती थीं परन्तु कथा-रचना के इस नए बोध का समवेत सर्जनात्मक विस्फोट कहानी विधा को समर्पित ‘कहानी’ नामक पत्रिका में हुआ, जिसके यशस्वी संपादक प्रेमचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र श्रीपत राय थे। इसकी पहचान अमरकान्त की डिप्टी कलक्टरी, मार्कण्डेय की ‘हंसा जाई अकेला’ कमलेश्वर की ‘राजा निरंबसिया’, राजेन्द्र यादव की ‘जहां लक्ष्मी कैद है’, शेखर जोशी की ‘कोसी का घटवार’, भीष्म साहनी की ‘चीफ की दावत’, उषा प्रियंवदा की ‘वापसी’, मोहन राकेश की ‘मलबे का मालिक’, निर्मल वर्मा की ‘परिंदे’ रांगेय राघव की ‘गदल’ कृष्णा सोबती की ‘बादलों के घेरे’ विष्णु प्रभाकर की ‘धरती अब भी घूम रही है’ आदि में मौजूद है। विभाजन की त्रासदी और तीखे मोहभंग के यथार्थ ने इस दौर में बहुआयामी अभिव्यक्ति पाई।
पांचवे दशक के आते-आते इस प्रवृत्ति ने हिन्दी कहानी में ‘अनुभव की प्रमाणिकता’ ने सहज और स्वाभाविक विस्तार पा लिया। बाद में इस अनुभव और रचना विस्तार को ‘नई कहानी’ का नाम दिया गया। जो कि एक आदोलन बना और जिसने हिन्दी कहानी के सरोकारों को, और स्वरूप को बदल कर उसके विकास क्रम का सार्थक रचना-मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि सन् उन्नीस सौ पचास के आस-पास से ही कहानियों के कथ्य और ट्रीटमेंट की शैली में परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। किन्तु इसका नामकरण सन् उन्नीस सौ पचपन में हो सका। इसकी नव्यता को पहचानकर इसे ‘नई कहानी’ की संज्ञा से अभिहित करने का काम प्रगतिशील धारा के कवि दुष्यंत कुमार ने ‘कल्पना’ पत्रिका के जनवरी 1955 के अंक में किया। कहानी के नए सरोकारों और प्रयोगधर्मिता को लेकर डॉ. धर्मवीर भारती ने ‘धर्मयुग’ में कहानी के बदले हुए स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहानीकारों-मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेन्द्र यादव का त्रिकोण स्थापित कर दिया। इसे कथालोचना में कुछ विचलन भी पैदा हुआ परन्तु सन् 1954 के ‘कहानी विशेषांक’ ने नई कहानी की वैचारिक भूमि पहले ही स्थापित कर दी थी। अमरकांत की कहानी ‘डिप्टी कलक्टरी’ और कमलेश्वर की कहानी ‘राजा निरबंसिया’ लिखी जा चुकी थीं। इसी क्रम में मोहन राकेश का कहानी संग्रह ‘नए बादल’ सन् 1956 में आया। इसी दौर में निर्मल वर्मा की कहानी ‘परिंदे’ और भुवनेश्वर की कहानी ‘भेडिये’ और उषा प्रियंवदा की कहानी ‘वापसी’ पर चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं। इन्हीं कहानियों को नई कहानी की प्रारंभिक कहानियों में गिना जाता है। इनके अलावा ‘कहानी’ और ‘नई कहानियां’ पत्रिकाओं ने इस आंदोलन की अधिकारिक रूप से घोषित पत्रिका थी।
दरअसल नए कहानीकारों ने यह महसूस किया कि वैचारिक स्तर पर यह मूल्यों के विघटन का दौर है। इस दौर में संदेह, अविश्वास, मोगभंग, भय और आशंका के व्यापार ने आदर्शवाद की सुखद कल्पनाओं को हाशिये पर डाल दिया था। इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, व्यक्तिवाद, साहित्यवाद, क्षणवाद, यथास्थितिवाद और इतिहासहीनता या फ्रॉयडवाद को नाकाफी समझ जाने लगा। और संबंधों के नए समीकरणों के बीच व्यवस्था के अंतर्विरोधी को सामने लाया गया। नई कहानी ने संयुक्त परिवार के ह्नास, नौकरी पेशा व शहरीकृत महत्वाकांक्षी नए मध्यवर्ग का उदय, शहरीकरण और पूंजी के बढ़ते वर्चस्व और बढ़ती आर्थिक-सामाजिक विषमता को खास तौर से रेखांकित किया। शहरीकरण और पारिवारिक विघटन के कथ्य भी सामने आए। नए कहानीकारों के तर्क के मुताबिक आजादी के बाद जिस प्रकार शहरी मध्यवर्ग की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई, उसी प्रकार उसकी समस्याओं का घनत्व भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। इन स्थितियों के प्रमाणिक स्वर उस दौर की कहानियों में मौजूद हैं। इस बीच आंचलिक कहानियों ने भाषाई देशजता और ग्रामीण यथार्थ की नई जमीन तोड़ी। मार्कण्डेय, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, विद्यासागर नौटियाल, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, विजयदान देखा आदि की कहानियों में आंचलिक यथार्थ का सघन, विद्रूपमय, और करुणापूरित संसार सामने आया। ऐसा नहीं कि इसमें उल्लास नहीं था, पर उल्लास के साथ-साथ ग्राम समाज की पीड़ा, परिवर्तनहीनता और बिडंबनाएं भी बड़ी शिद्दत से सामने आईं।
आंचलिकता के बाद के दौर की कहानियों का भी यह प्रिय विषय बना रहा। आज भी आंचलिक कहानियों काल यह कथा संसार नई प्रतीतियों, अपने दलित और दमित वर्गों के संत्रास और बदले हुए, अपराधग्रस्त समय का अन्वेषण कर रही हैं।
नई कहानी का कथ्य-विस्तार सचमुच चमत्कृत करता है। यह निश्चय ही उस कसौटी की देन थी जो स्वयं कथाकारों ने तैयार की थी और जिसे समीक्षा की शब्दावली में ‘अनुभव की प्रामाणिकता’ कहा गया। बाद में उसका विकृत रूप ‘भोगा हुआ यथार्थ’ भी प्रचलित हुआ।
और यह आकस्मिक नहीं था कि हिन्दी कहानी की परिधि में वह सब कुछ साकार हुआ जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज और देशकाल उस संक्रांति काल में आक्रांत और आहत था। यह एक महाजाति के दैहिक, भौतिक, पराभूत परलौकिक, वैचारिक संवेदना के बदलते प्रतिमानों, संबंधों के विघटन, नए संबंधों के निर्धारण, मूल्यों के विचलन और न्याय-अन्याय के प्रश्नों से जूझता हुआ संक्रमण काल था, जिसे नई कहानी ने समकालीन मनुष्य के संदर्भ में रचनात्मक दक्षता और गहरे मानवीय सरोकारों के साथ प्रस्तुत किया था। जन-मानस की सोच और सौंदर्य को बदला था। इसने साहित्य की परिपाटीबद्ध यथास्थिति को खारिज किया था। विधागत और परिभाषागत नए पैमानों और प्रतिमानों का संधान किया था। शास्त्रसम्मत कहानी के ढांचे को तोड़कर उसे समकालीन समय के लिए संभव और विशाल पाठक वर्ग के लिए मित्रवत दस्तावेजों के रूप में अनिवार्य बनाया था। गंभीर साहित्य के लेखक और जागरूक पाठकवर्ग के वैचारिक संबंधों की परस्परिकता का यह स्वर्णकाल था। भाषाई स्तर पर नई कहानी ने जातीय, जनजातीय, देशज और आंचलिक इलाकों की अस्मिता और उपस्थिति को पहचाना और आत्मसात किया था। इंद्रधनुषी-विप्लव कभी उपस्थित नहीं हुआ था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book