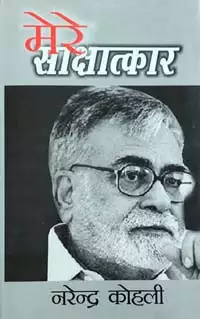|
नाटक-एकाँकी >> हत्यारे हत्यारेनरेन्द्र कोहली
|
100 पाठक हैं |
||||||
प्रसिद्ध लेखक नरेन्द्र कोहली का एक विशिष्ट नाटक
कागजी संस्करण
प्रसिद्ध लेखक नरेन्द्र कोहली ने उपन्यास, कहानी तथा व्यंग्य के अलावा
नाटक भी लिखे हैं जो बहुत पसन्द किए गए हैं। उस संकलन में उसके तीन
विशिष्ट नाटक एक-साथ प्रस्तुत किए गए हैं। ‘हत्यारे’, ‘शंबूक की हत्या और ‘गारे की दीवार’, तीनों ही नाटक सफलता पूर्वक मंचित होकर साहित्य-जगत में धूम मचा चुके हैं।
नरेन्द्र कोहली के सभी नाटक समाज और जीवन से जुड़ी उन मौलिक समस्याओं और स्थितियों से जद्दोजहद करते नज़र आते हैं जो समकालीन मनुष्य को परेशान कर रही हैं। इसमें तीखा व्यंग्य भी होता है जो पाठक को व्यापक सत्य के सामने खड़ा कर देता है।
नरेन्द्र कोहली के सभी नाटक समाज और जीवन से जुड़ी उन मौलिक समस्याओं और स्थितियों से जद्दोजहद करते नज़र आते हैं जो समकालीन मनुष्य को परेशान कर रही हैं। इसमें तीखा व्यंग्य भी होता है जो पाठक को व्यापक सत्य के सामने खड़ा कर देता है।
ये तीन नाटक
नाटक पढ़ने, देखने और खेलने में मेरी पर्याप्त रूचि रही है; किन्तु फिर भी
मैं स्वयं को सामान्यतः कथाकार ही मानता रहा हूँ। शंबूक की हत्या का जब
पहला आलेख तैयार किया था तो वह भी एक उपन्यास ही था। उसे मैं प्रकाशक के
यहाँ पहुँचा भी आया था। उन्होंने रख भी लिया था।...
किन्तु न तो प्रकाशक के यहाँ से उसकी स्वीकृति मिली और न ही मेरा अपना मन सन्तुष्ट हुआ। कोई कमी थी, जो कि खटक रही थी और यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस उपन्यास में कसर कहाँ है। अंततः मुझे लगा कि वस्तुतः मेरा अपना व्यक्तित्व कथा के कितना ही अनुकूल क्यों न हो, उसमे न तो शंबूक की हत्या की सामग्री केवल नाटक के ही अनुकूल हो सकती है। उसमें न तो कथा का विकास है और न ही कोई गति है। वस्तुतः उसमें घटना नहीं स्थितियाँ हैं। संवाद है। व्यंग्य है। वह देखा जा सकता है। सुना जा सकता है। शायद पढ़ा नहीं जा सकता। उसे तो नाटक ही होना होगा।
मैंने ये बातें अपने प्रकाशक से कहीं तो वे उछल गए। बोले, मैं भी सोच ही रहा था कि मैं न तो अस्वीकार कर पा रहा हूँ और न ही स्वीकृति दे पा रहा हूँ। आख़िर बात क्या है। अब आपके कहने से बात समझ में आई है।
मैं पांडुलिपि अपने साथ ले आया और फिर उसको नाटक के रुप में लिखा। तभी मैं यह समझ पाया कि विधा के चुनाव में जहाँ लेखक का व्यक्तितत्व एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, वहीं वह सामग्री भी अपना व्यक्तित्व रखती है। और उसको त्याग कर किसी भी अन्य विधा में ढल जाने को बाध्य नहीं है वह। आवश्यक नहीं कि किसी भी सामाग्री को लेखक अपने व्यक्तित्व की प्रिय विधा में ढाल ही ले।
मैंने मान लिया था कि मेरे उपन्यासों के बीच शंबूक की हत्या अपवाद स्वरूप नाटक के रूप में लिखा गया। मन में कहीं यह भी था कि संभव है कि फिर कोई नाटक लिखने का अवसर ही न आए; किन्तु जब अपने एक परिचित परिवार में एक दुखद अकाल मृत्यु हुई तो विचित्र स्थिति उठ खड़ी हुई। जब पहली सूचना आई तो वह एक कथा कह रही थी। सहसा कुछ और तथ्य उद्घाटित हुए तो उसका रुप ही बदल गया। फिर कुछ और...मेरी कल्पना उस पर कुछ और भी कथाएँ भी आरोपित करने लगी। मुझे लगा कि उसमें कथा आगे नहीं बढ़ रही, बस एक घटना पर से रहस्य के पर्दे उठते जा रहे हैं। अनेक व्यक्तियों के जाने-पहचाने चेहरों के नीचे से नए-नए चेहरे उद्घाटित होते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने चेहरे नहीं नकाब पहन रखे थे। एक ही दृश्य का पर्दा हटता था तो वह बदल कर कुछ और हो जाता था। घटना एक ही थी, पर कथाएँ अनेक थीं।
चेहरा एक ही था, किन्तु उसके रुप अनेक थे। उस सारी घटना ने मुझे बहुत आलोड़ित किया, किन्तु वह उपान्यास नहीं बन सका। वह संवादों, मंच और रुपक तत्व के बाहर ही नहीं निकला। तो उपन्यास कैसे लिखा जा सकता था। उसे नाटक ही बनना था और मुझे नाटक लिखना पड़ा। वह हत्यारे के रुप में प्रस्तुत हुआ। गारे की दीवार की रचना का सत्य और भी चामत्कारिक था। हम तीन-चार मित्रों के मकान आस-पास ही बन रहे थे। दिन भर मकान बनने की प्रकिया और मकान बनानेवालों के मनोविज्ञान के बीच घिरा मैं बहुत कुछ नया देख और सीख रहा था।
मैं भी अपना मकान बनवा रहा था किन्तु वह तो अपने रहने के लिए था। अपने मालिक-मकान से डरा हुआ मैं, अपने परिवार के लिए एक छत का प्रबन्ध कर रहा था। किन्तु यहाँ तो कोई और ही संसार था। मकान बनाने के पीछे व्यक्ति के सपने भी थे। उसकी सृजनधर्मिता भी थी, किन्तु उसका एक समाज भी था। उसका अहंकार भी था। उसका आडंबर और उसकी मन की अंधेरी गुफाओं में छिपा एक पशु भी था, जिसने अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान ओढ रखी थी।
वहीं गारे की चिनाई और एक दीवार के ढहने की चर्चा से इस नाटक का बीजवपन हुआ। वह मकान मेरे लिए एक मंच बन गया, जिस पर से अपने आप एक पर्दा हट जाता था और एक नया दृश्य आरंभ हो जाता था। समाज का कौन सा दृश्य कहाँ से आकर उसमें जुड़ जाता था, यह तत्काल समझ में नहीं आता था, किन्तु था वह हमारा समाज ही। वह समाज, जिसने अपराध को न केवल अपने जीवन में स्वीकार कर लिया था, वरन, उसे जीवन की उत्कृष्ट शैली मान कर गौरवान्वित भी कर रहा था। सफलता और अपराध में बहुत कम दूरी रह गई थी।
नाटक लिखने के पश्चात् सदा ही एक द्वन्द्व मन में होता है। कि पहले उसका मंचन हो और फिर वह पुस्तकाकार प्रकाशित हो या उसके मंचन की प्रतीक्षा किए बिना उसका प्रकाशन करवा दिया जाए, ताकि नए नाटक की पांडुलिपि खोजने वाले रंगकर्मियों तक वह तत्काल पहुँच सके। नाटक को प्रकाशन से पहले मंचित होना है। तो आवश्यक है। कि या तो लेखक की अपनी नाटक मंडली हो, अथवा वह किसी मंडली के इतने निकट हो कि उसके मेज़ से मंडली उसका नाटक उठा ले।
मैं आरम्भ से ही अपने कमरे में अकेला रहने वाला और मंडलियों से बहिष्कृत व्यक्ति हूँ। वैसे भी मेरे लेखन व्यस्तता, मुझे मंचन के लिए आवश्यक समय की सुविधा प्रदान नहीं करती। मैं मानता हूँ कि मैं लेखक हूँ। मैं मंचकर्मी कभी नहीं बन सका मैं यह भी कभी स्वीकार नहीं कर सका कि लेखक को निर्देशक के साथ मिल कर नाटक का मंचन करवाना चाहिए। मैं सदा मानता रहा हूँ कि लेखक का काम आलेख तैयार करने तक है। मंचन तो निर्देशक द्वारा अपनी रचना है। एक ही नाटक को दस निर्देशक दस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी में उन की मौलिकता है। मैंने अपने ही नाटकों के सन्दर्भ में देखा है। कि किसी निर्देशक ने मेरे नाटक को आलेख से भी सुन्दर बना कर प्रस्तुत किया और किसी निर्देशक ने अपनी नासमझी में उसे घटिया नाटक सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छो़ड़ी।
मेरे पास अच्छे प्रकाशक थे, इसलिए नाटक पहले प्रकाशित हुए और बाद में उनका मंचन होता रहा। अपने नाटकों के मंचन के सन्दर्भ में मुझे चन्द्रमोहन, ज़फ़र संजरी और राकेश डग बहुत याद आते हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं पूर्वाभ्यासों में कहीं उनके साथ रहूँ किन्तु मुझे सदा दर्शक के समान हॉल में बैठ कर नाटक देखना ही अच्छा लगा। सम्भव है कि अपने व्यव्हार के कारण मुझे कुछ हानि भी उठानी पड़ी हो; किन्तु मैं यह मानता हूँ। कि लेखक निर्देशक के साथ रहेगा तो उसका नाटक केवल एक ही प्रकार से मंचित हो सकेगा, जबकि नाटक एक ऐसी विधा है कि जो प्रत्येक निर्देशक, प्रत्येक मंडली और प्रत्येक अभिनेता के बदलते ही एक नया रूप ग्रहण कर लेता है। मैं लेखक के रूप में अपना कार्य कर चुका। उसके पश्चात, निर्देशक और अभिनेताओं की रचना आरम्भ होती है।
एक-एक कर छपने के वर्षो बाद आज ये तीन नाटक एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। यह विश्वनाथ जी की अपनी परिकल्पना है। मैं तो चाहता था कि नाटक सीधे पाठक तक पहुँचे, मैं बीच में न आऊँ; किन्तु विश्वनाथ जी की इच्छा है कि मैं पाठकों को नाटकों के सृजन का सत्य भी बताऊँ। कैसा संयोग है कि उन्होंने भी इनमें से किसी नाटक के निर्देशक की निर्देशकीय टिप्पणी नहीं माँगी, लेखक को ही अपना सच बताने को कहा। शायद यह इसलिए कि नाटक अपने मूल रूप में रहे और जब इनका मंचन हो तो निर्देशक अपनी कल्पना का मौलिक और सृजनात्मक प्रयोग कर सके।
5-1-1999
किन्तु न तो प्रकाशक के यहाँ से उसकी स्वीकृति मिली और न ही मेरा अपना मन सन्तुष्ट हुआ। कोई कमी थी, जो कि खटक रही थी और यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस उपन्यास में कसर कहाँ है। अंततः मुझे लगा कि वस्तुतः मेरा अपना व्यक्तित्व कथा के कितना ही अनुकूल क्यों न हो, उसमे न तो शंबूक की हत्या की सामग्री केवल नाटक के ही अनुकूल हो सकती है। उसमें न तो कथा का विकास है और न ही कोई गति है। वस्तुतः उसमें घटना नहीं स्थितियाँ हैं। संवाद है। व्यंग्य है। वह देखा जा सकता है। सुना जा सकता है। शायद पढ़ा नहीं जा सकता। उसे तो नाटक ही होना होगा।
मैंने ये बातें अपने प्रकाशक से कहीं तो वे उछल गए। बोले, मैं भी सोच ही रहा था कि मैं न तो अस्वीकार कर पा रहा हूँ और न ही स्वीकृति दे पा रहा हूँ। आख़िर बात क्या है। अब आपके कहने से बात समझ में आई है।
मैं पांडुलिपि अपने साथ ले आया और फिर उसको नाटक के रुप में लिखा। तभी मैं यह समझ पाया कि विधा के चुनाव में जहाँ लेखक का व्यक्तितत्व एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है, वहीं वह सामग्री भी अपना व्यक्तित्व रखती है। और उसको त्याग कर किसी भी अन्य विधा में ढल जाने को बाध्य नहीं है वह। आवश्यक नहीं कि किसी भी सामाग्री को लेखक अपने व्यक्तित्व की प्रिय विधा में ढाल ही ले।
मैंने मान लिया था कि मेरे उपन्यासों के बीच शंबूक की हत्या अपवाद स्वरूप नाटक के रूप में लिखा गया। मन में कहीं यह भी था कि संभव है कि फिर कोई नाटक लिखने का अवसर ही न आए; किन्तु जब अपने एक परिचित परिवार में एक दुखद अकाल मृत्यु हुई तो विचित्र स्थिति उठ खड़ी हुई। जब पहली सूचना आई तो वह एक कथा कह रही थी। सहसा कुछ और तथ्य उद्घाटित हुए तो उसका रुप ही बदल गया। फिर कुछ और...मेरी कल्पना उस पर कुछ और भी कथाएँ भी आरोपित करने लगी। मुझे लगा कि उसमें कथा आगे नहीं बढ़ रही, बस एक घटना पर से रहस्य के पर्दे उठते जा रहे हैं। अनेक व्यक्तियों के जाने-पहचाने चेहरों के नीचे से नए-नए चेहरे उद्घाटित होते जा रहे हैं, जैसे उन्होंने चेहरे नहीं नकाब पहन रखे थे। एक ही दृश्य का पर्दा हटता था तो वह बदल कर कुछ और हो जाता था। घटना एक ही थी, पर कथाएँ अनेक थीं।
चेहरा एक ही था, किन्तु उसके रुप अनेक थे। उस सारी घटना ने मुझे बहुत आलोड़ित किया, किन्तु वह उपान्यास नहीं बन सका। वह संवादों, मंच और रुपक तत्व के बाहर ही नहीं निकला। तो उपन्यास कैसे लिखा जा सकता था। उसे नाटक ही बनना था और मुझे नाटक लिखना पड़ा। वह हत्यारे के रुप में प्रस्तुत हुआ। गारे की दीवार की रचना का सत्य और भी चामत्कारिक था। हम तीन-चार मित्रों के मकान आस-पास ही बन रहे थे। दिन भर मकान बनने की प्रकिया और मकान बनानेवालों के मनोविज्ञान के बीच घिरा मैं बहुत कुछ नया देख और सीख रहा था।
मैं भी अपना मकान बनवा रहा था किन्तु वह तो अपने रहने के लिए था। अपने मालिक-मकान से डरा हुआ मैं, अपने परिवार के लिए एक छत का प्रबन्ध कर रहा था। किन्तु यहाँ तो कोई और ही संसार था। मकान बनाने के पीछे व्यक्ति के सपने भी थे। उसकी सृजनधर्मिता भी थी, किन्तु उसका एक समाज भी था। उसका अहंकार भी था। उसका आडंबर और उसकी मन की अंधेरी गुफाओं में छिपा एक पशु भी था, जिसने अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान ओढ रखी थी।
वहीं गारे की चिनाई और एक दीवार के ढहने की चर्चा से इस नाटक का बीजवपन हुआ। वह मकान मेरे लिए एक मंच बन गया, जिस पर से अपने आप एक पर्दा हट जाता था और एक नया दृश्य आरंभ हो जाता था। समाज का कौन सा दृश्य कहाँ से आकर उसमें जुड़ जाता था, यह तत्काल समझ में नहीं आता था, किन्तु था वह हमारा समाज ही। वह समाज, जिसने अपराध को न केवल अपने जीवन में स्वीकार कर लिया था, वरन, उसे जीवन की उत्कृष्ट शैली मान कर गौरवान्वित भी कर रहा था। सफलता और अपराध में बहुत कम दूरी रह गई थी।
नाटक लिखने के पश्चात् सदा ही एक द्वन्द्व मन में होता है। कि पहले उसका मंचन हो और फिर वह पुस्तकाकार प्रकाशित हो या उसके मंचन की प्रतीक्षा किए बिना उसका प्रकाशन करवा दिया जाए, ताकि नए नाटक की पांडुलिपि खोजने वाले रंगकर्मियों तक वह तत्काल पहुँच सके। नाटक को प्रकाशन से पहले मंचित होना है। तो आवश्यक है। कि या तो लेखक की अपनी नाटक मंडली हो, अथवा वह किसी मंडली के इतने निकट हो कि उसके मेज़ से मंडली उसका नाटक उठा ले।
मैं आरम्भ से ही अपने कमरे में अकेला रहने वाला और मंडलियों से बहिष्कृत व्यक्ति हूँ। वैसे भी मेरे लेखन व्यस्तता, मुझे मंचन के लिए आवश्यक समय की सुविधा प्रदान नहीं करती। मैं मानता हूँ कि मैं लेखक हूँ। मैं मंचकर्मी कभी नहीं बन सका मैं यह भी कभी स्वीकार नहीं कर सका कि लेखक को निर्देशक के साथ मिल कर नाटक का मंचन करवाना चाहिए। मैं सदा मानता रहा हूँ कि लेखक का काम आलेख तैयार करने तक है। मंचन तो निर्देशक द्वारा अपनी रचना है। एक ही नाटक को दस निर्देशक दस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी में उन की मौलिकता है। मैंने अपने ही नाटकों के सन्दर्भ में देखा है। कि किसी निर्देशक ने मेरे नाटक को आलेख से भी सुन्दर बना कर प्रस्तुत किया और किसी निर्देशक ने अपनी नासमझी में उसे घटिया नाटक सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छो़ड़ी।
मेरे पास अच्छे प्रकाशक थे, इसलिए नाटक पहले प्रकाशित हुए और बाद में उनका मंचन होता रहा। अपने नाटकों के मंचन के सन्दर्भ में मुझे चन्द्रमोहन, ज़फ़र संजरी और राकेश डग बहुत याद आते हैं। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं पूर्वाभ्यासों में कहीं उनके साथ रहूँ किन्तु मुझे सदा दर्शक के समान हॉल में बैठ कर नाटक देखना ही अच्छा लगा। सम्भव है कि अपने व्यव्हार के कारण मुझे कुछ हानि भी उठानी पड़ी हो; किन्तु मैं यह मानता हूँ। कि लेखक निर्देशक के साथ रहेगा तो उसका नाटक केवल एक ही प्रकार से मंचित हो सकेगा, जबकि नाटक एक ऐसी विधा है कि जो प्रत्येक निर्देशक, प्रत्येक मंडली और प्रत्येक अभिनेता के बदलते ही एक नया रूप ग्रहण कर लेता है। मैं लेखक के रूप में अपना कार्य कर चुका। उसके पश्चात, निर्देशक और अभिनेताओं की रचना आरम्भ होती है।
एक-एक कर छपने के वर्षो बाद आज ये तीन नाटक एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। यह विश्वनाथ जी की अपनी परिकल्पना है। मैं तो चाहता था कि नाटक सीधे पाठक तक पहुँचे, मैं बीच में न आऊँ; किन्तु विश्वनाथ जी की इच्छा है कि मैं पाठकों को नाटकों के सृजन का सत्य भी बताऊँ। कैसा संयोग है कि उन्होंने भी इनमें से किसी नाटक के निर्देशक की निर्देशकीय टिप्पणी नहीं माँगी, लेखक को ही अपना सच बताने को कहा। शायद यह इसलिए कि नाटक अपने मूल रूप में रहे और जब इनका मंचन हो तो निर्देशक अपनी कल्पना का मौलिक और सृजनात्मक प्रयोग कर सके।
5-1-1999
नरेन्द्र कोहली
हत्यारे
पात्र
अनिल
बनारसीदास
शान्ति
शालिनी
सुरेश
उर्मिला
परेश
वैजयन्ती
खन्ना
पुरुषः एक
परूषः दो
स्त्रीः एक
स्त्रीः दो
दृश्यः एक
नई दिल्ली
सन् 1982
( एक मध्यवर्गीय ड्राइंगरूम। सोफा, कुर्सियाँ और दीवान। आवश्यकतानुसार छोटी-बड़ी मेज़ें भी रखी जा सकती हैं। दीवार में एक खिड़की और एक अलमारी।
प्रकाश होने पर कमरे में बनारसीदास और शान्ति बैठे हैं। हाथ में एक पत्रिका लिए अनिल एक ओर खड़ा है, जैसे पढ़ रहा हो, किसी प्रतीक्षा में पत्रिका के पृष्ठ पलट रहा हो।
पत्रिका रख, वह धीरे-धीरे आकर, बनारसीदास के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। )
अनिलः तो क्या तय किया है। पापा, आपने ?
बनारसीदासः तय क्या करना है, बेटा ! मैं तो आ
ऑपरेशन के ही पक्ष में नहीं हूँ। जीवित शरीर की चीर-फाड़। मुझे डॉक्टर का यह हत्यारापन अच्छा नहीं लगता।
अनिलः तो आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर क्या करे ?
बनारसीदासः दवा दे। रोगी को दवा से अच्छा करना चाहिए। यह रक्तपात...
अनिलः पापा !
बनारसीदासः हाँ, बेटे।
अनिलः ऑपरेशन सम्बन्धी सैद्धान्तिक बहस हम फिर कर लेंगे। अपनी बात कहिए...आप अपना ऑपरेशन...
बनारसीदासः पचहत्तर वर्ष का हो गया। बहुत जी लिया। अब और क्या है, जिसके लिए मुझे जिलाए रखना चाहते हो ?
अनिलः आप से यह नहीं पूछा था मैंने !
बनारसीदासः अच्छा। मैंने समझा कि शायद यही पूछा था। (मुस्कराने लगता है। फिर उसके चेहरे से मुस्कान ग़ायब हो जाती है। व्यंग्य और प्रहार की मुद्रा अपनाकर) अपने स्कूली दिनों में मेरे साथ यही होता था। मास्टर कुछ पूछता था, और मैं कुछ और समझ बैठता था। परिणामतः सदा नालायक ही माना गया मैं। क्या पूछा था तुमने ?
अनिलः डॉ. मेहरा से ऑपरेशन का समय ले लूँ या आप मद्रास जाना चाहेंगे दीदी के पास डॉक्टर यहाँ अच्छा है और अस्पताल की सुविधाएँ, वहाँ अधिक हैं।
बनारसीदासः जब मैं ऑपरेशन ही नहीं कराना चाहता...
शान्तिः ओह-हो ! फिर वही हठ ! अरे, वह जो पूछ रहा है, उसका उत्तर दो।
बनारसीदासः पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर देना होगा ? अपनी बात नहीं कर सकता मैं ? घरेलू बातचीत में भी अब स्कूली परीक्षा का तौर-तरीका चलेगा क्या ?
शान्तिः हाँ ! अभी प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। अपनी बात फिर कहते रहिएगा।
बनारसीदासः तभी तो कहता हूँ कि इस जीवन का क्या करना है मुझे, जिस पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं रहा।
शान्तिः क्यों ? आपके अधिकारों में कहाँ कटौती हो गई ?
बनारसीदासः अपनी बात नहीं कह सकता। अपने ढंग से नहीं कह सकता। (रूककर) मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा ही होगा।
शान्तिः क्यों ?
बनारसीदासः बोझ हूँ। दूसरों पर आश्रित हूँ। इस पराये जीवन के लिए ऑपरेशन का कष्ट मैं क्यों सहूँ ?
अनिलः पापा। बात को ग़लत दिशा में मत मोड़िए।...हम जब छोटे थे, तब हमारा जीवन अपना नहीं था। तब हमें पूछे गए प्रश्नों का ही उत्तर देना था। अपनी बात हम कह नहीं सकते थे। तब हमें मर जाना चाहिए था क्या ?
बनारसीदासः (चि़ड़चिड़ाहट के स्पष्ट लक्षणों को छिपाकर मुस्कराता है।) अब बात को उल्टी दिशा में तुम ले जा रहे हो। बच्चों को उनके माँ-बाप ही पालते हैं।
अनिलः तो बाद में माँ-बाप को बच्चे ही पालते हैं।
बनारसीदासः चलो, यही सही। पर अब मुझे ही अपना जीवन बोझ लगने लगा है।
शान्तिः इनकी तो आदत ही है, बेटा ! ऐसी बातें करने की। अपने बच्चे भी होते न औरों के बच्चों जैसे...
बनारसीदासः कैसे ?
शान्तिः वैसे, जैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं।...तब आपको भी पता लगता।
बनारसीदासः क्या कहना चाहती हो-तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं।
शान्तिः बेटे क्या और बेटियाँ क्या। सभी अच्छे हैं...जिसको देखो, वही बुला रहा है, सिर-आँखों पर बैठा रहा है-बेटा हो या दामाद।
बनारसीदासः इसलिए तो मैं कहता हूँ, अधिक सन्तान लाभदायक होती हैं। जाने क्यों लोग हाथ धोकर परिवार नियोजन के पीछे पड़े हैं। सब कुछ है देश में। बताओ क्या नहीं है ? (शान्ति की ओर देखकर ) पर तुम क्या बताओगी, तुम्हे तो यह भी पता नहीं होता कि घर में क्या है और क्या नहीं होता।
शान्तिः मैं तो हूँ ही मूर्ख। आप अपनी बात कीजिए।
बनारसीदासः अपनी बात ही कह रहा हूँ। एक ही बेटा होता न हमारा भी तो तुम बहू के बर्तन धो रही होतीं। मैं उनके बच्चों को स्कूल पहुँचाने जाता और भोगल से सब्ज़ी ख़रीदता हुआ, थका-हारा लड़खड़ाता हुआ घर आता।
अनिलः पापा !
बनारसीदासः हाँ, बेटे ! यह तो अधिक बच्चों का ही लाभ है कि इशारा पाया और हमने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा।
अनिलः पापा ! आप तो फै़मिली प्लानिंग वालों का ऑपरेशन करने लगे।...मैं पूछ रहा था, आपका वह ऑपरेशन...
(नेपथ्य में घण्टी बजती है।)
शान्तिः देखूं तो कौन आया है। (उठने लगती है।)
अनिलः आप बैठी रहिए। शालिनी देख लेगी। नहीं तो मैं देखता हूँ। (उठते-उठते फिर बैठ जाता है।)...शालिनी गई है शायद।
शान्तिः वासन्ती की कोई चिठ्टी नहीं आई ? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
अनिलः अरे मम्मी ! जिसके पास सबसे ज्यादा नौकर-चाकर हों, उसी का आपको भी ध्यान रहता है। वासन्ती तो पापा को बुला रही है, ऑपरेशन के लिए। और आप उसके लिए ही चिन्तित हैं। उसे क्या कमी है !...
शान्तिः उसे कमी है अकल की; नहीं तो इतने नौकरों की क्या आवश्यकता है !
अनिलः सम्भव है, अधिक सन्तान के समान, अधिक नौकरों का भी कोई लाभ हो- जिसे वही जानती हो।
शान्तिः जैसे कोई काम एक न करे, तो दूसरा कर दे।
बनारसीदासः क्या मूर्खता है ! नौकर और बच्चे एक हैं क्या !
अनिलः बच्चे यदि अपने स्वार्थ के लिए पैदा किए जाएँ, तो फिर तो एक ही हैं।
(शालिनी आती है।)
अनिलः गया ? कौन था ?
शालिनीः (लिफाफा अनिल की ओर बढ़ा देती है।) तार !
बनारसीदासः अरे तार ! किसका है ? (उठने का उपक्रम करके रह जाता है।) कौन आ रहा है ?
(अनिल बढ़कर तार ले लेता है।)
शान्तिः तार क्या केवल किसी के आने का ही होता है ?
बनारसीदासः और क्या लाटरी खुलने का होता है ! इतनी ही भाग्यशालिनी होतीं तुम...
अनिलः (लिफ़ाफ़ा खोलकर, बिना सोचे-समझे, अभ्यासवश पढ़ जाता है।) ‘रमेश सीरियस। कम इमीडिएटली।’
शान्तिः (बनारसी के चेहरे को गम्भीर और चिन्तित होते देखती जाती है) क्या हुआ ? रमेश आ रहा है क्या ? (कोई कुछ नहीं कहता। उन तीनों की गम्भीरता देखकर शान्ति चिन्तित हो उठती है।)...यह मुँह-झौंसी अंग्रेजी़ ! अंग्रेज़ कब के चले गए, पर तार आज भी अंग्रेज़ी में ही आएगा...(उत्तेजना में उठना चाहती है।)
अनिलः ( जल्दी से शान्ति के पास पहुँचकर, कन्धों से पकड़कर उसे बैठाता है। हल्के से थपथपाता है।) कुछ नहीं, मम्मी ! आप बैठिए।...रमेश बीमार है शायद।
बनारसीदासः (जड़ मुद्रा क्रमशः सजीव होती है।) किसने दिया है तार ?
अनिलः कोई श्रीराम खन्ना है। (चेहरे पर खीझ और परेशानी स्पष्ट हो जाती है।) जाने कौन है ! कोई है भी, या किसी ने यूँ ही तार दे दिया हमें परेशान करने को।
शालिनीः ऐले ही कोई क्यों दे देगा ? क्या मिलेगा किसी को ?
अनिलः मिलता है, कुछ लोगों को।
बनारसीदासः अरे, कोई रोड एक्सिडेण्ट तो नहीं।...बम्बई की गाड़ियाँ भी...कहीं गाड़ी से चढ़ते- उतरते...
शान्तिः क्या गाड़ी से गिर पड़ा है ?
बनारसीदासः किसने कह दिया तुमसे कि गाड़ी से गिर पड़ा है। मूर्खों के समान...
अनिलः ओह हो पापा ! आप भी...
शालिनीः बम्बई फोन करके नहीं पूछा जा सकता ?
बनारसीदासः हाँ ! अगर फोन करके...
अनिलः हाँ ! हो सकता है।...अपनी कम्पनी के बम्बई ऑफिस में फोन करूँ तो...
बनारसीदासः वह है कहाँ ? घर में, अस्पताल में ?...
अनिलः अस्पताल में है। लिखा है न ‘टाटा हॉस्पिटल’।
बनारसीदासः लिखा है, पर तुमने पढ़ा तो नहीं।
शान्तिः (खीझकर) पढ़ा नहीं जाए तो लिखा हुआ मिट तो नहीं जाता।
अनिलः अच्छा ! मैं फोन करके देखता हूँ।
(अनिल भीतर चला जाता है। शालिनी आकर अनिल द्वारा खा़ली की गयी कुर्सी पर थकी-सी बैठ जाती है।)
शान्तिः तुम क्या सोचती हो, शालिनी ? वह बीमार होगा या...
शालिनीः (स्वयं को सम्भालती है।) मैं क्या कहूँ, मम्मी ! लिखा तो कुछ भी नहीं ही है। रमेश ने कभी-भी तो अपना ध्यान नहीं रखा...सदा का लापरवाह...
बनारसीदासः कहीं किसी से झगड़ा न किया हो। बम्बई में...
शालिनीः ( शान्ति के चिन्तित होते हुए चेहरे को देखती है और फिर पलटकर बनासीदास को) पापा ! आप सारी अनहोनी बातें कह-कहकर खुद भी परेशान होंगे, हमें भी करेंगे...
शान्तिः अभी क्या है, अभी तो ये एक-से-एक भयंकर बीमारियों का नाम ले-लेकर मुझे डराएँगे, तड़पाएँगे। ये तो चाहेंगे ही कि मेरी नींद हराम हो जाए और मैं रातभर बिस्तर पर करवटें बदलती रहूँ...
बनारसीदासः तुम सो नहीं पाओगी, तो मैं सो पाऊँगा क्या ? बेकार बोलती चली जाएगी। एक बार छिड़ पड़े तो थमने पर ही नहीं आती। (शालिनी की ओर देखकर) बेटा है मेरा। मुझे चिन्ता नहीं होगी ?...
शान्तिः मालूम है मुझे !...चिन्ता होगी कोई और बड़ी बीमारी क्यों न हुई उसे। अपना एक ऑपरेशन नहीं करवा सकते। उसके लिए दुनिया-भर के रोगों का नाम ले-लेकर मेरा दिल जलाओगे...
बनारसीदासः क्यों ? मेरा बेटा नहीं है वह ?
शान्तिः बेटा...(उसकी आँखों में एक खूँखार भाव उभरता है। बनारसीदास उसका सामना नहीं कर सकता। मुँह दूसरी ओर फेर लेता है।) जब वह आठवीं में फेल हुआ था...
शालिनीः (अचकचाकर शान्ति और बनारसीदास को देखती है।) पता नहीं उन्हें बम्बई की लाइन मिली या नहीं...
बनारसीदासः ( जैसे अपनी घुटन से छुटकारा पाने के लिए झरोखा मिल गया हो।) इतनी जल्दी कहाँ मिली होगी ! दिल्ली का एक नम्बर मिलने में तो घण्टा लग जाता है, बम्बई तक का नम्बर...
शालिनीः वैसे भी दिल्ली और बम्बई, दोनों ही बहुत बिज़ी एक्चेंज हैं। फिर दिन का समय...बिज़नेस वाले...
बनारसीदासः काम-धाम का बोझ तो समझ में आता है, पर...यहाँ तो एक्चेंज क्या, केबल्स क्या, आदमी क्या-सब कुछ ही सड़ा हुआ है। व्यवस्था ही सड़ रही है...
शान्तिः ( अँगुलियों से अपने माथे को दबाते हुए ) सड़ तो मेरा सिर रहा है...
बनारसीदासः कहता हूँ चिन्ता मत किया करो।... पर तुम क्यों मानोगी। तुम तो चाहोगी कि तुम्हारे सिर में दर्द हो और तुम मुझे परेशान करो। मैं डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटूँ ?
शान्तिः कब-कब काटे आपने डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर ?
बनारसीदासः नहीं काटे ?
शान्तिः अब मुँह मत खुलवाइए। जब तक स्वस्थ रही, आपकी रही। बीमार होते ही मायकेवालों के गले मढ़ देते थे आप !
बनारसीदासः और तो कुछ बस का है नहीं तुम्हारे। चिन्ता पड़ते ही मुझसे लड़ने लगती हो।
शालिनीः चलिए, मम्मी ! भीतर चलकर लेट जाइए। बैठे-बैठे वैसे भी थक गयी होंगी।
शान्तिः नहीं ! ठीक हूँ मैं । अभी नहीं लेटूँगी।
बनारसीदासः लेटकर भी चिन्ता की जा सकती है। लेटने से सिर-दर्द रूक नहीं जाएगा तुम्हारा...
शान्तिः आपकी जुबान भी नहीं रूकेगी !
शालिनीः (उठकर शान्ति के पास आती है) चलिए, मम्मी ! यहीं दीवान पर लेट जाइए। कुछ आराम मिलेगा।
शान्तिः नहीं ! मैं ठीक हूँ। अनिल को आ लेने दो। जाने वह क्या ख़बर लाता है !
बनारसीदासः तुम्हारे तनकर बैठे रहने से, ख़बर तुम से डरकर कुछ और नहीं हो जाएगी...
शालिनीः पापा ! (शान्ति के कन्धे पकड़कर) लेट जाइए मम्मी ! जो ख़बर आयगी, आपके सामने आयगी।
(शान्ति के विरोध को अनदेखा कर शालिनी उसे बाँह से पकड़कर उठाती है। शान्ति इच्छा-अनिच्छा के बीच, उठकर दीवान तक आती है। शान्ति के लेटने के बाद शालिनी उसका सिर उठाकर उसके नीचे गद्दी रख देती है। दो-तीन बार अपनी हथेलियों से उसका सिर दबाती भी है।)
शान्तिः नहीं ! रहने दे। ( हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। क्षण भर रूककर ) तू मेरा सिर दबाएगी, तो तेरे पापा मेरा गला दबा देंगे।
बनारसीदासः इसी से तो तुम्हारी जीभ मुँह से इतनी बाहर निकल आयी है।
शालिनीः पापा ! ( दीवान पायताने पड़ी चादर उठा, शान्ति को ओढ़ा देती है और लौटकर अपने स्थान पर आ जाती है।)
बनारसीदीसः बेटी ! तुम समझती होगी कि मैं बहुत झक्की हो गया हूँ।...
शालिनीः नहीं, पापा !
बनारसीदासः नहीं-नहीं ! थोड़ा बहुत हो भी गया हूँ।...पर कोई परेशानी आती है तो तुम्हारी माँ मुझसे लड़ने लगती है, जैसे परेशानी का कारण मैं ही हूँ।
शान्तिः इसलिए कि...
शालिनीः मम्मी !
बनारसीदासः अरे मैं कोई स्याहीसोख हूँ क्या स्याही किसी से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, सोखने के लिए उसे मुझ पर...
( आत्मलीन-सा अनिल, आकर सोफ़े के एक कोने में बैठ जाता है।)
शालिनीः मिला ?
अनिलः ( चौंककर शालिनी को देखता है। और फिर क्षण भर में उसका तात्पर्य समझकर हाँ ! मिल गया।
शान्तिः क्या बताया उन्होंने ?
अनिलः अभी तो नम्बर मिला है, मम्मी ! उनसे कहा है कि वे टाटा हॉस्पिटल से पता कर बताएँ।
शालिनीः सीधे अस्पताल को फोन करते तो क्या वे लोग इतनी-सी बात नहीं बता देते ?
अनिलः शायद बता देते...पर अस्पताल का नम्बर ?
शान्तिः तुम्हारे ऑफिस वाले कब बताएँगे, बेटा ?
शालिनीः कौन था लाइन पर ?
अनिलः बैनर्जी।
शालिनीः वही, जो पहले दिल्ली में था ?
अनिलः हाँ, वही ! अच्छा हुआ वह मिल गया। कई बार ढंग का कोई आदमी ही नहीं मिलता। इस देश में लोगों का आई. क्यू बहुत कम है और सिंसेयेरिटी तो है ही नहीं।
सन् 1982
( एक मध्यवर्गीय ड्राइंगरूम। सोफा, कुर्सियाँ और दीवान। आवश्यकतानुसार छोटी-बड़ी मेज़ें भी रखी जा सकती हैं। दीवार में एक खिड़की और एक अलमारी।
प्रकाश होने पर कमरे में बनारसीदास और शान्ति बैठे हैं। हाथ में एक पत्रिका लिए अनिल एक ओर खड़ा है, जैसे पढ़ रहा हो, किसी प्रतीक्षा में पत्रिका के पृष्ठ पलट रहा हो।
पत्रिका रख, वह धीरे-धीरे आकर, बनारसीदास के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। )
अनिलः तो क्या तय किया है। पापा, आपने ?
बनारसीदासः तय क्या करना है, बेटा ! मैं तो आ
ऑपरेशन के ही पक्ष में नहीं हूँ। जीवित शरीर की चीर-फाड़। मुझे डॉक्टर का यह हत्यारापन अच्छा नहीं लगता।
अनिलः तो आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर क्या करे ?
बनारसीदासः दवा दे। रोगी को दवा से अच्छा करना चाहिए। यह रक्तपात...
अनिलः पापा !
बनारसीदासः हाँ, बेटे।
अनिलः ऑपरेशन सम्बन्धी सैद्धान्तिक बहस हम फिर कर लेंगे। अपनी बात कहिए...आप अपना ऑपरेशन...
बनारसीदासः पचहत्तर वर्ष का हो गया। बहुत जी लिया। अब और क्या है, जिसके लिए मुझे जिलाए रखना चाहते हो ?
अनिलः आप से यह नहीं पूछा था मैंने !
बनारसीदासः अच्छा। मैंने समझा कि शायद यही पूछा था। (मुस्कराने लगता है। फिर उसके चेहरे से मुस्कान ग़ायब हो जाती है। व्यंग्य और प्रहार की मुद्रा अपनाकर) अपने स्कूली दिनों में मेरे साथ यही होता था। मास्टर कुछ पूछता था, और मैं कुछ और समझ बैठता था। परिणामतः सदा नालायक ही माना गया मैं। क्या पूछा था तुमने ?
अनिलः डॉ. मेहरा से ऑपरेशन का समय ले लूँ या आप मद्रास जाना चाहेंगे दीदी के पास डॉक्टर यहाँ अच्छा है और अस्पताल की सुविधाएँ, वहाँ अधिक हैं।
बनारसीदासः जब मैं ऑपरेशन ही नहीं कराना चाहता...
शान्तिः ओह-हो ! फिर वही हठ ! अरे, वह जो पूछ रहा है, उसका उत्तर दो।
बनारसीदासः पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर देना होगा ? अपनी बात नहीं कर सकता मैं ? घरेलू बातचीत में भी अब स्कूली परीक्षा का तौर-तरीका चलेगा क्या ?
शान्तिः हाँ ! अभी प्रश्न का ही उत्तर दीजिए। अपनी बात फिर कहते रहिएगा।
बनारसीदासः तभी तो कहता हूँ कि इस जीवन का क्या करना है मुझे, जिस पर मेरा अपना कोई अधिकार नहीं रहा।
शान्तिः क्यों ? आपके अधिकारों में कहाँ कटौती हो गई ?
बनारसीदासः अपनी बात नहीं कह सकता। अपने ढंग से नहीं कह सकता। (रूककर) मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा ही होगा।
शान्तिः क्यों ?
बनारसीदासः बोझ हूँ। दूसरों पर आश्रित हूँ। इस पराये जीवन के लिए ऑपरेशन का कष्ट मैं क्यों सहूँ ?
अनिलः पापा। बात को ग़लत दिशा में मत मोड़िए।...हम जब छोटे थे, तब हमारा जीवन अपना नहीं था। तब हमें पूछे गए प्रश्नों का ही उत्तर देना था। अपनी बात हम कह नहीं सकते थे। तब हमें मर जाना चाहिए था क्या ?
बनारसीदासः (चि़ड़चिड़ाहट के स्पष्ट लक्षणों को छिपाकर मुस्कराता है।) अब बात को उल्टी दिशा में तुम ले जा रहे हो। बच्चों को उनके माँ-बाप ही पालते हैं।
अनिलः तो बाद में माँ-बाप को बच्चे ही पालते हैं।
बनारसीदासः चलो, यही सही। पर अब मुझे ही अपना जीवन बोझ लगने लगा है।
शान्तिः इनकी तो आदत ही है, बेटा ! ऐसी बातें करने की। अपने बच्चे भी होते न औरों के बच्चों जैसे...
बनारसीदासः कैसे ?
शान्तिः वैसे, जैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं।...तब आपको भी पता लगता।
बनारसीदासः क्या कहना चाहती हो-तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं।
शान्तिः बेटे क्या और बेटियाँ क्या। सभी अच्छे हैं...जिसको देखो, वही बुला रहा है, सिर-आँखों पर बैठा रहा है-बेटा हो या दामाद।
बनारसीदासः इसलिए तो मैं कहता हूँ, अधिक सन्तान लाभदायक होती हैं। जाने क्यों लोग हाथ धोकर परिवार नियोजन के पीछे पड़े हैं। सब कुछ है देश में। बताओ क्या नहीं है ? (शान्ति की ओर देखकर ) पर तुम क्या बताओगी, तुम्हे तो यह भी पता नहीं होता कि घर में क्या है और क्या नहीं होता।
शान्तिः मैं तो हूँ ही मूर्ख। आप अपनी बात कीजिए।
बनारसीदासः अपनी बात ही कह रहा हूँ। एक ही बेटा होता न हमारा भी तो तुम बहू के बर्तन धो रही होतीं। मैं उनके बच्चों को स्कूल पहुँचाने जाता और भोगल से सब्ज़ी ख़रीदता हुआ, थका-हारा लड़खड़ाता हुआ घर आता।
अनिलः पापा !
बनारसीदासः हाँ, बेटे ! यह तो अधिक बच्चों का ही लाभ है कि इशारा पाया और हमने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा।
अनिलः पापा ! आप तो फै़मिली प्लानिंग वालों का ऑपरेशन करने लगे।...मैं पूछ रहा था, आपका वह ऑपरेशन...
(नेपथ्य में घण्टी बजती है।)
शान्तिः देखूं तो कौन आया है। (उठने लगती है।)
अनिलः आप बैठी रहिए। शालिनी देख लेगी। नहीं तो मैं देखता हूँ। (उठते-उठते फिर बैठ जाता है।)...शालिनी गई है शायद।
शान्तिः वासन्ती की कोई चिठ्टी नहीं आई ? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
अनिलः अरे मम्मी ! जिसके पास सबसे ज्यादा नौकर-चाकर हों, उसी का आपको भी ध्यान रहता है। वासन्ती तो पापा को बुला रही है, ऑपरेशन के लिए। और आप उसके लिए ही चिन्तित हैं। उसे क्या कमी है !...
शान्तिः उसे कमी है अकल की; नहीं तो इतने नौकरों की क्या आवश्यकता है !
अनिलः सम्भव है, अधिक सन्तान के समान, अधिक नौकरों का भी कोई लाभ हो- जिसे वही जानती हो।
शान्तिः जैसे कोई काम एक न करे, तो दूसरा कर दे।
बनारसीदासः क्या मूर्खता है ! नौकर और बच्चे एक हैं क्या !
अनिलः बच्चे यदि अपने स्वार्थ के लिए पैदा किए जाएँ, तो फिर तो एक ही हैं।
(शालिनी आती है।)
अनिलः गया ? कौन था ?
शालिनीः (लिफाफा अनिल की ओर बढ़ा देती है।) तार !
बनारसीदासः अरे तार ! किसका है ? (उठने का उपक्रम करके रह जाता है।) कौन आ रहा है ?
(अनिल बढ़कर तार ले लेता है।)
शान्तिः तार क्या केवल किसी के आने का ही होता है ?
बनारसीदासः और क्या लाटरी खुलने का होता है ! इतनी ही भाग्यशालिनी होतीं तुम...
अनिलः (लिफ़ाफ़ा खोलकर, बिना सोचे-समझे, अभ्यासवश पढ़ जाता है।) ‘रमेश सीरियस। कम इमीडिएटली।’
शान्तिः (बनारसी के चेहरे को गम्भीर और चिन्तित होते देखती जाती है) क्या हुआ ? रमेश आ रहा है क्या ? (कोई कुछ नहीं कहता। उन तीनों की गम्भीरता देखकर शान्ति चिन्तित हो उठती है।)...यह मुँह-झौंसी अंग्रेजी़ ! अंग्रेज़ कब के चले गए, पर तार आज भी अंग्रेज़ी में ही आएगा...(उत्तेजना में उठना चाहती है।)
अनिलः ( जल्दी से शान्ति के पास पहुँचकर, कन्धों से पकड़कर उसे बैठाता है। हल्के से थपथपाता है।) कुछ नहीं, मम्मी ! आप बैठिए।...रमेश बीमार है शायद।
बनारसीदासः (जड़ मुद्रा क्रमशः सजीव होती है।) किसने दिया है तार ?
अनिलः कोई श्रीराम खन्ना है। (चेहरे पर खीझ और परेशानी स्पष्ट हो जाती है।) जाने कौन है ! कोई है भी, या किसी ने यूँ ही तार दे दिया हमें परेशान करने को।
शालिनीः ऐले ही कोई क्यों दे देगा ? क्या मिलेगा किसी को ?
अनिलः मिलता है, कुछ लोगों को।
बनारसीदासः अरे, कोई रोड एक्सिडेण्ट तो नहीं।...बम्बई की गाड़ियाँ भी...कहीं गाड़ी से चढ़ते- उतरते...
शान्तिः क्या गाड़ी से गिर पड़ा है ?
बनारसीदासः किसने कह दिया तुमसे कि गाड़ी से गिर पड़ा है। मूर्खों के समान...
अनिलः ओह हो पापा ! आप भी...
शालिनीः बम्बई फोन करके नहीं पूछा जा सकता ?
बनारसीदासः हाँ ! अगर फोन करके...
अनिलः हाँ ! हो सकता है।...अपनी कम्पनी के बम्बई ऑफिस में फोन करूँ तो...
बनारसीदासः वह है कहाँ ? घर में, अस्पताल में ?...
अनिलः अस्पताल में है। लिखा है न ‘टाटा हॉस्पिटल’।
बनारसीदासः लिखा है, पर तुमने पढ़ा तो नहीं।
शान्तिः (खीझकर) पढ़ा नहीं जाए तो लिखा हुआ मिट तो नहीं जाता।
अनिलः अच्छा ! मैं फोन करके देखता हूँ।
(अनिल भीतर चला जाता है। शालिनी आकर अनिल द्वारा खा़ली की गयी कुर्सी पर थकी-सी बैठ जाती है।)
शान्तिः तुम क्या सोचती हो, शालिनी ? वह बीमार होगा या...
शालिनीः (स्वयं को सम्भालती है।) मैं क्या कहूँ, मम्मी ! लिखा तो कुछ भी नहीं ही है। रमेश ने कभी-भी तो अपना ध्यान नहीं रखा...सदा का लापरवाह...
बनारसीदासः कहीं किसी से झगड़ा न किया हो। बम्बई में...
शालिनीः ( शान्ति के चिन्तित होते हुए चेहरे को देखती है और फिर पलटकर बनासीदास को) पापा ! आप सारी अनहोनी बातें कह-कहकर खुद भी परेशान होंगे, हमें भी करेंगे...
शान्तिः अभी क्या है, अभी तो ये एक-से-एक भयंकर बीमारियों का नाम ले-लेकर मुझे डराएँगे, तड़पाएँगे। ये तो चाहेंगे ही कि मेरी नींद हराम हो जाए और मैं रातभर बिस्तर पर करवटें बदलती रहूँ...
बनारसीदासः तुम सो नहीं पाओगी, तो मैं सो पाऊँगा क्या ? बेकार बोलती चली जाएगी। एक बार छिड़ पड़े तो थमने पर ही नहीं आती। (शालिनी की ओर देखकर) बेटा है मेरा। मुझे चिन्ता नहीं होगी ?...
शान्तिः मालूम है मुझे !...चिन्ता होगी कोई और बड़ी बीमारी क्यों न हुई उसे। अपना एक ऑपरेशन नहीं करवा सकते। उसके लिए दुनिया-भर के रोगों का नाम ले-लेकर मेरा दिल जलाओगे...
बनारसीदासः क्यों ? मेरा बेटा नहीं है वह ?
शान्तिः बेटा...(उसकी आँखों में एक खूँखार भाव उभरता है। बनारसीदास उसका सामना नहीं कर सकता। मुँह दूसरी ओर फेर लेता है।) जब वह आठवीं में फेल हुआ था...
शालिनीः (अचकचाकर शान्ति और बनारसीदास को देखती है।) पता नहीं उन्हें बम्बई की लाइन मिली या नहीं...
बनारसीदासः ( जैसे अपनी घुटन से छुटकारा पाने के लिए झरोखा मिल गया हो।) इतनी जल्दी कहाँ मिली होगी ! दिल्ली का एक नम्बर मिलने में तो घण्टा लग जाता है, बम्बई तक का नम्बर...
शालिनीः वैसे भी दिल्ली और बम्बई, दोनों ही बहुत बिज़ी एक्चेंज हैं। फिर दिन का समय...बिज़नेस वाले...
बनारसीदासः काम-धाम का बोझ तो समझ में आता है, पर...यहाँ तो एक्चेंज क्या, केबल्स क्या, आदमी क्या-सब कुछ ही सड़ा हुआ है। व्यवस्था ही सड़ रही है...
शान्तिः ( अँगुलियों से अपने माथे को दबाते हुए ) सड़ तो मेरा सिर रहा है...
बनारसीदासः कहता हूँ चिन्ता मत किया करो।... पर तुम क्यों मानोगी। तुम तो चाहोगी कि तुम्हारे सिर में दर्द हो और तुम मुझे परेशान करो। मैं डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर काटूँ ?
शान्तिः कब-कब काटे आपने डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर ?
बनारसीदासः नहीं काटे ?
शान्तिः अब मुँह मत खुलवाइए। जब तक स्वस्थ रही, आपकी रही। बीमार होते ही मायकेवालों के गले मढ़ देते थे आप !
बनारसीदासः और तो कुछ बस का है नहीं तुम्हारे। चिन्ता पड़ते ही मुझसे लड़ने लगती हो।
शालिनीः चलिए, मम्मी ! भीतर चलकर लेट जाइए। बैठे-बैठे वैसे भी थक गयी होंगी।
शान्तिः नहीं ! ठीक हूँ मैं । अभी नहीं लेटूँगी।
बनारसीदासः लेटकर भी चिन्ता की जा सकती है। लेटने से सिर-दर्द रूक नहीं जाएगा तुम्हारा...
शान्तिः आपकी जुबान भी नहीं रूकेगी !
शालिनीः (उठकर शान्ति के पास आती है) चलिए, मम्मी ! यहीं दीवान पर लेट जाइए। कुछ आराम मिलेगा।
शान्तिः नहीं ! मैं ठीक हूँ। अनिल को आ लेने दो। जाने वह क्या ख़बर लाता है !
बनारसीदासः तुम्हारे तनकर बैठे रहने से, ख़बर तुम से डरकर कुछ और नहीं हो जाएगी...
शालिनीः पापा ! (शान्ति के कन्धे पकड़कर) लेट जाइए मम्मी ! जो ख़बर आयगी, आपके सामने आयगी।
(शान्ति के विरोध को अनदेखा कर शालिनी उसे बाँह से पकड़कर उठाती है। शान्ति इच्छा-अनिच्छा के बीच, उठकर दीवान तक आती है। शान्ति के लेटने के बाद शालिनी उसका सिर उठाकर उसके नीचे गद्दी रख देती है। दो-तीन बार अपनी हथेलियों से उसका सिर दबाती भी है।)
शान्तिः नहीं ! रहने दे। ( हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। क्षण भर रूककर ) तू मेरा सिर दबाएगी, तो तेरे पापा मेरा गला दबा देंगे।
बनारसीदासः इसी से तो तुम्हारी जीभ मुँह से इतनी बाहर निकल आयी है।
शालिनीः पापा ! ( दीवान पायताने पड़ी चादर उठा, शान्ति को ओढ़ा देती है और लौटकर अपने स्थान पर आ जाती है।)
बनारसीदीसः बेटी ! तुम समझती होगी कि मैं बहुत झक्की हो गया हूँ।...
शालिनीः नहीं, पापा !
बनारसीदासः नहीं-नहीं ! थोड़ा बहुत हो भी गया हूँ।...पर कोई परेशानी आती है तो तुम्हारी माँ मुझसे लड़ने लगती है, जैसे परेशानी का कारण मैं ही हूँ।
शान्तिः इसलिए कि...
शालिनीः मम्मी !
बनारसीदासः अरे मैं कोई स्याहीसोख हूँ क्या स्याही किसी से भी गिरे, कहीं से भी गिरे, सोखने के लिए उसे मुझ पर...
( आत्मलीन-सा अनिल, आकर सोफ़े के एक कोने में बैठ जाता है।)
शालिनीः मिला ?
अनिलः ( चौंककर शालिनी को देखता है। और फिर क्षण भर में उसका तात्पर्य समझकर हाँ ! मिल गया।
शान्तिः क्या बताया उन्होंने ?
अनिलः अभी तो नम्बर मिला है, मम्मी ! उनसे कहा है कि वे टाटा हॉस्पिटल से पता कर बताएँ।
शालिनीः सीधे अस्पताल को फोन करते तो क्या वे लोग इतनी-सी बात नहीं बता देते ?
अनिलः शायद बता देते...पर अस्पताल का नम्बर ?
शान्तिः तुम्हारे ऑफिस वाले कब बताएँगे, बेटा ?
शालिनीः कौन था लाइन पर ?
अनिलः बैनर्जी।
शालिनीः वही, जो पहले दिल्ली में था ?
अनिलः हाँ, वही ! अच्छा हुआ वह मिल गया। कई बार ढंग का कोई आदमी ही नहीं मिलता। इस देश में लोगों का आई. क्यू बहुत कम है और सिंसेयेरिटी तो है ही नहीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book