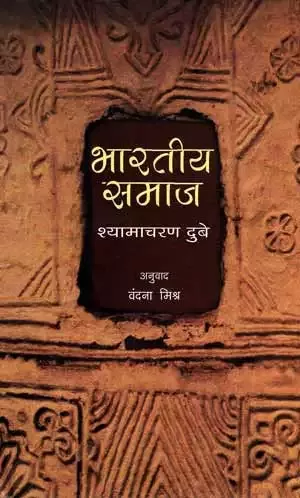|
संस्कृति >> भारतीय समाज भारतीय समाजश्यामाचरण दुबे
|
156 पाठक हैं |
|||||||
भारतीय विविधता और एकता के विकास की इसके जटिल इतिहास के माध्यम से खोज...
Bhartiya Samaj a hindi book by Shyamacharan Dubey - भारतीय समाज - श्यामाचरण दुबे
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मुख्य रूप से युवा पाठकों को संबोधित इस पुस्तक में विभिन्न स्रत्रों द्वारा भारतीय समाज के भूत और वर्तमान को निकट से देखने का प्रयास किया गया है। भारतीय विविधता और एकता के विकास को इसके जटिल इतिहास के माध्यम से खोजा गया है। सदियों से वर्ण, जाति, परिवार और नातेदारी की क्रियाशीलता का नगरीकरण एवं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है। आज के भारत का लेखा-जोखा देने के साथ ही पुस्तक में वर्तमान में हो रहे और भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तन की भी समीक्षा प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में, यह पुस्तक भारतीय समाज का एक प्रामाणिक दस्तावेज है।
प्रो. श्यामचरण दुबे, जिनका सन् 1996 आरंभ में निधन हुआ एक प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक थे। सन् 1955 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘इंडियन विलेज’ भारतीय समाज के अध्ययन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर थी। प्रो. दुबे ने देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में मानवविज्ञान और समाजविज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन उनका हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण लेखन मात्र सामाजिक विकास तक संकुचित नहीं है।
इस पुस्तक की अनुवादिका वंदना मिश्र पेशे से पत्रकार होने के साथ-साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी एक विश्वसनीय नाम है।
प्रो. श्यामचरण दुबे, जिनका सन् 1996 आरंभ में निधन हुआ एक प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक थे। सन् 1955 में पहली बार प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘इंडियन विलेज’ भारतीय समाज के अध्ययन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर थी। प्रो. दुबे ने देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में मानवविज्ञान और समाजविज्ञान का अध्ययन किया। लेकिन उनका हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण लेखन मात्र सामाजिक विकास तक संकुचित नहीं है।
इस पुस्तक की अनुवादिका वंदना मिश्र पेशे से पत्रकार होने के साथ-साथ अनुवाद के क्षेत्र में भी एक विश्वसनीय नाम है।
प्राक्कथन
यह पुस्तक उन युवा पाठकों को संबोधित है जो भारतीय समाज ऐतिहासिक जड़ों इसके विचारधारात्मक आधारों तथा सामाजिक संगठन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। अंतिम अध्याय में परिवर्तन की प्रमुख प्रवृत्तियों पर भी चर्चा की गयी है। आंकड़ों और व्याख्याओं के लिए इतिहास, भारतविद्या, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र जैसे विविध स्त्रोतों का सहारा लिया गया है। इन विषयों से प्राप्त अंतर्दृष्टियां, मेरे विचार से, भारत के सामाजिक यथार्थ पर प्रकाश डालने के लिए आवश्यक हैं।
भारत का एक सुदीर्घ इतिहास है और उसकी सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। इसके बहुरंगी संरूपों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करना आसान नहीं। इतनी छोटी पुस्तक में स्थानीय तथा क्षेत्रीय रीति-रिवाजों तथा सामाजिक रूपों के सूक्ष्म विवरणों पर चर्चा कर पाना तो स्पष्टतः असंभव है। फिर भी इसके कुछ उन विविधताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। एकीकरण के पक्षों की भी पड़ताल की गयी है। आशा है कि पुस्तक अपने पाठकों को न भ्रमित करेगी और न उन्हें चकरायेगी।
दो शब्द भाषा के विषय में। दशकों के दौरान समाजशास्त्र ने एक ऐसी दुहरू शब्दावली विकसित की है जो विषय का विशेष ज्ञान न रखने वाले मेधावी पाठकों को भी परेशान करती है। इस पुस्तक में एक सरल-शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है किंतु ऐसे शब्दों को, जहाँ वे पहली बार आये हैं, वहां अथवा शब्दावली में स्पष्ट कर दिया गया है।
कुछ हद तक सभी इतिहास तथा समाजशास्त्र पुनर्रचनाएं ही हैं और इनमें सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ लेखकों के भी विचारधारात्मक आग्रह प्रतिबिंबित होते हैं। संभव है इस पुस्तक में भी आत्मनिष्ठ झुकाव आ गये हो किंतु किसी विचारधारा विशेष के पक्षों में मैंने तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं है। अंत में एक संक्षिप्त पुस्तक सूची दी गयी है ताकि पाठक ऐसे दृष्टिकोणों से भी परिचित हो सकें जो संभवतः मेरे दृष्टिकोण से भिन्न हों।
ज्ञान के प्रमुख प्रकार्यों में से एक है मानसिक क्षितिज का विस्तार करना और यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गयी है। आशा है कि इससे भारत के सामाजिक व्यक्तित्व के विषय में कुछ आलोचनात्मक जागरुकता उत्पन्न होगी तथा हमारे देश के अतीत और वर्तमान के बारे में चिंतन की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास तथा परंपराओं को कभी-कभी बेहतर ढंग से समझा जाता है जब उन पर से रहस्य का आवरण हटा दिया जाता है।
इस पुस्तक पर सावधानीपूर्ण तथा रचनात्मक संपादकीय परामर्श के लिए मैं श्री रवि दलाल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
भारत का एक सुदीर्घ इतिहास है और उसकी सामाजिक संरचना बहुत जटिल है। इसके बहुरंगी संरूपों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करना आसान नहीं। इतनी छोटी पुस्तक में स्थानीय तथा क्षेत्रीय रीति-रिवाजों तथा सामाजिक रूपों के सूक्ष्म विवरणों पर चर्चा कर पाना तो स्पष्टतः असंभव है। फिर भी इसके कुछ उन विविधताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। एकीकरण के पक्षों की भी पड़ताल की गयी है। आशा है कि पुस्तक अपने पाठकों को न भ्रमित करेगी और न उन्हें चकरायेगी।
दो शब्द भाषा के विषय में। दशकों के दौरान समाजशास्त्र ने एक ऐसी दुहरू शब्दावली विकसित की है जो विषय का विशेष ज्ञान न रखने वाले मेधावी पाठकों को भी परेशान करती है। इस पुस्तक में एक सरल-शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है किंतु ऐसे शब्दों को, जहाँ वे पहली बार आये हैं, वहां अथवा शब्दावली में स्पष्ट कर दिया गया है।
कुछ हद तक सभी इतिहास तथा समाजशास्त्र पुनर्रचनाएं ही हैं और इनमें सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ लेखकों के भी विचारधारात्मक आग्रह प्रतिबिंबित होते हैं। संभव है इस पुस्तक में भी आत्मनिष्ठ झुकाव आ गये हो किंतु किसी विचारधारा विशेष के पक्षों में मैंने तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं है। अंत में एक संक्षिप्त पुस्तक सूची दी गयी है ताकि पाठक ऐसे दृष्टिकोणों से भी परिचित हो सकें जो संभवतः मेरे दृष्टिकोण से भिन्न हों।
ज्ञान के प्रमुख प्रकार्यों में से एक है मानसिक क्षितिज का विस्तार करना और यह पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गयी है। आशा है कि इससे भारत के सामाजिक व्यक्तित्व के विषय में कुछ आलोचनात्मक जागरुकता उत्पन्न होगी तथा हमारे देश के अतीत और वर्तमान के बारे में चिंतन की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास तथा परंपराओं को कभी-कभी बेहतर ढंग से समझा जाता है जब उन पर से रहस्य का आवरण हटा दिया जाता है।
इस पुस्तक पर सावधानीपूर्ण तथा रचनात्मक संपादकीय परामर्श के लिए मैं श्री रवि दलाल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
दिल्ली
जुलाई 1990
जुलाई 1990
-श्यामाचरण दुबे
1
भारतीय समाज का निर्माण
भारतीय समाज बहुत पुराना और अत्यधिक जटिल है। प्रचलित अनुमान के अनुसार पांच हजार वर्ष पूर्व की पहली ज्ञात सभ्यता के समय से आज तक लगभग पांच हजार वर्षों की अवधि इस समाज में समाहित है। इस लंबी अवधि में विभिन्न प्रजातिय लक्षणों वाले और विविध भाषा-परिवारों के आप्रवासियों की कई लहरें यहां आकर इसकी आबादी में घुल मिल गयीं और इसे समाज की विविधता, समृद्धि और जीवंतता में अपना-अपना योगदान दिया।
समकालीन भारत में सामाजिक क्रमविकास के कई अलग-अलग स्तर साथ-साथ मौजूद हैं जैसे आदिकालीन शिकारी और भोजन संग्राहक, झूम खेती करने वाले किसान जो हल-बैल से जुताई करने के बजाय आज भी कुदाली या आद्य हल का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के घुमंतू (बकरी-भेड़ और मवेशी पालक एक जगह से दूसरी जगह घूम-घूमकर व्यापार करने वाले और कारीगर तथा शिल्पी), एक ही जगह बसे किसान जो खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते हैं, दस्तकार और प्राचीन वंश परंपरा वाले हल का इस्तेमाल करते हैं, दस्तकार और प्राचीन वंश परंपरा वाले भूस्वामी तथा अभिजात वर्ग। दुनिया के अधिकतर प्रमुख धर्म-हिंदू, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध-यहां हैं और इनके साथ आस्था और कर्मकांड की दृष्टि से इतने अलग-अलग ढंग के संप्रदाय और पंथ भी यहां हैं जो विस्मय में डाल देते हैं। इन सबके साथ आधुनिक अकादमी अफसरशाही, औद्योगिक और वैग्यानिक अभिजन को भी जोड़ देने से हम देखते हैं कि यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों साथ-साथ रह रहे हैं। अपने क्रमविकास की प्रक्रिया में भारतीय समाज ने एक मिली-जुली संस्कृति विकसित की है जिसकी जानकारी विशेषता है बहुलवाद के कुछ स्थायी संरूप (पैटर्न)।
भारत के प्राचीनतम निवासियों की पहचान कर पाना कठिन है। आश्चर्य नहीं कि उनके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उस समय लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लोगों की मौखिक परंपरा से कोई खास मदद नहीं मिलती क्योंकि बाद में उसमें होने वाले जोड़-घटाव इस मौखिक परंपरा को इतिहास के मार्गदर्शन के रूप में भरोसेमंद नहीं रहने देते। प्रागैतिहासिक साक्ष्य अधिक भरोसेमंद हैं हालांकि इनसे पूरी कहानी नहीं जानी जा सकती। जीवन के तमाम छोटे-छोटे सूक्ष्म विवरण समय के थपेड़ों में खो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक मानव-गतिविधियां दूसरे अंतर-हिमानी युग में 400, 000 और 200,000 ई. पू. के बीच शुरू हो चुकी थी उस समय पत्थरों से बने उपकरण इस्तेमाल किये जाते थे।
देश के विभिन्न भागों में मिले गुफा चित्रों में उस प्रारंभिक काल के जीवन और पर्यावरण, कलात्मक अनुभूतियों और रचनात्मकता तथा संभवतः उस आदिकाल के आध्यात्मक विचारों को भी अभिव्यक्ति मिली हैं विशेषकर प्रायद्वीप भारत में मिलने वाले-महापाषाण (मेगालिथ्स) विशाल पत्थर जो अधिकतर मृतकों के स्मारक के रूप में इस्तेमाल किये गये थे-लोहे कांसे यहां तक कि सोने के भी प्रयोगों को दर्शाते हैं। नया पुरातत्व शास्त्र इन सब बातों पर तो अतिरिक्त जानकारी देने का काम शुरू कर रहा है कि लोग कैसे रहते थे, कौन-कौन सी फसले उगाते थे और क्या खाते-पीते थे, लेकिन वह यह नहीं बताता कि यहां सबसे पहले कौन आया और अन्य लोगों ने किस प्रकार क्रम में इस भूमि पर प्रवेश किया।
भारत की जनसंख्या के नृजातीत (एथनिक) तत्त्वों अर्थात प्रजातीय समूहों के संबंध में भौतिक मानवशास्त्र द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते है कि भारत के स्वस्थानिक आदिवासी-मूल या प्राचीनतम निवासी-कौन थे। इस विषय में बी. एस. गुहा द्वारा किया गया है वर्गीकरण सर्वाधिक आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। बी.ए. गुहा ने भारत की जनसंख्या में छह मुख्य प्रजातीय तत्त्वों की पहचान की हैः नेग्रीटो, प्रोटो-आस्ट्रलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागर (मेडीटरेनियन), पश्चिमी लघुशिरस्क (वेसेटर्न ब्रैसिसिफल) तथा नोर्डिक। इसमें से प्रथम तीन इस उपमहाद्वीप के पुराने निवासी हैं। वे छोटे-छोटे क्षेत्रों के भीतर ही सीमित हैं। दक्षिण में काडर, इरुला तथा पानियान और अंडमान द्वीपसमूह में ओंग और अंडमानियों में निश्चित नेग्रीटो विशेषताएं स्पष्ट हैं। इस समूह की कुछ विशेषताएं अंगीमी नागाओं तथा राजमहलों पहाड़ियों के बागड़ियों में पायी जाती हैं। पश्चिमी पट पर कुछ समूह ऐसे हैं जिनमें नेग्रीटो लक्षण बहुत स्पष्ट हैं लेकिन वे संभवतः बाद में यहाँ आने वाले उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं
समकालीन भारत में सामाजिक क्रमविकास के कई अलग-अलग स्तर साथ-साथ मौजूद हैं जैसे आदिकालीन शिकारी और भोजन संग्राहक, झूम खेती करने वाले किसान जो हल-बैल से जुताई करने के बजाय आज भी कुदाली या आद्य हल का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के घुमंतू (बकरी-भेड़ और मवेशी पालक एक जगह से दूसरी जगह घूम-घूमकर व्यापार करने वाले और कारीगर तथा शिल्पी), एक ही जगह बसे किसान जो खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते हैं, दस्तकार और प्राचीन वंश परंपरा वाले हल का इस्तेमाल करते हैं, दस्तकार और प्राचीन वंश परंपरा वाले भूस्वामी तथा अभिजात वर्ग। दुनिया के अधिकतर प्रमुख धर्म-हिंदू, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध-यहां हैं और इनके साथ आस्था और कर्मकांड की दृष्टि से इतने अलग-अलग ढंग के संप्रदाय और पंथ भी यहां हैं जो विस्मय में डाल देते हैं। इन सबके साथ आधुनिक अकादमी अफसरशाही, औद्योगिक और वैग्यानिक अभिजन को भी जोड़ देने से हम देखते हैं कि यहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों साथ-साथ रह रहे हैं। अपने क्रमविकास की प्रक्रिया में भारतीय समाज ने एक मिली-जुली संस्कृति विकसित की है जिसकी जानकारी विशेषता है बहुलवाद के कुछ स्थायी संरूप (पैटर्न)।
भारत के प्राचीनतम निवासियों की पहचान कर पाना कठिन है। आश्चर्य नहीं कि उनके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उस समय लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लोगों की मौखिक परंपरा से कोई खास मदद नहीं मिलती क्योंकि बाद में उसमें होने वाले जोड़-घटाव इस मौखिक परंपरा को इतिहास के मार्गदर्शन के रूप में भरोसेमंद नहीं रहने देते। प्रागैतिहासिक साक्ष्य अधिक भरोसेमंद हैं हालांकि इनसे पूरी कहानी नहीं जानी जा सकती। जीवन के तमाम छोटे-छोटे सूक्ष्म विवरण समय के थपेड़ों में खो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक मानव-गतिविधियां दूसरे अंतर-हिमानी युग में 400, 000 और 200,000 ई. पू. के बीच शुरू हो चुकी थी उस समय पत्थरों से बने उपकरण इस्तेमाल किये जाते थे।
देश के विभिन्न भागों में मिले गुफा चित्रों में उस प्रारंभिक काल के जीवन और पर्यावरण, कलात्मक अनुभूतियों और रचनात्मकता तथा संभवतः उस आदिकाल के आध्यात्मक विचारों को भी अभिव्यक्ति मिली हैं विशेषकर प्रायद्वीप भारत में मिलने वाले-महापाषाण (मेगालिथ्स) विशाल पत्थर जो अधिकतर मृतकों के स्मारक के रूप में इस्तेमाल किये गये थे-लोहे कांसे यहां तक कि सोने के भी प्रयोगों को दर्शाते हैं। नया पुरातत्व शास्त्र इन सब बातों पर तो अतिरिक्त जानकारी देने का काम शुरू कर रहा है कि लोग कैसे रहते थे, कौन-कौन सी फसले उगाते थे और क्या खाते-पीते थे, लेकिन वह यह नहीं बताता कि यहां सबसे पहले कौन आया और अन्य लोगों ने किस प्रकार क्रम में इस भूमि पर प्रवेश किया।
भारत की जनसंख्या के नृजातीत (एथनिक) तत्त्वों अर्थात प्रजातीय समूहों के संबंध में भौतिक मानवशास्त्र द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते है कि भारत के स्वस्थानिक आदिवासी-मूल या प्राचीनतम निवासी-कौन थे। इस विषय में बी. एस. गुहा द्वारा किया गया है वर्गीकरण सर्वाधिक आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप में मान्यता प्राप्त है। बी.ए. गुहा ने भारत की जनसंख्या में छह मुख्य प्रजातीय तत्त्वों की पहचान की हैः नेग्रीटो, प्रोटो-आस्ट्रलायड, मंगोलायड, भूमध्यसागर (मेडीटरेनियन), पश्चिमी लघुशिरस्क (वेसेटर्न ब्रैसिसिफल) तथा नोर्डिक। इसमें से प्रथम तीन इस उपमहाद्वीप के पुराने निवासी हैं। वे छोटे-छोटे क्षेत्रों के भीतर ही सीमित हैं। दक्षिण में काडर, इरुला तथा पानियान और अंडमान द्वीपसमूह में ओंग और अंडमानियों में निश्चित नेग्रीटो विशेषताएं स्पष्ट हैं। इस समूह की कुछ विशेषताएं अंगीमी नागाओं तथा राजमहलों पहाड़ियों के बागड़ियों में पायी जाती हैं। पश्चिमी पट पर कुछ समूह ऐसे हैं जिनमें नेग्रीटो लक्षण बहुत स्पष्ट हैं लेकिन वे संभवतः बाद में यहाँ आने वाले उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book