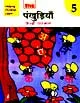|
भाषा एवं साहित्य >> हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहासमधु धवन
|
448 पाठक हैं |
||||||
इस पुस्तक में हिन्दी साहित्य के इतिहास को दर्शाया गया है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
"काशी नगरी प्रचारिणी सभा" की स्थापना द्विवेदी युग के उत्थान की संदेश
वाहिका है। इस सभा की स्थापना के कतिपय वर्षों के बाद ही "सरस्वती"
पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका सम्पादन आचार्य महावीरप्रसाद दिवेदी के
करकमलों से सम्पन्न हुआ। द्विवेदी जी ने इस उत्थान को जहाँ एक ओर अपनी
आलोचना की कूंची से स्वच्छ किया, वहीं दूसरी ओर गद्य-पद्य की नवीनतम
विद्याओं को प्रश्रय देकर हिन्दी साहित्य के मार्ग को व्यापक बनाया।
भारतेन्दु का काल गद्य का प्रयोग काल होने के कारण स्वच्छन्दता का युग था। उसमें शुद्धता का अभाव था। इस अभाव की ओर सबसे पहले आचार्य द्विवेदी जी का ध्यान गया। उन्होंने अशुद्ध भाषा लिखने वाले लेखकों की कटु आलोचना कर उन्हें शुद्ध भाषा लिखने को प्रेरित किया।
भक्तिकाल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। शुक्ल जी ने इस काल के समग्र साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत यह पाया कि इस काल का अधिकतर साहित्य भक्ति-रस से ओत-प्रोत है। अतः उन्होंने इसे भक्तिकाल कहना उचित समझा।
साहित्य, सामाजिक भावनाओं की परम्परागत धारा को, अपनी आधारशिला के रूप में ग्रहण करता है। सिद्धों, हठयोगियों और नाथपंथियों की यौगिक साधनाओं की जो परम्परा चली आ रही थी, कापालिक की जो जमघट लगी हुई थी, वह अपने रहस्यों, दुराचारों और गुप्त साधनाओं तथा भैरवीचक्रों के दूषित वातावरण की अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर गई; जिसको रोकना बहुत आवश्यक था।
भारतेन्दु का काल गद्य का प्रयोग काल होने के कारण स्वच्छन्दता का युग था। उसमें शुद्धता का अभाव था। इस अभाव की ओर सबसे पहले आचार्य द्विवेदी जी का ध्यान गया। उन्होंने अशुद्ध भाषा लिखने वाले लेखकों की कटु आलोचना कर उन्हें शुद्ध भाषा लिखने को प्रेरित किया।
भक्तिकाल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। शुक्ल जी ने इस काल के समग्र साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत यह पाया कि इस काल का अधिकतर साहित्य भक्ति-रस से ओत-प्रोत है। अतः उन्होंने इसे भक्तिकाल कहना उचित समझा।
साहित्य, सामाजिक भावनाओं की परम्परागत धारा को, अपनी आधारशिला के रूप में ग्रहण करता है। सिद्धों, हठयोगियों और नाथपंथियों की यौगिक साधनाओं की जो परम्परा चली आ रही थी, कापालिक की जो जमघट लगी हुई थी, वह अपने रहस्यों, दुराचारों और गुप्त साधनाओं तथा भैरवीचक्रों के दूषित वातावरण की अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर गई; जिसको रोकना बहुत आवश्यक था।
प्रस्तावना
सम्पूर्ण देश में हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास-विस्तार में विश्वविद्यालयों
की महती भूमिका है। जिस प्रकार सम्पूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन
बड़े-बड़े कारखानों में होता है, उसी प्रकार देश का बहुआयामी निर्माण देश
की शिक्षा संस्थानों में होता है।
स्वतन्त्रता के उपरांत विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना जोर-शोर से शुरू हुई। मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग सन् 1954 में खुला, जो हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन तथा शोध कार्य हितार्थ निरन्तर सक्रिय रहा। इस विभाग में प्रथम आचार्य शंकरराजू नायडू थे, जिन्होंने कम्ब रामायण और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। तिरुकुरल का हिन्दी में अनुवाद किया। उनके उपरांत एस.एन. गणशेन् आए जिन्होंने 1975 में हिन्दी और तमिल व्याकरण लिखा तथा सुब्रह्मण्य भारती की कविताओं का 1986 में तथा मणिमेखलै में 1990 में अनुवाद किया। उनके उपरांत डॉ. टी.एस. कुप्पुस्वामी आये जिनकी कृति ‘हिन्दी रीतिकाव्य’ 1990 में प्रकाशित हुई तथा विभाग की अन्य प्राध्यापिका डॉ. शारदा रमणी की कृति भारतेन्दु के गीतों में राष्ट्रीय चेतना 1990, संघम काल में नारी, 1992 में छपी।
सम्प्रति डॉ. सैयद रहमतुल्ला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने विभाग में कई चुनौती पूर्ण कार्य कर हिन्दी विभाग को प्रतिष्ठा प्रदान की है। सबसे पहले स्कूलों के अध्यापकों को एक साथ जोड़कर उन्हें मार्गदर्शन देते हुए पाठयक्रमों का चयन करवाया। कॉलेजों के पाठ्यक्रम में समयानुकूल बदलाव लाकर उसे बदलाव के अन्तर्गत लिखी गई कृति है। यह पुस्तक ‘हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास’ उसी बदलाव के अन्तर्गत लिखी गई कृति है। डॉ. सैयद रहमतुल्ला चाहते हैं कि हिन्दी पढ़ने वाला छात्र साहित्य का ज्ञानवर्द्धन करें, इसलिए पुस्तक में जहाँ सरल भाषा का प्रयोग किया गया है वहाँ इस बात पर भी विशेष ध्यान रखा गया है कि छात्र का स्तर संवृद्ध की ओर अग्रसर रहे।
यूँ तो कई विद्वानों ने पाठ्यक्रम हेतु ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ लिखा है लेकिन अक्सर यह पाया गया है कि या तो बहुत सरल है, स्तरीय नहीं है या फिर क्लिष्ट है। अत: इस तथ्य को मद्देनजर रखकर डॉ. सैयद रहमतुल्ला के मार्गदर्शन में यह ‘हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास’ लिखा गया है। इसमें नौवें दशक के बाद के साहित्य तथा साहित्यकार का परिचय देने का प्रयास किया गया है जिससे छात्र लाभान्वित हों।
सहर्ष कहा जाता है कि मद्रास में हिन्दी की साख बढ़ाने का श्रेय डॉ. सैयद रहमतुल्ला जी को जाता है क्योंकि विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन होते ही उन्होंने समस्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के सम्मिलित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। विभाग में कार्यरत प्राध्यापिका डॉ. चिट्टी अन्नपूर्णा भी कंधे-से-कंधा मिलाकर छात्रों के विकास में रत हैं। इस प्रकार मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य का विकास संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय है।
शुभकामनाओं सहित।
स्वतन्त्रता के उपरांत विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों की स्थापना जोर-शोर से शुरू हुई। मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग सन् 1954 में खुला, जो हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन तथा शोध कार्य हितार्थ निरन्तर सक्रिय रहा। इस विभाग में प्रथम आचार्य शंकरराजू नायडू थे, जिन्होंने कम्ब रामायण और तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। तिरुकुरल का हिन्दी में अनुवाद किया। उनके उपरांत एस.एन. गणशेन् आए जिन्होंने 1975 में हिन्दी और तमिल व्याकरण लिखा तथा सुब्रह्मण्य भारती की कविताओं का 1986 में तथा मणिमेखलै में 1990 में अनुवाद किया। उनके उपरांत डॉ. टी.एस. कुप्पुस्वामी आये जिनकी कृति ‘हिन्दी रीतिकाव्य’ 1990 में प्रकाशित हुई तथा विभाग की अन्य प्राध्यापिका डॉ. शारदा रमणी की कृति भारतेन्दु के गीतों में राष्ट्रीय चेतना 1990, संघम काल में नारी, 1992 में छपी।
सम्प्रति डॉ. सैयद रहमतुल्ला विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने विभाग में कई चुनौती पूर्ण कार्य कर हिन्दी विभाग को प्रतिष्ठा प्रदान की है। सबसे पहले स्कूलों के अध्यापकों को एक साथ जोड़कर उन्हें मार्गदर्शन देते हुए पाठयक्रमों का चयन करवाया। कॉलेजों के पाठ्यक्रम में समयानुकूल बदलाव लाकर उसे बदलाव के अन्तर्गत लिखी गई कृति है। यह पुस्तक ‘हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास’ उसी बदलाव के अन्तर्गत लिखी गई कृति है। डॉ. सैयद रहमतुल्ला चाहते हैं कि हिन्दी पढ़ने वाला छात्र साहित्य का ज्ञानवर्द्धन करें, इसलिए पुस्तक में जहाँ सरल भाषा का प्रयोग किया गया है वहाँ इस बात पर भी विशेष ध्यान रखा गया है कि छात्र का स्तर संवृद्ध की ओर अग्रसर रहे।
यूँ तो कई विद्वानों ने पाठ्यक्रम हेतु ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ लिखा है लेकिन अक्सर यह पाया गया है कि या तो बहुत सरल है, स्तरीय नहीं है या फिर क्लिष्ट है। अत: इस तथ्य को मद्देनजर रखकर डॉ. सैयद रहमतुल्ला के मार्गदर्शन में यह ‘हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास’ लिखा गया है। इसमें नौवें दशक के बाद के साहित्य तथा साहित्यकार का परिचय देने का प्रयास किया गया है जिससे छात्र लाभान्वित हों।
सहर्ष कहा जाता है कि मद्रास में हिन्दी की साख बढ़ाने का श्रेय डॉ. सैयद रहमतुल्ला जी को जाता है क्योंकि विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन होते ही उन्होंने समस्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के सम्मिलित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। विभाग में कार्यरत प्राध्यापिका डॉ. चिट्टी अन्नपूर्णा भी कंधे-से-कंधा मिलाकर छात्रों के विकास में रत हैं। इस प्रकार मद्रास विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य का विकास संतोषप्रद एवं प्रशंसनीय है।
शुभकामनाओं सहित।
-मधु धवन
भूमिका
हम सब यह जानते हैं कि कोई भी भाषा एक आदमी द्वारा बनाई नहीं जा सकती।
भाषा का निर्माण या विकास धीरे-धीरे समाज में आपस में बोलचाल से होता है।
समय के साथ-साथ भाषा बदलती रहती है, इसलिए एक भाषा से दूसरी भाषा बन जाती
है। हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास में उसकी पूर्ववर्ती भाषाओं का
महत्त्वपूर्ण योगदान है।
जब भारत ‘जगद्गुरु’ की संज्ञा से अभिहित था, इस समय वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। जो आदिकाल से ईसा पूर्व पाँचवीं शती तक प्रयुक्त होती रही। समय के साथ वैदिक संस्कृति ही संशोधन प्राप्त कर (व्याकरण के नियमों से सँवर कर) संस्कृत बनी और 500 ई. पूर्व से 100 ई. तक चलती रही। संस्कृत के बाद पहली प्राकृत या पाली आ गई। यह गौतमबुद्ध के समय बोली जाती थी, जो 500 ई. पूर्व से 100 ई. तक रही। इसके बाद दूसरी प्राकृत आ गई। जो पाँच नामों से जानी जाती थी- (1) महाराष्ट्री; (2) शौरसेनी; (3) मागधी; (4) अर्द्धमागधी; (5) पैशाची। इनका प्रचलन 100 ई. से 500 ई. तक रहा। इसी दूसरी प्राकृत से नई भाषा पनपी जिसे ‘अपभ्रंश’ कहा जाता है। जिसके तीन रूप थे- (1) नागर; (2) ब्राचड़; (3) उपनागर। इस अपभ्रंश से कई भाषाएँ विकसित हुईं। जैसे-हिन्दी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि। यदि हम गुजराती, मराठी आदि भाषाओं को एक-दूसरे की बहन कह दें तो अनुचित न होगा क्योंकि ‘अपभ्रंश’ इनकी जननी है। जिस प्रकार भारत में कई प्रांत के कई जिले हैं, उसी प्रकार हिन्दी भाषा में कई उपभाषाएँ हैं। इनमें ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल या राजस्थानी, बुंदेलखण्डी, खड़ी बोली, मैथिली भाषा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिन्दी का साहित्य माना जाता है क्योंकि ये भाषाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास में ‘अपभ्रंश’ काल से उन समस्त रचनाओं का अध्ययन किया जाता है उपर्युक्त उपभाषाओं में से भी लिखी हो।
जब भारत ‘जगद्गुरु’ की संज्ञा से अभिहित था, इस समय वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। जो आदिकाल से ईसा पूर्व पाँचवीं शती तक प्रयुक्त होती रही। समय के साथ वैदिक संस्कृति ही संशोधन प्राप्त कर (व्याकरण के नियमों से सँवर कर) संस्कृत बनी और 500 ई. पूर्व से 100 ई. तक चलती रही। संस्कृत के बाद पहली प्राकृत या पाली आ गई। यह गौतमबुद्ध के समय बोली जाती थी, जो 500 ई. पूर्व से 100 ई. तक रही। इसके बाद दूसरी प्राकृत आ गई। जो पाँच नामों से जानी जाती थी- (1) महाराष्ट्री; (2) शौरसेनी; (3) मागधी; (4) अर्द्धमागधी; (5) पैशाची। इनका प्रचलन 100 ई. से 500 ई. तक रहा। इसी दूसरी प्राकृत से नई भाषा पनपी जिसे ‘अपभ्रंश’ कहा जाता है। जिसके तीन रूप थे- (1) नागर; (2) ब्राचड़; (3) उपनागर। इस अपभ्रंश से कई भाषाएँ विकसित हुईं। जैसे-हिन्दी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि। यदि हम गुजराती, मराठी आदि भाषाओं को एक-दूसरे की बहन कह दें तो अनुचित न होगा क्योंकि ‘अपभ्रंश’ इनकी जननी है। जिस प्रकार भारत में कई प्रांत के कई जिले हैं, उसी प्रकार हिन्दी भाषा में कई उपभाषाएँ हैं। इनमें ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल या राजस्थानी, बुंदेलखण्डी, खड़ी बोली, मैथिली भाषा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिन्दी का साहित्य माना जाता है क्योंकि ये भाषाएँ हिन्दी साहित्य के इतिहास में ‘अपभ्रंश’ काल से उन समस्त रचनाओं का अध्ययन किया जाता है उपर्युक्त उपभाषाओं में से भी लिखी हो।
हिन्दी साहित्य इतिहास : रचना की आवश्यकता
समाज में उभरने वाली हर सामाजिक, राजनीतिक, साम्प्रदायिक, धार्मिक,
सांस्कृतिक स्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। जनता की भावनाएँ
बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों से
प्रभावित होती हैं। इसलिए साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण कहा गया है। इस
प्रकार यह बात उभर कर आती है कि साहित्य का इतिहास मात्र आँकड़े या नामवली
नहीं होती अपितु उसमें जीवन के विकास-क्रम का अध्ययन होता है।
मानव-सभ्यता-संस्कृति और उसके क्रमिक विकास को जानने का मुख्य साधन
साहित्य ही होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए उसमें मानव-मन
के चिन्तन-मनन, भावना और उसके विकास का रूप प्रतिबिम्बित रहता है। अत:
किसी भी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने और उसके प्रेरणास्रोत्रों को
जानने के लिए उसकी पूर्व-परम्पराओं और प्रवृत्तियों का ज्ञान आवश्यक है।
हिन्दी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए हमें विकास के इसी क्रम को
जानना होगा।
हिन्दी की पूर्ववर्ती भाषाएँ (सन् 1050 से पूर्व)
हिन्दी भाषा के उद्भव-विकास में उसकी पूर्ववर्ती भाषाओं का महत्त्वपूर्ण
योगदान रहा है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
• वैदिक संस्कृत-
जिस समय हमारा
देश जगद्गुरु की
संज्ञा से अभिहित था, वैदिक संस्कृत ही भारतीय आर्यों के विचारों की
अभिव्यक्ति करती थी। प्राय: यह आदि काल से ईसा पूर्व पाँचवीं शती तक
प्रयोग में लायी जाती रही।
• संस्कृत-
वैदिक संस्कृत ही समय
के साथ संस्कार
एवं संशोधन प्राप्त कर, व्याकरण के नियमों से सुसज्जित होकर संस्कृत भाषा
बन गई। ईसा से लगभग छ: शताब्दी पूर्व महर्षि पाणिनी की
‘अष्टाध्यायी’ के निर्माण के साथ ही संस्कृत में
एकरूपता आ
गई। यह भाषा 500 ई. पूर्व से 1000 ई. तक चलती रही।
• पहली प्राकृत या पाली-
संस्कृति
साहित्य में
व्याकरण के प्रवेश ने जहाँ एक ओर उसे परिमार्जित कर शिक्षितों की
व्यवहारिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया वहाँ दूसरी ओर उसे जनसाधारण की
पहुँच के बाहर कर दिया। ऐसे समय में लोक भाषा के रूप में मागधी पनप रही
थी, जिसका व्यवहार बौद्ध लोग अपने सिद्धान्त के प्रचारार्थ कर रहे थे। इसी
को पोली कहकर संबोधित किया गया।
• अशोक के शिलालेखों पर ब्राह्मी
और खरोष्ठी नामक
दो लिपियाँ मिलती हैं। इसी को कतिपय भाषा वैज्ञानिक पहली प्राकृत कहकर
पुकारते हैं इस भाषा का काल 500 ई. पूर्व से 100 ई. पूर्व तक निश्चित किया
है।
• दूसरी प्राकृत-
पहली प्राकृत
साहित्यकारों के
सम्पर्क में आते ही दूसरी प्राकृत बन बैठी और उसका प्रचलन होने लगा।
विभिन्न अंचलों में वह भिन्न-भिन्न नामों से पुकारी गई। इस प्रकार इसके
पाँच भेद हुए-
1. महाराष्ट्री-मराठी
2. शौरसेनी-पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती
3. मागधी-बिहारी, मागधी, उड़िया, असमिया
4. अर्द्ध मागधी-पूर्वी हिन्दी
5. पैशाची-लहंदा, पंजाबी
2. शौरसेनी-पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती
3. मागधी-बिहारी, मागधी, उड़िया, असमिया
4. अर्द्ध मागधी-पूर्वी हिन्दी
5. पैशाची-लहंदा, पंजाबी
प्राचीन हिन्दी
इस काल में आते-आते अपभ्रंश साहित्य का माध्यम बन गई। इसमें से ही देश का
जातीय साहित्य मुखरित हुआ। इस प्रकार क्रमश: लोकवाणी, प्रचलित बोलियों एवं
साहित्यिक भाषा के विकास क्रम ने प्राचीन हिन्दी को जन्म दिया जो खड़ी
बोली हिन्दी की जननी है। यही ‘प्राचीन हिन्दी’ या
‘हिन्दवी’ अपभ्रंश और आधुनिक खड़ी बोली के मिलनरेखा
के
मध्य-बिन्दु को निर्धारित करती है।
हिन्दी में इतिहास लिखने की परिपाटी
हिन्दी-साहित्य में इतिहास लिखना कब और कैसे प्रारम्भ हुआ, यह विचारणीय
प्रसंग है। इतिहास लिखने वालों की दृष्टि अपने आप चौरासी वैष्णव की वार्ता
और भक्तकाल की ओर खिंच जाती है परन्तु तथ्यों और खोजबीन से यह पता चलता है
कि इसका श्रीगणेश पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ठाकुर शिवसिंह सेंगर
(सन् 1883 ई.) द्वारा लिखित ‘कवियों के एक वृत्त
संग्रह’ के
द्वारा हुआ। इसके पहले अंग्रेज लेखक गार्साद तासी ने 72 कवियों का नाम
विवरणों के साथ अपने इतिहास (सन् 1839) में प्रस्तुत किया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book