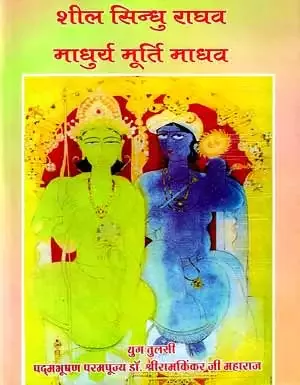|
आचार्य श्रीराम किंकर जी >> शील सिन्धु राघव माधुर्य मूर्ति माधव शील सिन्धु राघव माधुर्य मूर्ति माधवश्रीरामकिंकर जी महाराज
|
334 पाठक हैं |
|||||||
मानसरोवर और समुद्र में डुबकी लगाकर मुझे समग्रता का बोध होता है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य भी यही है।
Sheel Sindhu Raghav Madhurya Moorti Madhav
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भगवान वेदव्यास की कृति श्रीमद्भागवत एक विशाल महोदधि है। श्रीरामचरित मानस के मूल रचयिता भगवान शंकर ने अपनी कृति को समुद्र के स्थान पर सरोवर के रूप में प्रस्तुत किया। सागर और सरोवर की तुलना कैसी ? क्या उद्देश्य रहा होगा, सुकवि शिव का ? शंभु ने इसे साधारण सरोवर के रूप में नहीं, अपितु हिमालय में स्थित ‘‘मानसरोवर’’ की संज्ञा दी।
इसी मानसरोवर को ‘‘सरयू’’ के उद्गम-स्थल के रूप में देखा जाता है। सरयू ही उनके आराध्य की जन्मस्थली एवं लीलाभूमि है। उसके उद्गम को भगवान शिव महत्त्व दें, यह स्वाभाविक ही था। श्रीकृष्ण की लीला का प्राकट्य भी ‘यमुना’ तट पर हुआ, और लीला का विस्तार और संवरण समुद्र तट पर हुआ।
वे द्वारिकाधीश बने। भारत भूमि के उत्तर में है ‘‘नागाधिराज हिमालय’’ जो अनेक नदियों का उद्गम-स्थल है, और स्वयं भगवान शिव का निवास-स्थल भी है। दक्षिण में लहराता हुआ समुद्र, समस्त नदियों के संगम का केन्द्र है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। हिमालय की ऊँचाई और समुद्र की गहराई दोनों ही तीर्थ-यात्रियों को धन्य बनाती हैं। मानसरोवर और समुद्र में डुबकी लगाकर मुझे समग्रता का बोध होता है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य भी यही है।
इसी मानसरोवर को ‘‘सरयू’’ के उद्गम-स्थल के रूप में देखा जाता है। सरयू ही उनके आराध्य की जन्मस्थली एवं लीलाभूमि है। उसके उद्गम को भगवान शिव महत्त्व दें, यह स्वाभाविक ही था। श्रीकृष्ण की लीला का प्राकट्य भी ‘यमुना’ तट पर हुआ, और लीला का विस्तार और संवरण समुद्र तट पर हुआ।
वे द्वारिकाधीश बने। भारत भूमि के उत्तर में है ‘‘नागाधिराज हिमालय’’ जो अनेक नदियों का उद्गम-स्थल है, और स्वयं भगवान शिव का निवास-स्थल भी है। दक्षिण में लहराता हुआ समुद्र, समस्त नदियों के संगम का केन्द्र है, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। हिमालय की ऊँचाई और समुद्र की गहराई दोनों ही तीर्थ-यात्रियों को धन्य बनाती हैं। मानसरोवर और समुद्र में डुबकी लगाकर मुझे समग्रता का बोध होता है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य भी यही है।
-रामकिंकर
सुनि सीतापति-सील-सुभाउ।
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ।।1।।
सिसुपनतें पितु, मातु बंधु, गुरु, सेवक, सचिव, सखाउ।
कहत राम-बिधु बदन रिसोहैं सपनेहुँ लख्यो न काउ।।2।।
खेलत संग अनुज बालक नित, जोगवत अनट अपाउ।
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ।।3।।
सिला साप-संताप-बिगत भइ परसत पावन पाउ।
दई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुएको पछिताउ।।4।।
भव-धनु भंजि निदरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ।
छमि अपराध, छमाइ पाँय परि, इतौ न अनत समाउ।।5।।
कह्यो राज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गयो राउ।
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुघाउ।।6।।
कपि-सेवा-बस भये कनौड़े, कह्यौ पवनसुत आउ।
देबेको न कछु रिनियाँ हौं धनिक तूँ पत्र लिखाउ।।7।।
अपनाये सुग्रीव बिभीषन, तिन न तज्यो छल-छाउ।
भरत सभा सनमानि, सराहत, होत न हृदय अघाउ।।8।।
निज करुना करतूति भगतपर चपत चलत चरचाउ।
सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत, सुनत कहत फिरि गाउ।।9।।
समुझि समुझि गुनग्राम रामके, उर अनुराग बढ़ाउ।
तुलसिदास अनयास रामपद पाइहै प्रेम-पसाउ।।10।।
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ।।1।।
सिसुपनतें पितु, मातु बंधु, गुरु, सेवक, सचिव, सखाउ।
कहत राम-बिधु बदन रिसोहैं सपनेहुँ लख्यो न काउ।।2।।
खेलत संग अनुज बालक नित, जोगवत अनट अपाउ।
जीति हारि चुचुकारि दुलारत, देत दिवावत दाउ।।3।।
सिला साप-संताप-बिगत भइ परसत पावन पाउ।
दई सुगति सो न हेरि हरष हिय, चरन छुएको पछिताउ।।4।।
भव-धनु भंजि निदरि भूपति भृगुनाथ खाइ गये ताउ।
छमि अपराध, छमाइ पाँय परि, इतौ न अनत समाउ।।5।।
कह्यो राज, बन दियो नारिबस, गरि गलानि गयो राउ।
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज तन मरम कुघाउ।।6।।
कपि-सेवा-बस भये कनौड़े, कह्यौ पवनसुत आउ।
देबेको न कछु रिनियाँ हौं धनिक तूँ पत्र लिखाउ।।7।।
अपनाये सुग्रीव बिभीषन, तिन न तज्यो छल-छाउ।
भरत सभा सनमानि, सराहत, होत न हृदय अघाउ।।8।।
निज करुना करतूति भगतपर चपत चलत चरचाउ।
सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत, सुनत कहत फिरि गाउ।।9।।
समुझि समुझि गुनग्राम रामके, उर अनुराग बढ़ाउ।
तुलसिदास अनयास रामपद पाइहै प्रेम-पसाउ।।10।।
अपनी बात
श्रीरामचरित मानस पर, यदि मैं लिखूँ तो वह लोगों को स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। किन्तु श्रीमद्भागवत पर मेरे द्वारा कुछ लिखा जाना, कई लोगों की जिज्ञासा का कारण बन सकता है। अतः मुझे लगा कि यह उचित ही होगा, कि मैं इसकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दूँ।
श्रीराम और श्रीरामचरितमानस से मेरा परिचय कितना पुराना है, मेरे लिए बता पाना संभव नहीं है। इस संदर्भ मेरी मनः स्थिति गोस्वामी तुलसीदास से पूर्ण तादात्म्य रखती है। उन्होंने भी विनय-पत्रिका में लिखा है कि ‘‘केवल तुलसीदास के रूप में ही नहीं, न जाने कब से मेरा परिचय प्रभु से है’’—
श्रीराम और श्रीरामचरितमानस से मेरा परिचय कितना पुराना है, मेरे लिए बता पाना संभव नहीं है। इस संदर्भ मेरी मनः स्थिति गोस्वामी तुलसीदास से पूर्ण तादात्म्य रखती है। उन्होंने भी विनय-पत्रिका में लिखा है कि ‘‘केवल तुलसीदास के रूप में ही नहीं, न जाने कब से मेरा परिचय प्रभु से है’’—
तुलसी तोसों रामसों
कछु नई न जान-पहिचानि।।
(विनय-पत्रिका-193-9)
कछु नई न जान-पहिचानि।।
(विनय-पत्रिका-193-9)
पूर्वजन्मों की बात छोड़ भी दूँ, तो इस जन्म में भी, ऐसे पिता का पुत्र बना, आञ्जनेय हनुमान् के अनन्य भक्त थे, रामचरितमानस के प्रवक्ता थे। भले ही मेरी प्रवचन-शैली उनसे सर्वथा भिन्न रही हो, पर उनकी भक्ति का उत्तराधिकार, मुझे यत्किंचित मिलना स्वाभाविक था। जो कुछ उन्हें साधना के द्वारा मिला, वह मैंने कृपा के माध्यम से पा लिया।
मेरा सारा जीवन ही ‘प्रभु-कृपा’ से संचालित रहा है। मेरे लिए यह औपचारिक स्वीकृति मात्र नहीं। जीवन के प्रतिक्षण की अनुभूति इसी सत्य का दर्शन कराती रहती है।
मानस-वक्ता बनने का न तो मेरा कोई संकल्प था और न ऐसी कोई योग्यता ही स्वयं में पाता था। हिन्दी की शिक्षा के बाद, जब पिताश्री ने मुझसे पूछा, कि ‘तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो या अंग्रेजी ?’ तो मैंने संस्कृत का चुनाव किया। पर इसके पीछे भी, मेरा भय ही कार्य कर रहा था कि अंग्रेजी मेरे लिए कठिन है। यद्यपि यह बाल सुलभ धारणा ही थी, परन्तु इसके पीछे नियति ही कार्य कर रही थी।
बहुत वर्षों बाद, मेरे प्रवचन सुनकर, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पिताजी से कहा—‘‘आपने, अपने पुत्र को अंग्रेजी के माध्यम से यदि विधि-वेत्ता बनाया होता, तो वह देश के सर्वोच्च विधिवेत्ताओं में से एक होता !’’ उनकी यह उक्ति मेरी तर्क-शक्ति के प्रति एक प्रकार की प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति ही थी। उन्हें लगा होगा कि यह किशोर, कथावाचक बनकर क्या पा लेगा ? पर इसके कुछ वर्ष बाद ही, जब वे मुझसे मिले, तब तक, उस छोटी अवस्था में ही मैं विशिष्ट वक्ताओं की श्रेणी में, स्थापित ही नहीं हो गया था, अपितु ‘मानस’ की नई चिन्तन-धारा का प्रवर्तक भी मान लिया गया था ! पूर्व-न्यायाधीश ने अपनी धारणा में निःसंकोच संशोधन करते हुए कहा—‘कितनी हानि साहित्य और धर्म की हुई होती, यदि आप वकील बन गए होते !’’
मुझे इससे प्रसन्नता हुई, किन्तु गर्व नहीं। जो कुछ हुआ था, उसमें मेरा प्रयत्न-पुरुषार्थ, चिन्तन-मनन कुछ भी तो नहीं था। मैं किस बात के लिए अभिमान करता ? मैं तो एक माध्यम था, जिसे प्रभु ने अपनी कृपा की अभिव्यक्ति का उपकरण बना लिया था। प्रवचन के लिए जब मैं प्रथम बार प्रस्तुत हो गया, तो पिता श्री भी चकित थे। कोई तैयारी भी नहीं। यह कैसे संभव है ? पर एक नन्हें-से स्वप्न ने मुझमें जो विश्वास भर दिया था, उसका पता उन्हें नहीं था, मैंने बताया भी नहीं था। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। पर आञ्जनेय के द्वारा दिया जाने वाला यह स्वप्न साधारण सपनों से भिन्न था। बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया। पर इसके अंतराल में जो कुछ घटित हुआ, वे सभी घटनाएँ अप्रत्याशित ही थीं।
प्रारम्भ के वर्षों में ही, एक और मोड़ लिया। जबलपुर में, ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज का आगमन हुआ। ‘कुचैनी मन्दिर’ के नन्हें—से प्रांगण में, मेरे माध्यम से रामकथा चल रही थी। उनके प्रवचन का आयोजन एक वृह्त प्रांगण में किया गया था। अतः उनके श्रीमुख से तत्त्व और रस से ओत-प्रोत श्रीमद्भागवत की कथा सुनने का वह दिव्य सुअवसर मुझे भी मिला। मैं भाव-विभोर था। वे जहाँ विराजमान थे, वहाँ भी नित्य, दिन में जाने लगा था। सत्संगी श्रद्धालुओं की भीड़ में, मैं मिल जाता। उनकी दृष्टि में एक सम्मोहन था, वाणी में मस्ती और मिठास जो मुझे अभिभूत कर देती थी। परिचय हुआ, वह भी उन्हीं की ओर से ! मैंने अपना परिचय देने की कोई चेष्टा नहीं की। प्रश्न भी नहीं करता था। पर उनकी कृपादृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने पास बैठा लिया। उनके वात्सल्य का कहना ही क्या ? स्नेह से पीठ पर हाथ रखकर थपकी देते रहते थे। एक मास बाद, जब वे जाने लगे तब मुझे अपार कष्ट हु्आ। उस समय उन्होंने कहा—‘‘कभी वृन्दावन आना, अभी तो हमें तुमसे बहुत बार मिलते ही रहना है।’’
कुछ महीने बाद कथा-रसिक श्रोता श्री नारायणप्रसाद अग्रवाल ने मुझसे पूछा—‘‘क्या मेरे साथ हरिद्वार चलना आपके लिए संभव है ? लौटते हुए दो-तीन दिन वृन्दावन भी हो लेंगे।’’ मैं प्रस्तुत हो गया। हरिद्वार के बाद वृन्दावनधाम पहुँच गया। पू. स्वामीजी का पुनः सान्निध्य मिला और वे तीन दिन, तीन वर्ष के रूप में परिणत हो गए ! बीच में श्री ‘हनुमद्-जयन्ती’ के लिए ही गाँव जाना पड़ता था, नहीं तो कहीं अन्यत्र जाने की कल्पना भी मन में नहीं उठती थी। ‘‘आली ! म्हाँने लागे बृन्दावन नीको’’—मीरा की यह पंक्ति साकार हो उठी थी। दिन कब व्यतीत हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और दिनचर्या भी आनंदरस से ओत-प्रोत ! प्रातःकालीन जप आदि से निवृत्त होकर सभामण्डप में पहुँच जाना, जहाँ नित्य रासलीला का आयोजन होता था। मण्डप में विराजमान होते थे-परमसिद्ध सन्त श्री उड़ियाबाबाजी, भक्त-शिरोमणि संत श्री हरिबाबाजी महाराज, अपने स्वामी श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती। रासलीलाओं का आयोजन तो होता ही रहता है, पर ऐसे दिव्य दर्शक कहाँ मिलेंगे ? बीच-बीच में श्री हरिबाबा जी उठकर चँवर या पंखा, ‘रास-स्वरूपों’ को झलने लगते। उस समय ‘रास- स्वरूप’ साधारण बालक प्रतीत हो ही नहीं सकते थे। कैसा होता था, श्रीकृष्णलीला का वह दिव्य साक्षात्कार ! उसकी स्मृति आज भी पुलकित बना देती है।
मध्याह्न-भोजन के बाद कीर्तन-प्रवचन का क्रम प्रारंभ होता था। उसमें श्रोता-वक्ता बनने का विलक्षण अवसर मिलता था। सन्त-समाज की उपस्थिति, उनके समक्ष ‘‘वक्ता’’ के रूप में ‘‘रामकथा’’ का प्रवचन करना भी एक अद्भुत अनुभूति थी। कितना आनंद लेता था, संत-समाज ! कितने वात्सल्य भरे हृदय से सुनते थे, वे इस शिशु सेवक की वाणी को ! अन्त में समापन होता था, महाराजश्री के प्रवचन से। श्रीमद्भागवत की निगूढ़, तात्त्विक, रसमयी व्याख्या, उनके श्रीमुख से सुनना, अपने आप में एक अनुभव था, मंगल महोत्सव था। दशम और एकादश स्कन्ध की चर्चा ही मुख्य होती। ‘सप्ताह’ और ‘पाक्षिक’ प्रवचन भी कभी-कभी आयोजित होते।
इस तरह श्रीकृष्ण-रस का आस्वादन प्राप्त होता रहा। कैसी अद्भुत लीला थी प्रभु की। रामभक्ति से जुड़े हुए इस किंकर को उन्हेंने जिन महापुरुषों के सान्निध्य का अवसर दिया, वे श्रीकृष्णभक्त थे। ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ होते हुए भी, उनकी साधना के केन्द्र ‘श्रीकृष्ण’ ही थे। पर उनकी विशेषता और अभेद दृष्टि का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी मुझे रामभक्ति छोड़कर कृष्ण-भावना की ओर मोड़ने की चेष्टा नहीं की। इतना ही क्यों, वे बहुधा मेरा ही पक्ष लेते, मेरी भावना का समर्थन करते। श्रीकृष्ण भक्तों की उस भीड़ में दो ही व्यक्ति राघव के उपासक थे—‘श्री सीताराम बाबा’ और यह किंकर। सीताराम बाबा की जीवनगाथा भी अनोखी थी।
वे रामानन्द सम्प्रदाय में दीक्षित साधु थे। हरिबाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी और उन्हीं के नाते वे वृन्दावन-आश्रम में रहने के लिए आ गए। यहाँ श्याम रँग में रँग गए। कई वर्षों तक वे श्रीकृष्णभक्ति में डूबे रहे। पर अचानक उन्हें एक अनोखा स्वप्न दिखाई दिया और दूसरे दिन से वे पुनः ‘राम-दास’ बन गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं वृन्दावन पहुँचा और वहाँ नित्य रामकथा मेरे माध्यम से कही जाने लगी। इसे वे प्रभु राम का चमत्कार ही मानते थे। वे भाव-विभोर होकर गद्गद कंठ से कहते थे—‘‘तुम्हें तो रामभद्र ने मेरे लिए ही भेजा है’’। पूज्य स्वामीजी महाराज उनकी बातों में बड़ा रस लेते थे। श्रीकृष्णभक्तों के और मेरे बीच जब कभी राम-कृष्ण को लेकर प्रेमभरा विवाद छिड़ता, तब कई बार वे सीताराम बाबा को बुलवा लेते, कहते—‘‘अपना सपना तो सुनाओ’’। सीताराम बाबा पूरी भाव-भंगिमा से इसका वर्णन करते। आँखों में आँसू और गद्गद कंठ से जब वे स्वप्न सुनाते, तो वह दृश्य जैसे साकार हो जाता।
एक बार पूज्य स्वामीजी ने मुझे ‘कल्याण’ के लिए लिखने का आदेश दिया। वह लिखा ही नहीं गया पर प्रकाशित भी हो गया। उसकी शीर्षक था—‘‘भगवान् राम का सौन्दर्य’। इसके बाद तो अनेकों लेख प्रकाशित होते चले गए। पर इस प्रथम लेख की मीठी प्रतिक्रिया, मेरे किशोर सहपाठी मित्र पं. द्वारिका प्रसाद नवेरिया के मन में हुई। संस्कृत पाठशाला में, हम दोनों सहपाठी ही नहीं, मित्र भी थे। यद्यपि, वे मुझसे एक वर्ष आगे थे। उनका मुझ पर विशेष स्नेह था। उनके बारे में जिस समय मुझे यह ज्ञात हुआ था कि वे पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द जी सरस्वती महाराज के सान्निध्य में वृन्दावन चले गए हैं, उस समय तक मैंने पू. स्वामीजी महाराज का दर्शन भी नहीं किया था।
किन्तु नियति ने हमें पुनः एकत्र कर दिया। द्वारिकाप्रसादजी वृन्दावन में रहते हुए, साधना और अध्ययन दोनों में ही संलग्न थे। उन्होंने वहीं रहते हुए ‘पुराणेतिहास शास्त्री’ की परीक्षा पास की। साधना में भी उनकी स्थिति बड़ी उच्चकोटि की थी। आज तो वे श्रीमद्भागवत के उच्चकोटि के वक्ता हैं। पू. स्वामीजी का अलौकिक श्रीमद्भागवत-ज्ञान उन्हें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। पर उन दिनों हम दोनों ही किशोर और युवावस्था के अंतराल में स्थिति थे। वृन्दावन में वे श्रीकृष्ण की रसमयी भक्ति में सराबोर थे। अतः ‘‘श्रीराम के सौन्दर्य’’ की तुलना में उन्होंने ‘‘श्रीकृष्ण के सौन्दर्य’’ पर एक सुन्दर लेख लिखा। पू. स्वामीजी ने उन्हें भी सराहा, प्रोत्साहित किया। वह लेख भी ‘कल्याण’ में प्रकाशित हुआ। इस तरह की प्रेमिल नोंक-झोंक चलना स्वाभाविक ही था। श्रीकृष्ण की लीलास्थली में रामकथा का गायन करने का भी अपना आनंद था।
वृन्दावन में रहते हुए, मुझे एक ऐसे महान् सन्त का दर्शन और मिला, जो बहिरंग रूप से साधारण गृहस्थ जैसे दिखाई देते थे। इस वेष का आश्रय उन्होंने इसीलिए लिया था, कि प्रणाम, चरणस्पर्श को कोई संत रोक न दे। दूसरों को सम्मान देना उनका स्वभाव था। स्वयं तो वे पूर्ण अमानी थे-
सबहि मानप्रद आपु अमानी (रा.चा.मा.7/37/4) के वे आदर्श दृष्टान्त थे। उनके लम्बे-चोंगानुमान कुर्ते पर, श्रीकृष्ण राधारानी का नाम भी अंकित होता था। ये सन्त ‘सिंधा साईं’ के रूप में जाने जाते थे। पू. श्रीउड़िया बाबाजी महाराज तथा पू. स्वामीजी के प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा थी। कथा-सत्संग में उनकी रुचि थी। श्री वृन्दावनधाम में उनका निवास-आश्रम भी था। स्वामीजी को भी वे अपने आश्रम में आमंत्रित करते रहते थे, जहाँ पर उनके अन्तरंग भक्तों के बीच स्वामीजी महाराज का सत्संग होता था। वहाँ जो आनन्द का तरंगायित रूप दृष्टिगोचर होता, वह अन्यत्र दुर्लभ था। पर एक अनोखी बात तो तब सामने आई, जब मुझे बताया गया कि वे श्री कोसलेन्द्र और मैथिली के अन्यत्र भक्त हैं। उनकी भक्ति का रूप भी अद्भुत था। भक्ति का वह सुकुमार स्वरूप मुझे अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उनके यहाँ प्रभु रामभद्र को प्रणाम करना निषिद्ध था, सारे सत्संगी मिथलेशनन्दिनी और राघव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते-
मेरा सारा जीवन ही ‘प्रभु-कृपा’ से संचालित रहा है। मेरे लिए यह औपचारिक स्वीकृति मात्र नहीं। जीवन के प्रतिक्षण की अनुभूति इसी सत्य का दर्शन कराती रहती है।
मानस-वक्ता बनने का न तो मेरा कोई संकल्प था और न ऐसी कोई योग्यता ही स्वयं में पाता था। हिन्दी की शिक्षा के बाद, जब पिताश्री ने मुझसे पूछा, कि ‘तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो या अंग्रेजी ?’ तो मैंने संस्कृत का चुनाव किया। पर इसके पीछे भी, मेरा भय ही कार्य कर रहा था कि अंग्रेजी मेरे लिए कठिन है। यद्यपि यह बाल सुलभ धारणा ही थी, परन्तु इसके पीछे नियति ही कार्य कर रही थी।
बहुत वर्षों बाद, मेरे प्रवचन सुनकर, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने पिताजी से कहा—‘‘आपने, अपने पुत्र को अंग्रेजी के माध्यम से यदि विधि-वेत्ता बनाया होता, तो वह देश के सर्वोच्च विधिवेत्ताओं में से एक होता !’’ उनकी यह उक्ति मेरी तर्क-शक्ति के प्रति एक प्रकार की प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति ही थी। उन्हें लगा होगा कि यह किशोर, कथावाचक बनकर क्या पा लेगा ? पर इसके कुछ वर्ष बाद ही, जब वे मुझसे मिले, तब तक, उस छोटी अवस्था में ही मैं विशिष्ट वक्ताओं की श्रेणी में, स्थापित ही नहीं हो गया था, अपितु ‘मानस’ की नई चिन्तन-धारा का प्रवर्तक भी मान लिया गया था ! पूर्व-न्यायाधीश ने अपनी धारणा में निःसंकोच संशोधन करते हुए कहा—‘कितनी हानि साहित्य और धर्म की हुई होती, यदि आप वकील बन गए होते !’’
मुझे इससे प्रसन्नता हुई, किन्तु गर्व नहीं। जो कुछ हुआ था, उसमें मेरा प्रयत्न-पुरुषार्थ, चिन्तन-मनन कुछ भी तो नहीं था। मैं किस बात के लिए अभिमान करता ? मैं तो एक माध्यम था, जिसे प्रभु ने अपनी कृपा की अभिव्यक्ति का उपकरण बना लिया था। प्रवचन के लिए जब मैं प्रथम बार प्रस्तुत हो गया, तो पिता श्री भी चकित थे। कोई तैयारी भी नहीं। यह कैसे संभव है ? पर एक नन्हें-से स्वप्न ने मुझमें जो विश्वास भर दिया था, उसका पता उन्हें नहीं था, मैंने बताया भी नहीं था। स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। पर आञ्जनेय के द्वारा दिया जाने वाला यह स्वप्न साधारण सपनों से भिन्न था। बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया। पर इसके अंतराल में जो कुछ घटित हुआ, वे सभी घटनाएँ अप्रत्याशित ही थीं।
प्रारम्भ के वर्षों में ही, एक और मोड़ लिया। जबलपुर में, ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती महाराज का आगमन हुआ। ‘कुचैनी मन्दिर’ के नन्हें—से प्रांगण में, मेरे माध्यम से रामकथा चल रही थी। उनके प्रवचन का आयोजन एक वृह्त प्रांगण में किया गया था। अतः उनके श्रीमुख से तत्त्व और रस से ओत-प्रोत श्रीमद्भागवत की कथा सुनने का वह दिव्य सुअवसर मुझे भी मिला। मैं भाव-विभोर था। वे जहाँ विराजमान थे, वहाँ भी नित्य, दिन में जाने लगा था। सत्संगी श्रद्धालुओं की भीड़ में, मैं मिल जाता। उनकी दृष्टि में एक सम्मोहन था, वाणी में मस्ती और मिठास जो मुझे अभिभूत कर देती थी। परिचय हुआ, वह भी उन्हीं की ओर से ! मैंने अपना परिचय देने की कोई चेष्टा नहीं की। प्रश्न भी नहीं करता था। पर उनकी कृपादृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने पास बैठा लिया। उनके वात्सल्य का कहना ही क्या ? स्नेह से पीठ पर हाथ रखकर थपकी देते रहते थे। एक मास बाद, जब वे जाने लगे तब मुझे अपार कष्ट हु्आ। उस समय उन्होंने कहा—‘‘कभी वृन्दावन आना, अभी तो हमें तुमसे बहुत बार मिलते ही रहना है।’’
कुछ महीने बाद कथा-रसिक श्रोता श्री नारायणप्रसाद अग्रवाल ने मुझसे पूछा—‘‘क्या मेरे साथ हरिद्वार चलना आपके लिए संभव है ? लौटते हुए दो-तीन दिन वृन्दावन भी हो लेंगे।’’ मैं प्रस्तुत हो गया। हरिद्वार के बाद वृन्दावनधाम पहुँच गया। पू. स्वामीजी का पुनः सान्निध्य मिला और वे तीन दिन, तीन वर्ष के रूप में परिणत हो गए ! बीच में श्री ‘हनुमद्-जयन्ती’ के लिए ही गाँव जाना पड़ता था, नहीं तो कहीं अन्यत्र जाने की कल्पना भी मन में नहीं उठती थी। ‘‘आली ! म्हाँने लागे बृन्दावन नीको’’—मीरा की यह पंक्ति साकार हो उठी थी। दिन कब व्यतीत हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और दिनचर्या भी आनंदरस से ओत-प्रोत ! प्रातःकालीन जप आदि से निवृत्त होकर सभामण्डप में पहुँच जाना, जहाँ नित्य रासलीला का आयोजन होता था। मण्डप में विराजमान होते थे-परमसिद्ध सन्त श्री उड़ियाबाबाजी, भक्त-शिरोमणि संत श्री हरिबाबाजी महाराज, अपने स्वामी श्री अखण्डानन्दजी सरस्वती। रासलीलाओं का आयोजन तो होता ही रहता है, पर ऐसे दिव्य दर्शक कहाँ मिलेंगे ? बीच-बीच में श्री हरिबाबा जी उठकर चँवर या पंखा, ‘रास-स्वरूपों’ को झलने लगते। उस समय ‘रास- स्वरूप’ साधारण बालक प्रतीत हो ही नहीं सकते थे। कैसा होता था, श्रीकृष्णलीला का वह दिव्य साक्षात्कार ! उसकी स्मृति आज भी पुलकित बना देती है।
मध्याह्न-भोजन के बाद कीर्तन-प्रवचन का क्रम प्रारंभ होता था। उसमें श्रोता-वक्ता बनने का विलक्षण अवसर मिलता था। सन्त-समाज की उपस्थिति, उनके समक्ष ‘‘वक्ता’’ के रूप में ‘‘रामकथा’’ का प्रवचन करना भी एक अद्भुत अनुभूति थी। कितना आनंद लेता था, संत-समाज ! कितने वात्सल्य भरे हृदय से सुनते थे, वे इस शिशु सेवक की वाणी को ! अन्त में समापन होता था, महाराजश्री के प्रवचन से। श्रीमद्भागवत की निगूढ़, तात्त्विक, रसमयी व्याख्या, उनके श्रीमुख से सुनना, अपने आप में एक अनुभव था, मंगल महोत्सव था। दशम और एकादश स्कन्ध की चर्चा ही मुख्य होती। ‘सप्ताह’ और ‘पाक्षिक’ प्रवचन भी कभी-कभी आयोजित होते।
इस तरह श्रीकृष्ण-रस का आस्वादन प्राप्त होता रहा। कैसी अद्भुत लीला थी प्रभु की। रामभक्ति से जुड़े हुए इस किंकर को उन्हेंने जिन महापुरुषों के सान्निध्य का अवसर दिया, वे श्रीकृष्णभक्त थे। ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञ होते हुए भी, उनकी साधना के केन्द्र ‘श्रीकृष्ण’ ही थे। पर उनकी विशेषता और अभेद दृष्टि का ही परिणाम था कि उन्होंने कभी मुझे रामभक्ति छोड़कर कृष्ण-भावना की ओर मोड़ने की चेष्टा नहीं की। इतना ही क्यों, वे बहुधा मेरा ही पक्ष लेते, मेरी भावना का समर्थन करते। श्रीकृष्ण भक्तों की उस भीड़ में दो ही व्यक्ति राघव के उपासक थे—‘श्री सीताराम बाबा’ और यह किंकर। सीताराम बाबा की जीवनगाथा भी अनोखी थी।
वे रामानन्द सम्प्रदाय में दीक्षित साधु थे। हरिबाबा के प्रति उनकी श्रद्धा थी और उन्हीं के नाते वे वृन्दावन-आश्रम में रहने के लिए आ गए। यहाँ श्याम रँग में रँग गए। कई वर्षों तक वे श्रीकृष्णभक्ति में डूबे रहे। पर अचानक उन्हें एक अनोखा स्वप्न दिखाई दिया और दूसरे दिन से वे पुनः ‘राम-दास’ बन गए। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैं वृन्दावन पहुँचा और वहाँ नित्य रामकथा मेरे माध्यम से कही जाने लगी। इसे वे प्रभु राम का चमत्कार ही मानते थे। वे भाव-विभोर होकर गद्गद कंठ से कहते थे—‘‘तुम्हें तो रामभद्र ने मेरे लिए ही भेजा है’’। पूज्य स्वामीजी महाराज उनकी बातों में बड़ा रस लेते थे। श्रीकृष्णभक्तों के और मेरे बीच जब कभी राम-कृष्ण को लेकर प्रेमभरा विवाद छिड़ता, तब कई बार वे सीताराम बाबा को बुलवा लेते, कहते—‘‘अपना सपना तो सुनाओ’’। सीताराम बाबा पूरी भाव-भंगिमा से इसका वर्णन करते। आँखों में आँसू और गद्गद कंठ से जब वे स्वप्न सुनाते, तो वह दृश्य जैसे साकार हो जाता।
एक बार पूज्य स्वामीजी ने मुझे ‘कल्याण’ के लिए लिखने का आदेश दिया। वह लिखा ही नहीं गया पर प्रकाशित भी हो गया। उसकी शीर्षक था—‘‘भगवान् राम का सौन्दर्य’। इसके बाद तो अनेकों लेख प्रकाशित होते चले गए। पर इस प्रथम लेख की मीठी प्रतिक्रिया, मेरे किशोर सहपाठी मित्र पं. द्वारिका प्रसाद नवेरिया के मन में हुई। संस्कृत पाठशाला में, हम दोनों सहपाठी ही नहीं, मित्र भी थे। यद्यपि, वे मुझसे एक वर्ष आगे थे। उनका मुझ पर विशेष स्नेह था। उनके बारे में जिस समय मुझे यह ज्ञात हुआ था कि वे पूज्य स्वामी श्री अखण्डानन्द जी सरस्वती महाराज के सान्निध्य में वृन्दावन चले गए हैं, उस समय तक मैंने पू. स्वामीजी महाराज का दर्शन भी नहीं किया था।
किन्तु नियति ने हमें पुनः एकत्र कर दिया। द्वारिकाप्रसादजी वृन्दावन में रहते हुए, साधना और अध्ययन दोनों में ही संलग्न थे। उन्होंने वहीं रहते हुए ‘पुराणेतिहास शास्त्री’ की परीक्षा पास की। साधना में भी उनकी स्थिति बड़ी उच्चकोटि की थी। आज तो वे श्रीमद्भागवत के उच्चकोटि के वक्ता हैं। पू. स्वामीजी का अलौकिक श्रीमद्भागवत-ज्ञान उन्हें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। पर उन दिनों हम दोनों ही किशोर और युवावस्था के अंतराल में स्थिति थे। वृन्दावन में वे श्रीकृष्ण की रसमयी भक्ति में सराबोर थे। अतः ‘‘श्रीराम के सौन्दर्य’’ की तुलना में उन्होंने ‘‘श्रीकृष्ण के सौन्दर्य’’ पर एक सुन्दर लेख लिखा। पू. स्वामीजी ने उन्हें भी सराहा, प्रोत्साहित किया। वह लेख भी ‘कल्याण’ में प्रकाशित हुआ। इस तरह की प्रेमिल नोंक-झोंक चलना स्वाभाविक ही था। श्रीकृष्ण की लीलास्थली में रामकथा का गायन करने का भी अपना आनंद था।
वृन्दावन में रहते हुए, मुझे एक ऐसे महान् सन्त का दर्शन और मिला, जो बहिरंग रूप से साधारण गृहस्थ जैसे दिखाई देते थे। इस वेष का आश्रय उन्होंने इसीलिए लिया था, कि प्रणाम, चरणस्पर्श को कोई संत रोक न दे। दूसरों को सम्मान देना उनका स्वभाव था। स्वयं तो वे पूर्ण अमानी थे-
सबहि मानप्रद आपु अमानी (रा.चा.मा.7/37/4) के वे आदर्श दृष्टान्त थे। उनके लम्बे-चोंगानुमान कुर्ते पर, श्रीकृष्ण राधारानी का नाम भी अंकित होता था। ये सन्त ‘सिंधा साईं’ के रूप में जाने जाते थे। पू. श्रीउड़िया बाबाजी महाराज तथा पू. स्वामीजी के प्रति उनमें बड़ी श्रद्धा थी। कथा-सत्संग में उनकी रुचि थी। श्री वृन्दावनधाम में उनका निवास-आश्रम भी था। स्वामीजी को भी वे अपने आश्रम में आमंत्रित करते रहते थे, जहाँ पर उनके अन्तरंग भक्तों के बीच स्वामीजी महाराज का सत्संग होता था। वहाँ जो आनन्द का तरंगायित रूप दृष्टिगोचर होता, वह अन्यत्र दुर्लभ था। पर एक अनोखी बात तो तब सामने आई, जब मुझे बताया गया कि वे श्री कोसलेन्द्र और मैथिली के अन्यत्र भक्त हैं। उनकी भक्ति का रूप भी अद्भुत था। भक्ति का वह सुकुमार स्वरूप मुझे अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उनके यहाँ प्रभु रामभद्र को प्रणाम करना निषिद्ध था, सारे सत्संगी मिथलेशनन्दिनी और राघव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते-
सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसीदास के ईस !
(रा.च.मा.1/169)
(रा.च.मा.1/169)
प्रणाम तो वे भगवान् श्रीकृष्ण को करते थे, उनकी कृष्ण-पूजा का उद्देश्य यही था कि कृष्ण प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें कि ‘‘उनके परम प्रियतम रामभद्र अपनी प्रिया के साथ, निरंतर आनन्दमय विहार करते रहें।’’ अतः निवास के लिए भी उन्होंने श्रीधाम वृन्दावन का चुनाव किया था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book