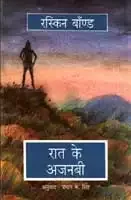|
सामाजिक >> रात के अजनबी रात के अजनबीप्रभात के. सिंह
|
30 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है दो लघु उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रात के अजनबी में संकलित दोनों लघु-उपन्यास-मुट्ठीभर बादाम
और कामी-पुरुष-रस्किन बॉण्ड की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। मुट्ठीभर बादाम भरत
के एक छोटे से कस्बानुमा पर्वतीय शहर में जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए
एक संवेदनशील किशोर की रोमांचक एवं अत्यंत मनोहर कहानी है। तरुणाई की
शरारतें, रोमांस और बात-बात में मित्रों की दखलंदाजी जैसी चित्त को भंग
करने वाली बातों के बावजूद इसका मुख्य पात्र एक प्रतिष्ठित लेखक बनने का
अटल निश्चय लिए संघर्षरत दिखाता है। यह लघु-उपन्यास बॉण्ड की ताजगी भरी
एवं सम्मोहक लेखन-शैली का एक अनूठा नमूना है।
कामीपुरुष प्रबल यौन प्रवृत्तियों वाले एक व्यक्ति का विचारमग्न आत्मविश्लेषण प्रस्तुत करता है। लैंगिक सुख भोग की अतिशयता में भरे जोखिम और आनंद, प्रयोगों और मुसीबतों की यह कहानी बेहद रोचक है और निष्ठुर रूप से खुले शब्दों में कही गई है। इसका मुख्य पात्र अपने आपसे समझौता करने के प्रयास में अपने अंदर के दानव से जूझता नजर आता है। रस्किन बॉण्ड ने कामविषयक जिज्ञासाओं एवं अनुभवों को एक ऐसे कथानक में बाँधा है कि पाठक इसे एक ही सांस में पढ़ने को विवश हो जाता है।
अनुवादक प्रभात के. सिंह ने अंगरेजी साहित्य में आलोचना की तीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो काफी प्रशंसित हुई हैं। उनमें से एक द क्रिएटवि कॉनटुअस ऑफ रस्किन बॉण्ड को बॉण्ड साहित्य पर लिखित विश्व की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इनकी अंगरेजी कविताओं का प्रथम संग्रह पेस में है। सम्प्रति स्नातकोत्तर अंगरेजी विभाग, गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय) में उपाचार्य पद पर कार्यरत।
कामीपुरुष प्रबल यौन प्रवृत्तियों वाले एक व्यक्ति का विचारमग्न आत्मविश्लेषण प्रस्तुत करता है। लैंगिक सुख भोग की अतिशयता में भरे जोखिम और आनंद, प्रयोगों और मुसीबतों की यह कहानी बेहद रोचक है और निष्ठुर रूप से खुले शब्दों में कही गई है। इसका मुख्य पात्र अपने आपसे समझौता करने के प्रयास में अपने अंदर के दानव से जूझता नजर आता है। रस्किन बॉण्ड ने कामविषयक जिज्ञासाओं एवं अनुभवों को एक ऐसे कथानक में बाँधा है कि पाठक इसे एक ही सांस में पढ़ने को विवश हो जाता है।
अनुवादक प्रभात के. सिंह ने अंगरेजी साहित्य में आलोचना की तीन पुस्तकें प्रकाशित की हैं जो काफी प्रशंसित हुई हैं। उनमें से एक द क्रिएटवि कॉनटुअस ऑफ रस्किन बॉण्ड को बॉण्ड साहित्य पर लिखित विश्व की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। इनकी अंगरेजी कविताओं का प्रथम संग्रह पेस में है। सम्प्रति स्नातकोत्तर अंगरेजी विभाग, गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय) में उपाचार्य पद पर कार्यरत।
अनुवादक की कलम से
‘‘Translating is one of the most complex activities
in cosmos’’
I. A. Richards
विश्व विख्यात लेखक और पिछले ही सप्ताह अपने
बाल साहित्य
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार ‘Hans Christian Anderson
Award’ हेतु मनोनीत होने वाले प्रथम भारतीय रस्किन बॉण्ड के
नवीनतम
प्रकाशन Strangers in the Night (Penguin India, 1996) जो दो लघु
उपन्यासों- A Handful of Nuts और The Sensualist (A Cautionary Tale)- का
संकलित रूप है, का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा
है। रात के अजनबी में दोनों लघु उपन्यास क्रमशः मुट्ठीभर बादाम तथा कामी
पुरुष (एक सचेतक कथा) शीर्षक के तहत अनूदित किए गए हैं।
रस्किन बॉण्ड के ये दोनों लघु उपन्यास बेहद रोचक हैं। इनमें नायक के तरुणाई और उसकी कामविषयक जिज्ञासा एवं ज्ञान की परतों का अनावरण बड़े ही बेबाक किन्तु शिष्ट सांकेतिक शब्दों में किया गया है। किशोरवय नायक अपने अस्तित्व की लड़ाई चेतना के बौद्धिक, संवेगात्मक एवं भौतिक-तीनों स्तरों पर एक साथ लड़ता हुआ दिखता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच के सूक्ष्म सम्बन्ध तथा हास्य और गांभीर्य के सुरुचिपूर्ण मिश्रण बॉण्ड के कथा-साहित्य में कथ्य एवं तथ्य तथा भाषा एवं भाव के तादात्म्य को सम्पुष्ट करते हैं। खासकर विषय की नवीनता के कारण इन लघु उपन्यासों के कथानक पाठकों को रस्किन बॉण्ड की लेखन कला के एक नये आयाम से परिचित कराते हैं। इन्हीं विशिष्टताओं ने मुझे बॉण्ड की मूल रचना Strangers in the Night को जिसकी एक प्रति उपहारस्वरुप उन्होंने मुझे भेजी थी और जो मेरे लिए वर्ष 1997 की पहली अनुपम भेंट थी, एक ही साँस में पढ़ जाने के लिए बाध्य कर दिया था। और तत्काल बाद उसे हिन्दी में अनूदित करने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मैं इस आशय का प्रस्ताव उनके सामने रखने का लोभ संवरण न कर सका। कहना न होगा कि प्रस्तुत अनुवाद जो आज हिन्दी जगत के विशाल पाठक समुदाय को उपलब्ध है, उनकी कृपापूर्ण अनुमति से ही सम्भव हो पाया।
कहते हैं अमूमन ‘Translation is s woman if beautiful not faithful, if faithful not beautiful.’ आप क्या कहते हैं ?
रस्किन बॉण्ड के ये दोनों लघु उपन्यास बेहद रोचक हैं। इनमें नायक के तरुणाई और उसकी कामविषयक जिज्ञासा एवं ज्ञान की परतों का अनावरण बड़े ही बेबाक किन्तु शिष्ट सांकेतिक शब्दों में किया गया है। किशोरवय नायक अपने अस्तित्व की लड़ाई चेतना के बौद्धिक, संवेगात्मक एवं भौतिक-तीनों स्तरों पर एक साथ लड़ता हुआ दिखता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच के सूक्ष्म सम्बन्ध तथा हास्य और गांभीर्य के सुरुचिपूर्ण मिश्रण बॉण्ड के कथा-साहित्य में कथ्य एवं तथ्य तथा भाषा एवं भाव के तादात्म्य को सम्पुष्ट करते हैं। खासकर विषय की नवीनता के कारण इन लघु उपन्यासों के कथानक पाठकों को रस्किन बॉण्ड की लेखन कला के एक नये आयाम से परिचित कराते हैं। इन्हीं विशिष्टताओं ने मुझे बॉण्ड की मूल रचना Strangers in the Night को जिसकी एक प्रति उपहारस्वरुप उन्होंने मुझे भेजी थी और जो मेरे लिए वर्ष 1997 की पहली अनुपम भेंट थी, एक ही साँस में पढ़ जाने के लिए बाध्य कर दिया था। और तत्काल बाद उसे हिन्दी में अनूदित करने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मैं इस आशय का प्रस्ताव उनके सामने रखने का लोभ संवरण न कर सका। कहना न होगा कि प्रस्तुत अनुवाद जो आज हिन्दी जगत के विशाल पाठक समुदाय को उपलब्ध है, उनकी कृपापूर्ण अनुमति से ही सम्भव हो पाया।
कहते हैं अमूमन ‘Translation is s woman if beautiful not faithful, if faithful not beautiful.’ आप क्या कहते हैं ?
प्रभात के. सिंह
भूमिका
प्रारम्भ में ही यह खुलासा कर देना चाहूँगा कि यह पुस्तक स्कूली कक्षाओं
के लिए नहीं लिखी गई है।
विगत वर्षों में मेरी कई कहानियाँ, जो विशेष रूप से तरुण पाठकों के लिए लिखी गई थीं, भारत तथा विदेशों में स्कूल अथवा कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान पा चुकी हैं। मेरे लेखन का यह पक्ष मेरे लिए सदैव संतोष का विषय रहा है। किन्तु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मैं वयस्कों के लिए कभी न लिखूँ। या कि दैहिक संवेगों और मानवीय इच्छाओं के सीमाक्षेत्र मेरे लिए वर्जित हैं। जब-तब मैंने भी सफेद चादर उतार कर सहज फक्कड़पन अथवा किसी चाहत के किस्से का रस देवदार तले लिया है।
मगर मेरे भद्र पाठकगण ! आप तनावमुक्त रहें। मैं आपके सामने अश्लीलता की तश्तरी पेश करने नहीं जा रहा। ‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्यूअलिस्ट) एक ऐसे शख्स की कहानी है जो प्रबल यौन प्रवृत्तियों का दास बन चुका था और जिसने उसे आत्मनाश के सर्पीले ढलान पर ला छोड़ा। आप कह सकते हैं कि इस कथा में एक नैतिक सीख है।
‘मुट्ठीभर बादाम’ (ए हैण्डफुल ऑफ नट्स) में एहसास भरा है मेरे जीवन के इक्कीसवें वर्ष का-उम्र का एक ऐसा पड़ाव जो हर किसी के लिए अहम होता है। यह वह आयु है जब हम सबों को जीवन-यात्रा की कठोरता को झेलने के लिए अपने मूल स्वभाव से समझौता करना होता है।
मेरा इक्कीसवाँ वर्ष मेरे लिए विशेष महत्त्व का था। मेरी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मैं आशा और आकांक्षा से भरा था-किसी भी प्रयत्न के लिए तत्पर। मुझमें एक अनन्य प्रेमी के सभी लक्षण मौजूद थे, जैसा कि इस उम्र में प्रायः हम सबों के साथ होता है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि महान प्रेमी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं।
जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है मेरा जीवन उत्तरोत्तर हास्यकर होता जा रहा प्रतीत होता है और मैं अपने आप को एक विदूषक की भूमिका के सर्वथा योग्य पाता हूँ न कि किसी रोमानी नायक की भूमिका के।
उम्र के इक्कीसवें बसंत में हम सभी रोमानी नायक (या नायिका) बनना चाहते हैं, जिसका प्रतिफल प्रायः विनाशकारी होता है। यह एक विचित्र उम्र है। इसके लिए आवश्यक है कि या तो आपके पास पर्याप्त धन हो या फिर एक सुन्दर आकृति। पर मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था।
‘मुट्ठीभर बादाम’ मैंने बीते शरद के साढ़े तीन महीनों में लिखा, जब ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों ने मुझे पहाड़ों में बसे मेरे छोटे से घर में कैद कर रखा था। अपनी किशोरावस्था के दिनों की नीरसता को फिर से महसूस करने की इच्छा जाग उठी और मैंने इस लघु उपन्यास में उस समय और स्थान की स्मृतियों को कलमबन्द करने का प्रयास किया। तथापि इसे सीधे-सीधे मेरी आत्मकथा न मान लें। इनमें से कुछ पात्र और स्थान सच्चे हैं और घटनाएँ भी सच्ची हैं और शेष मेरी कल्पना की उपज। कहते हैं, एक अच्छा किस्सागो वही होता है, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो और जो आशान्वित हो कि अन्य लोगों के पास इसका पूर्ण अभाव है। मैं नहीं मानता कि मेरी स्मरण शक्ति किसी और की तुलना में ज्यादा अच्छी है, परन्तु यह निश्चित रूप से चयनात्मक है जैसा कि एक लेखक की होनी चाहिए। और यदि मैंने किन्हीं प्रमुख मित्रों को इस लघु उपन्यास में भुला दिया है तो वे निश्चिय ही किसी अन्य कथानक के लिए सुरक्षित मेरी पूँजी होंगे।
‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्युअलिस्ट) भी किसी भी रूप में आत्मकथात्मक नहीं है। हम सबों में एक जेकिअल और हाइड छिपा है-दो परस्पर विरोधी व्यक्तित्व-और यहीं तक लेखक की आत्मा झलकती है। मार्क ट्वेन के शब्दों में, जो किसी अन्य सन्दर्भ में कहे गए थे, ऐसी कहानी ‘‘रोचक होती है, यदि सत्य हो, और यदि असत्य, तब भी रोचक’’।
‘‘कामी पुरुष’ आज से कोई बाईस वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसका प्रथम प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित ‘डेबॅनेअ’ नामक पत्रिका में तीन-चार किस्तों में हुआ। गर्मी में एक दिन जब मैं अपने मसूरी निवास के बाहर मेपॅल की छाँव का आनन्द ले रहा था, तभी पुलिस का एक सिपाही मेरी गिरफ्तारी का परवाना लेकर आ धमका। यह एक गैरज़मानती वारंट था। सिपाही भी स्थानीय थाने का नहीं था। वह सीधा बम्बई से मुझे गिरफ्तार करने आया था। उस निर्मल शहर में मुझे पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था और अदालती वांरट में मुझे फ़रार घोषित किया गया था।
उन दिनों देश में आपातकाल घोषित था और लेखकों तथा पत्रकारों के लिए समय प्रतिकूल था। विनोद मेहता ने ‘डेबॅनेअ’ का कार्यभार सँभाला ही था कि उनका स्वागत मुकदमों की भीड़ से हुआ।
मसूरी के एस.डी.एम. ने सहृदयतावश अपने स्व-निर्णय का प्रयोग कर मुझे ज़मानत दी और एक-दो महीनों बाद मैं मन्थर गति से चलनेवाली एक सवारी रेलगाड़ी से बम्बई पहुँचा, जहाँ एक प्रत्यक्षतः कठोर एवं अड़ियल जज की अदालत में मेरी पेशी हुई। मुकदमा एक-दो वर्षों तक खिंचा, जिस दरम्यान अपने निर्दोष होने की दलील के साथ मुझे रुक-रुक कर अदालत में हा़ज़िर होना पड़ा। इसी बीच सरकारी वकील की हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने अश्लीलता के आरोप के साथ मेरे खिलाफ़ मुकदमा दायर किया था, उनकी इसमें रुचि निरंतर घटती गई। ‘डेबॅनेअ’ ने बचाव की जोरदार पैरवी की और निसीम इज़ेंकिअल तथा विजय तेन्दुलकर सरीखे लेखकों ने मेरे पक्ष में अदालत में बयान दिए। तब कहीं जाकर जज को मेरी कहानी में कुछ गुण नजर आए और उसने हम सबों को बाइज़्ज़त आरोप-मुक्त कर दिया। आज भी साठ पृष्ठों का फैसला बम्बई कोर्ट के लेखागार में सुरक्षित है।
बहरहाल, मैंने इस कहानी को पुनः प्रकाशित नहीं करवाया। आखिरकार मुझे आत्मरक्षात्मक जो होना पड़ा था। किन्तु लगभग एक वर्ष पूर्व पेन्ग्विन इंडिया ने अपने दसवें वार्षिकोत्सव के क्रम में इसे मेरी रचनाओं के सर्वसंग्रह में सम्मिलित करने का निर्णय किया और मुझे सम्मानित किया। ‘आउटलुक’ नामक पत्रिका के साहित्यालोचक ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि यह कहानी लेखक के व्यक्तित्व के एक रोचक तथा जटिल पक्ष का अनावरण करती है और आशा व्यक्त की कि इसी तरह की और भी रचनाओं की कड़ियाँ जुड़ेगी।
पता नहीं ‘मुट्ठीभर बादाम’ उसी तरह की रचना है या नहीं पर निश्चय ही यह एक भिन्न लघु उपन्यास है एक ऐसा साहित्यिक रूप-विधान जो मेरी शैली और मेरे चित्त के अनुरूप है। केवल फ्रांसीसी (और कभी-कभी अमरीकी भी) साहित्यकारों ने ही लघु उपन्यास की विधा के साथ पूर्ण न्याय किया है। ब्रिटिश उपन्यासकार प्रचुर रूप से लम्बे उपन्यासों को ही तरजीह देते हैं और ब्रिटिश प्रकाशक तो उपन्यासिकाओं को नजर उठा के भी नहीं देखते। वे शब्दों की अधिकता में अपना धन देखते हैं। किन्तु संरचनात्मक कसाव तथा अवधारणा की एकरूपता के कारण लघु उपन्यास का अपना स्थान है जैसा कि कॉनरेड ने अपने उपन्यासों ‘हार्ट ऑफ डार्कनेस’, ‘द शैडो लाइन’, ‘यूथ’ तथा ‘द निगर ऑफ द नारसिसस’ में प्रदर्शित किया है। हालाँकि वह एक पोलैंडवासी था, जो अँगरेजी में लिखता था।
यों तो मैं दूसरा कॉनरेड नहीं बन सकता किन्तु शायद उस उत्कृष्ट कथाकार के संस्कार के कुछ छींटे मुझ पर भी पड़े हों क्योंकि ‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्यूअलिस्ट) में विचारमग्नता तथा निराशावाद के कुछ लक्षण मौजूद हैं, जो मेरी रुचि के प्रतिकूल हैं। साथ ही मैंने ‘कथा के अन्दर कथा’ जैसी वर्णन शैली का भी प्रयोग किया है। पहाड़ों में रहने वाला एकान्तवासी मेरी ही आत्मा का दूसरा रूप है-मेरी ‘गुप्त सहभागी’। ‘मुट्ठीभर बादाम’ में ऐसा कोई भी पात्र नहीं है। वहाँ मैं मात्र अपने सामान्य आदरविहीन रूप में हूँ। यह उपन्यास एक लेखक का संवेदनशील तथा कभी-कभी शरारती युवक वाला आत्मचित्र है। या यूँ कहें कि एक शरारती प्रौढ़ लेखक के अपने निश्छल तरुणाई की ओर मुड़ कर देखने का चित्रण है।
मुट्ठीभर बादाम
विगत वर्षों में मेरी कई कहानियाँ, जो विशेष रूप से तरुण पाठकों के लिए लिखी गई थीं, भारत तथा विदेशों में स्कूल अथवा कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान पा चुकी हैं। मेरे लेखन का यह पक्ष मेरे लिए सदैव संतोष का विषय रहा है। किन्तु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मैं वयस्कों के लिए कभी न लिखूँ। या कि दैहिक संवेगों और मानवीय इच्छाओं के सीमाक्षेत्र मेरे लिए वर्जित हैं। जब-तब मैंने भी सफेद चादर उतार कर सहज फक्कड़पन अथवा किसी चाहत के किस्से का रस देवदार तले लिया है।
मगर मेरे भद्र पाठकगण ! आप तनावमुक्त रहें। मैं आपके सामने अश्लीलता की तश्तरी पेश करने नहीं जा रहा। ‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्यूअलिस्ट) एक ऐसे शख्स की कहानी है जो प्रबल यौन प्रवृत्तियों का दास बन चुका था और जिसने उसे आत्मनाश के सर्पीले ढलान पर ला छोड़ा। आप कह सकते हैं कि इस कथा में एक नैतिक सीख है।
‘मुट्ठीभर बादाम’ (ए हैण्डफुल ऑफ नट्स) में एहसास भरा है मेरे जीवन के इक्कीसवें वर्ष का-उम्र का एक ऐसा पड़ाव जो हर किसी के लिए अहम होता है। यह वह आयु है जब हम सबों को जीवन-यात्रा की कठोरता को झेलने के लिए अपने मूल स्वभाव से समझौता करना होता है।
मेरा इक्कीसवाँ वर्ष मेरे लिए विशेष महत्त्व का था। मेरी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। मैं आशा और आकांक्षा से भरा था-किसी भी प्रयत्न के लिए तत्पर। मुझमें एक अनन्य प्रेमी के सभी लक्षण मौजूद थे, जैसा कि इस उम्र में प्रायः हम सबों के साथ होता है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि महान प्रेमी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं।
जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाती है मेरा जीवन उत्तरोत्तर हास्यकर होता जा रहा प्रतीत होता है और मैं अपने आप को एक विदूषक की भूमिका के सर्वथा योग्य पाता हूँ न कि किसी रोमानी नायक की भूमिका के।
उम्र के इक्कीसवें बसंत में हम सभी रोमानी नायक (या नायिका) बनना चाहते हैं, जिसका प्रतिफल प्रायः विनाशकारी होता है। यह एक विचित्र उम्र है। इसके लिए आवश्यक है कि या तो आपके पास पर्याप्त धन हो या फिर एक सुन्दर आकृति। पर मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं था।
‘मुट्ठीभर बादाम’ मैंने बीते शरद के साढ़े तीन महीनों में लिखा, जब ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों ने मुझे पहाड़ों में बसे मेरे छोटे से घर में कैद कर रखा था। अपनी किशोरावस्था के दिनों की नीरसता को फिर से महसूस करने की इच्छा जाग उठी और मैंने इस लघु उपन्यास में उस समय और स्थान की स्मृतियों को कलमबन्द करने का प्रयास किया। तथापि इसे सीधे-सीधे मेरी आत्मकथा न मान लें। इनमें से कुछ पात्र और स्थान सच्चे हैं और घटनाएँ भी सच्ची हैं और शेष मेरी कल्पना की उपज। कहते हैं, एक अच्छा किस्सागो वही होता है, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो और जो आशान्वित हो कि अन्य लोगों के पास इसका पूर्ण अभाव है। मैं नहीं मानता कि मेरी स्मरण शक्ति किसी और की तुलना में ज्यादा अच्छी है, परन्तु यह निश्चित रूप से चयनात्मक है जैसा कि एक लेखक की होनी चाहिए। और यदि मैंने किन्हीं प्रमुख मित्रों को इस लघु उपन्यास में भुला दिया है तो वे निश्चिय ही किसी अन्य कथानक के लिए सुरक्षित मेरी पूँजी होंगे।
‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्युअलिस्ट) भी किसी भी रूप में आत्मकथात्मक नहीं है। हम सबों में एक जेकिअल और हाइड छिपा है-दो परस्पर विरोधी व्यक्तित्व-और यहीं तक लेखक की आत्मा झलकती है। मार्क ट्वेन के शब्दों में, जो किसी अन्य सन्दर्भ में कहे गए थे, ऐसी कहानी ‘‘रोचक होती है, यदि सत्य हो, और यदि असत्य, तब भी रोचक’’।
‘‘कामी पुरुष’ आज से कोई बाईस वर्ष पूर्व लिखा गया था और इसका प्रथम प्रकाशन बम्बई से प्रकाशित ‘डेबॅनेअ’ नामक पत्रिका में तीन-चार किस्तों में हुआ। गर्मी में एक दिन जब मैं अपने मसूरी निवास के बाहर मेपॅल की छाँव का आनन्द ले रहा था, तभी पुलिस का एक सिपाही मेरी गिरफ्तारी का परवाना लेकर आ धमका। यह एक गैरज़मानती वारंट था। सिपाही भी स्थानीय थाने का नहीं था। वह सीधा बम्बई से मुझे गिरफ्तार करने आया था। उस निर्मल शहर में मुझे पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया था और अदालती वांरट में मुझे फ़रार घोषित किया गया था।
उन दिनों देश में आपातकाल घोषित था और लेखकों तथा पत्रकारों के लिए समय प्रतिकूल था। विनोद मेहता ने ‘डेबॅनेअ’ का कार्यभार सँभाला ही था कि उनका स्वागत मुकदमों की भीड़ से हुआ।
मसूरी के एस.डी.एम. ने सहृदयतावश अपने स्व-निर्णय का प्रयोग कर मुझे ज़मानत दी और एक-दो महीनों बाद मैं मन्थर गति से चलनेवाली एक सवारी रेलगाड़ी से बम्बई पहुँचा, जहाँ एक प्रत्यक्षतः कठोर एवं अड़ियल जज की अदालत में मेरी पेशी हुई। मुकदमा एक-दो वर्षों तक खिंचा, जिस दरम्यान अपने निर्दोष होने की दलील के साथ मुझे रुक-रुक कर अदालत में हा़ज़िर होना पड़ा। इसी बीच सरकारी वकील की हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने अश्लीलता के आरोप के साथ मेरे खिलाफ़ मुकदमा दायर किया था, उनकी इसमें रुचि निरंतर घटती गई। ‘डेबॅनेअ’ ने बचाव की जोरदार पैरवी की और निसीम इज़ेंकिअल तथा विजय तेन्दुलकर सरीखे लेखकों ने मेरे पक्ष में अदालत में बयान दिए। तब कहीं जाकर जज को मेरी कहानी में कुछ गुण नजर आए और उसने हम सबों को बाइज़्ज़त आरोप-मुक्त कर दिया। आज भी साठ पृष्ठों का फैसला बम्बई कोर्ट के लेखागार में सुरक्षित है।
बहरहाल, मैंने इस कहानी को पुनः प्रकाशित नहीं करवाया। आखिरकार मुझे आत्मरक्षात्मक जो होना पड़ा था। किन्तु लगभग एक वर्ष पूर्व पेन्ग्विन इंडिया ने अपने दसवें वार्षिकोत्सव के क्रम में इसे मेरी रचनाओं के सर्वसंग्रह में सम्मिलित करने का निर्णय किया और मुझे सम्मानित किया। ‘आउटलुक’ नामक पत्रिका के साहित्यालोचक ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि यह कहानी लेखक के व्यक्तित्व के एक रोचक तथा जटिल पक्ष का अनावरण करती है और आशा व्यक्त की कि इसी तरह की और भी रचनाओं की कड़ियाँ जुड़ेगी।
पता नहीं ‘मुट्ठीभर बादाम’ उसी तरह की रचना है या नहीं पर निश्चय ही यह एक भिन्न लघु उपन्यास है एक ऐसा साहित्यिक रूप-विधान जो मेरी शैली और मेरे चित्त के अनुरूप है। केवल फ्रांसीसी (और कभी-कभी अमरीकी भी) साहित्यकारों ने ही लघु उपन्यास की विधा के साथ पूर्ण न्याय किया है। ब्रिटिश उपन्यासकार प्रचुर रूप से लम्बे उपन्यासों को ही तरजीह देते हैं और ब्रिटिश प्रकाशक तो उपन्यासिकाओं को नजर उठा के भी नहीं देखते। वे शब्दों की अधिकता में अपना धन देखते हैं। किन्तु संरचनात्मक कसाव तथा अवधारणा की एकरूपता के कारण लघु उपन्यास का अपना स्थान है जैसा कि कॉनरेड ने अपने उपन्यासों ‘हार्ट ऑफ डार्कनेस’, ‘द शैडो लाइन’, ‘यूथ’ तथा ‘द निगर ऑफ द नारसिसस’ में प्रदर्शित किया है। हालाँकि वह एक पोलैंडवासी था, जो अँगरेजी में लिखता था।
यों तो मैं दूसरा कॉनरेड नहीं बन सकता किन्तु शायद उस उत्कृष्ट कथाकार के संस्कार के कुछ छींटे मुझ पर भी पड़े हों क्योंकि ‘कामी पुरुष’ (द सेन्स्यूअलिस्ट) में विचारमग्नता तथा निराशावाद के कुछ लक्षण मौजूद हैं, जो मेरी रुचि के प्रतिकूल हैं। साथ ही मैंने ‘कथा के अन्दर कथा’ जैसी वर्णन शैली का भी प्रयोग किया है। पहाड़ों में रहने वाला एकान्तवासी मेरी ही आत्मा का दूसरा रूप है-मेरी ‘गुप्त सहभागी’। ‘मुट्ठीभर बादाम’ में ऐसा कोई भी पात्र नहीं है। वहाँ मैं मात्र अपने सामान्य आदरविहीन रूप में हूँ। यह उपन्यास एक लेखक का संवेदनशील तथा कभी-कभी शरारती युवक वाला आत्मचित्र है। या यूँ कहें कि एक शरारती प्रौढ़ लेखक के अपने निश्छल तरुणाई की ओर मुड़ कर देखने का चित्रण है।
रस्किन बॉण्ड
मुट्ठीभर बादाम
एक
यह छत की कोठरी नहीं, एक बड़ा-सा कमरा
था-सामने एक छज्जा
और पीछे एक छोटा-सा बरामदा। यह पुरानी दूकानों के एक समूह, जो आज भी
‘ऐस्टली हॉल’ के नाम से जाना जाता है, की पहली मंजिल
पर था।
भवन के सामने ही शहर की मुख्य सड़क थी, पर इसका अपना प्रवेश-मार्ग जो एक
दीवार से घिरा था-इसे सड़क की पटरी से अलग करता था। भवन के सामने नीम का
एक पेड़ भी था, जिसके फल बरसात के शुरुआती दिनों में धरती पर पैरों तले
पिसकर एक ऐसी गहरी तीखी सुगन्ध फैलाते थे, जिसे मैं भुला नहीं सकता।
मैंने बस पैंतीस रुपए महीने के किराए पर इस कमरे को ले रखा था, जिसका अग्रिम भुगतान उस मजबूत कद-काठी वाली पंजाबी, बेवा को करना होता था, जो नीचे अपनी दूकान चलाती थी। उसकी दूकान में चावल, मसूर और मसाले मिलते थे। पर उन दिनों मैं खाना खुद नहीं बनाता था। समय भी नहीं मिलता था। इसलिए हल्के नाश्ते के लिए सड़क पार जाकर समोसे और वेजिटेबल-पैटी खा लेता था। जब कभी मेरी कहानियों के लिए मुझे अच्छी रकम मिलती, मैं डबलरोटी और सूअर के मांस के कतले पर खर्च करता और स्वयं भी इनके सैंडविच बनाता। मेरे दोस्तों में से कोई भी, जैसे जयशंकर या विलियम मैथिसन, यदि साथ होता तो वह भी कई प्रकार के सैन्डविच बनाता।
मुझे कभी नहीं लगा कि मैं भूखा हूँ। पर मैं निश्चय ही कम वजन का और अल्पपोषित था-सस्ते रेस्तराँ अथवा ढाबों में अनियमित भोजन करता हुआ और बार-बार पेट में उथल-पुथल से पीड़ित। मेरे चार वर्षों के इंग्लैंड प्रवास ने मेरे शारीरिक गठन को जरा भी नहीं सुधारा था क्योंकि वहाँ भी मैं ज़्यादातर हल्के-नाश्ते व शराब-घर के काउंटर पर बिकने वाली चीजों पर ही निर्भर रहता था, जिनमें प्रमुख थे- पावरोटी पर सेंके हुए सेम।
भवन समूह के कोने पर ओरिएण्ट सिनेमा के पास ‘कोमल-दा-रेस्तराँ’ था जिसे एक तोंदियल सिख चलाता था। वह खिड़की से सटी अपनी सीट कभी नहीं छोड़ता था। यहाँ मुझे उचित कीमत पर दाल, चावल और एक गीली सब्जी दो तीन रुपए में खाने को मिल जाती थी।
इस रेस्तराँ के कुछ नियमित ग्राहक थे, जैसे एक कॉलेज प्राध्यापक, एक-दो बिक्रीकर्ता और कभी-कभी सिनेमा-शो के शुरू होने के इन्तज़ार में खड़े लोग। विलियम और जय मेरे पीछे यहाँ तक नहीं आते थे क्योंकि यह रेस्तराँ उनके लिहाज से निम्न स्तर का था-(विलियम एक स्विस था और जय दून स्कूल वाला), न ही यहाँ छात्र या बच्चे ज़्यादा आते थे। वास्तव में यह निम्न-मध्यम वर्गीय लोगों के लिए था-वे पेशेवर लोग जो अब तक क्वाँरे थे और शहर में बाहर खाने के लिए मजबूर। मुझे यहाँ किसी से कोई परेशानी नहीं थी। बल्कि यह स्थान अन्य कारणों से भी मुझे भाता था। मसलन, इसके करीब ही एक समाचार-स्टॉल था, जहाँ से मैं अखबार या कोई पत्रिका खरीदकर भोजन के पहले या बाद उस पर एक सरसरी निगाह डाल पाता था। चूँकि मैंने यह निश्चल कर रखा था कि लेखन कार्य को ही अपनी जीविका का साधन बनाऊँगा इसलिए अँगरेजी के सारे प्रकाशनों, जो देहरा में उपलब्ध थे, को पढ़ना मैंने अपनी ड्यूटी बना ली थी ताकि मैं जान सकूँ कि उनमें से कौन लघु उपन्यास का प्रकाशन करती हैं। आश्चर्यजनक रूप से काफी संख्या में पत्रिकाएँ छोटी कहानियाँ छापती थीं बस कठिनाई यह थी कि पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा नहीं था। औसतन मात्र पच्चीस रुपए प्रति कहानी। प्रति माह दस कहानियों की दर से मुझे ढाई सौ रुपए मिल जाते थे। गुज़ारे के लिए काफी थे।
‘कोमल-दा-रेस्तराँ’ में खाना खाने के बाद मैं ऊपरी बाजार के ‘इंडियाना’ में एक कप कॉफी पीने गया। वहाँ इससे अधिक मेरी औकात के बाहर था। ‘इंडियाना’ फैशनेबल लोगों के लिए था। हर शाम यहाँ तीन वाद्ययंत्रों का एक सेट भी बजता था। आप चाहें तो अपने जोड़े के साथ नृत्य भी कर सकते थे, हालाँकि कपोल-से-कपोल सटाकर नृत्य करने का फैशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो चुका था। दोपहर से लेकर तीन बजे तक देहरादून का नौजवान, लैरी गोम्स, जो असल में गोआ का था, पियानो पर अपने प्रिय गीतों अथवा नई सफल लोकप्रिय धुनों को बजाता रहता था।
उस बासन्ती सुबह केवल एक-दो टेबल ही भरे थे-सिर्फ व्यवसायी लोग जिनकी संगीत में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए लैरी ने मेरी खातिर कुछ पुरानी धुनें छेड़ दीं, जैसे ‘सेप्टेम्बर सौंग’ और ‘आई विल सी यू अगेन’। बीस की उम्र में मैं बड़े ही पुराने ख़यालों का था। लैरी को प्रति माह तीन सौ रुपए मिलते थे और साथ में एक बार का खाना मुफ्त। इसलिए उसकी माली हालत मुझसे कुछ बेहतर थी। पास ही उसके पिता की एक संगीत एवं गीत के रेकॉर्डों की दूकान भी थी।
जब मैं कॉफी की चुस्की लेता हुआ अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार कर रहा था-(जिसकी कोई पहचान नहीं थी क्योंकि मेरे पास धन था ही नहीं) तभी मेगाडोर की दौलतमंद और फूली-फूली आँखों वाली महारानी ने अपनी पुत्री के साथ प्रवेश किया। मैं उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ और बदले में उन्होंने एक कृपापूर्ण मुस्कान फेंकी।
वह जानती थी कि पाँच वर्ष पूर्व जब मैं स्कूल के अन्तिम वर्ष में था तो उनकी पुत्री पर मोहित हो गया था। उन्होंने मेरा एक प्रेम-पत्र बीच में ही पकड़ भी लिया था, हालाँकि इसे उन्होंने बड़ी सहजता से लिया और मुझे कहा कि मैंने एक अच्छा पत्र लिखा था। वह जानती थीं कि अब मैं पत्र-पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ लिखा करता हूँ। उन्होंने कहा, ‘हम लोगों ने तुम्हारी कहानी पिछले सप्ताह ‘वीकली’ पत्रिका में पढ़ी। काफी आकर्षक थी। मैंने कहा न था कि तुम एक अच्छे लेखक बनोगे !’ मैं शरमा गया पर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया जबकि इन्दु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह अब भी कॉलेज में पढ़ती थी।
‘किसी दिन हमारे घर जाओ !’ महारानी ने कहा और शाही अन्दाज में आगे बढ़ गईं। दुबली-पतली ठिगनी इन्दु जो नीली-पोशाक में थी, पहले कभी इतनी तितलीनुमा नहीं लगी-कोमल, नाजुक, छूने के विचार से ही फुर्र हो जाने वाली।
कोने में एक टेबल पर बैठ गईं और मैं लौट आया, मेजपोश पर फैल गए कॉफी के धब्बे के मुतल्लिक अपने विचारों में। वास्तव में मैंने अपनी कॉफी के छींटे चारों तरफ फैला लिये थे।
लैरी ने मेरी उलझन भाँप ली थी और इसके कारण के विषय में अटकलें लगाता हुआ एक बहुत पुरानी धुन छेड़ दी जो सिर्फ इन्दु की माँ ही पहचान सकती थीं-‘‘आई किस योर लिटल हैंड्स मैडम, आई लौंग टु किस योर लिप्स...’
जब मैं बाहर निकल रहा था लैरी ने मेरी आँखों में झाँका और आँख मार दी।
‘तुम्हारी बख्शीश दूसरी बार !’ मैंने कहा।
‘उसे वेटर के लिए बचा कर रखो !’ लैरी ने जवाब दिया।
यह अप्रैल की गर्म धूप थी और मैं अपने कमरे की तरफ इस ख़्वाहिश के साथ चल पड़ा कि काश पंखे की सुविधा होती।
मैं गंजी और अण्डरवीयर में बिस्तर पर लेट गया और छत की तरफ एकटक देखने लगा। छत भी मेरी ओर देख रही थी। मैंने करवट बदल कर छज्जे के पार नीम के पत्तों की तरफ देखा। वे पूर्णतः स्थिर थे। हवा की कोई उम्मीद भी न थी।
मुझे झपकी-सी लगी और सपने में मैंने अपनी राजकुमारी को देखा-उसकी गहरी काली आँखें और कपोलों पर छिटकी शरद की चाँदनी। मैंने देखा हमलोग धवल चाँदनी के तालाब में स्नान कर रहे थे और सोने तथा चाँदी की मछलियाँ और सीपियाँ हमारी जाँघों के बीच में से निकल-निकल जाती थीं। झरने के ताजे जल से मैंने उसके सुन्दर अंगों को धोया और जवाकुसम के फूल उसके सुनहरे उरोजों के बीच तथा कान के पीछे लगा दिया। कामुकता से भरकर मैंने अपने आप को उस पर पूरी तरह डाल दिया और वह चाँदी की परतों वाली मछली में रुपान्तरित हो गई।
जब मैंने आँखें खोली धोबी-पुत्र सीताराम को अपने पायताने बैठा पाया। सीताराम लगभग सोलह वर्ष का होगा-दुबला पतला, लम्बे हाथ-पाँव और बड़े-बड़े कान। उसके होंठ खुले और कामुक थे-एक अनाकर्षक युवक जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी। किन्तु चूँकि वह मेरे फ्लैट के पिछवाड़े वाले आवास में ही अपने माता-पिता के साथ रहता था इसलिए उससे बचना मुश्किल था।
‘तुम यहाँ कैसे घुस आए ?’ मैंने रूखा-सा सवाल किया।
‘किवाड़ खुले थे।’
‘इसका यह अर्थ नहीं कि तुम सीधे अन्दर चले आओ। क्या बात है ?’
‘क्या आपको कपड़े नहीं धुलवाने हैं ? मेरे बापू ने पूछा है।’
‘मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ।’
‘और चादर ?’ उसने चादर को जिसपर मैं लेटा था, गौर से देखा। ‘आप अपनी चादर नहीं धोते ?’ यह तो बहुत गन्दी है।’
‘असल में मेरे पास बस यही एक चादर है। अच्छा, तुम अब कहीं और जाकर भनभनाओ।’
लेकिन उसने तो मेरे नीचे से चादर खींचना शुरू कर दिया था। ‘मैं इसे आपके लिए मुफ्त में धो दूँगा आप बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ कहती है कि आप सीधे-सादे हैं, एकदम निर्दोष।’
‘मैं निर्दोष नहीं हूँ और मुझे चादर की आवश्यकता है।’
‘मैं आपके लिए दूसरी ला दूँगा। यह उधार भी मुफ्त का होगा। हमें बहुत से चादर धोने को मिलते हैं। कल ही अस्पताल से छः चादर आए। कुछ लोग बस-दुर्घटना में मर गए थे।’
‘तुम्हारा मतलब है, चादर मुर्दाघर की है जो शवों को ढकने के काम आती है ? मुझे मुर्दाघर की चादर नहीं चाहिए।’
‘लेकिन वे बहुत साफ हैं। आपको पता है, शवों पर खटमल नहीं होते। वे ताजा खून पसन्द करते हैं।’
वह मेरी चादर ले गया और पाँच मिनट बाद इस्तरी की हुई दूसरी चादर ले आया।
‘बेफिक्र रहिए, उसने कहा, ‘यह अस्पताल की नहीं है।’
‘फिर कहाँ की है ?’
‘‘इंडियाना’ होटल की। मैं उन्हें अस्पताल वाली एक चादर बदले में दे दूँगा।’
मैंने बस पैंतीस रुपए महीने के किराए पर इस कमरे को ले रखा था, जिसका अग्रिम भुगतान उस मजबूत कद-काठी वाली पंजाबी, बेवा को करना होता था, जो नीचे अपनी दूकान चलाती थी। उसकी दूकान में चावल, मसूर और मसाले मिलते थे। पर उन दिनों मैं खाना खुद नहीं बनाता था। समय भी नहीं मिलता था। इसलिए हल्के नाश्ते के लिए सड़क पार जाकर समोसे और वेजिटेबल-पैटी खा लेता था। जब कभी मेरी कहानियों के लिए मुझे अच्छी रकम मिलती, मैं डबलरोटी और सूअर के मांस के कतले पर खर्च करता और स्वयं भी इनके सैंडविच बनाता। मेरे दोस्तों में से कोई भी, जैसे जयशंकर या विलियम मैथिसन, यदि साथ होता तो वह भी कई प्रकार के सैन्डविच बनाता।
मुझे कभी नहीं लगा कि मैं भूखा हूँ। पर मैं निश्चय ही कम वजन का और अल्पपोषित था-सस्ते रेस्तराँ अथवा ढाबों में अनियमित भोजन करता हुआ और बार-बार पेट में उथल-पुथल से पीड़ित। मेरे चार वर्षों के इंग्लैंड प्रवास ने मेरे शारीरिक गठन को जरा भी नहीं सुधारा था क्योंकि वहाँ भी मैं ज़्यादातर हल्के-नाश्ते व शराब-घर के काउंटर पर बिकने वाली चीजों पर ही निर्भर रहता था, जिनमें प्रमुख थे- पावरोटी पर सेंके हुए सेम।
भवन समूह के कोने पर ओरिएण्ट सिनेमा के पास ‘कोमल-दा-रेस्तराँ’ था जिसे एक तोंदियल सिख चलाता था। वह खिड़की से सटी अपनी सीट कभी नहीं छोड़ता था। यहाँ मुझे उचित कीमत पर दाल, चावल और एक गीली सब्जी दो तीन रुपए में खाने को मिल जाती थी।
इस रेस्तराँ के कुछ नियमित ग्राहक थे, जैसे एक कॉलेज प्राध्यापक, एक-दो बिक्रीकर्ता और कभी-कभी सिनेमा-शो के शुरू होने के इन्तज़ार में खड़े लोग। विलियम और जय मेरे पीछे यहाँ तक नहीं आते थे क्योंकि यह रेस्तराँ उनके लिहाज से निम्न स्तर का था-(विलियम एक स्विस था और जय दून स्कूल वाला), न ही यहाँ छात्र या बच्चे ज़्यादा आते थे। वास्तव में यह निम्न-मध्यम वर्गीय लोगों के लिए था-वे पेशेवर लोग जो अब तक क्वाँरे थे और शहर में बाहर खाने के लिए मजबूर। मुझे यहाँ किसी से कोई परेशानी नहीं थी। बल्कि यह स्थान अन्य कारणों से भी मुझे भाता था। मसलन, इसके करीब ही एक समाचार-स्टॉल था, जहाँ से मैं अखबार या कोई पत्रिका खरीदकर भोजन के पहले या बाद उस पर एक सरसरी निगाह डाल पाता था। चूँकि मैंने यह निश्चल कर रखा था कि लेखन कार्य को ही अपनी जीविका का साधन बनाऊँगा इसलिए अँगरेजी के सारे प्रकाशनों, जो देहरा में उपलब्ध थे, को पढ़ना मैंने अपनी ड्यूटी बना ली थी ताकि मैं जान सकूँ कि उनमें से कौन लघु उपन्यास का प्रकाशन करती हैं। आश्चर्यजनक रूप से काफी संख्या में पत्रिकाएँ छोटी कहानियाँ छापती थीं बस कठिनाई यह थी कि पारिश्रमिक बहुत ज़्यादा नहीं था। औसतन मात्र पच्चीस रुपए प्रति कहानी। प्रति माह दस कहानियों की दर से मुझे ढाई सौ रुपए मिल जाते थे। गुज़ारे के लिए काफी थे।
‘कोमल-दा-रेस्तराँ’ में खाना खाने के बाद मैं ऊपरी बाजार के ‘इंडियाना’ में एक कप कॉफी पीने गया। वहाँ इससे अधिक मेरी औकात के बाहर था। ‘इंडियाना’ फैशनेबल लोगों के लिए था। हर शाम यहाँ तीन वाद्ययंत्रों का एक सेट भी बजता था। आप चाहें तो अपने जोड़े के साथ नृत्य भी कर सकते थे, हालाँकि कपोल-से-कपोल सटाकर नृत्य करने का फैशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो चुका था। दोपहर से लेकर तीन बजे तक देहरादून का नौजवान, लैरी गोम्स, जो असल में गोआ का था, पियानो पर अपने प्रिय गीतों अथवा नई सफल लोकप्रिय धुनों को बजाता रहता था।
उस बासन्ती सुबह केवल एक-दो टेबल ही भरे थे-सिर्फ व्यवसायी लोग जिनकी संगीत में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए लैरी ने मेरी खातिर कुछ पुरानी धुनें छेड़ दीं, जैसे ‘सेप्टेम्बर सौंग’ और ‘आई विल सी यू अगेन’। बीस की उम्र में मैं बड़े ही पुराने ख़यालों का था। लैरी को प्रति माह तीन सौ रुपए मिलते थे और साथ में एक बार का खाना मुफ्त। इसलिए उसकी माली हालत मुझसे कुछ बेहतर थी। पास ही उसके पिता की एक संगीत एवं गीत के रेकॉर्डों की दूकान भी थी।
जब मैं कॉफी की चुस्की लेता हुआ अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार कर रहा था-(जिसकी कोई पहचान नहीं थी क्योंकि मेरे पास धन था ही नहीं) तभी मेगाडोर की दौलतमंद और फूली-फूली आँखों वाली महारानी ने अपनी पुत्री के साथ प्रवेश किया। मैं उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ और बदले में उन्होंने एक कृपापूर्ण मुस्कान फेंकी।
वह जानती थी कि पाँच वर्ष पूर्व जब मैं स्कूल के अन्तिम वर्ष में था तो उनकी पुत्री पर मोहित हो गया था। उन्होंने मेरा एक प्रेम-पत्र बीच में ही पकड़ भी लिया था, हालाँकि इसे उन्होंने बड़ी सहजता से लिया और मुझे कहा कि मैंने एक अच्छा पत्र लिखा था। वह जानती थीं कि अब मैं पत्र-पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ लिखा करता हूँ। उन्होंने कहा, ‘हम लोगों ने तुम्हारी कहानी पिछले सप्ताह ‘वीकली’ पत्रिका में पढ़ी। काफी आकर्षक थी। मैंने कहा न था कि तुम एक अच्छे लेखक बनोगे !’ मैं शरमा गया पर मैंने उन्हें धन्यवाद दिया जबकि इन्दु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह अब भी कॉलेज में पढ़ती थी।
‘किसी दिन हमारे घर जाओ !’ महारानी ने कहा और शाही अन्दाज में आगे बढ़ गईं। दुबली-पतली ठिगनी इन्दु जो नीली-पोशाक में थी, पहले कभी इतनी तितलीनुमा नहीं लगी-कोमल, नाजुक, छूने के विचार से ही फुर्र हो जाने वाली।
कोने में एक टेबल पर बैठ गईं और मैं लौट आया, मेजपोश पर फैल गए कॉफी के धब्बे के मुतल्लिक अपने विचारों में। वास्तव में मैंने अपनी कॉफी के छींटे चारों तरफ फैला लिये थे।
लैरी ने मेरी उलझन भाँप ली थी और इसके कारण के विषय में अटकलें लगाता हुआ एक बहुत पुरानी धुन छेड़ दी जो सिर्फ इन्दु की माँ ही पहचान सकती थीं-‘‘आई किस योर लिटल हैंड्स मैडम, आई लौंग टु किस योर लिप्स...’
जब मैं बाहर निकल रहा था लैरी ने मेरी आँखों में झाँका और आँख मार दी।
‘तुम्हारी बख्शीश दूसरी बार !’ मैंने कहा।
‘उसे वेटर के लिए बचा कर रखो !’ लैरी ने जवाब दिया।
यह अप्रैल की गर्म धूप थी और मैं अपने कमरे की तरफ इस ख़्वाहिश के साथ चल पड़ा कि काश पंखे की सुविधा होती।
मैं गंजी और अण्डरवीयर में बिस्तर पर लेट गया और छत की तरफ एकटक देखने लगा। छत भी मेरी ओर देख रही थी। मैंने करवट बदल कर छज्जे के पार नीम के पत्तों की तरफ देखा। वे पूर्णतः स्थिर थे। हवा की कोई उम्मीद भी न थी।
मुझे झपकी-सी लगी और सपने में मैंने अपनी राजकुमारी को देखा-उसकी गहरी काली आँखें और कपोलों पर छिटकी शरद की चाँदनी। मैंने देखा हमलोग धवल चाँदनी के तालाब में स्नान कर रहे थे और सोने तथा चाँदी की मछलियाँ और सीपियाँ हमारी जाँघों के बीच में से निकल-निकल जाती थीं। झरने के ताजे जल से मैंने उसके सुन्दर अंगों को धोया और जवाकुसम के फूल उसके सुनहरे उरोजों के बीच तथा कान के पीछे लगा दिया। कामुकता से भरकर मैंने अपने आप को उस पर पूरी तरह डाल दिया और वह चाँदी की परतों वाली मछली में रुपान्तरित हो गई।
जब मैंने आँखें खोली धोबी-पुत्र सीताराम को अपने पायताने बैठा पाया। सीताराम लगभग सोलह वर्ष का होगा-दुबला पतला, लम्बे हाथ-पाँव और बड़े-बड़े कान। उसके होंठ खुले और कामुक थे-एक अनाकर्षक युवक जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी। किन्तु चूँकि वह मेरे फ्लैट के पिछवाड़े वाले आवास में ही अपने माता-पिता के साथ रहता था इसलिए उससे बचना मुश्किल था।
‘तुम यहाँ कैसे घुस आए ?’ मैंने रूखा-सा सवाल किया।
‘किवाड़ खुले थे।’
‘इसका यह अर्थ नहीं कि तुम सीधे अन्दर चले आओ। क्या बात है ?’
‘क्या आपको कपड़े नहीं धुलवाने हैं ? मेरे बापू ने पूछा है।’
‘मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ।’
‘और चादर ?’ उसने चादर को जिसपर मैं लेटा था, गौर से देखा। ‘आप अपनी चादर नहीं धोते ?’ यह तो बहुत गन्दी है।’
‘असल में मेरे पास बस यही एक चादर है। अच्छा, तुम अब कहीं और जाकर भनभनाओ।’
लेकिन उसने तो मेरे नीचे से चादर खींचना शुरू कर दिया था। ‘मैं इसे आपके लिए मुफ्त में धो दूँगा आप बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ कहती है कि आप सीधे-सादे हैं, एकदम निर्दोष।’
‘मैं निर्दोष नहीं हूँ और मुझे चादर की आवश्यकता है।’
‘मैं आपके लिए दूसरी ला दूँगा। यह उधार भी मुफ्त का होगा। हमें बहुत से चादर धोने को मिलते हैं। कल ही अस्पताल से छः चादर आए। कुछ लोग बस-दुर्घटना में मर गए थे।’
‘तुम्हारा मतलब है, चादर मुर्दाघर की है जो शवों को ढकने के काम आती है ? मुझे मुर्दाघर की चादर नहीं चाहिए।’
‘लेकिन वे बहुत साफ हैं। आपको पता है, शवों पर खटमल नहीं होते। वे ताजा खून पसन्द करते हैं।’
वह मेरी चादर ले गया और पाँच मिनट बाद इस्तरी की हुई दूसरी चादर ले आया।
‘बेफिक्र रहिए, उसने कहा, ‘यह अस्पताल की नहीं है।’
‘फिर कहाँ की है ?’
‘‘इंडियाना’ होटल की। मैं उन्हें अस्पताल वाली एक चादर बदले में दे दूँगा।’
दो
बगीचे दूधिया चाँदनी में नहाए हुए थे।
देहरा की सँकरी पुरानी सड़कों पर चहलकदमी करते हुए मैं महारानी के भवन के सामने रुका और कम ऊँची चारदीवारी के अन्दर झाँका। कुछ कमरे अब भी रोशन थे। कुछ क्षण रुकने पर इन्दु खिड़की के पास आती दिखी। उसके हाथ में एक पुस्तक देख मैंने अनुमान लगाया कि वह पढ़ रही थी। हो सकता था यदि मैं उसे अपनी कविता भेजता तो वह उसे पढ़ती। एक छोटे क्वाँरे लाल गुलाब वाली कविता।
लेकिन इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे।
मैं बाजार की तरफ लौट पड़ा-सिनेमा हॉलों की चमकीली रोशनी और छोटे-छोटे भोजनलय। बस आठ बजे थे। सड़क अब भी भीड़ भरी थी। अब यहाँ सवारियों की भरमार है, कभी केवल लोग हुआ करते थे। और इसीलिए लोग से लोग टकरा जाते थे-परिचित भी, अजनबी भी।
मैं भारतीय सिने तारिकाओं में सबसे अधिक सेक्सी दिखने वाली निम्मी के इस्तेहार देख रहा था, जब एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मुड़ा तो जयशंकर खड़ा था, दून स्कूल का प्रतिभाशाली छात्र जिसके पिता ‘न्यू अम्पायर’ सिनेमा के मालिक थे।
‘जलेबियाँ, रस्किन, जलेबियाँ,’ वह गुनगुनाया। हालाँकि वह एक सम्पन्न परिवार का था पर ऐसा कभी नहीं लगा कि उसके पास जेब-खर्च के लिए पैसे थे। वैसे भी एक गरीब आदमी से उधार मिलना आसान होता है किसी अमीर की तुलना में। पता नहीं, ऐसा क्यों होता है ? उदाहरण के लिए विलियम मैथिसन को ही ले लें। वह एक ऊँचे स्तर के महँगे छात्रावास में रहता था पर हमेशा मुझसे पैसे मागँता रहता था-कभी लॉन्ड्री-बिल के भुगतान के लिए तो कभी चारमीनार सिगरेट के लिए जिसके बिना वह बेचैन और उत्तेजित हो जाता था। यही बात जयशंकर के मामले में जलेबी से जुड़ी थी...
‘कई सप्ताह से मुझे कोई चेक नहीं मिला है।’ मैंने उसे बताया।
‘बी.बी.सी के लिए जो कहानी तुम लिख रहे थे उसका क्या हुआ ?’
‘वो तो मैंने अभी-अभी भेजा है।’
‘और जो उपन्यास तुम लिख रहे थे ?’
‘मैं अभी लिख ही रहा हूँ।’
‘जलेबी में तो मात्र दो रुपए लगेंगे।’
‘ओह,....ठीक है...’
जयशंकर ने पेट भर ठूँस कर जलेबी खाया जबकि मुझे बस एक समोसे पर संतोष करना पड़ा। जय एक कलाकार बनना चाहता था, एक कवि, एक दैनिकी-लेखक, आंद्र जीत् की तरह। उसने मुझे आंद्र जीत् लिखित ‘फ्रूट्स ऑफ द अर्थ’ की एक प्रति भी दी थी ताकि मैं भी उसी दिशा में प्रभावित हो सकूँ। वह आज चालीस वर्ष बाद भी मेरे पास है, जिसके शीर्षक-पृष्ठ पर मकड़ीदार लिखावट में घिसटा उसका संदेश और नृत्य करती परी का चित्र अंकित है। हमारी प्रिय पुस्तकें हमारे सपनों से ज्यादा दीर्घायु होती हैं...
देहरा की सँकरी पुरानी सड़कों पर चहलकदमी करते हुए मैं महारानी के भवन के सामने रुका और कम ऊँची चारदीवारी के अन्दर झाँका। कुछ कमरे अब भी रोशन थे। कुछ क्षण रुकने पर इन्दु खिड़की के पास आती दिखी। उसके हाथ में एक पुस्तक देख मैंने अनुमान लगाया कि वह पढ़ रही थी। हो सकता था यदि मैं उसे अपनी कविता भेजता तो वह उसे पढ़ती। एक छोटे क्वाँरे लाल गुलाब वाली कविता।
लेकिन इससे मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे।
मैं बाजार की तरफ लौट पड़ा-सिनेमा हॉलों की चमकीली रोशनी और छोटे-छोटे भोजनलय। बस आठ बजे थे। सड़क अब भी भीड़ भरी थी। अब यहाँ सवारियों की भरमार है, कभी केवल लोग हुआ करते थे। और इसीलिए लोग से लोग टकरा जाते थे-परिचित भी, अजनबी भी।
मैं भारतीय सिने तारिकाओं में सबसे अधिक सेक्सी दिखने वाली निम्मी के इस्तेहार देख रहा था, जब एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मुड़ा तो जयशंकर खड़ा था, दून स्कूल का प्रतिभाशाली छात्र जिसके पिता ‘न्यू अम्पायर’ सिनेमा के मालिक थे।
‘जलेबियाँ, रस्किन, जलेबियाँ,’ वह गुनगुनाया। हालाँकि वह एक सम्पन्न परिवार का था पर ऐसा कभी नहीं लगा कि उसके पास जेब-खर्च के लिए पैसे थे। वैसे भी एक गरीब आदमी से उधार मिलना आसान होता है किसी अमीर की तुलना में। पता नहीं, ऐसा क्यों होता है ? उदाहरण के लिए विलियम मैथिसन को ही ले लें। वह एक ऊँचे स्तर के महँगे छात्रावास में रहता था पर हमेशा मुझसे पैसे मागँता रहता था-कभी लॉन्ड्री-बिल के भुगतान के लिए तो कभी चारमीनार सिगरेट के लिए जिसके बिना वह बेचैन और उत्तेजित हो जाता था। यही बात जयशंकर के मामले में जलेबी से जुड़ी थी...
‘कई सप्ताह से मुझे कोई चेक नहीं मिला है।’ मैंने उसे बताया।
‘बी.बी.सी के लिए जो कहानी तुम लिख रहे थे उसका क्या हुआ ?’
‘वो तो मैंने अभी-अभी भेजा है।’
‘और जो उपन्यास तुम लिख रहे थे ?’
‘मैं अभी लिख ही रहा हूँ।’
‘जलेबी में तो मात्र दो रुपए लगेंगे।’
‘ओह,....ठीक है...’
जयशंकर ने पेट भर ठूँस कर जलेबी खाया जबकि मुझे बस एक समोसे पर संतोष करना पड़ा। जय एक कलाकार बनना चाहता था, एक कवि, एक दैनिकी-लेखक, आंद्र जीत् की तरह। उसने मुझे आंद्र जीत् लिखित ‘फ्रूट्स ऑफ द अर्थ’ की एक प्रति भी दी थी ताकि मैं भी उसी दिशा में प्रभावित हो सकूँ। वह आज चालीस वर्ष बाद भी मेरे पास है, जिसके शीर्षक-पृष्ठ पर मकड़ीदार लिखावट में घिसटा उसका संदेश और नृत्य करती परी का चित्र अंकित है। हमारी प्रिय पुस्तकें हमारे सपनों से ज्यादा दीर्घायु होती हैं...
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book