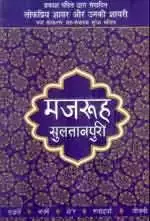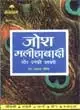|
गजलें और शायरी >> लोकप्रिय शायर और उनकी शायरी - मज़रूह सुल्तानपुरी लोकप्रिय शायर और उनकी शायरी - मज़रूह सुल्तानपुरीप्रकाश पंडित
|
245 पाठक हैं |
||||||
मजरूह सुल्तानपुरी की जिन्दगी और उनकी बेहतरीन गजलें, नज्में, शेर और रुबाइयां
Majrur sultanpuri Aur Unki Shayari
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
उर्दू के लोकप्रिय शायर
वर्षों पहले नागरी लिपि में उर्दू की चुनी हुई शायरी के संकलन प्रकाशित कर राजपाल एण्ड सन्ज ने पुस्तक प्रकाशन की दुनिया में एक नया कदम उठाया था। उर्दू लिपि न जानने वाले लेकिन शायरी को पसंद करने वाले अनगिनत लोगों के लिए यह एक बड़ी नियामत साबित हुआ और सभी ने इससे बहुत लाभ उठाया।
ज्यादातर संकलन उर्दू के सुप्रसिद्ध सम्पादक प्रकाश पंडित ने किये हैं। उन्होंने शायर के सम्पूर्ण लेखन से चयन किया है और कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दे दिये हैं। इसी के साथ, शायर के जीवन और कार्य पर-जिनमें से समकालीन उनके परिचित ही थे-बहुत रोचक और चुटीली भूमिकाएं लिखी हैं। ये बोलती तस्वीरें हैं जो सोने में सुहागे का काम करती हैं।
ज्यादातर संकलन उर्दू के सुप्रसिद्ध सम्पादक प्रकाश पंडित ने किये हैं। उन्होंने शायर के सम्पूर्ण लेखन से चयन किया है और कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दे दिये हैं। इसी के साथ, शायर के जीवन और कार्य पर-जिनमें से समकालीन उनके परिचित ही थे-बहुत रोचक और चुटीली भूमिकाएं लिखी हैं। ये बोलती तस्वीरें हैं जो सोने में सुहागे का काम करती हैं।
मजरूह सुलतानपुरी
मजरूह न केवल हमें ग़ज़ल की प्राचीन परम्पराओं का उत्तराधिकारी नज़र आता है बल्कि उसके यहां हमें ऐतिहासिक सच्चाइयों की भी सुन्दर झलक मिलती है। ख़िज़ा, बहार, साक़ी, महफ़िल, शराब, पैमाना, गुल, गुलिस्तां, सय्याद इत्यादि परम्परागत शब्दों द्वारा मजरूह ने बड़ी कलाकौशलता से अपना काम निकाला है। मजरूह ने आवश्यकतानुसार इन शब्दों के लिबास में कुछ नये शब्दों द्वारा और भी रंगीनी और ख़ूबसूरती पैदा करने की कोशिश की है।
अब खुलके कहूंगा हर ग़मे-दिल मज़रूह नहीं वो वक़्त कि जब
अश्कों में सुनाता था मुझको आहों में ग़ज़ल-ख़्वां होना था
वही मजरूह समझे सब जिसे आवारा-ए-ज़ुल्मत1
वही है एक शमए-सुर्ख़ का2 परवाना बरसों से
बम्बई में यह 25 दिसम्बर, 1958 कि रात है। और यह उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिशील शायर सरदार जाफ़री का घर है। क्रिस्मस की रात मनाने शायर और अदीब आ रहे हैं। क्षण-भर के लिए अफ़सोस होता है कि मां के आपरेशन के कारण कृश्नचन्दर यहां आने के बजाय आज ही दिल्ली चले गये। एक क्षण के लिए अफ़सोस होता है कि किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के कारण राजेन्द्रसिंह बेदी और ख़्वाजा अहमद अब्बास भी नहीं आ रहे। लेकिन कुछ क्षण के बाद यह अफ़सोस खुशी में बदल जाता है जब डाक्टर मुल्कराज आनन्द आ जाते हैं। इस्मत चुग़ताई और उनके पति शाहिद लतीफ़ आ जाते हैं। नख़शब जार्जवी और जांनिसार अख़्तर आ जाते हैं। साहिर लुधियानवी और प्रकाश पण्डित आ जाते हैं। गप्पे हो रही हैं। मज़ाक़ हो रहे हैं। डाक्टर आनन्द इस्मत और शाहिद लतीफ़ में झगड़ा कराने की विफल कोशिश कर रहे हैं। इस्मत साहिर और मजरूह में झगड़ा कराने की विफल कोशिश कर रही हैं। यहां तक की हर कोई हर किसी के साथ झगड़ा करने की विफल कोशिश कर रहा है। हर कोशिश चूंकि विफल जा रही है इसलिए बला का शोर मच रहा है और टेप-रिकार्डर पर इस ऐतिहासिक बैठक की हर आवाज़ रिकार्ड हो रही है। एकाएक मजरूह की आवाज़
----------------------------------------------------
1.अंधेरों में भटकने वाला 2.(सुर्ख) समाजवादी दीपक का
सब आवाज़ों पर छा जाती है। फिर धीरे-धीरे सब आवाज़ें उसकी आवाज़ में विलीन हो जाती हैं और सब-के-सब उसकी ग़ज़ल पर सिर धुनने लगते हैं।
मजरूह ग़ज़ल का शायर है और उसका कहना है कि वह अपनी ग़ज़लों में इस बात को साबित कर देता है कि मौजूदा ज़माने के मसाइल (समस्याओं) को शायराना रूप देने के लिए ग़ज़ल नामौजूं (अनुपयुक्त) नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी मंज़िलें भी हैं जहां सिर्फ़ ग़ज़ल ही शायर का साथ दे सकती है। हालांकि उर्दू के एक समालोचक कलीम-उल्ला की नज़र में ग़ज़ल एक नीम-वहशी (अर्धसभ्य) काव्य-रूप है और कुछ वर्ष पूर्व कुछ प्रगतिशील साहित्यकारों ने भी इसे मरते हुए सामन्ती समाज का अंग और केवल आत्मभाव (Subjectiveness) का चमत्कार कहकर इसके उन्मूलन की माँग की थी।
लगभग इसी प्रकार की एक मांग रूस की क्रांति से पहले कुछ क्रांतिकारी युवकों ने भी की थी। वे अतीत की समस्त अच्छी-बुरी परम्पराओं को रूढ़ि और सामन्त-काल की जूठन कहकर उन्हें समाप्त कर डालने पर तुल गये थे और इस सम्बन्ध में कोई सैद्धान्तिक युक्ति भी सुनने को तैयार न थे। अतएव जब वहां के महान लेखक तुर्गनेव ने अपने उपन्यासों में ऐसे संकीर्णतावादी पात्रों के प्रस्तुत करना और उनका खेदजनक परिणाम दिखाना शुरू किया तो उन युवकों ने उसे रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, बल्कि क्रांति-विरोधी तक कह डाला और मुतालबा किया कि उसकी समस्त पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाय क्योंकि उनके अध्ययन से क्रान्तिकारी युवकों के भटकने की सम्भावना है।
क्रान्ति से छिछला लगाव रखनेवाले भारतीय लेखक भी ग़ज़ल के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए इस तात्विक सिद्धांत को भूल गये कि हर नई चीज़ पुरानी कोख से जन्म लेती है। भाषा तथा साहित्य और संस्कृति तथा सभ्यता से लेकर शारीरिक वस्त्रों तक कोई चीज़ शून्य में आगे नहीं बढ़ती बल्कि इसे अपने पिछले फ़ैशन का सहारा लेना पड़ता है। और जहां तक आत्मभाव का संबंध है, आत्मभाव किसी चिकने घड़े का नाम नहीं है बल्कि आत्मभाव भी पदार्थ-विषयता का प्रतिबिम्ब होती है। अपने मन की दुनिया में रहना किसी पागल के लिए तो सम्भव है लेकिन कोई चेतन व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इन जोशीले लेकिन विमूढ़ साहित्यकारों के बारे में, जो पुरानेपन के इतने विरोधी थे, उर्दू के एक समालोचक ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि उन्होंने टब के गंदले पानी के साथ-साथ और बच्चो को भी फेंक देने की ठान ली थी।
सौभाग्यवश उर्दू के उन संकीर्णतावादी साहित्यकारों ने बहुत शीघ्र अपनी भूल स्वीकार कर ली और साहित्य, इतिहास और सामाजिक परिस्थितियों के गहरे अध्ययन और निरीक्षण के बाद अब वे बच्चे और टब को नहीं, केवल टब के गंदले पानी को फेंकने और उसकी जगह निर्मल और स्वच्छ पानी भरने के लिए प्रयत्नशील हैं।
यह ठीक है कि उर्दू शायरी का एक विशेष रूप होने के कारण ग़ज़ल की कुछ अपनी विशेष परम्पराएं हैं और वह सामन्त-काल की उपज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग़ज़ल की परम्पराओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या नहीं हो सकता। विश्व, समाज और मानव-जीवन की प्रत्येक वस्तु की तरह ग़ज़ल की परम्पराओं में भी बराबर परिवर्तन होता रहा है और मीर, सौदा, दर्द, मोमिन, ग़ालिब, दाग़ के कलाम के क्रमशः अध्ययन से हम इस परिवर्तन या विकास की रूप-रेखा देख सकते जागीरदारी के पतन और इस कारण ग़ज़ल की अधोगति के बाद बीसवीं सदी में जिन शायरों ने ग़ज़ल की रूढ़िगत परम्पराओं में परिवर्तन लाने के सफल प्रयत्न किये, उनमें हसरत मोहानी, इक़बाल, जिगर, फ़िराक़, मजाज़, फ़ैज़, और जज़्बी के नाम सबसे ऊपर हैं। इस प्रसंग में मजरूह सुलतानपुरी ग़ज़ल के क्षेत्र में नवागन्तुक है।
मजरूह सुलतानपुरी ग़ज़ल के क्षेत्र में नवागन्तुक अवश्य है लेकिन अनाड़ी नहीं। उर्दू ग़ज़ल के शयनागार में वह एक सिमटी-सिमटाई लजीली दुल्हन की तरह नहीं बल्कि एक निडर और बेबाक दूल्हे की तरह दाख़िल हुआ है और कुछ ऐसे स्वाभिमान के साथ दाख़िल हुआ है कि शयनागार का मदमाता वातावरण चकाचौंध प्रकाश में परिवर्तित हो गया।
इस सम्बन्ध में मजरूह के कविता-संग्रह ग़ज़ल में मजरूह का परिचय कराते हुए सरदार जाफ़री ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि :
एक और ख़ुसूसियत (विशेषता) जो मजरूह को आ़म ग़ज़ल-गो शायरों से मुम्ताज़ (विशिष्ट) करती है, यह है कि उसने समाजी और सियासी मौज़ूआत (विषयों) को बड़ी कामियाबी के साथ ग़ज़ल के पैराया (शैली) में ढाल लिया है। आ़म तौर पर ग़ज़लगो शायरी समाजी और सियासी मौज़ूआत के बयान में फीके-सीठे हो जाते हैं या उनका अन्दाज़े-बयां (वर्णन-शैली) ऐसा हो जाता है कि नज़्म और ग़ज़ल का फ़र्क बाक़ी नहीं रहता। मजरूह के यहां यह बात नहीं है।
और इस कविता-संग्रह की प्रस्तावना में स्वर्गीय क़ाज़ी अब्दुल ग़फ़्फ़ार लिखते हैं :
हिन्दोस्तान की नौजवान नस्ल के आतिशख़ाने (अग्निकुंड) से जो चिंगारियां निकल रही हैं, उनमें एक बहुत रौशन चिंगारी मजरूह सुलतानपुरी है, जिसने तग़ज़्ज़ुल के वजदान (अंतःप्रेरणा) में अपनी बेताब रूह को उरियां (नग्न) किया है। उसका शुमार (गणना) उन तरक़्क़ी पसंद (प्रगतिशील शायरों में होता है जो कम कहते हैं और (शायद इसीलिए) बहुत अच्छा कहते हैं। ग़ज़ल के मैदान में उसने वह सब कुछ कहा है जिसके लिए बाज़ तरक़्क़ीपसंद शायर सिर्फ़ नज़्म का ही पैराया ज़रूरी और नागुज़ीर (अनिवार्य) समझते हैं। सही तौर पर उसने ग़ज़ल के कदीम (पुराने) शीशे में (बोतल में) एक नई शराब भर दी है।
ग़ज़ल के कदीम शीशे में नई शराब यों ही नहीं भर गई। इसके लिए मजरूह को बड़ी तपस्या करनी पड़ी है। शिक्षा के अभाव के बावजूद उसने राजनीतिक बोध की प्राप्ति और सामाजिक विकास और गति के नियमों को समझने के लिए घोर परिश्रम किया है, तब जाके उसकी शायरी में उस यथार्थवादी की झलक आ पाई है जिसके बिना कोई शायर बड़ा शायर नहीं कहला सकता। अतएव जब वह कहता है कि :
अब खुलके कहूंगा हर ग़मे-दिल मज़रूह नहीं वो वक़्त कि जब
अश्कों में सुनाता था मुझको आहों में ग़ज़ल-ख़्वां होना था
वही मजरूह समझे सब जिसे आवारा-ए-ज़ुल्मत1
वही है एक शमए-सुर्ख़ का2 परवाना बरसों से
बम्बई में यह 25 दिसम्बर, 1958 कि रात है। और यह उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिशील शायर सरदार जाफ़री का घर है। क्रिस्मस की रात मनाने शायर और अदीब आ रहे हैं। क्षण-भर के लिए अफ़सोस होता है कि मां के आपरेशन के कारण कृश्नचन्दर यहां आने के बजाय आज ही दिल्ली चले गये। एक क्षण के लिए अफ़सोस होता है कि किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य के कारण राजेन्द्रसिंह बेदी और ख़्वाजा अहमद अब्बास भी नहीं आ रहे। लेकिन कुछ क्षण के बाद यह अफ़सोस खुशी में बदल जाता है जब डाक्टर मुल्कराज आनन्द आ जाते हैं। इस्मत चुग़ताई और उनके पति शाहिद लतीफ़ आ जाते हैं। नख़शब जार्जवी और जांनिसार अख़्तर आ जाते हैं। साहिर लुधियानवी और प्रकाश पण्डित आ जाते हैं। गप्पे हो रही हैं। मज़ाक़ हो रहे हैं। डाक्टर आनन्द इस्मत और शाहिद लतीफ़ में झगड़ा कराने की विफल कोशिश कर रहे हैं। इस्मत साहिर और मजरूह में झगड़ा कराने की विफल कोशिश कर रही हैं। यहां तक की हर कोई हर किसी के साथ झगड़ा करने की विफल कोशिश कर रहा है। हर कोशिश चूंकि विफल जा रही है इसलिए बला का शोर मच रहा है और टेप-रिकार्डर पर इस ऐतिहासिक बैठक की हर आवाज़ रिकार्ड हो रही है। एकाएक मजरूह की आवाज़
----------------------------------------------------
1.अंधेरों में भटकने वाला 2.(सुर्ख) समाजवादी दीपक का
सब आवाज़ों पर छा जाती है। फिर धीरे-धीरे सब आवाज़ें उसकी आवाज़ में विलीन हो जाती हैं और सब-के-सब उसकी ग़ज़ल पर सिर धुनने लगते हैं।
मजरूह ग़ज़ल का शायर है और उसका कहना है कि वह अपनी ग़ज़लों में इस बात को साबित कर देता है कि मौजूदा ज़माने के मसाइल (समस्याओं) को शायराना रूप देने के लिए ग़ज़ल नामौजूं (अनुपयुक्त) नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी मंज़िलें भी हैं जहां सिर्फ़ ग़ज़ल ही शायर का साथ दे सकती है। हालांकि उर्दू के एक समालोचक कलीम-उल्ला की नज़र में ग़ज़ल एक नीम-वहशी (अर्धसभ्य) काव्य-रूप है और कुछ वर्ष पूर्व कुछ प्रगतिशील साहित्यकारों ने भी इसे मरते हुए सामन्ती समाज का अंग और केवल आत्मभाव (Subjectiveness) का चमत्कार कहकर इसके उन्मूलन की माँग की थी।
लगभग इसी प्रकार की एक मांग रूस की क्रांति से पहले कुछ क्रांतिकारी युवकों ने भी की थी। वे अतीत की समस्त अच्छी-बुरी परम्पराओं को रूढ़ि और सामन्त-काल की जूठन कहकर उन्हें समाप्त कर डालने पर तुल गये थे और इस सम्बन्ध में कोई सैद्धान्तिक युक्ति भी सुनने को तैयार न थे। अतएव जब वहां के महान लेखक तुर्गनेव ने अपने उपन्यासों में ऐसे संकीर्णतावादी पात्रों के प्रस्तुत करना और उनका खेदजनक परिणाम दिखाना शुरू किया तो उन युवकों ने उसे रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, बल्कि क्रांति-विरोधी तक कह डाला और मुतालबा किया कि उसकी समस्त पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाय क्योंकि उनके अध्ययन से क्रान्तिकारी युवकों के भटकने की सम्भावना है।
क्रान्ति से छिछला लगाव रखनेवाले भारतीय लेखक भी ग़ज़ल के प्रति अपना रोष प्रकट करते हुए इस तात्विक सिद्धांत को भूल गये कि हर नई चीज़ पुरानी कोख से जन्म लेती है। भाषा तथा साहित्य और संस्कृति तथा सभ्यता से लेकर शारीरिक वस्त्रों तक कोई चीज़ शून्य में आगे नहीं बढ़ती बल्कि इसे अपने पिछले फ़ैशन का सहारा लेना पड़ता है। और जहां तक आत्मभाव का संबंध है, आत्मभाव किसी चिकने घड़े का नाम नहीं है बल्कि आत्मभाव भी पदार्थ-विषयता का प्रतिबिम्ब होती है। अपने मन की दुनिया में रहना किसी पागल के लिए तो सम्भव है लेकिन कोई चेतन व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इन जोशीले लेकिन विमूढ़ साहित्यकारों के बारे में, जो पुरानेपन के इतने विरोधी थे, उर्दू के एक समालोचक ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि उन्होंने टब के गंदले पानी के साथ-साथ और बच्चो को भी फेंक देने की ठान ली थी।
सौभाग्यवश उर्दू के उन संकीर्णतावादी साहित्यकारों ने बहुत शीघ्र अपनी भूल स्वीकार कर ली और साहित्य, इतिहास और सामाजिक परिस्थितियों के गहरे अध्ययन और निरीक्षण के बाद अब वे बच्चे और टब को नहीं, केवल टब के गंदले पानी को फेंकने और उसकी जगह निर्मल और स्वच्छ पानी भरने के लिए प्रयत्नशील हैं।
यह ठीक है कि उर्दू शायरी का एक विशेष रूप होने के कारण ग़ज़ल की कुछ अपनी विशेष परम्पराएं हैं और वह सामन्त-काल की उपज है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ग़ज़ल की परम्पराओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या नहीं हो सकता। विश्व, समाज और मानव-जीवन की प्रत्येक वस्तु की तरह ग़ज़ल की परम्पराओं में भी बराबर परिवर्तन होता रहा है और मीर, सौदा, दर्द, मोमिन, ग़ालिब, दाग़ के कलाम के क्रमशः अध्ययन से हम इस परिवर्तन या विकास की रूप-रेखा देख सकते जागीरदारी के पतन और इस कारण ग़ज़ल की अधोगति के बाद बीसवीं सदी में जिन शायरों ने ग़ज़ल की रूढ़िगत परम्पराओं में परिवर्तन लाने के सफल प्रयत्न किये, उनमें हसरत मोहानी, इक़बाल, जिगर, फ़िराक़, मजाज़, फ़ैज़, और जज़्बी के नाम सबसे ऊपर हैं। इस प्रसंग में मजरूह सुलतानपुरी ग़ज़ल के क्षेत्र में नवागन्तुक है।
मजरूह सुलतानपुरी ग़ज़ल के क्षेत्र में नवागन्तुक अवश्य है लेकिन अनाड़ी नहीं। उर्दू ग़ज़ल के शयनागार में वह एक सिमटी-सिमटाई लजीली दुल्हन की तरह नहीं बल्कि एक निडर और बेबाक दूल्हे की तरह दाख़िल हुआ है और कुछ ऐसे स्वाभिमान के साथ दाख़िल हुआ है कि शयनागार का मदमाता वातावरण चकाचौंध प्रकाश में परिवर्तित हो गया।
इस सम्बन्ध में मजरूह के कविता-संग्रह ग़ज़ल में मजरूह का परिचय कराते हुए सरदार जाफ़री ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि :
एक और ख़ुसूसियत (विशेषता) जो मजरूह को आ़म ग़ज़ल-गो शायरों से मुम्ताज़ (विशिष्ट) करती है, यह है कि उसने समाजी और सियासी मौज़ूआत (विषयों) को बड़ी कामियाबी के साथ ग़ज़ल के पैराया (शैली) में ढाल लिया है। आ़म तौर पर ग़ज़लगो शायरी समाजी और सियासी मौज़ूआत के बयान में फीके-सीठे हो जाते हैं या उनका अन्दाज़े-बयां (वर्णन-शैली) ऐसा हो जाता है कि नज़्म और ग़ज़ल का फ़र्क बाक़ी नहीं रहता। मजरूह के यहां यह बात नहीं है।
और इस कविता-संग्रह की प्रस्तावना में स्वर्गीय क़ाज़ी अब्दुल ग़फ़्फ़ार लिखते हैं :
हिन्दोस्तान की नौजवान नस्ल के आतिशख़ाने (अग्निकुंड) से जो चिंगारियां निकल रही हैं, उनमें एक बहुत रौशन चिंगारी मजरूह सुलतानपुरी है, जिसने तग़ज़्ज़ुल के वजदान (अंतःप्रेरणा) में अपनी बेताब रूह को उरियां (नग्न) किया है। उसका शुमार (गणना) उन तरक़्क़ी पसंद (प्रगतिशील शायरों में होता है जो कम कहते हैं और (शायद इसीलिए) बहुत अच्छा कहते हैं। ग़ज़ल के मैदान में उसने वह सब कुछ कहा है जिसके लिए बाज़ तरक़्क़ीपसंद शायर सिर्फ़ नज़्म का ही पैराया ज़रूरी और नागुज़ीर (अनिवार्य) समझते हैं। सही तौर पर उसने ग़ज़ल के कदीम (पुराने) शीशे में (बोतल में) एक नई शराब भर दी है।
ग़ज़ल के कदीम शीशे में नई शराब यों ही नहीं भर गई। इसके लिए मजरूह को बड़ी तपस्या करनी पड़ी है। शिक्षा के अभाव के बावजूद उसने राजनीतिक बोध की प्राप्ति और सामाजिक विकास और गति के नियमों को समझने के लिए घोर परिश्रम किया है, तब जाके उसकी शायरी में उस यथार्थवादी की झलक आ पाई है जिसके बिना कोई शायर बड़ा शायर नहीं कहला सकता। अतएव जब वह कहता है कि :
बचा लिया मुझे तूफ़ां की मौज ने वर्ना
किनारे बाले सफ़ीना1 मेरा डुबो देते
मेरे काम आ गईं आख़िरश2 यही काविशें3 यही गर्दिशें
बढ़ीं इस कद़र मेरी मंज़िलें कि क़दम के ख़ार4 निकल गये
किनारे बाले सफ़ीना1 मेरा डुबो देते
मेरे काम आ गईं आख़िरश2 यही काविशें3 यही गर्दिशें
बढ़ीं इस कद़र मेरी मंज़िलें कि क़दम के ख़ार4 निकल गये
तो केवल इतना ही नहीं कि मजरूह हमें ग़ज़ल की प्राचीन परम्पराओं का उत्तराधिकारी नज़र आता है बल्कि उसके यहां हमें ऐतिहासिक सच्चाइयों की भी बड़ी सुन्दर झलक मिलती है। ख़िज़ां,
1. नाव 2. आख़िर 3. प्रयत्न 4. कांटे
बहार, साक़ी, महफ़िल, शराब, पैमाना, गुल, गुलिस्तां, सय्याद इत्यादि शब्दों से, जो प्राचीन ग़ज़ल के पात्र हैं, मजरूह ने बड़ी कला-कौशलता से अपना काम निकाला है। इन शब्दों को पहनाया हुआ उसका नया अर्थ इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि शायरी के अन्य रूपों की तरह ग़ज़ल भी एक लिबास है जो विचारों के शरीर को ढांपता है और अपनी तराश-ख़राश और रंग-रूप के आधार पर किसी भी दूसरे लिबास के कम सुन्दर नहीं। मजरूह ने आवश्यकतानुसार इस लिबास में कुछ नये शब्दों द्वारा अपनी और भी रंगीनी खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की है। अपनी इस कोशिश में कहीं-कहीं तो वह बहुत सफल रहा है। उदाहरणस्वरूप, पूंजीवाद के प्रति अपनी घृणा प्रकट करते हुए उसके सबसे बड़े लक्षण बैंक को वह इस प्रकार अपने शेर में बांधता है :
1. नाव 2. आख़िर 3. प्रयत्न 4. कांटे
बहार, साक़ी, महफ़िल, शराब, पैमाना, गुल, गुलिस्तां, सय्याद इत्यादि शब्दों से, जो प्राचीन ग़ज़ल के पात्र हैं, मजरूह ने बड़ी कला-कौशलता से अपना काम निकाला है। इन शब्दों को पहनाया हुआ उसका नया अर्थ इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि शायरी के अन्य रूपों की तरह ग़ज़ल भी एक लिबास है जो विचारों के शरीर को ढांपता है और अपनी तराश-ख़राश और रंग-रूप के आधार पर किसी भी दूसरे लिबास के कम सुन्दर नहीं। मजरूह ने आवश्यकतानुसार इस लिबास में कुछ नये शब्दों द्वारा अपनी और भी रंगीनी खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की है। अपनी इस कोशिश में कहीं-कहीं तो वह बहुत सफल रहा है। उदाहरणस्वरूप, पूंजीवाद के प्रति अपनी घृणा प्रकट करते हुए उसके सबसे बड़े लक्षण बैंक को वह इस प्रकार अपने शेर में बांधता है :
जबीं पर1 ताजे-ज़र2, पहलू में ज़िंदां3, बैंक छाती पर
उठेगा बेकफ़न कब ये जनाज़ा हम भी देखेंगे
उठेगा बेकफ़न कब ये जनाज़ा हम भी देखेंगे
और क्रान्ति का स्वागत करते हुए वह ज़मीन, हल, जौ के दाने, और कारख़ाने ऐसे शब्दों को, जो, नज़्मों में तो किसी तरह खप सकते हैं लेकिन, ग़ज़ल की नाज़ुक कमर इनका बोझ मुश्किल ही से उठा सकती है, बड़ी शान से यों प्रयोग में लाता है :
अब ज़मीन गायेगी हल के साज पर नग़्में
वादियों में नाचेंगे हर तरफ़ तराने-से
अहले-दिल उगायेंगे ख़ाक से महो-अंजुम4
अब गुहर5 सुबक6 होगा जौ के एक दाने से
मनचले बुनेंगे अब रंगो-बू के पैराहन7
अब संवर के निकलेगा हुस्न कारख़ाने से
वादियों में नाचेंगे हर तरफ़ तराने-से
अहले-दिल उगायेंगे ख़ाक से महो-अंजुम4
अब गुहर5 सुबक6 होगा जौ के एक दाने से
मनचले बुनेंगे अब रंगो-बू के पैराहन7
अब संवर के निकलेगा हुस्न कारख़ाने से
----------------
1. माथे पर 2. पूंजी-रूपी ताज 3. जेलख़ाना 4. चाँद-सितारे 5. मोती 6. हल्का (कम क़ीमत का) 7. लिबास।
लेकिन कभी-कभी नये शब्दों के प्रयोग की धुन में और राजनीति-सम्बन्धी सामयिक आन्दोलनों की धारा में बहकर वह कला की दृष्टि से असफल भी रहता है और उस कोमल सम्बन्ध को भुला देता है जो राजनीतिक बोध और उसके कलात्मक वर्णन के बीच होना चाहिए। उसके ऐसे शेर देखिये :
अम्न का झंडा इस धरती पर, किसने कहा लहराने न पाये
ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार के साथी जाने न पाये
इस श्रेणी के शेर यद्यपि उसके यहां आटे में नमक के बराबर हैं फिर भी मेरे तुच्छ विचार में मजरूह को इस प्रकार के वर्णन से पहलू बचाना चाहिये, क्योंकि यह भी कुछ उसी प्रकार की संकीर्णता है, जिसने रूस के महान कलाकार तुर्गनेव को क्रान्तिविरोधी ठहराया था और क्रान्ति आन्दोलन में योग देने की बजाय क्रान्ति को हानि पहुंचाई थी।
आधुनिक उर्दू ग़ज़ल का यह क्रान्तिवादी शायर, जो अपने साधारण जीवन में बड़ा सौन्दर्य-प्रेमी है, कभी भद्दे वस्त्र नहीं पहनता, कभी भद्दा खाना नहीं खाता, भद्दे मकान में नहीं रहता, भद्दी पुस्तकें नहीं रखता, भद्दी बातें नहीं करता और इसीलिए बहुत कम भद्दे शेर कहता है, ज़िला आज़मगढ़ के एक क़स्बे निज़ामाबाद में पैदा हुआ और हकीम बनते-बनते संयोग से शायर बन गया। उसकी जीवनी उसकी अपनी ज़बान से सुनिये :
मैं एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा हूं, जो मुलाज़मत के दौरान आज़मगढ़ (यू.पी.) में रहे और वहीं निज़ामाबाद में 1919 में मेरी पैदाइश हुई और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम (उर्दू, फ़ारसी, अरबी) वहीं हासिल की। 1930 में मैं आज़मगढ़ से क़स्बा टांडा ज़िला फ़ैजाबाद आया और वहां अरबी दर्स निज़ामिया की तकमील (पूर्ति) करनी चाही लेकिन कर नहीं सका और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के अरबी इन्तिहानों मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल की फ़िक्र की कि इस ज़रिये से किसी स्कूल में टीचरी मिल सकेगी। लेकिन आलिम तक पढ़कर उसे भी छोड़ दिया और तिब्ब (चिकित्सा-शास्त्र) की तकमील के लिए लखनऊ आया और यहां अरबी ज़बान में तिब्ब की तकमील की। यह ज़माना 1938 का है। चन्द महीनों तक मतब (औषधालय) किया लेकिन चूंकि सुलतानपुर में कुछ शेर-ओ-अदब की भी चर्चा थी इसलिए मुझ में भी शेर कहने का शौक़ पैदा हुआ। 1941 में जिगर मुरादाबादी ने मुझे शायर में सुना और अपने साथ लेकर कई एक मुशायरों में गये। इस दौरान उन्होंने मुझे दो बातें बताईं। उनमें से एक यह थी कि अगर किसी का कोई अच्छा शेर सुनो तो कभी नक़ल न करो बल्कि जो गुज़रे (आत्मानुभव हो) वही कहो। बाक़ायदा इस्लाह (संशोधन) मैंने किसी से नहीं ली। बिल्कुल शुरू की दो ग़जलों पर आ़सी साहब महरूम से इस्लाह ली थी। लेकिन वे ग़ज़लें मेरे हाफ़िजे (मस्तिष्क) में बिल्कुल नहीं हैं। 1945 में एक मुशायरे से सिलसिले में बम्बई आया और यहीं फ़िल्मों के गीत वग़ैरा लिखने लगा और अब तक यहीं हूं। 1947 में अंजुमने-तरक़्क़ीपसंद-मुसन्नफ़ीन (प्रगतिशील लेखक संघ) से वाबस्ता हूं1
1. इससे पूर्व मजरूह प्रगतिशील धारणा से सहमत नहीं था। अर्थात् वह साहित्य और कला के सामाजिक उद्देश्य का पक्षपाती न था। लेकिन सरदार जाफ़री के कथनानुसार एक बार जब मजरूह अजन्ता और एलोरा देखने गया तो अजन्ता में गौतम बुद्ध की शिक्षा, जीवन और उस काल के वातावरण के चित्रण ने मजरूह को स्तब्ध कर दिया और उसी समय से उसे विश्वास हो गया कि सामाजिक उद्देश्य के बिना महान कला जन्म नहीं ले सकती। उसने कहा, अजन्ता फ़न (कला) का आलातरीन (महानतम्) नमूना है। फिर भी प्रौपेगंडा है। वह जाविदां (अमर) इसलिए है कि उसने रूहे-अस्त्र (युग की आत्मा) को असीर (बन्दी) कर लिया है। यही ख़याल बाद को इस शेर में इस तरह ढल गया :
1. माथे पर 2. पूंजी-रूपी ताज 3. जेलख़ाना 4. चाँद-सितारे 5. मोती 6. हल्का (कम क़ीमत का) 7. लिबास।
लेकिन कभी-कभी नये शब्दों के प्रयोग की धुन में और राजनीति-सम्बन्धी सामयिक आन्दोलनों की धारा में बहकर वह कला की दृष्टि से असफल भी रहता है और उस कोमल सम्बन्ध को भुला देता है जो राजनीतिक बोध और उसके कलात्मक वर्णन के बीच होना चाहिए। उसके ऐसे शेर देखिये :
अम्न का झंडा इस धरती पर, किसने कहा लहराने न पाये
ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार के साथी जाने न पाये
इस श्रेणी के शेर यद्यपि उसके यहां आटे में नमक के बराबर हैं फिर भी मेरे तुच्छ विचार में मजरूह को इस प्रकार के वर्णन से पहलू बचाना चाहिये, क्योंकि यह भी कुछ उसी प्रकार की संकीर्णता है, जिसने रूस के महान कलाकार तुर्गनेव को क्रान्तिविरोधी ठहराया था और क्रान्ति आन्दोलन में योग देने की बजाय क्रान्ति को हानि पहुंचाई थी।
आधुनिक उर्दू ग़ज़ल का यह क्रान्तिवादी शायर, जो अपने साधारण जीवन में बड़ा सौन्दर्य-प्रेमी है, कभी भद्दे वस्त्र नहीं पहनता, कभी भद्दा खाना नहीं खाता, भद्दे मकान में नहीं रहता, भद्दी पुस्तकें नहीं रखता, भद्दी बातें नहीं करता और इसीलिए बहुत कम भद्दे शेर कहता है, ज़िला आज़मगढ़ के एक क़स्बे निज़ामाबाद में पैदा हुआ और हकीम बनते-बनते संयोग से शायर बन गया। उसकी जीवनी उसकी अपनी ज़बान से सुनिये :
मैं एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा हूं, जो मुलाज़मत के दौरान आज़मगढ़ (यू.पी.) में रहे और वहीं निज़ामाबाद में 1919 में मेरी पैदाइश हुई और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम (उर्दू, फ़ारसी, अरबी) वहीं हासिल की। 1930 में मैं आज़मगढ़ से क़स्बा टांडा ज़िला फ़ैजाबाद आया और वहां अरबी दर्स निज़ामिया की तकमील (पूर्ति) करनी चाही लेकिन कर नहीं सका और इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के अरबी इन्तिहानों मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल की फ़िक्र की कि इस ज़रिये से किसी स्कूल में टीचरी मिल सकेगी। लेकिन आलिम तक पढ़कर उसे भी छोड़ दिया और तिब्ब (चिकित्सा-शास्त्र) की तकमील के लिए लखनऊ आया और यहां अरबी ज़बान में तिब्ब की तकमील की। यह ज़माना 1938 का है। चन्द महीनों तक मतब (औषधालय) किया लेकिन चूंकि सुलतानपुर में कुछ शेर-ओ-अदब की भी चर्चा थी इसलिए मुझ में भी शेर कहने का शौक़ पैदा हुआ। 1941 में जिगर मुरादाबादी ने मुझे शायर में सुना और अपने साथ लेकर कई एक मुशायरों में गये। इस दौरान उन्होंने मुझे दो बातें बताईं। उनमें से एक यह थी कि अगर किसी का कोई अच्छा शेर सुनो तो कभी नक़ल न करो बल्कि जो गुज़रे (आत्मानुभव हो) वही कहो। बाक़ायदा इस्लाह (संशोधन) मैंने किसी से नहीं ली। बिल्कुल शुरू की दो ग़जलों पर आ़सी साहब महरूम से इस्लाह ली थी। लेकिन वे ग़ज़लें मेरे हाफ़िजे (मस्तिष्क) में बिल्कुल नहीं हैं। 1945 में एक मुशायरे से सिलसिले में बम्बई आया और यहीं फ़िल्मों के गीत वग़ैरा लिखने लगा और अब तक यहीं हूं। 1947 में अंजुमने-तरक़्क़ीपसंद-मुसन्नफ़ीन (प्रगतिशील लेखक संघ) से वाबस्ता हूं1
1. इससे पूर्व मजरूह प्रगतिशील धारणा से सहमत नहीं था। अर्थात् वह साहित्य और कला के सामाजिक उद्देश्य का पक्षपाती न था। लेकिन सरदार जाफ़री के कथनानुसार एक बार जब मजरूह अजन्ता और एलोरा देखने गया तो अजन्ता में गौतम बुद्ध की शिक्षा, जीवन और उस काल के वातावरण के चित्रण ने मजरूह को स्तब्ध कर दिया और उसी समय से उसे विश्वास हो गया कि सामाजिक उद्देश्य के बिना महान कला जन्म नहीं ले सकती। उसने कहा, अजन्ता फ़न (कला) का आलातरीन (महानतम्) नमूना है। फिर भी प्रौपेगंडा है। वह जाविदां (अमर) इसलिए है कि उसने रूहे-अस्त्र (युग की आत्मा) को असीर (बन्दी) कर लिया है। यही ख़याल बाद को इस शेर में इस तरह ढल गया :
नवा है जाविदां मजरूह जिसमें रूहे-साअ़त हो
कहा किसने मेरा नग़्मा ज़माने के चलन तक है
कहा किसने मेरा नग़्मा ज़माने के चलन तक है
बाद में अपनी प्रगतिशील शायरी का उसे दंड भी मिलापूरे एक वर्ष का कारावास ! लेकिन एक बार जो कुलाह कज हुई1 फिर :
सर पर हवा-ए-जुल्म2 चले सौ जतन के साथ
अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ
अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ
2. टोपी टेढ़ी हुई 2. अत्याचार की हवा
और रोज़-ब-रोज़ (अगरचे फ़ुर्सत कम मिलती है) इसी कोशिश में हूं कि ग़ज़ल के पस मंज़र (पृष्ठ-भूमि) में मार्कसिज़्म को रखकर, समाजी, सियासी और इश्क़िया शायरी कर सकूं। चुनांचे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अच्छा शायर हूं और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी हूं। तुम मुझे दोनों एतिबार से जानते हो, जो चाहो फ़ैसला कर लो।
इस सम्बोधन का तुम चूंकि मैं हूं इसलिए मेरा फैसला यह है कि मजरूह आदमी भी बहुत अच्छा है और शायर भी बहुत प्रतिभाशाली।
1.
मजरूह सुलतानपुरी ने पचास से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। यह काम इतने लंबे समय तक शायद किसी और ने कभी नहीं किया। आजादी मिलने से दो साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने बम्बई गए थे और तब उस समय के मशहूर फिल्म-निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर दिया था। दरअस्ल उनका चुनाव एक प्रतियोगिता के द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म के गीत प्रसिद्ध गायक सहगल ने गाए थे और बात की बात में गीतों के साथ गीतकार भी मशहूर हो गया। ये गीत थे-गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनके संगीतकार नौशाद साहब थे। मजरूह के साथ उनकी दोस्ती खूब जमी।
जिन फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे उनमें से कुछ के नाम हैं-सी.आई.डी., चलती का नाम गाड़ी, नौ-दो ग्यारह, पेइंग गेस्ट, काला पानी, तुम सा नहिं देखा, दिल देके देखो, दिल्ली का ठग, इत्यादि।
पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीली कविता लिखने के कारण आपको सवा साल जेल में रहना पड़ा। इस अवधि में राजकपूर ने उनकी बड़ी मदद की। 1994 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 1980 में उन्हें ग़ालिब एवार्ड और 1992 में इकबाल एवार्ड प्राप्त हुए थे। वे जीवन के अंत तक फिल्मों से जुड़े रहे। जून 2000 में उनका देहांत हो गया।
और रोज़-ब-रोज़ (अगरचे फ़ुर्सत कम मिलती है) इसी कोशिश में हूं कि ग़ज़ल के पस मंज़र (पृष्ठ-भूमि) में मार्कसिज़्म को रखकर, समाजी, सियासी और इश्क़िया शायरी कर सकूं। चुनांचे कुछ लोग कहते हैं कि मैं अच्छा शायर हूं और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी हूं। तुम मुझे दोनों एतिबार से जानते हो, जो चाहो फ़ैसला कर लो।
इस सम्बोधन का तुम चूंकि मैं हूं इसलिए मेरा फैसला यह है कि मजरूह आदमी भी बहुत अच्छा है और शायर भी बहुत प्रतिभाशाली।
1.
मजरूह सुलतानपुरी ने पचास से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। यह काम इतने लंबे समय तक शायद किसी और ने कभी नहीं किया। आजादी मिलने से दो साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने बम्बई गए थे और तब उस समय के मशहूर फिल्म-निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने का अवसर दिया था। दरअस्ल उनका चुनाव एक प्रतियोगिता के द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म के गीत प्रसिद्ध गायक सहगल ने गाए थे और बात की बात में गीतों के साथ गीतकार भी मशहूर हो गया। ये गीत थे-गम दिए मुस्तकिल और जब दिल ही टूट गया जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनके संगीतकार नौशाद साहब थे। मजरूह के साथ उनकी दोस्ती खूब जमी।
जिन फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे उनमें से कुछ के नाम हैं-सी.आई.डी., चलती का नाम गाड़ी, नौ-दो ग्यारह, पेइंग गेस्ट, काला पानी, तुम सा नहिं देखा, दिल देके देखो, दिल्ली का ठग, इत्यादि।
पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीली कविता लिखने के कारण आपको सवा साल जेल में रहना पड़ा। इस अवधि में राजकपूर ने उनकी बड़ी मदद की। 1994 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व 1980 में उन्हें ग़ालिब एवार्ड और 1992 में इकबाल एवार्ड प्राप्त हुए थे। वे जीवन के अंत तक फिल्मों से जुड़े रहे। जून 2000 में उनका देहांत हो गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book