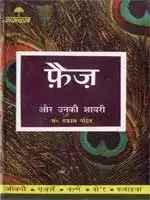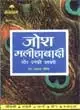|
गजलें और शायरी >> फ़ैज़ और उनकी शायरी फ़ैज़ और उनकी शायरीप्रकाश पंडित
|
316 पाठक हैं |
||||||
फ़ैज़ की जिन्दगी और उनकी बेहतरीन शायरी गज़लें, नज्में, शेर
Faij Aur Unki Shayari
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वर्षों पहले नागरी लिपि में उर्दू की चुनी हुई शायरी के संकलन प्रकाशित कर राजपाल एण्ड सन्ज़ ने पुस्तक प्रकाशन की दुनिया में एक नया कदम उठाया था। उर्दू लिपि न जानने वाले लेकिन शायरी को पसंद करने वाले अनगिनत लोगों के लिए यह एक बड़ी नियामत साबित हुआ और सभी ने इससे बहुत लाभ उठाया।
ज्यादातर संकलन उर्दू के सुप्रसिद्ध सम्पादक प्रकाश पंडित ने किये हैं। उन्होंने शायर के सम्पूर्ण लेखन से चयन किया है और कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दे दिये हैं। इसी के साथ, शायर के जीवन और कार्य पर-जिनमें से समकालीन उनके परिचित ही थे-बहुत रोचक और चुटीली भूमिकाएं लिखी हैं। ये बोलती तस्वीरें हैं जो सोने में सुहागे का काम करती हैं।
ज्यादातर संकलन उर्दू के सुप्रसिद्ध सम्पादक प्रकाश पंडित ने किये हैं। उन्होंने शायर के सम्पूर्ण लेखन से चयन किया है और कठिन शब्दों के अर्थ साथ ही दे दिये हैं। इसी के साथ, शायर के जीवन और कार्य पर-जिनमें से समकालीन उनके परिचित ही थे-बहुत रोचक और चुटीली भूमिकाएं लिखी हैं। ये बोलती तस्वीरें हैं जो सोने में सुहागे का काम करती हैं।
‘फ़ैज़’
‘फ़ैज़’ आज के उर्दू शायरों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। उनकी शायरी ने उर्दू ग़ज़लों और नज़्मों को एक नया रंग, एक नया तेवर दिया है। नई पीढ़ी का कोई भी शायर ऐसा नहीं कि वह ‘फ़ैज़’ से प्रभावित न हुआ हो।
रूप और रस, प्रेम और राजनीति और कला और विचार का जैसा संगम फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ ने प्रस्तुत किया है, उनकी इस देन पर जितना भी गर्व करे, कम है।
रूप और रस, प्रेम और राजनीति और कला और विचार का जैसा संगम फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ ने प्रस्तुत किया है, उनकी इस देन पर जितना भी गर्व करे, कम है।
पाकिस्तान टाइम्ज़ लाहौर
11-10-57
11-10-57
बरादरम प्रकाश पण्डित, तस्लीमा !
आपके दो ख़त मिले। भई, मुझे अपने हालाते-ज़िन्दगी में क़तई दिलचस्पी नहीं है, न मैं चाहता हूं कि आप उन पर अपने पढ़ने वालों का वक्त ज़ाया करें। इन्तिख़ाब (कविताओं के चयन) और उसकी इशाअत (प्रकाशन) की आपको इजाज़त है। अपने बारे में मुख़्तसर मालूमात लिखे देता हूं। पैदाइश सियालकोट, 1911, तालीम स्कॉट मिशन हाई स्कूल सियालकोट, गवर्नमेंट, कालेज लाहौर (एम.ए.अंग्रेज़ी 1933, एम.ए. अरबी 1934)। मुलाज़मत एम.ए. ओ. कालेज अमृतसर 1934 से 1940 तक। हेली कालेज लाहौर 1940 से 1942 तक। फ़ौज में (कर्नल की हैसियत से) 1942 से 1947 तक। इसके बाद ‘पाकिस्तान टाइम्ज़’ और ‘इमरोज़’ की एडीटरी ताहाल (अब तक)। मार्च 1951 से अप्रैल 1955 तक जेलख़ाना (रावलपिंडी कान्सपिरेंसी केस के सिलसिले में)। किताबें ‘नक्शे-फ़र्यादी’, ‘दस्ते सबा’ और ‘ज़िन्दांनामा’।
आपके दो ख़त मिले। भई, मुझे अपने हालाते-ज़िन्दगी में क़तई दिलचस्पी नहीं है, न मैं चाहता हूं कि आप उन पर अपने पढ़ने वालों का वक्त ज़ाया करें। इन्तिख़ाब (कविताओं के चयन) और उसकी इशाअत (प्रकाशन) की आपको इजाज़त है। अपने बारे में मुख़्तसर मालूमात लिखे देता हूं। पैदाइश सियालकोट, 1911, तालीम स्कॉट मिशन हाई स्कूल सियालकोट, गवर्नमेंट, कालेज लाहौर (एम.ए.अंग्रेज़ी 1933, एम.ए. अरबी 1934)। मुलाज़मत एम.ए. ओ. कालेज अमृतसर 1934 से 1940 तक। हेली कालेज लाहौर 1940 से 1942 तक। फ़ौज में (कर्नल की हैसियत से) 1942 से 1947 तक। इसके बाद ‘पाकिस्तान टाइम्ज़’ और ‘इमरोज़’ की एडीटरी ताहाल (अब तक)। मार्च 1951 से अप्रैल 1955 तक जेलख़ाना (रावलपिंडी कान्सपिरेंसी केस के सिलसिले में)। किताबें ‘नक्शे-फ़र्यादी’, ‘दस्ते सबा’ और ‘ज़िन्दांनामा’।
‘फ़ैज़’
बेरुत, लेबनान
25-6-1981
25-6-1981
मुकर्रमी प्रकाश पण्डित, तस्लीम !
आपका ख़त बेरुत वापसी पर अभी-अभी मौसूल हुआ है, इसलिए जवाब में ताख़ीर हुई। नई किताब या आपकी पुरानी किताब की नई इशाअत (प्रकाशन) के सिलसिले में सूरत यह है कि बाद के कलाम का एक इंतिख़ाब (चयन) शीला सिंधू, राजकमल की तरफ़ से छाप चुकी हैं, और ताज़ा मजमूआ (संग्रह) ‘मिरे दिल, मिले मुसाफ़िर’ भी उसके पास है। मुझे ठीक से इल्म नहीं कि उनके इंतिख़ाब में जो ‘फ़ैज़’ के नाम से छपा है, कौन सी मनज़ूमात (नज़्में) शामिल हैं, इसलिए आपकी इशाइत के लिए कुछ तजवीज़ करना मुश्किल है। मेरी सारी किताबें देहली में दस्तयाब (प्राप्य) हैं। कुछ ग़लत-सलत मतबूआत (पुस्तकों) के अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, देहली की किताबें काफ़ी सलीक़े से छपी हैं। आप उनमें से ख़ुद ही इंतिख़ाब कर लीजिए।
हमारी ज़िन्दगी या ‘कारनामो ’ की फ़हरिस्त भी शीला सिंधू वाली किताब में है, वहां से ले लीजिए।
आपकी अलालत (बीमारी) का सुनकर तशवीश हुई। उमीद है, यह आई बला टल गई होगी।
आपका ख़त बेरुत वापसी पर अभी-अभी मौसूल हुआ है, इसलिए जवाब में ताख़ीर हुई। नई किताब या आपकी पुरानी किताब की नई इशाअत (प्रकाशन) के सिलसिले में सूरत यह है कि बाद के कलाम का एक इंतिख़ाब (चयन) शीला सिंधू, राजकमल की तरफ़ से छाप चुकी हैं, और ताज़ा मजमूआ (संग्रह) ‘मिरे दिल, मिले मुसाफ़िर’ भी उसके पास है। मुझे ठीक से इल्म नहीं कि उनके इंतिख़ाब में जो ‘फ़ैज़’ के नाम से छपा है, कौन सी मनज़ूमात (नज़्में) शामिल हैं, इसलिए आपकी इशाइत के लिए कुछ तजवीज़ करना मुश्किल है। मेरी सारी किताबें देहली में दस्तयाब (प्राप्य) हैं। कुछ ग़लत-सलत मतबूआत (पुस्तकों) के अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया, देहली की किताबें काफ़ी सलीक़े से छपी हैं। आप उनमें से ख़ुद ही इंतिख़ाब कर लीजिए।
हमारी ज़िन्दगी या ‘कारनामो ’ की फ़हरिस्त भी शीला सिंधू वाली किताब में है, वहां से ले लीजिए।
आपकी अलालत (बीमारी) का सुनकर तशवीश हुई। उमीद है, यह आई बला टल गई होगी।
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़
अब मैं सीधे ‘फ़ैज़’ की शायरी की ओर आता हूं, जिसके पीछे वर्षों बल्कि सदियों की साहित्यिक पूंजी है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि स्वयं साहित्य और समाज दोनों मिलकर वर्षों तपस्या करते हैं, तब जाकर ऐसी मन्त्र-मुग्ध कर देने वाली शायरी जन्म लेती है।
‘‘ ‘शे’र लिखना जुर्म न सही लेकिन बेवजह शे’र लिखते रहना ऐसी अक़्लमंदी भी नहीं है।’’ ‘फ़ैज़’ के पहले कविता संग्रह ‘नक़्शे-फ़रियादी’ की भूमिका में इस वाक्य को पढ़ते हुए मुझे ‘ग़ालिब’ का वह वाक्य याद आ गया, जिसमें उर्दू के सबसे बड़े शायर ने कहा था कि जब से मेरे सीने (छाती) का नासूर बन्द हो गया है, मैंने शे’र कहना छोड़ दिया है।
सीने का नासूर चाहे इश्क़ या प्रणय की भावना हो, चाहे स्वतंत्रता, देश एवं मानव-प्रेम की भावना, कविता ही के लिए नहीं समस्त ललित कलाओं के लिए अनिवार्य है। अध्ययन और अभ्यास से हमें बात कहने का सलीक़ा तो आ सकता है लेकिन आपनी बात को वज़नी बनाने और दूसरे के मन में बिठाने के लिए स्वयं हमें अपने मन में उतारना पड़ता है।
विश्व-साहित्य में बहुत-सी मिसालें मिलती हैं कि किसी कवि अथवा लेखक ने कुछ एक बहुत अच्छी कविताएं, एक बहुत अच्छा उपन्यास या दस-पन्द्रह बहुत अच्छी कहानियां लिखने के बाद लिखने से हाथ खींच लिया और फिर समालोचकों या पाठकों के तक़ाजों से जब उसने पुनः कलम उठाई तो वह बात पैदा न हो सकी, जो उसके ‘कच्चेपन’ के जमाने में हुई थी। कदाचित इसी बात को लेकर ‘नक़्शे-फ़रियादी’ की भूमिका में ‘फ़ैज़’ ने अपनी दो-चार नज़्मों को क़ाबिले-बर्दाश्त क़रार देते हुए लिखा था। कि ‘‘आज से कुछ बरस पहले एक मुअय्यन जज़्बे (निश्चित भावना) के ज़ेरे-असर अशआर (शे’र) ख़ुद-ब-ख़ुद वारिद (आगत) होते थे, लेकिन अब मज़ामीन (विषय) के लिए तजस्सुस (तलाश) करना पड़ता है...हममें से बेहतर की शायरी किसी दाखली या खारिजी मुहर्रक (आंतरिक या बाह्य प्रेरक) की दस्ते-निगर (आभारी) होती है और अगर उन मुहर्रिकात की शिद्दत (तीव्रता) में कमी आ जाए या उनके इज़हार (अभिव्यक्ति) के लिए कोई सहल रास्ता पेशेनज़र न हो तो या तो तजुर्बात को मस्ख़ (विकृत) करना पड़ता है या तरीके-इज़हार को। ऐसी सूरते-हालात पैदा होने से पहले ही ज़ौक और मसलहत का तक़ाज़ा यही है कि शायर को जो कुछ कहना हो कह ले, अहले-महफ़िल का शुक्रिया अदा करे और इज़ाज़त चाहे।’’
‘फ़ैज़’ के आंतरिक या बाह्य प्रेरकों में सबसे बड़ा प्रेरक ‘हुस्नो-इश्क’, है; बल्कि उसने तो यहां तक कह दिया था कि:
‘‘ ‘शे’र लिखना जुर्म न सही लेकिन बेवजह शे’र लिखते रहना ऐसी अक़्लमंदी भी नहीं है।’’ ‘फ़ैज़’ के पहले कविता संग्रह ‘नक़्शे-फ़रियादी’ की भूमिका में इस वाक्य को पढ़ते हुए मुझे ‘ग़ालिब’ का वह वाक्य याद आ गया, जिसमें उर्दू के सबसे बड़े शायर ने कहा था कि जब से मेरे सीने (छाती) का नासूर बन्द हो गया है, मैंने शे’र कहना छोड़ दिया है।
सीने का नासूर चाहे इश्क़ या प्रणय की भावना हो, चाहे स्वतंत्रता, देश एवं मानव-प्रेम की भावना, कविता ही के लिए नहीं समस्त ललित कलाओं के लिए अनिवार्य है। अध्ययन और अभ्यास से हमें बात कहने का सलीक़ा तो आ सकता है लेकिन आपनी बात को वज़नी बनाने और दूसरे के मन में बिठाने के लिए स्वयं हमें अपने मन में उतारना पड़ता है।
विश्व-साहित्य में बहुत-सी मिसालें मिलती हैं कि किसी कवि अथवा लेखक ने कुछ एक बहुत अच्छी कविताएं, एक बहुत अच्छा उपन्यास या दस-पन्द्रह बहुत अच्छी कहानियां लिखने के बाद लिखने से हाथ खींच लिया और फिर समालोचकों या पाठकों के तक़ाजों से जब उसने पुनः कलम उठाई तो वह बात पैदा न हो सकी, जो उसके ‘कच्चेपन’ के जमाने में हुई थी। कदाचित इसी बात को लेकर ‘नक़्शे-फ़रियादी’ की भूमिका में ‘फ़ैज़’ ने अपनी दो-चार नज़्मों को क़ाबिले-बर्दाश्त क़रार देते हुए लिखा था। कि ‘‘आज से कुछ बरस पहले एक मुअय्यन जज़्बे (निश्चित भावना) के ज़ेरे-असर अशआर (शे’र) ख़ुद-ब-ख़ुद वारिद (आगत) होते थे, लेकिन अब मज़ामीन (विषय) के लिए तजस्सुस (तलाश) करना पड़ता है...हममें से बेहतर की शायरी किसी दाखली या खारिजी मुहर्रक (आंतरिक या बाह्य प्रेरक) की दस्ते-निगर (आभारी) होती है और अगर उन मुहर्रिकात की शिद्दत (तीव्रता) में कमी आ जाए या उनके इज़हार (अभिव्यक्ति) के लिए कोई सहल रास्ता पेशेनज़र न हो तो या तो तजुर्बात को मस्ख़ (विकृत) करना पड़ता है या तरीके-इज़हार को। ऐसी सूरते-हालात पैदा होने से पहले ही ज़ौक और मसलहत का तक़ाज़ा यही है कि शायर को जो कुछ कहना हो कह ले, अहले-महफ़िल का शुक्रिया अदा करे और इज़ाज़त चाहे।’’
‘फ़ैज़’ के आंतरिक या बाह्य प्रेरकों में सबसे बड़ा प्रेरक ‘हुस्नो-इश्क’, है; बल्कि उसने तो यहां तक कह दिया था कि:
लेकिन उस शोख़ के आहिस्ता से खुलते हुए होंट
हाए उस जिस्म के कमबख़्त दिलावेज़ खुतूत1
आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफ़सूं2 होंगे
अपना मौज़ूए-सुख़न3 इनके सिवा और नहीं
तबए-शायर का4 वतन इनके सिवा और नहीं
हाए उस जिस्म के कमबख़्त दिलावेज़ खुतूत1
आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफ़सूं2 होंगे
अपना मौज़ूए-सुख़न3 इनके सिवा और नहीं
तबए-शायर का4 वतन इनके सिवा और नहीं
(‘मौज़ूए-सुख़न’)
मगर इस बंद के शुरू के ‘लेकिन’ से पहले उसने जिन चीज़ों को अपना मौज़ूए-सुख़न बनाना पसंद नहीं किया था और :
इन दमकते हुए शहरों की फ़रावां मख़लूक़5
क्यों फ़क़त मरने की हसरत में जिया करती है
ये हसीं खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका
किसलिए इन में फ़क़त भूक उगा करती है
क्यों फ़क़त मरने की हसरत में जिया करती है
ये हसीं खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका
किसलिए इन में फ़क़त भूक उगा करती है
ऐसे प्रश्न हल किए बिना छोड़ दिए थे, वही ‘साधारण’ प्रश्न बाद में उसकी आंतरिक और बाह्म प्रेरणाओं का स्रोत बने और यही वे प्रश्न थे जिन्होंने उसे अहले-महफ़िल का शुक्रिया अदा करके उठ जाने से रोका और उर्दू साहित्य को एक बड़ा शायर प्रदान किया।
फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ आधुनिक काल के उन चंद बड़े शायरों में से हैं जिन्होंने काव्य-कला में नए प्रयोग तो किए लेकिन उनकी बुनियाद पुराने प्रयोगों पर रखी और इस आधार-भूत तथ्य को कभी नहीं भुलाया कि हर नई चीज़ पुरानी कोख से जन्म लेती है। यही कारण है कि उसकी शायरी का अध्ययन करते समय हमें किसी प्रकार की अजनबियत
-----------------------
1.हृदयाकर्षक रेखाएं (बनावट) 2. जादू 3.काव्य-विषय 4.शायर की प्रवृत्ति 5.विशाल जनता
महसूस नहीं होती। पेचीदा और अस्पष्ट उपमाओं से वह हमें उलझन में नहीं डालता बल्कि अपने कोमल स्वर में वह हमसे सरगोशियां करता है और उसकी सरगोशी इतनी अर्थपूर्ण होती है कि कुछ शब्द कान में पड़ते ही मनोभाव उभर आते हैं। ‘फ़ैज़’ के पहले कविता-संग्रह ‘नक़्शे-फ़रियादी’ का पहला पन्ना ही देखिए :
फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ आधुनिक काल के उन चंद बड़े शायरों में से हैं जिन्होंने काव्य-कला में नए प्रयोग तो किए लेकिन उनकी बुनियाद पुराने प्रयोगों पर रखी और इस आधार-भूत तथ्य को कभी नहीं भुलाया कि हर नई चीज़ पुरानी कोख से जन्म लेती है। यही कारण है कि उसकी शायरी का अध्ययन करते समय हमें किसी प्रकार की अजनबियत
-----------------------
1.हृदयाकर्षक रेखाएं (बनावट) 2. जादू 3.काव्य-विषय 4.शायर की प्रवृत्ति 5.विशाल जनता
महसूस नहीं होती। पेचीदा और अस्पष्ट उपमाओं से वह हमें उलझन में नहीं डालता बल्कि अपने कोमल स्वर में वह हमसे सरगोशियां करता है और उसकी सरगोशी इतनी अर्थपूर्ण होती है कि कुछ शब्द कान में पड़ते ही मनोभाव उभर आते हैं। ‘फ़ैज़’ के पहले कविता-संग्रह ‘नक़्शे-फ़रियादी’ का पहला पन्ना ही देखिए :
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई
जैसे वीराने में चुपके-से बहार आ जाए
जैसे सहराओं में1 हौले से चले बादे-नसीम2
जैसे बीमार को बेवजह क़रार आ जाए
जैसे वीराने में चुपके-से बहार आ जाए
जैसे सहराओं में1 हौले से चले बादे-नसीम2
जैसे बीमार को बेवजह क़रार आ जाए
प्रेयसी की याद कोई नया काव्य-विषय नहीं है; लेकिन इन सुन्दर उपमाओं और अपनी विशेष वर्णन शैली से उसने इसे बिलकुल नया बल्कि अछूता बना दिया है। इस एक क़त’ए ही की नहीं यह उसकी समूची शायरी की विशेषता है कि वह नई भी है और पुरानी भी। वर्तमान की उपज है; लेकिन अतीत की उत्तराधिकारी है। नए विषय पुरानी शैली में और पुराने विषय नए ढंग से प्रस्तुत करने का जो कला-कौशल ‘फ़ैज़’ को प्राप्त है, आधुनिक काल के बहुत कम शायर उसकी गर्द को पहुंचते हैं। ज़रा ‘ग़ालिब’ का यह शे’र देखिए :
दिया है दिल अगर उसको बशर है क्या कहिए
हुआ रक़ीब3 तो हो, नामावर4 है क्या कहिए
हुआ रक़ीब3 तो हो, नामावर4 है क्या कहिए
और अब इसी विषय को ‘फ़ैज़’की नज़्म ‘रक़ीब से’ के दो शे’रों में
देखिए :
देखिए :
तूने देखी है वो पेशानी5, वो रुख़्सार6, वो होंट
ज़िन्दगी जिनके तसव्वुर में7 लुटा दी हमने
हमने इस इश्क़ में क्या खोया है क्या पाया है
जुज़ तेरे8 और को समझाऊं तो समझा न सकूं
ज़िन्दगी जिनके तसव्वुर में7 लुटा दी हमने
हमने इस इश्क़ में क्या खोया है क्या पाया है
जुज़ तेरे8 और को समझाऊं तो समझा न सकूं
----------------
1.मरुस्थलों में 2.मृदुल समीर 3.प्रतिद्वन्द्वी 4. पत्र-वाहक 5.माथा 6.कपोल 7.कल्पना में 8.तेरे सिवा
महबूब, आशिक़ रक़ीब और इश्क़ के मुआमलों तक ही सीमित नहीं, ‘फ़ैज़’ ने हर जगह नई और पुरानी बातों और नई और पुरानी शैली का बड़ा सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है। ‘गालिब’ का एक और शे’र है:
1.मरुस्थलों में 2.मृदुल समीर 3.प्रतिद्वन्द्वी 4. पत्र-वाहक 5.माथा 6.कपोल 7.कल्पना में 8.तेरे सिवा
महबूब, आशिक़ रक़ीब और इश्क़ के मुआमलों तक ही सीमित नहीं, ‘फ़ैज़’ ने हर जगह नई और पुरानी बातों और नई और पुरानी शैली का बड़ा सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है। ‘गालिब’ का एक और शे’र है:
लिखते रहे जुनूं की1 हिकायाते-खूंचका2
हरचंद इसमें हाथ हमारे क़लम हुए3
हरचंद इसमें हाथ हमारे क़लम हुए3
और ‘फ़ैज़’ का शे’र है :
हम परवरिशे-लौहो-क़लम4 करते रहेंगे
जो दिल पे गुज़रती है रक़म करते रहेंगे5
जो दिल पे गुज़रती है रक़म करते रहेंगे5
इन उदाहरणों में से मेरा उद्देश्य ‘फ़ैज़’ और ‘ग़ालिब’ की शायरी के तुलनात्मक मूल्य दर्शाना नहीं है और यह भी अभिप्राय नहीं है कि हमें अतीत की समस्त परम्पराओं को ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। कुछ परम्पराएं, चाहे वे साहित्य की हों, संस्कृति की हों या अन्य सामाजिक क्षेत्रों की, अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाने के बाद अपनी मौत आप मर जाती हैं। उन्हें नए सिरे से जिलाने का मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना और ऐतिहासिक विकास से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि नयेपन के उन्माद में पुरानी चीज़ों को केवल इसलिए घृणा के योग्य मान लिया जाए कि वे पुरानी हैं। धरती, आकाश, चांद, सितारे, सूरज, समुद्र और पहाड़ सब पुराने हैं, लेकिन हमें ये चीजें पसंद हैं; और इसलिए पसंद हैं कि हम प्रतिक्षण इन्हें बदलते रहते हैं-यानी इनके सम्बन्ध में हमारा दृष्णिकोण बदलता रहता है। हम इनके बारे में नई बातें मालूम कर लेते हैं और इस तरह ये समस्त पुरानी चीजें सदैव नई बनी रहती हैं।
यह एक बड़ी विचित्र लेकिन प्रशंसनीय वास्तविकता है कि प्राचीन
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.प्रेमोन्माद की 2.रक्तिम कथा 3.कट गए 4.तख्ती और कलम का प्रयोग 5.लिखते रहेंगे।
और नवीन शायरों की महफ़िल में खपकर भी ‘फ़ैज़’ की अपनी एक अलग हैसियत है। उसने काव्य-कला के नियमों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया, और न कभी अपनी अद्वितीयता प्रकट करने के लिए ‘मीराजी’ (उर्दू के एक प्रयोगवादी शायर) की तरह यह कहा है कि ‘‘अकसरियत (बहुजनों) की नज्में अलग हैं और मेरी नज़्में अलग; और चूंकि दुनिया की हर बात हर शख़्स के लिए नहीं होती इसलिए मेरी नज़्में भी सिर्फ़ उनके लिए हैं जो उन्हें समझने के अहल हों।’’ (यह अद्वितीयता शायर की है, शायरी की नहीं) फिर भी उसके किसी शे’र पर उसका नाम पढ़े बिना हम बता सकते हैं कि यह ‘फै़ज़’ का शे’र है। ‘फ़ैज़’ की शायरी की ‘अद्वितीयता’ आधारित है उसकी शैली के लोच और मंदगति पर, कोमल, मृदुल और सौ-सौ जादू जगाने वाले शब्दों के चयन पर, ‘तरसी हुई नाकाम निगाहें’ और ‘आवाज़ में सोई हुई शीरीनियां’ ऐसी अलंकृत परिभाषाओं और रुपकों पर, और इन समस्त विशेषताओं के साथ गूढ़ से गूढ़ बात कहने के सलीके पर। उर्दू के एक बुजुर्ग शायर ‘असर’ लखनवी ने शायद बिलकुल ठीक लिखा है कि ‘‘ ‘फ़ैज़’ की शायरी तरक़्की के मदारिज (दर्जे’ तय करके अब इस नुक्ता-ए-उरूज (शिखर-बिन्दु) पर पहुंच गई है, जिस तक शायद ही किसी दूसरे तरक्क़ी-पसंद (प्रगतिशील) शायर की रसाई हुई हो। तख़य्युल (कल्पना) ने सनाअत (शिल्प) के जौहर दिखाए हैं और मासूम जज़्बात को हसीन पैकर (आकार) बख़्शा है। ऐसा मालूम होता है कि परियों का एक ग़ौल (झुण्ड) एक तिलिस्मी फ़ज़ा (जादुई वातावरण) में इस तरह मस्ते-परवाज़ (उड़ने में मस्त) है कि एक पर एक की छूत पड़ रही है और क़ौसे-कुज़ह (इन्द्रधनुष) के अक़्कास (प्रतिरूपक) बादलों से सबरंगी बारिश हो रही है......................।’’
अपनी शायरी की तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ‘फ़ैज़’ को किसी ने ऊंचा बोलते नहीं सुना। बातचीत के अतिरिक्त मुशायरों में भी वह इस तरह अपने शे’र पढ़ता है जैसे उसके होंठों से यदि एक ज़रा ऊंची आवाज़ निकल गई तो न जाने कितने मोती चकनाचूर हो जाएंगे। वह सेना में कर्नल रहा, जहां किसी नर्मदिल अधिकारी की गुंजाइश नहीं होती। उसने कालेज की प्रोफ़ेसरी की, जहां कालेज के लड़के प्रोफ़ेसर तो प्रोफ़ेसर शैतान तक को अपना स्वभाव बदलने पर विवश कर दें। उसने रेडियो की नौकरी की, जहां अपने मातहतों को न डांटने का स्वभाव अफ़सर की नालायक़ी समझा जाता है। उसने पत्रकारिता जैसा जोखिम का पेशा भी अपनाया और फिर जब पाकिस्तान सरकार ने इस देवता-स्वरूप व्यक्ति पर हिंसात्मक विद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया तब भी मेजर मोहम्मद इसहाक़ (फ़ैज़’ के जेल के साथी) के कथनानुसार, ‘‘कहीं पास-पड़ोस में तू-तू मैं-मैं हो, दोस्तों में तल्ख़-कलामी हो, या यूं ही किसी ने त्योरी चढ़ा रखी हो, फ़ैज़’ की तबीयत ज़रूर खराब हो जाती थी और इसके साथ ही शायरी की कैफ़ियत (मूड) भी काफूर हो जाती थी।’’ ‘‘फ़ैज़’ ने अपने निर्दोष होने का तथा उच्चाधिकारियों के षड्यंत्रों का जिक़्र किया भी तो इस भाषा में :
यह एक बड़ी विचित्र लेकिन प्रशंसनीय वास्तविकता है कि प्राचीन
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1.प्रेमोन्माद की 2.रक्तिम कथा 3.कट गए 4.तख्ती और कलम का प्रयोग 5.लिखते रहेंगे।
और नवीन शायरों की महफ़िल में खपकर भी ‘फ़ैज़’ की अपनी एक अलग हैसियत है। उसने काव्य-कला के नियमों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया, और न कभी अपनी अद्वितीयता प्रकट करने के लिए ‘मीराजी’ (उर्दू के एक प्रयोगवादी शायर) की तरह यह कहा है कि ‘‘अकसरियत (बहुजनों) की नज्में अलग हैं और मेरी नज़्में अलग; और चूंकि दुनिया की हर बात हर शख़्स के लिए नहीं होती इसलिए मेरी नज़्में भी सिर्फ़ उनके लिए हैं जो उन्हें समझने के अहल हों।’’ (यह अद्वितीयता शायर की है, शायरी की नहीं) फिर भी उसके किसी शे’र पर उसका नाम पढ़े बिना हम बता सकते हैं कि यह ‘फै़ज़’ का शे’र है। ‘फ़ैज़’ की शायरी की ‘अद्वितीयता’ आधारित है उसकी शैली के लोच और मंदगति पर, कोमल, मृदुल और सौ-सौ जादू जगाने वाले शब्दों के चयन पर, ‘तरसी हुई नाकाम निगाहें’ और ‘आवाज़ में सोई हुई शीरीनियां’ ऐसी अलंकृत परिभाषाओं और रुपकों पर, और इन समस्त विशेषताओं के साथ गूढ़ से गूढ़ बात कहने के सलीके पर। उर्दू के एक बुजुर्ग शायर ‘असर’ लखनवी ने शायद बिलकुल ठीक लिखा है कि ‘‘ ‘फ़ैज़’ की शायरी तरक़्की के मदारिज (दर्जे’ तय करके अब इस नुक्ता-ए-उरूज (शिखर-बिन्दु) पर पहुंच गई है, जिस तक शायद ही किसी दूसरे तरक्क़ी-पसंद (प्रगतिशील) शायर की रसाई हुई हो। तख़य्युल (कल्पना) ने सनाअत (शिल्प) के जौहर दिखाए हैं और मासूम जज़्बात को हसीन पैकर (आकार) बख़्शा है। ऐसा मालूम होता है कि परियों का एक ग़ौल (झुण्ड) एक तिलिस्मी फ़ज़ा (जादुई वातावरण) में इस तरह मस्ते-परवाज़ (उड़ने में मस्त) है कि एक पर एक की छूत पड़ रही है और क़ौसे-कुज़ह (इन्द्रधनुष) के अक़्कास (प्रतिरूपक) बादलों से सबरंगी बारिश हो रही है......................।’’
अपनी शायरी की तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ‘फ़ैज़’ को किसी ने ऊंचा बोलते नहीं सुना। बातचीत के अतिरिक्त मुशायरों में भी वह इस तरह अपने शे’र पढ़ता है जैसे उसके होंठों से यदि एक ज़रा ऊंची आवाज़ निकल गई तो न जाने कितने मोती चकनाचूर हो जाएंगे। वह सेना में कर्नल रहा, जहां किसी नर्मदिल अधिकारी की गुंजाइश नहीं होती। उसने कालेज की प्रोफ़ेसरी की, जहां कालेज के लड़के प्रोफ़ेसर तो प्रोफ़ेसर शैतान तक को अपना स्वभाव बदलने पर विवश कर दें। उसने रेडियो की नौकरी की, जहां अपने मातहतों को न डांटने का स्वभाव अफ़सर की नालायक़ी समझा जाता है। उसने पत्रकारिता जैसा जोखिम का पेशा भी अपनाया और फिर जब पाकिस्तान सरकार ने इस देवता-स्वरूप व्यक्ति पर हिंसात्मक विद्रोह का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया तब भी मेजर मोहम्मद इसहाक़ (फ़ैज़’ के जेल के साथी) के कथनानुसार, ‘‘कहीं पास-पड़ोस में तू-तू मैं-मैं हो, दोस्तों में तल्ख़-कलामी हो, या यूं ही किसी ने त्योरी चढ़ा रखी हो, फ़ैज़’ की तबीयत ज़रूर खराब हो जाती थी और इसके साथ ही शायरी की कैफ़ियत (मूड) भी काफूर हो जाती थी।’’ ‘‘फ़ैज़’ ने अपने निर्दोष होने का तथा उच्चाधिकारियों के षड्यंत्रों का जिक़्र किया भी तो इस भाषा में :
फ़िक्रे-दिलदारिये-गुलज़ार1 करूं या न करूं
ज़िक्रे-मुर्ग़ाने-गिरफ़्तार2 करूं या न करूं
क़िस्सए-साजिशे-अग़ियार3 कहूं या न कहूं
शिकवए-यारे-तरहदार4 करूं या न करूं
जाने क्या वजअ5 है अब रस्मे-वफ़ा6 की ऐ दिल
वज्ए-देरीना पे7 इसरार8 करूं या न करूं
ज़िक्रे-मुर्ग़ाने-गिरफ़्तार2 करूं या न करूं
क़िस्सए-साजिशे-अग़ियार3 कहूं या न कहूं
शिकवए-यारे-तरहदार4 करूं या न करूं
जाने क्या वजअ5 है अब रस्मे-वफ़ा6 की ऐ दिल
वज्ए-देरीना पे7 इसरार8 करूं या न करूं
‘फ़ैज़’ के स्वर की यह नर्मी और गंभीरता उसके प्राचीन साहित्य के विस्तृत अध्ययन और मौलिक रूप से रोमांटिक ‘शायर होने की देन’
---------------
1.देश-रूपी वाटिका की दिलदारी की चिन्ता 2. कैदी पक्षियों की चर्चा 3. शत्रुओं के षड्यन्त्र की कहानी 4. रंगीले यार की शिकायत 5. तरीक़ा 6.प्रेम निभाने की परिपाटी 7.पुराने ढंग पर 8. आग्रह
है लेकिन उसका रोमांसवाद चूंकि भौतिक संसार का रोमांसवाद है (प्रारम्भ की नज़्मों को छोड़कर) और शायर का कर्त्तव्य उसके मतानुसार यह है कि वह जीवन से अनुभव प्राप्त करे और उस पर अपनी छाप लगाकर उसे फिर से जीवन को लौटा दे, इसलिए उसने बहुत शीघ्र सुर्ख होंठों पर तबस्सुम की ज़िया1 मरमरीं हाथों की लर्ज़िशों, मखमली बांहों और दमकते हुए रुख़्सारों2 के सुनहले पर्दों के उस पार वास्तविकता की झलक देख ली*। आरजुओं के मक़तल3, भूख उगाने वाले खेत, खाक में लिथड़े और खून में नहलाये हुए जिस्म, बाजारों में बिकता हुआ मज़दूर का गोश्त और नातुवानों4 के निवालों पर झपटते हुए उक्क़ाव5 देख लिए और कहने को तो उसने अपनी प्रेयसी से कहा लेकिन वास्तव में वह अपनी रोमांटिक शायरी से सम्बोधित हुआ :
---------------
1.देश-रूपी वाटिका की दिलदारी की चिन्ता 2. कैदी पक्षियों की चर्चा 3. शत्रुओं के षड्यन्त्र की कहानी 4. रंगीले यार की शिकायत 5. तरीक़ा 6.प्रेम निभाने की परिपाटी 7.पुराने ढंग पर 8. आग्रह
है लेकिन उसका रोमांसवाद चूंकि भौतिक संसार का रोमांसवाद है (प्रारम्भ की नज़्मों को छोड़कर) और शायर का कर्त्तव्य उसके मतानुसार यह है कि वह जीवन से अनुभव प्राप्त करे और उस पर अपनी छाप लगाकर उसे फिर से जीवन को लौटा दे, इसलिए उसने बहुत शीघ्र सुर्ख होंठों पर तबस्सुम की ज़िया1 मरमरीं हाथों की लर्ज़िशों, मखमली बांहों और दमकते हुए रुख़्सारों2 के सुनहले पर्दों के उस पार वास्तविकता की झलक देख ली*। आरजुओं के मक़तल3, भूख उगाने वाले खेत, खाक में लिथड़े और खून में नहलाये हुए जिस्म, बाजारों में बिकता हुआ मज़दूर का गोश्त और नातुवानों4 के निवालों पर झपटते हुए उक्क़ाव5 देख लिए और कहने को तो उसने अपनी प्रेयसी से कहा लेकिन वास्तव में वह अपनी रोमांटिक शायरी से सम्बोधित हुआ :
अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा
मुझसे पहली-सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग !
और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा
राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा
मुझसे पहली-सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग !
और फिर रोमांसवाद से पूर्णतया मुक्त उसने राजनीतिक नज़्में भी लिखीं और देश प्रेम को ठीक उसी वेदना और व्यथा के साथ व्यक्त किया जैसा कि प्रेयसी के प्रेम को किया था।
उर्दू के एक आलोचक मुम्ताज़ हुसैन के कथनानुसार उसकी शायरी में अगर एक परम्परा क़ैस (मजनूं) की है तो दूसरी मन्सूर6 की। ‘फ़ैज़’
---------------------
1.मुस्कान की ज्योति 2.कपोलों 3. वध-स्थल 4. दुर्बलों 5.बाजपक्षी 6. एक प्रसिद्ध ईरानी वली जिनका विश्वास था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और उन्होंने ‘अनल-हक’ (सोऽहं-मैं ही परमात्मा हूं) की आवाज़ उठाई थी। उस समय के मुसलमानों को उनका यह नारा अधार्मिक लगा और उन्होंने उन्हें फांसी दे दी।
*(मेरे विचार में इसका एक कारण यह भी है कि इश्क़ ने ‘फ़ैज़’ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उसे अपने-आप में नहीं उलझाए रखा।)
ने इन दोनों परम्पराओं को अपनी शायरी में कुछ इस प्रकार समो लिया है कि उसकी शायरी स्वयं एक परम्परा बन गई है। वह जब भी महफिल में आया, एक छोटी-सी पुस्तक, एक क़तआ़, ग़ज़ल के कुछ शे’र, कुछ यूं ही-सा काव्य-अभ्यास और कुछ क्षमा-याचना की बातें लेकर आया, लेकिन जब भी और जैसे भी आया खूब आया। दोस्त-दुश्मनों ने सिर हिलाया, चर्चा हुई। कुछ लोगों ने यह कहकर पुस्तक पटक दी-इसमें रखा ही क्या है; लेकिन फिर वही पुस्तक के शे’रों को गुनगुनाने भी लगे1। कैसी आश्चर्यजनक वास्तविकता है कि केवल चंद नज़्मों और चंद ग़ज़लों का शायर होने पर भी ‘फ़ैज़’ की शायरी एक बाक़ायदा ‘स्कूल आफ थॉट’ का दर्जा रखती है और नई पीढ़ी का कोई उर्दू शायर अपनी छाती पर हाथ रखकर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी-न-किसी रूप में ‘फ़ैज़’ से प्रभावित नहीं हुआ। रूप और रस, प्रेम और राजनीति कला और विचार का जैसा सराहनीय समन्वय फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ ने प्रस्तुत किया है और प्राचीन परम्पराओं पर नवीन परम्पराओं का महल उसारा है, निःसंदेह वह उसी का हिस्सा है और आधुनिक उर्दू शायरी उसकी इस देन पर जितना गर्व करे कम है।
उर्दू के एक आलोचक मुम्ताज़ हुसैन के कथनानुसार उसकी शायरी में अगर एक परम्परा क़ैस (मजनूं) की है तो दूसरी मन्सूर6 की। ‘फ़ैज़’
---------------------
1.मुस्कान की ज्योति 2.कपोलों 3. वध-स्थल 4. दुर्बलों 5.बाजपक्षी 6. एक प्रसिद्ध ईरानी वली जिनका विश्वास था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और उन्होंने ‘अनल-हक’ (सोऽहं-मैं ही परमात्मा हूं) की आवाज़ उठाई थी। उस समय के मुसलमानों को उनका यह नारा अधार्मिक लगा और उन्होंने उन्हें फांसी दे दी।
*(मेरे विचार में इसका एक कारण यह भी है कि इश्क़ ने ‘फ़ैज़’ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है और उसे अपने-आप में नहीं उलझाए रखा।)
ने इन दोनों परम्पराओं को अपनी शायरी में कुछ इस प्रकार समो लिया है कि उसकी शायरी स्वयं एक परम्परा बन गई है। वह जब भी महफिल में आया, एक छोटी-सी पुस्तक, एक क़तआ़, ग़ज़ल के कुछ शे’र, कुछ यूं ही-सा काव्य-अभ्यास और कुछ क्षमा-याचना की बातें लेकर आया, लेकिन जब भी और जैसे भी आया खूब आया। दोस्त-दुश्मनों ने सिर हिलाया, चर्चा हुई। कुछ लोगों ने यह कहकर पुस्तक पटक दी-इसमें रखा ही क्या है; लेकिन फिर वही पुस्तक के शे’रों को गुनगुनाने भी लगे1। कैसी आश्चर्यजनक वास्तविकता है कि केवल चंद नज़्मों और चंद ग़ज़लों का शायर होने पर भी ‘फ़ैज़’ की शायरी एक बाक़ायदा ‘स्कूल आफ थॉट’ का दर्जा रखती है और नई पीढ़ी का कोई उर्दू शायर अपनी छाती पर हाथ रखकर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी-न-किसी रूप में ‘फ़ैज़’ से प्रभावित नहीं हुआ। रूप और रस, प्रेम और राजनीति कला और विचार का जैसा सराहनीय समन्वय फ़ैज़ अहमद ‘फ़ैज़’ ने प्रस्तुत किया है और प्राचीन परम्पराओं पर नवीन परम्पराओं का महल उसारा है, निःसंदेह वह उसी का हिस्सा है और आधुनिक उर्दू शायरी उसकी इस देन पर जितना गर्व करे कम है।
-प्रकाश पंडित
---------------------------
1.1992 में जब ‘फ़ैज़’जेल में था और उसकी दूसरी पुस्तक ‘दस्ते-सबा’ प्रकाशित हुई थी तो स्वर्गीय सज्जाद ज़हीर (उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार, कम्युनिस्ट नेता और ‘फ़ैज़’ के जेल के साथी) न तो यहां तक कह दिया था कि ‘‘बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद जब लोग रावलपिंडी साज़िश के मुकद्दमे को भूल जाएंगे। और पाकिस्तान का मुवर्रिख़ (इतिहासकार) 1952 के अहम वाक़यात पर नज़र डालेगा तो ग़ालिबन इस साल का सबसे अहम तारीख़ी वाक़या (ऐतिहासिक घटना) नज़्मों की इस छोटी-सी किताब की इशाअत (प्रकाशन) को ही क़रार दिया जाएगा।’’
1.1992 में जब ‘फ़ैज़’जेल में था और उसकी दूसरी पुस्तक ‘दस्ते-सबा’ प्रकाशित हुई थी तो स्वर्गीय सज्जाद ज़हीर (उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार, कम्युनिस्ट नेता और ‘फ़ैज़’ के जेल के साथी) न तो यहां तक कह दिया था कि ‘‘बहुत अरसा गुज़र जाने के बाद जब लोग रावलपिंडी साज़िश के मुकद्दमे को भूल जाएंगे। और पाकिस्तान का मुवर्रिख़ (इतिहासकार) 1952 के अहम वाक़यात पर नज़र डालेगा तो ग़ालिबन इस साल का सबसे अहम तारीख़ी वाक़या (ऐतिहासिक घटना) नज़्मों की इस छोटी-सी किताब की इशाअत (प्रकाशन) को ही क़रार दिया जाएगा।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book