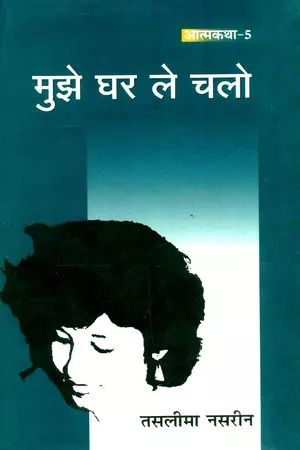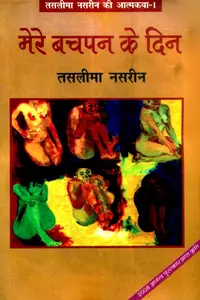|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
बहरहाल समलैंगिक होना मेरा सपना था। मैंने तो सोचा था कि मैं समलैंगिक शायद हो गई हूँ। लेकिन नहीं, इतने सबके बाद भी, इतने बोधोदय के बाद भी, दानियल जैसी जबर्दस्त समझौताहीन नारीवादी के संग-साथ के बावजूद, मर्द के परित्याग करने के लिए, समलैंगिक होने की जरूरत की तमाम अ-आ, क-ख जान-समझ लेने के बावजूद, आखिरकार मैं समलैंगिक नहीं बन सकी। सुदर्शन पुरुष देखते ही मेरे मन में कामवासना जाग उठती है।
बर्लिन में काफी लंबे अर्से तक मैं गहरी उदासी झेलती रही। यह रोग झेलते हुए उद्भ्रांत की तरह, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं की वेचैनी में कटती है। मेरे भी दिन कुछ इसी तरह गुजरते रहे। एक दौर ऐसा भी आया, जब मैं बंगालियों के अड्डे में जा पड़ी। उन्हीं दिनों एक सुदर्शन पुरुष से मेरी जान-पहचान हो गई, लेकिन वह सुदर्शन बेचारा उत्थानरहित था, पर ऐसा भी नहीं था कि मैंने उसे उसी पल धता वता दी। जब बदन की पोर-पोर में निःसंगता की आग धधक रही हो, तुम किसी रैस्केल' को भी दूर कर देने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन मन के आवेग लढककर दोस्ती पर उतर आते हैं और जब तुम यह शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाते हो, तब वह दोस्ती भी लुढ़कती-पुढ़कती किसी अतल सागर में उतर जाती है और टुप् से रुल-मिलकर जिंदगी-भर के लिए गुम हो जाती है। इसका मैंने बखूबी नजारा किया है। आमंत्रण पाकर मैं नए-नए शहरों में जाती हूँ, सात दिनों में ही किसी-किसी से गाढ़ी दोस्ती कायम हो जाती है। कितने ही देशों में, कितने ही शहरों में, जाने कितनी एलिजाबेथ, कितनी ऐन, कितनी मारिया, कितनी डायना, कितने-कितने जन, कितनी क्रिश्चन, कितने पीटर, कितनी पैट्रीशिया, कितनी मिशेल, कितनी मार्गरेटा के साथ दोस्ती हुई। जाने कितनी औरतें विदा देते समय लिपटकर रोईं। विदा लेते समय मैं भी सोचती हूँ कि उनसे मेरा नाता-रिश्ता जिंदगी-भर बना रहेगा, लेकिन जैसे ही वह शहर छोड़कर वापस लौटती हूँ। उन लोगों से संपर्क का सारा पता-ठिकाना, कागजों के ढेर में जाने किस कोने में गुम हो जाता है। महीना गुजरते ही उसका नाम-धाम कुछ भी याद नहीं रहता। समूचे कमरे में कागजों का ढेर लगा रहता है। विभिन्न देशों, विभिन्न संगठनों, संग्रामी महिलाओं, सेकुलर मानववादियों, लेखक-कवियों के पते-ठिकानों के अंबार! बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारी दोस्ती कायम हो जाती है। बाद में जब तुम घर में अकेले होते हो, तब तुम यह फैसला नहीं कर पाते कि किसे छोइँ और किससे संपर्क करूँ! तुम किसी का खत खोलकर नहीं पढ़ते। तुम फैक्स पर नज़र डालकर, छोड़ देते हो। तुम खत का जवाब नहीं देते, दूर के सभी लोगों को तुम भूल जाते हो। जो लोग आस-पास होते हैं, वस तुम उन्हीं लोगों में व्यस्त हो जाते हो। यह क्या काफी कुछ अस्तित्ववादियों जैसा जीवन है? का डियम में विश्वास करना? या जो लोग गहरी उदासी और हताशा के शिकार हैं, उनका आचरण क्या ऐसा ही होता है? मैं इन सबके बारे में बूंद-भर भी नहीं सोचती। मानो मैं बस-स्टैंड पर खड़ी हूँ। लोग आ-जा रहे हैं। मैं किसी-किसी से एकाध बातें कर लेती हूँ। मैं अपने घर जाने के लिए बस के इंतज़ार में हूँ। मेरे सच्चे यार-दोस्त वही हैं, मेरे सच्चे स्वजन वहीं हैं। अब, सुयेनसन की ही बात करें। किसी एक दिन उसके साथ पूरी एक रात गुजार दी। लंबे दो सालों बाद, किसी पुरुष का अंग-संग! पहली ही रात सुयेनसन ने अपनी हल्की-फुल्की उँगलियों से सहलाते हुए ऐसा स्पर्श दिया, मानो वे उँगलियाँ नहीं, रेशम-पांखें हों। किसी बंगाली प्रेमी से ऐसा प्यार मुझे कभी नहीं मिला। वह सिर्फ मिशनरी आसन में, अचल बैठा नहीं रहता। पश्चिम के परम जैसा वह भले न हो, उसने दो-तीन ऐसे विचित्र-विचित्र आसनों की राह दिखाई कि आँखों में अज्ञान का अँधेरा लिए, मैं एक-दो कदम बढ़ने लगी। उसे अपने करीब पाने के लिए मेरी व्याकुलता बढ़ने लगी। वह शख्स सूरत-शक्ल से चाहे जैसा भी हो, वह सुदर्शन नहीं था। उसके प्रति मेरे मन में हल्का-सा मोह भी जागे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कल्पनातीत ढंग से मैं वह सब करती रही। मैं सुयेनसन के लिए व्याकुल हो उठी। जितना मैं आकुल होती थी, उससे दुगुना मेरा शरीर अकुलाता था। सुयेनसन के प्रति आकुल-व्याकुल होने की वजह यह थी कि वह घोर असामाजिक, अरसिक, असुंदर भले ही हो, उसका आचरण-व्यवहार भले ही अस्वाभाविक हो, उसके दिमाग में भले ही अॅरिजम नामक रोग पल रहा हो, लेकिन वह उत्थानरहित नहीं था। मैं निश्चित सेक्स-संपर्क की उम्मीद में सुयेनसन से चिपकी रही। मुझे लगभग यह अहसास तो होता रहा कि उसके साथ मेरा प्रेम जैसा कुछ होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, शायद दोस्ती जैसी कुछ होने वाली थी। असल में शायद दोस्ती भी नहीं हुई, बस, मुझे ऐसा अहसास होता रहा। मैं खुद ही सोचती रही और अपने मन को दिलासा देती रही। मेरे सामने जो निःसंगता मुँह बाए खड़ी थी, उससे मैं अपने को बचाती रही।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ