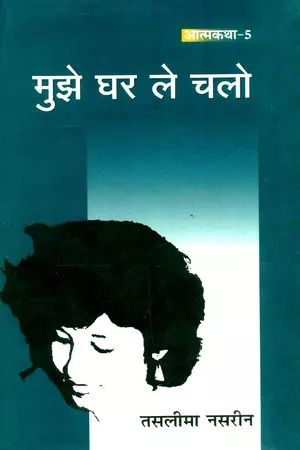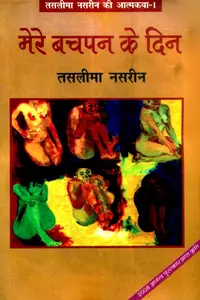|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
मैं यूरोप लौट आयी। अपने अकेले घर में! जिंदगी के जिस आंगन में मेरे टूटे हुए सपने बिखरे पड़े थे, उसी आंगन में!
...किसी वक्त, एक बार फिर, मैं जमा करने लगती हूँ सपने!
जमा करती जाती हूँ और बुदबुदाती हूँ-
"मैं सजा रही हूँ, जी, अपने बक्से-पिटारी
जाना है मुझे ढाका, कलकत्ता!"
वहाँ किसी दोस्त या रिश्तेदार का दर खटखटाते ही,
कोई-न-कोई खोल ही देगा, अपने दरवाजे!
मुझे बिठाएगा, मछली-भात खिलाएगा और पान की गिलौरी भी!
विदेश आखिर कब तक सहा जाए?
कब तक सहा जाए घर-मकान, बाज़ार-हाट?
मशीन-वशीन, कौड़ी-कौड़ी हिसाब-किताब?
यहाँ कोई, किसी के इंतज़ार में नहीं होता,
इंसान अपने घर में अकेले ही पड़ा रोता,
अकेले-अकेले ही दम तोड़ देता है!
मुझे तो जाना है, ढाका! कलकत्ता!
चलूँगी-फिरूँगी भीड़ भरी सड़कों पर,
कभी ट्राम, कभी बस में, कभी रिक्शे में
या फिर हनहनाती हुई पैदल-पैदल, कहीं किसी ओर!
किसी बरामदे की रेलिंग से छाती टिकाए,
खोजभरी आँखों से निहार रहा होगा, गली का मोड़,
कोई अपने आंचल से पोंछेगी, मेरे माथे का पसीना,
मेरी खैरियत पूछते हुए, रो देगा कोई बूढ़ा, झर!झर!
हाँ, मैं समेट रही हूँ, अपना बक्सा-पिटारा,
मुझे अपने देश जाना है,
जहाँ झाड़-जंगल में, जल में, डोंगी में धरा है मेरा हृदय,
मुझे जाना है, ढाका! कलकत्ता!
चौरंगी से चितपुर, श्यामली से शांतिवाग़ तक बहड़ाकर,
किसी दुःखवती देह में लगी आग बुझाने को,
लगाऊँगी छलांग मैं, किसी दिन!
अब आती है मौत, तो आए भले!
लगाये रहती हूँ कान...
डालवी से सोल निलसन नामक एक लड़की, ट्रेन से दो घंटे का सफ़र तय करके महीने में दो वार मुझसे मिलने आती है। वह लड़की अपने साथ पापड़, काजू, बादाम, तेंतुल, आम का अचार, रसगुल्ले की व्यंजन-विधि वगैरह भी लाती है। उसका ख्याल है कि ये सब चीज़े मुझे थोड़ा-बहुत अपने देश का स्वाद देंगी।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ