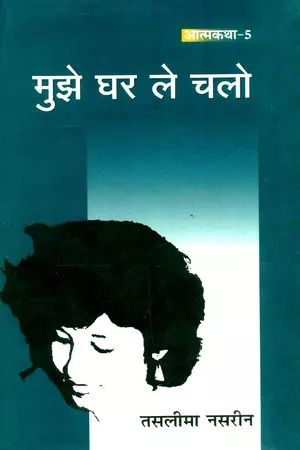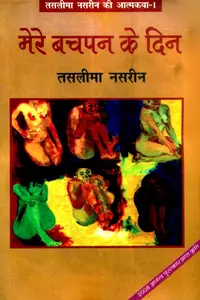|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
में जहाँ भी रहूँ, जहाँ भी जाऊँ, मेरा मन देश में ही पड़ा रहता है! मैं किसी हाल भी अपने मन को, अपने पास नहीं रख पाती। मेरा मन, इस निस्तब्ध जीवन में किसी हाल भी नहीं रहना चाहता। मेरी आधी-आधी रातें निपट गूंगी हो जाती हैं और उन रातों में सिर्फ सिवारों के हुँआ-हुँआ की आवाजें गूंजती हैं। मेरी आँखों की पलकें समूची रात-रात भर खुली रहती हैं!
आधी रात के फोन तुम वजो मत!
तुम्हें दे रही हूँ तकिया, काँथा-कम्बल, नींद की दवा, सब कुछ
तुम सो जाओ।
पूरा शहर पड़ा है मुर्दे जैसा इस वक्त, आकाश भी सो गया है सितारे
बुझाकर।
तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में बहने लगती है ढेर सारी बर्फ,
मैं हो जाती हूँ पत्थर,
काल बैसाखी में जिस तरह काँपते हैं जराजीणं खजूर के पत्ते
वैसी ही काँपती है मेरी देह।
पलक झपकते ही उतर आते हैं टिड्डीदल मेरे धान दूर्वा पर...
स्वजन बंधुहीन पड़ी हूँ अकेली, इतनी दूर वर्फ के देश में।
अचानक ही अट्टहास
करने लगती हैं खबरें राजनीति के पंकिल मैदान में
दौड़ते हैं मूर्ख उनके पीछे,
मौका पाते ही आँगन में, मैदान में,
धान खेतों में रोपने लगते हैं धर्म के बीज।
बस रही हैं बस्तियाँ, गाँव भरते जा रहे हैं पतिताओं, पीरों, भिखारियों से।
पिता के दिल का दर्द, पता चला, बढ़ जाता है इधर और,
आँखों से भी दिखता है कम,
न जाने दोस्त अहबाब एक-एक करके जाने कहाँ रहे हैं भाग-
आधी रात के फोन, बजो मत! इतनी रात को कोई नहीं है जगा,
रात के शराबी भी सब सो गए हैं,
तुम भी सो जाओ।
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ