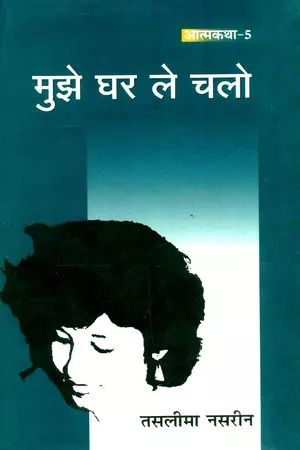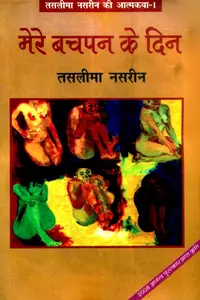|
जीवनी/आत्मकथा >> मुझे घर ले चलो मुझे घर ले चलोतसलीमा नसरीन
|
419 पाठक हैं |
|||||||
औरत की आज़ादी में धर्म और पुरुष-सत्ता सबसे बड़ी बाधा बनती है-बेहद साफ़गोई से इसके समर्थन में, बेबाक बयान
नहीं, यह कोई वोलपुर नहीं, वनानी या बंग वाज़ार की भीड़ भी नहीं! मैं अकेली हूँ! भयंकर अकेली! हज़ारों लोगों की भीड़ घेरे हुए! फिर भी मुझ जैसी अकेली और कोई भी नहीं। नहीं, इस दुनिया में इतनी अकेली, और कोई नहीं है। मेरे इस घर का हर सामान पराये देश का है। हर सामान में, हर चीज में कुछ अजनबी सी गंध! मैं खुद अपनी नज़रों में अजनवी होती जा रही हूँ। पागलों की तरह, हाँ, निपट पागलों की तरह ही, मैं वावर्चीखाने में जा घुसती हूँ, दिन में, रात में, आधी रात में! प्लेट में भात निकालती हूँ। जन्म-जन्म का जाना-पहचाना भात!
इन दिनों खाने की मेज पर लगातार बैठती हूँ लेकर मछली-भात
कलाई डुबोकर लेती हूँ दाल, सानती हूँ,
हिलता है वायाँ हाथ बार-बार मक्खियाँ भगाने की तरह
स्कैंडेनेविया के शीत नियंत्रित घर में।
कीट-पतंगों का नामोनिशान न होने के बावजूद
फिर भी न जाने क्या भगाती रहती हूँ मन ही मन
दुःख?
मछली के मलिन टुकड़े, सब्जी थाली के एक छोर रखे नमक
और रसे से तर सने हुए भात से हटना नहीं चाहता हाथ
इच्छा करती है इसी तरह सानती रहूँ भात, खाती जाऊँ,
अपने गोपन में क्या मैं यह समझती नहीं कि सोने की चम्मच छोड़कर
क्यों इतनी लालायित रहती हूँ भात का स्वाद-गंध लेने हेतु।
असल में भात के स्पर्श से भात नहीं
लगता है मुट्ठी में आ जाता है भरपूर बांग्लादेश!
|
|||||
- जंजीर
- दूरदीपवासिनी
- खुली चिट्टी
- दुनिया के सफ़र पर
- भूमध्य सागर के तट पर
- दाह...
- देह-रक्षा
- एकाकी जीवन
- निर्वासित नारी की कविता
- मैं सकुशल नहीं हूँ