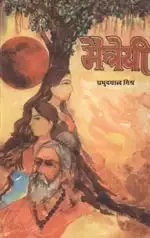|
पौराणिक >> मैत्रेयी मैत्रेयीप्रभुदयाल मिश्र
|
366 पाठक हैं |
||||||
औपनिषदिक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
.....‘‘इस कथानक की मैत्रैयी स्वयं से पूछ सकती है—उसे
क्यों आवश्यक है आत्म साक्षात्कार के अनेक युगों के पश्चात् स्त्री-स्त्री
और पुरुष की त्रिकोणीय परिधि में प्रस्तुत होना ! उसे तो अब अपने आपको
शास्त्रार्थ की विषय वस्तु के रूप में भी परोसना होगा। और इसमें यदि
व्यंग्य, विनोद और उपहास का पात्र बनती है, तो क्या यह उसकी नियति है ? आज
जनक (महज एक पात्र !) की ज्ञान सभा में खुली हुई केश राशि, आवेगपूर्ण मुख
मण्डल और गहन जीवनानुभव की बोझिल वाणी से शास्त्रार्थ को उद्यत मैत्रेयी
पुनः एक चुनौती है, किसी याज्ञावल्क्य की नहीं, स्वयं और समाज की
भी।
धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं
शरं ह्युपासनानिशितं सन्धयीत
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि।
शरं ह्युपासनानिशितं सन्धयीत
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि।
(मुंडकोपनिषद् 2, सं.2, मं.3)
(हे सौम्य, उपनिषद् के धनुषरूपी महास्त्र पर उपासना के तीक्ष्ण बाण का
सन्धान करके अपनी चेतना को उसके भाव से तदाकार करते हुए अक्षर ब्रह्म का
लक्ष्य भेद कर।)
यह उपन्यास
उपनिषदों का शिल्प कथात्मक संवाद का है। इन कथाओं का ओर-छोर पाना प्रायः
आसान नहीं है। पुराण और इतिहास के माध्यम से अटूट मिथक परम्परा का
ताना-बाना बुनने वाली प्राचीन भारतीय मेधा उपनिषदों में कुछ सूत्र पकड़कर
जैसे अदृश्य हो जाती है। मुझे लगा है कि यदि इन बिखरे हुए कथा-सूत्रों को
पिरो दिया जाय तो जो इतिवृत्त बनता है वह कथा साहित्य की रोचक धरोहर बन
सकता है।
छांदोग्योपनिषद् की पृष्ठभूमि में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का ‘अनामदास का पोथा’ (अथ रैक्व आख्यान) संभवतः इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया था। छांदोग्योपनिषद् के रहस्यपूर्ण ऋषि रैक्व प्रायः अपनी पीठ खुजलाते हुए एक बालगाड़ी के नीचे पड़े रहते, किन्तु उनसे यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि ‘सबकुछ हवा है’ महाराज जानश्रुति अपार संपत्ति और अपनी चन्द्रमुखी कन्या का भी दान कर देते हैं।
आत्म तत्त्व के अन्वीक्षण और ब्रह्मवार्ता में निमग्न वैदिक ऋषियों की विज्ञान यात्रा संवेदनाशून्य नहीं थी। जनक की ज्ञान सभा में वचक्नु की पुत्री गार्गी से याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ मुझे ‘याज्ञवल्क्य द्वे भार्ये वभूवतुः’ (याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं—बृहदारण्यकोपनिषद् 4/5/1) की आधार भूमि लगता रहा है।
उपनिषद् के अनुसार इनके नाम कात्यायनी और मैत्रेयी थे। मुझे अपनी धारणा के समर्थन में डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर के भारतीय भाषा परिषद् कलकत्ता से प्रकाशित संस्कृत वाङ्मय कोष के प्रथम खण्ड, पृष्ठ 419 में मत प्राप्त हुआ कि ‘योगी याज्ञवल्क्य के संपादक पी.सी.दीवाणजी ने गार्गी को याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद् में—याज्ञवल्क्य द्वे भार्ये वभूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च— कहा गया है। इस वाक्य में केवल दो पत्नियों का निर्देश होने से वाचक्नवी गार्गी का ही अपर नाम मैत्रेयी माना जाता है।’
प्राचीन राजाओं की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश भी पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं, किन्तु जहाँ राजवंश राजाओं के कुलों का अनुसरण कर तैयार किये गए हैं, वहाँ ऋषियों के वंश प्रायः सर्वत्र शिष्य परंपरा के रूप में हैं। यथार्थ में इसे ‘विद्यावंश’ कहा जा सकता है। किन्तु उपनिषदों के ऋषियों के नाम और उनकी परंपरा को एक सूत्र में पिरोना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। बृहदारण्यक उपनिषद् के छठें अध्याय के पाँचवें ब्राह्मण में ऋषियों की एक वंशावली भी दी है जिसमें शिष्य के नाम के आगे उसके गुरु के नाम का उल्लेख है।
इन नामों में दिलचस्प बात यह है कि ये ऋषि के मूल नाम न होकर प्रायः उनके परंपरामूलक नाम है। इसका एक और रोचक तथ्य यह है कि ये सभी नाम प्रायः मातृपरक हैं।
इतिहास और वह भी वैदिक इतिहास की पुनर्रचना किसी मानवीय सामर्थ्य का विष नहीं है। अतः इस दिशा में यदि किंचित् भी प्रयास संभव है, तो वह इस परंपरा के उस संवेदी स्वर की पहचान का हो सकता है, जो शाश्वत है और चिरनवीन भी।
इस कथानक की मैत्रेयी स्वयं से पूछ सकती है—उसे क्यों आवश्यक है आत्मसाक्षात्कार के अनेक युगों के पश्चात स्त्री-पुरुष की त्रिकोणीय परिधि में प्रस्तुत होना ! और यदि वह एक अर्थ में अनजान रही तो अनेक नाम और रूपों में लगातार प्रकट भी तो थी ! इसलिए उसे एक युग और काल की ही विशिष्ठ पहचान क्यों आवश्यक है ?
वह यह अच्छी तरह जानती है कि इस प्रकार उसके सार्वजनिक हो जाने पर उसे स्वयं से इन दुरह प्रश्नों को पूछना ही होगा। अब उसे अपने आपको शास्त्रार्थियों की सभा की विषय-वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत करना होगा। और इसमें यदि वह व्यंग्य, विनोद और उपहास की पात्र भी बनती है, तो यह उसी नियति है। आज जनक की ज्ञान-सभा में खुली हुई केशराशि, आवेगपूर्ण मुखमण्डल और गहन जीवनानुभव की बोझिल वाणी से शास्त्रार्थ को उद्यत मैत्रेयी पुनः एक चुनौती है, किसी याज्ञवल्क्य को ही नहीं बल्कि स्वयं और समाज को भी।
छांदोग्योपनिषद् की पृष्ठभूमि में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का ‘अनामदास का पोथा’ (अथ रैक्व आख्यान) संभवतः इसी पृष्ठभूमि में लिखा गया था। छांदोग्योपनिषद् के रहस्यपूर्ण ऋषि रैक्व प्रायः अपनी पीठ खुजलाते हुए एक बालगाड़ी के नीचे पड़े रहते, किन्तु उनसे यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि ‘सबकुछ हवा है’ महाराज जानश्रुति अपार संपत्ति और अपनी चन्द्रमुखी कन्या का भी दान कर देते हैं।
आत्म तत्त्व के अन्वीक्षण और ब्रह्मवार्ता में निमग्न वैदिक ऋषियों की विज्ञान यात्रा संवेदनाशून्य नहीं थी। जनक की ज्ञान सभा में वचक्नु की पुत्री गार्गी से याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ मुझे ‘याज्ञवल्क्य द्वे भार्ये वभूवतुः’ (याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं—बृहदारण्यकोपनिषद् 4/5/1) की आधार भूमि लगता रहा है।
उपनिषद् के अनुसार इनके नाम कात्यायनी और मैत्रेयी थे। मुझे अपनी धारणा के समर्थन में डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर के भारतीय भाषा परिषद् कलकत्ता से प्रकाशित संस्कृत वाङ्मय कोष के प्रथम खण्ड, पृष्ठ 419 में मत प्राप्त हुआ कि ‘योगी याज्ञवल्क्य के संपादक पी.सी.दीवाणजी ने गार्गी को याज्ञवल्क्य की पत्नी कहा है। बृहदारण्यक उपनिषद् में—याज्ञवल्क्य द्वे भार्ये वभूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च— कहा गया है। इस वाक्य में केवल दो पत्नियों का निर्देश होने से वाचक्नवी गार्गी का ही अपर नाम मैत्रेयी माना जाता है।’
प्राचीन राजाओं की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश भी पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं, किन्तु जहाँ राजवंश राजाओं के कुलों का अनुसरण कर तैयार किये गए हैं, वहाँ ऋषियों के वंश प्रायः सर्वत्र शिष्य परंपरा के रूप में हैं। यथार्थ में इसे ‘विद्यावंश’ कहा जा सकता है। किन्तु उपनिषदों के ऋषियों के नाम और उनकी परंपरा को एक सूत्र में पिरोना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। बृहदारण्यक उपनिषद् के छठें अध्याय के पाँचवें ब्राह्मण में ऋषियों की एक वंशावली भी दी है जिसमें शिष्य के नाम के आगे उसके गुरु के नाम का उल्लेख है।
इन नामों में दिलचस्प बात यह है कि ये ऋषि के मूल नाम न होकर प्रायः उनके परंपरामूलक नाम है। इसका एक और रोचक तथ्य यह है कि ये सभी नाम प्रायः मातृपरक हैं।
इतिहास और वह भी वैदिक इतिहास की पुनर्रचना किसी मानवीय सामर्थ्य का विष नहीं है। अतः इस दिशा में यदि किंचित् भी प्रयास संभव है, तो वह इस परंपरा के उस संवेदी स्वर की पहचान का हो सकता है, जो शाश्वत है और चिरनवीन भी।
इस कथानक की मैत्रेयी स्वयं से पूछ सकती है—उसे क्यों आवश्यक है आत्मसाक्षात्कार के अनेक युगों के पश्चात स्त्री-पुरुष की त्रिकोणीय परिधि में प्रस्तुत होना ! और यदि वह एक अर्थ में अनजान रही तो अनेक नाम और रूपों में लगातार प्रकट भी तो थी ! इसलिए उसे एक युग और काल की ही विशिष्ठ पहचान क्यों आवश्यक है ?
वह यह अच्छी तरह जानती है कि इस प्रकार उसके सार्वजनिक हो जाने पर उसे स्वयं से इन दुरह प्रश्नों को पूछना ही होगा। अब उसे अपने आपको शास्त्रार्थियों की सभा की विषय-वस्तु के रूप में भी प्रस्तुत करना होगा। और इसमें यदि वह व्यंग्य, विनोद और उपहास की पात्र भी बनती है, तो यह उसी नियति है। आज जनक की ज्ञान-सभा में खुली हुई केशराशि, आवेगपूर्ण मुखमण्डल और गहन जीवनानुभव की बोझिल वाणी से शास्त्रार्थ को उद्यत मैत्रेयी पुनः एक चुनौती है, किसी याज्ञवल्क्य को ही नहीं बल्कि स्वयं और समाज को भी।
प्रभुदयाल मिश्र
‘‘.....‘‘इस कथानक की मैत्रैयी
स्वयं से पूछ सकती
है—उसे क्यों आवश्यक है आत्म साक्षात्कार के अनेक युगों के
पश्चात्
स्त्री-स्त्री और पुरुष की त्रिकोणीय परिधि में प्रस्तुत होना ! उसे तो अब
अपने आपको शास्त्रार्थ की विषय वस्तु के रूप में भी परोसना होगा। और इसमें
यदि व्यंग्य, विनोद और उपहास का पात्र बनती है, तो क्या यह उसकी नियति है
? आज जनक (महज एक पात्र !) की ज्ञान सभा में खुली हुई केश राशि, आवेगपूर्ण
मुख मण्डल और गहन जीवनानुभव की बोझिल वाणी से शास्त्रार्थ को उद्यत
मैत्रेयी पुनः एक चुनौती है, किसी याज्ञवल्क्य की नही, स्वयं और समाज की
भी।
मधुकाण्ड
‘मैत्रेयी, ओ मैत्रेयी’। ऋषि याज्ञवल्क्य ने
प्रातःकालीन सन्ध्या, तर्पणादि नित्य विधान से निवृत्त होकर पुकारा।
ऋषि की प्रथम पत्नी कात्यायनी उनके निकट ही उपस्थित थीं। उन्होंने अनुमान किया कि ऋषिवर को अग्निहोत्र के लिए समिधाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। वे तत्काल काष्ठादि के कोष से कुछ समिधायें लेकर उनके पास पहुँच गईं।
‘भगवन् लीजिए, आपकी परम प्रिया तो आज किसी गहन आध्यात्म चिन्तन में लगी हुई हैं। ब्रह्म मुहूर्त से मैं अनेक बार उसके पास होकर लौट आई हूँ, किन्तु उसकी समाधि टूटने का नाम ही नहीं ले रही है।’
‘बैठो, कात्यायनी बैठो। मुझे तुम दोनों से ही एक महत्त्वपूर्ण बात करनी है।
अरी मैत्रेयी...।’
‘मैं आई ब्रह्मवादिन, अभी आई।’ मैत्रेयी का दूरस्थ स्वर निकट होने लगा है।
‘आपकी क्या सेवा करूँ देव ?’
‘यहाँ बैठो। तुम दोनों मेरे समक्ष बैठो और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनो।’
ऋषि याज्ञवल्क्य गम्भीर हो चले थे। ऋषि-पत्नियाँ स्पष्ट देख रही थीं कि ऋषि की दृष्टि सामने बैठी उस नारी-मूर्तियों के पार बहुत दूर कहीं छिटकी हुई है। जैसे ऋषि चेतनतया वहाँ थे ही नहीं जहाँ उनकी भौतिक देह उपस्थित थी।
‘भगवान् ! कात्यायनी ने चिन्ताकुल होकर कहा। ‘मुझसे कोई अवज्ञा तो नहीं हुई है ? कहीं मैत्रेयी को मुझसे कोई कष्ट तो नहीं पहुँचा है ? क्या मैंने आपको किसी प्रकार रुष्ट कर दिया है, स्वामी ?’
‘नहीं, नहीं कात्यायनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम स्त्रीधर्म, गार्हस्थिक कर्म और संसार साधन में परम निपुण हो। तुम्हारे व्यवहार में किसी प्रकार की त्रुटि का प्रश्न नहीं उठता।’
‘वास्तव में निरंतर त्रुटि करते हुए भी मुझे दण्ड न देना आपने आपना स्वभाव बना लिया है, मुनिवर’, मैत्रेयी बोल उठी। ‘एक ओर तो गृह-कार्य में देवी कात्यायनी की कोई सहायता नहीं करती हूँ और दूसरी ओर आपके कर्म और उपासना से पृथक् कर बार-बार ज्ञान खण्ड में ले जाकर आपकी साधना की एकनिष्ठता में भी बाधा उत्पन्न करती हूँ।’’
‘देवियों, तुम दोनों ही अपनी-अपनी पृथक् पहचान से मुझे परम प्रिय हो। वास्तव में इससे ही तुम्हारे व्यक्तित्वों को वह विशिष्टता मिली है, जो तुम्हें एक-दूसरे की पूरक बनाती है। फिर एक-दूसरे की छिद्रान्वेषिता के स्थान पर तुम परस्पर अपनी ही त्रुटियों के निराकरण में लगी रहती हो। इससे तुममें कलह की कभी कोई स्थित उत्पन्न नहीं होती। स्पष्ट तो यही है कि तुममें से कोई भी मेरे किसी असंतोष का कारण नहीं है।’
‘देववर, तब ‘मैत्रेयी बोली, ‘आज आप इतने गम्भीर क्यों हैं ? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने अग्निहोत्र भी अब तक नहीं किया है।’
‘तुम्हें ज्ञात है मैत्रेयी, विदेह राजा जनक की सभा में वह प्रसंग जिसमें परम ज्ञानी राजा ने समस्त भूमण्डल के विद्याव्यसनियों को एकत्र कर स्वर्ण से मंडित श्रृंगों वाली एक सहस्र गायें ब्रह्मवेत्ता को दिए जाने की घोषणा की थी। उस सभा में उपस्थित अपूर्ण विद्वत् मण्डली में अश्वल, आर्त्तभाग, लाह्यायनि भुज्यु, चाक्रायण उषस्त, कहोल, आरुणि, उद्दालक और परम विदुषी के रूप में तुम स्वयं उपस्थित थीं।
वास्तव में उस अपार गोधन को देखकर उस समय मुझे एक क्षण को राजा जनक की उस शर्त का स्मरण नहीं हो रहा। इस आश्रम से जाते हुए मुझे तो केवल कात्यायनी का अभावग्रस्त आँगन ही दिखाई दे रहा था। उस दिन इस देवी ने मेरे प्रातःकालीन अग्निहोत्र में अपने संग्रह का समस्त गोघृत समाप्त कर दिया था।’
मैत्रेयी, नहीं गार्गी, वाचक्वनी गार्गी, मेधावी, तार्किक, ब्रह्मविदुषी गार्गी। अगणित ब्रह्मवेत्ताओं से सुशोभित राजा जनक की सभा में अपनी वाग्विदग्धता और प्रखर तार्किकता से चमत्कृत कर देने वाली एक तेजस्विनी युवती गार्गी !
याज्ञवल्क्य को अपने अतीत का वह परम रोमांचक पल याद आ रहा है। उन्हें अभी अपना शास्त्राज्ञान पूरा किये हुए कुछ ही समय बीता था। अपने विद्याध्ययनकाल से लेकर अब तक उन्हें कोई ऐसा अपूर्व शास्त्रज्ञान और आत्मज्ञानी नहीं मिला था, जो ज्ञानवल में उनसे न्यून न ठहरा हो। किन्तु अब उन्हें कात्यायनी की गृहस्थी और अपने आश्रम को भी व्यवस्थित करना था। इसके लिए पर्याप्त गोधन और स्वर्ण का संचय आवश्यक था।
ऐसे ही समय उन्हें राजा जनक की सभा का जब शास्त्रार्थ कि निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उन्होंने कात्यायनी को आश्वस्त किया था कि अब उसे गोधन और स्वरण सम्पदा की उपलब्धता के प्रति निश्चिंत होना चाहिए। पृथ्वी लोक में तत्समय उन्हें आत्मज्ञान के क्षेत्र में कोई पराजित कर सकेगा, ऐसा उनके अनुमान में नहीं आया था।
किन्तु आज गार्गी और उसके बाद की बनी यह मैत्रेयी भी निश्चित ही अपराजेय थी। गंगा की धवल धारा-सी उद्गम वेग वाली वह शुभ्र बाला उन्हें उस समय कुछ अधिक ज्ञानोन्मत ही प्रतीत हो रही थी। उस रूपवासना में स्त्रीजनोचित लज्जा के स्थान पर उन्हें ज्ञान का गुमान ही तो दिखाई देता था।
ऋषि की प्रथम पत्नी कात्यायनी उनके निकट ही उपस्थित थीं। उन्होंने अनुमान किया कि ऋषिवर को अग्निहोत्र के लिए समिधाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। वे तत्काल काष्ठादि के कोष से कुछ समिधायें लेकर उनके पास पहुँच गईं।
‘भगवन् लीजिए, आपकी परम प्रिया तो आज किसी गहन आध्यात्म चिन्तन में लगी हुई हैं। ब्रह्म मुहूर्त से मैं अनेक बार उसके पास होकर लौट आई हूँ, किन्तु उसकी समाधि टूटने का नाम ही नहीं ले रही है।’
‘बैठो, कात्यायनी बैठो। मुझे तुम दोनों से ही एक महत्त्वपूर्ण बात करनी है।
अरी मैत्रेयी...।’
‘मैं आई ब्रह्मवादिन, अभी आई।’ मैत्रेयी का दूरस्थ स्वर निकट होने लगा है।
‘आपकी क्या सेवा करूँ देव ?’
‘यहाँ बैठो। तुम दोनों मेरे समक्ष बैठो और मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनो।’
ऋषि याज्ञवल्क्य गम्भीर हो चले थे। ऋषि-पत्नियाँ स्पष्ट देख रही थीं कि ऋषि की दृष्टि सामने बैठी उस नारी-मूर्तियों के पार बहुत दूर कहीं छिटकी हुई है। जैसे ऋषि चेतनतया वहाँ थे ही नहीं जहाँ उनकी भौतिक देह उपस्थित थी।
‘भगवान् ! कात्यायनी ने चिन्ताकुल होकर कहा। ‘मुझसे कोई अवज्ञा तो नहीं हुई है ? कहीं मैत्रेयी को मुझसे कोई कष्ट तो नहीं पहुँचा है ? क्या मैंने आपको किसी प्रकार रुष्ट कर दिया है, स्वामी ?’
‘नहीं, नहीं कात्यायनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम स्त्रीधर्म, गार्हस्थिक कर्म और संसार साधन में परम निपुण हो। तुम्हारे व्यवहार में किसी प्रकार की त्रुटि का प्रश्न नहीं उठता।’
‘वास्तव में निरंतर त्रुटि करते हुए भी मुझे दण्ड न देना आपने आपना स्वभाव बना लिया है, मुनिवर’, मैत्रेयी बोल उठी। ‘एक ओर तो गृह-कार्य में देवी कात्यायनी की कोई सहायता नहीं करती हूँ और दूसरी ओर आपके कर्म और उपासना से पृथक् कर बार-बार ज्ञान खण्ड में ले जाकर आपकी साधना की एकनिष्ठता में भी बाधा उत्पन्न करती हूँ।’’
‘देवियों, तुम दोनों ही अपनी-अपनी पृथक् पहचान से मुझे परम प्रिय हो। वास्तव में इससे ही तुम्हारे व्यक्तित्वों को वह विशिष्टता मिली है, जो तुम्हें एक-दूसरे की पूरक बनाती है। फिर एक-दूसरे की छिद्रान्वेषिता के स्थान पर तुम परस्पर अपनी ही त्रुटियों के निराकरण में लगी रहती हो। इससे तुममें कलह की कभी कोई स्थित उत्पन्न नहीं होती। स्पष्ट तो यही है कि तुममें से कोई भी मेरे किसी असंतोष का कारण नहीं है।’
‘देववर, तब ‘मैत्रेयी बोली, ‘आज आप इतने गम्भीर क्यों हैं ? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने अग्निहोत्र भी अब तक नहीं किया है।’
‘तुम्हें ज्ञात है मैत्रेयी, विदेह राजा जनक की सभा में वह प्रसंग जिसमें परम ज्ञानी राजा ने समस्त भूमण्डल के विद्याव्यसनियों को एकत्र कर स्वर्ण से मंडित श्रृंगों वाली एक सहस्र गायें ब्रह्मवेत्ता को दिए जाने की घोषणा की थी। उस सभा में उपस्थित अपूर्ण विद्वत् मण्डली में अश्वल, आर्त्तभाग, लाह्यायनि भुज्यु, चाक्रायण उषस्त, कहोल, आरुणि, उद्दालक और परम विदुषी के रूप में तुम स्वयं उपस्थित थीं।
वास्तव में उस अपार गोधन को देखकर उस समय मुझे एक क्षण को राजा जनक की उस शर्त का स्मरण नहीं हो रहा। इस आश्रम से जाते हुए मुझे तो केवल कात्यायनी का अभावग्रस्त आँगन ही दिखाई दे रहा था। उस दिन इस देवी ने मेरे प्रातःकालीन अग्निहोत्र में अपने संग्रह का समस्त गोघृत समाप्त कर दिया था।’
मैत्रेयी, नहीं गार्गी, वाचक्वनी गार्गी, मेधावी, तार्किक, ब्रह्मविदुषी गार्गी। अगणित ब्रह्मवेत्ताओं से सुशोभित राजा जनक की सभा में अपनी वाग्विदग्धता और प्रखर तार्किकता से चमत्कृत कर देने वाली एक तेजस्विनी युवती गार्गी !
याज्ञवल्क्य को अपने अतीत का वह परम रोमांचक पल याद आ रहा है। उन्हें अभी अपना शास्त्राज्ञान पूरा किये हुए कुछ ही समय बीता था। अपने विद्याध्ययनकाल से लेकर अब तक उन्हें कोई ऐसा अपूर्व शास्त्रज्ञान और आत्मज्ञानी नहीं मिला था, जो ज्ञानवल में उनसे न्यून न ठहरा हो। किन्तु अब उन्हें कात्यायनी की गृहस्थी और अपने आश्रम को भी व्यवस्थित करना था। इसके लिए पर्याप्त गोधन और स्वर्ण का संचय आवश्यक था।
ऐसे ही समय उन्हें राजा जनक की सभा का जब शास्त्रार्थ कि निमंत्रण प्राप्त हुआ तो उन्होंने कात्यायनी को आश्वस्त किया था कि अब उसे गोधन और स्वरण सम्पदा की उपलब्धता के प्रति निश्चिंत होना चाहिए। पृथ्वी लोक में तत्समय उन्हें आत्मज्ञान के क्षेत्र में कोई पराजित कर सकेगा, ऐसा उनके अनुमान में नहीं आया था।
किन्तु आज गार्गी और उसके बाद की बनी यह मैत्रेयी भी निश्चित ही अपराजेय थी। गंगा की धवल धारा-सी उद्गम वेग वाली वह शुभ्र बाला उन्हें उस समय कुछ अधिक ज्ञानोन्मत ही प्रतीत हो रही थी। उस रूपवासना में स्त्रीजनोचित लज्जा के स्थान पर उन्हें ज्ञान का गुमान ही तो दिखाई देता था।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book