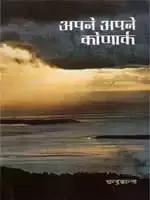|
उपन्यास >> अपने अपने कोणार्क अपने अपने कोणार्कचन्द्रकान्ता
|
358 पाठक हैं |
||||||
इसमें कश्मीर से उड़ीसा तक का सफर का वर्णन
Apne Apne Konark a hindi book by Chandrakanta - अपने अपने कोणार्क - चन्द्रकान्ता
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
अपने-अपने कोणार्क यानी कश्मीर से उड़ीसा का सफर ! कश्मीर की सरसब्ज़ वादी में जन्मी और पली-बढ़ी चन्द्रकान्ता को भारत के अनेक प्रान्तों में रहने-बसने का मौका मिला। लेकिन उड़ीसा में बिताए गए छह वर्ष उनकी सर्जनात्मकता के लिए अमूल्य बन गए। उन्होंने वहाँ की जीवन-शैली, लोक रंगों और परंपराओं की महक महसूस की है, जिसका जीवंत प्रमाण है अपने-अपने कोणार्क !
उड़ीसा की संस्कृति धरोहर—पुरी और कोणार्क, जीवन के दो पहलू ; सम्पूर्ण जीवन का फलसफा यहाँ मौजूद है, जिसे लेखिका ने ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य के साथ की सच्चाइयों से जोड़कर देखा है। उपन्यास की नायिका कुनी के माध्यम से उन्होंने आम ओडिया जन को उसके विगत और वर्तमाव के साथ प्रस्तुत किया है। ‘मोर गौरव जगन्नाथ’ में विश्वास करता आम ओडिया जन अपने परंपरागत आलोक से मुग्ध, रक्षणशील तथा संस्कारवान भी है और हम सबकी तरह अंधविश्वासी और रूढ़ मानसकिता से ग्रस्त भी। कुनी इसी रक्षणशील परिवार की बड़ी बेटी है, हजारहा दायित्वों की साँकलों में कैद, गोकि वह उन्हें साँकलें समझती नहीं। वह अपनी लीक आप बनाती, वक्त की सच्चाइयों के रू-ब-रू होते अपने भीतर को जानने और पाने की कोशिश करती है।
उड़ीसा की पृष्ठभूमि में वहाँ के इंद्रधनुषी रंगों को समेटे कुनी की यह कहानी सच की तलाश है।
उड़ीसा की संस्कृति धरोहर—पुरी और कोणार्क, जीवन के दो पहलू ; सम्पूर्ण जीवन का फलसफा यहाँ मौजूद है, जिसे लेखिका ने ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य के साथ की सच्चाइयों से जोड़कर देखा है। उपन्यास की नायिका कुनी के माध्यम से उन्होंने आम ओडिया जन को उसके विगत और वर्तमाव के साथ प्रस्तुत किया है। ‘मोर गौरव जगन्नाथ’ में विश्वास करता आम ओडिया जन अपने परंपरागत आलोक से मुग्ध, रक्षणशील तथा संस्कारवान भी है और हम सबकी तरह अंधविश्वासी और रूढ़ मानसकिता से ग्रस्त भी। कुनी इसी रक्षणशील परिवार की बड़ी बेटी है, हजारहा दायित्वों की साँकलों में कैद, गोकि वह उन्हें साँकलें समझती नहीं। वह अपनी लीक आप बनाती, वक्त की सच्चाइयों के रू-ब-रू होते अपने भीतर को जानने और पाने की कोशिश करती है।
उड़ीसा की पृष्ठभूमि में वहाँ के इंद्रधनुषी रंगों को समेटे कुनी की यह कहानी सच की तलाश है।
शुरुआत से पहले
सत्य की दुनिया का कोई मार्ग नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं ही खोजना होता है....
जे. कृष्णमूर्ति
मेरे पहले दो उपन्यास-ऐलान गली ज़िंदा है और यहाँ वितस्ता बहती है-कश्मीर के मध्यवर्गीय जन की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भाव-भूमि के आख्यान हैं। और अपने-अपने कोणार्क ! यानी कश्मीर से उड़ीसा का सफ़र। कश्मीर की सरसब्ज़ वादी मेरी जन्मभूमि है। वहाँ का विशिष्ट परिवेश और वहाँ के लोकरंग मेरे मन में बसे हैं, मेरी सोंच और मेरे संस्कारों का हिस्सा हैं। लेकिन फिर भारत के अनेक प्रांतों में रहने–बसने का अवसर मुझे मिला-आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदि की जीवन-शैली, लोकरंगों और परंपराओं की महक मैंने महसूस की है और उनके विशिष्ट परिवेश को तहेदिल से जिया भी है।
उड़ीसा में छह वर्ष रहकर मैंने बहुत-कुछ पाया और बहुत-कुछ महसूसा। वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कोणार्क के शिल्पियों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। पुरी और कोणार्क-जीवन के दो पहलू ! अर्कक्षेत्र और श्रीक्षेत्र के भिन्न रंग ! संपूर्ण जीवन का फलसफा यहाँ मौजूद है। उसे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य के साथ, वर्तमान की सच्चाइयों के साथ जोड़कर देखा, तो अपने-अपने कोणार्क बन गया। संयोग से मुझे वहाँ कुनी मिली, उसने मुझे कायाप्रवेश की इजाज़त दी। वह माध्यम बनी आम ओड़िया जन को उसके विगत और वर्तमान के साथ प्रस्तुत करने के लिए। ‘मोर गौरव जगन्नाथ’ में विश्वास करता आम ओड़िया जन अपने पारंपरिक आलोक से मुग्ध, रक्षणशील एवं संस्कारवान भी है और हम सबकी तरह अंधविश्वासी एवं रूढ़ मानसिकता से ग्रस्त भी।
कुनी ऐसे ही एक रक्षणशील परिवार की बड़ी बेटी है-हजारहा दायित्वों की साँकलों में कैद, जिसके लिए परपुरुष से प्रेम, पाप है। लेकिन एक दिन कुनी ने रामकृष्ण को पढ़ा और जाना कि यदि चाहना पाप है, तो मन में चाह का उगना भी पाप है। कुनी तमाम हदबंदियों के बावजूद मन में चाह का उगना रोक नहीं पाई, और यहीं उसके आस्थावादी सोच में दरार पड़ गई। सच क्या है और झूठ क्या ? अंतरंग और बहिरंग दोनों को खँगालकर वह किस सच तक पहुँच पाई ? उड़ीसा की पृष्ठभूमि में वहाँ के इंद्रधनुषी रंगों को समेटे कुनी की यह कहानी सच की तलाश है....
उड़ीसा में छह वर्ष रहकर मैंने बहुत-कुछ पाया और बहुत-कुछ महसूसा। वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर कोणार्क के शिल्पियों ने मुझे बेहद प्रभावित किया। पुरी और कोणार्क-जीवन के दो पहलू ! अर्कक्षेत्र और श्रीक्षेत्र के भिन्न रंग ! संपूर्ण जीवन का फलसफा यहाँ मौजूद है। उसे ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिदृश्य के साथ, वर्तमान की सच्चाइयों के साथ जोड़कर देखा, तो अपने-अपने कोणार्क बन गया। संयोग से मुझे वहाँ कुनी मिली, उसने मुझे कायाप्रवेश की इजाज़त दी। वह माध्यम बनी आम ओड़िया जन को उसके विगत और वर्तमान के साथ प्रस्तुत करने के लिए। ‘मोर गौरव जगन्नाथ’ में विश्वास करता आम ओड़िया जन अपने पारंपरिक आलोक से मुग्ध, रक्षणशील एवं संस्कारवान भी है और हम सबकी तरह अंधविश्वासी एवं रूढ़ मानसिकता से ग्रस्त भी।
कुनी ऐसे ही एक रक्षणशील परिवार की बड़ी बेटी है-हजारहा दायित्वों की साँकलों में कैद, जिसके लिए परपुरुष से प्रेम, पाप है। लेकिन एक दिन कुनी ने रामकृष्ण को पढ़ा और जाना कि यदि चाहना पाप है, तो मन में चाह का उगना भी पाप है। कुनी तमाम हदबंदियों के बावजूद मन में चाह का उगना रोक नहीं पाई, और यहीं उसके आस्थावादी सोच में दरार पड़ गई। सच क्या है और झूठ क्या ? अंतरंग और बहिरंग दोनों को खँगालकर वह किस सच तक पहुँच पाई ? उड़ीसा की पृष्ठभूमि में वहाँ के इंद्रधनुषी रंगों को समेटे कुनी की यह कहानी सच की तलाश है....
चंद्रकान्ता
एक
आज एक मुद्दत बाद फिर किसी का हाथ थामे मैं कोणार्क के सागर तट पर बैठी हूँ। पाँवों-तले भूरी सुनहरी रेत का सुकूनदेह अहसास, ऊपर छितरी रुई के बिनौले समेटता नीला आसमान और नजरों की हदें बांधता दिगंत तक फैला बेअंत, बेकरार समुद्र ! ऐसे में कई साल पहले पूछा सिद्धार्थ का एक प्रश्न अचानक मेरे ज़ेहन में गूँज उठा है-क्या शांब का यह मुक्ति-स्थल तुम्हारी मुक्ति की जगह नहीं हो सकती ?’
सिद्धार्थ आज यहाँ नहीं है। उसे गए एक अरसा हो गया है। और मैं ? मैं भी तो वह कुनी नहीं हूँ जिससे सिद्धार्थ ने यह सवाल पूछा था। कितना कुछ तो रीत गया है बीच के वक़्त के साथ। फिर सालों-साल बीतने के बाद भी यह आवाज़ यहाँ रुक कैसे गई है ?
सागर की छाती में उमगता झागल लहरों का उफ़ान कई-कई गज़ ऊँचा उठता किनारों की तरफ़ लपक रहा है और ढेर सारे शंख-सीपियों के तोहफ़े थमाकर लौट जाता है, फिर आने का वादा करता हुआ। हम मुग्ध होकर देख रहे हैं, मैं और अनिरुद्ध। बिल्कुल ख़ामोश। बेताब सूर्य, किरणों का जाल उतावली में समेट रहा है और पारे से थिरकते सुवर्ण रंगों में सागर बेहद कोमल हो उठा है। एक-दूसरे में आत्मलीन होने का यह रोमांच, कई साल पहले, यहीं, इसी भुरभुरी नरम रेती के कालीन पर बैठे मैंने महसूस किया था। लेकिन तब मेरे साथ अनिरुद्ध नहीं, सिद्धार्थ था, और शायद यही इस आवाज़ के लौटने का कारण है। मैं यही थी पर मन दूसरा था। उजली दूब-सा मुग्ध हरा मन ! पक्की उम्र होने के बावजूद अछूता। आसमान की ऊँचाइयों में उड़ान भरती सोनचिरी नन्हे पंखों से आकाश मापने के उछाह से भरी थी। फेनिल लहरों के भीतर घुसकर पानी का बेपरवाह दबाव महसूस करते हमने उन लहरों से खिलवाड़ किया था। सागर ने मुझमें हिलोर भर दी थी। मेरे पाँव में घुँघरू बाँध दिए थे। वह क्या मैं ही थी ? कोणार्क के नृत्य-मंडप की कोई सोई नर्तकी अँगड़ाई लेकर जाग उठी थी, सदियों की नींद के बाद, और अथाह लहरों पर ताल देती बेसुध होकर थिरकने लगी थी।
यह मैं हूँ, मैं कुनी ! तुमने मेरे पैरों में नृत्य की लय भर दी है। मेरे मन में सदियों की प्यास ! मेरे भीतर छिपे मनाहीवाले कक्ष में ज्वारभाटों का झागल उफान भर दिया है तुमने। सागर ! तुम साक्षी हो मेरे भीतर फूटते इन रंगीन आबशारों के, जिनके फूटने को रोकना किसी के बस में नहीं। लेकिन उम्र के कई पड़ाव पार कर जहाँ आज मैं खड़ी हूँ वहाँ उन्माद-भरी शोखी में थिरकते पाँव वक़्त की धूल में चलते मंद पड़ा गए हैं। समय उन्माद को थाम लेना जानता है न ? यहीं, सागर-तट की इसी बालू पर एक दिन सिद्धार्थ ने दो नाम लिखे थे-कुनी-सिद्धार्थ ! जिन्हें जिद्दी लहरें बार-बार मिटाती जा रही थीं और वह बार-बार लिखता जा रहा था। आज जब अनिरुद्ध ने भी दो नाम इसी बालू पर लिखे, तो मैं अनायास ही सालों पहले लिखे दो नाम ढ़ूँढने लगी। कुछ पल आश्चर्य से अनिरुद्ध को देखा। वक़्त ने दागदार बनाते भी उसके भीतर कोई सोता बचाए रखा है। वह बड़ी उदारता से हँस पड़ा, ज्यों कहना चाह रहा हो, ‘मेरे भीतर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी नहीं।’ तब अचानक पीछे छूटे समय का कोई बेशकीमती टुकड़ा मेरे सामने ज़िंदा हो गया-जैसे बड़े सहज भाव से कंधा छूकर किसी ने मुड़कर पीछे देखने के लिए उकसा दिया हो। नहीं, मन में कोई अपराधबोध नहीं जगा। पीछे छूटे का अफ़सोस भी नहीं। बस, यादों की एक बंद खिड़की खुल गई।
अनिरुद्ध के साथ मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत-जैसा कुछ करने जा रही हूँ। पर क्या ज़िंदगी की शुरुआत जन्म लेते ही नहीं होती ? हर अनुभव उसमें नये सत्य जोड़ देता है। खोना-पाना, सब मानी हुई शर्तें हैं।
सिद्धार्थ मालूम नहीं, आज कहाँ है। उसके लिए कुछ मायने रखता था तो वह था अंतरात्मा से स्वीकार किए अनुभवों को ईमानदारी से जीना, जोड़-तोड़ के फलसफ़ों के बिना। उसके प्रभावों को बिना शिकवे सह लेना। यही वह बार-बार कहता था। आज वह जहाँ भी हो, पर सागर सांध्य की इस मिलन बेला में बरसों पहले उसका मेरे साथ यहाँ होना उतना ही सच था जितना आज अनिरुद्ध के साथ मेरा यहाँ होना। आज सागर में उतरते सूर्य की छुअन से गुलाबी-सुनहरे रंगों में सराबोर लहरों को अपलक देखते मेरा मन पीछे लौटने लगा है। मुड़कर पीछे देखने को उतावला हो उठा है। क्यों ? नहीं जानती। किसलिए ? वह भी नहीं। यों मैं आदी नहीं हूँ मुड़कर पीछे देखने की। फिर आज क्यों ? नहीं, प्रश्न नहीं पूछना। है कोई ऐसा जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा ? तमाम दावों के बावजूद ! मैंने तो कोई दावे किए ही नहीं।
पड़ाव-दर-पड़ाव ज़िंदगी जीती रही। आज खुद से अलग होकर खुद को देखने की चाह जगी है। आत्मावलोकन ? खुद को समझने की ख़ातिर ? या कि अपने से जुड़ा तमाम जनों की मानसिकता को जानने के लिए ? शायद जी चुके वक़्त की सच्चाइयों में अपनी अर्थवत्ता को खोजने के लिए ! जीवन में जो भी निर्णय मैंने लिए, फिर से उन्हें जी लूँ तो क्या वे निर्णय दूसरे होंगे ? जैसे जी ली उससे हटकर कुछ अलग ठंग से जीना होगा क्या ? शायद नहीं। वह सब तो वैसे ही होना था। उस दिन भी जब सामने यही समुद्र था, यही पानियों की छुअन से भीग-भीग जाता तट ! देर तक हम यहीं बैठे इसे अपने भीतर उतरते महसूस करते रहे थे। वह जैसे मुझे पहली बार देख रहा था। उसका एकटक देखते रहना मुझमें उलझन पैदा कर रहा था।
‘‘क्या देख रहे हो इस तरह ?’’
‘‘किस तरह ?’’
‘‘ऐसे घूर-घूरकर।’’
‘‘यह घूरना है ? धत् तेरे की ! पूरे रोमांस का कचरा कर दिया।’’
‘‘मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह देखना।’’ मैं उसकी हंसी से और भी सिकुड़ गई थी। लगता था कि मेरे धड़कते दिल की आवाज़ भी वह सुन रहा है।
‘‘कुनी ! मुझसे कोई पूछे कि मुझे तुममे क्या अच्छा लगता है तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा।’’
‘‘मुझमें ऐसा कुछ ख़ास तो है ही नहीं....’’
‘‘नहीं, नहीं अभी जो तुम्हें घूर रहा था’, तुम्हारे कहे, तो मुझे फ़िराक़ का एक शेर याद आया। इजाज़त हो तो सुनाऊँ ?’’
फ़िराक़ ? कौन फ़िराक़ ? मैं फ़िराक़ गोरखपुरी को तब तक जानती ही कहाँ थी ! उसने शेर सुनाया था-‘फिज़ा को जैसे कोई राग चीरता जाय, तेरी निगाह दिल में यूँ ही उतर आयी... तुम्हारी इन नज़रों में ही कोई ख़ास बात है।’’
‘‘मेरी निगाह क्या कोई खंजर है ? कोई चाकू जो दिल को चीर जाए...’’
‘‘फिर मेरे मूड को हलाल कर रही हो, देखो,’’ वह धमकाते लहज़े में बोला था। हमने पता नहीं क्या-क्या अनर्गल कहा, सुना, हल्का-गहरा, बचकाना सब, अच्चा लगा। बीच-बीच में वह गंभीर हो उठता।
‘‘कुनी ! मैं अकेला होता हूँ तो सागर मुझे उदास कर देता है, अपने भीतर डूबने को उकसाता है, पर तुम्हारे साथ वह मुझे अल्हड़ बना गया है।’’ एक-दूसरे का हाथ पकड़े हम दोनों घुटनों-घुटनों पानी में उतरे थे, एक-दूसरे को भिगोते छेड़ते सागर की फेनिल लहरों के ज्वारभाटे हमारे भीतर भी पछाड़ें मारने लगे थे पर हर मन की उस भावदशा को एक-दूसरे से छिपा रहे थे। मैं शायद उससे ज्यादा। उसके करीब आने पर मैं बार-बार खुद को सिकोड़ लेती थी। तभी नारियल-पानी पीते उसने मुझसे सीधा-सा सवाल किया था, ‘‘कुनी ! तुम तो आज तक प्रेम को अश्लील समझती खुद को पवित्र बनाए रखने का दंभ पालती रही हो, क्या ईमानदारी से कह सकती हो कि तुम्हारे मन में प्रेम करने की इच्छा कभी जगी ही नहीं ?’’
‘‘शायद नहीं।’’ इस अचानक, बिना भूमिका बाँधे किए प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूँ, समझ नहीं पाई।
‘‘आज भी नहीं, मेरे साथ ? सच कहना।’’
पता नहीं वह किस एक्सरे नज़र से मेरे भीतर के अचीन्हें कोने तलाशने लगा था। मुझे जैसे किसी ने चोरी करते रँगे हाथ पकड़ लिया। इतना सीधा सवाल ?
‘‘मैं नहीं जानती।’’ पता नहीं मैं कैसे कह गयी। मेरे भीतर अचानक कोई उन्मादी लहर उफनाने लगी थी और मेरा बरसों का तप छलकने लगा था।
‘‘सचमुच नहीं जानतीं, या जानना नहीं चाहतीं ?’’
‘‘प्लीज़ सिद्धार्थ, मुझसे ऐसे सवाल न करो।’’ मेरी आवाज़ टूटने लगी थी। ‘‘इतना करीब तो मैं पहले किसी के नहीं आई।’’ मेरा लहज़ा आत्म-स्वीकार का था।
उसने हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया था। अपने कंधे से मेरा माथा टिकाकर, झुककर उस पर होंठ रख दिए थे। बस, कहा कुछ भी नहीं। मेरी आँखें छलक आईं और मैं बाहों का घेरा बनाकर उसके करीब खिंच आई। हमारा वह पहला चुंबन इसी सागर ने देखा और खुशी से उफन पड़ा। लहरें हमें छाती तक भिगो गईं।
यही टूरिस्ट बँगला था, यही झाऊ का वन ! इन लंबे-ऊँचे पेड़ों के बीच एक-दूसरे का हाथ थामें हम साथ-साथ चले थे। मैं हवा पर पाँव रखे आकाश में उड़ रही थी। मेरे चारों ओर की दुनिया या तो रसातल में समा गई थी या मैं ही धरती से ऊपर उठ गई थी। वहाँ कोई भय, कोई चिंता, कोई पीछा करती आँख मुझ तक पहुँच नहीं सकती थी। सिद्धार्थ चलते-चलते जी. शंकर कुरुप की पंक्तियाँ गुनगुना रहा था और मैं एक-एक शब्द पी रही थी। उसकी आवाज़ बेहद मीठी थी। झाऊ के वनों के बीच तैरती हुई-सी बह रही थी-
सिद्धार्थ आज यहाँ नहीं है। उसे गए एक अरसा हो गया है। और मैं ? मैं भी तो वह कुनी नहीं हूँ जिससे सिद्धार्थ ने यह सवाल पूछा था। कितना कुछ तो रीत गया है बीच के वक़्त के साथ। फिर सालों-साल बीतने के बाद भी यह आवाज़ यहाँ रुक कैसे गई है ?
सागर की छाती में उमगता झागल लहरों का उफ़ान कई-कई गज़ ऊँचा उठता किनारों की तरफ़ लपक रहा है और ढेर सारे शंख-सीपियों के तोहफ़े थमाकर लौट जाता है, फिर आने का वादा करता हुआ। हम मुग्ध होकर देख रहे हैं, मैं और अनिरुद्ध। बिल्कुल ख़ामोश। बेताब सूर्य, किरणों का जाल उतावली में समेट रहा है और पारे से थिरकते सुवर्ण रंगों में सागर बेहद कोमल हो उठा है। एक-दूसरे में आत्मलीन होने का यह रोमांच, कई साल पहले, यहीं, इसी भुरभुरी नरम रेती के कालीन पर बैठे मैंने महसूस किया था। लेकिन तब मेरे साथ अनिरुद्ध नहीं, सिद्धार्थ था, और शायद यही इस आवाज़ के लौटने का कारण है। मैं यही थी पर मन दूसरा था। उजली दूब-सा मुग्ध हरा मन ! पक्की उम्र होने के बावजूद अछूता। आसमान की ऊँचाइयों में उड़ान भरती सोनचिरी नन्हे पंखों से आकाश मापने के उछाह से भरी थी। फेनिल लहरों के भीतर घुसकर पानी का बेपरवाह दबाव महसूस करते हमने उन लहरों से खिलवाड़ किया था। सागर ने मुझमें हिलोर भर दी थी। मेरे पाँव में घुँघरू बाँध दिए थे। वह क्या मैं ही थी ? कोणार्क के नृत्य-मंडप की कोई सोई नर्तकी अँगड़ाई लेकर जाग उठी थी, सदियों की नींद के बाद, और अथाह लहरों पर ताल देती बेसुध होकर थिरकने लगी थी।
यह मैं हूँ, मैं कुनी ! तुमने मेरे पैरों में नृत्य की लय भर दी है। मेरे मन में सदियों की प्यास ! मेरे भीतर छिपे मनाहीवाले कक्ष में ज्वारभाटों का झागल उफान भर दिया है तुमने। सागर ! तुम साक्षी हो मेरे भीतर फूटते इन रंगीन आबशारों के, जिनके फूटने को रोकना किसी के बस में नहीं। लेकिन उम्र के कई पड़ाव पार कर जहाँ आज मैं खड़ी हूँ वहाँ उन्माद-भरी शोखी में थिरकते पाँव वक़्त की धूल में चलते मंद पड़ा गए हैं। समय उन्माद को थाम लेना जानता है न ? यहीं, सागर-तट की इसी बालू पर एक दिन सिद्धार्थ ने दो नाम लिखे थे-कुनी-सिद्धार्थ ! जिन्हें जिद्दी लहरें बार-बार मिटाती जा रही थीं और वह बार-बार लिखता जा रहा था। आज जब अनिरुद्ध ने भी दो नाम इसी बालू पर लिखे, तो मैं अनायास ही सालों पहले लिखे दो नाम ढ़ूँढने लगी। कुछ पल आश्चर्य से अनिरुद्ध को देखा। वक़्त ने दागदार बनाते भी उसके भीतर कोई सोता बचाए रखा है। वह बड़ी उदारता से हँस पड़ा, ज्यों कहना चाह रहा हो, ‘मेरे भीतर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी नहीं।’ तब अचानक पीछे छूटे समय का कोई बेशकीमती टुकड़ा मेरे सामने ज़िंदा हो गया-जैसे बड़े सहज भाव से कंधा छूकर किसी ने मुड़कर पीछे देखने के लिए उकसा दिया हो। नहीं, मन में कोई अपराधबोध नहीं जगा। पीछे छूटे का अफ़सोस भी नहीं। बस, यादों की एक बंद खिड़की खुल गई।
अनिरुद्ध के साथ मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत-जैसा कुछ करने जा रही हूँ। पर क्या ज़िंदगी की शुरुआत जन्म लेते ही नहीं होती ? हर अनुभव उसमें नये सत्य जोड़ देता है। खोना-पाना, सब मानी हुई शर्तें हैं।
सिद्धार्थ मालूम नहीं, आज कहाँ है। उसके लिए कुछ मायने रखता था तो वह था अंतरात्मा से स्वीकार किए अनुभवों को ईमानदारी से जीना, जोड़-तोड़ के फलसफ़ों के बिना। उसके प्रभावों को बिना शिकवे सह लेना। यही वह बार-बार कहता था। आज वह जहाँ भी हो, पर सागर सांध्य की इस मिलन बेला में बरसों पहले उसका मेरे साथ यहाँ होना उतना ही सच था जितना आज अनिरुद्ध के साथ मेरा यहाँ होना। आज सागर में उतरते सूर्य की छुअन से गुलाबी-सुनहरे रंगों में सराबोर लहरों को अपलक देखते मेरा मन पीछे लौटने लगा है। मुड़कर पीछे देखने को उतावला हो उठा है। क्यों ? नहीं जानती। किसलिए ? वह भी नहीं। यों मैं आदी नहीं हूँ मुड़कर पीछे देखने की। फिर आज क्यों ? नहीं, प्रश्न नहीं पूछना। है कोई ऐसा जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा ? तमाम दावों के बावजूद ! मैंने तो कोई दावे किए ही नहीं।
पड़ाव-दर-पड़ाव ज़िंदगी जीती रही। आज खुद से अलग होकर खुद को देखने की चाह जगी है। आत्मावलोकन ? खुद को समझने की ख़ातिर ? या कि अपने से जुड़ा तमाम जनों की मानसिकता को जानने के लिए ? शायद जी चुके वक़्त की सच्चाइयों में अपनी अर्थवत्ता को खोजने के लिए ! जीवन में जो भी निर्णय मैंने लिए, फिर से उन्हें जी लूँ तो क्या वे निर्णय दूसरे होंगे ? जैसे जी ली उससे हटकर कुछ अलग ठंग से जीना होगा क्या ? शायद नहीं। वह सब तो वैसे ही होना था। उस दिन भी जब सामने यही समुद्र था, यही पानियों की छुअन से भीग-भीग जाता तट ! देर तक हम यहीं बैठे इसे अपने भीतर उतरते महसूस करते रहे थे। वह जैसे मुझे पहली बार देख रहा था। उसका एकटक देखते रहना मुझमें उलझन पैदा कर रहा था।
‘‘क्या देख रहे हो इस तरह ?’’
‘‘किस तरह ?’’
‘‘ऐसे घूर-घूरकर।’’
‘‘यह घूरना है ? धत् तेरे की ! पूरे रोमांस का कचरा कर दिया।’’
‘‘मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह देखना।’’ मैं उसकी हंसी से और भी सिकुड़ गई थी। लगता था कि मेरे धड़कते दिल की आवाज़ भी वह सुन रहा है।
‘‘कुनी ! मुझसे कोई पूछे कि मुझे तुममे क्या अच्छा लगता है तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा।’’
‘‘मुझमें ऐसा कुछ ख़ास तो है ही नहीं....’’
‘‘नहीं, नहीं अभी जो तुम्हें घूर रहा था’, तुम्हारे कहे, तो मुझे फ़िराक़ का एक शेर याद आया। इजाज़त हो तो सुनाऊँ ?’’
फ़िराक़ ? कौन फ़िराक़ ? मैं फ़िराक़ गोरखपुरी को तब तक जानती ही कहाँ थी ! उसने शेर सुनाया था-‘फिज़ा को जैसे कोई राग चीरता जाय, तेरी निगाह दिल में यूँ ही उतर आयी... तुम्हारी इन नज़रों में ही कोई ख़ास बात है।’’
‘‘मेरी निगाह क्या कोई खंजर है ? कोई चाकू जो दिल को चीर जाए...’’
‘‘फिर मेरे मूड को हलाल कर रही हो, देखो,’’ वह धमकाते लहज़े में बोला था। हमने पता नहीं क्या-क्या अनर्गल कहा, सुना, हल्का-गहरा, बचकाना सब, अच्चा लगा। बीच-बीच में वह गंभीर हो उठता।
‘‘कुनी ! मैं अकेला होता हूँ तो सागर मुझे उदास कर देता है, अपने भीतर डूबने को उकसाता है, पर तुम्हारे साथ वह मुझे अल्हड़ बना गया है।’’ एक-दूसरे का हाथ पकड़े हम दोनों घुटनों-घुटनों पानी में उतरे थे, एक-दूसरे को भिगोते छेड़ते सागर की फेनिल लहरों के ज्वारभाटे हमारे भीतर भी पछाड़ें मारने लगे थे पर हर मन की उस भावदशा को एक-दूसरे से छिपा रहे थे। मैं शायद उससे ज्यादा। उसके करीब आने पर मैं बार-बार खुद को सिकोड़ लेती थी। तभी नारियल-पानी पीते उसने मुझसे सीधा-सा सवाल किया था, ‘‘कुनी ! तुम तो आज तक प्रेम को अश्लील समझती खुद को पवित्र बनाए रखने का दंभ पालती रही हो, क्या ईमानदारी से कह सकती हो कि तुम्हारे मन में प्रेम करने की इच्छा कभी जगी ही नहीं ?’’
‘‘शायद नहीं।’’ इस अचानक, बिना भूमिका बाँधे किए प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूँ, समझ नहीं पाई।
‘‘आज भी नहीं, मेरे साथ ? सच कहना।’’
पता नहीं वह किस एक्सरे नज़र से मेरे भीतर के अचीन्हें कोने तलाशने लगा था। मुझे जैसे किसी ने चोरी करते रँगे हाथ पकड़ लिया। इतना सीधा सवाल ?
‘‘मैं नहीं जानती।’’ पता नहीं मैं कैसे कह गयी। मेरे भीतर अचानक कोई उन्मादी लहर उफनाने लगी थी और मेरा बरसों का तप छलकने लगा था।
‘‘सचमुच नहीं जानतीं, या जानना नहीं चाहतीं ?’’
‘‘प्लीज़ सिद्धार्थ, मुझसे ऐसे सवाल न करो।’’ मेरी आवाज़ टूटने लगी थी। ‘‘इतना करीब तो मैं पहले किसी के नहीं आई।’’ मेरा लहज़ा आत्म-स्वीकार का था।
उसने हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया था। अपने कंधे से मेरा माथा टिकाकर, झुककर उस पर होंठ रख दिए थे। बस, कहा कुछ भी नहीं। मेरी आँखें छलक आईं और मैं बाहों का घेरा बनाकर उसके करीब खिंच आई। हमारा वह पहला चुंबन इसी सागर ने देखा और खुशी से उफन पड़ा। लहरें हमें छाती तक भिगो गईं।
यही टूरिस्ट बँगला था, यही झाऊ का वन ! इन लंबे-ऊँचे पेड़ों के बीच एक-दूसरे का हाथ थामें हम साथ-साथ चले थे। मैं हवा पर पाँव रखे आकाश में उड़ रही थी। मेरे चारों ओर की दुनिया या तो रसातल में समा गई थी या मैं ही धरती से ऊपर उठ गई थी। वहाँ कोई भय, कोई चिंता, कोई पीछा करती आँख मुझ तक पहुँच नहीं सकती थी। सिद्धार्थ चलते-चलते जी. शंकर कुरुप की पंक्तियाँ गुनगुना रहा था और मैं एक-एक शब्द पी रही थी। उसकी आवाज़ बेहद मीठी थी। झाऊ के वनों के बीच तैरती हुई-सी बह रही थी-
‘‘दिन लंबा नहीं है
और उजाले को
लूट ले जानेवाली रात भी दूर नहीं
हमेशा के लिए सो जाना पड़ेगा
उससे पहले ही दोनों हाथ लूट लो
जीवन की मदिरा
व्यर्थ न करो उसका एक कण भी....’’
और उजाले को
लूट ले जानेवाली रात भी दूर नहीं
हमेशा के लिए सो जाना पड़ेगा
उससे पहले ही दोनों हाथ लूट लो
जीवन की मदिरा
व्यर्थ न करो उसका एक कण भी....’’
उसकी आवाज़ मुझे छू रही थी। हाथों की छुअन शिराओं को नरम-गरम टकोरे दे रही थी। बहुत पास हम एक-दूसरे की धड़कनों की आवाज़ सुन रहे थे, देह की बेआवाज़ पुकार ! लेकिन मैं इतना जल्दी पिघलकर बहना नहीं चाहती थी। सड़क जोकि सूनी थी, कहीं इक्का-दुक्का सैलानी, खेत-मज़दूर या पास के गाँवों की ओर आते-जाते स्त्री-पुरुष दिखाई पड़ते। मैं किसी-न-किसी चीज़ की तरफ उसका ध्यान खींचती। यह शायद एक सभ्य तरीका था उसे और अपने-आपको अन्यत्र व्यस्त रखने का। रास्ते में नग्न निरावरण दो बँडा स्त्रियाँ हमारे पास से गुज़रीं तो उसके अभिजात्य को हल्का-सा धक्का लगा। उसने ढेर सारे सवाल किये-‘‘यहाँ कैसे आईं ? कपड़े क्यों नहीं पहने ? गज-भर कपड़ा भी नहीं इनके पास ?’’
मैंने रोका, गज-भर कपड़े की बात नहीं। यह आदिवासी बँडा स्त्रियाँ हैं, निर्वस्त्र ही घूमती हैं। इन्हें शाप मिला है।’’
‘‘शाप ! किसका ? कैसी बातें करती हो ?’’
वह कई बातों से अत्तेजित होने लगता था, जैसे मैंने गुज़री सदी की बात की हो, या निपट गँवारों की तरह सदियों पुराने तर्कहीन विश्वास आँख मूँदकर अपना लिए हों। मुझे उसे चिढ़ाने में मजा भी आता था
‘‘यह विश्वासों और किंवदंतियों का प्रदेश है सिद्धार्थ ! यहाँ के लोगों को जानना चाहो तो उनके विश्वासों को भी जानना होगा।’’
‘‘तो इन निर्वस्त्र घूमती स्त्रियों के सोंच के पीछे भी कोई विश्वास है, यही कहना चाहती हो न ?’’
मैंने कथा सुनाई थी, बँडा राज्य की राजधानी मुदलीपाड़ा में किंकू बोड़क नाले की-जिसमें, कहते हैं सीता वनवास के दौरान एक बार जब निर्वस्त्र नहा रही थीं तो उधर से गुज़रती एक बंडा लड़की उन पर हँस पड़ी। सीता ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि कलियुग में बंडा लड़कियाँ वस्त्रहीन होकर घूमेंगी। यौवन को ढँकना पाप समझा जाएगा। तभी से बँडा लड़कियाँ कपड़े नहीं पहनतीं। कमर में एक फुट चौड़ी केरंग, गले से कमर तक कई तहों का रंग-बिरंगा हार, सिर मुंडा हुआ, उस पर चौंड़े ताड़ की पट्टी ‘रेऊर’ और कानों में लिंबरी (झालदार रिंग) यही इनका पहरावा है।
‘‘ताज्जुब है ! दुनिया बदल गई पर हमारे यहाँ अभी भी आदिम सभ्यता और अंधविश्वासों में जीनेवाले लोग बहुतायत में मौजूद हैं, पिछड़े हुए असभ्य लोग।’’
वह भी मुझे चिढ़ाने-खिजाने से बाज़ नहीं आता।
‘‘पता नहीं, सभ्य है या असभ्य। हमारे नीति-नियम इन पर लागू नहीं होते। इनके अपने कानून हैं, अपनी आचारसंहिता। बंडा पुरुष अस्त्रों से लैस, ताड़ी में धुत्त अपनी सीमा में निःशंक घूमता है, शिकार करता है। खूँखार है ! स्त्री घर और बच्चों का दायित्व निभाती है। पर यहाँ एक अच्छी बात तो ज़रूर है।’’
‘‘कौन-सी ?’’ उसने लापरवाही से पूछा था, यानि कि यहाँ अच्छा क्या हो सकता है !
‘‘प्रेम करने में कोई रोक नहीं। और विवाह आपसी सहमति से तय होता है।’’
‘‘चलो, यहाँ ये लोग हमसे बाजी मार ले गए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूगा। तुम्हारे यहाँ विश्वासों-किंवदंतियों में शापों की मात्रा बहुत ज्यादा है। वह गाइड छोकरा कह रहा था कि कृष्ण ने भी अपने बेटे शांब को शाप दिया था। आश्चर्य होता है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना।’’
‘‘तुम भूलते हो। शाप भी है पर शाप-मुक्ति के उपाय भी हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि तुम यहाँ ऐसा भी कुछ सुनोगे जो पहले कभी नहीं सुना। कृष्ण ने अपने बेटे शांब को शाप दिया, इसके पीछे नारद का छल था। शांब ने नारद का अपमान किया था। वह बदला लेना चाहता था। तभी उसने रैवतक पर्वत पर बाप-बेटे दोनों को मौका देखकर बुलाया। उस वक्त गोपियाँ पुष्करिणी में नहा रही थीं। शांब को देखकर उन्हें कृष्ण का भ्रम हुआ, जो सूरत में उनसे काफी मिलते थे। गोपियाँ शांब से लिपट गईं और कृष्ण ने आकर देख लिया। तभी कृष्ण ने गुस्सा होकर शांब को शाप दिया, ‘तुझे कुष्ठ हो जाय।’ लेकिन बाद में नारद ने ही शांब को शाप-मुक्ति का रास्ता बताया।
‘‘ ‘भारत के पूर्वी तट पर मैत्रेय वन में चंद्रभागा के किनारे सूर्य की उपासना करो, तुम रोगमुक्त हो जाओगे।’ शांब ने ऐसा ही किया और शाप टल गया। कहते हैं यही चंद्रभागा में स्नान करते शांब को सूर्य की प्रतिमा मिली थी। उसकी स्थापना की गई और सूर्य मंदिर बन गया। तो एक तरह से तुम इस वक़्त शाप-मुक्ति की जगह पर खड़े हो।’’
‘‘कोणार्क मठ की बात कर रही हो ?’’
‘‘हाँ, चार हज़ार वर्ष पुराने शांब के इस साधना पीठ का ही नाम कोणार्क मठ है। यही तब मैत्रेय वन कहलाता था और आज जो ज़रा-सी पुष्करिणी रह गई है, कभी गुमान से भरी नदी चंद्रभागा हुआ करती थी। यहीं शांब शाप-मुक्त हुए थे।’’
बातों-बातों में ही टूरिस्ट बँगला आ गया था। वक़्त कैसे कटा, मालूम ही न हुआ। हम चाय नाश्ते के लिए होटल पर रुके। हाथ मुँह धोकर ताज़ा हुए। शाम होने लगी थी।-‘‘अब चलना चाहिए, देर हो जाएगी।’’ मैं फिर धरती पर आ गई थी।
‘‘हाँ चलेंगे, पर पहले मेरी बात का जवाब ?’’
कौन-सी बात ?’’
‘‘वही जो कोणार्क के समुद्र-तट पर पूछी थी। इतनी जल्दी भूल गईं ?’’
मैंने आहत होकर उसे देखा, ‘क्यों पूछ-पूछकर कौंच रहे हो। तुम ज़रा-सा छूते हो तो मेरा जिस्म, मेरे रक्त का प्रवाह हज़ार ज़बानों में बोलने लगता है। तुम क्या देह की यह भाषा नहीं समझते ?’ कहना चाहती थी पर होंठ खुलें तभी तो कुछ कह पाती। अपने बारे में खुलकर कहना मुमकिन नहीं हो पा रहा था।
‘‘कुनी ! तुमने मुझे अभी तक शाप-मुक्ति की कथा सुनाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी यहाँ शाप-मुक्त हो जाओ ? शांब का यह मुक्ति-स्थल तुम्हारी मुक्ति की जगह नहीं हो सकती ?’’
मैं देखती रही बिना बोले। पूछा नहीं, ‘किस शाप-मुक्ति की बात कर रहे हो ? मैं तो बत्तीस बरसों से कई शाप-शेरों से बिंधी जी रही हूँ। रक्षणशील परिवार में जन्म लेने का शाप, घर की बड़ी बेटी होने का शाप, या शायद अपने यहाँ महज़ उम्रदराज़ लड़की होने का शाप ही काफ़ी है अंधी खोहों में बंद होने के लिए।’’
उसने कंधों से घेरकर मुझे अपने पास बिठाया, मन की यह कुंठाएँ, यह गाँठें, जो तुम्हें सहज नहीं होने देतीं, यह क्या किसी शाप से कम हैं ? या तुम सोच रही हो कि अपने भीतर की आवाज़ दबाकर तुम कोई महान त्याग कर रही हो ? कब से देख रहा हूँ, मेरे करीब होकर भी तुम मुझसे कितनी दूर हो। तुम एक स्त्री हो, पर मुझे लगता है मैं किसी बेजान चीज़ के साथ बतिया रहा हूँ। बल्कि सच कहूँ तो डर-सा लगता है, इस तरह तुम्हारा रवैया ठंडा और निर्जीव रहा तो मैं भी एक दिन पत्थर हो जाऊँगा। ना, भई, मेरे अन्दर थोड़ी ऊष्मा रहने दो।’’
‘‘सिद्धार्थ ! तुम नहीं समझोगे।’’
मैं उसके तमाम सवालों के जवाब में, उसे अपना सोच समझाना चाहती थी, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने दिया था, या जिसकी दिशा मेरी शिक्षा ने तय कर दी थी। वह सोच एक दिन या माह में बदलनेवाला कैसे हो सकता था ? पर मैं जानती थी कि वह मेरी गंभीरता से की बात को भी हँसकर उड़ा देगा क्योंकि मेरी सोच, मेरी परवरिश, मेरा माहौल, सबकुछ तो उससे अलग था।
‘‘मैं नहीं समझूँगा तो समझाओ मत। मगर कुनी, ज़रा खुले दिल और दिमाग से सोचो, फूलों को खिलने से और धरती से हरी दूब के फूटने को कोई रोक सका है ? कोई रोक सका है सागर के सीने में घुमड़ते ज्वारभाटों को ? बोलो कुनी, मेरी तरफ़ देखकर बोलो। मैं तुम्हारे सच को पहचान लूँगा...’’
मेरे भीतर लहरों का उन्माद सिर पटकने लगा था। सिद्धार्थ की साँसें मुझे छू रही थीं। एक अवश आँच मेरी देह झुलसाने लगी थी। मैं झूठ नहीं बोल पाई। इतना पास होकर झूठ बोला भी कैसे जा सकता था ? जब भीतर कोणार्क के प्रेमी युगल अँगड़ाई लेकर जागने लगे हों और ज़ेहन में क्रीड़ाएँ करने लगे हों तो चुप्पी भी बातूनी हो जाती है। सिद्धार्थ ने मुझे थाम लिया और मैं तूफ़ानी लहरों पर बहती रही। मैंने खुद को रोका नहीं या शायद रोकना मुमकिन ही नहीं था। ऐसी तेज झालदार लहर थी वह कि बहने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। एक-दूसरे को डूबने से बचाते, हम दोनों साथ-साथ बहने लगे, एक-दूसरे को जकड़े हुए।
डरी हुई चंद्रभागा सागर में कूद पड़ी और सूर्य उसके पीछे-पीछे सागर तल तक उसे ढूढ़ता रहा। हहराते सागर ने दोनों को अपनी विशाल छाती में अँकोर लिया...
घर लौटते वक़्त हम शांत थे, अपने भीतर की दुनिया में कुछ देर के लिए बंद। सिद्धार्थ भी चुप था। हवा के तेज़ झोंके चेहरों पर झेलते हम एक यादगार दिन को सहेजे अपने-अपने कठघरों में लौट रहे थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि सच दो तरह के होते हैं, भीतर और बाहर के रंगों-द्वंद्वों से सराबोर। दोनों अलग पर दोनों कहीं एक-दूसरे से गुँथे भी, क्योंकि दोनों हमारे होने को प्रमाणित करते हैं। सुख भी शायद दो तरह के हैं, एक नशे से बहकानेवाला बड़बोला, दूसरा अंदर तक ख़ामोश करनेवाला बेजुबान !
सिद्धार्थ ने मुझसे कुछ भी न छिपाया। तीस साल का युवा साफ़-सुथरी ज़िंदगी जीने का कायल, पर अनुभवहीन नहीं था। वह मान गया कि मैंने उसे आश्चर्य और उलझन में डाल दिया था। परिवार नियोजन के इस युग में, जहाँ टी.वी. के माध्यम से बच्चे भी माला, मस्ती, निरोध और लाल तिकोन के अर्थ जान गए हैं, मेरे बत्तीस-तैंतीस सालों के कौमार्य को उसने किस सोच से स्वीकार किया, मालूम नहीं। अविश्वास या कहीं कुछ ग़लत होने की आशंका के साथ ? इतनी बुरी तो मैं नहीं लगती कि कोई प्रशंसक की नज़र मुझ पर ठहरी न हो। सिद्धार्थ ने जो भी सोचा हो, कहा कुछ नहीं। कहता भी तो क्या मेरे बीते को सही ढंग से समझने का दावा कर पाता ? मैं, जो दूसरों के लिए जन्मी, घर-परिवार की सहूलियतों, ज़रूरतों की टोह लेती जी और खुद को बज़िद भूलती रही, इस बीच अच्छी लड़की का खिताब पाने के साथ, मेरे भीतर कितना कुछ रीत गया और विराग का मुखौटा मेरे समूचे वजूद पर चस्पाँ हो गया, यह तो मैं भी देर से जान पाई।
पर उस वक़्त अपने भीतर के अंधड़ों से घिरी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर हैरत-भरी नज़रों से मुझे देखने के बाद, उसने बड़ी कोमलता से मुझे छाती से लगाया-‘‘कुनी, तुम बहुत भोली हो, बहुत सीधी। आई रियली लव यू।’’ बस, और कोई प्रश्न नहीं !
अपने यौवन के पहले अंतरंग अनुभव को इस अप्रत्याशित ढंग से पाना और सहज होकर स्वीकारना मेरे लिए आसान नहीं था।
मैंने रोका, गज-भर कपड़े की बात नहीं। यह आदिवासी बँडा स्त्रियाँ हैं, निर्वस्त्र ही घूमती हैं। इन्हें शाप मिला है।’’
‘‘शाप ! किसका ? कैसी बातें करती हो ?’’
वह कई बातों से अत्तेजित होने लगता था, जैसे मैंने गुज़री सदी की बात की हो, या निपट गँवारों की तरह सदियों पुराने तर्कहीन विश्वास आँख मूँदकर अपना लिए हों। मुझे उसे चिढ़ाने में मजा भी आता था
‘‘यह विश्वासों और किंवदंतियों का प्रदेश है सिद्धार्थ ! यहाँ के लोगों को जानना चाहो तो उनके विश्वासों को भी जानना होगा।’’
‘‘तो इन निर्वस्त्र घूमती स्त्रियों के सोंच के पीछे भी कोई विश्वास है, यही कहना चाहती हो न ?’’
मैंने कथा सुनाई थी, बँडा राज्य की राजधानी मुदलीपाड़ा में किंकू बोड़क नाले की-जिसमें, कहते हैं सीता वनवास के दौरान एक बार जब निर्वस्त्र नहा रही थीं तो उधर से गुज़रती एक बंडा लड़की उन पर हँस पड़ी। सीता ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि कलियुग में बंडा लड़कियाँ वस्त्रहीन होकर घूमेंगी। यौवन को ढँकना पाप समझा जाएगा। तभी से बँडा लड़कियाँ कपड़े नहीं पहनतीं। कमर में एक फुट चौड़ी केरंग, गले से कमर तक कई तहों का रंग-बिरंगा हार, सिर मुंडा हुआ, उस पर चौंड़े ताड़ की पट्टी ‘रेऊर’ और कानों में लिंबरी (झालदार रिंग) यही इनका पहरावा है।
‘‘ताज्जुब है ! दुनिया बदल गई पर हमारे यहाँ अभी भी आदिम सभ्यता और अंधविश्वासों में जीनेवाले लोग बहुतायत में मौजूद हैं, पिछड़े हुए असभ्य लोग।’’
वह भी मुझे चिढ़ाने-खिजाने से बाज़ नहीं आता।
‘‘पता नहीं, सभ्य है या असभ्य। हमारे नीति-नियम इन पर लागू नहीं होते। इनके अपने कानून हैं, अपनी आचारसंहिता। बंडा पुरुष अस्त्रों से लैस, ताड़ी में धुत्त अपनी सीमा में निःशंक घूमता है, शिकार करता है। खूँखार है ! स्त्री घर और बच्चों का दायित्व निभाती है। पर यहाँ एक अच्छी बात तो ज़रूर है।’’
‘‘कौन-सी ?’’ उसने लापरवाही से पूछा था, यानि कि यहाँ अच्छा क्या हो सकता है !
‘‘प्रेम करने में कोई रोक नहीं। और विवाह आपसी सहमति से तय होता है।’’
‘‘चलो, यहाँ ये लोग हमसे बाजी मार ले गए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूगा। तुम्हारे यहाँ विश्वासों-किंवदंतियों में शापों की मात्रा बहुत ज्यादा है। वह गाइड छोकरा कह रहा था कि कृष्ण ने भी अपने बेटे शांब को शाप दिया था। आश्चर्य होता है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना।’’
‘‘तुम भूलते हो। शाप भी है पर शाप-मुक्ति के उपाय भी हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि तुम यहाँ ऐसा भी कुछ सुनोगे जो पहले कभी नहीं सुना। कृष्ण ने अपने बेटे शांब को शाप दिया, इसके पीछे नारद का छल था। शांब ने नारद का अपमान किया था। वह बदला लेना चाहता था। तभी उसने रैवतक पर्वत पर बाप-बेटे दोनों को मौका देखकर बुलाया। उस वक्त गोपियाँ पुष्करिणी में नहा रही थीं। शांब को देखकर उन्हें कृष्ण का भ्रम हुआ, जो सूरत में उनसे काफी मिलते थे। गोपियाँ शांब से लिपट गईं और कृष्ण ने आकर देख लिया। तभी कृष्ण ने गुस्सा होकर शांब को शाप दिया, ‘तुझे कुष्ठ हो जाय।’ लेकिन बाद में नारद ने ही शांब को शाप-मुक्ति का रास्ता बताया।
‘‘ ‘भारत के पूर्वी तट पर मैत्रेय वन में चंद्रभागा के किनारे सूर्य की उपासना करो, तुम रोगमुक्त हो जाओगे।’ शांब ने ऐसा ही किया और शाप टल गया। कहते हैं यही चंद्रभागा में स्नान करते शांब को सूर्य की प्रतिमा मिली थी। उसकी स्थापना की गई और सूर्य मंदिर बन गया। तो एक तरह से तुम इस वक़्त शाप-मुक्ति की जगह पर खड़े हो।’’
‘‘कोणार्क मठ की बात कर रही हो ?’’
‘‘हाँ, चार हज़ार वर्ष पुराने शांब के इस साधना पीठ का ही नाम कोणार्क मठ है। यही तब मैत्रेय वन कहलाता था और आज जो ज़रा-सी पुष्करिणी रह गई है, कभी गुमान से भरी नदी चंद्रभागा हुआ करती थी। यहीं शांब शाप-मुक्त हुए थे।’’
बातों-बातों में ही टूरिस्ट बँगला आ गया था। वक़्त कैसे कटा, मालूम ही न हुआ। हम चाय नाश्ते के लिए होटल पर रुके। हाथ मुँह धोकर ताज़ा हुए। शाम होने लगी थी।-‘‘अब चलना चाहिए, देर हो जाएगी।’’ मैं फिर धरती पर आ गई थी।
‘‘हाँ चलेंगे, पर पहले मेरी बात का जवाब ?’’
कौन-सी बात ?’’
‘‘वही जो कोणार्क के समुद्र-तट पर पूछी थी। इतनी जल्दी भूल गईं ?’’
मैंने आहत होकर उसे देखा, ‘क्यों पूछ-पूछकर कौंच रहे हो। तुम ज़रा-सा छूते हो तो मेरा जिस्म, मेरे रक्त का प्रवाह हज़ार ज़बानों में बोलने लगता है। तुम क्या देह की यह भाषा नहीं समझते ?’ कहना चाहती थी पर होंठ खुलें तभी तो कुछ कह पाती। अपने बारे में खुलकर कहना मुमकिन नहीं हो पा रहा था।
‘‘कुनी ! तुमने मुझे अभी तक शाप-मुक्ति की कथा सुनाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी यहाँ शाप-मुक्त हो जाओ ? शांब का यह मुक्ति-स्थल तुम्हारी मुक्ति की जगह नहीं हो सकती ?’’
मैं देखती रही बिना बोले। पूछा नहीं, ‘किस शाप-मुक्ति की बात कर रहे हो ? मैं तो बत्तीस बरसों से कई शाप-शेरों से बिंधी जी रही हूँ। रक्षणशील परिवार में जन्म लेने का शाप, घर की बड़ी बेटी होने का शाप, या शायद अपने यहाँ महज़ उम्रदराज़ लड़की होने का शाप ही काफ़ी है अंधी खोहों में बंद होने के लिए।’’
उसने कंधों से घेरकर मुझे अपने पास बिठाया, मन की यह कुंठाएँ, यह गाँठें, जो तुम्हें सहज नहीं होने देतीं, यह क्या किसी शाप से कम हैं ? या तुम सोच रही हो कि अपने भीतर की आवाज़ दबाकर तुम कोई महान त्याग कर रही हो ? कब से देख रहा हूँ, मेरे करीब होकर भी तुम मुझसे कितनी दूर हो। तुम एक स्त्री हो, पर मुझे लगता है मैं किसी बेजान चीज़ के साथ बतिया रहा हूँ। बल्कि सच कहूँ तो डर-सा लगता है, इस तरह तुम्हारा रवैया ठंडा और निर्जीव रहा तो मैं भी एक दिन पत्थर हो जाऊँगा। ना, भई, मेरे अन्दर थोड़ी ऊष्मा रहने दो।’’
‘‘सिद्धार्थ ! तुम नहीं समझोगे।’’
मैं उसके तमाम सवालों के जवाब में, उसे अपना सोच समझाना चाहती थी, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने दिया था, या जिसकी दिशा मेरी शिक्षा ने तय कर दी थी। वह सोच एक दिन या माह में बदलनेवाला कैसे हो सकता था ? पर मैं जानती थी कि वह मेरी गंभीरता से की बात को भी हँसकर उड़ा देगा क्योंकि मेरी सोच, मेरी परवरिश, मेरा माहौल, सबकुछ तो उससे अलग था।
‘‘मैं नहीं समझूँगा तो समझाओ मत। मगर कुनी, ज़रा खुले दिल और दिमाग से सोचो, फूलों को खिलने से और धरती से हरी दूब के फूटने को कोई रोक सका है ? कोई रोक सका है सागर के सीने में घुमड़ते ज्वारभाटों को ? बोलो कुनी, मेरी तरफ़ देखकर बोलो। मैं तुम्हारे सच को पहचान लूँगा...’’
मेरे भीतर लहरों का उन्माद सिर पटकने लगा था। सिद्धार्थ की साँसें मुझे छू रही थीं। एक अवश आँच मेरी देह झुलसाने लगी थी। मैं झूठ नहीं बोल पाई। इतना पास होकर झूठ बोला भी कैसे जा सकता था ? जब भीतर कोणार्क के प्रेमी युगल अँगड़ाई लेकर जागने लगे हों और ज़ेहन में क्रीड़ाएँ करने लगे हों तो चुप्पी भी बातूनी हो जाती है। सिद्धार्थ ने मुझे थाम लिया और मैं तूफ़ानी लहरों पर बहती रही। मैंने खुद को रोका नहीं या शायद रोकना मुमकिन ही नहीं था। ऐसी तेज झालदार लहर थी वह कि बहने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। एक-दूसरे को डूबने से बचाते, हम दोनों साथ-साथ बहने लगे, एक-दूसरे को जकड़े हुए।
डरी हुई चंद्रभागा सागर में कूद पड़ी और सूर्य उसके पीछे-पीछे सागर तल तक उसे ढूढ़ता रहा। हहराते सागर ने दोनों को अपनी विशाल छाती में अँकोर लिया...
घर लौटते वक़्त हम शांत थे, अपने भीतर की दुनिया में कुछ देर के लिए बंद। सिद्धार्थ भी चुप था। हवा के तेज़ झोंके चेहरों पर झेलते हम एक यादगार दिन को सहेजे अपने-अपने कठघरों में लौट रहे थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि सच दो तरह के होते हैं, भीतर और बाहर के रंगों-द्वंद्वों से सराबोर। दोनों अलग पर दोनों कहीं एक-दूसरे से गुँथे भी, क्योंकि दोनों हमारे होने को प्रमाणित करते हैं। सुख भी शायद दो तरह के हैं, एक नशे से बहकानेवाला बड़बोला, दूसरा अंदर तक ख़ामोश करनेवाला बेजुबान !
सिद्धार्थ ने मुझसे कुछ भी न छिपाया। तीस साल का युवा साफ़-सुथरी ज़िंदगी जीने का कायल, पर अनुभवहीन नहीं था। वह मान गया कि मैंने उसे आश्चर्य और उलझन में डाल दिया था। परिवार नियोजन के इस युग में, जहाँ टी.वी. के माध्यम से बच्चे भी माला, मस्ती, निरोध और लाल तिकोन के अर्थ जान गए हैं, मेरे बत्तीस-तैंतीस सालों के कौमार्य को उसने किस सोच से स्वीकार किया, मालूम नहीं। अविश्वास या कहीं कुछ ग़लत होने की आशंका के साथ ? इतनी बुरी तो मैं नहीं लगती कि कोई प्रशंसक की नज़र मुझ पर ठहरी न हो। सिद्धार्थ ने जो भी सोचा हो, कहा कुछ नहीं। कहता भी तो क्या मेरे बीते को सही ढंग से समझने का दावा कर पाता ? मैं, जो दूसरों के लिए जन्मी, घर-परिवार की सहूलियतों, ज़रूरतों की टोह लेती जी और खुद को बज़िद भूलती रही, इस बीच अच्छी लड़की का खिताब पाने के साथ, मेरे भीतर कितना कुछ रीत गया और विराग का मुखौटा मेरे समूचे वजूद पर चस्पाँ हो गया, यह तो मैं भी देर से जान पाई।
पर उस वक़्त अपने भीतर के अंधड़ों से घिरी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर हैरत-भरी नज़रों से मुझे देखने के बाद, उसने बड़ी कोमलता से मुझे छाती से लगाया-‘‘कुनी, तुम बहुत भोली हो, बहुत सीधी। आई रियली लव यू।’’ बस, और कोई प्रश्न नहीं !
अपने यौवन के पहले अंतरंग अनुभव को इस अप्रत्याशित ढंग से पाना और सहज होकर स्वीकारना मेरे लिए आसान नहीं था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book