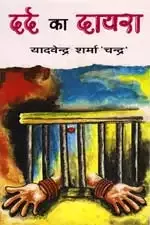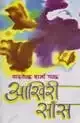|
नारी विमर्श >> दर्द का दायरा दर्द का दायरायादवेन्द्र शर्मा
|
24 पाठक हैं |
||||||
एक रोचक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी व राजस्थानी के विशिष्ट लेखक यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र का यह
उपन्यास दर्द की विभिन्न स्थितियों को व्यक्त करता हुआ जीवन के अनेक
मोड़ों से गुज़रता है। साहित्य एकादमी, मीरा व फणीश्वरनाथ रेणु आदि अनेक
पुरस्कारों से सम्मानित चन्द्र ने इस कृति में स्त्री के विभिन्न रुपों का
वर्णन करके उनकी गुह्य परतों को उकेरा है। उपन्यास द्वन्द्व, संघर्ष और
अपनत्व के माध्यम से दर्द की परतें खोलता है। बहुत रोचक है उपन्यास और
सार्थक भी और इसमें हम सबकी सच्चाइयाँ हैं !
प्रकाशक
एक
मालती ने चुटकी ली, ‘‘सीता दीदी, आज तुम उदास क्यों
हो ? आज तो तुम्हारे चेहरे पर हँसी होनी चाहिए।’’
सीता निरुत्तर रही।
देखो सीता दीदी, यह असमय की उदासी मुझे उच्छी नहीं लगती। पति के आगमन पर अपार प्रसन्नता देखना चाहती हूँ।’’ मालती सहसा गंभीर हो गई। उसके स्वर में दर्द सा तैर उठा, शुभ बेला है न, अनागत मंगल की सूचक इन घड़ियों में तुम्हारी आँखों में व्यथा कैसी ? हर प्रतीक्षारत युवती विकल रहती है-अपने प्रीतम के लिए। उसकी पलक-पंखुड़ियाँ प्रीतम के पथ में बिछ जाती हैं और आत्मा की सहस्र ध्वनियाँ समवेत स्वर में कहती हैं-तुम मेरी आत्मा और भाव लोक के स्वामी हो, मेरे हृदय-पट अवरुद्ध नहीं है। उसकी समस्त अभिलाषाएँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए आतुर हैं। अब तुम देर न करो।’... हाँ दीदी, तुम भी अपने अन्तर पट के सारे द्वार खोल दो। अधरों पर मुस्कान ले आओ ताकि आने वाला प्रीतम तुम्हारे पावन-मुख के दर्शन मात्र से धन्य-धन्य हो उठे !’’ मालती के नयन भर आए। अन्तर्मन में सुसुप्त व्यथाएँ एक साथ जाग पड़ी हों, ऐसा उसके नयनों में उमड़े सावन भादों से लगा।
सीता सावधान हो गई। मालती के अश्रुपूरित मुख को देखकर वह विकल हो उठी। होंठों पर सूखी मुस्कान लाकर वह बोली, ‘‘तुम मुस्कराओ मालती, मेरे होंठों पर मुस्कान स्वयं नाच उठेगी।’’
‘‘भाग्यहीनों के जीवन में मुस्कान अपराध है।’
‘‘नहीं मालती, अपने आप पर इतनी निष्ठुर मत बनो। वैसे तुम्हारी तरह इस समाज की युवती की मांग का सिन्दूर न पोंछा गया हो पर दुर्भाग्य उसका तुमसे कम नहीं है। यहाँ होंठों की मुस्कानें भी अभिनय से सम्बन्ध रखती हैं।’’
‘‘क्यों दीदी ?’’
‘‘मालती, कुछ प्रारब्ध को अमिट मानकर सन्तोष कर लेते हैं। कुछ प्रारब्ध को कुछ नहीं समझते, तब उसे बहुत पीड़ाएँ उठानी पड़ती है।..मैं प्रारब्ध और विधि को नहीं मानती। ईश्वर की आस्था और उसके अस्तित्व में भी मुझे अधिक विश्वास नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा जीवनाधार कौन हो सकता है !’’
‘‘प्रभु ने तुम्हें पति दिया है।’’ मालती ने न चाहते हुए यह कहा।
‘‘हर पति हर पत्नी का आधार नहीं बन सकता।’’
‘‘तुम्हारे पास धन है।’’
‘‘धन आन्तरिक आनन्द का सृष्टा नहीं।’’
‘‘तुम्हें तुम्हारा पति अन्तरतम से चाहता है।’’ मालती सहम गयी।
‘‘वस्तुस्थिति इसके नितान्त विपरीत है।’’
मालती के मन में बादलों का घोर गर्जन सा हुआ। वह हतप्रभ सीता को देखती रही। स्थिर दृष्टि में अनेक प्रश्न ज्वलित हो उठे। कुछ क्षण अपने को सँभालने में उसे लग गए। अप्रिय और अवांछित बात सीता के मुँह से स्पष्ट एवं गम्भीर स्वर में सुनकर वह जड़ सी हो गई।
‘‘मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। मालती, वैधव्य की आग में सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली कवयित्री मालती से, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। वर्षोपरान्त मेरा स्वामी आ रहा है लगभग छ: वर्ष बाद; अर्धयुग बीत गया है। किन्तु मैं अपने स्वामी से प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वह किंचित भी प्रिय नहीं है।’’
‘‘दीदी ?’’
‘‘कुतूहल और दुख में डूब गई हो ? कठोर सत्य सुनने के लिए पत्थर का हृदय भी होना चाहिए। तुम्हारे जैसी कोमल मन वाली मेरी तीखी बातें नहीं सुन पाएगी। मैं मिथ्या-भाषण की आदी नहीं हूँ। झूठ बोलकर मैं अपने आपको अपराधी नहीं बना सकती। सब कहूँगी साफ-साफ।’’
‘‘किन्तु ऐसा सत्य निन्दनीय होता है। वह मनुष्य को श्रेष्ठ दृष्टि से गिरा देता है। मालती ने सँभलकर कहा।
अपने कंठ-स्वर में स्वाभाविक मृदुता लाती हुई सीता धीरे से बोली, ‘‘मेरे विचार तुमसे सर्वथा भिन्न है। तुम मीरा की तरह कन्हैया को अपना सर्वस्व मानकर अपनी वासना को, अपने अन्तस के उद्दाम को, अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को आध्यात्मिक बाना पहना सकती हो। तुम बावरी मीरा बनकर अपने भौतिक सुखों को त्याग सकती हो। तुम अपनी कविता में वियोग की ज्वाला को शब्दों का रूप देकर तीव्र स्वर में कह सकती हो-मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मैं जीवन भर प्रतीक्षा करूँगी-लेकिन मैं इसे एक पलायन मानती हूँ। खैर, उन्हें आने दो। घर खुला है। नौकर स्वागत-सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।’’
मालती तनिक उन्मन्न सी हो उठी।
धीरे-धीरे सन्ध्या का आगमन होने लगा। प्रतीची के प्राँगण में अरुणिमा का सरोवर फैल गया। मालती अपने घर की छत पर जाकर उसे अनिभेष दृष्टि से देखने लगी।
‘‘सीता दीदी, इतना कठोर वचन क्यों कहती हैं। वह ऐसा सत्य क्यों बोलती हैं जो सबको अप्रिय और पीड़क लगे। पति से घृणा करती है पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका वह उद्घोष भी करें। ऐसा करना सर्वथा अनुचित एवं विवेक-शून्य है।’’ वह मन ही मन उन्मन्न सी हो उठी, तभी उसकी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं है।’’
दो राजस्थानी परिवार।
घर भी आमने-सामने। सभ्यता के प्रतीक। रंग-पुते। वैश्य जाति के। बीच की गली यही तीन-चार फीट की।
एक की स्वामिनी है-सीता। सास के देहान्त के उपरान्त अपने घर की एक तरह की मालकिन। उम्र तीस वर्ष। न ननद और न कोई और। अकेली, नितान्त अकेली। पैसे वाली।
दूसरी है-मालती। पूर्ण यौवन। विधवा। भावुक। कविता करती है। हर घड़ी, हर पहर, रात-दिन अपने भाव-लोक में विस्मृत रहती है। सास की सेवा करती है, ससुर के पाँव दबाती है बड़े देवर गिरधर को कॉलेज के लिए तैयार करती है, छोटे-छोटे चार देवरों और एक ननद को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, लिखाती-पढ़ाती है। उम्र है सोलह वर्ष। देवर से एक वर्ष छोटी।
वह पड़ौसिन है इसलिए सीता को प्राय: दीदी और कभी-कभी भाभी कहती है। सीता के पति को भैया कहकर सम्बोधित करेगी। ऐसा वह सोचती है, निश्चय कर चुकी है। इस बार वह उससे प्रत्यक्ष परिचय करेगी सीता के प्रति उसकी अच्छी दृष्टि नहीं है। अत: कभी-कभी उनमें काफी तनाव व कटुता भी आ जाती है।
सूरज क्षितिज का अन्तिम चुम्बन लेकर अस्त हो गया। अँधेरे का उमड़ता हुआ सैलाब संसार पर छाने लगा। मालती अब भी विचार-विमूढ़ खड़ी थी।
अचानक सीता की दृष्टि उस पर पड़ी। वह स्नान करके धोती सुखाने ऊपर आई थी। मालती को विचारों में खोई जानकर वह तुरन्त बोली, ‘‘क्या कोई नई कविता लिखने की सोच रही हो ? सुनो मालती, यह अन्धकार है न, थोड़ी देर में हम सबको अपने में समेट लेगा। क्यों न एक कविता इस अन्धकार पर लिख दो।’’
मालती का मन विपुल विषाद से भर आया। आँखें सजल हो उठीं। विगलित-स्वर में बोली, ‘‘क्यों सताती हो दीदी, बार-बार कविता-कविता कहोगी तो मैं कविता क्या, तुमसे बातचीत करना भी बन्द कर दूंगी।’’
‘‘ऐसा नहीं हो सकता है। यह सम्भव नहीं है। तुम हजार बार मुझसे लड़ चुकी हो फिर दोस्ती कर लेती हो।’’ सीता के स्वर में दृढ़ता थी।
‘‘मैं कहती हूँ मुझे अपरिसीम वेदना मत दो। मुझे आवश्यकता से अधिक तंग न करो। मीरा की उपमा से मुझे दु:ख न पहुँचाओ।’’...‘तुम वैधव्य की वेदना को क्या समझो ? जीवन में सदा तुमने कुकृत्य किए हैं। तुम्हारा चरित्र बुराइयों का दर्पण है। तुम पतन की चरम सीमा को देख चुकी हो। फिर भी तुम दर्प से सिर ऊंचा करके समाज में चलती हो। तुम उन्हीं प्राणियों में गिनी जाती हो जो अपमान को मान और घृणा को प्यार ही समझते हैं। उसके भेद-विभेद को नहीं समझते।’’ मालती का सारा शरीर आवेश में काँपने लगा।
सीता मुस्कराती रही। उसकी आँखों में सहज तारल्य था। स्वाभाविक दीप्ति थी।
‘‘तुम इतना सुनकर भी मुस्कराती हो। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर तुम्हारा सिर नीचा नहीं होता। कैसी हो तुम ?’’ मालती चिढ़ गयी।
‘‘मैं तुम सभी से अच्छी हूँ। मैंने पाप किए हैं पर प्रच्छन्न नहीं। उन पापों के द्वारा मैंने किसी के हृदय को आघात नहीं पहुँचाया। मालती ! मैं इतना जानती हूँ-मेरा अपराध महापाप होकर भी अभिशाप नहीं हो सका, किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें। एक पल के लिए भी सुख नहीं दे सकता। तुम प्यासे पपीहे की तरह स्वाति बूँद की प्रतीक्षा करती रहती हो और मेरे मुँह में स्वाति बूँदें स्वत: आ आकर गिरती हैं, क्योंकि मेरा पाप सृष्टि की दृष्टि में है, यथार्थ के मूल में नहीं।’’
लेकिन समाज में तुम्हारा क्या स्थान है ?’’
‘‘मैं समाज, परिवार और पति की कोई चिंता नहीं करती। मैं सबकी छाती पर मूँग दलना जानती हूँ। मुझ में अदम्य साहस है। मैं किसी की परवाह नहीं करती।’’
‘‘थोड़ा और इन्तजार करो जब उम्र आदमी की कमर तोड़ देती है तब आदमी को यौवन में की गयी उच्छृंखलताओं का पश्चाताप करना पड़ता है। तब भूलें-दानवी पंजों की तरह उसके अंग-अंग को नोचती हैं।’’
‘‘मैं इतनी दुर्बल नहीं हूँ, मालती !’’ उसने सहजता से कहा, ‘तुम समाज के प्रहार से पलायन कर सकती हो, आत्महत्या कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकती। मैं इस घोर एकान्त में सुख की उपलब्धियों को एकत्रित करना जानती हूँ तुम्हारे समाज और परिवार के अतिरिक्त भी दुनिया बहुत बड़ी है।’’
मालती की सास ने पुकार लिया था, इसलिए वह चली गयी।
अँधेरा और एकान्त।
सीता विचलित सी खड़ी रही। उसका मन अवश हो उठा। वह नीचे आकर अपने अन्धकारपूर्ण कमरे में पड़ गयी। उसका मन भारी हो गया। आज मालती ने दैवात् उसके बारे में जो कहा, वह कटोक्ति की तरह उसे बेध गया। किंतु वह भी बहुत दु:खी है। भावुक है औचित्य और अनौचित्य का ख्याल ही नहीं रखती। फिर जैसे वह संभली। उसे उस पर इतना व्यंग्य नहीं करना चाहिए था।
कल सवेरे ही वह उससे क्षमा माँग लेगी। उसे फिर राजी कर लेगी। उसे अपनी बना लेगी। ऐसा सीता ने सोचा।
वह उठी। रोशनी की
भोजन आदि से निवृत्त होकर वह अपने पाले हुए चार तोतों को मिर्चे खिलाने लगी। तोते पिजरों से निकल-निकलकर उसके हाथों और कन्धों पर बैठ गए। तभी उसका कोचवान दूला आ गया। वह उसका ताँगा चलाता था। दिन भर की मजदूरी अपनी सेठानी के हाथ में रखकर उसने छुट्टी मांगी।
‘सुनों दूला !’’
दुला एक सिपाही की मुद्रा में तनकर खड़ा हो गया।
‘‘मूलिया और चम्पिया अभी तक नहीं आए ?’’
‘‘वे आते ही होंगे, सेठानी जी, वे ताँगों की अन्तिम खेप करने गए हैं। घंटे आधा घंटे में लौट आएँगे।’’
सीता गंभीर हो गयी। थोड़े रोष-मिश्रित स्वर में वह बोली, ‘‘हजार बार उन्हें आगाह कर दिया है कि ठीक आठ बजे घोड़ों को खोल दिया करो। आखिर उन निरीह जानवरों में भी प्राण होते हैं। वे भी थकते और टूटते हैं। पर इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे खुद हैं वैसे ही सबका प्रयोग करते हैं। छि:, जाओ और कल सुबह उन्हें इसके लिए आगाह कर देना।’’
दूला चला गया।
सीता फिर नीरव एकान्त में अपने आप में तन्मय सी हो गयी। मालती के साथ हुआ अरुचिकर और अप्रिय वाद-विवाद उसे फिर याद आने लगा। वह याद करती-करती विहँस पड़ी। अपने आप से कह उठी-यहाँ प्राणी बद्ध-मूल संस्कारों से आक्रान्त है। उसके विरुद्ध में उठाए गए किसी भी कदम को वह हेय दृष्टि से देखता है। पाप-पुण्य धर्म-अधर्म नैतिक अनैतिक के मिथ्यादर्श के चक्कर में वह जीवन की सहज प्रक्रियाओं को विस्मृत करके समाज की मान्यताओं के निर्देशन में चलता है। आत्म-पीड़न वंचना, हनन सहकर भी वह उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है जो वस्तुत: निगूढ़ सत्य है।
तभी उसकी पाली हुई तोती बोल उठी, ‘‘माँ-माँ, मुझे प्यार करो।’’
सीता ने अपने परिवार की उस अभिन्न सदस्या तोती को अपने हाथ की उँगुलियों पर बिठा दिया। ममता-भरे हाथ से उसे दुलराया और दुलराती रही। शेष सभी तोते को उसने पिंजरों में बन्द कर दिया।
तब उसके मानस-पटल पर एक सुसुप्त स्मृति जाग उठी। तब वह बहुत छोटी थी। यही सात-आठ वर्ष की भोली-नादान। तब उसके पति ने उसे एक कहानी सुनाई थी। उसे वह अक्षरश: तो याद नहीं है पर वह उसे पूर्णरूप से भूली भी नहीं है। इसलिए उसने अपने विचारों को केन्द्रित किया। वह उसे याद आने लगी-
एक राजकुमारी सुन्दर उपवन में फूल तोड़ने लगी। आम्र वृक्ष पर उसने एक सुन्दर तोती को गीत गाते सुना। पलक उठाकर उस ने जैसे ही उस तोती को देखा वैसे ही उसे पाने के लिए वह उत्कंठित हो गयी। शीघ्र ही उसने उस तोती को पकड़ने के उपाय किये। तोती पकड़ ली गयी। वह अत्यन्त रूपवती और आकर्षक पंख वाली थी।
फिर उसके लिए एक पिंजरा, सोने का पिंजरा बनाया गया। उसमें उसे डाल दिया गया। बेचारी तोती उसमें उदास सी, बुझी-बुझी सी अन्तर्वेदना में जलती रहती थी। उसने गुनगुनाना और बोलना सर्वथा बन्द कर दिया। राजकुमारी का अहम् उसे सहन नहीं कर सका। उसने तोती को डाँटना शुरू कर दिया। तब तोती पिंजरें में ही इधर से उधर उड़ने लगी।
एक रात राजकुमारी बहुत उदास थी। उसका मन संगीत और क्रीड़ा में नहीं लग रहा था। तब उसने तोती से कहा-‘कोई कहानी सुनाओ।’ तोती ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। राजकुमारी गुस्सा हो गयी। उसे भला-बुरा कहा। पर तोती भी पूरी हठीली थी। नहीं मानी तो नहीं मानी। तब राजकुमारी ने निर्दयी शिकारी की तरह उसके एक पंख की एक पंखुड़ी नोच डाली। तोती मर्मान्तक चीत्कार कर उठी। बोली-‘मुझे पंखहीन मत करो राजकुमारी, मुझे जीवित मृत्यु न दो। मैं आपके पाँव छूती हूँ। मुझे बहुत दु:ख है, उस दु:ख में मुझे मौन रहने दो, मुझे आजाद कर दो।’
राजकुमारी के होंठों पर कुटिल-मुस्कान थिरक गयी और उसने उसी निष्ठुरता से तोती के पंख की एक पंखुड़ी और तोड़ डाली। तोती दर्द से चीख पड़ी। दुख से तड़पकर बोली, ‘‘सुनाती हूँ सुनाती हूँ, लो सुनो।’ और उस दिन से उस राजकुमारी ने अपना यह निश्चय बना लिया कि जब तोती उसकी बात न माने तब वह उसके पंख की एक पंखुड़ी तोड़ डाले। अन्ततोगत्वा सुन्दर तोती को उसने पंखहीन कर दिया; कुरूप और विकृत रूपवाली बना दिया। अब वह उड़ भी नहीं सकती थी। पिंजड़े में फड़फड़ा भी नहीं सकती। इस बीच तोती ने अपनी आपबीती सुनाई थी। आपबीती-हाँ, अपने जीवन की गाथा।
तोती और सीता।
आपबीती और उसका अतीत।
रात ढलते-ढलते अपने यौवन पर आ गई। नौकरानी सीता का खाना रखकर घर के निचले कमरे में खुर्राटे भरने लग गयी थी। सीता ने एक बार खिड़की की राह बाहर झांका। बाहर गहरा सन्नाटा था। घाटियों जैसी शून्यता प्रतीत हो रही थी। सीता उस तिमिर में एकटक देखती रही।
तोती के अतिरिक्त पिंजरे के सारे तोते सो गए थे।
सीता उन्हें देखती रही, देखती रही। फिर तकिए का संबल लेकर वह लेट गयी। पास में उसने अपनी तोती को बुला लिया। अप्रत्याशित उसने तोती के पंख की पंखुड़ी को तोड़ डाला। वह करुण-क्रन्दन कर उठी। उसकी छोटी-छोटी अँखियों में व्यथा भर आयी।...‘कहानी सुनाओ न ? सुनाओ न कहानी, मैं कहती हूँ चुप क्यों हो ?’ और उसने तोती को कस के पकड़ा। तोती रोई। सीता की आँखें भर आईं। उँगुलियों का बन्धन ढीला पड़ गया। तोती भयभीत सी एक ओर उड़कर बैठ गयी। सीता की भंगिमा कठोर हो गयी। अश्रुपूरित विचित्र भंगिमा से प्रतीत होता था कि वह आन्तरिक पीड़ा से पागल सी हो उठी है। जैसे उसके मन में अतीत की दुखद स्मृतियाँ और दुष्कल्पनाएँ सहस्र साँपों के फनों सी उसे डस रही हैं। उसका अंग-अंग दुख रहा हो-कितना पीड़ाजनक अतीत ! कितने जुल्म ! असह्य यंत्रणाएँ।
सीता ने एक बार अपनी प्रिय तोती की ओर फिर देखा। उसे लगा उसकी प्यारी तोती बोली रही है-कहानी सुना रही है।
बाइस वर्ष पहले की बात है-
सीता की आँखें आँसुओं के वाष्प से धुँधली-धुँधली हो गयी। उस धुँधलके में उसे तोती की आकृति दीखी। तोती कह रही थी-
बाइस वर्ष पूर्व-
जबलपुर में जहाँ मारवाड़ी परिवार आकर बस गए हैं, उन्हीं परिवारों में से एक घर, उच्च मध्य श्रेणी का घर। छोटी-सी परचून की दुकान है उनकी। अच्छी मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। उस घर की कथा भी बड़ी विचित्र है। उनके पुरखे लगातार दो पीढ़ियों से अजीब तरह से मरे थे। कोई हँसता मर गया और कोई दुख में पागल होकर मर गया। कोई भी स्वाभाविक मौत नहीं मरा एकदम अप्रत्याशित, बिलकुल आकस्मिक। कारण भी स्पष्ट था-बड़े दुस्साहस से वे व्यापार करते थे। अति लाभ में मृत्यु !....उसे दैवात् और ईश्वरीय लीला समझा जाए अथवा साधारण में विशेष !
उस परिवार का मुखिया आजकल दीनानाथ था। दीनानाथ के चार बेटे और दो पुत्रियाँ थीं। तीन बेटे व्यापार में लग गए थे और चौथा बेटा पढ़ रहा था। एक पुत्री का विवाह हो चुका था और दूसरी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। लड़कियों के नाम थे-सावित्री और सीता। सीता स्वभाव की अत्यंत चंचल और बातूनी थी। उसकी एक सहेली थी गीता, जो मराठी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार की बेटी थी। दोनों में गहरी और आत्मीय मित्रता। इसलिए वे दोनों साहित्य में अभिरुचि रखने लगीं। कविता भी करने लगीं। सीता, गीता को अपनी बालोपयोगी कविता सुनाती थी और गीता अपनी कविताएँ सीता को सुनाती थी फिर दोनों में बहस आरम्भ हो जाती थी। कोई अपनी कविता को एक-दूसरे से कम नहीं मानती थी। कभी-कभी उन में झगड़ा तक हो जाता था। इस झगड़े को निपटाने के लिए वे दोनों गीता के पिताजी के पास जाती थीं। मामला तय हो जाता था। गीता के पिताजी हँसकर कहते-एक-दूसरी की कविता-एक-दूसरी से बढ़कर है। दोनों राजी हो जातीं। अन्तस का वैमनस्य धुल जाता। मित्रता पूर्ववत् प्रगाढ़ हो जाती।
कभी-कभी दोनों सहेलियाँ परस्पर वार्तालाप करतीं। सीता उदास होकर कहा करती थी, ‘‘गीता, मेरे भाईजी (पिताजी) मेरी कभी भी तारीफ नहीं करते।
सीता निरुत्तर रही।
देखो सीता दीदी, यह असमय की उदासी मुझे उच्छी नहीं लगती। पति के आगमन पर अपार प्रसन्नता देखना चाहती हूँ।’’ मालती सहसा गंभीर हो गई। उसके स्वर में दर्द सा तैर उठा, शुभ बेला है न, अनागत मंगल की सूचक इन घड़ियों में तुम्हारी आँखों में व्यथा कैसी ? हर प्रतीक्षारत युवती विकल रहती है-अपने प्रीतम के लिए। उसकी पलक-पंखुड़ियाँ प्रीतम के पथ में बिछ जाती हैं और आत्मा की सहस्र ध्वनियाँ समवेत स्वर में कहती हैं-तुम मेरी आत्मा और भाव लोक के स्वामी हो, मेरे हृदय-पट अवरुद्ध नहीं है। उसकी समस्त अभिलाषाएँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए आतुर हैं। अब तुम देर न करो।’... हाँ दीदी, तुम भी अपने अन्तर पट के सारे द्वार खोल दो। अधरों पर मुस्कान ले आओ ताकि आने वाला प्रीतम तुम्हारे पावन-मुख के दर्शन मात्र से धन्य-धन्य हो उठे !’’ मालती के नयन भर आए। अन्तर्मन में सुसुप्त व्यथाएँ एक साथ जाग पड़ी हों, ऐसा उसके नयनों में उमड़े सावन भादों से लगा।
सीता सावधान हो गई। मालती के अश्रुपूरित मुख को देखकर वह विकल हो उठी। होंठों पर सूखी मुस्कान लाकर वह बोली, ‘‘तुम मुस्कराओ मालती, मेरे होंठों पर मुस्कान स्वयं नाच उठेगी।’’
‘‘भाग्यहीनों के जीवन में मुस्कान अपराध है।’
‘‘नहीं मालती, अपने आप पर इतनी निष्ठुर मत बनो। वैसे तुम्हारी तरह इस समाज की युवती की मांग का सिन्दूर न पोंछा गया हो पर दुर्भाग्य उसका तुमसे कम नहीं है। यहाँ होंठों की मुस्कानें भी अभिनय से सम्बन्ध रखती हैं।’’
‘‘क्यों दीदी ?’’
‘‘मालती, कुछ प्रारब्ध को अमिट मानकर सन्तोष कर लेते हैं। कुछ प्रारब्ध को कुछ नहीं समझते, तब उसे बहुत पीड़ाएँ उठानी पड़ती है।..मैं प्रारब्ध और विधि को नहीं मानती। ईश्वर की आस्था और उसके अस्तित्व में भी मुझे अधिक विश्वास नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा जीवनाधार कौन हो सकता है !’’
‘‘प्रभु ने तुम्हें पति दिया है।’’ मालती ने न चाहते हुए यह कहा।
‘‘हर पति हर पत्नी का आधार नहीं बन सकता।’’
‘‘तुम्हारे पास धन है।’’
‘‘धन आन्तरिक आनन्द का सृष्टा नहीं।’’
‘‘तुम्हें तुम्हारा पति अन्तरतम से चाहता है।’’ मालती सहम गयी।
‘‘वस्तुस्थिति इसके नितान्त विपरीत है।’’
मालती के मन में बादलों का घोर गर्जन सा हुआ। वह हतप्रभ सीता को देखती रही। स्थिर दृष्टि में अनेक प्रश्न ज्वलित हो उठे। कुछ क्षण अपने को सँभालने में उसे लग गए। अप्रिय और अवांछित बात सीता के मुँह से स्पष्ट एवं गम्भीर स्वर में सुनकर वह जड़ सी हो गई।
‘‘मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। मालती, वैधव्य की आग में सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली कवयित्री मालती से, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। वर्षोपरान्त मेरा स्वामी आ रहा है लगभग छ: वर्ष बाद; अर्धयुग बीत गया है। किन्तु मैं अपने स्वामी से प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वह किंचित भी प्रिय नहीं है।’’
‘‘दीदी ?’’
‘‘कुतूहल और दुख में डूब गई हो ? कठोर सत्य सुनने के लिए पत्थर का हृदय भी होना चाहिए। तुम्हारे जैसी कोमल मन वाली मेरी तीखी बातें नहीं सुन पाएगी। मैं मिथ्या-भाषण की आदी नहीं हूँ। झूठ बोलकर मैं अपने आपको अपराधी नहीं बना सकती। सब कहूँगी साफ-साफ।’’
‘‘किन्तु ऐसा सत्य निन्दनीय होता है। वह मनुष्य को श्रेष्ठ दृष्टि से गिरा देता है। मालती ने सँभलकर कहा।
अपने कंठ-स्वर में स्वाभाविक मृदुता लाती हुई सीता धीरे से बोली, ‘‘मेरे विचार तुमसे सर्वथा भिन्न है। तुम मीरा की तरह कन्हैया को अपना सर्वस्व मानकर अपनी वासना को, अपने अन्तस के उद्दाम को, अपनी अतृप्त अभिलाषाओं को आध्यात्मिक बाना पहना सकती हो। तुम बावरी मीरा बनकर अपने भौतिक सुखों को त्याग सकती हो। तुम अपनी कविता में वियोग की ज्वाला को शब्दों का रूप देकर तीव्र स्वर में कह सकती हो-मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मैं जीवन भर प्रतीक्षा करूँगी-लेकिन मैं इसे एक पलायन मानती हूँ। खैर, उन्हें आने दो। घर खुला है। नौकर स्वागत-सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।’’
मालती तनिक उन्मन्न सी हो उठी।
धीरे-धीरे सन्ध्या का आगमन होने लगा। प्रतीची के प्राँगण में अरुणिमा का सरोवर फैल गया। मालती अपने घर की छत पर जाकर उसे अनिभेष दृष्टि से देखने लगी।
‘‘सीता दीदी, इतना कठोर वचन क्यों कहती हैं। वह ऐसा सत्य क्यों बोलती हैं जो सबको अप्रिय और पीड़क लगे। पति से घृणा करती है पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका वह उद्घोष भी करें। ऐसा करना सर्वथा अनुचित एवं विवेक-शून्य है।’’ वह मन ही मन उन्मन्न सी हो उठी, तभी उसकी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं है।’’
दो राजस्थानी परिवार।
घर भी आमने-सामने। सभ्यता के प्रतीक। रंग-पुते। वैश्य जाति के। बीच की गली यही तीन-चार फीट की।
एक की स्वामिनी है-सीता। सास के देहान्त के उपरान्त अपने घर की एक तरह की मालकिन। उम्र तीस वर्ष। न ननद और न कोई और। अकेली, नितान्त अकेली। पैसे वाली।
दूसरी है-मालती। पूर्ण यौवन। विधवा। भावुक। कविता करती है। हर घड़ी, हर पहर, रात-दिन अपने भाव-लोक में विस्मृत रहती है। सास की सेवा करती है, ससुर के पाँव दबाती है बड़े देवर गिरधर को कॉलेज के लिए तैयार करती है, छोटे-छोटे चार देवरों और एक ननद को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, लिखाती-पढ़ाती है। उम्र है सोलह वर्ष। देवर से एक वर्ष छोटी।
वह पड़ौसिन है इसलिए सीता को प्राय: दीदी और कभी-कभी भाभी कहती है। सीता के पति को भैया कहकर सम्बोधित करेगी। ऐसा वह सोचती है, निश्चय कर चुकी है। इस बार वह उससे प्रत्यक्ष परिचय करेगी सीता के प्रति उसकी अच्छी दृष्टि नहीं है। अत: कभी-कभी उनमें काफी तनाव व कटुता भी आ जाती है।
सूरज क्षितिज का अन्तिम चुम्बन लेकर अस्त हो गया। अँधेरे का उमड़ता हुआ सैलाब संसार पर छाने लगा। मालती अब भी विचार-विमूढ़ खड़ी थी।
अचानक सीता की दृष्टि उस पर पड़ी। वह स्नान करके धोती सुखाने ऊपर आई थी। मालती को विचारों में खोई जानकर वह तुरन्त बोली, ‘‘क्या कोई नई कविता लिखने की सोच रही हो ? सुनो मालती, यह अन्धकार है न, थोड़ी देर में हम सबको अपने में समेट लेगा। क्यों न एक कविता इस अन्धकार पर लिख दो।’’
मालती का मन विपुल विषाद से भर आया। आँखें सजल हो उठीं। विगलित-स्वर में बोली, ‘‘क्यों सताती हो दीदी, बार-बार कविता-कविता कहोगी तो मैं कविता क्या, तुमसे बातचीत करना भी बन्द कर दूंगी।’’
‘‘ऐसा नहीं हो सकता है। यह सम्भव नहीं है। तुम हजार बार मुझसे लड़ चुकी हो फिर दोस्ती कर लेती हो।’’ सीता के स्वर में दृढ़ता थी।
‘‘मैं कहती हूँ मुझे अपरिसीम वेदना मत दो। मुझे आवश्यकता से अधिक तंग न करो। मीरा की उपमा से मुझे दु:ख न पहुँचाओ।’’...‘तुम वैधव्य की वेदना को क्या समझो ? जीवन में सदा तुमने कुकृत्य किए हैं। तुम्हारा चरित्र बुराइयों का दर्पण है। तुम पतन की चरम सीमा को देख चुकी हो। फिर भी तुम दर्प से सिर ऊंचा करके समाज में चलती हो। तुम उन्हीं प्राणियों में गिनी जाती हो जो अपमान को मान और घृणा को प्यार ही समझते हैं। उसके भेद-विभेद को नहीं समझते।’’ मालती का सारा शरीर आवेश में काँपने लगा।
सीता मुस्कराती रही। उसकी आँखों में सहज तारल्य था। स्वाभाविक दीप्ति थी।
‘‘तुम इतना सुनकर भी मुस्कराती हो। निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर तुम्हारा सिर नीचा नहीं होता। कैसी हो तुम ?’’ मालती चिढ़ गयी।
‘‘मैं तुम सभी से अच्छी हूँ। मैंने पाप किए हैं पर प्रच्छन्न नहीं। उन पापों के द्वारा मैंने किसी के हृदय को आघात नहीं पहुँचाया। मालती ! मैं इतना जानती हूँ-मेरा अपराध महापाप होकर भी अभिशाप नहीं हो सका, किंतु तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें। एक पल के लिए भी सुख नहीं दे सकता। तुम प्यासे पपीहे की तरह स्वाति बूँद की प्रतीक्षा करती रहती हो और मेरे मुँह में स्वाति बूँदें स्वत: आ आकर गिरती हैं, क्योंकि मेरा पाप सृष्टि की दृष्टि में है, यथार्थ के मूल में नहीं।’’
लेकिन समाज में तुम्हारा क्या स्थान है ?’’
‘‘मैं समाज, परिवार और पति की कोई चिंता नहीं करती। मैं सबकी छाती पर मूँग दलना जानती हूँ। मुझ में अदम्य साहस है। मैं किसी की परवाह नहीं करती।’’
‘‘थोड़ा और इन्तजार करो जब उम्र आदमी की कमर तोड़ देती है तब आदमी को यौवन में की गयी उच्छृंखलताओं का पश्चाताप करना पड़ता है। तब भूलें-दानवी पंजों की तरह उसके अंग-अंग को नोचती हैं।’’
‘‘मैं इतनी दुर्बल नहीं हूँ, मालती !’’ उसने सहजता से कहा, ‘तुम समाज के प्रहार से पलायन कर सकती हो, आत्महत्या कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकती। मैं इस घोर एकान्त में सुख की उपलब्धियों को एकत्रित करना जानती हूँ तुम्हारे समाज और परिवार के अतिरिक्त भी दुनिया बहुत बड़ी है।’’
मालती की सास ने पुकार लिया था, इसलिए वह चली गयी।
अँधेरा और एकान्त।
सीता विचलित सी खड़ी रही। उसका मन अवश हो उठा। वह नीचे आकर अपने अन्धकारपूर्ण कमरे में पड़ गयी। उसका मन भारी हो गया। आज मालती ने दैवात् उसके बारे में जो कहा, वह कटोक्ति की तरह उसे बेध गया। किंतु वह भी बहुत दु:खी है। भावुक है औचित्य और अनौचित्य का ख्याल ही नहीं रखती। फिर जैसे वह संभली। उसे उस पर इतना व्यंग्य नहीं करना चाहिए था।
कल सवेरे ही वह उससे क्षमा माँग लेगी। उसे फिर राजी कर लेगी। उसे अपनी बना लेगी। ऐसा सीता ने सोचा।
वह उठी। रोशनी की
भोजन आदि से निवृत्त होकर वह अपने पाले हुए चार तोतों को मिर्चे खिलाने लगी। तोते पिजरों से निकल-निकलकर उसके हाथों और कन्धों पर बैठ गए। तभी उसका कोचवान दूला आ गया। वह उसका ताँगा चलाता था। दिन भर की मजदूरी अपनी सेठानी के हाथ में रखकर उसने छुट्टी मांगी।
‘सुनों दूला !’’
दुला एक सिपाही की मुद्रा में तनकर खड़ा हो गया।
‘‘मूलिया और चम्पिया अभी तक नहीं आए ?’’
‘‘वे आते ही होंगे, सेठानी जी, वे ताँगों की अन्तिम खेप करने गए हैं। घंटे आधा घंटे में लौट आएँगे।’’
सीता गंभीर हो गयी। थोड़े रोष-मिश्रित स्वर में वह बोली, ‘‘हजार बार उन्हें आगाह कर दिया है कि ठीक आठ बजे घोड़ों को खोल दिया करो। आखिर उन निरीह जानवरों में भी प्राण होते हैं। वे भी थकते और टूटते हैं। पर इनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे खुद हैं वैसे ही सबका प्रयोग करते हैं। छि:, जाओ और कल सुबह उन्हें इसके लिए आगाह कर देना।’’
दूला चला गया।
सीता फिर नीरव एकान्त में अपने आप में तन्मय सी हो गयी। मालती के साथ हुआ अरुचिकर और अप्रिय वाद-विवाद उसे फिर याद आने लगा। वह याद करती-करती विहँस पड़ी। अपने आप से कह उठी-यहाँ प्राणी बद्ध-मूल संस्कारों से आक्रान्त है। उसके विरुद्ध में उठाए गए किसी भी कदम को वह हेय दृष्टि से देखता है। पाप-पुण्य धर्म-अधर्म नैतिक अनैतिक के मिथ्यादर्श के चक्कर में वह जीवन की सहज प्रक्रियाओं को विस्मृत करके समाज की मान्यताओं के निर्देशन में चलता है। आत्म-पीड़न वंचना, हनन सहकर भी वह उस सत्य को स्वीकार नहीं करता है जो वस्तुत: निगूढ़ सत्य है।
तभी उसकी पाली हुई तोती बोल उठी, ‘‘माँ-माँ, मुझे प्यार करो।’’
सीता ने अपने परिवार की उस अभिन्न सदस्या तोती को अपने हाथ की उँगुलियों पर बिठा दिया। ममता-भरे हाथ से उसे दुलराया और दुलराती रही। शेष सभी तोते को उसने पिंजरों में बन्द कर दिया।
तब उसके मानस-पटल पर एक सुसुप्त स्मृति जाग उठी। तब वह बहुत छोटी थी। यही सात-आठ वर्ष की भोली-नादान। तब उसके पति ने उसे एक कहानी सुनाई थी। उसे वह अक्षरश: तो याद नहीं है पर वह उसे पूर्णरूप से भूली भी नहीं है। इसलिए उसने अपने विचारों को केन्द्रित किया। वह उसे याद आने लगी-
एक राजकुमारी सुन्दर उपवन में फूल तोड़ने लगी। आम्र वृक्ष पर उसने एक सुन्दर तोती को गीत गाते सुना। पलक उठाकर उस ने जैसे ही उस तोती को देखा वैसे ही उसे पाने के लिए वह उत्कंठित हो गयी। शीघ्र ही उसने उस तोती को पकड़ने के उपाय किये। तोती पकड़ ली गयी। वह अत्यन्त रूपवती और आकर्षक पंख वाली थी।
फिर उसके लिए एक पिंजरा, सोने का पिंजरा बनाया गया। उसमें उसे डाल दिया गया। बेचारी तोती उसमें उदास सी, बुझी-बुझी सी अन्तर्वेदना में जलती रहती थी। उसने गुनगुनाना और बोलना सर्वथा बन्द कर दिया। राजकुमारी का अहम् उसे सहन नहीं कर सका। उसने तोती को डाँटना शुरू कर दिया। तब तोती पिंजरें में ही इधर से उधर उड़ने लगी।
एक रात राजकुमारी बहुत उदास थी। उसका मन संगीत और क्रीड़ा में नहीं लग रहा था। तब उसने तोती से कहा-‘कोई कहानी सुनाओ।’ तोती ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। राजकुमारी गुस्सा हो गयी। उसे भला-बुरा कहा। पर तोती भी पूरी हठीली थी। नहीं मानी तो नहीं मानी। तब राजकुमारी ने निर्दयी शिकारी की तरह उसके एक पंख की एक पंखुड़ी नोच डाली। तोती मर्मान्तक चीत्कार कर उठी। बोली-‘मुझे पंखहीन मत करो राजकुमारी, मुझे जीवित मृत्यु न दो। मैं आपके पाँव छूती हूँ। मुझे बहुत दु:ख है, उस दु:ख में मुझे मौन रहने दो, मुझे आजाद कर दो।’
राजकुमारी के होंठों पर कुटिल-मुस्कान थिरक गयी और उसने उसी निष्ठुरता से तोती के पंख की एक पंखुड़ी और तोड़ डाली। तोती दर्द से चीख पड़ी। दुख से तड़पकर बोली, ‘‘सुनाती हूँ सुनाती हूँ, लो सुनो।’ और उस दिन से उस राजकुमारी ने अपना यह निश्चय बना लिया कि जब तोती उसकी बात न माने तब वह उसके पंख की एक पंखुड़ी तोड़ डाले। अन्ततोगत्वा सुन्दर तोती को उसने पंखहीन कर दिया; कुरूप और विकृत रूपवाली बना दिया। अब वह उड़ भी नहीं सकती थी। पिंजड़े में फड़फड़ा भी नहीं सकती। इस बीच तोती ने अपनी आपबीती सुनाई थी। आपबीती-हाँ, अपने जीवन की गाथा।
तोती और सीता।
आपबीती और उसका अतीत।
रात ढलते-ढलते अपने यौवन पर आ गई। नौकरानी सीता का खाना रखकर घर के निचले कमरे में खुर्राटे भरने लग गयी थी। सीता ने एक बार खिड़की की राह बाहर झांका। बाहर गहरा सन्नाटा था। घाटियों जैसी शून्यता प्रतीत हो रही थी। सीता उस तिमिर में एकटक देखती रही।
तोती के अतिरिक्त पिंजरे के सारे तोते सो गए थे।
सीता उन्हें देखती रही, देखती रही। फिर तकिए का संबल लेकर वह लेट गयी। पास में उसने अपनी तोती को बुला लिया। अप्रत्याशित उसने तोती के पंख की पंखुड़ी को तोड़ डाला। वह करुण-क्रन्दन कर उठी। उसकी छोटी-छोटी अँखियों में व्यथा भर आयी।...‘कहानी सुनाओ न ? सुनाओ न कहानी, मैं कहती हूँ चुप क्यों हो ?’ और उसने तोती को कस के पकड़ा। तोती रोई। सीता की आँखें भर आईं। उँगुलियों का बन्धन ढीला पड़ गया। तोती भयभीत सी एक ओर उड़कर बैठ गयी। सीता की भंगिमा कठोर हो गयी। अश्रुपूरित विचित्र भंगिमा से प्रतीत होता था कि वह आन्तरिक पीड़ा से पागल सी हो उठी है। जैसे उसके मन में अतीत की दुखद स्मृतियाँ और दुष्कल्पनाएँ सहस्र साँपों के फनों सी उसे डस रही हैं। उसका अंग-अंग दुख रहा हो-कितना पीड़ाजनक अतीत ! कितने जुल्म ! असह्य यंत्रणाएँ।
सीता ने एक बार अपनी प्रिय तोती की ओर फिर देखा। उसे लगा उसकी प्यारी तोती बोली रही है-कहानी सुना रही है।
बाइस वर्ष पहले की बात है-
सीता की आँखें आँसुओं के वाष्प से धुँधली-धुँधली हो गयी। उस धुँधलके में उसे तोती की आकृति दीखी। तोती कह रही थी-
बाइस वर्ष पूर्व-
जबलपुर में जहाँ मारवाड़ी परिवार आकर बस गए हैं, उन्हीं परिवारों में से एक घर, उच्च मध्य श्रेणी का घर। छोटी-सी परचून की दुकान है उनकी। अच्छी मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। उस घर की कथा भी बड़ी विचित्र है। उनके पुरखे लगातार दो पीढ़ियों से अजीब तरह से मरे थे। कोई हँसता मर गया और कोई दुख में पागल होकर मर गया। कोई भी स्वाभाविक मौत नहीं मरा एकदम अप्रत्याशित, बिलकुल आकस्मिक। कारण भी स्पष्ट था-बड़े दुस्साहस से वे व्यापार करते थे। अति लाभ में मृत्यु !....उसे दैवात् और ईश्वरीय लीला समझा जाए अथवा साधारण में विशेष !
उस परिवार का मुखिया आजकल दीनानाथ था। दीनानाथ के चार बेटे और दो पुत्रियाँ थीं। तीन बेटे व्यापार में लग गए थे और चौथा बेटा पढ़ रहा था। एक पुत्री का विवाह हो चुका था और दूसरी एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। लड़कियों के नाम थे-सावित्री और सीता। सीता स्वभाव की अत्यंत चंचल और बातूनी थी। उसकी एक सहेली थी गीता, जो मराठी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार की बेटी थी। दोनों में गहरी और आत्मीय मित्रता। इसलिए वे दोनों साहित्य में अभिरुचि रखने लगीं। कविता भी करने लगीं। सीता, गीता को अपनी बालोपयोगी कविता सुनाती थी और गीता अपनी कविताएँ सीता को सुनाती थी फिर दोनों में बहस आरम्भ हो जाती थी। कोई अपनी कविता को एक-दूसरे से कम नहीं मानती थी। कभी-कभी उन में झगड़ा तक हो जाता था। इस झगड़े को निपटाने के लिए वे दोनों गीता के पिताजी के पास जाती थीं। मामला तय हो जाता था। गीता के पिताजी हँसकर कहते-एक-दूसरी की कविता-एक-दूसरी से बढ़कर है। दोनों राजी हो जातीं। अन्तस का वैमनस्य धुल जाता। मित्रता पूर्ववत् प्रगाढ़ हो जाती।
कभी-कभी दोनों सहेलियाँ परस्पर वार्तालाप करतीं। सीता उदास होकर कहा करती थी, ‘‘गीता, मेरे भाईजी (पिताजी) मेरी कभी भी तारीफ नहीं करते।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book