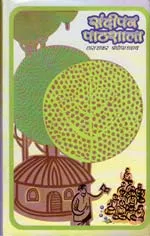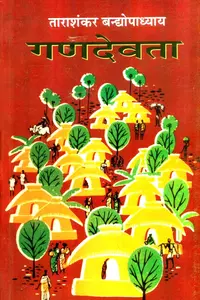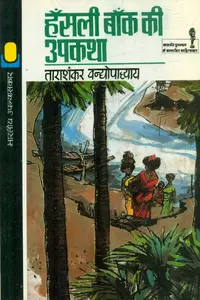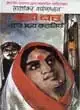|
दलित >> संदीपन पाठशाला संदीपन पाठशालाताराशंकर वन्द्योपाध्याय
|
438 पाठक हैं |
||||||
बांग्ला उपन्यास का हिन्दी अनुवाद...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘संदीपन पाठशाला’ प्रसिद्ध बांगला उपन्यासकार
ताराशंकर
बंद्योपाध्याय का एक अत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास है। इसमें लेखक ने सीताराम
नामक पाठशाला के एक अध्यापक का धरती के मानव का आसमान की बुलन्दियों को
छूने के लिए अनवरत संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण किया है। बीसवीं शताब्दी
के आरम्भिक दशकों की शिक्षा-पद्धिति-, ग्राम्य पाठ शालाओं और उनके पंडितों
की दयनीय दशा, सामन्ती और उच्चवर्गीय ग्राम्य शोषण का इसमें सजीव चित्रण
हुआ है। लेखक के शब्दों में ‘‘सीताराम मेरे लिए
यथार्थ है।
उसके मन का परिचय कितने ही बाद मुझे मिला है। उसको साहित्य के रूपदान करने
की वासना बहुत दिनों से भी वह सम्भव होने से मैं स्वयं सबसे अधिक आनन्दित
हूँ।’’
सीताराम बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में किस प्रकार मछुआ, सोनार टोला, साहा टोला आदि निम्न वर्ग के बालकों के लिए ‘संदीपन पाठशाला’ खोलता है। नीचे तबके के बच्चों को उच्च वर्ग के बड़े स्कूल के बच्चों की स्पर्द्धा में ऊँचा उठाने का उसका संकल्प कितना भव्य, कितना मानवीय और उदात्त है-यह सब वर्ग-चेतना की प्रगतिशील विचारधारा का द्योतक है।
आशा है बांगला के इस प्रसिद्ध उपन्यास का हिन्दी जगत् में अपूर्व स्वागत होगा।
सीताराम बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में किस प्रकार मछुआ, सोनार टोला, साहा टोला आदि निम्न वर्ग के बालकों के लिए ‘संदीपन पाठशाला’ खोलता है। नीचे तबके के बच्चों को उच्च वर्ग के बड़े स्कूल के बच्चों की स्पर्द्धा में ऊँचा उठाने का उसका संकल्प कितना भव्य, कितना मानवीय और उदात्त है-यह सब वर्ग-चेतना की प्रगतिशील विचारधारा का द्योतक है।
आशा है बांगला के इस प्रसिद्ध उपन्यास का हिन्दी जगत् में अपूर्व स्वागत होगा।
ताराशंकर बंद्योपाध्याय
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार पदमश्री एवं पद्मभूषण
से सम्मानित ताराशंकर बद्योपाध्याय बागला के एक सर्वप्रसिद्ध एवं
बहुचर्चित लेखक थे। उन्होंने लगभग 50 श्रेष्ठ उपन्यासों, डेढ़
सौ से
ऊपर उत्तम कहानियों और कई नाटकों की रचना की। उनका जन्म सन् 1898 में
लाभपुर जिला बीरभूम में हुआ था। किशोरावस्था से ही उनकी रुचि
क्रान्तिकारियों के साथ ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध कार्य करने की हो गई थी
जिसकी वजह से इन्होंने सेन्ट जेवियर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। सन् 1930 में
उन्होंने गांधी-आन्दोलन में भाग लिया और एक साल का कारावास काटा। जेल से
छूटने पर ताराशंकर ने लेखक को ही अपना उपजीव्य बना लिया। दलित और आपेक्षित
मानवता के लिए अथाह प्यार और सहानुभूति उनकी रचनाओं में उमड़-घुमड़ प्रकट
होने लगीं।
लेखक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता राजनीति से नहीं जनता-जनार्धन से थी। मनुष्य की पूर्णता में उनका विश्वास था।’ ‘गणदेवता’ का देबू ‘धातृदेवता’ का शिवनाथ, ‘संदीपन पाठशाला’ का सीताराम आदि उनके मनुष्य के इसी पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। जन-जीवन के अभाव, उनकी सभ्यता और संस्कृति उनके दुख-सुख उनके जाने-पहचाने थे। देश और राष्ट्र की कोई अमूर्त कल्पना वह नहीं करते थे। इनसे तात्पर्य है लोग धरती फसलें, खेती कर और लगान, ऋण जलकर, अकाल भूखमरी, बाढ़ गरीबों और मजदूरों का शोषण। इन सबका मार्मिक चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। यहीं उनकी सफलता का रहस्य है। लगभग 40 वर्ष तक अनवरत साहित्य-साधना करने के उपरान्त 74 वर्ष की आयु में वह स्वर्ग सिधार गए।
लेखक के रूप में उनकी प्रतिबद्धता राजनीति से नहीं जनता-जनार्धन से थी। मनुष्य की पूर्णता में उनका विश्वास था।’ ‘गणदेवता’ का देबू ‘धातृदेवता’ का शिवनाथ, ‘संदीपन पाठशाला’ का सीताराम आदि उनके मनुष्य के इसी पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। जन-जीवन के अभाव, उनकी सभ्यता और संस्कृति उनके दुख-सुख उनके जाने-पहचाने थे। देश और राष्ट्र की कोई अमूर्त कल्पना वह नहीं करते थे। इनसे तात्पर्य है लोग धरती फसलें, खेती कर और लगान, ऋण जलकर, अकाल भूखमरी, बाढ़ गरीबों और मजदूरों का शोषण। इन सबका मार्मिक चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। यहीं उनकी सफलता का रहस्य है। लगभग 40 वर्ष तक अनवरत साहित्य-साधना करने के उपरान्त 74 वर्ष की आयु में वह स्वर्ग सिधार गए।
एक
प्रतिष्ठा की कामना जब मनुष्य की रोटी-कपड़े की चिन्ता को भुला देती है तब
उसका राह चलना आसमान की ओर मुँह किए चलने के समान हो जाता है। अति-यथार्थ
मिट्टी की धरती के बाधा-विघ्नों को वह उस समय भूल ही जाता है।
एक कहानी हैः एक ज्योतिर्विद अँधेरी रात में आकाश के तारों की ओर देखते हुए राह चलते एक कुएँ में गिर गए थे। जिस पर व्यक्ति ने उनका उद्धार किया था, उद्धार करने के बाद ही निवृत्त् नहीं हुआ था, साथ ही साथ एक अनमोल उपदेश भी दे गया था। कहा था, अजी, धरती का हालचाल पहले जान लो, फिर आसमान की ओर देखना।
इस मशहूर अंग्रेजी कहानी के बारे में सीताराम जानता है, बचपन में उसने यह कहानी पढ़ी है, याद भी है।
सीताराम का पिता वह कहानी नहीं जानता, उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी बंगला पढ़ाई भी नहीं के बराबर। यही बात वह दूसरे ढंग से कहता है। कहता है, बेटा, ऊपर की ओर मत देखना। नीचे की ओर निगाह डालो। तुमसे कितने लोगों का हाल बेहतर है, कितने लोग तुमसे ज्यादा मान-सम्मान पाते हैं, उसका हिसाब मत लगाना वर्ना अशान्ति की आग बुझेगी ही नहीं। इससे बेहतर होगा कि तुमसे लोगों की हालत खराब है, तुमसे मान-सम्मान में कितने लोग छोटे हैं, उन्हीं का हिसाब लगाओ। इससे सुख न भी मिले, शान्ति में बीत जाएँगे तुम्हारे दिन।
सीताराम के कुल-गुरु कहते हैं, बेटा, कामना और आग में कोई फर्क नहीं, आग की लौ की भाँति कामना का स्वभाव भी ऊर्ध्वमुखी है। कितना भी उसे नीचे की ओर घुमा दो, वह फौरन पलटकर ऊपर की ओर सिर उठा लेगी। लेकिन जब वह बुझ जाती है। तब जीवन जली हुई लकड़ी जैसा हो जाता है, राख और कोयले के ढेर-सा।
बातें सीताराम के दिल को भी छू गई थीं। लेकिन फिर वे सारी बातें वह आज किसी कदर मान ही नहीं पा रहा है। किसान का बेटा जमाने के रिवाज के मुताबिक स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ने गया था। वहाँ अंग्रेजी अपने काबू में कराने के बूते की कमी के कारण व्यर्थमनोरथ हो अन्त में हुगली नार्मल स्कूल में पढ़ने चला गया था। वहाँ भी दो-दो बार फेल हो कर फिर सिर झुकाए लौट आया है। लेकिन इसी बीच जाने कब उच्चाशा की आग मन में सुलग उठी और वह नौकरी करना चाहता है। वह नौकरीपेशा बाबू बनेगा। पण्डित के रूप में संसार में जाना-माना जाएगा। लेकिन बाप रामनाथ ने कहा, नहीं यह इरादा छोड़ दो तुम। हम लोग किसान हैं, सिरजन की घड़ी से बाप-दादों का खानदानी काम है काश्तकारी। हम लोग खा-पी ओढ़-पहन अपनी औलाद को जर-जमीन दे, राम का नाम लेकर आँखें मूँदते चले आए हैं। यह सब छोड़कर तुम नौकरी ढूँढ़ रहे हो ! सो भी किसी कायदे की नौकरी होती तो बात कुछ समझ में आती। हाय ! हाय रे हाय रे किस्मत ! दाहिने हाथ से खुरपा चलाकर वह नींबू के एक दरख्त के नीचे से घास की निराई कर रहा था, बाएँ हाथ में हुक्का थामे तमाखू पी रहा था। बेटे से बातें करते समय दोनों ही काम बन्द थे, अब बीच में अधूरी छोड़ वह फिर से वे दोनों काम करने लग गया।
सीताराम सिर झुकाए खड़ा ही रहा।
अचानक फिर अपने हाथ का काम रोककर रमानाथ ने मुँह उठाकर पूछा, क्या है ? बताओ ! अपना इरादा तो बताओ।
सीताराम अबकी बार बोला, कैसी भी हो, एक नौकरी जब मिली है तो मैं कोशिश करके देखूँगा ही।
रमानाथ ने खेद और श्लेश दोनों मिलाकर कहा, तकदीर तुम्हारी ! नौकरी तो क्या, पेट-भर खाना और चार रुपये तनख्वाह ! आज दस साल स्कूल की फीस, बोर्डिंग का खर्च भरने के बाद आखिर में चार रुपये तनख्वाह और खुराकी, सो भी कपड़ा लत्ता नहीं। जो लोग बिना पढ़े-लिखे नौकर-खानसामे का काम करते हैं वे भी खुराकी और तनख्वाह के साथ कपड़े पाते हैं, बेटा !
सीताराम खामोश सिर झुकाए अब बाप के पास से चला गया। बेटे के बिन-बोले चले जाने में ही रमानाथ को उसका जवाब मिल गया। वह मौन रहकर बाप के प्रस्ताव का समर्थन नहीं जता गया। वही काम वह करेगा। खुराकी और चार रुपये तनख्वाह ही उसके लिए काफी है। कुछ देर उसके जाने के रास्ते की ओर एकटक देखने के बाद एक लम्बी साँस लेकर रमानाथ फिर काम में लग गया। इतनी देर में अचानक ही उसकी निगाह पड़ी, बातें करने की बेशुधी में जाने कब उसने पौधे की एक मोटी-सी जड़ काट डाली है ! शायद यह पौधा न भी जी सके। कड़वी-सी मुस्कराहट रमानाथ के चेहरे पर झलकी, उसे लगा, उसके जीवन के आशा-तरु की मूल ही उसने काट डाली है।
‘‘मुखिया दादा हैं क्या ?’’ उनके गाँव के आठ-आने हिस्से की जमीदारी का पुराना और खेती-बाड़ी की देखभाल करने वाला एतबारी कारिन्दा कन्हाई राय आकर खड़ा हो गया। यह कन्हाई राय मुजस्सम कलि है। नल-दमयन्ती जिन दिनों एक ही धोती में वनवास के दिन काट रहे थे-एक-दूसरे से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय कलि ने नल के हाथ में एक तेज छुरा जुटा दिया था। बस उसी कलि जैसे ही कन्हाई राय ने सीता के हाथों में यह नौकरी ला दी है। इसी कन्हाई राय ने ही सीताराम की नौकरी तय की है। उसी ने उसको प्रलुब्ध किया है। उसको देखकर रमानाथ अपने को सँभाल न सका, बोल पडा, आपने मुझसे यह दुश्मनी क्यों की यह तो बताइए ?
दुश्मनी ! –कन्हाई राय आश्चर्य करने लगा।
दुश्मनी तो है ही-रमानाथ ने कहा, अकेली औलाद है यह मेरी।
माँ मर गई इस बेटे की तो मैंने पाला-पोसा गोद में। पढ़ाई में आज चार साल से अलग-थलग रहा, सो भी मैंने कहा, झख मारने दो, बेटा पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो। फेल होगा, यह तो मुझे मालूम ही था। लेकिन मैने कहा, खैर, शौक पूरा कर ले। वहीं फेल होकर घर लौट आया। सोचा था, बहरहाल लड़के की साध तो पूरी हो गई, अब थिर होकर घर पर बैठेगा। मेरा दाहिनी हाथ बनेगा, खेती-बाड़ी देखेगा। बूढ़ा हो गया हूँ, पास रहेगा। सो नहीं, तुमने भला यह कैसी अक्ल दे दी उसे ?
राय ने ऐसी शिकायत की प्रत्याशा नहीं की थी। सीताराम से उसे प्यार है और उसी प्यार के कारण उसका अभिप्राय समझकर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है।
रमानाथ ने आँखें पोंछीं। आँखों में आँसू आ गए थे, बोला, अचानक अगर मर जाऊँ तो शायद बेटे के हाथों आग भी न मिले।
अब राय से बिना हँसे नहीं रहा गया। बोला, अरे ढाई मील का ही तो रास्ता है, दूर क्या कहते हो ? शाम को लड़के को पढ़ाकर खा-पीकर रोजाना घर भी आ सकेगा। उसका सिर भी दुखे तो इत्तिला मिलते ही घंटे-भर में घर आ जाएगा।
रमानाथ को इस बात का कोई जवाब ढूँढ़े नहीं मिला। खामोश मिट्टी की ओर नज़र गड़ाए घास के एक गुच्छे की जड़ पकड़कर खींचने लगा।
राय ने उसे समझाते हुए कहा, आप इसमें एतराज न करें। सीताराम का इसमें भला होगा, आपका भी। आठ आने हिस्सा के जमींदार के घर के लड़के का मास्टर बनेगा सीताराम, इससे,.....
रमानाथ ने यकायक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सरिश्तेखाने का कामकाज सीख ले, ऐसा कर देना भाई।
राय ने कहा, यह कौन-सा मुश्किल काम है ! गाहे-बगाहे अगर सरिश्तेखाने के नायब के पास बैठे तो सीखने में कै रोज लगेंगे ? खैर यह बात मैं रानी माँ से बता दूँगा।
हाँ, बाबू लोगों की गुमाश्तागिरी अगर मिल जाए हमारे गाँव की तो इज्जत तो मिलेगी ही, दो-दस रुपये भी; घर पर रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा।
अदृश्य विधाता हँसे, आग की छूत लगते ही आग सुलग उठती है। ऐन ऐसे ही समय सीताराम आकर खड़ा हो गया।
मैं जा रहा हूँ बप्पा !
रमानाथ खड़ा हो गया। बोला, ‘जा रहा हूँ’ नहीं कहा जाता है बेटा, आ रहा हूँ’ कहना चाहिए। चलो तिलक लगा दूँ, फूल दूँ, भगवान् को मत्था टेक लो चलो।
सीताराम चला गया। रमानाथ उदास-मन हुक्का लेकर ओसारे में बैठ गया।
एक कहानी हैः एक ज्योतिर्विद अँधेरी रात में आकाश के तारों की ओर देखते हुए राह चलते एक कुएँ में गिर गए थे। जिस पर व्यक्ति ने उनका उद्धार किया था, उद्धार करने के बाद ही निवृत्त् नहीं हुआ था, साथ ही साथ एक अनमोल उपदेश भी दे गया था। कहा था, अजी, धरती का हालचाल पहले जान लो, फिर आसमान की ओर देखना।
इस मशहूर अंग्रेजी कहानी के बारे में सीताराम जानता है, बचपन में उसने यह कहानी पढ़ी है, याद भी है।
सीताराम का पिता वह कहानी नहीं जानता, उसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी बंगला पढ़ाई भी नहीं के बराबर। यही बात वह दूसरे ढंग से कहता है। कहता है, बेटा, ऊपर की ओर मत देखना। नीचे की ओर निगाह डालो। तुमसे कितने लोगों का हाल बेहतर है, कितने लोग तुमसे ज्यादा मान-सम्मान पाते हैं, उसका हिसाब मत लगाना वर्ना अशान्ति की आग बुझेगी ही नहीं। इससे बेहतर होगा कि तुमसे लोगों की हालत खराब है, तुमसे मान-सम्मान में कितने लोग छोटे हैं, उन्हीं का हिसाब लगाओ। इससे सुख न भी मिले, शान्ति में बीत जाएँगे तुम्हारे दिन।
सीताराम के कुल-गुरु कहते हैं, बेटा, कामना और आग में कोई फर्क नहीं, आग की लौ की भाँति कामना का स्वभाव भी ऊर्ध्वमुखी है। कितना भी उसे नीचे की ओर घुमा दो, वह फौरन पलटकर ऊपर की ओर सिर उठा लेगी। लेकिन जब वह बुझ जाती है। तब जीवन जली हुई लकड़ी जैसा हो जाता है, राख और कोयले के ढेर-सा।
बातें सीताराम के दिल को भी छू गई थीं। लेकिन फिर वे सारी बातें वह आज किसी कदर मान ही नहीं पा रहा है। किसान का बेटा जमाने के रिवाज के मुताबिक स्थानीय हाई स्कूल में पढ़ने गया था। वहाँ अंग्रेजी अपने काबू में कराने के बूते की कमी के कारण व्यर्थमनोरथ हो अन्त में हुगली नार्मल स्कूल में पढ़ने चला गया था। वहाँ भी दो-दो बार फेल हो कर फिर सिर झुकाए लौट आया है। लेकिन इसी बीच जाने कब उच्चाशा की आग मन में सुलग उठी और वह नौकरी करना चाहता है। वह नौकरीपेशा बाबू बनेगा। पण्डित के रूप में संसार में जाना-माना जाएगा। लेकिन बाप रामनाथ ने कहा, नहीं यह इरादा छोड़ दो तुम। हम लोग किसान हैं, सिरजन की घड़ी से बाप-दादों का खानदानी काम है काश्तकारी। हम लोग खा-पी ओढ़-पहन अपनी औलाद को जर-जमीन दे, राम का नाम लेकर आँखें मूँदते चले आए हैं। यह सब छोड़कर तुम नौकरी ढूँढ़ रहे हो ! सो भी किसी कायदे की नौकरी होती तो बात कुछ समझ में आती। हाय ! हाय रे हाय रे किस्मत ! दाहिने हाथ से खुरपा चलाकर वह नींबू के एक दरख्त के नीचे से घास की निराई कर रहा था, बाएँ हाथ में हुक्का थामे तमाखू पी रहा था। बेटे से बातें करते समय दोनों ही काम बन्द थे, अब बीच में अधूरी छोड़ वह फिर से वे दोनों काम करने लग गया।
सीताराम सिर झुकाए खड़ा ही रहा।
अचानक फिर अपने हाथ का काम रोककर रमानाथ ने मुँह उठाकर पूछा, क्या है ? बताओ ! अपना इरादा तो बताओ।
सीताराम अबकी बार बोला, कैसी भी हो, एक नौकरी जब मिली है तो मैं कोशिश करके देखूँगा ही।
रमानाथ ने खेद और श्लेश दोनों मिलाकर कहा, तकदीर तुम्हारी ! नौकरी तो क्या, पेट-भर खाना और चार रुपये तनख्वाह ! आज दस साल स्कूल की फीस, बोर्डिंग का खर्च भरने के बाद आखिर में चार रुपये तनख्वाह और खुराकी, सो भी कपड़ा लत्ता नहीं। जो लोग बिना पढ़े-लिखे नौकर-खानसामे का काम करते हैं वे भी खुराकी और तनख्वाह के साथ कपड़े पाते हैं, बेटा !
सीताराम खामोश सिर झुकाए अब बाप के पास से चला गया। बेटे के बिन-बोले चले जाने में ही रमानाथ को उसका जवाब मिल गया। वह मौन रहकर बाप के प्रस्ताव का समर्थन नहीं जता गया। वही काम वह करेगा। खुराकी और चार रुपये तनख्वाह ही उसके लिए काफी है। कुछ देर उसके जाने के रास्ते की ओर एकटक देखने के बाद एक लम्बी साँस लेकर रमानाथ फिर काम में लग गया। इतनी देर में अचानक ही उसकी निगाह पड़ी, बातें करने की बेशुधी में जाने कब उसने पौधे की एक मोटी-सी जड़ काट डाली है ! शायद यह पौधा न भी जी सके। कड़वी-सी मुस्कराहट रमानाथ के चेहरे पर झलकी, उसे लगा, उसके जीवन के आशा-तरु की मूल ही उसने काट डाली है।
‘‘मुखिया दादा हैं क्या ?’’ उनके गाँव के आठ-आने हिस्से की जमीदारी का पुराना और खेती-बाड़ी की देखभाल करने वाला एतबारी कारिन्दा कन्हाई राय आकर खड़ा हो गया। यह कन्हाई राय मुजस्सम कलि है। नल-दमयन्ती जिन दिनों एक ही धोती में वनवास के दिन काट रहे थे-एक-दूसरे से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय कलि ने नल के हाथ में एक तेज छुरा जुटा दिया था। बस उसी कलि जैसे ही कन्हाई राय ने सीता के हाथों में यह नौकरी ला दी है। इसी कन्हाई राय ने ही सीताराम की नौकरी तय की है। उसी ने उसको प्रलुब्ध किया है। उसको देखकर रमानाथ अपने को सँभाल न सका, बोल पडा, आपने मुझसे यह दुश्मनी क्यों की यह तो बताइए ?
दुश्मनी ! –कन्हाई राय आश्चर्य करने लगा।
दुश्मनी तो है ही-रमानाथ ने कहा, अकेली औलाद है यह मेरी।
माँ मर गई इस बेटे की तो मैंने पाला-पोसा गोद में। पढ़ाई में आज चार साल से अलग-थलग रहा, सो भी मैंने कहा, झख मारने दो, बेटा पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो। फेल होगा, यह तो मुझे मालूम ही था। लेकिन मैने कहा, खैर, शौक पूरा कर ले। वहीं फेल होकर घर लौट आया। सोचा था, बहरहाल लड़के की साध तो पूरी हो गई, अब थिर होकर घर पर बैठेगा। मेरा दाहिनी हाथ बनेगा, खेती-बाड़ी देखेगा। बूढ़ा हो गया हूँ, पास रहेगा। सो नहीं, तुमने भला यह कैसी अक्ल दे दी उसे ?
राय ने ऐसी शिकायत की प्रत्याशा नहीं की थी। सीताराम से उसे प्यार है और उसी प्यार के कारण उसका अभिप्राय समझकर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है।
रमानाथ ने आँखें पोंछीं। आँखों में आँसू आ गए थे, बोला, अचानक अगर मर जाऊँ तो शायद बेटे के हाथों आग भी न मिले।
अब राय से बिना हँसे नहीं रहा गया। बोला, अरे ढाई मील का ही तो रास्ता है, दूर क्या कहते हो ? शाम को लड़के को पढ़ाकर खा-पीकर रोजाना घर भी आ सकेगा। उसका सिर भी दुखे तो इत्तिला मिलते ही घंटे-भर में घर आ जाएगा।
रमानाथ को इस बात का कोई जवाब ढूँढ़े नहीं मिला। खामोश मिट्टी की ओर नज़र गड़ाए घास के एक गुच्छे की जड़ पकड़कर खींचने लगा।
राय ने उसे समझाते हुए कहा, आप इसमें एतराज न करें। सीताराम का इसमें भला होगा, आपका भी। आठ आने हिस्सा के जमींदार के घर के लड़के का मास्टर बनेगा सीताराम, इससे,.....
रमानाथ ने यकायक उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सरिश्तेखाने का कामकाज सीख ले, ऐसा कर देना भाई।
राय ने कहा, यह कौन-सा मुश्किल काम है ! गाहे-बगाहे अगर सरिश्तेखाने के नायब के पास बैठे तो सीखने में कै रोज लगेंगे ? खैर यह बात मैं रानी माँ से बता दूँगा।
हाँ, बाबू लोगों की गुमाश्तागिरी अगर मिल जाए हमारे गाँव की तो इज्जत तो मिलेगी ही, दो-दस रुपये भी; घर पर रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा।
अदृश्य विधाता हँसे, आग की छूत लगते ही आग सुलग उठती है। ऐन ऐसे ही समय सीताराम आकर खड़ा हो गया।
मैं जा रहा हूँ बप्पा !
रमानाथ खड़ा हो गया। बोला, ‘जा रहा हूँ’ नहीं कहा जाता है बेटा, आ रहा हूँ’ कहना चाहिए। चलो तिलक लगा दूँ, फूल दूँ, भगवान् को मत्था टेक लो चलो।
सीताराम चला गया। रमानाथ उदास-मन हुक्का लेकर ओसारे में बैठ गया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book