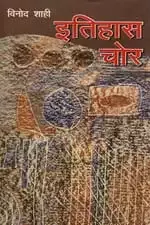|
कहानी संग्रह >> इतिहास चोर इतिहास चोरविनोद शाही
|
281 पाठक हैं |
||||||
हम आज़ाद तो हुए लेकिन हमारा इतिहास अभी तक उपनिवेशित है। साम्राज्य-वाद द्वारा विस्तारित नवउपनिवेशवाद के खिलाफ़ हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन अब वह लड़ाई हमारी सरकारें या सत्ता-वर्चस्वी वर्ग नहीं लड़ रहे।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘इतिहास चोर’ की कहानियां न तो अर्थ में ‘ओरिएण्टलिस्ट’ हैं कि इनमें तीसरी दुनिया के उस विशिष्ट यथार्थ को भारतीय संदर्भ में पकड़ने की कोशिश हुई है जो इन्हें आधुनिकता या उत्तर-आधुनिकता का विकल्प तलाशने की ओर ले जाता है; और न ही आप इन कहानियों को यथार्थवाद के अभी तक महत्त्वपूर्ण बने रहने का ऐसा सबूत मान सकते हैं, जो सामाजिक यथार्थ के करीब होने की कोशिश में इनमें झलकता है।
दरअसल, ये कहानियां इतिहास और चेतना के बीच, यथार्थ और मनुष्य के बीच तथा संघर्ष और आत्मान्वेषण के बीच एक पुल बनाने के बजाय, यह खोज़ करती हैं कि इन दोनों विरोधी प्रतीत होने वाले ध्रुवों के बीच कोई बुनियादी या तात्त्विक अखंडता या एकात्मता की कोई संभावित भूमि है या नहीं। इसलिए इन कहानियों में आप जन के भीतर से मनुष्य को तलाशने की बेचैनी को देख पायेंगे और उस छटपटाहट को भी जो इतिहास के समाज-सांस्कृतिक पक्ष के जीवन के अपने जैव-चेतन इतिहास की तरह पुनरुपलब्ध करने की ओर ले जाती हैं।
कहानियों की मार्फत जीवन और यथार्थ के विराट सवालों से टकराने की बजाय मौजूदा कहानी क्षण, स्थिति या कोण को इतना महत्त्व देने लगी है कि बड़े सवाल इस विधा की सृजन-सीमा से बाहर हो रहे हैं। ये कहानियां कहानी विधा की इस सीमा को तोड़ने की एक कोशिश है।
दरअसल, ये कहानियां इतिहास और चेतना के बीच, यथार्थ और मनुष्य के बीच तथा संघर्ष और आत्मान्वेषण के बीच एक पुल बनाने के बजाय, यह खोज़ करती हैं कि इन दोनों विरोधी प्रतीत होने वाले ध्रुवों के बीच कोई बुनियादी या तात्त्विक अखंडता या एकात्मता की कोई संभावित भूमि है या नहीं। इसलिए इन कहानियों में आप जन के भीतर से मनुष्य को तलाशने की बेचैनी को देख पायेंगे और उस छटपटाहट को भी जो इतिहास के समाज-सांस्कृतिक पक्ष के जीवन के अपने जैव-चेतन इतिहास की तरह पुनरुपलब्ध करने की ओर ले जाती हैं।
कहानियों की मार्फत जीवन और यथार्थ के विराट सवालों से टकराने की बजाय मौजूदा कहानी क्षण, स्थिति या कोण को इतना महत्त्व देने लगी है कि बड़े सवाल इस विधा की सृजन-सीमा से बाहर हो रहे हैं। ये कहानियां कहानी विधा की इस सीमा को तोड़ने की एक कोशिश है।
गंभीर पाठकों के लिए एक अत्यंत रोचक, पठनीय और विचारणीय संग्रह है यह।
सीधे मुख़ातिब भी
हम आज़ाद तो हुए लेकिन हमारा इतिहास अभी तक उपनिवेशित है। साम्राज्य-वाद
द्वारा विस्तारित नवउपनिवेशवाद के खिलाफ़ हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन अब
वह लड़ाई हमारी सरकारें या सत्ता-वर्चस्वी वर्ग नहीं लड़ रहे। वह लड़ाई
बेहद सूक्ष्म, ज़टिल और व्यापक आयामों पर अपनी पूरी ज़िंदगी के लगभग हर
पहलू को हथियार बनाने की ज़रूरत के साथ, ख़ुद हमें हमारे मुल्क़ के हर आम
आदमी को लड़नी पड़ रही है। सत्ता के गलियारों में ज़रा सी आहट भी नहीं
होती और जन अनाम समरभूमि में बेनाम मृत्यु के अंधेरे में खोता जाता है। तो
वे, जिन्होंने इस तीसरी दुनिया के इतिहास को नष्ट किया है-हालांकि
जिन्होंने ‘इतिहास के अंत’ का शोर दूसरी दुनिया के
संदर्भ में
बरपा किया है और तीसरी दुनिया के इतिहास के बेरहम क़त्ल को तवज्जो देने
लायक़ भी नहीं समझा है-उनसे, अपने इतिहास को वापस लाने की ज़द्दोज़हद, अब
ख़ुद हमें, अपने ही बूते पर, अपने क़मजोर पैरों पर खड़े हो कर, करनी है और
चूंकि हम इतिहास-हंताओं के दरबार में सामने से दाख़िल होने के अयोग्य करार
दिये जा चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा करने के लिए चोर-रास्तों को तलाशना है।
यही है मेरे इस ‘इतिहास चोर’ का साहसिक अभियान।
उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ हमें घेरे हुए हैं, परंतु इसी वज़ह से हमारा इतिहास ‘दोयम’ (सबाल्टर्न) इतिहास नहीं हो जाता। परंतु जब तक हम अपने अंतर्विरोधों से घिरे हैं-अपने सामाजिक अंतर्विभाजानों की नींव पर बने सांप्रदायिक-सांस्कृतिक गुंबजों की एक दूसरे को काटती गूंजों-अनुगूजों द्वारा अकसर बहरे हुए जाते हैं- संवेदनहीन, जड़, सहानुभूतिशून्य, बर्बर-तब तक हमें आतंकवादी साज़िशों की परछाइयों से निजात कैसे मिल सकती है ? बेशक वे साजिशें साम्राज्यवाद के द्वारा मुहैया किये गये अंधेरे महफ़ूज कोनों में छिप कर सरअंजाम होती हैं, लेकिन वजह बनते हैं; हमारे अपने विभाजन, अंतर्विभाजन, अंतर्विरोध, विरोधाभास, जो विडंबनापूर्ण परिणतियों में बदल जाते हैं। मेरी कुछ कहानियां पंजाब के आतंकवाद की छायाओं को इन्हीं प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, समाज-सांस्कृतिक अंतर्विरोधों-विभाजनों की शक्ल में पकड़ती हुई उस आदमी को तलाशती हैं, जो एक विकल्प बन सके-किसी ‘आत्मगर्भा’ की तरह या ‘खालिस लोग’ को ‘रिपुदमन’ और ‘थम्मन’ की तरह। बेशक मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, परंतु इतने भर से मुझे संतोष नहीं होता। मैं और गहरे में उतरना चाहता हूं-उन जड़ों तक, उन स्रोतों के आसपास, जहां यह पूरा जागतिक परिवेश किन्हीं जैविक गुत्थियों की शक्ल में हमारी अनुभूति के आलोक में परत दर परत खुलने की प्रक्रिया में आता जा रहा हो....
‘चर्म-गांठ’ रैदास की प्रसिद्ध पंक्ति ‘चरम-गाठ न जानई, लोग गठावैं पनुही’ से प्रेरित है। परिवेश की भयानक, व्यापक गहन गुत्थियां अंतत: हमें एक तरह की चर्म-गांठ की तरह पुनरुपलब्ध होती हैं, जहां से उस गांठ को खोलने की कोशिश करते हुए हम व्यापक संदर्भों में दिशाएँ तलाशा करते हैं। इस कहानी में मस्तिष्क में दो हिस्सो में अंतर्विभाजन का रूपक मुझे अपने परिवेश की बाबत एक जैविक स्टेटमेंट की तरह मिला। एक दलित डॉक्टर के हाथों उसका उपचार मेरे लिए महज ‘ओरिएंटलिस्ट’ मुक्ति नहीं है, क्योंकि हम तो अपना पुनःसृजन करते हुए पहली दुनिया के वर्चस्व और अपनी दोयम स्थिति-दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। हम मौजूदा दौर के समूचे वैश्विक अंतर्विभाजन का वह केंद्र या धुरी बन गये हैं, जो खुद उसकी न तो वज़ह है और न परिणाम, बल्कि मूकद्रष्टा की तरह मूकभोक्ता होने की पीड़ा उसके हिस्से आती है। वज़ह और परिणाम-दोनों वर्चस्वी वर्गों की मुट्ठियों में कैद हैं और हम तीसरी दुनिया के सामान्य जन, उनके उत्पीड़न की कीली होने के बावजूद सिवाय संघर्ष-चिंतन या आत्म-साधना के फ़िलहाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन यही तो भूमिका है। वास्तविक इतिहास-जनेतिहास तो अभी लिखा जाना शुरू ही हुआ है। बेशक फ़िलहाल हम विस्थापित मज़दूरों की तरह ‘दलदल’ में फंसे हैं और ग़रीब किसानों की तरह ‘ख़ुदकुशी’ के पुराण लिख रहे हैं। बाज़ारवाद के शोषणकारी समीकरणों से घिरे हम उत्तर पाने का स्वप्न तक भी नहीं देख पा रहे हैं। परंतु गहरे में, उत्पीड़न के भीतर, जो शिद्दत भरा मंथन इस सबसे पैदा होता है, वह इतिहास के गर्भ के भीतर छिपी अनेक बेशकीमती विधियों को भी उजागर करता ही है।
इसी उम्मीद में, इन कहानियों की मार्फत फिलहाल मंथन-आलोड़न में धैर्य धारण किये बैठा हूं, संभवतः यही इन कहानियों का भी मूल स्वर है।
उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ हमें घेरे हुए हैं, परंतु इसी वज़ह से हमारा इतिहास ‘दोयम’ (सबाल्टर्न) इतिहास नहीं हो जाता। परंतु जब तक हम अपने अंतर्विरोधों से घिरे हैं-अपने सामाजिक अंतर्विभाजानों की नींव पर बने सांप्रदायिक-सांस्कृतिक गुंबजों की एक दूसरे को काटती गूंजों-अनुगूजों द्वारा अकसर बहरे हुए जाते हैं- संवेदनहीन, जड़, सहानुभूतिशून्य, बर्बर-तब तक हमें आतंकवादी साज़िशों की परछाइयों से निजात कैसे मिल सकती है ? बेशक वे साजिशें साम्राज्यवाद के द्वारा मुहैया किये गये अंधेरे महफ़ूज कोनों में छिप कर सरअंजाम होती हैं, लेकिन वजह बनते हैं; हमारे अपने विभाजन, अंतर्विभाजन, अंतर्विरोध, विरोधाभास, जो विडंबनापूर्ण परिणतियों में बदल जाते हैं। मेरी कुछ कहानियां पंजाब के आतंकवाद की छायाओं को इन्हीं प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में, समाज-सांस्कृतिक अंतर्विरोधों-विभाजनों की शक्ल में पकड़ती हुई उस आदमी को तलाशती हैं, जो एक विकल्प बन सके-किसी ‘आत्मगर्भा’ की तरह या ‘खालिस लोग’ को ‘रिपुदमन’ और ‘थम्मन’ की तरह। बेशक मुझे ऐसे लोगों की तलाश है, परंतु इतने भर से मुझे संतोष नहीं होता। मैं और गहरे में उतरना चाहता हूं-उन जड़ों तक, उन स्रोतों के आसपास, जहां यह पूरा जागतिक परिवेश किन्हीं जैविक गुत्थियों की शक्ल में हमारी अनुभूति के आलोक में परत दर परत खुलने की प्रक्रिया में आता जा रहा हो....
‘चर्म-गांठ’ रैदास की प्रसिद्ध पंक्ति ‘चरम-गाठ न जानई, लोग गठावैं पनुही’ से प्रेरित है। परिवेश की भयानक, व्यापक गहन गुत्थियां अंतत: हमें एक तरह की चर्म-गांठ की तरह पुनरुपलब्ध होती हैं, जहां से उस गांठ को खोलने की कोशिश करते हुए हम व्यापक संदर्भों में दिशाएँ तलाशा करते हैं। इस कहानी में मस्तिष्क में दो हिस्सो में अंतर्विभाजन का रूपक मुझे अपने परिवेश की बाबत एक जैविक स्टेटमेंट की तरह मिला। एक दलित डॉक्टर के हाथों उसका उपचार मेरे लिए महज ‘ओरिएंटलिस्ट’ मुक्ति नहीं है, क्योंकि हम तो अपना पुनःसृजन करते हुए पहली दुनिया के वर्चस्व और अपनी दोयम स्थिति-दोनों से एक साथ लड़ रहे हैं। हम मौजूदा दौर के समूचे वैश्विक अंतर्विभाजन का वह केंद्र या धुरी बन गये हैं, जो खुद उसकी न तो वज़ह है और न परिणाम, बल्कि मूकद्रष्टा की तरह मूकभोक्ता होने की पीड़ा उसके हिस्से आती है। वज़ह और परिणाम-दोनों वर्चस्वी वर्गों की मुट्ठियों में कैद हैं और हम तीसरी दुनिया के सामान्य जन, उनके उत्पीड़न की कीली होने के बावजूद सिवाय संघर्ष-चिंतन या आत्म-साधना के फ़िलहाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन यही तो भूमिका है। वास्तविक इतिहास-जनेतिहास तो अभी लिखा जाना शुरू ही हुआ है। बेशक फ़िलहाल हम विस्थापित मज़दूरों की तरह ‘दलदल’ में फंसे हैं और ग़रीब किसानों की तरह ‘ख़ुदकुशी’ के पुराण लिख रहे हैं। बाज़ारवाद के शोषणकारी समीकरणों से घिरे हम उत्तर पाने का स्वप्न तक भी नहीं देख पा रहे हैं। परंतु गहरे में, उत्पीड़न के भीतर, जो शिद्दत भरा मंथन इस सबसे पैदा होता है, वह इतिहास के गर्भ के भीतर छिपी अनेक बेशकीमती विधियों को भी उजागर करता ही है।
इसी उम्मीद में, इन कहानियों की मार्फत फिलहाल मंथन-आलोड़न में धैर्य धारण किये बैठा हूं, संभवतः यही इन कहानियों का भी मूल स्वर है।
विनोद शाही
चर्म-गांठ
वर दे ! वीणावादिनी वर दे !...’ कॉलेज के परिसर में खड़े कोई
तीन
हज़ार छात्र-छात्राएं समवेत स्वर में सुबह की प्रार्थना के इस साप्ताहिक
कर्मकांड को दोहरा रहे थे। नंदन मुश्किल से यहां पहुंचते-पहुंचते ही
पहुंचा था। छात्राओं के झुरमुट के पीछे खड़े होने में आसानी थी। इधर जगह
थोड़ी खुली थी। दूसरी तरफ़ तो जैसे किसी भीड़ का माहौल था। आज वह ज़िद
करके अपनी कार पर कॉलेज आया था। पिता शहर के नामी डॉक्टरों में से एक थे।
स्कूटर रात को ही पंक्चर हो गया था। पिता ने कहा भी कि रिक्शा करके चले
जाना, पर तब तो वह और भी देरी से पहुंचता। कुछ तो जल्दी थी ही, कार के
एक्सीलरेटर पर पांव भी उसका ज़्यादा दब जाता था। शहर की सड़कों पर
साठ-सत्तर की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, पर वह संभाल लेता था। लेकिन
आज यह क्या हुआ था ? अभी तक उसके जैसे होश उड़े हुए थे। तब शायद वह
अरुणिमा की बाबत ही सोच रहा था। शायद...कुछ याद नहीं पड़ता कि वह कहां
खोया था कि तभी उसे एक झटका सा लगा। कार चलाते हुए उसने देखा, काली साड़ी
पहने अरुणिमा बेखौफ़ सड़क पार कर रही थी।
यह यकीनन अरुणिमा ही थी। उससे एक साल सीनियर। उसे उसने मंच पर भाषण देते अकसर सुना था। होशियार लड़की थी। वह कभी उसके सामने पड़ जाता तो उससे दब कर बात करता। नहीं, उसे धोखा नहीं हुआ था। उसे देखते ही उसने ज़ोर से कार की ब्रेकें लगा दी थीं। बीच रास्ते में यूं कार रोकने की वजह से पीछे का सारा ट्रैफिक परेशानी में पड़ गया था। किसका शुक्र अदा करे वह कि टक्कर होते होते रह गयी। कार रुकी तो अरुणिमा का कोई पता नहीं था। तब वह वहां कहीं भी थी ही नहीं..वह कहीं भी नहीं थी। परसों सड़क पार करते वक़्त एक बस के आगे आ जाने के बाद उसकी मौत हो गयी थी। कल इसी वज़ह से कॉलेज बंद रहा था, तो आज वह उसे कैसे दिखायी दी ? वह जान रहा था कि यह मतिभ्रम था। उसके पिता मनोचिकित्सक थे। वह खुद भी मेडिकल ऐट्रेंस की तैयारी में जुटा था। वह जानता था, हेलुसीनेशन का क्या अर्थ होता है। लेकिन जो उसे दिखायी दिया था उस पर अविश्वास करने के लिए उसका मन राजी नहीं था।
कॉलेज में अफ़वाह थी,...नहीं, शायद यही सच था। उसकी करीबी सहेलियों ने बताया था कि वह एक्सीडेंट नहीं था, आत्महत्या थी। हो भी सकता था। वह और उसकी कुछ सहेलियां पिछले साल मेडिकल ऐट्रेंस में असफ़ल हो गयी थीं और अब अगले साल में दाखिला लेने के बावजूद ऐंट्रेस एग्ज़ाम की दोबारा तैयारी में जुटी थी। वह ख़ुद भी जानता था कि तैयारी कितनी मुश्किल हो गयी थी। इतना कंपीटीशन, इतनी प्रोफ़ेशनलिज़्म कि सुबह चार बजे से लगे हुए हैं और रात के ग्यारह-बारह बज़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का बोझ बढ़ता ही जाता है। विषय की ट्यूशन अलग, आब्जेक्टिव टेस्ट की ट्यूशनें अलग। जगह जगह प्राइवेट कोचिंग शॉप्स खुली हुई थीं शहर में। कोई कंप्यूटर कोचिंग का लालच देकर फुसलाता था, तो कोई इंसानी दिमाग़ की श्रेष्ठता को साबित करता हुआ। गुरु लोग पहले अध्यापकों में बदले थे, अब अध्यापक ज्ञान के माल के प्रोड्यूसर और सेल्समैन बन रहे थे। छात्रों के रूप में उनकी हालत इतनी खराब थी कि जिस दुकान पर जाते, लगता, दूसरी दुकान का माल बेहतर था।
उसके पिता ने कल ही हिसाब लगाया था कि उसकी ट्यूशनों पर अब तक कोई अस्सी हज़ार रुपया ख़र्च हो चुका था और अभी तीस-चालीस हज़ार और हो सकता था, इसके बावजूद कोई उम्मीद नहीं थी। निकल गये तो निकल ही गये, वरना..वरना हो सकता है, अरुणिमा की राह पर निकलने की नौबत आ जाये। बाजी जी जान की थी-न कम, न ज़्यादा। नंदन को शायद पैसे की इतनी फ़िक्र न थी। उसके पिता के पास काफ़ी पैसा था, लेकिन सब तो ऐसे नहीं थे ? नंदन को लगता था कि उसके पिता इसके लिए कसूरवार थे। उनकी इतनी ज़िद न रही होती तो शायद वह ऐसे कंपटीसन की राह ही न पकड़ता। पिता को वारिस चाहिए, एक क़ाबिल वारिस, जो उनकी प्रैक्टिस संभाल सके। लेकिन उनका वारिस हो सकने की क़ीमत कितनी बड़ी थी ? उसे लग रहा था जैसे अरुणिमा उसके भीतर कहीं, शायद दृष्टि नाड़ी के पीछे मध्य मस्तिष्क के किसी कोष में, उतर कर आसन ज़माये बैठी है। वही काले रंग की साड़ी, छोटी सी अर्ध चंद्राकार मैरून बिंदी, मछलीनुमा छोटे छोटे टॉप्स, पीछे की तरफ़ पूरी ताक़त से खींच कर बांधे गये बाल..कितनी खुश, कुछ गुनगुनाती हुई, बेफ़िक्र शरारती...
वर दे, वीणावादिनी वर दे..प्रार्थना ख़त्म होने जा रही थी। उससे थोड़ा आगे खड़ी उसकी क्लासफेलो आयशा ने पीछे मुड़ कर देखा। अरुणिमा का चेहरा उसके साथ गड्ड-मड्ड हो गया। वह चीखा, ‘काली साड़ी में अरुणिमाऽऽऽ!’’ आयशा भयभीत बदहवास सी और जोर से चीख़ पड़ी, ‘अरुणिमा..काली साड़ीऽऽऽ!’ पीछे पीछे लगभग सारी छात्राएं चीख़ने लगीं। आयशा ने भागना शुरू कर दिया। सब तरफ़ सारे छात्र-छात्राएं एक दूसरे को धकेलते-गिराते सब सब के ऊपर से कूदते-फ़लांगते आत्मरक्षा में जाने कहां कहां हो लिये ! चार-पांच छात्राएं नीचे गिरने की वज़ह से कुचली गयीं। अध्यापक उन्हें नियंत्रित करने की असफ़ल कोशिश करने लगे। प्रिंसिपल ने प्रार्थना करती छात्राओं से माइक पकड़ कर डांटने-डपटने के सुर में चीख़ना शुरू कर दिया। कोई असर नहीं। जिसे जिधर ज़गह मिलती, उधर, उस दिशा में कहीं जा कर समा जाता। कोई दस-पंद्रह मिनट बाद हालात काबू में आ गये। नीचे गिरी छात्राएं ज़ख्मी हो गयी थीं। एक की बांह हड्डी टूट जाने से फूल रही थी। एक के दांतों से खून बह रहा था। बाकी दोनों सिर थामे घुटने समेटे उकड़ूं हुई बैठी थीं। उनके उपचार के लिए प्रिंसिपल ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था।
उधर कुणाल पूछ रहा था नंदन से, ‘‘आख़िर हुआ क्या था ?’’
जवाब में नंदन कुछ पल ख़ामोश रह कर बोला था, ‘‘शायद मुझे ही कुछ हो गया था।’’
‘‘रात को देर तक पढ़ता रहा क्या ?’’
‘‘नहीं, रोज़ की तरह एक-डेढ़ बजे सो ही गया था।’’
‘‘सुबह फिर ज़ल्दी उठ गया होगा। एकाध दिन ऑफ ले कर आराम क्यों नहीं करता घर पर ?’’
‘‘एकाध दिन ?...घर पर दिन में भी कभी एक-दो घंटे नींद ले लो तो मम्मी नाराज़ होने लगती हैं। छह घंटे यहां कालेज़ खा लेता है, चार घंटे ट्यूशन, एक घंटा खाने-पीने और तैयार होने का, अब बाकी जो बचता है उसमें एक दो घंटे सो जाऊं तो पढ़ूँगा कब ?’’
‘‘मुझे लगता है, ट्यूशन का फायदा है तो सही, पर इतना नहीं।’’
‘‘भेड़ चाल है, पर क्या करें ? छोड़ दें तो वैसे जी घबराने लगता है कि पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं ! अब क्या करूँ ? इस वक्त भी सिर ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है। क्लासेज़ नहीं लगा सकूंगा आज।’’
‘‘तू बैठ, मैं करता हूं कुछ इंतज़ाम। नहीं तो एक बजे से पहले निकलने नहीं देगा कोई यहां से।’’
कुणाल गया, वाइस प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन ले कर नंदन को उसके घर छोड़ आया। वह अकसर उसके घर आता-जाता रहता था। उसके घर के हालात ऐसे थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की फ़ीस दे सकता था। जो था, जितना था, उतना भी उसके लिए काफ़ी था। नंदन उस पर मेहरबान था, सो उसे उससे उसकी ट्यूशन के नोट्स और टेस्ट वग़ैरह मिल जाते थे। ट्यूशनें न करने का उसे उलटा दोहरा फ़यदा हो रहा था।
इससे उसे सेल्फ स्टडी के लिए क़ाफ़ी वक़्त मिल जाता था, और साथ ही बने-बनाये नोट्स भी। लेकिन चाहे जो हो, नंदन का मुक़ाबला करना उसके बस की बात न थी। जिन सरकारी स्कूलों में वह पढ़ा था, उनके और नंदन के अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ था। फिर घर पर न माहौल था और न उतनी सुविधाएं, लेकिन इस सबके बावजूद उसके नंबर अच्छे आते थे। इसकी वजह शायद यह थी कि वह वाकई कुछ सीखना चाहता था-कुछ नया, कुछ ज़रूरी, जो आदमी के लिए सचमुच मायने रखता हो, वही उसकी भीतरी प्यास को बुझाने की सामर्थ्य रखता था। बारहवीं कक्षा के छात्र से ऐसी प्यास की उम्मीद करनी बेतुकी थी, लेकिन वह थी ज़रूर। इतनी साफ़ तो नहीं, पर कहीं गहरे अवचेतन-अमूर्त रूप में वह मौजूद थी। इस मौजूदगी की एक वजह, एक इतिहास भी था।
कुणाल के पिता धर्मचंद औरतों की बैलियां डिज़ाइन करने के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। घर के छोटे से ड्राइंगरूम को उनकी दुकान में बदल जाने के बाद अब उनके छोटे से घर में एक कमरा और रसोई जितनी जगह ही बची रह गयी थी। छत पर एक ओर पाखाने का इंतज़ाम था, तो दूसरी तरफ ख़ुद ही एंगल आयरन खड़े कर ऊपर डाली टीन की छत वाली एक मियानी थी। वहां कुछ चारपाइयां, गोल किये बिस्तर और टूटा-फूटा सामान पड़ा रहता था। एक तरह से यही कुणाल का स्टडी रूम भी था। सो एक लिहाज से वह ख़ुशक़िस्मत था कि अपनी बिरादरी वालों की तुलना में कम से कम उसके पास एक ऐसी जगह ज़रूर थी, जो उसे पढ़ने के लिए तन्हाई दे सकती थी। पिता ज़्यादातर नीचे अपनी दुकान पर बैठे काम करते रहते। मां सुबह का नाश्ता बना कर जो काम पर निकलती तो उसके लौटने का कोई ठिकाना न होता। वह नजदीक के किसी गांव के सरकारी हेल्थ सेंटर पर दाई का काम करती थी।
वहां उसे काफ़ी काम प्राइवेट तौर पर भी मिल जाता था, सो लंच का कोई ठौर-ठिकाना न था। दोपहर के लिए एक सब्जी या दाल वह बना जाती और आटा गूंथ कर रख देती। अपने लिए वह दो रोटियां बना कर साथ ले जाती। अब पीछे बाप-बेटे में से जिसे भूख लगती या जिसके पास जब वक़्त होता, तो अपनी अपनी रोटी ख़ुद बना कर तवे पर सेंक लेते। इस मामले में कोई किसी पर निर्भर न रहता और न ही कोई किसी की फ़िक्र ही करता। जिसे जिंदा रहना हो, रोटी उसे ही पकानी पड़ती। कुणाल के लिए यह बात उतनी परेशानी की नहीं थी, जितनी यह कि कभी-कभार उसे भी अपने पिता की जगह दुकान पर बैठना पड़ता। वैसे वहां कम ही ग्राहक आया करते थे, यह दुकान जानकार लोगों की ग्राहकी पर चलती थी। जिन्हें धर्मचंद के हुनर का पता था, वही यहां औरतों के पैरों का नाप देने आते। कुछ दूसरे दुकानदार भी धर्मचंद को अपने आर्डर दे जाते थे, लेकिन उनसे बनवायी पूरी वसूल नहीं होती थी, सो धर्मचंद की ज़्यादा रुचि सीधे ग्राहकों में ही रहती। पिता की गैरमौजूदगी में कुणाल वहां बैठता तो भी वह कुछ ज़रूर पढ़ ही लेता था, लेकिन चलती सड़क की वजह से एकाग्रता उतनी नहीं हो पाती थी। वह इसे नापसंद करता था, पर मज़बूर था।
दुकान ज़्यादा देर खाली छोड़ देने पर ग्राहकी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। वैसे इस बात को नापसंद करने की सिर्फ़ यही एक वजह नहीं थी। एक और वजह भी थी, जिसे ले कर वह मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। इसका ताल्लुक उसके पिता की एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि से था। इसका पता उनकी बिरादरी में लगभग सभी लोगों को था। कई लोग इस वजह से धर्मचंद का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वह हंस कर टाल जाता था। कुणाल सोचता कि अगर उसके पिता में यह खराबी न होती तो उनका बिजनेस कमाल का होता। वैसे कहीं गहरे में वह अपने पिता से थोड़ा सहमत भी हो जाता और तब...तब उसे अपने आपसे, अपने खानदान से, अपनी बिरादरी के छोटेपन और मजबूरियों से नफ़रत होने लगती। तब वह सोचता कि वह ज़्यादा देर उनका हिस्सा बन कर नहीं रहेगा। वह इन सब के कहीं पार निकल जायेगा-अपनी मां की तरह, अपनी मां से कहीं बेहतर तरीके से, क्योंकि वह अपनी मां की तुलना में ऐसा करने में ज़्यादा समर्थ हो सकता है...और यह सब सोच कर उसमें कुछ जानने, कर दिखाने की आग सी जलने लगती। उसकी अंदरूनी प्यास का स्रोत खुद उसके पिता थे और आज भी वह वही सब दोहराने जा रहे थे।
नंदन की अस्वस्थता की वजह से कुणाल जल्दी लौट आया था। उसके पिता उसे देख कर एकदम खुश हो गये।’’ अच्छा हो गया जो तू आ गया। सोच रहा था, किसे दुकान पर बिठा कर निकलूं। वो वाली नयी बैली बिक गयी है। ऐसा डिजैन बनाया था कि वो औरत उसे पहनते ही जैसे ज़मीन से एक हाथ ऊपर चलने लगी। तू देखता तो कहता..कौन सा शोरूम है इस शहर का जो उसके मुक़ाबले की बैली रखता हो। एकदम मुलायम। अंदर चारों तरफ़ जो फर लगायी थी, ज़रा ज़रा सी बाहर जो झलक रही थी। वो औरत कहने लगी, इंपोरटेड लगती है एकदम !’ जी ख़ुश हो गया। ले, बैठ अब सामान लाना है। तीन और आर्डर आये पड़े हैं। कल तक निपटा लूंगा किसी न किसी तरह।’
कुणाल बिना कुछ बोले शर्मसार वहीं बैठ गया। उसे पता था कि अब उसके पिता रात से पहले शायद ही लौटेंगे। वह कल्पना कर रहा था कि अब वे मुख्य सड़क पार करके पतली गली में दाखिल हो गये होंगे। फिर उन्होंने अपनी टोपी को जेब से निकाल कर सिर पर रख लिया होगा। अब वे रुके होंगे-दूसरी जेब से चश्मा निकाल कर उसे साफ करने के लिए। यह दूर की नजर के लिए था। चेहरे पर इतनी तबदीलियाँ काफ़ी थीं और अब वे खुद को महफ़ूज समझ रहे होंगे कि उन्हें बहुत जानकार लोगों के सिवाय कभी कभार मिलने वाले आसानी से पहचान नहीं पायेंगे। अब वे एकदम दूसरे आदमी हो गये थे। अब उन्हें किसी तरह की जवाबदेही की, मान-अपमान की ज़्यादा चिंता नहीं रही थी।
कुणाल यह सब ब्यौरेबार इसलिए जानता था, क्योंकि आस-पड़ोस और खुद अपनी मां से अपने पिता की बुराई सुन कर उसने एक दिन उनका पीछा किया था। उन सबके मुताबिक वे आवारागर्द थे। शहर की ऊंची जातियों की महिलाओं का पीछा करते थे। इस सबका मतलब यह था कि उनका चाल-चलन ठीक नहीं था। कुणाल के लिए इस पर यकीन करना सहज संभव नहीं था। लेकिन जब पिता का पीछा करते हुए उसने उनकी वे हरकतें देखीं तो वह पेरशान होने लगा। उस दिन उसने देखा कि चेहरा-मोहरा थोड़ा बहुत बदल लेने के बाद उन्होंने अपने पर्स से डायरी निकाली थी, जिस पर आम तौर पर वे अपने ग्राहकों के पैरों का नाप लेने के बाद उनके पते-ठिकाने नोट किया करते थे। इसके बाद वे एक पॉश लोकेलिटी की बड़ी सी कोठी के बाहर एक पेड़ की छाया के नीचे यूं उकड़ूं हो कर बैठ गये थे, जैसे कोई बेहद थका-मांदा आदमी ज़रा देर को दम मारने के लिए बैठ गया हो ! वहां के आधेक घंटा बैठे रहे।
फिर अचानक उस कोठी से किसी औरत के निकलने के बाद वे चौकन्ने हो गये। उनकी आंखों में जाने कैसी दैवी चमक सी आ गयी। वह औरत बाहर निकली, फिर बाहर पार्क की गयी अपनी कार में बैठ कर जाने कहां चली गयी। इसके बाद वे उठे और वहां जा कर कुछ तलाशने लगे, जहां अभी अभी वह कार खड़ी हुई थी, फिर उन्होंने जमीन को हथेलियों से छू छू कर आंखों को लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे उठे और उस दिशा में चल पड़े जिस ओर उस कार में बैठी हुई महिला आगे जा कर गायब हो गयी थी। कुणाल ने देखा था कि उसके पिता उस वक़्त अपने आप में नहीं थे। उनकी आँखें किसी अद्भुत प्रकाश से भरी हुई थीं और चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे कोई आदमी अभी अभी समाधि लगा कर उठा हो ! कुणाल को अपने पिता पर तरस भी आया, ख़ुद में शर्म भी महसूस हुई लेकिन वह अपने पिता से नफ़रत नहीं कर पाया। उससे रहा नहीं गया और फिर वह अचानक आगे बढ़ कर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। जिस्म से गर्मी फूट रही थी। वह कुछ पूछना चाहता था, पर उसके पास कोई लफ़्ज कहां थे। कुणाल के पिता ने उसे देखा, रुके, फिर हंस दिये, जा जा कर अपनी जिंदगी बना, कुछ पढ़-लिख। मेरे पीछे वक़्त क्यों बरबाद करता है ?’
कुणाल के पैर ज़मीन से जैसे पत्थर बन कर चिपक गये थे। वह किसी बेजान बुत की तरह था लेकिन इस तरह कांप रहा था, जैसे कि नीचे भूचाल आ जाने से धरती ही कांप रही हो। पिता फिर हंसे, फिर उन्होंने बेटे को छू कर प्यार किया और इशारा करके अपने साथ नीचे ज़मीन पर बैठने को कहा। इसके बाद उनकी आंखें आधी मुंद गयीं और वे ख़ुद में डूबे डूबे गंभीर आवाज़ में बोलने लगे, ‘‘मैं औरतों की जूतियां बनाता हूं। वो मेरा धरम है, रोज़गार है। पर मैं सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए ही जूतियां नहीं बनाता। मैं उनमें ख़ुद को डाल देता हूं। एक एक जूती मेरी सांसों को, मेरी धड़कनों को, मेरे जिस्म में डोलते लहू की हरकतों को ख़ुद में संजोये रहती है। मैं तब तक उसे नहीं सींता जब तक कि अपने जिस्म से हाथ भर ऊपर न उठ जाऊं और फिर एक दिन कोई न कोई औरत आती है, चार पैसे फेंक कर समझती है कि उसने उसकी कीमत चुका दी।
मैं हंस कर, जो मिलता है, ले लेता हूं, पर ज्योंही वो जूती मेरी दुकान से बाहर जाती है, मुझे लगता है, कोई मुझे अधमरा करके छोड़ गया है। फिर मेरा वहां दिल नहीं लगता। मैं अपनी जूती का पीछा करने निकल पड़ता हूं। जब जवान था तो लोग ये समझ कर कि मैं उन औरतों के पीछे जाता हूं, मेरी पिटाई भी कर देते थे। पर मैं उन्हें क्या बताता, क्या समझाता ? मार खा लेता, फिर चुपचाप लौट आता। अब मैं अपनी शकल बदल लेता हूं। अब लगता है जैसे कि मैं बूढ़ा भी हो चला हूं, तो अब लोग मजाक उड़ा कर छोड़ देते हैं, मारते-पीटते नहीं। पर मैं क्या करूं ? मजबूर हूं। मैं अपनी जिंदगी से पराया हो के कैसे जीऊं ? जब तक मुझे अपनी वही जूती पहने वह औरत दिखायी नहीं देती, जब तक मैं उसे इस वजह से ख़ुश नहीं देख लेता और जब तक उस ज़मीन को चूम कर उसकी मिट्टी अपनी आंखों से नहीं लगा लेता, मेरी देह में प्राण लौटते ही नहीं। क्या करूँ ? तेरी मां भी मुझे कभी समझ नहीं पायी। तू ही बता देना उसे कि मुझे दूसरी औरतों से कुछ लेना-देना नहीं...’।
यह यकीनन अरुणिमा ही थी। उससे एक साल सीनियर। उसे उसने मंच पर भाषण देते अकसर सुना था। होशियार लड़की थी। वह कभी उसके सामने पड़ जाता तो उससे दब कर बात करता। नहीं, उसे धोखा नहीं हुआ था। उसे देखते ही उसने ज़ोर से कार की ब्रेकें लगा दी थीं। बीच रास्ते में यूं कार रोकने की वजह से पीछे का सारा ट्रैफिक परेशानी में पड़ गया था। किसका शुक्र अदा करे वह कि टक्कर होते होते रह गयी। कार रुकी तो अरुणिमा का कोई पता नहीं था। तब वह वहां कहीं भी थी ही नहीं..वह कहीं भी नहीं थी। परसों सड़क पार करते वक़्त एक बस के आगे आ जाने के बाद उसकी मौत हो गयी थी। कल इसी वज़ह से कॉलेज बंद रहा था, तो आज वह उसे कैसे दिखायी दी ? वह जान रहा था कि यह मतिभ्रम था। उसके पिता मनोचिकित्सक थे। वह खुद भी मेडिकल ऐट्रेंस की तैयारी में जुटा था। वह जानता था, हेलुसीनेशन का क्या अर्थ होता है। लेकिन जो उसे दिखायी दिया था उस पर अविश्वास करने के लिए उसका मन राजी नहीं था।
कॉलेज में अफ़वाह थी,...नहीं, शायद यही सच था। उसकी करीबी सहेलियों ने बताया था कि वह एक्सीडेंट नहीं था, आत्महत्या थी। हो भी सकता था। वह और उसकी कुछ सहेलियां पिछले साल मेडिकल ऐट्रेंस में असफ़ल हो गयी थीं और अब अगले साल में दाखिला लेने के बावजूद ऐंट्रेस एग्ज़ाम की दोबारा तैयारी में जुटी थी। वह ख़ुद भी जानता था कि तैयारी कितनी मुश्किल हो गयी थी। इतना कंपीटीशन, इतनी प्रोफ़ेशनलिज़्म कि सुबह चार बजे से लगे हुए हैं और रात के ग्यारह-बारह बज़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का बोझ बढ़ता ही जाता है। विषय की ट्यूशन अलग, आब्जेक्टिव टेस्ट की ट्यूशनें अलग। जगह जगह प्राइवेट कोचिंग शॉप्स खुली हुई थीं शहर में। कोई कंप्यूटर कोचिंग का लालच देकर फुसलाता था, तो कोई इंसानी दिमाग़ की श्रेष्ठता को साबित करता हुआ। गुरु लोग पहले अध्यापकों में बदले थे, अब अध्यापक ज्ञान के माल के प्रोड्यूसर और सेल्समैन बन रहे थे। छात्रों के रूप में उनकी हालत इतनी खराब थी कि जिस दुकान पर जाते, लगता, दूसरी दुकान का माल बेहतर था।
उसके पिता ने कल ही हिसाब लगाया था कि उसकी ट्यूशनों पर अब तक कोई अस्सी हज़ार रुपया ख़र्च हो चुका था और अभी तीस-चालीस हज़ार और हो सकता था, इसके बावजूद कोई उम्मीद नहीं थी। निकल गये तो निकल ही गये, वरना..वरना हो सकता है, अरुणिमा की राह पर निकलने की नौबत आ जाये। बाजी जी जान की थी-न कम, न ज़्यादा। नंदन को शायद पैसे की इतनी फ़िक्र न थी। उसके पिता के पास काफ़ी पैसा था, लेकिन सब तो ऐसे नहीं थे ? नंदन को लगता था कि उसके पिता इसके लिए कसूरवार थे। उनकी इतनी ज़िद न रही होती तो शायद वह ऐसे कंपटीसन की राह ही न पकड़ता। पिता को वारिस चाहिए, एक क़ाबिल वारिस, जो उनकी प्रैक्टिस संभाल सके। लेकिन उनका वारिस हो सकने की क़ीमत कितनी बड़ी थी ? उसे लग रहा था जैसे अरुणिमा उसके भीतर कहीं, शायद दृष्टि नाड़ी के पीछे मध्य मस्तिष्क के किसी कोष में, उतर कर आसन ज़माये बैठी है। वही काले रंग की साड़ी, छोटी सी अर्ध चंद्राकार मैरून बिंदी, मछलीनुमा छोटे छोटे टॉप्स, पीछे की तरफ़ पूरी ताक़त से खींच कर बांधे गये बाल..कितनी खुश, कुछ गुनगुनाती हुई, बेफ़िक्र शरारती...
वर दे, वीणावादिनी वर दे..प्रार्थना ख़त्म होने जा रही थी। उससे थोड़ा आगे खड़ी उसकी क्लासफेलो आयशा ने पीछे मुड़ कर देखा। अरुणिमा का चेहरा उसके साथ गड्ड-मड्ड हो गया। वह चीखा, ‘काली साड़ी में अरुणिमाऽऽऽ!’’ आयशा भयभीत बदहवास सी और जोर से चीख़ पड़ी, ‘अरुणिमा..काली साड़ीऽऽऽ!’ पीछे पीछे लगभग सारी छात्राएं चीख़ने लगीं। आयशा ने भागना शुरू कर दिया। सब तरफ़ सारे छात्र-छात्राएं एक दूसरे को धकेलते-गिराते सब सब के ऊपर से कूदते-फ़लांगते आत्मरक्षा में जाने कहां कहां हो लिये ! चार-पांच छात्राएं नीचे गिरने की वज़ह से कुचली गयीं। अध्यापक उन्हें नियंत्रित करने की असफ़ल कोशिश करने लगे। प्रिंसिपल ने प्रार्थना करती छात्राओं से माइक पकड़ कर डांटने-डपटने के सुर में चीख़ना शुरू कर दिया। कोई असर नहीं। जिसे जिधर ज़गह मिलती, उधर, उस दिशा में कहीं जा कर समा जाता। कोई दस-पंद्रह मिनट बाद हालात काबू में आ गये। नीचे गिरी छात्राएं ज़ख्मी हो गयी थीं। एक की बांह हड्डी टूट जाने से फूल रही थी। एक के दांतों से खून बह रहा था। बाकी दोनों सिर थामे घुटने समेटे उकड़ूं हुई बैठी थीं। उनके उपचार के लिए प्रिंसिपल ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था।
उधर कुणाल पूछ रहा था नंदन से, ‘‘आख़िर हुआ क्या था ?’’
जवाब में नंदन कुछ पल ख़ामोश रह कर बोला था, ‘‘शायद मुझे ही कुछ हो गया था।’’
‘‘रात को देर तक पढ़ता रहा क्या ?’’
‘‘नहीं, रोज़ की तरह एक-डेढ़ बजे सो ही गया था।’’
‘‘सुबह फिर ज़ल्दी उठ गया होगा। एकाध दिन ऑफ ले कर आराम क्यों नहीं करता घर पर ?’’
‘‘एकाध दिन ?...घर पर दिन में भी कभी एक-दो घंटे नींद ले लो तो मम्मी नाराज़ होने लगती हैं। छह घंटे यहां कालेज़ खा लेता है, चार घंटे ट्यूशन, एक घंटा खाने-पीने और तैयार होने का, अब बाकी जो बचता है उसमें एक दो घंटे सो जाऊं तो पढ़ूँगा कब ?’’
‘‘मुझे लगता है, ट्यूशन का फायदा है तो सही, पर इतना नहीं।’’
‘‘भेड़ चाल है, पर क्या करें ? छोड़ दें तो वैसे जी घबराने लगता है कि पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं ! अब क्या करूँ ? इस वक्त भी सिर ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है। क्लासेज़ नहीं लगा सकूंगा आज।’’
‘‘तू बैठ, मैं करता हूं कुछ इंतज़ाम। नहीं तो एक बजे से पहले निकलने नहीं देगा कोई यहां से।’’
कुणाल गया, वाइस प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन ले कर नंदन को उसके घर छोड़ आया। वह अकसर उसके घर आता-जाता रहता था। उसके घर के हालात ऐसे थे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज की फ़ीस दे सकता था। जो था, जितना था, उतना भी उसके लिए काफ़ी था। नंदन उस पर मेहरबान था, सो उसे उससे उसकी ट्यूशन के नोट्स और टेस्ट वग़ैरह मिल जाते थे। ट्यूशनें न करने का उसे उलटा दोहरा फ़यदा हो रहा था।
इससे उसे सेल्फ स्टडी के लिए क़ाफ़ी वक़्त मिल जाता था, और साथ ही बने-बनाये नोट्स भी। लेकिन चाहे जो हो, नंदन का मुक़ाबला करना उसके बस की बात न थी। जिन सरकारी स्कूलों में वह पढ़ा था, उनके और नंदन के अंग्रेज़ी स्कूलों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ था। फिर घर पर न माहौल था और न उतनी सुविधाएं, लेकिन इस सबके बावजूद उसके नंबर अच्छे आते थे। इसकी वजह शायद यह थी कि वह वाकई कुछ सीखना चाहता था-कुछ नया, कुछ ज़रूरी, जो आदमी के लिए सचमुच मायने रखता हो, वही उसकी भीतरी प्यास को बुझाने की सामर्थ्य रखता था। बारहवीं कक्षा के छात्र से ऐसी प्यास की उम्मीद करनी बेतुकी थी, लेकिन वह थी ज़रूर। इतनी साफ़ तो नहीं, पर कहीं गहरे अवचेतन-अमूर्त रूप में वह मौजूद थी। इस मौजूदगी की एक वजह, एक इतिहास भी था।
कुणाल के पिता धर्मचंद औरतों की बैलियां डिज़ाइन करने के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। घर के छोटे से ड्राइंगरूम को उनकी दुकान में बदल जाने के बाद अब उनके छोटे से घर में एक कमरा और रसोई जितनी जगह ही बची रह गयी थी। छत पर एक ओर पाखाने का इंतज़ाम था, तो दूसरी तरफ ख़ुद ही एंगल आयरन खड़े कर ऊपर डाली टीन की छत वाली एक मियानी थी। वहां कुछ चारपाइयां, गोल किये बिस्तर और टूटा-फूटा सामान पड़ा रहता था। एक तरह से यही कुणाल का स्टडी रूम भी था। सो एक लिहाज से वह ख़ुशक़िस्मत था कि अपनी बिरादरी वालों की तुलना में कम से कम उसके पास एक ऐसी जगह ज़रूर थी, जो उसे पढ़ने के लिए तन्हाई दे सकती थी। पिता ज़्यादातर नीचे अपनी दुकान पर बैठे काम करते रहते। मां सुबह का नाश्ता बना कर जो काम पर निकलती तो उसके लौटने का कोई ठिकाना न होता। वह नजदीक के किसी गांव के सरकारी हेल्थ सेंटर पर दाई का काम करती थी।
वहां उसे काफ़ी काम प्राइवेट तौर पर भी मिल जाता था, सो लंच का कोई ठौर-ठिकाना न था। दोपहर के लिए एक सब्जी या दाल वह बना जाती और आटा गूंथ कर रख देती। अपने लिए वह दो रोटियां बना कर साथ ले जाती। अब पीछे बाप-बेटे में से जिसे भूख लगती या जिसके पास जब वक़्त होता, तो अपनी अपनी रोटी ख़ुद बना कर तवे पर सेंक लेते। इस मामले में कोई किसी पर निर्भर न रहता और न ही कोई किसी की फ़िक्र ही करता। जिसे जिंदा रहना हो, रोटी उसे ही पकानी पड़ती। कुणाल के लिए यह बात उतनी परेशानी की नहीं थी, जितनी यह कि कभी-कभार उसे भी अपने पिता की जगह दुकान पर बैठना पड़ता। वैसे वहां कम ही ग्राहक आया करते थे, यह दुकान जानकार लोगों की ग्राहकी पर चलती थी। जिन्हें धर्मचंद के हुनर का पता था, वही यहां औरतों के पैरों का नाप देने आते। कुछ दूसरे दुकानदार भी धर्मचंद को अपने आर्डर दे जाते थे, लेकिन उनसे बनवायी पूरी वसूल नहीं होती थी, सो धर्मचंद की ज़्यादा रुचि सीधे ग्राहकों में ही रहती। पिता की गैरमौजूदगी में कुणाल वहां बैठता तो भी वह कुछ ज़रूर पढ़ ही लेता था, लेकिन चलती सड़क की वजह से एकाग्रता उतनी नहीं हो पाती थी। वह इसे नापसंद करता था, पर मज़बूर था।
दुकान ज़्यादा देर खाली छोड़ देने पर ग्राहकी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता था। वैसे इस बात को नापसंद करने की सिर्फ़ यही एक वजह नहीं थी। एक और वजह भी थी, जिसे ले कर वह मन ही मन बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। इसका ताल्लुक उसके पिता की एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि से था। इसका पता उनकी बिरादरी में लगभग सभी लोगों को था। कई लोग इस वजह से धर्मचंद का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन वह हंस कर टाल जाता था। कुणाल सोचता कि अगर उसके पिता में यह खराबी न होती तो उनका बिजनेस कमाल का होता। वैसे कहीं गहरे में वह अपने पिता से थोड़ा सहमत भी हो जाता और तब...तब उसे अपने आपसे, अपने खानदान से, अपनी बिरादरी के छोटेपन और मजबूरियों से नफ़रत होने लगती। तब वह सोचता कि वह ज़्यादा देर उनका हिस्सा बन कर नहीं रहेगा। वह इन सब के कहीं पार निकल जायेगा-अपनी मां की तरह, अपनी मां से कहीं बेहतर तरीके से, क्योंकि वह अपनी मां की तुलना में ऐसा करने में ज़्यादा समर्थ हो सकता है...और यह सब सोच कर उसमें कुछ जानने, कर दिखाने की आग सी जलने लगती। उसकी अंदरूनी प्यास का स्रोत खुद उसके पिता थे और आज भी वह वही सब दोहराने जा रहे थे।
नंदन की अस्वस्थता की वजह से कुणाल जल्दी लौट आया था। उसके पिता उसे देख कर एकदम खुश हो गये।’’ अच्छा हो गया जो तू आ गया। सोच रहा था, किसे दुकान पर बिठा कर निकलूं। वो वाली नयी बैली बिक गयी है। ऐसा डिजैन बनाया था कि वो औरत उसे पहनते ही जैसे ज़मीन से एक हाथ ऊपर चलने लगी। तू देखता तो कहता..कौन सा शोरूम है इस शहर का जो उसके मुक़ाबले की बैली रखता हो। एकदम मुलायम। अंदर चारों तरफ़ जो फर लगायी थी, ज़रा ज़रा सी बाहर जो झलक रही थी। वो औरत कहने लगी, इंपोरटेड लगती है एकदम !’ जी ख़ुश हो गया। ले, बैठ अब सामान लाना है। तीन और आर्डर आये पड़े हैं। कल तक निपटा लूंगा किसी न किसी तरह।’
कुणाल बिना कुछ बोले शर्मसार वहीं बैठ गया। उसे पता था कि अब उसके पिता रात से पहले शायद ही लौटेंगे। वह कल्पना कर रहा था कि अब वे मुख्य सड़क पार करके पतली गली में दाखिल हो गये होंगे। फिर उन्होंने अपनी टोपी को जेब से निकाल कर सिर पर रख लिया होगा। अब वे रुके होंगे-दूसरी जेब से चश्मा निकाल कर उसे साफ करने के लिए। यह दूर की नजर के लिए था। चेहरे पर इतनी तबदीलियाँ काफ़ी थीं और अब वे खुद को महफ़ूज समझ रहे होंगे कि उन्हें बहुत जानकार लोगों के सिवाय कभी कभार मिलने वाले आसानी से पहचान नहीं पायेंगे। अब वे एकदम दूसरे आदमी हो गये थे। अब उन्हें किसी तरह की जवाबदेही की, मान-अपमान की ज़्यादा चिंता नहीं रही थी।
कुणाल यह सब ब्यौरेबार इसलिए जानता था, क्योंकि आस-पड़ोस और खुद अपनी मां से अपने पिता की बुराई सुन कर उसने एक दिन उनका पीछा किया था। उन सबके मुताबिक वे आवारागर्द थे। शहर की ऊंची जातियों की महिलाओं का पीछा करते थे। इस सबका मतलब यह था कि उनका चाल-चलन ठीक नहीं था। कुणाल के लिए इस पर यकीन करना सहज संभव नहीं था। लेकिन जब पिता का पीछा करते हुए उसने उनकी वे हरकतें देखीं तो वह पेरशान होने लगा। उस दिन उसने देखा कि चेहरा-मोहरा थोड़ा बहुत बदल लेने के बाद उन्होंने अपने पर्स से डायरी निकाली थी, जिस पर आम तौर पर वे अपने ग्राहकों के पैरों का नाप लेने के बाद उनके पते-ठिकाने नोट किया करते थे। इसके बाद वे एक पॉश लोकेलिटी की बड़ी सी कोठी के बाहर एक पेड़ की छाया के नीचे यूं उकड़ूं हो कर बैठ गये थे, जैसे कोई बेहद थका-मांदा आदमी ज़रा देर को दम मारने के लिए बैठ गया हो ! वहां के आधेक घंटा बैठे रहे।
फिर अचानक उस कोठी से किसी औरत के निकलने के बाद वे चौकन्ने हो गये। उनकी आंखों में जाने कैसी दैवी चमक सी आ गयी। वह औरत बाहर निकली, फिर बाहर पार्क की गयी अपनी कार में बैठ कर जाने कहां चली गयी। इसके बाद वे उठे और वहां जा कर कुछ तलाशने लगे, जहां अभी अभी वह कार खड़ी हुई थी, फिर उन्होंने जमीन को हथेलियों से छू छू कर आंखों को लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे उठे और उस दिशा में चल पड़े जिस ओर उस कार में बैठी हुई महिला आगे जा कर गायब हो गयी थी। कुणाल ने देखा था कि उसके पिता उस वक़्त अपने आप में नहीं थे। उनकी आँखें किसी अद्भुत प्रकाश से भरी हुई थीं और चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसे कोई आदमी अभी अभी समाधि लगा कर उठा हो ! कुणाल को अपने पिता पर तरस भी आया, ख़ुद में शर्म भी महसूस हुई लेकिन वह अपने पिता से नफ़रत नहीं कर पाया। उससे रहा नहीं गया और फिर वह अचानक आगे बढ़ कर उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। जिस्म से गर्मी फूट रही थी। वह कुछ पूछना चाहता था, पर उसके पास कोई लफ़्ज कहां थे। कुणाल के पिता ने उसे देखा, रुके, फिर हंस दिये, जा जा कर अपनी जिंदगी बना, कुछ पढ़-लिख। मेरे पीछे वक़्त क्यों बरबाद करता है ?’
कुणाल के पैर ज़मीन से जैसे पत्थर बन कर चिपक गये थे। वह किसी बेजान बुत की तरह था लेकिन इस तरह कांप रहा था, जैसे कि नीचे भूचाल आ जाने से धरती ही कांप रही हो। पिता फिर हंसे, फिर उन्होंने बेटे को छू कर प्यार किया और इशारा करके अपने साथ नीचे ज़मीन पर बैठने को कहा। इसके बाद उनकी आंखें आधी मुंद गयीं और वे ख़ुद में डूबे डूबे गंभीर आवाज़ में बोलने लगे, ‘‘मैं औरतों की जूतियां बनाता हूं। वो मेरा धरम है, रोज़गार है। पर मैं सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए ही जूतियां नहीं बनाता। मैं उनमें ख़ुद को डाल देता हूं। एक एक जूती मेरी सांसों को, मेरी धड़कनों को, मेरे जिस्म में डोलते लहू की हरकतों को ख़ुद में संजोये रहती है। मैं तब तक उसे नहीं सींता जब तक कि अपने जिस्म से हाथ भर ऊपर न उठ जाऊं और फिर एक दिन कोई न कोई औरत आती है, चार पैसे फेंक कर समझती है कि उसने उसकी कीमत चुका दी।
मैं हंस कर, जो मिलता है, ले लेता हूं, पर ज्योंही वो जूती मेरी दुकान से बाहर जाती है, मुझे लगता है, कोई मुझे अधमरा करके छोड़ गया है। फिर मेरा वहां दिल नहीं लगता। मैं अपनी जूती का पीछा करने निकल पड़ता हूं। जब जवान था तो लोग ये समझ कर कि मैं उन औरतों के पीछे जाता हूं, मेरी पिटाई भी कर देते थे। पर मैं उन्हें क्या बताता, क्या समझाता ? मार खा लेता, फिर चुपचाप लौट आता। अब मैं अपनी शकल बदल लेता हूं। अब लगता है जैसे कि मैं बूढ़ा भी हो चला हूं, तो अब लोग मजाक उड़ा कर छोड़ देते हैं, मारते-पीटते नहीं। पर मैं क्या करूं ? मजबूर हूं। मैं अपनी जिंदगी से पराया हो के कैसे जीऊं ? जब तक मुझे अपनी वही जूती पहने वह औरत दिखायी नहीं देती, जब तक मैं उसे इस वजह से ख़ुश नहीं देख लेता और जब तक उस ज़मीन को चूम कर उसकी मिट्टी अपनी आंखों से नहीं लगा लेता, मेरी देह में प्राण लौटते ही नहीं। क्या करूँ ? तेरी मां भी मुझे कभी समझ नहीं पायी। तू ही बता देना उसे कि मुझे दूसरी औरतों से कुछ लेना-देना नहीं...’।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book