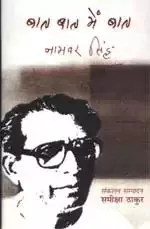|
भाषा एवं साहित्य >> बात बात में बात बात बात में बातनामवर सिंह
|
315 पाठक हैं |
||||||
संवाद कहिए या बातचीत- उसका यह दूसरा संकलन है। इसमें 1993 से 2005 तक के कुल 14 संवाद संकलित है...
Baat Baat Mein Baat a hindi book by Namvar Singh - बात बात में बात- नामवर सिंह
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मैं अपने तईं मानता हूँ कि आलोचक को दो भूमिकाएँ निभानी चाहिए। आलोचक वही काम करता है जो फौज में, जिसे ‘सैपर्स एण्ड माइनर्स’ करते हैं, इंजीनियर करता है। फौज के मार्च करने से पहले झाड़-जंगल साफ करके नदी-नाले पर जरूरी पुल बनाते हुए फौज को आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करने का जोखिम उठाए, सड़क बनाए। साहित्य में इस रूपक के माध्यम से मैं कहूँ कि जहाँ विचारों, विचारधाराओं, राजनीतिक सामाजिक प्रश्नों आदि के बारे में उलझनें हैं, वह अपने विचारों के माध्यम से थोड़ा सुलझाए, कोई बना-बनाया विचार न दे ताकि रचनाकारों को स्वयं अपने लिए सुविधा हो। ये मैं आलोचक के लिए ‘सैपर्स एण्ड माइनर्स’ की भूमिका मानता हूँ क्योंकि आगे-आगे वही चलता है और पहले वही मारा जाता है। दुश्मन आ रहा है तो जोखिम उठाने के लिए सबसे पहले मोर्चे पर वही बढ़ता है और ज़ख्मी होने का ख़तरा भी वही उठाता है। यह काम आलोचक करता है और उसे करना भी चाहिए।
क्योंकि हम रचनाकारों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक काम हुआ। दूसरा, रास्ता बनाने के साथ ही वह उनके साथ-साथ चलता भी है। वह रचनाकार का सहचर है। इसलिए आलोचक को ‘सहृदय’ कहते हैं। समान हृदय वाला। आलोचक को किसी की आलोचना करने से पहले उसी भावभूमि पर होने चाहिए जिस भाव भूमि पर पहुँचकर रचनाकार रचना कर रहा है। गुण दोष बाद में देखना चाहिए। लेकिन जिस लहर मान पर वह है, आप मन से वहीं पहुँचे। और वहीं पहुँचकर देखें कि सचमुच वो कहाँ है ? कहाँ से बोल रहा है ? निराला जी के शब्दों में वह किस कोठे से बोल रहा है ? इसलिए आलोचक-कर्म जो है मूलतः सहृदय का है।
आलोचक न्यायाधीश नहीं है। है तो वह वकील और ऐसा वकील जो सफाई पक्ष का है, ‘डिफेंस’ का है मुख्य रूप से, और डिफेंस का ऐसा ईमानदार वकील जो अपना केस लेकर आने वालों को सब बता देता है कि तुम्हारा केस कमजोर है; कहाँ हो ? कैसे हो ? बावजूद इसके वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि हम रचनाकारों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यह एक काम हुआ। दूसरा, रास्ता बनाने के साथ ही वह उनके साथ-साथ चलता भी है। वह रचनाकार का सहचर है। इसलिए आलोचक को ‘सहृदय’ कहते हैं। समान हृदय वाला। आलोचक को किसी की आलोचना करने से पहले उसी भावभूमि पर होने चाहिए जिस भाव भूमि पर पहुँचकर रचनाकार रचना कर रहा है। गुण दोष बाद में देखना चाहिए। लेकिन जिस लहर मान पर वह है, आप मन से वहीं पहुँचे। और वहीं पहुँचकर देखें कि सचमुच वो कहाँ है ? कहाँ से बोल रहा है ? निराला जी के शब्दों में वह किस कोठे से बोल रहा है ? इसलिए आलोचक-कर्म जो है मूलतः सहृदय का है।
आलोचक न्यायाधीश नहीं है। है तो वह वकील और ऐसा वकील जो सफाई पक्ष का है, ‘डिफेंस’ का है मुख्य रूप से, और डिफेंस का ऐसा ईमानदार वकील जो अपना केस लेकर आने वालों को सब बता देता है कि तुम्हारा केस कमजोर है; कहाँ हो ? कैसे हो ? बावजूद इसके वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं।
नामवर सिंह
दो शब्द
संवाद कहिए या बातचीत- उसका यह दूसरा संकलन है। इसमें 1993 से 2005 तक के कुल 14 संवाद संकलित हैं। सभी संवाद किसी न किसी पत्रिका या पुस्तक में पहले प्रकाशित हो चुके हैं। इस दौर के कुछ प्रकाशित संवाद और भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो सहज सुलभ हो गए वही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रस्तुति के विषय में सूचनार्थ निवेदन है कि फीते से कागज़ पर उतारते समय बातचीत में जहाँ स्खलन और अस्पष्टता दृष्टिगोचर हुई वहाँ वार्ताकार से परामर्श करके पाठ को सम्पादित कर दिया गया है। वार्ताएँ कालक्रम के अनुसार देने की अपेक्षा बहुत कुछ विषयानुसार संयोजित की गई हैं।
अंत में वार्ता में भाग लेने वाले सभी साहित्यकार बंधुओं और पहली बार प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं के सामान्य संपादकों के सौजन्य के प्रति हार्दिक आभार।
अंत में वार्ता में भाग लेने वाले सभी साहित्यकार बंधुओं और पहली बार प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं के सामान्य संपादकों के सौजन्य के प्रति हार्दिक आभार।
समीक्षा ठाकुर
वाचिक विमर्श क्यों ?
(आशुतोष दुबे और रवीन्द्र व्यास के साथ)
वैसे तो हिन्दी में विवादास्पद होने को विरुद की तरह बरता जाता है लेकिन नामवर सिंह शायद हिन्दी साहित्य के अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका बोलना-और न बोलना भी-नित नए विवादों को जन्म देता रहता है। हिन्दी परिदृश्य में उन्हें दुर्लभ केन्द्रीयता हासिल है। अरुण कमल के शब्दों में, ‘‘पूरे वातावरण को स्फूर्ति से भरे हुए, जाफरान की खुशबू से तर किए, भोर की तन्द्रा को दोपहर की गहमागहमी में बदलते, आपको हमेशा अपने चौबों पर तैयार रहने को बाध्य करते, बेचैनी और तड़प से भरते द्वन्द्व के लिए ललकारते कभी निःशास्त्र करते, कभी वार चूकते-डॉ. नामवर सिंह हमारे सबसे बड़े संवादक रहे हैं।’’ ऐसे संवादक से एक चमकीली सुबह में आवेग के लिए संवाद करते हुए कोशिश रही कि बातचीत आलोचना पर एकाग्र हो; लेकिन बात निकली तो फिर उसे दूर तक-वह भी अनेक वीथियों-से जाना ही था...
प्रश्न : नामवर जी, वे कौन सी स्थितियाँ, कारण या मनोदशाएँ रही हैं कि आपने लिखने की अपेक्षा बोलने को ही आलोचना का माध्यम बना लिया। क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगा कि इससे आलोचना का भी नुकसान हुआ और व्यक्तिगत रूप से आपका भी या साहित्य का भी?
नामवर सिंह : यह मेरी विवशता है कि पिछले कुछ वर्षों से बोलने का काम अधिक कर रहा हूँ, उसकी तुलना में लिखने का कम। और इससे साहित्य का क्या बना-बिगड़ा ये तो दूसरे जानते होंगे लेकिन मेरी दृष्टि में, बहुत सी बातें हैं जो सुरक्षित नहीं कही जा सकतीं; जिसे जीवन की अन्तिम घड़ी में कह सकूँ कि ये कुछ छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिथ गढ़ते है। किंवदंती एक गढ़ दी गई है कि ये तो बोलते हैं, लिखते नहीं ! और उसका एक तर्क भी ढूँढ़ लेते हैं कि बोलने से जुबान नहीं कटती है, लिखने से हाथ कट जाते हैं। आप लिखते इसलिए नहीं कि लिखने से आपका एक कमिटमेंट हो जाता है। बोलने में आप अपनी बात बदल सकते हैं, मुकर सकते हैं। उस ब्यौरे में जाने से पहले मैं यह कह दूँ कि गोष्ठियों में मैं बोलता रहा हूँ, अखबारों में उसकी सही गलत रिपोर्टिंग भी होती है और मैंने उसमें किसी बात का खण्डन नहीं किया क्योंकि राजनीतिज्ञों की जवाबदेही एक खास तरह की होती है; बल्कि फैशन भी है-राजनीतिज्ञ कहकर मुकर जाते हैं, लेकिन साहित्य में मैं यह मानकर चलता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा, रिपोर्ट करने वाले ने जैसा समझा उसने लिख दिया। इसका मतलब है कि मेरी बात इसी रूप में पहुँची होगी उस तक, उसने वही समझा होगा और हो सकता है बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें रिपोर्टिंग में छूट भी गई होंगी।
साहित्य में यह चल सकता है, राजनीति में यह नहीं चलता। लेकिन लोग साहित्य को भी मानते हैं कि उसी तरह का राजनीतिक वक्तव्य है। जो महत्त्वपूर्ण बातें किसी लेखक के बारे में या कृति के बारे में मैंने कहीं, उससे मुकरने का सवाल ही नहीं उठता। आज तक मैंने अपने किसी दिए हुए वक्तव्य के बारे में यह नहीं कहा कि मैंने यह नहीं कहा। दूसरा कारण यह भी है कि बोलने के बारे में कह रहा हूँ-लोग यह भूल जाते हैं कि मैं अध्यापक हूँ और क्लास में कुछ निश्चित विषय पढ़ाता रहा हूँ और उसके नोट्स भी लिए जाते रहे हैं। विदेशों में यह होता है कि कुछ लोगों के क्लास लेक्चर्स को ही उनके शिष्यों ने पुस्तक के रूप में छपाया। फरदीनांदों सस्योर की एक किताब है। 1916 में उनके दो शिष्यों ने नोट्स लिए थे, उनके मरने के पचास साल बाद प्रकाशित किए। हमारे यहाँ यह परम्परा नहीं है। और लोग होंगे, मैं सभी अध्यापकों के बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने जोधपुर में चार साल तक क्लास लेक्चर्स दिए। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी में 1974 से 1992 तक मैंने व्याख्यान दिए। कम ही विद्यार्थी होते थे। मैं लगातार दो पीरियड लेता था। तो ये व्याख्यान मेरे विद्यार्थियों के पास होंगे। इसलिए अब लोगों को गोष्ठियाँ दिखाई पड़ती हैं कि मैं बोलता हूँ; उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि जिन्दगी में तीस साल बोलता ही रहा हूँ। और जितना बोला उतना सब लिखा तो नहीं है।
तीसरी बात, इसके अलावा ये कि लिखने के कारण होते हैं, उद्देश्य होते हैं। मैंने ‘आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ’ एक किताब लिखी। ‘छायावाद’ किताब लिखी। एक ही साल में 1954 में ये लिखीं और कुछ लेख भी लिखे। तो रचनाकाल देखें और पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष देखें तो 1955, 56, 57 में मेरी इकट्ठी पाँच किताबें आईं। आगे चलकर आप देखेंगे कि रफ्तार कम हो गई। तब भी मैं गोष्ठियों में जाता था, तब भी मैं पढ़ाता था। ‘कहानी, पत्रिकाओं के लिए लिखा। उसके काफी वर्ष बाद ‘कविता के नए प्रतिमान’ लिखी और उसके बाद 1982 में ‘दूसरी परम्परा की खोज’ लिखी। इस बीच आलोचना में मेरे अनेक लेख प्रकाशित हुए। उनमें से कुछ लेख मैंने वाद विवाद संवाद’ (1991) में प्रकाशित किए जबकि उसके कुछ लेख मैं पहले ही लिख चुका था। इसके अलावा कम-से-कम सौ लेख पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं किए।
पुस्तक के रूप में प्रकाशन करने के लिए कुछ लोग हर साल, हर महीने दनादन, दनादन किताबें निकालते रहते हैं। अपना ये कभी स्वप्न नहीं रहा। आलोचना मैंने हिन्दी में हस्तक्षेप के रूप में की है। जहाँ जरूरी लगा कि साहित्य में जो चल रहा है, उसमें मैं हस्तक्षेप करूँ, बदलूँ, साहित्य की किसी धारा को या प्रवृत्ति को। कोई नई चीज उभर रही है और उसकी उपेक्षा हो रही है तो उस पर बल दूँ। सार्थक आलोचना वही होगी। वर्ना केवल ग्रन्थों को प्रकाशित करते जाने और लायब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए आलोचना नहीं की। मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने साहित्य में, अपनी संस्कृति में और समाज में साहित्य-सम्बन्धी क्या सोच विचार चल रहा है, उसको कैसे बदला जा सके, उसको समृद्ध किया जाए। यह एक काम है और यह बोलकर भी किया जा सकता है और लिखकर भी किया जा सकता है। मैंने केवल वक्तृत्व कला के मामले में ये नहीं कहा, हाँ, मैंने कहा था कि जिस समाज में साक्षरता 50 फीसदी से भी कम हो, हिन्दी समाज में, वहाँ वाचिक परम्परा के द्वारा ही महत्त्वपूर्ण काम किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी आलोचना को, मेरे बोले हुए को-मौखिक आलोचना को आप लोक-साहित्य मान लीजिए।
एक उदाहरण देता हूँ। मैं पटना में एक गोष्ठी में गया था। पटना में कामरेड रामजी राय जन संस्कृति मंच के प्रखर प्रतिनिधि हैं-उन्होंने कहा कि आपने किसी साक्षात्कार में कहा था-मार्क्स के भी अंध-बिन्दु हैं। तो अंध-बिन्दु से आपका क्या आशय है और मार्क्स में आप क्या अंध-बिन्दु देखते हैं ? जवाब से पहले मैंने कहा कि हे तात ! अभी आपने किसी इण्टरव्यू में पढ़ लिया है तो आपको याद है ‘वाद-विवाद- संवाद’ के अन्त में जो सूत्र दिए गए हैं। उसमें यह बात मैं 1991 में कह चुका हूँ दस साल पहले। तब आपने यह नहीं पूछा और किसी ने नहीं कहा। अब साक्षात्कार में कह दिया तो आप उसका हवाला दे रहे हैं, जबकि यह बात मैं दस साल पहले लिख चुका हूँ। तो ये लोग जो शिकायत करते हैं वो हमारे लिखे हुए को तो पढ़ते नहीं हैं और बोले हुए पर बहस करते हैं।
इस प्रकरण पर ज्यादा बोल गया मैं; लेकिन जैसे-जैसे आदमी परिपक्व होता है, एक खास उमर में आप जितनी गति से लिखते हैं, बाद में सोच-विचार, अनेक सन्देह शंकाएँ पैदा होती हैं। मैं यह मानता हूँ कि आलोचना को उतना ही सुलिखित होना चाहिए जैसे कि कविता, कहानी या उपन्यास। मैं चाहता हूँ कि मेरे विचारों से जो असहमत हों, वे भी कम से कम गद्य को तो पसन्द करें क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं इस भाषा में लिख रहा हूँ जिसमें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का गद्य मेरे सामने है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का गद्य मेरे सामने है, सरलता और सहजता में रामविलास शर्मा का गद्य मेरे सामने है। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक डायरी का गद्य मेरे सामने हैं। लोगों को नहीं मालूम है, पुस्तक लिखने में मुझे कम समय लगा है, एक लेख लिखने में पुस्तक लिखने से ज्यादा लगता है; यह नहीं मालूम लोगों को। मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं-एक हफ्ते या दस दिन में लिखी हैं। लिखने के पहले सारी सामग्री इकट्ठा कर लेता हूँ।
लिखते समय कभी-कभी अपने नोट्स देख लेता हूँ। बस। ‘छायावाद’ पुस्तक मैंने कुल दस दिन में लिखी। ‘कविता के ने प्रतिमान’ इक्कीस दिन में लिखी हुई किताब है। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ दस दिन में लिखी हुई किताब है। बाकी कुछ लेख धारावाहिक या अन्तराल के साथ दस दिन में लिखी हुई किताब है। बाकी कुछ लेख धारावाहिक या अन्तराल के साथ लिखित हैं। अभी ‘आलोचना’ में एक लेख मैंने रामविलास जी पर लिखा है-‘इतिहास की शव-साधना’। बहुत से लोगों की चिट्ठियाँ आई हैं। इस अकेले लेख को लिखने में सोचने में विचारने में कितना समय लगा, इसका अन्दाजा नहीं होगा लोगों को। पर लिखा तो रात दस बजे से शुरू कुया और सुबह दस बजे खत्म किया। मैं इसी तरह एक साँस में लिखता हूँ; उसमें बाधा नहीं आती और वह मेरे लिए एक साधना है। जो लोग शिकायत करते हैं, वही लोग मुझे बोलने के लिए बुलाते हैं। कई बार कहता हूँ कि भाई मुझे लिखने दीजिए। लिखने देते नहीं और शिकायत करते हैं। यह हालत हो गई है। अपना दुःखड़ा किससे रोएँ ?
प्रश्न : अपने एक पुराने साक्षात्कार में आपने कहा था जिस लेखक से आपके विचारों का मेल न हो उसका विरोध बेशक कीजिए लेकिन उसका साहित्यिक महत्त्व यदि कुछ है तो उसे स्वीकार कीजिए। आज के परिदृश्य में जबकि वैचारिक ध्रुवीकरण के चलते कट्टरताएँ बहुत बढ़ गई हैं, क्या आपको लगता है कि जिस सदाशयता को आपने कभी प्रस्तावित किया था, उसकी स्पेस–विशेषतः समकालीन साहित्यकारों में ही, जिसमें सभी लोग शामिल हैं; आप भी-कम होती जा रही है ?
नामवर सिंह : पहली बात तो यह है कि मैं अपने लिए यह सब मानता हूँ, तो दूसरे को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि, उदाहरण के लिए, मैं निर्मल वर्मा के विचारों से सहमत नहीं हूँ-विशेषतः वे विचार जो भारतीयता को लेकर हैं। मार्क्सवाद का वे विरोध करते हैं; मैं नहीं सहमत हूँ। लेकिन निर्मल वर्मा महत्त्वपूर्ण साहित्यकार हैं, इसको स्वीकार भी करता हूँ। यह कोई कुफ्र नहीं है। मार्क्स ने खुद बालज़ाक के बारे में कहा था कि उसके राजनीतिक विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन बालज़ाक बड़ा साहित्यकार है। लेनिन ने भी टायस्टॉय के बारे में ऐसा ही कहा है। गरज कि अपने भ्रामक विचारों के बावजूद एक साहित्यकार बड़ा साहित्यकार हो सकता है।
आलोचक के लिए यह बड़ा जटिल प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है ? उदाहरण के लिए तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े कवि हैं, इस बारे में दो राय नहीं। ये और बात है कि दलित लोग यह न मानें। लेकिन यह सही है कि वे वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते थे, उनके रामराज्य में वही व्यवस्था है। यही नहीं, बल्कि कबीर के बारे में उन्होंने कुछ तल्ख बातें कही हैं; लगभग गाली सी-दी है उन्होंने। भले ही यह कहा जाए कि उनके राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, लेकिन उन्होंने शंबूक वध की कहानी नहीं लिखी। सीता की महिमा गाई है लेकिन स्त्री के बारे में उनके विचार वही नहीं थे जो आज के स्त्रीवादी लोग मानेंगे। बावजूद इसके वे बड़े कलाकार हैं। तो साहित्य में ऐसा होता है। और इसका कारण यह है कि साहित्य में विचार के अलावा इन्द्रिय बोध भी होता है, भावबोध भी होता है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति सही बात कहे तो यह जरूरी नहीं है कि बहुत ही समाज-विरोधी और मानवद्रोही विचार किसी के हों और कलाकार भी बड़ा हो लेकिन उन विचारों के कारण उसके बड़प्पन में खरोंच तो आती है और कभी भी आती है। अगर वह न हो तो वह और बड़ा हो। दुनिया में अनेक ऐसे कलाकार हुए हैं। दार्शनिक भी हुए हैं-जैसे मार्टिन हाइडेगर फासिज्म के समर्थक थे, हिटलर की पार्टी के सदस्य थे और सदस्य ही नहीं बने थे, सदस्य बनकर युनिवर्सिटी के रेक्टर बने थे। बावजूद इसके हाइडेगर कई दार्शनिकों की दृष्टि में बहुत बड़े दार्शनिक हैं। अब फासिज्म से बढ़कर कोई मानव विरोधी दर्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन एक इतना बड़ा दार्शनिक हुआ। कई साहित्यकार ऐसे हुए हैं जर्मनी में, इटली में। अब ये गुत्थी सुलझाई जानी चाहिए और यह रचना प्रक्रिया के गहन विश्लेषण द्वारा ही जाना जा सकता है।
इसलिए मैं अपने लिए तो आचार-संहिता बना सकता हूँ कि जिससे असहमत हूँ, उसको सम्मान दूँ। अगर साहित्य में यह नहीं होगा तो इतनी एकरसता होगी, दोहराव होगा, तोतारटंत समाज हो जाएगा। इसलिए बौद्धिकता के लिए जरूरी है कि मतभेद को हम स्वीकार करें और सम्मान करें। मैं अपने लिए यह मानता हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारी हिन्दी की परम्परा में जो पहले के आलोचक रहे हैं वो इसे मानते रहे हैं। रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहिष्णु भी रहे हैं। उदाहरण के लिए कहूँ तो जब शीतयुद्ध का जमाना था-1950 से लेकर 1965 तक, इलाहाबाद में परिमल और प्रगतिशील लेखक संघ के बीच घनघोर वाद-विवाद होता था बल्कि मार्क्सवादी लेखकों के अन्दर भी पोलिमिक्स हुई है। तुलसीदास और रामचरितमानस को लेकर यशपाल और रामविलास शर्मा के बीच विवाद हुआ, लेकिन दुश्मनी नहीं थी। मिलते थे रोज़, गोष्ठियों में भी और बाहर भी। वहाँ विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर भारती इन लोगों के साथ बहस होती थी। कहा जाता है कि वादे-वादे जायते तत्त्वबोधः। अब यह कम हो रहा है। संकीर्णता की प्रवृत्ति कुछ बढ़ रही है और यह चिन्ता की बात है। जिसे आप ध्रुवीकरण कह रहे हैं, वह कोई ध्रुवीकरण नहीं है। ध्रुवीकरण तब होता है जब अपने विचारों पर आप दृढ़ हों और आपके पास विचार हों। राजनीति में कहाँ ध्रुवीकरण है ?
लगभग साहित्य की वही स्थिति हो गई है। जैसे कि एक तरफ सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष में है कांग्रेस। इनमें कोई वास्तविक ध्रुवीकरण नहीं है, नूरा कुश्ती चल रही है। साहित्य में भी इस तरह की बहुत नूरा कुश्तियाँ चल रही हैं। अगर सचमुच ध्रुवीकरण विचारों का होता तो मैं समझता हूँ, साहित्य में सम्बन्ध बेहतर होते। जहाँ स्पष्ट जानकारी हो कि विरोधी पक्ष का विचार क्या है, एक दूसरे के विचार को जहाँ समझते हों, फर्क साफ़ मालूम हो; तब संवाद की गुंजाइश रहती है। जब मैं समझूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप कहाँ खड़े हैं, तब बात हो सकती है। बात तब नहीं होती जब पता नहीं चलता कि सचमुच आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ। इसलिए ध्रुवीकरण नहीं है। यदि सच्चा ध्रुवीकरण होता-उदाहरण के लिए भारत भवन वाले अशोक वाजपेयी और उनके सहयोगी हैं, जो समझते हैं कि प्रगतिशीलों ने तो, साहित्य को विचारधारा का उपनिवेश बना रखा है।
सवाल ये है कि खुद उन्होंने विचारों का अपना उपनिवेश बनाया है कि नहीं हम तो विचार के उपनिवेश हैं लेकिन आपके यहाँ विचार नाम का कोई देश है जो आपका उपनिवेश है ? आपके कुछ विचार हैं कि नहीं ! एक तरह से यह विचार शून्य साहित्य या साहित्य में विचार शून्यता का प्रचार है। ऐसी हालत में तो ध्रुवीकरण विचार और विचार-शून्यता के बीच है। मुक्तिबोध के शब्दों पार्टनर ! तुम अपनी पालिटिक्स तो बताओ ! बात तभी हो सकती है। अपनी राजनीति वो बताएँगे नहीं। क्यों नहीं बताएँगे यह हम जानते हैं क्योंकि बता नहीं सकते। तुलसीदास ने कहा है; ‘चोर नारी जिमि प्रकट न रोई।’ चोर की औरत रोने लगे तो यह मालूम हो जाएगा कि वह चोर की बीवी है। इसीलिए कुछ लोग अपनी राजनीति नहीं बताते क्योंकि बहुत असुविधाजनक होगा अपनी राजनीति बताना। एक पूरी सूची बनाई जाए और उनसे जवाब माँगा जाए तो निकल आएगा कि उनकी राजनीति क्या है। फिर भी दावा यही करते हैं कि वे सिर्फ शुद्ध साहित्य ही करते हैं। और दूसरे राजनीति करते हैं। कठिनाई यही है इसलिए क्या साहित्य में बात की जाए। ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुलता या बहुवचन की बात आप स्वीकार करते हैं।
भारतीय समाज में, सभी धर्मों, सभी भाषाओं के लिए, सभी विचारों के लिए जगह है, इसे ही लोकतन्त्र कहते हैं। इसलिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। वे समझते हैं कि हम लोग एक मत वाले हैं और बहुवचन और बहुलता आकर्षक शब्द हैं-स्वीकार कर लिया; लेकिन उनकी पत्रिका को देखिए। उस पत्रिका में वही आधे दर्जन, एक दर्जन नाम हैं जो हर अंक में दिखाई पड़ते हैं। यह कैसी बहुलता और कैसा बहुवचन है जिसमें एक छोटा-सा गुट है सब एक विचार के, एक ही भावबोध के, एक ही तरह की भाषा लिखने वाले, उन्हीं लोगों को बीस साल तक छापते आ रहे हैं-‘पूर्वग्रह’ से लेकर ‘बहुबचन’ तक और नाम लेते हैं बहुलता का। अब मैं क्या कहूँ ? तो एकवचनवादी बहुवचनवादी हो गए और हम लोग जो बहुवचनवादी हैं-हम लोगों को कहा जाता है-तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए संवाद कठिन है।
प्रश्न : दलित साहित्य को स्वीकृति देते हुए आपने अपने पूर्व कथन में, पूर्व निष्कर्ष में परिवर्तन को स्वीकार किया है। क्या आपके कुछ अन्य मतों में या निष्कर्षों में कोई और परिवर्तन आया है ? ऐसा परिवर्तन जो बहुत स्पष्टता से शायद व्यक्त न हो पाया हो ?
नामवर सिंह : कई चीजों में। राजेन्द्र यादव की शिकायत है कि नामवर में ‘कन्सिस्टेन्सी’ नहीं है। वे अपने विचार को बदलते रहते हैं। चिन्तन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि ये गुण है। वे समझते हैं कि दोष है। रचनात्मक साहित्य को देखिए। सृजन का धर्म ही है-नवाचार, पुनर्नवता। कुछ नया करना। नहीं तो यह सृजन नहीं है और आप अपने को ही दोहराते चले जा रहे हैं। निराला ने जो पहली कविता लिखी थी अगर वही कविता अन्त तक लिखते रहे होते तो उनमें और सुमित्रानन्दन पन्त में फर्क नहीं रह जाता। रामचन्द्र शुक्ल संचयन की भूमिका में मैंने लिखा है कि ‘कविता क्या है’ लेख उन्होंने 1909 में ‘सरस्वती’ में लिखा था उसे ‘विचार वीथी’ में 1930 में कितना बदल दिया। रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास जिस रूप में नागरी प्रचारिणी सभा से 1928 में छपाया था उसे 1941 में इतना बदल दिया।
आपने दलित साहित्य का नाम लिया। पहले मैं मानता था कि दलितों के बारे में जो भी साहित्य लिखा जाए उसे दलित साहित्य माना जाए, लिखने वाला चाहे गैर दलित हो या दलित।
प्रेमचन्द्र ने जो साहित्य लिखा उसमें दलित साहित्य भी है। लेकिन ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ और उनका कहानी संग्रह सलाम जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो उसके पहले मैं नहीं जानता था। मरे हुए बैल की खाल निकालने का काम और मरे हुए जानवर को उठाना और उसको कैसे पहुँचाना बाजार में। कैसे उस समाज में रहने वाले लोग-सूअर मारने वाली घटना है-कैसे अपनी जात छुपाते हैं। हम सवर्णों को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा। हम अपनी जात छुपाते नहीं बल्कि धड़ल्ले से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया हैं, हम जैन हैं। कोई शर्म नहीं मालूम होती और एक आदमी है जो अपनी जात छिपाता फिरता है। ये दर्द जब मैंने जाना, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे अनुभव हैं जो दलित-कुल में जन्म लेने के बाद ही कोई आदमी जान सकता है। इसलिए सच्चा दलित साहित्य तो वही होगा। इसका मतलब ये नहीं है जो भी दलित होगा वह श्रेष्ठ साहित्यकार भी होगा।
साहित्य में भी उत्तम-मध्यम जो भी दलित होगा वह श्रेष्ठ साहित्यकार भी होगा। दलित साहित्य में भी उत्तम-मध्यम है और स्वयं दलित लेखक भी जानते हैं कि एक स्तर की कविताएँ सभी दलित कवियों की नहीं है ! एक ही स्तर की कहानियाँ सभी दलित कहानीकारों की नहीं हैं। एक ही स्तर की आत्मकथाएँ भी नहीं हैं। तो मेरे विचार बदले हैं-मैंने यह ऐलानिया स्वीकार किया है। पहले मैं ये मानता था अब नहीं मानता। उदाहरण के लिए पहले मेरी धारणा थी कि एक ही परम्परा होती है और इस बात की खोज करने में 20-30 वर्ष लगे जब मुझे यह अहसास हुआ कि कोई और परम्परा भी है। जब मैं अपने गरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आया-तब मुझमें ये बोझ नहीं जागा। उनके देहावसान के बाद उन्हीं को फिर पढ़ने लगा तो अचानक फ्लैश की तरह दूसरी परम्परा का खयाल आया।
वे सारी बातें पहले बता चुके थे लेकिन तब मुझे नहीं सूझा कि हमारी भारतीय परम्परा में एक और परम्परा है और वह परम्परा विद्रोह, विरोध और प्रतिरोध की परम्परा है। यानी तुलसी और कबीर दोनों एक ही परम्परा के नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक ही परम्परा को माननेवाले अक्सर मुख्य धारा की बात करते हैं और इस तरह कुछ को हाशिए पर फेंक देते हैं। साफ है कि परम्परा का प्रश्न वर्चश्व से जुड़ा है और वही संघर्ष है। ऐसे भी दौर आते हैं कि जिसे आपने हाशिये पर डाल दिया है वह मुख्य धारा बन जाती हैं और मुख्य धारा हाशिये पर चली जाती है। अगर हम सचमुच ही मानते हैं कि इतिहास में वर्ग-संघर्ष रहा है तो वर्ण-संघर्ष भी रहा है। लगभग 1980 में ही मैं इस बात को समझ सका।
प्रश्न : नामवर जी, वे कौन सी स्थितियाँ, कारण या मनोदशाएँ रही हैं कि आपने लिखने की अपेक्षा बोलने को ही आलोचना का माध्यम बना लिया। क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगा कि इससे आलोचना का भी नुकसान हुआ और व्यक्तिगत रूप से आपका भी या साहित्य का भी?
नामवर सिंह : यह मेरी विवशता है कि पिछले कुछ वर्षों से बोलने का काम अधिक कर रहा हूँ, उसकी तुलना में लिखने का कम। और इससे साहित्य का क्या बना-बिगड़ा ये तो दूसरे जानते होंगे लेकिन मेरी दृष्टि में, बहुत सी बातें हैं जो सुरक्षित नहीं कही जा सकतीं; जिसे जीवन की अन्तिम घड़ी में कह सकूँ कि ये कुछ छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मिथ गढ़ते है। किंवदंती एक गढ़ दी गई है कि ये तो बोलते हैं, लिखते नहीं ! और उसका एक तर्क भी ढूँढ़ लेते हैं कि बोलने से जुबान नहीं कटती है, लिखने से हाथ कट जाते हैं। आप लिखते इसलिए नहीं कि लिखने से आपका एक कमिटमेंट हो जाता है। बोलने में आप अपनी बात बदल सकते हैं, मुकर सकते हैं। उस ब्यौरे में जाने से पहले मैं यह कह दूँ कि गोष्ठियों में मैं बोलता रहा हूँ, अखबारों में उसकी सही गलत रिपोर्टिंग भी होती है और मैंने उसमें किसी बात का खण्डन नहीं किया क्योंकि राजनीतिज्ञों की जवाबदेही एक खास तरह की होती है; बल्कि फैशन भी है-राजनीतिज्ञ कहकर मुकर जाते हैं, लेकिन साहित्य में मैं यह मानकर चलता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा, रिपोर्ट करने वाले ने जैसा समझा उसने लिख दिया। इसका मतलब है कि मेरी बात इसी रूप में पहुँची होगी उस तक, उसने वही समझा होगा और हो सकता है बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें रिपोर्टिंग में छूट भी गई होंगी।
साहित्य में यह चल सकता है, राजनीति में यह नहीं चलता। लेकिन लोग साहित्य को भी मानते हैं कि उसी तरह का राजनीतिक वक्तव्य है। जो महत्त्वपूर्ण बातें किसी लेखक के बारे में या कृति के बारे में मैंने कहीं, उससे मुकरने का सवाल ही नहीं उठता। आज तक मैंने अपने किसी दिए हुए वक्तव्य के बारे में यह नहीं कहा कि मैंने यह नहीं कहा। दूसरा कारण यह भी है कि बोलने के बारे में कह रहा हूँ-लोग यह भूल जाते हैं कि मैं अध्यापक हूँ और क्लास में कुछ निश्चित विषय पढ़ाता रहा हूँ और उसके नोट्स भी लिए जाते रहे हैं। विदेशों में यह होता है कि कुछ लोगों के क्लास लेक्चर्स को ही उनके शिष्यों ने पुस्तक के रूप में छपाया। फरदीनांदों सस्योर की एक किताब है। 1916 में उनके दो शिष्यों ने नोट्स लिए थे, उनके मरने के पचास साल बाद प्रकाशित किए। हमारे यहाँ यह परम्परा नहीं है। और लोग होंगे, मैं सभी अध्यापकों के बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने जोधपुर में चार साल तक क्लास लेक्चर्स दिए। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी में 1974 से 1992 तक मैंने व्याख्यान दिए। कम ही विद्यार्थी होते थे। मैं लगातार दो पीरियड लेता था। तो ये व्याख्यान मेरे विद्यार्थियों के पास होंगे। इसलिए अब लोगों को गोष्ठियाँ दिखाई पड़ती हैं कि मैं बोलता हूँ; उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि जिन्दगी में तीस साल बोलता ही रहा हूँ। और जितना बोला उतना सब लिखा तो नहीं है।
तीसरी बात, इसके अलावा ये कि लिखने के कारण होते हैं, उद्देश्य होते हैं। मैंने ‘आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ’ एक किताब लिखी। ‘छायावाद’ किताब लिखी। एक ही साल में 1954 में ये लिखीं और कुछ लेख भी लिखे। तो रचनाकाल देखें और पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष देखें तो 1955, 56, 57 में मेरी इकट्ठी पाँच किताबें आईं। आगे चलकर आप देखेंगे कि रफ्तार कम हो गई। तब भी मैं गोष्ठियों में जाता था, तब भी मैं पढ़ाता था। ‘कहानी, पत्रिकाओं के लिए लिखा। उसके काफी वर्ष बाद ‘कविता के नए प्रतिमान’ लिखी और उसके बाद 1982 में ‘दूसरी परम्परा की खोज’ लिखी। इस बीच आलोचना में मेरे अनेक लेख प्रकाशित हुए। उनमें से कुछ लेख मैंने वाद विवाद संवाद’ (1991) में प्रकाशित किए जबकि उसके कुछ लेख मैं पहले ही लिख चुका था। इसके अलावा कम-से-कम सौ लेख पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं किए।
पुस्तक के रूप में प्रकाशन करने के लिए कुछ लोग हर साल, हर महीने दनादन, दनादन किताबें निकालते रहते हैं। अपना ये कभी स्वप्न नहीं रहा। आलोचना मैंने हिन्दी में हस्तक्षेप के रूप में की है। जहाँ जरूरी लगा कि साहित्य में जो चल रहा है, उसमें मैं हस्तक्षेप करूँ, बदलूँ, साहित्य की किसी धारा को या प्रवृत्ति को। कोई नई चीज उभर रही है और उसकी उपेक्षा हो रही है तो उस पर बल दूँ। सार्थक आलोचना वही होगी। वर्ना केवल ग्रन्थों को प्रकाशित करते जाने और लायब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए आलोचना नहीं की। मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने साहित्य में, अपनी संस्कृति में और समाज में साहित्य-सम्बन्धी क्या सोच विचार चल रहा है, उसको कैसे बदला जा सके, उसको समृद्ध किया जाए। यह एक काम है और यह बोलकर भी किया जा सकता है और लिखकर भी किया जा सकता है। मैंने केवल वक्तृत्व कला के मामले में ये नहीं कहा, हाँ, मैंने कहा था कि जिस समाज में साक्षरता 50 फीसदी से भी कम हो, हिन्दी समाज में, वहाँ वाचिक परम्परा के द्वारा ही महत्त्वपूर्ण काम किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी आलोचना को, मेरे बोले हुए को-मौखिक आलोचना को आप लोक-साहित्य मान लीजिए।
एक उदाहरण देता हूँ। मैं पटना में एक गोष्ठी में गया था। पटना में कामरेड रामजी राय जन संस्कृति मंच के प्रखर प्रतिनिधि हैं-उन्होंने कहा कि आपने किसी साक्षात्कार में कहा था-मार्क्स के भी अंध-बिन्दु हैं। तो अंध-बिन्दु से आपका क्या आशय है और मार्क्स में आप क्या अंध-बिन्दु देखते हैं ? जवाब से पहले मैंने कहा कि हे तात ! अभी आपने किसी इण्टरव्यू में पढ़ लिया है तो आपको याद है ‘वाद-विवाद- संवाद’ के अन्त में जो सूत्र दिए गए हैं। उसमें यह बात मैं 1991 में कह चुका हूँ दस साल पहले। तब आपने यह नहीं पूछा और किसी ने नहीं कहा। अब साक्षात्कार में कह दिया तो आप उसका हवाला दे रहे हैं, जबकि यह बात मैं दस साल पहले लिख चुका हूँ। तो ये लोग जो शिकायत करते हैं वो हमारे लिखे हुए को तो पढ़ते नहीं हैं और बोले हुए पर बहस करते हैं।
इस प्रकरण पर ज्यादा बोल गया मैं; लेकिन जैसे-जैसे आदमी परिपक्व होता है, एक खास उमर में आप जितनी गति से लिखते हैं, बाद में सोच-विचार, अनेक सन्देह शंकाएँ पैदा होती हैं। मैं यह मानता हूँ कि आलोचना को उतना ही सुलिखित होना चाहिए जैसे कि कविता, कहानी या उपन्यास। मैं चाहता हूँ कि मेरे विचारों से जो असहमत हों, वे भी कम से कम गद्य को तो पसन्द करें क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं इस भाषा में लिख रहा हूँ जिसमें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का गद्य मेरे सामने है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का गद्य मेरे सामने है, सरलता और सहजता में रामविलास शर्मा का गद्य मेरे सामने है। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक डायरी का गद्य मेरे सामने हैं। लोगों को नहीं मालूम है, पुस्तक लिखने में मुझे कम समय लगा है, एक लेख लिखने में पुस्तक लिखने से ज्यादा लगता है; यह नहीं मालूम लोगों को। मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं-एक हफ्ते या दस दिन में लिखी हैं। लिखने के पहले सारी सामग्री इकट्ठा कर लेता हूँ।
लिखते समय कभी-कभी अपने नोट्स देख लेता हूँ। बस। ‘छायावाद’ पुस्तक मैंने कुल दस दिन में लिखी। ‘कविता के ने प्रतिमान’ इक्कीस दिन में लिखी हुई किताब है। ‘दूसरी परम्परा की खोज’ दस दिन में लिखी हुई किताब है। बाकी कुछ लेख धारावाहिक या अन्तराल के साथ दस दिन में लिखी हुई किताब है। बाकी कुछ लेख धारावाहिक या अन्तराल के साथ लिखित हैं। अभी ‘आलोचना’ में एक लेख मैंने रामविलास जी पर लिखा है-‘इतिहास की शव-साधना’। बहुत से लोगों की चिट्ठियाँ आई हैं। इस अकेले लेख को लिखने में सोचने में विचारने में कितना समय लगा, इसका अन्दाजा नहीं होगा लोगों को। पर लिखा तो रात दस बजे से शुरू कुया और सुबह दस बजे खत्म किया। मैं इसी तरह एक साँस में लिखता हूँ; उसमें बाधा नहीं आती और वह मेरे लिए एक साधना है। जो लोग शिकायत करते हैं, वही लोग मुझे बोलने के लिए बुलाते हैं। कई बार कहता हूँ कि भाई मुझे लिखने दीजिए। लिखने देते नहीं और शिकायत करते हैं। यह हालत हो गई है। अपना दुःखड़ा किससे रोएँ ?
प्रश्न : अपने एक पुराने साक्षात्कार में आपने कहा था जिस लेखक से आपके विचारों का मेल न हो उसका विरोध बेशक कीजिए लेकिन उसका साहित्यिक महत्त्व यदि कुछ है तो उसे स्वीकार कीजिए। आज के परिदृश्य में जबकि वैचारिक ध्रुवीकरण के चलते कट्टरताएँ बहुत बढ़ गई हैं, क्या आपको लगता है कि जिस सदाशयता को आपने कभी प्रस्तावित किया था, उसकी स्पेस–विशेषतः समकालीन साहित्यकारों में ही, जिसमें सभी लोग शामिल हैं; आप भी-कम होती जा रही है ?
नामवर सिंह : पहली बात तो यह है कि मैं अपने लिए यह सब मानता हूँ, तो दूसरे को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि, उदाहरण के लिए, मैं निर्मल वर्मा के विचारों से सहमत नहीं हूँ-विशेषतः वे विचार जो भारतीयता को लेकर हैं। मार्क्सवाद का वे विरोध करते हैं; मैं नहीं सहमत हूँ। लेकिन निर्मल वर्मा महत्त्वपूर्ण साहित्यकार हैं, इसको स्वीकार भी करता हूँ। यह कोई कुफ्र नहीं है। मार्क्स ने खुद बालज़ाक के बारे में कहा था कि उसके राजनीतिक विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन बालज़ाक बड़ा साहित्यकार है। लेनिन ने भी टायस्टॉय के बारे में ऐसा ही कहा है। गरज कि अपने भ्रामक विचारों के बावजूद एक साहित्यकार बड़ा साहित्यकार हो सकता है।
आलोचक के लिए यह बड़ा जटिल प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है ? उदाहरण के लिए तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े कवि हैं, इस बारे में दो राय नहीं। ये और बात है कि दलित लोग यह न मानें। लेकिन यह सही है कि वे वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते थे, उनके रामराज्य में वही व्यवस्था है। यही नहीं, बल्कि कबीर के बारे में उन्होंने कुछ तल्ख बातें कही हैं; लगभग गाली सी-दी है उन्होंने। भले ही यह कहा जाए कि उनके राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, लेकिन उन्होंने शंबूक वध की कहानी नहीं लिखी। सीता की महिमा गाई है लेकिन स्त्री के बारे में उनके विचार वही नहीं थे जो आज के स्त्रीवादी लोग मानेंगे। बावजूद इसके वे बड़े कलाकार हैं। तो साहित्य में ऐसा होता है। और इसका कारण यह है कि साहित्य में विचार के अलावा इन्द्रिय बोध भी होता है, भावबोध भी होता है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति सही बात कहे तो यह जरूरी नहीं है कि बहुत ही समाज-विरोधी और मानवद्रोही विचार किसी के हों और कलाकार भी बड़ा हो लेकिन उन विचारों के कारण उसके बड़प्पन में खरोंच तो आती है और कभी भी आती है। अगर वह न हो तो वह और बड़ा हो। दुनिया में अनेक ऐसे कलाकार हुए हैं। दार्शनिक भी हुए हैं-जैसे मार्टिन हाइडेगर फासिज्म के समर्थक थे, हिटलर की पार्टी के सदस्य थे और सदस्य ही नहीं बने थे, सदस्य बनकर युनिवर्सिटी के रेक्टर बने थे। बावजूद इसके हाइडेगर कई दार्शनिकों की दृष्टि में बहुत बड़े दार्शनिक हैं। अब फासिज्म से बढ़कर कोई मानव विरोधी दर्शन तो हो नहीं सकता। लेकिन एक इतना बड़ा दार्शनिक हुआ। कई साहित्यकार ऐसे हुए हैं जर्मनी में, इटली में। अब ये गुत्थी सुलझाई जानी चाहिए और यह रचना प्रक्रिया के गहन विश्लेषण द्वारा ही जाना जा सकता है।
इसलिए मैं अपने लिए तो आचार-संहिता बना सकता हूँ कि जिससे असहमत हूँ, उसको सम्मान दूँ। अगर साहित्य में यह नहीं होगा तो इतनी एकरसता होगी, दोहराव होगा, तोतारटंत समाज हो जाएगा। इसलिए बौद्धिकता के लिए जरूरी है कि मतभेद को हम स्वीकार करें और सम्मान करें। मैं अपने लिए यह मानता हूँ और मेरा ख्याल है कि हमारी हिन्दी की परम्परा में जो पहले के आलोचक रहे हैं वो इसे मानते रहे हैं। रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहिष्णु भी रहे हैं। उदाहरण के लिए कहूँ तो जब शीतयुद्ध का जमाना था-1950 से लेकर 1965 तक, इलाहाबाद में परिमल और प्रगतिशील लेखक संघ के बीच घनघोर वाद-विवाद होता था बल्कि मार्क्सवादी लेखकों के अन्दर भी पोलिमिक्स हुई है। तुलसीदास और रामचरितमानस को लेकर यशपाल और रामविलास शर्मा के बीच विवाद हुआ, लेकिन दुश्मनी नहीं थी। मिलते थे रोज़, गोष्ठियों में भी और बाहर भी। वहाँ विजयदेव नारायण साही, धर्मवीर भारती इन लोगों के साथ बहस होती थी। कहा जाता है कि वादे-वादे जायते तत्त्वबोधः। अब यह कम हो रहा है। संकीर्णता की प्रवृत्ति कुछ बढ़ रही है और यह चिन्ता की बात है। जिसे आप ध्रुवीकरण कह रहे हैं, वह कोई ध्रुवीकरण नहीं है। ध्रुवीकरण तब होता है जब अपने विचारों पर आप दृढ़ हों और आपके पास विचार हों। राजनीति में कहाँ ध्रुवीकरण है ?
लगभग साहित्य की वही स्थिति हो गई है। जैसे कि एक तरफ सत्ता में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष में है कांग्रेस। इनमें कोई वास्तविक ध्रुवीकरण नहीं है, नूरा कुश्ती चल रही है। साहित्य में भी इस तरह की बहुत नूरा कुश्तियाँ चल रही हैं। अगर सचमुच ध्रुवीकरण विचारों का होता तो मैं समझता हूँ, साहित्य में सम्बन्ध बेहतर होते। जहाँ स्पष्ट जानकारी हो कि विरोधी पक्ष का विचार क्या है, एक दूसरे के विचार को जहाँ समझते हों, फर्क साफ़ मालूम हो; तब संवाद की गुंजाइश रहती है। जब मैं समझूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप कहाँ खड़े हैं, तब बात हो सकती है। बात तब नहीं होती जब पता नहीं चलता कि सचमुच आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचता हूँ। इसलिए ध्रुवीकरण नहीं है। यदि सच्चा ध्रुवीकरण होता-उदाहरण के लिए भारत भवन वाले अशोक वाजपेयी और उनके सहयोगी हैं, जो समझते हैं कि प्रगतिशीलों ने तो, साहित्य को विचारधारा का उपनिवेश बना रखा है।
सवाल ये है कि खुद उन्होंने विचारों का अपना उपनिवेश बनाया है कि नहीं हम तो विचार के उपनिवेश हैं लेकिन आपके यहाँ विचार नाम का कोई देश है जो आपका उपनिवेश है ? आपके कुछ विचार हैं कि नहीं ! एक तरह से यह विचार शून्य साहित्य या साहित्य में विचार शून्यता का प्रचार है। ऐसी हालत में तो ध्रुवीकरण विचार और विचार-शून्यता के बीच है। मुक्तिबोध के शब्दों पार्टनर ! तुम अपनी पालिटिक्स तो बताओ ! बात तभी हो सकती है। अपनी राजनीति वो बताएँगे नहीं। क्यों नहीं बताएँगे यह हम जानते हैं क्योंकि बता नहीं सकते। तुलसीदास ने कहा है; ‘चोर नारी जिमि प्रकट न रोई।’ चोर की औरत रोने लगे तो यह मालूम हो जाएगा कि वह चोर की बीवी है। इसीलिए कुछ लोग अपनी राजनीति नहीं बताते क्योंकि बहुत असुविधाजनक होगा अपनी राजनीति बताना। एक पूरी सूची बनाई जाए और उनसे जवाब माँगा जाए तो निकल आएगा कि उनकी राजनीति क्या है। फिर भी दावा यही करते हैं कि वे सिर्फ शुद्ध साहित्य ही करते हैं। और दूसरे राजनीति करते हैं। कठिनाई यही है इसलिए क्या साहित्य में बात की जाए। ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुलता या बहुवचन की बात आप स्वीकार करते हैं।
भारतीय समाज में, सभी धर्मों, सभी भाषाओं के लिए, सभी विचारों के लिए जगह है, इसे ही लोकतन्त्र कहते हैं। इसलिए उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। वे समझते हैं कि हम लोग एक मत वाले हैं और बहुवचन और बहुलता आकर्षक शब्द हैं-स्वीकार कर लिया; लेकिन उनकी पत्रिका को देखिए। उस पत्रिका में वही आधे दर्जन, एक दर्जन नाम हैं जो हर अंक में दिखाई पड़ते हैं। यह कैसी बहुलता और कैसा बहुवचन है जिसमें एक छोटा-सा गुट है सब एक विचार के, एक ही भावबोध के, एक ही तरह की भाषा लिखने वाले, उन्हीं लोगों को बीस साल तक छापते आ रहे हैं-‘पूर्वग्रह’ से लेकर ‘बहुबचन’ तक और नाम लेते हैं बहुलता का। अब मैं क्या कहूँ ? तो एकवचनवादी बहुवचनवादी हो गए और हम लोग जो बहुवचनवादी हैं-हम लोगों को कहा जाता है-तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए संवाद कठिन है।
प्रश्न : दलित साहित्य को स्वीकृति देते हुए आपने अपने पूर्व कथन में, पूर्व निष्कर्ष में परिवर्तन को स्वीकार किया है। क्या आपके कुछ अन्य मतों में या निष्कर्षों में कोई और परिवर्तन आया है ? ऐसा परिवर्तन जो बहुत स्पष्टता से शायद व्यक्त न हो पाया हो ?
नामवर सिंह : कई चीजों में। राजेन्द्र यादव की शिकायत है कि नामवर में ‘कन्सिस्टेन्सी’ नहीं है। वे अपने विचार को बदलते रहते हैं। चिन्तन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि ये गुण है। वे समझते हैं कि दोष है। रचनात्मक साहित्य को देखिए। सृजन का धर्म ही है-नवाचार, पुनर्नवता। कुछ नया करना। नहीं तो यह सृजन नहीं है और आप अपने को ही दोहराते चले जा रहे हैं। निराला ने जो पहली कविता लिखी थी अगर वही कविता अन्त तक लिखते रहे होते तो उनमें और सुमित्रानन्दन पन्त में फर्क नहीं रह जाता। रामचन्द्र शुक्ल संचयन की भूमिका में मैंने लिखा है कि ‘कविता क्या है’ लेख उन्होंने 1909 में ‘सरस्वती’ में लिखा था उसे ‘विचार वीथी’ में 1930 में कितना बदल दिया। रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास जिस रूप में नागरी प्रचारिणी सभा से 1928 में छपाया था उसे 1941 में इतना बदल दिया।
आपने दलित साहित्य का नाम लिया। पहले मैं मानता था कि दलितों के बारे में जो भी साहित्य लिखा जाए उसे दलित साहित्य माना जाए, लिखने वाला चाहे गैर दलित हो या दलित।
प्रेमचन्द्र ने जो साहित्य लिखा उसमें दलित साहित्य भी है। लेकिन ओमप्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा ‘जूठन’ और उनका कहानी संग्रह सलाम जब मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए जो उसके पहले मैं नहीं जानता था। मरे हुए बैल की खाल निकालने का काम और मरे हुए जानवर को उठाना और उसको कैसे पहुँचाना बाजार में। कैसे उस समाज में रहने वाले लोग-सूअर मारने वाली घटना है-कैसे अपनी जात छुपाते हैं। हम सवर्णों को कभी इस बात का एहसास नहीं होगा। हम अपनी जात छुपाते नहीं बल्कि धड़ल्ले से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बनिया हैं, हम जैन हैं। कोई शर्म नहीं मालूम होती और एक आदमी है जो अपनी जात छिपाता फिरता है। ये दर्द जब मैंने जाना, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे अनुभव हैं जो दलित-कुल में जन्म लेने के बाद ही कोई आदमी जान सकता है। इसलिए सच्चा दलित साहित्य तो वही होगा। इसका मतलब ये नहीं है जो भी दलित होगा वह श्रेष्ठ साहित्यकार भी होगा।
साहित्य में भी उत्तम-मध्यम जो भी दलित होगा वह श्रेष्ठ साहित्यकार भी होगा। दलित साहित्य में भी उत्तम-मध्यम है और स्वयं दलित लेखक भी जानते हैं कि एक स्तर की कविताएँ सभी दलित कवियों की नहीं है ! एक ही स्तर की कहानियाँ सभी दलित कहानीकारों की नहीं हैं। एक ही स्तर की आत्मकथाएँ भी नहीं हैं। तो मेरे विचार बदले हैं-मैंने यह ऐलानिया स्वीकार किया है। पहले मैं ये मानता था अब नहीं मानता। उदाहरण के लिए पहले मेरी धारणा थी कि एक ही परम्परा होती है और इस बात की खोज करने में 20-30 वर्ष लगे जब मुझे यह अहसास हुआ कि कोई और परम्परा भी है। जब मैं अपने गरुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आया-तब मुझमें ये बोझ नहीं जागा। उनके देहावसान के बाद उन्हीं को फिर पढ़ने लगा तो अचानक फ्लैश की तरह दूसरी परम्परा का खयाल आया।
वे सारी बातें पहले बता चुके थे लेकिन तब मुझे नहीं सूझा कि हमारी भारतीय परम्परा में एक और परम्परा है और वह परम्परा विद्रोह, विरोध और प्रतिरोध की परम्परा है। यानी तुलसी और कबीर दोनों एक ही परम्परा के नहीं चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक ही परम्परा को माननेवाले अक्सर मुख्य धारा की बात करते हैं और इस तरह कुछ को हाशिए पर फेंक देते हैं। साफ है कि परम्परा का प्रश्न वर्चश्व से जुड़ा है और वही संघर्ष है। ऐसे भी दौर आते हैं कि जिसे आपने हाशिये पर डाल दिया है वह मुख्य धारा बन जाती हैं और मुख्य धारा हाशिये पर चली जाती है। अगर हम सचमुच ही मानते हैं कि इतिहास में वर्ग-संघर्ष रहा है तो वर्ण-संघर्ष भी रहा है। लगभग 1980 में ही मैं इस बात को समझ सका।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book