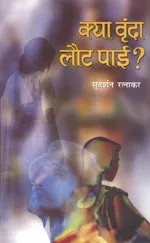|
सांस्कृतिक >> क्या वृंदा लौट पाई क्या वृंदा लौट पाईसुदर्शन रत्नाकर
|
372 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत उपन्यास आज के उपन्यासों से अलग है। अति साधारण-सा लगने के बावजूद अति विशिष्ट है
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सुदर्शन रत्नाकर की कृतियाँ एक समाधान प्रस्तुत करती हैं, कथा के प्रति एक
आत्मीयता का भाव भी।’ ‘क्या वृंदा लौट पाई’ में एक संसार
के भीतर अनेक-अनेक समाए संसार सहज ही खोजे जा सकते हैं। विभाजन से पूर्व
पंजाब की स्थिति, सभी संप्रदायों में एक गहरा आत्मीय भाव, किंतु विभाजन के
पश्चात् एक और ही दृश्य प्रस्तुत होता है। अंतहीन संघर्षों का सिलसिला।
किंतु इन घटनाओं में कहीं भी राजनीति का रंग नहीं दीखता ! कहानी एक परिवार की परिधि में घूमती है। उसमें कृष्ण है गौतम है, वृंदा है, बाऊजी हैं, बीजी तथा और भी कितने जीते-जगाते, चलते-फिरते पात्र हैं। धीरे-धीरे कहानी कहानी न रहकर एक जीवंत यथार्थ बन जाती है। नानी, रहमान चाचा सर्वत्र अपनी सहज उपस्थिति का अहसाह जगाते रहते हैं।
यह उपन्यास आज के उपन्यासों से अलग है। अति साधारण-सा लगने के बावजूद अति विशिष्ट है।
किंतु इन घटनाओं में कहीं भी राजनीति का रंग नहीं दीखता ! कहानी एक परिवार की परिधि में घूमती है। उसमें कृष्ण है गौतम है, वृंदा है, बाऊजी हैं, बीजी तथा और भी कितने जीते-जगाते, चलते-फिरते पात्र हैं। धीरे-धीरे कहानी कहानी न रहकर एक जीवंत यथार्थ बन जाती है। नानी, रहमान चाचा सर्वत्र अपनी सहज उपस्थिति का अहसाह जगाते रहते हैं।
यह उपन्यास आज के उपन्यासों से अलग है। अति साधारण-सा लगने के बावजूद अति विशिष्ट है।
हिमांशु जोशी
प्रेरणा स्रोत
महामहिम राष्ट्रपिता डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
को सादर समर्पित।
महामहिम राष्ट्रपिता डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
को सादर समर्पित।
दो शब्द
उपन्यास ‘क्या वृंदा लौट पाई ?’ लिखने से पहले दो घटनाएँ
चेतना में घूमते रहती थीं। हमारे पड़ोस में ही दो भाइयों के परिवार थे। एक
डॉक्टर था दूसरा वकील। तीसरा भाई शिमला में उपायुक्त था। उसकी पत्नी इन
दोनों भाईयों के पास रहती थी। वह अशिक्षित थी। पति के पद के अनुसार उसमें
योग्यता नहीं थी। इसलिए वह त्याज्य हो गई। उपेक्षित बन मझले भाई के घर
रहती थी। घर का काम-काज करती, घर सँभालती और दो समय का खाना खा लेती। कोई
माँग नहीं कोई इच्छा नहीं। छोटे-बड़े, बच्चों, पड़ोसियों सबकी वह भाभी थी।
फिर पता नहीं क्यों एकाएक वह विक्षिप्त हो गई। इलाज करवाया पर कोई लाभ न
हुआ। घुटनों के बल घिसटती हुई बाहर चली जाती। कहाँ गई, पता ही नहीं चलता।
उसे इस स्थिति में देखती तो मन भर आता। फिर एक दिन एक वाहन उसे कुचलता हुआ
आगे निकल गया। एक अभिशप्त जीवन का अन्त हो गया।
दूसरी घटना भी वहीं की है। वह एक विद्यालय की मुख्याध्यापिका थी। लगभग चालीस वर्ष की सुंदर, सुशील अविवाहित। उसके घर वर्ष में एकाध बार कोई आता था। कुछ घण्टे रुकता फिर चला जाता। पता, चला, वह उसका प्रेमी था। लाहौर (पाकिस्तान) में उसके घर आमने-सामने थे। प्यार हो गया पर शादी नहीं हो पाई। वे विजातीय थे। दोनों ने विवाह सूत्र में न बँधने का निर्णय ले लिया। लड़की ने अपना प्रण निभाया लड़का माता-पिता की इकलौती संतान था। माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। विवाह कर लिया। घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी निभाता, लेकिन प्रेमिका के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा करता। उससे कभी-कभार मिलने आता। उसने पत्नी से कुछ नहीं छुपाया। उसका प्यार पवित्र था।
ये दोनों पात्र मेरे अंतस में घूमते रहते थे। इनको लेकर कुछ लिखना चाहती थी। अंत में दोनों पात्रों को लेकर इस उपन्यास को लिखने का संकल्प किया। लेकिन कार्यान्वित करने में अपरिहार्य करणों से विलंब होता गया। इस बीच बहुत कुछ लिखा, लेकिन इन पात्रों के दर्द को लेखनीबद्ध नहीं कर पाई। समय निकलता गया। लेकिन अब ये दोनों पात्र मेरे इस उपन्यास के केंद्रबिंदु हैं। इसके आस-पास शब्दों का, घटनाओं का ताना-बाना बुना है।
जानती हूँ, इक्कीसवीं सदी के आरंभ में आज जीवन-मूल्य वे नहीं रहे। सामाजिकता बदल गई है। ऐसी घटनाएँ प्रासंगिक नहीं रहीं। बेशक आज उपेक्षिता नारी अपने पाँवों पर खड़ी होने की क्षमता रखती है; पर सभी नहीं। आज भी समाज में ऐसी नारियों की कमी नहीं जो त्यक्ता हैं, शोषिता हैं, जिंदा जलाई जाती हैं। मानसिक व शारीरिक यंत्रणा सहन करने को बाध्य हैं। समय बदला है, समाज नहीं बदला, नारी के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। आज आवश्यकता है उन्हें शिक्षित करने की, अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने की, नारी की पीड़ा पहचानने की। तभी तो समाज बदलेगा, रूढ़ियों की जंजीरें टूटेंगी।
भारत-विभाजन की घटना हुए छह दशक होने को हैं, लेकिन उस त्रासदि को आज भी कुछ परिवार भुगत रहे हैं। बहुत कुछ सहा है लोगों ने। पाकिस्तान से भारत आते हुए लोगों ने जो कुछ भुगता, जो कुछ सहा, मैं अपनी प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ। कुछ धुँधली-सी घटनाएँ स्मृति में थीं, कुछ का वर्णन परिवार ने किया, जो स्वयं भुक्तभोगी हैं।
वृंदा-कृष्ण, गौतमी-श्याम, बीजी-बाऊजी, सरला-हरि, रहमान चाचा, बाबा- माँ जैसे पात्र अपने हैं। जिन्हें हम अपने आस-पास देखते हैं।
अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। पर अभी कट्टरता, संकीर्णता में कमी नहीं आई है। जातिवाद, संप्रदायवाद का अभी भी बोलबाला है। कुछ बातें, कुछ घटनाएँ कालजयी होती हैं। गौतमी और वृंदा जैसे पात्र आज भी हैं। पाठक इस बात का ध्यान रखते हुए उपन्यास का रसास्वादन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।
मैं हिन्दी के प्रख्यात कथाकार श्री हिमांशु जोशीजी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने उपन्यास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर मुझे अनुगृहीत किया है।
दूसरी घटना भी वहीं की है। वह एक विद्यालय की मुख्याध्यापिका थी। लगभग चालीस वर्ष की सुंदर, सुशील अविवाहित। उसके घर वर्ष में एकाध बार कोई आता था। कुछ घण्टे रुकता फिर चला जाता। पता, चला, वह उसका प्रेमी था। लाहौर (पाकिस्तान) में उसके घर आमने-सामने थे। प्यार हो गया पर शादी नहीं हो पाई। वे विजातीय थे। दोनों ने विवाह सूत्र में न बँधने का निर्णय ले लिया। लड़की ने अपना प्रण निभाया लड़का माता-पिता की इकलौती संतान था। माँ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। विवाह कर लिया। घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी निभाता, लेकिन प्रेमिका के प्रति भी अपना कर्तव्य पूरा करता। उससे कभी-कभार मिलने आता। उसने पत्नी से कुछ नहीं छुपाया। उसका प्यार पवित्र था।
ये दोनों पात्र मेरे अंतस में घूमते रहते थे। इनको लेकर कुछ लिखना चाहती थी। अंत में दोनों पात्रों को लेकर इस उपन्यास को लिखने का संकल्प किया। लेकिन कार्यान्वित करने में अपरिहार्य करणों से विलंब होता गया। इस बीच बहुत कुछ लिखा, लेकिन इन पात्रों के दर्द को लेखनीबद्ध नहीं कर पाई। समय निकलता गया। लेकिन अब ये दोनों पात्र मेरे इस उपन्यास के केंद्रबिंदु हैं। इसके आस-पास शब्दों का, घटनाओं का ताना-बाना बुना है।
जानती हूँ, इक्कीसवीं सदी के आरंभ में आज जीवन-मूल्य वे नहीं रहे। सामाजिकता बदल गई है। ऐसी घटनाएँ प्रासंगिक नहीं रहीं। बेशक आज उपेक्षिता नारी अपने पाँवों पर खड़ी होने की क्षमता रखती है; पर सभी नहीं। आज भी समाज में ऐसी नारियों की कमी नहीं जो त्यक्ता हैं, शोषिता हैं, जिंदा जलाई जाती हैं। मानसिक व शारीरिक यंत्रणा सहन करने को बाध्य हैं। समय बदला है, समाज नहीं बदला, नारी के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। आज आवश्यकता है उन्हें शिक्षित करने की, अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने की, नारी की पीड़ा पहचानने की। तभी तो समाज बदलेगा, रूढ़ियों की जंजीरें टूटेंगी।
भारत-विभाजन की घटना हुए छह दशक होने को हैं, लेकिन उस त्रासदि को आज भी कुछ परिवार भुगत रहे हैं। बहुत कुछ सहा है लोगों ने। पाकिस्तान से भारत आते हुए लोगों ने जो कुछ भुगता, जो कुछ सहा, मैं अपनी प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ। कुछ धुँधली-सी घटनाएँ स्मृति में थीं, कुछ का वर्णन परिवार ने किया, जो स्वयं भुक्तभोगी हैं।
वृंदा-कृष्ण, गौतमी-श्याम, बीजी-बाऊजी, सरला-हरि, रहमान चाचा, बाबा- माँ जैसे पात्र अपने हैं। जिन्हें हम अपने आस-पास देखते हैं।
अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। पर अभी कट्टरता, संकीर्णता में कमी नहीं आई है। जातिवाद, संप्रदायवाद का अभी भी बोलबाला है। कुछ बातें, कुछ घटनाएँ कालजयी होती हैं। गौतमी और वृंदा जैसे पात्र आज भी हैं। पाठक इस बात का ध्यान रखते हुए उपन्यास का रसास्वादन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।
मैं हिन्दी के प्रख्यात कथाकार श्री हिमांशु जोशीजी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने उपन्यास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर मुझे अनुगृहीत किया है।
सुदर्शन रत्नाकार
भाग-1
एक
गाड़ी सुबह पाँच बजे स्टेशन पहुँची। बाहर बारिश हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर
मैं थो़ड़ी देर तक रुकी रही। बारिश के थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे
थे। मैं प्रतीक्षालय में आकर बैठ गयी। मेरे पास समय कम था, उस पर यह
वर्षा। जितनी देर से पहुँचूँगी, मुझे कृष्ण से मिलने का उतना ही कम समय
मिलेगा। इतने वर्षों के पश्चात वह पहचान भी पाएगा कि नहीं ? पर इतना समय
भी नहीं हुआ कि न पहचानने तक की नौबत आ जाये। बरसों बाद उसका चित्र
पत्रिका में देखकर मैं उसे पहचान गयी थी। समय की रेखाएँ उसके चेहरे पर
अंकित थीं। कैसा लगेगा उससे मिलना ? इस आयु में भी मैं षोडशियों की तरह
शरमा गई। मुझे स्वयं पर हँसी आ गई।
कलकत्ता से चलने तक मैंने यहाँ के बारे में सोचा भी नहीं था; लेकिन दिल्ली आने के बाद मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। भीतर-ही-भीतर कुछ उमड़ने लगा था, पिघलने लगा था, कुछ मिलने की आकाँक्षा, कुछ सबके बारे में जानने की उत्सुकता। बस ऐसा ही कुछ था, जो मुझे वहाँ खींच लिए चला आया। काम समाप्त होते ही मैं रात की गाड़ी से चली आई हूँ। सुबह की प्रतीक्षा भी नहीं की। वर्षा अभी हो रही थी। पर मैं अब और नहीं रुकूँगी। ऐसे तो समय हाथ से निकलता जाएगा। मैं अटैची लेकर स्टेशन के बाहरी गेट पर आ गई। वहाँ एक ऑटोरिक्शा खड़ा था। इशारे से बुलाया। ऑटो में बैठने तक भी मैं भीग गई। बौछार सामने की थी। मैं सिकुड़कर बैठ गई। शॉल को मैंने पाँव तक फैला लिया।
आजादी के इतने वर्षों बाद भी शहर बिल्कुल नहीं बदला था। सड़क के दोनों ओर कुछ दुकानें और बढ़ गई थीं। हरियाली के नाम पर दो-चार पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। सड़कों की दशा दैनीय थी। बार-बार कोई गड्ढ़ा आ जाता। ऑटो झटके खा जाता और पानी मेरे ऊपर आ जाता।
एक हाथ से मैंने ऑटो को मजबूती से पकड़ रखा था, कहीं गिर न जाऊँ। कहने को तो हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन सड़कों की दशा हर छोटे-बड़े शहर में ऐसी ही है। पर इस क्षेत्र की सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए थीं, एक सांसद के घर जाती है। उसके साथ ही मुझे ध्यान आ गया कि कृष्ण घर पर ही मिलेगा भी कि नहीं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर अब जबकि आ गई हूँ तो मिलकर ही जाऊँगी। घर में और सब तो होगे ही।
पुल उतरते ही कृष्ण आ गया। ऑटोवाले को किराया देकर मैं गेट पर आ गई। भीग तो पहले ही गयी थी, उससे बचने का कोई लाभ न था। गेट खोलकर अन्दर आ गई। वर्षा से बचने के लिए पुलिस कर्मी एक ओर बैठा था। मैं समझ गई, कृष्ण घर पर ही है। मेरे दिल की धड़कने तेज हो गईं। पल भर में ही जाने मैंने कितना कुछ सोच लिया। अटैची नीचे रखकर मैंने हाथ पोंछकर घंटी बजाई। थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खुला। दोबारा बजाने पर दरवाजा उसी समय खुल गया-और मेरे सामने कृष्ण खड़ा था।
हम दोनों अपलक देर तक एक-दूसरे को देखते रहे। कृष्ण में अभी भी वही आकर्षण था, आँखों में वही मस्ती। समय और परिस्थियों ने हमें दूर जरूर कर दिया था लेकिन वह दूरी शारीरिक रूप से थी, मन से तो हम कभी दूर नहीं जा पाए थे। बँधे थे एक-दूसरे से और वही बन्धन की चाह, वही प्यार मैं कृष्ण की आँखों में देख रही थी और वह मेरी आँखों में। हम सब कुछ भूलकर एक-दूसरे की आँखों में कुछ-कुछ नहीं, बहुत कुछ ढूँढ़ रहे थे। प्यार भी कितना अद्भुत होता है ! उसके लिए आयु-सीमा, जात-पाँत कुछ नहीं होती; प्यार बस प्यार होता है-किसी से भी किसी भी अवस्था में हो सकता है। कृष्ण। कृष्ण और मैं दुनिया की, लोगों की दृष्टि में प्यार करने की आयु रेखा पार कर चुके थे; लेकिन उस समय हमें कोई देखता तो सोच भी नहीं सकता था कि किसी की आँखों में इस उम्र में भी इतना प्यार हो सकता है, जो उस समय हम दोनों की आँखों में झलक रहा था। उन कुछेक क्षणों के सुखद आनंद से मैं बरसों की पीड़ा को भूल गई।
मेरी तंद्रा तब टूटी जब कष्ण मेरा हाथ पकड़कर अन्दर ले आया और मुझे सोफे पर बिठाया, स्वयं भी मेरे साथ बैठ गया। वह धीरे-धीरे मेरे सिर को सहलाने लगा। मेरी आँखें खुशी से छलछला आईं। मैंने आँसुओं को बह जाने दिया। जाने कब से रोक रखे थे। समय जैसे थम गया था। बरसों से कृष्ण से मिलने की आकांक्षा पूरी हो रही थी। कैसा-कैसा सोचती थी उसके बारे में ! अब वे पल, वे क्षण मेरे सामने थे। मैं पूरी तरह उन क्षणों को बाँध लेना चाहती थी। बाहर अभी-भी वर्षा हो रही थी। लेकिन मेरे भीतर का तूफान कृष्ण के स्पर्श से थमने लगा था। मैं यह भूल गई कि मैं उससे अभी-अभी मिली हूँ। बरसों का अन्तराल जैसे समाप्त हो गया था। सारी दुनिया सिमट रही थी। मैंने कृष्ण का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगा लिया। अपनी भीगी पलकों को उसके हाथों से पोंछने लगी। धीरे-धीरे मैं सँभल रही थी। मैंने अपना सिर कृष्ण के कंधे से हटा लिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगी।
कृष्ण ने पूछा, ‘‘कैसी हो वृन्दा ?’’
मैं मुस्करा दी। एकाएक कृष्ण के दोनों हाथ छोड़ दिए। मुझे ध्यान आया वह घर में अकेला नहीं है। बच्चे भी कितने बड़े हो गये होंगे विवाह के बँधन में बँधने के बाद कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, कितने बन जाते हैं। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ उत्तरदायित्व-सब मिलकर कितना कुछ बदल देते हैं। मैं इधर-उधर देखने लगी तो कृष्ण समझ गया।
‘‘घर में कोई नहीं है वृंदा।’’
मैंने प्रश्नार्थ उसे देखा।
उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
‘‘वृंदा तुम कपड़े बदल लो गीले हो रहे हैं। मैं चाय लाता हूँ, एकदम कड़क।’’
तुम्हें याद है कृष्ण ?’’
‘‘मैं कुछ भी नहीं भूला वृंदा कहकर जाने लगा। मैंने आवाज देकर कहा मैंने चाय पीनी छोड़ दी है।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तुम्हें अच्छा नहीं लगता था मेरा कड़क चाय पीना।’’
‘‘वह तब की बात थी वृंदा तब तो मैं बहुत कुछ चाहता था पर कहाँ हो पाया था ! अब बहुत कुछ नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है।’’
‘‘नहीं कृष्ण, ऐसी बात नहीं है। वह तो बीमार होने पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। बस उसके बाद पी ही नहीं। अच्छी भी नहीं लगती अब।’’ मैंने कहा।
‘‘दूध तो पी लोगी न ?’’
मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया।
मैं कृष्ण को कमरे से बाहर जाते देखती रही वह इतनी जल्दी तैयार हो गया था शायद उसे कहीं बाहर जाना था उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। अटैची से दूसरी साड़ी निकाल कर पहन ली आसमानी रंग की साड़ी मैं साथ ही लाई थी। यह रंग कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। शायद उसे यह याद भी है कि नहीं। गीले कपड़े इकट्ठे कर दिए। वर्षा अभी हो रही थी। फैलाने का कोई लाभ नहीं था।
दरवाजे पर आवाज हुई। खोला तो कृष्ण हाथ में ट्रे लिये खड़ा था। मुझे अपलक देखने लगा।
‘‘तुम पर यह रंग अब भी कितना खिलता है वृंदा !’’
मैं मुस्करा दी वास्तव में कृष्ण कुछ भी नहीं भूला था।
‘‘तुम स्वयं क्यों लाये हो ?’’ मैंने कहा।
‘‘मैंने बताया था न घर में कोई नहीं है। नौकरानी अभी सो रही है।’’ कहते हुए वह अन्दर आ गया। मैंने उसके हाथ से ट्रे ले ली। कृष्ण अपने लिए चाय लाया था। साथ में टोस्ट और बिस्कुट थे।
‘‘तुम्हें कहीं जाना है ?’’ मैंने पूछा।
‘‘नहीं तो।’’
‘‘तैयार हो न, इसलिए समझी...।’’
‘‘सुबह जल्दी उठ गया था। कुछ करने को नहीं था। वर्षा के कारण अभी अखबार नहीं आया। सोचा, तैयार हो जाऊँ। कहीं जाना भी होता तो भी नहीं जाता, वृंदा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आई हो। तुमने मुझे सौगंध देकर ऐसा बांध लिया था कि मैंने सोच लिया था, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी।’’
‘‘सोचा तो मैंने भी था, कृष्ण लेकिन अब वे परिस्थियाँ नहीं रहीं। मुझे तो इससे पहले भी आकर मिलना चाहिए था; पर अपनी ही सौगंध में, निश्चय में मैं स्वयं बँधी थी।’’
‘‘अब निश्चय कैसे बदल लिया तुमने ?’’
‘‘तीन दिन से मैं दिल्ली में थी। एक सेमिनार में आई थी तो आने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन इन तीन दिनों में मन्थन करती रही जाऊँ या न जाऊँ के द्वंद्व में मैंने एक दिन निकाल लिया। अंत में विजय भावना कि हुई और मैंने अपना निश्चय बदल लिया। फिर मैंने सुबह होने की भी प्रतीक्षा नहीं की और रात की गाड़ी से ही चली आई।’’
‘‘कुछ लो न।’’ चाय का घूँट पीते हुए कृष्ण ने कहा। ‘‘नहीं, बस दूध ही लूँगी।’’ मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा।
‘‘तुम खाने-पीने के मामले में बदल गई हो वृंदा, पहले तो बिना सोचें खूब खाया करती थी।’’
‘‘वह तब की बात थी अब तब में बहुत अन्तर आ गया है समय भी तो कितना बदल गया है ! कितना समय, कितना कुछ हमारे हाथ से निकल गया है !’’
‘‘नहीं वृंदा, समय बस कुछ देर के लिए थम गया था; पर तुम हर पल हर समय मेरे साथ थीं- मेरी सोच में, मेरे खयालों में और मेरे.....’’
‘‘दिल में।’’ मैं वाक्य पूरा करके खिलखिला कर हँस पड़ी। ‘‘तुम्हें तो कवि होना चाहिए था। राजनीति में कैसे आ गये तुम ?’’
‘‘तुम्हारे कारण।’’
‘‘मैं इसका कारण कैसे बन गई ?’’
‘‘तुम आजादी की लड़ाई में साथ दे रही थीं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, इसलिए मैं भी एक सिपाही बन गया था।’’
‘‘वह देश की आजादी के लिए था। सभी क्रान्तिकारी, सत्याग्रही राजनीति में नहीं आए। कई तो गुमनामी के अँधेरों में ही खो गए। कुछ अता-पता ही नहीं। मुझे ही देख लो न ! तुमसे अधिक सक्रिय रही थी मैं। पर मेरा पता तो तुम भी नहीं लगा सके।’’
‘‘तुम व्यंग्य कर रही हो ?’’
‘‘नहीं, मैं सच्चाई बता रही हूँ। इन बीस वर्षों में एक बार भी मेरे बारे में जानने का प्रयत्न किया। मैं कहाँ कैसी हूँ ? राजनीति की तरह तुम स्वयं भी रूखे हो गये हो।’’
‘‘तुमने भी तो सौगंध दी थी।’’
‘‘मैंने न मिलने की सौगंध दी थी, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम मेरे बारे में कुछ जानो ही नहीं। तुम व्यस्त होते चले गए और मुझे स्वयं से दूर कर लिया तुमने, कृष्ण।’’
‘‘तुम नाराज हो गई हो वृंदा ! पर तुम्हें अधिकार है, तुम कहती जाओ। मैं सुनता रहूँगा, क्योंकि मैं दोषी हूँ। घर-गृहस्थी, राजनीतिः सब में इतना खोया रहा अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम मुझसे जुड़ी हो, इसलिए जितना मैंने अपने बारे में सोचा है उतनी ही सोच में तुम भी थीं।’’
‘‘तुम साथ ही तो थीं, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, भूल तो पराए जाते हैं। तुम मेरी अपनी हो, उतनी ही अपनी बरसों पहले थीं। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाया, वृंदा।’’
‘‘तुम भावुक हो रही हो।’’
‘‘अभी तुम मुझे शुष्क कह रही थीं, शुष्क व्यवहारवाले भावुक नहीं हो सकते क्या ? दोनों में से कोई एक धारणा बनाओं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह भावुकता ही मुझे राजनीति में खींच लाई थी। लोगों के दुःख-दर्द को समझने के लिए उन्हें दूर करने में मैं व्यस्त होता गया और फिर उसका नेता बन गया। एक बार जो इस दलदल में फंसा तो फँसता ही गया। मृगतृष्णा ही तो है। पर अब जल्दी ही संन्यास लेने जा रहा हूँ। जो सोचा था, वह नहीं हो पाया। कठपुतली ही मात्र ही हैं हम। डोर ऊपर रहती है, जिधर खिंचती है उधर रह जाना पड़ता है जिस छवि से प्रेरित होकर यह रास्ता अपनाया था, वह धूमिल हो रही है, यह तो तुम भी जानती हो। पार्टीवाद, जातिवाद में विघटित देश किस कगार पर खड़ा है, कुकुरमुत्ता की तरह नित्य नए-नए उगते राजनीतिक दल स्वार्थ के दलदल में स्वयं भी फंसा रहे हैं। अपनी पार्टी की बुराइयों के लिए मैं भी उत्तरदायी हूँ तभी तो उन बुराइयों को ढोए चला जा रहा हूँ। बस, अब कंधे भारी हो गए हैं, और गंदगी को ढोना मेरे बस में नहीं रहा।’’
‘‘हर व्यक्ति यही सोचता तो स्वच्छ छविवाले लोग राजनीति में रहेंगे ही नहीं, तो गंदगी और बढ़ जाएगी, कृष्ण। फिर यह तो हार मान लेने वाली बात हुई। जिस उद्देश्य के लेकर चले हो, उसे पूरा करो।’’
‘‘उद्देश्य तो और भी बहुत सारे थे, वे कब पूरे हुए हैं। भटकता ही रहा हूँ। मन ने जो चाहा, वह कभी पूरा नहीं हुआ। सोचता कुछ और हूँ, होता कुछ और है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है, वृंदा ?
‘‘तुम इतने निराश तो कभी नहीं हुए थे, कृष्ण ! समय कभी एक-सा नहीं रहता, कुछ अप्रिय हो गया है तो ठीक हो जाएगा। समस्याएँ जीवन में सक्रियता लाती हैं, निष्क्रियता नहीं, समय के अनुसार बदलना, उसके साथ चलना सीखो, सबकुछ अपने आप सुलझता जाएगा। यही प्रकृति का नियम है।’’
‘‘ठीक कहती हो वृंदा ! परिवर्तन शाश्वत है। उसे स्वीकारना होगा- अच्छा-बुरा कुछ भी। अब मेरे ही जीवन को लो, कितना कुछ घटित हो गया है। जो कभी नहीं चाहा था वह भी हो गया, हो रहा है।’’
‘‘तुम झूठ बोल रहे हो।’’
‘वह कैसे ?’’
‘‘तुमने कभी सोचा था कि मैं तुमसे आकर मिलूँगी। अप्रत्याशित, यों काल बरसते बादलों में कालिदास की नायिका की तरह भीगा बदन, भीगा मन लिये। तुम आश्चर्यचकित नहीं हो गए थे। थोड़ी देर पहले ही की तो बात है। जब अचानक किसी प्रिय का मिलन हो सकता है। तो बिछुड़ना भी हो सकता है, कृष्ण।’’
‘‘तुम आज भी अपनी बात मनवाने की क्षमता रखती हो। तुम्हारे तर्कों के आगे मैं सदैव ही निरुत्तर हो जाता हूँ। होगा वही जो तुम चाहोगी।’’
चाय का प्याला रखकर कृष्ण मेरे हाथ को सहलाने लगा।
‘‘तुम मुझसे दूर क्यों चली गयी थीं ? क्या तुम्हें इसका अफसोस कभी नहीं हुआ ?’’
‘‘वह अतीत की बात है। उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। समय की परिस्थियों में वही ठीक था। दूरी ने हमारे प्यार को कम नहीं किया। मैं तो तब भी तुम्हारी थी कृष्ण, और आज भी तुम्हारी हूँ।’’
थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच निस्तब्धता छाई रही। जो जिह्वा नहीं कह पा रही थी, आँखें कह रही थीं। कहते है न, आँखों की अपनी भाषा होती है और वही भाषा हम एक-दूसरे की आँखों में पढ़ रहे थे। बहुत सारा प्यार बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारे उपालंभ, बहुत सी कही-अनकही बातें, जिसका लेखा-जोखा करने बैठें तो पता ही नहीं कितना समय लग जाए। पर वह मौन का आदान-प्रदान दूरियाँ मिटा रहा था। बाहर वर्षा कुछ-कुछ थमने लगी थी, लेकिन मेरे भीतर फिर कुछ उमड़ने लगा। मेरे आँसू फिर से बहने लगे थे।
‘‘नहीं वृंदा, नहीं, ऐसे मत रोओ। मेरा दोष मुझे कचोटने लगता है, ग्लानि होने लगती है। मैंने कभी स्वयं को क्षमा नहीं किया। करता भी कैसे, दोष भी कोई कम नहीं था।’’
‘‘ऐसा मत कहो, कृष्ण मैंने अपने आँसुओं पोंछते हुए कहा, ‘‘जो कुछ हुआ हमारा अतीत है। वह तो लौटकर आएगा नहीं। दोषी हम दोनों ही नहीं थे। बस परिस्थितियाँ ही तो ऐसी थीं।, फिर भाग्य की भी बात होती है।’’
‘‘तुम तो भाग्य को नहीं मानती थीं।’’
‘‘अब मानने लगीं हूँ। जो कुछ हमारे हिस्से का होता है, वह हमें अवश्य मिलता है और जो नहीं होता उसे हम चाहकर भी नहीं पा सकते। मेरी-तुम्हारी बात, कुछ और दृष्टांत-इन सबको देखकर विश्वास होने लगा है कि इन हथेलियों की लकीरों से भी बहुत कुछ होता है। मैं जानती हूँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा; पर यह सच है कृष्ण, कि मेरे विचार में परिवर्तन आ गया है। होता है ऐसा, समय के साथ-साथ हमारी सोच भी बदलती रहती है और परिपक्वता भी आती है। यौवनावस्था की मस्ती में बहुत से विचार उधार लिए होते हैं; लेकिन जैसे-जैसे हम समय की सीढ़ियाँ लाँघते जाते हैं, उधार का लाबादा उतरता जाता है और हम अपने मन के भीतर अधिक झाँकने लगते हैं। आँखों के आगे के भ्रम के सुनहरे परदे हटने लगते हैं तथा वास्तविक और अवास्तविक की पहचान करने की क्षमता आती है। इसी से विचारों में प्रौढ़ता आती है। सच्चाई को स्वीकीरने लगते हैं हम। वह भावुकता तब गौण हो जाती है, जिसके आवेश में बहकर सही-गलत की पहचान भी नहीं कर पाते ।’’
कलकत्ता से चलने तक मैंने यहाँ के बारे में सोचा भी नहीं था; लेकिन दिल्ली आने के बाद मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। भीतर-ही-भीतर कुछ उमड़ने लगा था, पिघलने लगा था, कुछ मिलने की आकाँक्षा, कुछ सबके बारे में जानने की उत्सुकता। बस ऐसा ही कुछ था, जो मुझे वहाँ खींच लिए चला आया। काम समाप्त होते ही मैं रात की गाड़ी से चली आई हूँ। सुबह की प्रतीक्षा भी नहीं की। वर्षा अभी हो रही थी। पर मैं अब और नहीं रुकूँगी। ऐसे तो समय हाथ से निकलता जाएगा। मैं अटैची लेकर स्टेशन के बाहरी गेट पर आ गई। वहाँ एक ऑटोरिक्शा खड़ा था। इशारे से बुलाया। ऑटो में बैठने तक भी मैं भीग गई। बौछार सामने की थी। मैं सिकुड़कर बैठ गई। शॉल को मैंने पाँव तक फैला लिया।
आजादी के इतने वर्षों बाद भी शहर बिल्कुल नहीं बदला था। सड़क के दोनों ओर कुछ दुकानें और बढ़ गई थीं। हरियाली के नाम पर दो-चार पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। सड़कों की दशा दैनीय थी। बार-बार कोई गड्ढ़ा आ जाता। ऑटो झटके खा जाता और पानी मेरे ऊपर आ जाता।
एक हाथ से मैंने ऑटो को मजबूती से पकड़ रखा था, कहीं गिर न जाऊँ। कहने को तो हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन सड़कों की दशा हर छोटे-बड़े शहर में ऐसी ही है। पर इस क्षेत्र की सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए थीं, एक सांसद के घर जाती है। उसके साथ ही मुझे ध्यान आ गया कि कृष्ण घर पर ही मिलेगा भी कि नहीं। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था, पर अब जबकि आ गई हूँ तो मिलकर ही जाऊँगी। घर में और सब तो होगे ही।
पुल उतरते ही कृष्ण आ गया। ऑटोवाले को किराया देकर मैं गेट पर आ गई। भीग तो पहले ही गयी थी, उससे बचने का कोई लाभ न था। गेट खोलकर अन्दर आ गई। वर्षा से बचने के लिए पुलिस कर्मी एक ओर बैठा था। मैं समझ गई, कृष्ण घर पर ही है। मेरे दिल की धड़कने तेज हो गईं। पल भर में ही जाने मैंने कितना कुछ सोच लिया। अटैची नीचे रखकर मैंने हाथ पोंछकर घंटी बजाई। थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खुला। दोबारा बजाने पर दरवाजा उसी समय खुल गया-और मेरे सामने कृष्ण खड़ा था।
हम दोनों अपलक देर तक एक-दूसरे को देखते रहे। कृष्ण में अभी भी वही आकर्षण था, आँखों में वही मस्ती। समय और परिस्थियों ने हमें दूर जरूर कर दिया था लेकिन वह दूरी शारीरिक रूप से थी, मन से तो हम कभी दूर नहीं जा पाए थे। बँधे थे एक-दूसरे से और वही बन्धन की चाह, वही प्यार मैं कृष्ण की आँखों में देख रही थी और वह मेरी आँखों में। हम सब कुछ भूलकर एक-दूसरे की आँखों में कुछ-कुछ नहीं, बहुत कुछ ढूँढ़ रहे थे। प्यार भी कितना अद्भुत होता है ! उसके लिए आयु-सीमा, जात-पाँत कुछ नहीं होती; प्यार बस प्यार होता है-किसी से भी किसी भी अवस्था में हो सकता है। कृष्ण। कृष्ण और मैं दुनिया की, लोगों की दृष्टि में प्यार करने की आयु रेखा पार कर चुके थे; लेकिन उस समय हमें कोई देखता तो सोच भी नहीं सकता था कि किसी की आँखों में इस उम्र में भी इतना प्यार हो सकता है, जो उस समय हम दोनों की आँखों में झलक रहा था। उन कुछेक क्षणों के सुखद आनंद से मैं बरसों की पीड़ा को भूल गई।
मेरी तंद्रा तब टूटी जब कष्ण मेरा हाथ पकड़कर अन्दर ले आया और मुझे सोफे पर बिठाया, स्वयं भी मेरे साथ बैठ गया। वह धीरे-धीरे मेरे सिर को सहलाने लगा। मेरी आँखें खुशी से छलछला आईं। मैंने आँसुओं को बह जाने दिया। जाने कब से रोक रखे थे। समय जैसे थम गया था। बरसों से कृष्ण से मिलने की आकांक्षा पूरी हो रही थी। कैसा-कैसा सोचती थी उसके बारे में ! अब वे पल, वे क्षण मेरे सामने थे। मैं पूरी तरह उन क्षणों को बाँध लेना चाहती थी। बाहर अभी-भी वर्षा हो रही थी। लेकिन मेरे भीतर का तूफान कृष्ण के स्पर्श से थमने लगा था। मैं यह भूल गई कि मैं उससे अभी-अभी मिली हूँ। बरसों का अन्तराल जैसे समाप्त हो गया था। सारी दुनिया सिमट रही थी। मैंने कृष्ण का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगा लिया। अपनी भीगी पलकों को उसके हाथों से पोंछने लगी। धीरे-धीरे मैं सँभल रही थी। मैंने अपना सिर कृष्ण के कंधे से हटा लिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर देखने लगी।
कृष्ण ने पूछा, ‘‘कैसी हो वृन्दा ?’’
मैं मुस्करा दी। एकाएक कृष्ण के दोनों हाथ छोड़ दिए। मुझे ध्यान आया वह घर में अकेला नहीं है। बच्चे भी कितने बड़े हो गये होंगे विवाह के बँधन में बँधने के बाद कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, कितने बन जाते हैं। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ उत्तरदायित्व-सब मिलकर कितना कुछ बदल देते हैं। मैं इधर-उधर देखने लगी तो कृष्ण समझ गया।
‘‘घर में कोई नहीं है वृंदा।’’
मैंने प्रश्नार्थ उसे देखा।
उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
‘‘वृंदा तुम कपड़े बदल लो गीले हो रहे हैं। मैं चाय लाता हूँ, एकदम कड़क।’’
तुम्हें याद है कृष्ण ?’’
‘‘मैं कुछ भी नहीं भूला वृंदा कहकर जाने लगा। मैंने आवाज देकर कहा मैंने चाय पीनी छोड़ दी है।’’
‘‘क्यों ?’’
‘‘तुम्हें अच्छा नहीं लगता था मेरा कड़क चाय पीना।’’
‘‘वह तब की बात थी वृंदा तब तो मैं बहुत कुछ चाहता था पर कहाँ हो पाया था ! अब बहुत कुछ नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है।’’
‘‘नहीं कृष्ण, ऐसी बात नहीं है। वह तो बीमार होने पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। बस उसके बाद पी ही नहीं। अच्छी भी नहीं लगती अब।’’ मैंने कहा।
‘‘दूध तो पी लोगी न ?’’
मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया।
मैं कृष्ण को कमरे से बाहर जाते देखती रही वह इतनी जल्दी तैयार हो गया था शायद उसे कहीं बाहर जाना था उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया। अटैची से दूसरी साड़ी निकाल कर पहन ली आसमानी रंग की साड़ी मैं साथ ही लाई थी। यह रंग कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। शायद उसे यह याद भी है कि नहीं। गीले कपड़े इकट्ठे कर दिए। वर्षा अभी हो रही थी। फैलाने का कोई लाभ नहीं था।
दरवाजे पर आवाज हुई। खोला तो कृष्ण हाथ में ट्रे लिये खड़ा था। मुझे अपलक देखने लगा।
‘‘तुम पर यह रंग अब भी कितना खिलता है वृंदा !’’
मैं मुस्करा दी वास्तव में कृष्ण कुछ भी नहीं भूला था।
‘‘तुम स्वयं क्यों लाये हो ?’’ मैंने कहा।
‘‘मैंने बताया था न घर में कोई नहीं है। नौकरानी अभी सो रही है।’’ कहते हुए वह अन्दर आ गया। मैंने उसके हाथ से ट्रे ले ली। कृष्ण अपने लिए चाय लाया था। साथ में टोस्ट और बिस्कुट थे।
‘‘तुम्हें कहीं जाना है ?’’ मैंने पूछा।
‘‘नहीं तो।’’
‘‘तैयार हो न, इसलिए समझी...।’’
‘‘सुबह जल्दी उठ गया था। कुछ करने को नहीं था। वर्षा के कारण अभी अखबार नहीं आया। सोचा, तैयार हो जाऊँ। कहीं जाना भी होता तो भी नहीं जाता, वृंदा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम आई हो। तुमने मुझे सौगंध देकर ऐसा बांध लिया था कि मैंने सोच लिया था, तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी।’’
‘‘सोचा तो मैंने भी था, कृष्ण लेकिन अब वे परिस्थियाँ नहीं रहीं। मुझे तो इससे पहले भी आकर मिलना चाहिए था; पर अपनी ही सौगंध में, निश्चय में मैं स्वयं बँधी थी।’’
‘‘अब निश्चय कैसे बदल लिया तुमने ?’’
‘‘तीन दिन से मैं दिल्ली में थी। एक सेमिनार में आई थी तो आने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन इन तीन दिनों में मन्थन करती रही जाऊँ या न जाऊँ के द्वंद्व में मैंने एक दिन निकाल लिया। अंत में विजय भावना कि हुई और मैंने अपना निश्चय बदल लिया। फिर मैंने सुबह होने की भी प्रतीक्षा नहीं की और रात की गाड़ी से ही चली आई।’’
‘‘कुछ लो न।’’ चाय का घूँट पीते हुए कृष्ण ने कहा। ‘‘नहीं, बस दूध ही लूँगी।’’ मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा।
‘‘तुम खाने-पीने के मामले में बदल गई हो वृंदा, पहले तो बिना सोचें खूब खाया करती थी।’’
‘‘वह तब की बात थी अब तब में बहुत अन्तर आ गया है समय भी तो कितना बदल गया है ! कितना समय, कितना कुछ हमारे हाथ से निकल गया है !’’
‘‘नहीं वृंदा, समय बस कुछ देर के लिए थम गया था; पर तुम हर पल हर समय मेरे साथ थीं- मेरी सोच में, मेरे खयालों में और मेरे.....’’
‘‘दिल में।’’ मैं वाक्य पूरा करके खिलखिला कर हँस पड़ी। ‘‘तुम्हें तो कवि होना चाहिए था। राजनीति में कैसे आ गये तुम ?’’
‘‘तुम्हारे कारण।’’
‘‘मैं इसका कारण कैसे बन गई ?’’
‘‘तुम आजादी की लड़ाई में साथ दे रही थीं और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था, इसलिए मैं भी एक सिपाही बन गया था।’’
‘‘वह देश की आजादी के लिए था। सभी क्रान्तिकारी, सत्याग्रही राजनीति में नहीं आए। कई तो गुमनामी के अँधेरों में ही खो गए। कुछ अता-पता ही नहीं। मुझे ही देख लो न ! तुमसे अधिक सक्रिय रही थी मैं। पर मेरा पता तो तुम भी नहीं लगा सके।’’
‘‘तुम व्यंग्य कर रही हो ?’’
‘‘नहीं, मैं सच्चाई बता रही हूँ। इन बीस वर्षों में एक बार भी मेरे बारे में जानने का प्रयत्न किया। मैं कहाँ कैसी हूँ ? राजनीति की तरह तुम स्वयं भी रूखे हो गये हो।’’
‘‘तुमने भी तो सौगंध दी थी।’’
‘‘मैंने न मिलने की सौगंध दी थी, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम मेरे बारे में कुछ जानो ही नहीं। तुम व्यस्त होते चले गए और मुझे स्वयं से दूर कर लिया तुमने, कृष्ण।’’
‘‘तुम नाराज हो गई हो वृंदा ! पर तुम्हें अधिकार है, तुम कहती जाओ। मैं सुनता रहूँगा, क्योंकि मैं दोषी हूँ। घर-गृहस्थी, राजनीतिः सब में इतना खोया रहा अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम मुझसे जुड़ी हो, इसलिए जितना मैंने अपने बारे में सोचा है उतनी ही सोच में तुम भी थीं।’’
‘‘तुम साथ ही तो थीं, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, भूल तो पराए जाते हैं। तुम मेरी अपनी हो, उतनी ही अपनी बरसों पहले थीं। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाया, वृंदा।’’
‘‘तुम भावुक हो रही हो।’’
‘‘अभी तुम मुझे शुष्क कह रही थीं, शुष्क व्यवहारवाले भावुक नहीं हो सकते क्या ? दोनों में से कोई एक धारणा बनाओं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह भावुकता ही मुझे राजनीति में खींच लाई थी। लोगों के दुःख-दर्द को समझने के लिए उन्हें दूर करने में मैं व्यस्त होता गया और फिर उसका नेता बन गया। एक बार जो इस दलदल में फंसा तो फँसता ही गया। मृगतृष्णा ही तो है। पर अब जल्दी ही संन्यास लेने जा रहा हूँ। जो सोचा था, वह नहीं हो पाया। कठपुतली ही मात्र ही हैं हम। डोर ऊपर रहती है, जिधर खिंचती है उधर रह जाना पड़ता है जिस छवि से प्रेरित होकर यह रास्ता अपनाया था, वह धूमिल हो रही है, यह तो तुम भी जानती हो। पार्टीवाद, जातिवाद में विघटित देश किस कगार पर खड़ा है, कुकुरमुत्ता की तरह नित्य नए-नए उगते राजनीतिक दल स्वार्थ के दलदल में स्वयं भी फंसा रहे हैं। अपनी पार्टी की बुराइयों के लिए मैं भी उत्तरदायी हूँ तभी तो उन बुराइयों को ढोए चला जा रहा हूँ। बस, अब कंधे भारी हो गए हैं, और गंदगी को ढोना मेरे बस में नहीं रहा।’’
‘‘हर व्यक्ति यही सोचता तो स्वच्छ छविवाले लोग राजनीति में रहेंगे ही नहीं, तो गंदगी और बढ़ जाएगी, कृष्ण। फिर यह तो हार मान लेने वाली बात हुई। जिस उद्देश्य के लेकर चले हो, उसे पूरा करो।’’
‘‘उद्देश्य तो और भी बहुत सारे थे, वे कब पूरे हुए हैं। भटकता ही रहा हूँ। मन ने जो चाहा, वह कभी पूरा नहीं हुआ। सोचता कुछ और हूँ, होता कुछ और है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है, वृंदा ?
‘‘तुम इतने निराश तो कभी नहीं हुए थे, कृष्ण ! समय कभी एक-सा नहीं रहता, कुछ अप्रिय हो गया है तो ठीक हो जाएगा। समस्याएँ जीवन में सक्रियता लाती हैं, निष्क्रियता नहीं, समय के अनुसार बदलना, उसके साथ चलना सीखो, सबकुछ अपने आप सुलझता जाएगा। यही प्रकृति का नियम है।’’
‘‘ठीक कहती हो वृंदा ! परिवर्तन शाश्वत है। उसे स्वीकारना होगा- अच्छा-बुरा कुछ भी। अब मेरे ही जीवन को लो, कितना कुछ घटित हो गया है। जो कभी नहीं चाहा था वह भी हो गया, हो रहा है।’’
‘‘तुम झूठ बोल रहे हो।’’
‘वह कैसे ?’’
‘‘तुमने कभी सोचा था कि मैं तुमसे आकर मिलूँगी। अप्रत्याशित, यों काल बरसते बादलों में कालिदास की नायिका की तरह भीगा बदन, भीगा मन लिये। तुम आश्चर्यचकित नहीं हो गए थे। थोड़ी देर पहले ही की तो बात है। जब अचानक किसी प्रिय का मिलन हो सकता है। तो बिछुड़ना भी हो सकता है, कृष्ण।’’
‘‘तुम आज भी अपनी बात मनवाने की क्षमता रखती हो। तुम्हारे तर्कों के आगे मैं सदैव ही निरुत्तर हो जाता हूँ। होगा वही जो तुम चाहोगी।’’
चाय का प्याला रखकर कृष्ण मेरे हाथ को सहलाने लगा।
‘‘तुम मुझसे दूर क्यों चली गयी थीं ? क्या तुम्हें इसका अफसोस कभी नहीं हुआ ?’’
‘‘वह अतीत की बात है। उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। समय की परिस्थियों में वही ठीक था। दूरी ने हमारे प्यार को कम नहीं किया। मैं तो तब भी तुम्हारी थी कृष्ण, और आज भी तुम्हारी हूँ।’’
थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच निस्तब्धता छाई रही। जो जिह्वा नहीं कह पा रही थी, आँखें कह रही थीं। कहते है न, आँखों की अपनी भाषा होती है और वही भाषा हम एक-दूसरे की आँखों में पढ़ रहे थे। बहुत सारा प्यार बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारे उपालंभ, बहुत सी कही-अनकही बातें, जिसका लेखा-जोखा करने बैठें तो पता ही नहीं कितना समय लग जाए। पर वह मौन का आदान-प्रदान दूरियाँ मिटा रहा था। बाहर वर्षा कुछ-कुछ थमने लगी थी, लेकिन मेरे भीतर फिर कुछ उमड़ने लगा। मेरे आँसू फिर से बहने लगे थे।
‘‘नहीं वृंदा, नहीं, ऐसे मत रोओ। मेरा दोष मुझे कचोटने लगता है, ग्लानि होने लगती है। मैंने कभी स्वयं को क्षमा नहीं किया। करता भी कैसे, दोष भी कोई कम नहीं था।’’
‘‘ऐसा मत कहो, कृष्ण मैंने अपने आँसुओं पोंछते हुए कहा, ‘‘जो कुछ हुआ हमारा अतीत है। वह तो लौटकर आएगा नहीं। दोषी हम दोनों ही नहीं थे। बस परिस्थितियाँ ही तो ऐसी थीं।, फिर भाग्य की भी बात होती है।’’
‘‘तुम तो भाग्य को नहीं मानती थीं।’’
‘‘अब मानने लगीं हूँ। जो कुछ हमारे हिस्से का होता है, वह हमें अवश्य मिलता है और जो नहीं होता उसे हम चाहकर भी नहीं पा सकते। मेरी-तुम्हारी बात, कुछ और दृष्टांत-इन सबको देखकर विश्वास होने लगा है कि इन हथेलियों की लकीरों से भी बहुत कुछ होता है। मैं जानती हूँ, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा; पर यह सच है कृष्ण, कि मेरे विचार में परिवर्तन आ गया है। होता है ऐसा, समय के साथ-साथ हमारी सोच भी बदलती रहती है और परिपक्वता भी आती है। यौवनावस्था की मस्ती में बहुत से विचार उधार लिए होते हैं; लेकिन जैसे-जैसे हम समय की सीढ़ियाँ लाँघते जाते हैं, उधार का लाबादा उतरता जाता है और हम अपने मन के भीतर अधिक झाँकने लगते हैं। आँखों के आगे के भ्रम के सुनहरे परदे हटने लगते हैं तथा वास्तविक और अवास्तविक की पहचान करने की क्षमता आती है। इसी से विचारों में प्रौढ़ता आती है। सच्चाई को स्वीकीरने लगते हैं हम। वह भावुकता तब गौण हो जाती है, जिसके आवेश में बहकर सही-गलत की पहचान भी नहीं कर पाते ।’’
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book