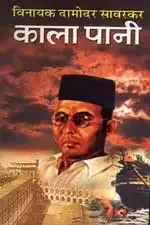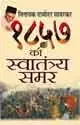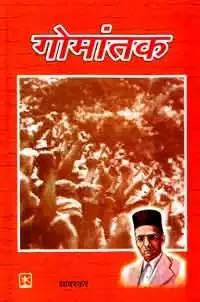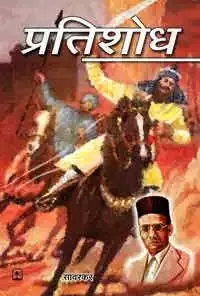|
ऐतिहासिक >> काला पानी काला पानीविनायक दामोदर सावरकर
|
240 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत उपन्यास में काला पानी के ऐसे-ऐसे सत्यों एवं तथ्यों का उद्घाटन हुआ है, जिन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
काला पानी की भयंकरता का अनुमान इसी एक बात से लगाया जा सकता है कि इसका नाम सुनते ही आदमी सिहर उठता है। काला पानी की विभीषिका, यातना एवं
त्रासदी किसी नरक से कम नहीं थी। विनायक दामोदर सावरकर चूँकि वहाँ आजीवन
कारावास भोग रहे थे, अतः उनके द्वारा लिखित यह उपन्यास आँखों-देखे वर्णन
का-सा पठन-सुख देता है।
इस उपन्यास में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन सश्रम कारावास का भयानक दण्ड भुगत रहे थे। काला पानी के कैदियों पर कैसे-कैसे नृशंस अत्याचार एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते थे, उनका तथा वहाँ की नारकीय स्थतियों का इसमें त्रासद वर्णन हैं। इसमें हत्यारों, अपराधियों का जीवन-चित्र भी उकेरा गया हैं।
इस उपन्यास में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन सश्रम कारावास का भयानक दण्ड भुगत रहे थे। काला पानी के कैदियों पर कैसे-कैसे नृशंस अत्याचार एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते थे, उनका तथा वहाँ की नारकीय स्थतियों का इसमें त्रासद वर्णन हैं। इसमें हत्यारों, अपराधियों का जीवन-चित्र भी उकेरा गया हैं।
आमुख
‘काला पानी’ स्वातंत्र्य वीर सावरकर का द्वितीय गद्यात्मक
उपन्यास है। उनका प्रथम उपन्यास ‘मोपलों का विद्रोह’ अथवा
‘मुझे इससे क्या ?’ था। इससे पूर्व अंदमान में विचरित उनके
दीर्घ काव्य ‘गोमांतक’ को मेरे विचार से कथा-वस्तु तथा गद्य
रूपांतर की दृष्टि से उपन्यास विधा में ही सम्मिलित किया जा सकता है।
‘मुझे इससे क्या ?’ शीर्षक उपन्यास के पश्चात सावरकर ने ‘मेरा आजीवन कारावास’ के रूप में अपने आत्मकथ्य का एक अंश लिखा था। इस आत्मकथ्य में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन का वर्णन किया गया है। जो अंदमान अथवा ‘काले पानी’ में सश्रय कारावास का भयानक दंड भुगत रहे है। इस आत्मकथ्य में कुछ हत्यारों, लुटेरों, डाकुओं तथा क्रूर, स्वार्थी व्यसनाधीन अपराधियों का जीवन-चित्र उकेरा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें दो ऐसे प्रकरण हैं जिनमें इन विषयों की चर्चा की गई है कि हमारी राष्टभाषा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी हो तथा अहिंदुओं का हिंदुकरण करना आवश्यक है। ‘मेरा आजीवन कारावास’ में ‘बालिश्त भर हिंदु राज्य-ओस का एक मोती’ जैसी संकल्पना का भी समावेश है। इस पुस्तक का गुजराती भाग में अनुवाद होने के उपरांत कुछ राजनीतिज्ञों ने ब्रिटिश प्रशासकों ने ‘मेरा आजीवन कारावास’ शीर्षक पुस्तक पर तारीख 17 अप्रैल 1934 को प्रतिबंद लगाया।
इस प्रतिबंध को हटाने का प्रयास जारी रखते हुए भी यह ज्यों-का-त्यों रह गया। तथापि यह दरशाने के उद्देश्य से कि अंदमान के बंदीगृह में किस तरह कष्टप्रद, तापदायी, आमानुषिक एवं उत्पाती जीवनयापन करना अनिवार्य होता है, सावरकर ने ‘काला पानी’ शीर्षक उपन्यास लिखा। अगस्त 1936 से ‘मनोहर’ पत्रिका में प्रकाशित हो गया।
‘काला पानी’ उपन्यास की कथा-वस्तु कल्पित अथवा मनगढ़त नहीं है। वह एक दंडित के न्यायालयी अभियोग पर आधारित है। वीर सावरकर की टिप्पणियों में इस तरह का उल्लेख किया गया है। यद्यपि रफीउद्दीन, योगानंद, मालती आदि नाम काल्पनिक हैं, तथापि वे उक्त अभियोगांतक मूल नामों से मिलते-जुलते ही हैं। बीच में विख्यात गायक तथा चित्रपट निर्माता श्री सुधीर फड़के इस उपन्यास पर चित्रपट तैयार करना चाहते थे, परन्तु नियंत्रक मंडल ने अनुरोध किया कि उसमें रफीउद्दीन नामक जो मुसलिम पात्र है, उसमें परिवर्तन किया जाय। उसके अनुसार नामांतर की अनुज्ञा की माँग जब वीर सावरकर से की गई तब उन्होंने स्पष्ट तथा ठोस शब्दों में कहा, ‘‘इस तरह नामांतरण की अर्थात मुसलिम नाम हटाकर हिन्दू नीम का समावेश करने के लिए मैं कदापि अनुमति नहीं दूँगा। यह दिखावा कि कुछ मुसलिम शिष्ट, साधु वृत्ति के होते है, परन्तु मुसलिम नाम में परिवर्तन करने के लिए मैं अनुमति नहीं दूँगा।’’
प्रस्तुत उपन्यास में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का चरित्र वर्णन है, जिसे सन् 1857 के स्वातंत्रता संग्राम में दंड मिला था। दंड भुगतकर मुक्ति प्राप्त वह सेनानी अंदमान का बाशिंदा बना हुआ है। यह योद्धा कपोलकल्पित नहीं है। जब सावरकर अंदमान में थे, उस काल में इस तरह के दो-तीन योद्धा थे जिनकी आयु अस्सी-पचासी के आसपास होगी। इस आयु में भी वे पके पान उधर ही रहते थे तथा उन्होंने सावरकर से गुप्त संर्पक किया था। सावरकर के साथ उनकी साठ-गाँठ थी।
इस उपन्यास की कुछ समीक्षाओं की सावरकर ने टिप्पणियाँ रखी हैं। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि इसमें से कौन से वाक्य ‘मनोहर’ पत्रिका ने निकाल दिए हैं। हो सकता है, उस काल में ऐसे दो-तीन वाक्य अश्लील प्रतीत होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया हो।
सावरकर के साहित्य में काम्य अथवा ग्राम्य अश्लीलता दुर्लभ ही है, तथापि आचार्य अत्रे तथा प्रों फड़के जैसे दिग्गजों में जो विवाद हुआ था उसमें प्रों. फड़के ने यह कहा था कि आचार्य फड़के के साहित्य की हमेशा यह कहकर आलोचना करते हैं कि उसमें अश्लील, बीभत्स प्रसंगों का चित्रण किया जाता है, परंतु सावरकर के साहित्यांतर्गत तत्सम वर्णनों के संबंध में वे कभी चूँ तक नहीं करते, न ही कोई फच्चर अड़ाते हैं। प्रो. फड़के के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य अत्रे कहते हैं, ‘‘फड़के-वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय पाठक के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि वह भी उसी तरह किसी पर बालात्कार करे। परन्तु सावरकर-वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय क्रोध से खून खौलने लगता है और यह उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है कि उस बालात्कारी पापी, चांडाल पर सौ-सौ कोड़े बरसाकर उसकी चमड़ी उधेड़े, उसे कठोर-से-कठोर दंड दें।’’ आचार्य अत्रे की मीमांसा मुझे उचित प्रतीत होती है। यह पढ़कर सुधी पाठक स्यवं निर्णय करें।
इस उपन्यास के सिलसिले में एक पाठक श्री वाचासुंदर सोनमोह, ता. कटोल ने सावरकर के लिखे पत्र में कहा है-‘‘मेरी यह धारणा थी कि आपका साहित्य नीरस होता है।
मेरा विचार था कि आपका यह उपन्यास भी रसहीन होगा। परंतु पहला वाक्य पढ़ते ही दूसरा वाक्य पढ़ते ही दूसरा वाक्य पढ़ने की ललक उत्पन्न हो गई और दूसरा वाक्य पढ़ते ही पूरा अनुच्छेद पढ़ने के लिए मन उछलने लगा। फिर अधिकारियों की ओर ध्यान न देते हुए प्रकरण पाँच और छह के बारह पन्ने लगे हाथ पड़ डाले। आपकी मालती ने जितना मेरा दिल जलाया होगा। आज तक मैनें सैकड़ों उपन्यास तथा कहानियाँ पढ़ी हैं, परंतु मालती ने मेरा हृदय ही चीरकर रख दिया है। आपके रफीउद्दीन ने मेरी विचार-धारणाओं का ही कायाकल्प कर दिया है।’’
इस प्रकार के और अनेक पत्र और अभिमत समय-समय पर प्रकाशित किए गए है। अधिवक्ता श्री भा.गं. देशपांडे लिखित-‘काला पानी-समीक्षण’ नामक सात प्रकरणों और छत्तीस पृष्ठों की एक पुस्तिका नागपुर के विधिज्ञ श्री ल.वा. चरणे ने प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में इस उपन्यास के विविध साहित्यिक निष्कषों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्यिक समीक्षा की गई है। इन तमाम कसौटियों पर यह उपन्यास कुंदन हो गया है।
‘मुझे इससे क्या ?’ शीर्षक उपन्यास के पश्चात सावरकर ने ‘मेरा आजीवन कारावास’ के रूप में अपने आत्मकथ्य का एक अंश लिखा था। इस आत्मकथ्य में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन का वर्णन किया गया है। जो अंदमान अथवा ‘काले पानी’ में सश्रय कारावास का भयानक दंड भुगत रहे है। इस आत्मकथ्य में कुछ हत्यारों, लुटेरों, डाकुओं तथा क्रूर, स्वार्थी व्यसनाधीन अपराधियों का जीवन-चित्र उकेरा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें दो ऐसे प्रकरण हैं जिनमें इन विषयों की चर्चा की गई है कि हमारी राष्टभाषा संस्कृतनिष्ठ हिन्दी हो तथा अहिंदुओं का हिंदुकरण करना आवश्यक है। ‘मेरा आजीवन कारावास’ में ‘बालिश्त भर हिंदु राज्य-ओस का एक मोती’ जैसी संकल्पना का भी समावेश है। इस पुस्तक का गुजराती भाग में अनुवाद होने के उपरांत कुछ राजनीतिज्ञों ने ब्रिटिश प्रशासकों ने ‘मेरा आजीवन कारावास’ शीर्षक पुस्तक पर तारीख 17 अप्रैल 1934 को प्रतिबंद लगाया।
इस प्रतिबंध को हटाने का प्रयास जारी रखते हुए भी यह ज्यों-का-त्यों रह गया। तथापि यह दरशाने के उद्देश्य से कि अंदमान के बंदीगृह में किस तरह कष्टप्रद, तापदायी, आमानुषिक एवं उत्पाती जीवनयापन करना अनिवार्य होता है, सावरकर ने ‘काला पानी’ शीर्षक उपन्यास लिखा। अगस्त 1936 से ‘मनोहर’ पत्रिका में प्रकाशित हो गया।
‘काला पानी’ उपन्यास की कथा-वस्तु कल्पित अथवा मनगढ़त नहीं है। वह एक दंडित के न्यायालयी अभियोग पर आधारित है। वीर सावरकर की टिप्पणियों में इस तरह का उल्लेख किया गया है। यद्यपि रफीउद्दीन, योगानंद, मालती आदि नाम काल्पनिक हैं, तथापि वे उक्त अभियोगांतक मूल नामों से मिलते-जुलते ही हैं। बीच में विख्यात गायक तथा चित्रपट निर्माता श्री सुधीर फड़के इस उपन्यास पर चित्रपट तैयार करना चाहते थे, परन्तु नियंत्रक मंडल ने अनुरोध किया कि उसमें रफीउद्दीन नामक जो मुसलिम पात्र है, उसमें परिवर्तन किया जाय। उसके अनुसार नामांतर की अनुज्ञा की माँग जब वीर सावरकर से की गई तब उन्होंने स्पष्ट तथा ठोस शब्दों में कहा, ‘‘इस तरह नामांतरण की अर्थात मुसलिम नाम हटाकर हिन्दू नीम का समावेश करने के लिए मैं कदापि अनुमति नहीं दूँगा। यह दिखावा कि कुछ मुसलिम शिष्ट, साधु वृत्ति के होते है, परन्तु मुसलिम नाम में परिवर्तन करने के लिए मैं अनुमति नहीं दूँगा।’’
प्रस्तुत उपन्यास में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का चरित्र वर्णन है, जिसे सन् 1857 के स्वातंत्रता संग्राम में दंड मिला था। दंड भुगतकर मुक्ति प्राप्त वह सेनानी अंदमान का बाशिंदा बना हुआ है। यह योद्धा कपोलकल्पित नहीं है। जब सावरकर अंदमान में थे, उस काल में इस तरह के दो-तीन योद्धा थे जिनकी आयु अस्सी-पचासी के आसपास होगी। इस आयु में भी वे पके पान उधर ही रहते थे तथा उन्होंने सावरकर से गुप्त संर्पक किया था। सावरकर के साथ उनकी साठ-गाँठ थी।
इस उपन्यास की कुछ समीक्षाओं की सावरकर ने टिप्पणियाँ रखी हैं। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि इसमें से कौन से वाक्य ‘मनोहर’ पत्रिका ने निकाल दिए हैं। हो सकता है, उस काल में ऐसे दो-तीन वाक्य अश्लील प्रतीत होने के कारण उन्हें निकाल दिया गया हो।
सावरकर के साहित्य में काम्य अथवा ग्राम्य अश्लीलता दुर्लभ ही है, तथापि आचार्य अत्रे तथा प्रों फड़के जैसे दिग्गजों में जो विवाद हुआ था उसमें प्रों. फड़के ने यह कहा था कि आचार्य फड़के के साहित्य की हमेशा यह कहकर आलोचना करते हैं कि उसमें अश्लील, बीभत्स प्रसंगों का चित्रण किया जाता है, परंतु सावरकर के साहित्यांतर्गत तत्सम वर्णनों के संबंध में वे कभी चूँ तक नहीं करते, न ही कोई फच्चर अड़ाते हैं। प्रो. फड़के के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य अत्रे कहते हैं, ‘‘फड़के-वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय पाठक के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि वह भी उसी तरह किसी पर बालात्कार करे। परन्तु सावरकर-वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय क्रोध से खून खौलने लगता है और यह उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है कि उस बालात्कारी पापी, चांडाल पर सौ-सौ कोड़े बरसाकर उसकी चमड़ी उधेड़े, उसे कठोर-से-कठोर दंड दें।’’ आचार्य अत्रे की मीमांसा मुझे उचित प्रतीत होती है। यह पढ़कर सुधी पाठक स्यवं निर्णय करें।
इस उपन्यास के सिलसिले में एक पाठक श्री वाचासुंदर सोनमोह, ता. कटोल ने सावरकर के लिखे पत्र में कहा है-‘‘मेरी यह धारणा थी कि आपका साहित्य नीरस होता है।
मेरा विचार था कि आपका यह उपन्यास भी रसहीन होगा। परंतु पहला वाक्य पढ़ते ही दूसरा वाक्य पढ़ते ही दूसरा वाक्य पढ़ने की ललक उत्पन्न हो गई और दूसरा वाक्य पढ़ते ही पूरा अनुच्छेद पढ़ने के लिए मन उछलने लगा। फिर अधिकारियों की ओर ध्यान न देते हुए प्रकरण पाँच और छह के बारह पन्ने लगे हाथ पड़ डाले। आपकी मालती ने जितना मेरा दिल जलाया होगा। आज तक मैनें सैकड़ों उपन्यास तथा कहानियाँ पढ़ी हैं, परंतु मालती ने मेरा हृदय ही चीरकर रख दिया है। आपके रफीउद्दीन ने मेरी विचार-धारणाओं का ही कायाकल्प कर दिया है।’’
इस प्रकार के और अनेक पत्र और अभिमत समय-समय पर प्रकाशित किए गए है। अधिवक्ता श्री भा.गं. देशपांडे लिखित-‘काला पानी-समीक्षण’ नामक सात प्रकरणों और छत्तीस पृष्ठों की एक पुस्तिका नागपुर के विधिज्ञ श्री ल.वा. चरणे ने प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में इस उपन्यास के विविध साहित्यिक निष्कषों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्यिक समीक्षा की गई है। इन तमाम कसौटियों पर यह उपन्यास कुंदन हो गया है।
बाल सावरकर
प्रकरण-1
मालती
‘‘अम्मा री, एक ओवी1 सुनाओ न ! हम इतनी सारी
मीठी-मीठी ओवियाँ
सुना रहे हैं तुम्हें, पर हो कि मुझे एक भी नहीं सुना रही हो।
उँह....!’’ मालती ने अपने हिंडोल को एक पेंग मारते
हुए बड़े
लाड़ से रमा देवी को अनुरोध भरा उलाहना दिया।
‘‘बेटी, भला एक ही क्यों ? लाखों ओवियाँ गाऊँगी अपनी लाड़ली के लिए। परंतु अब मेरी अम्मा के स्वर में तेरी जैसी मिठास नहीं रही। बेटी ! केले के बकले के धागे में गेंदे के फूल भले ही पिरोए जाएँ, जूही के नाजुक कोमल माला पिरोने के लिए नरम-नरम, रेशमी मुलायम धागा ही चाहिए, अन्यथा माला के फूल मसले जाएँगे। वे प्यारी-प्यारी ओवियाँ मिश्री की डली जैसे तेरे मीठे स्वर में जब गाई जाती हैं। तब वे और भी मधुर दुलारी प्रतीत होती हैं। अतः ऐसी राजदुलारी, मधुर ओवियाँ तुम बेटियाँ गाओ और हम माताएँ उन्हें प्रेम से सुनें। यदि मैं गीत गाने लगूँ न, तो इस गीत की मिठास गल जाएगी और मेरी इस चिरकती-दरकती आवाज पर-जो किसी फटे सितार की तरह फटी-सी लग रही है, तुम जी भरकर हँसोगी।’’
‘‘भई, आने दो हँसी। आनंद होगा, तभी तो हँसी आएगी न ! मेरा मन बहलाने के खातिर तो तुम्हें दो-चार ओवियाँ तो सुनानी ही पड़ेगी। हाँ, कहे दे रहे हूँ।’’
‘‘तुम भगवान के लिए ओवियाँ और स्तोत्र-पठन घंटों-घटों करती रहती हो, भला तब नहीं तुम्हारी आवाज फटती ! परन्तु मुझपर रची दो-चार ओवियाँ सुनाते ही आनन-फानन सितार चिरकने लगते है। यदि माताएँ बेटियों की ओवियाँ सिर्फ सुनती ही रही तो उन ओवियों की रचना भला क्यों की जाती जो माताएँ गाती हैं ! कितनी सारी ममता भरी ओवियाँ हैं जो माताएँ गाती है ! मुझे भी कुछ-कुछ कंठस्थ हैं।’’
‘‘तो फिर जब तुम माँ बनोगी न तब सुनाना अपने लाड़ले को।’’ कहते हुए रमा देवी खिलखलाकर हँस पड़ीं।
ओवी-मराठी पद्य-विधा में प्रचलित एक छंद, जिसमें चार चरण होते हैं-गीत।
लज्जा झेंपती मालती ने रूठे स्वर में कहा, ‘‘भई, मैं सुनाऊँ या न सुनाऊँ, तुम मेरे लिए एक मधुर सी ओवी गाओगी न !’’ और तुरंत माँ से लिपटकर उनकी ठोड़ी से अपने-अपने नरम-नरम, नन्हें-नन्हें होठ सटाकर वह किशोरी माँ की चिरौरियाँ करने लगीं।
‘‘यह क्या अम्मा तुम मेरी माँ हो न ! फिर तुम नहीं तो भला और कौन गाएगा मेरे लिए माँ की दुलार भरी ओवी !’’
‘‘तुम मेरी माँ हो न ! अपनी इकलौती बिटिया के ये स्नेहसिक्त बोल सुनते ही रमा देवी के हृदय में ममता के स्रोत इस तरह ठाठें मरने लगे कि उनकी तीव्र इच्छा हुई कि किसी दूध-पीते बच्चे की तरह अपनी बेटी का सुन्दर-सलोना मुखड़ा अपने सीने से भींच लें। उसे जी भरकर चूमने के लिए उनके होंठ मचलने लगे। परंतु माँ की ममता जितनी उत्कठ होती है, उतनी ही सयानी हो रही अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते समय संकोची भी होती है।
मालती के कपोलों से सटा हुआ मुख हटाते हुए उसकी माँ ने यौवन की दहलीज पर खड़ी अपनी बेटी का बदन पल भर के लिए दोनों हाथों से दबाया और हौले से उसे पीछे हटाकर मालती को आश्वत किया।
‘‘अच्छा बाबा, चल तुझे सुनाती हूँ कुछ गीत। बस, सिर्फ दो-तीन ! बस ! बोल मंजूर !’’
‘‘हाँ जी हाँ। अब आएगा मजा।’’ उमंग से भरपूर स्वर में मालती ने झूले को धरती की ओर से टखनों के बल पर ठेला और पेंग के ऊपर पेंग ली।
‘‘अरे यह क्या ? गाओ भी। किसी कामचोर गायक की तरह ताल-सुर लगाने में ही आँधी रात गँवा रही हो।’’ मालती के इस तरह उलाहना देने पर रमा देवी वहीं ओवी गाने लगीं जो होठों पर आई-
‘‘बेटी, भला एक ही क्यों ? लाखों ओवियाँ गाऊँगी अपनी लाड़ली के लिए। परंतु अब मेरी अम्मा के स्वर में तेरी जैसी मिठास नहीं रही। बेटी ! केले के बकले के धागे में गेंदे के फूल भले ही पिरोए जाएँ, जूही के नाजुक कोमल माला पिरोने के लिए नरम-नरम, रेशमी मुलायम धागा ही चाहिए, अन्यथा माला के फूल मसले जाएँगे। वे प्यारी-प्यारी ओवियाँ मिश्री की डली जैसे तेरे मीठे स्वर में जब गाई जाती हैं। तब वे और भी मधुर दुलारी प्रतीत होती हैं। अतः ऐसी राजदुलारी, मधुर ओवियाँ तुम बेटियाँ गाओ और हम माताएँ उन्हें प्रेम से सुनें। यदि मैं गीत गाने लगूँ न, तो इस गीत की मिठास गल जाएगी और मेरी इस चिरकती-दरकती आवाज पर-जो किसी फटे सितार की तरह फटी-सी लग रही है, तुम जी भरकर हँसोगी।’’
‘‘भई, आने दो हँसी। आनंद होगा, तभी तो हँसी आएगी न ! मेरा मन बहलाने के खातिर तो तुम्हें दो-चार ओवियाँ तो सुनानी ही पड़ेगी। हाँ, कहे दे रहे हूँ।’’
‘‘तुम भगवान के लिए ओवियाँ और स्तोत्र-पठन घंटों-घटों करती रहती हो, भला तब नहीं तुम्हारी आवाज फटती ! परन्तु मुझपर रची दो-चार ओवियाँ सुनाते ही आनन-फानन सितार चिरकने लगते है। यदि माताएँ बेटियों की ओवियाँ सिर्फ सुनती ही रही तो उन ओवियों की रचना भला क्यों की जाती जो माताएँ गाती हैं ! कितनी सारी ममता भरी ओवियाँ हैं जो माताएँ गाती है ! मुझे भी कुछ-कुछ कंठस्थ हैं।’’
‘‘तो फिर जब तुम माँ बनोगी न तब सुनाना अपने लाड़ले को।’’ कहते हुए रमा देवी खिलखलाकर हँस पड़ीं।
ओवी-मराठी पद्य-विधा में प्रचलित एक छंद, जिसमें चार चरण होते हैं-गीत।
लज्जा झेंपती मालती ने रूठे स्वर में कहा, ‘‘भई, मैं सुनाऊँ या न सुनाऊँ, तुम मेरे लिए एक मधुर सी ओवी गाओगी न !’’ और तुरंत माँ से लिपटकर उनकी ठोड़ी से अपने-अपने नरम-नरम, नन्हें-नन्हें होठ सटाकर वह किशोरी माँ की चिरौरियाँ करने लगीं।
‘‘यह क्या अम्मा तुम मेरी माँ हो न ! फिर तुम नहीं तो भला और कौन गाएगा मेरे लिए माँ की दुलार भरी ओवी !’’
‘‘तुम मेरी माँ हो न ! अपनी इकलौती बिटिया के ये स्नेहसिक्त बोल सुनते ही रमा देवी के हृदय में ममता के स्रोत इस तरह ठाठें मरने लगे कि उनकी तीव्र इच्छा हुई कि किसी दूध-पीते बच्चे की तरह अपनी बेटी का सुन्दर-सलोना मुखड़ा अपने सीने से भींच लें। उसे जी भरकर चूमने के लिए उनके होंठ मचलने लगे। परंतु माँ की ममता जितनी उत्कठ होती है, उतनी ही सयानी हो रही अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते समय संकोची भी होती है।
मालती के कपोलों से सटा हुआ मुख हटाते हुए उसकी माँ ने यौवन की दहलीज पर खड़ी अपनी बेटी का बदन पल भर के लिए दोनों हाथों से दबाया और हौले से उसे पीछे हटाकर मालती को आश्वत किया।
‘‘अच्छा बाबा, चल तुझे सुनाती हूँ कुछ गीत। बस, सिर्फ दो-तीन ! बस ! बोल मंजूर !’’
‘‘हाँ जी हाँ। अब आएगा मजा।’’ उमंग से भरपूर स्वर में मालती ने झूले को धरती की ओर से टखनों के बल पर ठेला और पेंग के ऊपर पेंग ली।
‘‘अरे यह क्या ? गाओ भी। किसी कामचोर गायक की तरह ताल-सुर लगाने में ही आँधी रात गँवा रही हो।’’ मालती के इस तरह उलाहना देने पर रमा देवी वहीं ओवी गाने लगीं जो होठों पर आई-
अगे रत्नांचिया खाणी। नको मिखूं ऐठ मोठी।
बघ माईयाही ये पोटीं। रत्न ‘माला’।।1।।
जाता येता राजकुँवर। नको पाहूं लोभनिया।
दृष्ट पटेल माझिया। मालतीला।।2।।
देते माझं पुण्य सारं। सात जन्मवेरी।
माइयी रक्षावे श्रीहरि। लेकुरा या।।3।।
पुरोनी उरू द्यावी। जन्मभरी नारायणा।
कन्या माझी सुलक्षण। एकूलती।।4।।
बघ माईयाही ये पोटीं। रत्न ‘माला’।।1।।
जाता येता राजकुँवर। नको पाहूं लोभनिया।
दृष्ट पटेल माझिया। मालतीला।।2।।
देते माझं पुण्य सारं। सात जन्मवेरी।
माइयी रक्षावे श्रीहरि। लेकुरा या।।3।।
पुरोनी उरू द्यावी। जन्मभरी नारायणा।
कन्या माझी सुलक्षण। एकूलती।।4।।
(अर्थः (1)
अरी ओ रत्नों की खानि ! इस तरह मत इतराना। देखो तो सही, मेरी कोख से तो इस सुंदर रत्न ‘माला’ ने जन्म लिया है।
(2) हे राजकुमार आते-जाते इस तरह ललचाई दृष्टि से मत देखो, मेरी मालती को नजर लग जाएगी।
(3) मेरे सात जन्मों का सारा पुण्य संचय, हे श्रीहरि ! मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ, मेरी मालती की रक्षा करो !
(4) हे नारायण ! मेरी इकलौती कन्या मुझे आजन्म मिले।)
गाने की धुन में ‘इकलौती’ शब्द का उच्चारण करते ही रमा देवी को यों लगा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा है। किसी तीव्र गति की स्मृति से उनका मन कसमसाने लगा। ऐसे हर्षोल्लास की घड़ी में उनकी बेटी को भी यह कसक न हो, वह भी उदास न हो, इसलिए रमा देवी ने अपने चेहरे पर उदासी का साया तक नहीं उभरने दिया; फिर भी उनके कंठ में गीत अटक-सा गया। मालती ने सोचा, गाते-गाते माँ को अचानक साँस फूल जाने से वह अचानक चुप हो गई हैं। माँ को तनिक विश्वास मिले और उनकी गाने की मधुर ध्वनि बँध गई है वह टूट न जाए, इसलिए यह समझकर कि अब उसकी बारी है, वह अपनी अगली ओवियाँ गाने लगी। उसकी माँ ने उसके लिए ममता से लबालब भरी जो ओवियाँ गाई थी, उलकी मिठास से भरपूर हर शब्द के साथ उसके दिल में हर्ष भरी गुदगुदियाँ हो रही थीं।
अपने साजन की प्रेमपूर्ण आराधना की आस लगने से पहले लड़कियों के माँ के प्यार-दुलार भरे कौतुक में जितनी रूचि होती है, उतनी अन्य किसी में भी नहीं।
संध्या की बेला में पश्चिम की ओर को सायबान पर, जिसका सामनेवाला बाजू खुला है-हिंडोले पर बैठी वह सुंदर-सलोनी, छरछरे बदन की किशोरी अपने सुरीले गीत की मधुरता का स्वयं ही आस्वाद लेती हुई ऊँची पेंगे भरने लगी। हिंडोला जब एक ओर की ऊँचाई से नीचे उतरता तब हवा के झोको से उसका आँचल फड़फड़ाता हुआ लहराता रहता। तब ऐसा प्रतीत होता कि संधया समय सुंदर पक्षियों का झुंड अपने सुदूर नीड़ की ओर उड़ रहा है और उस झुंड में एक पखेरू पीछे रह गया है, जो पंख फैलाकर आलाप के पीछे आलाप छेड़ते हुए पता नहीं कब हर्षोल्लास के आकाश में उड़ जाएगा।
अरी ओ रत्नों की खानि ! इस तरह मत इतराना। देखो तो सही, मेरी कोख से तो इस सुंदर रत्न ‘माला’ ने जन्म लिया है।
(2) हे राजकुमार आते-जाते इस तरह ललचाई दृष्टि से मत देखो, मेरी मालती को नजर लग जाएगी।
(3) मेरे सात जन्मों का सारा पुण्य संचय, हे श्रीहरि ! मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ, मेरी मालती की रक्षा करो !
(4) हे नारायण ! मेरी इकलौती कन्या मुझे आजन्म मिले।)
गाने की धुन में ‘इकलौती’ शब्द का उच्चारण करते ही रमा देवी को यों लगा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा है। किसी तीव्र गति की स्मृति से उनका मन कसमसाने लगा। ऐसे हर्षोल्लास की घड़ी में उनकी बेटी को भी यह कसक न हो, वह भी उदास न हो, इसलिए रमा देवी ने अपने चेहरे पर उदासी का साया तक नहीं उभरने दिया; फिर भी उनके कंठ में गीत अटक-सा गया। मालती ने सोचा, गाते-गाते माँ को अचानक साँस फूल जाने से वह अचानक चुप हो गई हैं। माँ को तनिक विश्वास मिले और उनकी गाने की मधुर ध्वनि बँध गई है वह टूट न जाए, इसलिए यह समझकर कि अब उसकी बारी है, वह अपनी अगली ओवियाँ गाने लगी। उसकी माँ ने उसके लिए ममता से लबालब भरी जो ओवियाँ गाई थी, उलकी मिठास से भरपूर हर शब्द के साथ उसके दिल में हर्ष भरी गुदगुदियाँ हो रही थीं।
अपने साजन की प्रेमपूर्ण आराधना की आस लगने से पहले लड़कियों के माँ के प्यार-दुलार भरे कौतुक में जितनी रूचि होती है, उतनी अन्य किसी में भी नहीं।
संध्या की बेला में पश्चिम की ओर को सायबान पर, जिसका सामनेवाला बाजू खुला है-हिंडोले पर बैठी वह सुंदर-सलोनी, छरछरे बदन की किशोरी अपने सुरीले गीत की मधुरता का स्वयं ही आस्वाद लेती हुई ऊँची पेंगे भरने लगी। हिंडोला जब एक ओर की ऊँचाई से नीचे उतरता तब हवा के झोको से उसका आँचल फड़फड़ाता हुआ लहराता रहता। तब ऐसा प्रतीत होता कि संधया समय सुंदर पक्षियों का झुंड अपने सुदूर नीड़ की ओर उड़ रहा है और उस झुंड में एक पखेरू पीछे रह गया है, जो पंख फैलाकर आलाप के पीछे आलाप छेड़ते हुए पता नहीं कब हर्षोल्लास के आकाश में उड़ जाएगा।
माउलीवी माया। न ये आणिकाला।
पोवळया माणिकाया। रंग चढ़े।।1।।
न ये आणिकाला। माया ही माउलीची।
छाया देवाच्या दयेची। भूमीवरी।।2।।
माउलीची माया। कन्या-पुत्रांत वांटली।
वाट्या प्रत्येकाच्या तरी। सारीचि ये।।3।।
जीवाला देते जीव। जीव देईन आपूला।
चाफा कशाने सूकला। भाई राजा।।4।।
माझं ग आयुष्य। कमी करोनी मारूती।
घाल शंभर पूरतीं। भाई राजा।।5।।
पोवळया माणिकाया। रंग चढ़े।।1।।
न ये आणिकाला। माया ही माउलीची।
छाया देवाच्या दयेची। भूमीवरी।।2।।
माउलीची माया। कन्या-पुत्रांत वांटली।
वाट्या प्रत्येकाच्या तरी। सारीचि ये।।3।।
जीवाला देते जीव। जीव देईन आपूला।
चाफा कशाने सूकला। भाई राजा।।4।।
माझं ग आयुष्य। कमी करोनी मारूती।
घाल शंभर पूरतीं। भाई राजा।।5।।
(अर्थः(1) माँ की ममता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मूँगा-माणिक रत्नों पर
रंग छा जाता है।
(2) माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। वह ईश्वर की दया पर बिखरी हुई छाया है।
(3) माँ की ममता कन्या-पुत्रों में बाँटने पर भी सभी के हिस्से में संपूर्ण रूप में ही आती है।
(4) हे भाई राजा ! मैं आप के लिए अपनी जान दे दूँगी ! यह चंपा का फूल क्यों सूख गया ?
(5) हे बजरंगबली ! मेरी आयु कम करके मेरे राजा भैया के सौ साल पूरे करो !)
गीतों के बहाव में जो मुँह में आया, मालती वहीं ओवी गाती जा रही थी। पहली ओवियाँ उसकी अपनी मन की बोलियों में रची हुई थीं। अपनी माँ से जो उसे जो लाड़-दुलार भरी ममता थी, उन्हीं गीतों को चुन-चुनकर वह अपने कंठ की शहनाई तक गा रही थी। परंतु अगली ओवियाँ अर्थ के लिए चुनकर नहीं गाई गई थीं। वह वैसे ही गाती गई, जैसे कोई मराठी गायक पदों के अर्थ पर खास गौर न करते हुए उस गीत की धुन के कारण वह गाता है। परंतु उसकी माँ का ध्यान उन ओवियों के अर्थ की ओर भी था, अतः मालती गाने के बहाव में जब वह ओवियाँ गाती गई, जो उसके भाई राजा पर लागू होती थीं, तब उसकी माँ की छाती दुःख से रूध गई और उसे दुख लगने लगा कि अब रोई, कि तब रोई। उनके दुख का साया मालती के उस हँसते-खेलते हर्षोल्लास पर पड़ने से वह स्याह न हो, इसलिए रमा देवी ने मालती की ओवियाँ, जो अब असहनीय हो रहा थीं, बंद करने के लिए उसे बीच में टोका, ‘‘माला, बेटी अब रूक जा। भई, मुझे तो अब चक्कर सा आने लगा है। कितनी ऊँची-ऊँची पेंगें भर रहीं हो ।’’ ऐसा ही कुछ बहानाकर माँ ने अपने पैरों का जोर देकर हिंडोला रोका। उसको साथ ही न केवल मालती ही झूने से नीचे उरती, उसका मन भी, जो ऊँचे-ऊँचे आलापों के झोंको पर सवार होकर मदहोश हो गया था, उन गीतों के हिंडोले से नीचे उतरकर होश में आ गया।
उसने देखा तो माँ के नयन आँसुओं से भीगे हुए थे। दुःखावेग की तीव्र स्मृति से चेहरे का रंग पीला पड़ गया मालती को तुरंत स्मरण हो गया कि अरे हाँ, अपने लापता भैया की स्मृति से अम्मा दुःखी हो गई है। अपने मुख से सहजतापूर्वक निकली हुई ओवियों को, जिनमें भैया का वर्णन है, सुनकर अम्मा का मन बिहल हो उठा है। उस हादसे को इतने साल बीतने के बाद भी उसकी माँ को अपने गुमशुदा बेटे की स्मृति कभी-कभी इस तरह प्रसंगवशात् असहनीय होती थी, जैसे दुःख का ताजा घाव हो और फिर वह ममता की मूरत फूट-फूटकर रोया करती। मालती जानती थी, उस सनय अम्मा को किस तरह समझाना है। वह यह भी जानती थी कि कौन सा इलाज है, जो माँ के दुःख को टाल तो नहीं सकता पर अचेत और संवेदनाशून्य बना सकता है।
उसने झट से माँ की गोद पर अपना सिर रख दिया। उसके साथ अपने आप उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आँखें भर आईं और अपनी आदत के अनुसार अपना चेहरा माँ की ठोड़ी से सटाकर अकुलाते हुए उसने कहा, ‘‘नहीं, ऐसा दिल छोटा नहीं करते, अम्मा ! मैं तो तुम्हारें मन को रिझाने के लिए गा रही थी और तुम्हारे दुःख का घाव ताजा हो गया और वह झट से अपना मुखड़ा समेटकर मालती को ढाढ़स बँधाने लगीं।
‘‘चल, पगली, कहीं की ! अरी बावली तुम्हारे गीतों के कारण नहीं, मैं ही ओवी गाते-गाते ‘मेरा बबुआ’ कह गई न, उसी का मुझे दुःख हुआ। भगवान् ने मेरी झोली में दो-दो बच्चे डाले थे, पर हाय ! नियति ने एक को मुझसे छीनकर बस एक ही मेरे लिए बाकी रखा-यही कसक मुझे अचानक चुभ गई। मत रो बेटी, मत रो। चुप हो जा। तुमने नेरा जख्म हरा नहीं किया बल्कि तुम्हारे खिले-खिले मुख पर थिरकती सुखद मुस्कान ही वह रसायन है जो इस दुख को तनिक हल्का कर सके। जो बीत गया सो बीत गई, वह वापस थोड़े ही आनेवाला है ! तेरा भाई तुझपर इतना जान झिड़कता था कि यदि मैंने तुझे उसके वियोग के दुख से भी रुलाया तो भी वह मुझसे नाराज होगा। उसकी आत्मा जहा कहीं भी होगी, उसी स्थान पर तड़पेगी। तुमने तो उसका स्थान ले ही लिया है। न, न, चुप हो जा, अरी हाँ, आज उस नए आए हुए साधू महाराज का भजन सुनने चलेगे न, ! चल उठ, मैं चूल्हा जलाती हूँ, तुम झाँड़-बुहाड़कर खाना बनाने की तैयारी करो। भोजन आदि से निपटते ही नायडू बहनजी बुलाने के लिए आ जाएँगी।’’
माँ-बेटी भीतर चली गईं। रमा देवी ने एक शानदार मकान पिछले महीने ही मथुरा में रहने के लिए स्वतंत्र रूप से किराये पर लिया था।
रमा देवी के पति का दो बच्चो के पिता होने के बाद अचानक स्वर्गवास हो गया। उनके पति ने रमा देवी के इतना पैसा और जेवरात छोड़े थे, जिससे उनकी दाल-रोटी आराम से चल सके। उसी के सहारे कुछ नागपुर के पास अपने गाँव में रमा देवी ने अपने दोनों बच्चों को पाला-पोसा था। आगे चलकर उनका बेटा जब फौज में भर्ती हो गया तब उनकी बेटी मालती ही उनके पास बची थी। दो-चार वर्षों से ही हिंदुस्थान से बाहर अंग्रेजों से छिड़े किसी युद्ध में भारतीय फौज भेजी गई। उसमें रमा देवी के पुत्र को भी जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वह लापता हो गया। बड़ी दौड़-धूप, कोशिशों के बाद रमा देवी को अफसरों से पता चला कि वह फौजी कुछ कारणवश अफसरों से लड़-झगड़कर फरार हो गया और हो सकता है, दुश्मनी के हाँथों मारा गया हो।
(2) माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। वह ईश्वर की दया पर बिखरी हुई छाया है।
(3) माँ की ममता कन्या-पुत्रों में बाँटने पर भी सभी के हिस्से में संपूर्ण रूप में ही आती है।
(4) हे भाई राजा ! मैं आप के लिए अपनी जान दे दूँगी ! यह चंपा का फूल क्यों सूख गया ?
(5) हे बजरंगबली ! मेरी आयु कम करके मेरे राजा भैया के सौ साल पूरे करो !)
गीतों के बहाव में जो मुँह में आया, मालती वहीं ओवी गाती जा रही थी। पहली ओवियाँ उसकी अपनी मन की बोलियों में रची हुई थीं। अपनी माँ से जो उसे जो लाड़-दुलार भरी ममता थी, उन्हीं गीतों को चुन-चुनकर वह अपने कंठ की शहनाई तक गा रही थी। परंतु अगली ओवियाँ अर्थ के लिए चुनकर नहीं गाई गई थीं। वह वैसे ही गाती गई, जैसे कोई मराठी गायक पदों के अर्थ पर खास गौर न करते हुए उस गीत की धुन के कारण वह गाता है। परंतु उसकी माँ का ध्यान उन ओवियों के अर्थ की ओर भी था, अतः मालती गाने के बहाव में जब वह ओवियाँ गाती गई, जो उसके भाई राजा पर लागू होती थीं, तब उसकी माँ की छाती दुःख से रूध गई और उसे दुख लगने लगा कि अब रोई, कि तब रोई। उनके दुख का साया मालती के उस हँसते-खेलते हर्षोल्लास पर पड़ने से वह स्याह न हो, इसलिए रमा देवी ने मालती की ओवियाँ, जो अब असहनीय हो रहा थीं, बंद करने के लिए उसे बीच में टोका, ‘‘माला, बेटी अब रूक जा। भई, मुझे तो अब चक्कर सा आने लगा है। कितनी ऊँची-ऊँची पेंगें भर रहीं हो ।’’ ऐसा ही कुछ बहानाकर माँ ने अपने पैरों का जोर देकर हिंडोला रोका। उसको साथ ही न केवल मालती ही झूने से नीचे उरती, उसका मन भी, जो ऊँचे-ऊँचे आलापों के झोंको पर सवार होकर मदहोश हो गया था, उन गीतों के हिंडोले से नीचे उतरकर होश में आ गया।
उसने देखा तो माँ के नयन आँसुओं से भीगे हुए थे। दुःखावेग की तीव्र स्मृति से चेहरे का रंग पीला पड़ गया मालती को तुरंत स्मरण हो गया कि अरे हाँ, अपने लापता भैया की स्मृति से अम्मा दुःखी हो गई है। अपने मुख से सहजतापूर्वक निकली हुई ओवियों को, जिनमें भैया का वर्णन है, सुनकर अम्मा का मन बिहल हो उठा है। उस हादसे को इतने साल बीतने के बाद भी उसकी माँ को अपने गुमशुदा बेटे की स्मृति कभी-कभी इस तरह प्रसंगवशात् असहनीय होती थी, जैसे दुःख का ताजा घाव हो और फिर वह ममता की मूरत फूट-फूटकर रोया करती। मालती जानती थी, उस सनय अम्मा को किस तरह समझाना है। वह यह भी जानती थी कि कौन सा इलाज है, जो माँ के दुःख को टाल तो नहीं सकता पर अचेत और संवेदनाशून्य बना सकता है।
उसने झट से माँ की गोद पर अपना सिर रख दिया। उसके साथ अपने आप उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आँखें भर आईं और अपनी आदत के अनुसार अपना चेहरा माँ की ठोड़ी से सटाकर अकुलाते हुए उसने कहा, ‘‘नहीं, ऐसा दिल छोटा नहीं करते, अम्मा ! मैं तो तुम्हारें मन को रिझाने के लिए गा रही थी और तुम्हारे दुःख का घाव ताजा हो गया और वह झट से अपना मुखड़ा समेटकर मालती को ढाढ़स बँधाने लगीं।
‘‘चल, पगली, कहीं की ! अरी बावली तुम्हारे गीतों के कारण नहीं, मैं ही ओवी गाते-गाते ‘मेरा बबुआ’ कह गई न, उसी का मुझे दुःख हुआ। भगवान् ने मेरी झोली में दो-दो बच्चे डाले थे, पर हाय ! नियति ने एक को मुझसे छीनकर बस एक ही मेरे लिए बाकी रखा-यही कसक मुझे अचानक चुभ गई। मत रो बेटी, मत रो। चुप हो जा। तुमने नेरा जख्म हरा नहीं किया बल्कि तुम्हारे खिले-खिले मुख पर थिरकती सुखद मुस्कान ही वह रसायन है जो इस दुख को तनिक हल्का कर सके। जो बीत गया सो बीत गई, वह वापस थोड़े ही आनेवाला है ! तेरा भाई तुझपर इतना जान झिड़कता था कि यदि मैंने तुझे उसके वियोग के दुख से भी रुलाया तो भी वह मुझसे नाराज होगा। उसकी आत्मा जहा कहीं भी होगी, उसी स्थान पर तड़पेगी। तुमने तो उसका स्थान ले ही लिया है। न, न, चुप हो जा, अरी हाँ, आज उस नए आए हुए साधू महाराज का भजन सुनने चलेगे न, ! चल उठ, मैं चूल्हा जलाती हूँ, तुम झाँड़-बुहाड़कर खाना बनाने की तैयारी करो। भोजन आदि से निपटते ही नायडू बहनजी बुलाने के लिए आ जाएँगी।’’
माँ-बेटी भीतर चली गईं। रमा देवी ने एक शानदार मकान पिछले महीने ही मथुरा में रहने के लिए स्वतंत्र रूप से किराये पर लिया था।
रमा देवी के पति का दो बच्चो के पिता होने के बाद अचानक स्वर्गवास हो गया। उनके पति ने रमा देवी के इतना पैसा और जेवरात छोड़े थे, जिससे उनकी दाल-रोटी आराम से चल सके। उसी के सहारे कुछ नागपुर के पास अपने गाँव में रमा देवी ने अपने दोनों बच्चों को पाला-पोसा था। आगे चलकर उनका बेटा जब फौज में भर्ती हो गया तब उनकी बेटी मालती ही उनके पास बची थी। दो-चार वर्षों से ही हिंदुस्थान से बाहर अंग्रेजों से छिड़े किसी युद्ध में भारतीय फौज भेजी गई। उसमें रमा देवी के पुत्र को भी जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वह लापता हो गया। बड़ी दौड़-धूप, कोशिशों के बाद रमा देवी को अफसरों से पता चला कि वह फौजी कुछ कारणवश अफसरों से लड़-झगड़कर फरार हो गया और हो सकता है, दुश्मनी के हाँथों मारा गया हो।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book