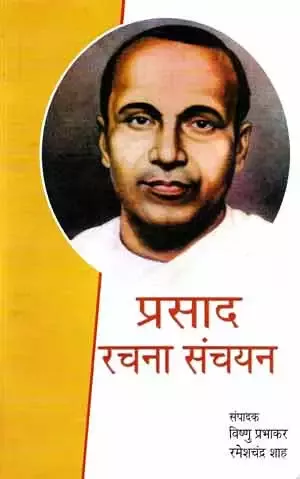|
संचयन >> प्रसाद रचना संचयन प्रसाद रचना संचयनविष्णु प्रभाकर, रमेशचंद्र शाह
|
444 पाठक हैं |
|||||||
प्रसाद जी की सृजनात्मक कल्पना जहाँ एक ओर मानवीय करूणा से सम्बद्ध और प्रतिबद्ध रही है वहीं दूसरी ओर आनन्दवाद के प्रति समर्पित भी।
Prasad Rachana Sanchyan - A hindi Book by - Vishnu Prabhakar प्रसाद रचना संचयन - विष्णु प्रभाकर, रमेशचंद्र शाह
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रसाद के नाटकों (विशाख, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, एक घूँट, ध्रुवस्वामिनी आदि) पर भी उनका काव्यकार पक्ष हावी रहा है और उसमें जीवन और जगत के अनिवार्य संघर्ष की मुखर अभिव्यक्ति भी सूक्ष्मतर ढंग से होती रही। चूँकि उनका काव्य-चिन्तन शैव दर्शन से प्रभावित था इसलिए भारतीय पुरूषार्थवाद के आलोक में वे मानव मन को उद्धिग्न और अंतर्मथित करनेवाले शाश्वत प्रश्नों के समुचित उत्तर भी ढूँढ़ सके। ऐसा करते हुए उन्होंने भारत की सांस्कृतिक अवधारणाओं, अभिप्रायों और प्रेरणाओं का यथोचित्त एवं रचनात्मक विनियोग किया। उनकी सृजनात्मक कल्पना जहाँ एक ओर मानवीय करूणा से सम्बद्ध और प्रतिबद्ध रही है वहाँ दूसरी ओर आनन्दवाद के प्रति समर्पित भी।
अपने विचारप्रधान निबंधों पर भी प्रसाद जी के वैदुष्य का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। विषयानुरूप भाव और भाषा के साथ ही वे अपने पाठकों का रूचि-संस्कार भी करते जाते हैं, जो उनके लेखन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि कथा-साहित्य (कहानी एवं उपन्यास) में उन्होंने प्राचीन और आधुनिक भारतीय दृष्टि का स्वस्थ समन्वय प्रस्तुत किया और उनकी मानवीय दृष्टि कभी धुँधली नहीं हुई। अड़तालीस वर्ष की छोटी-सी आयु में उनका निधन आज भी भारतीय साहित्य की अपूरणीय क्षति के रूप में याद किया जाता है।
अकादेमी को इस बात की प्रसन्नता है कि जयशंकर प्रसाद जी की चुनी हुई रचनाएँ प्रस्तुत संचयन में और एक ही जिल्द में पाठक तक पहुँच रही हैं। इस संचयन के लिए प्रतिनिधि सामग्री का संकलन हिन्दी के वरिष्ट कथाकार, नाटककार और चिन्तक श्री विष्णु प्रभाकर और प्रबुद्ध लेखक-कवि-समीक्षक श्री रमेशचन्द्र शाह ने किया है और एक उपयोगी भूमिका भी लिखी है।
आशा है, साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित अन्य संचयनों की तरह यह संचयन भी हिन्दी के सुधी पाठकों के बीच विशिष्ट स्थान बना सकेगा।
जिन भारतीय साहित्यकारों ने अपनी मौलिक प्रतिभा और रचना मनीषा द्वारा समस्त भारतीय साहित्य को आन्दोलित किया, विपुल साहित्य-सर्जना न केवल समकालीनों को बल्कि परवर्ती पीढ़ियों को भी प्रभावित किया-उनके रचना-संसार का श्रेष्ठांश सुलभ मूल पर अधिकाधिक पाठकों तक पहुँचाने का संकल्प साहित्य अकादेमी ने किया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के विशिष्ट हस्ताक्षरों के प्रतिनिधि रचनाओं का प्रकाशन बहुत लोकप्रिय हुआ है। इन संचयनों के लिए सामग्री का चयन किसी अधिकारी विद्वान या सम्पादन-मंडल के अधीन कराया जाता है और विशद एंव विद्वात्तापूर्ण भूमिका के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि इन विशिष्ट रचनाकारों के ऐतिहासिक योगदान और रचना कर्म को व्यापक परिदृश्य में रखकर देखा जा सके। इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में रवीन्द्र रचना संचयन (सम्पादक : असितकुमारक बन्द्योपाध्याय) तथा मुक्तिबोध की कविताएँ (सम्पादक : त्रिलोचन शास्त्री) का प्रकाशन किया जा चुका है।
अपने विचारप्रधान निबंधों पर भी प्रसाद जी के वैदुष्य का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। विषयानुरूप भाव और भाषा के साथ ही वे अपने पाठकों का रूचि-संस्कार भी करते जाते हैं, जो उनके लेखन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि कथा-साहित्य (कहानी एवं उपन्यास) में उन्होंने प्राचीन और आधुनिक भारतीय दृष्टि का स्वस्थ समन्वय प्रस्तुत किया और उनकी मानवीय दृष्टि कभी धुँधली नहीं हुई। अड़तालीस वर्ष की छोटी-सी आयु में उनका निधन आज भी भारतीय साहित्य की अपूरणीय क्षति के रूप में याद किया जाता है।
अकादेमी को इस बात की प्रसन्नता है कि जयशंकर प्रसाद जी की चुनी हुई रचनाएँ प्रस्तुत संचयन में और एक ही जिल्द में पाठक तक पहुँच रही हैं। इस संचयन के लिए प्रतिनिधि सामग्री का संकलन हिन्दी के वरिष्ट कथाकार, नाटककार और चिन्तक श्री विष्णु प्रभाकर और प्रबुद्ध लेखक-कवि-समीक्षक श्री रमेशचन्द्र शाह ने किया है और एक उपयोगी भूमिका भी लिखी है।
आशा है, साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित अन्य संचयनों की तरह यह संचयन भी हिन्दी के सुधी पाठकों के बीच विशिष्ट स्थान बना सकेगा।
जिन भारतीय साहित्यकारों ने अपनी मौलिक प्रतिभा और रचना मनीषा द्वारा समस्त भारतीय साहित्य को आन्दोलित किया, विपुल साहित्य-सर्जना न केवल समकालीनों को बल्कि परवर्ती पीढ़ियों को भी प्रभावित किया-उनके रचना-संसार का श्रेष्ठांश सुलभ मूल पर अधिकाधिक पाठकों तक पहुँचाने का संकल्प साहित्य अकादेमी ने किया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के विशिष्ट हस्ताक्षरों के प्रतिनिधि रचनाओं का प्रकाशन बहुत लोकप्रिय हुआ है। इन संचयनों के लिए सामग्री का चयन किसी अधिकारी विद्वान या सम्पादन-मंडल के अधीन कराया जाता है और विशद एंव विद्वात्तापूर्ण भूमिका के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि इन विशिष्ट रचनाकारों के ऐतिहासिक योगदान और रचना कर्म को व्यापक परिदृश्य में रखकर देखा जा सके। इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी में रवीन्द्र रचना संचयन (सम्पादक : असितकुमारक बन्द्योपाध्याय) तथा मुक्तिबोध की कविताएँ (सम्पादक : त्रिलोचन शास्त्री) का प्रकाशन किया जा चुका है।
प्राक्कथन
हिन्दी साहित्य के इतिहास में जो युग ‘छायावाद’ के नाम से जाना जाता है, वह मुख्यताः चार बड़ी प्रतिभा वाले कवियों की सर्जनात्मक ऊर्जा से आलोकित है : प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी। एक शक्तिशाली काव्यान्दोलन को, जिसमें एक साथ इतनी विविध और विलक्षण प्रतिभाओं का योगदान रहा हो, उसे परिभाषित करने के लिए ‘छायावाद’ संज्ञा उपयुक्त नहीं जान पड़ती। इस आन्दोलन का आरम्भ और राष्ट्रीय रंगमंच पर गाँधीजी के नेतृत्व का आविर्भाव लगभग आस-पास ही हुआ। कवि आलोचक विजयदेव नारायण साही ने इसलिए इस युग को सत्याग्रह-युग की संज्ञा दी है, जोकि, निश्चय ही अधिक अपयुक्त और तर्कसंगत है। इसमें संदेह नहीं, कि ‘सत्य को अन्तर्ध्वनित होते हुए पकड़ने’ की गाँधीजी की शैली में और ‘सत्य को उसके मूल चारुत्व में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति से ग्रहण कर लेने’ के प्रसादीय आग्रह के बीच कहीं कोई गहरा संबंध है अवश्य। ‘कामायनी’ के इड़ा सर्ग में विक्षुब्ध प्रजा मनु पर एक ओर तो यह आरोप लगाती है कि ‘‘तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला/लोभ सिखाकर इस विचार संकट में डाला’’, और दूसरी ओर यह भी कि.....‘‘प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी/शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर, झीनी’’।
कहना न होगा, जयशंकर प्रसाद के कवित्व में निहित यह ‘जीवन के आलोचना’ सत्याग्रह युग की केन्द्रीय अनुभूति और विचार-दृष्टि के मेल में ही है। आख़िर अंग्रेज़ी राज के शैतानी चरित्र का साक्षात्कार गाँधी जी को भी एकाएक नहीं हो गया था। धीरे-धीरे ही वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे और तब भी उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी। वे इस मुक्ति-चेष्टा की नीव को ही मजबूत बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने देश के ‘अर्धक्षुधित, शोषित निरस्त्रजन’ के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था। इसी तादात्म्य के फलस्वरूप वे समझ सके थे कि कोरी ‘राजनीति’ या कोरी ‘संस्कृति’ के द्वारा जनजागरण की दुहाई देने से काम चलने वाला नहीं है बजाए इस तरह की कल्पनाओं से अपने को बहलाने के, गाँधीजी ने समाज की आर्थिक मानसिक पुनर्रचना के उद्देश्य से नियोजित एक गहन रंचनात्मक कार्यक्रम सामने रक्खा था और बताया था कि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम सामूहिक आत्मनिर्भर और सामूहिक दायित्व-भावना का विकास कर सकते हैं, जिसके बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं।
ठोस व्यवहारिक बुद्धि के धनी प्रसादजी निश्चय ही इस विवेक के कायल रहे होंगे। स्वयं उनके काव्य और नाटकों में सर्वत्र रचे हुए ‘करुणा’ के तत्व का इस संदर्भ में स्मरण आना स्वाभाविक है। किंतु इस समानता के साथ की ओर भी ध्यान जाता है और वह है- करुणा के साथ-साथ ‘आनन्द’ पर प्रसाद जी का आग्रह। यह आनन्दवाही दर्शन-जो उनके समस्त लेखन का मूलाधार सरीखा है, मात्र एक अतीत-युग की मानसिकता को पुनर्जीवित करने का पलायन वादी उपक्रम नहीं है। प्रसाद जी का समग्र कृतित्व इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जीवन और संसार की निरपवाद स्वीकृति का यह दर्शन- जोकि उदासीनता से एकदम अलग चीज़ है- मानव-जीवन में निहित द्धैत के गहरे करुण्य बोध की अनुभूति के मूल्यवान नहीं हो सकता। यह आनन्दवाद महज यूनानी ‘एपिक्योरिनिज़्म’ या चार्वाकीय सुखवाद नहीं है। उनके काव्य में जो दो शब्द बीज-शब्दों की तरह बार-बार प्रयुक्त हुए हैं, वे हैं -‘मधु’ और ‘करुणा’। यही पर्याप्त संकेत है कि उनकी मूल्य-चेतना और जीवनानुभूति में एक दोहरी संवेदना और दोहरा विवेक निरन्तर सक्रिय रहे हैं। करुणा प्रमुखतः बौद्ध अन्तर्दृष्टि है, जबकि ‘मधु’ वैदिक आर्यों के जीवन बोध में निहित अन्तःस्फूर्ति और सृष्टि-सामान्य पर जोर देनेवाला तत्त्व।
यों, हिन्दी साहित्य में नवीन राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हो चुका था जो कि कई मानों में प्रसाद जी के अग्रज थे। इस साहित्यिक संबंध पर बल देना इसलिए जरूरी जान पड़ता है कि जयशंकर प्रसाद के न केवल गद्य-साहित्य में बल्कि काव्य-कृतित्व में भी हमें उस मौलिक मानविष्ठ दृष्टि का भरपूर परिपारक मिलता है जिसका आरंभिक बीज हम भारतेंदु में ढूँढ़ सकते हैं। प्रसाद के कृतित्व के आस्वादन और मूल्यांकन में यह बात बुनियादी महत्त्व की है और इसका थोड़ा खुलासा यहाँ ज़रूरी होगा।
प्रसाद का वैशिष्ट्य करुणा और आनन्द के अतिरिक्त जिन दो तत्वों से प्रेरित है, वे है उनका इतिहास-बोध और आत्म-बोध। पहली दृष्टि में परस्पर विरोधी लगते हुए भी ये दोनों चीज़ें उनके कृतित्व में इतने अविच्छेद्य रूप में जुड़ी हुई हैं कि लगता है, दोनों का विकास दो लगातार पास आती हुई और अंत में एक बिन्दु पर मिल जाने वाली रेखाओं की तरह हुआ। यह बिन्दु निश्चय ही ‘कामायनी’ है। किन्तु इस परिर्णात के काफ़ी पहले भी हम लगातार देख सकते है कि उनका कृतित्व अपने इतिहास-बोध के कारण ही अपनी उतनी ही विशिष्ट चारित्रिक पहचान बनाने लगा है, जितना कि अपने उत्कट आत्मबोध के कारण। प्रसाद के जीवन और कृत्तित्त का जो असली संघर्ष है, वह एक एकाकीकृत भावबोध की उपलब्धि का संघर्ष है। व्यक्तिगत विषाद से उन्मोचन विश्व-वेदना की प्रगाड़ अनुभूति में, और उस अनुभूति को अपनी सांस्कृतिक चेतना एवं इतिहास बोध के माध्यम से सर्वजनिक सार्थकता देने की प्रेरणा-इसी में से प्रसाद जी की रचनात्मक सिद्धि का वृत्त बनता है। एक ओर से पढ़ते हैं:-
कहना न होगा, जयशंकर प्रसाद के कवित्व में निहित यह ‘जीवन के आलोचना’ सत्याग्रह युग की केन्द्रीय अनुभूति और विचार-दृष्टि के मेल में ही है। आख़िर अंग्रेज़ी राज के शैतानी चरित्र का साक्षात्कार गाँधी जी को भी एकाएक नहीं हो गया था। धीरे-धीरे ही वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे और तब भी उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं थी। वे इस मुक्ति-चेष्टा की नीव को ही मजबूत बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने देश के ‘अर्धक्षुधित, शोषित निरस्त्रजन’ के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया था। इसी तादात्म्य के फलस्वरूप वे समझ सके थे कि कोरी ‘राजनीति’ या कोरी ‘संस्कृति’ के द्वारा जनजागरण की दुहाई देने से काम चलने वाला नहीं है बजाए इस तरह की कल्पनाओं से अपने को बहलाने के, गाँधीजी ने समाज की आर्थिक मानसिक पुनर्रचना के उद्देश्य से नियोजित एक गहन रंचनात्मक कार्यक्रम सामने रक्खा था और बताया था कि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम सामूहिक आत्मनिर्भर और सामूहिक दायित्व-भावना का विकास कर सकते हैं, जिसके बिना राजनीतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं।
ठोस व्यवहारिक बुद्धि के धनी प्रसादजी निश्चय ही इस विवेक के कायल रहे होंगे। स्वयं उनके काव्य और नाटकों में सर्वत्र रचे हुए ‘करुणा’ के तत्व का इस संदर्भ में स्मरण आना स्वाभाविक है। किंतु इस समानता के साथ की ओर भी ध्यान जाता है और वह है- करुणा के साथ-साथ ‘आनन्द’ पर प्रसाद जी का आग्रह। यह आनन्दवाही दर्शन-जो उनके समस्त लेखन का मूलाधार सरीखा है, मात्र एक अतीत-युग की मानसिकता को पुनर्जीवित करने का पलायन वादी उपक्रम नहीं है। प्रसाद जी का समग्र कृतित्व इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जीवन और संसार की निरपवाद स्वीकृति का यह दर्शन- जोकि उदासीनता से एकदम अलग चीज़ है- मानव-जीवन में निहित द्धैत के गहरे करुण्य बोध की अनुभूति के मूल्यवान नहीं हो सकता। यह आनन्दवाद महज यूनानी ‘एपिक्योरिनिज़्म’ या चार्वाकीय सुखवाद नहीं है। उनके काव्य में जो दो शब्द बीज-शब्दों की तरह बार-बार प्रयुक्त हुए हैं, वे हैं -‘मधु’ और ‘करुणा’। यही पर्याप्त संकेत है कि उनकी मूल्य-चेतना और जीवनानुभूति में एक दोहरी संवेदना और दोहरा विवेक निरन्तर सक्रिय रहे हैं। करुणा प्रमुखतः बौद्ध अन्तर्दृष्टि है, जबकि ‘मधु’ वैदिक आर्यों के जीवन बोध में निहित अन्तःस्फूर्ति और सृष्टि-सामान्य पर जोर देनेवाला तत्त्व।
यों, हिन्दी साहित्य में नवीन राष्ट्रीय चेतना का सूत्रपात भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हो चुका था जो कि कई मानों में प्रसाद जी के अग्रज थे। इस साहित्यिक संबंध पर बल देना इसलिए जरूरी जान पड़ता है कि जयशंकर प्रसाद के न केवल गद्य-साहित्य में बल्कि काव्य-कृतित्व में भी हमें उस मौलिक मानविष्ठ दृष्टि का भरपूर परिपारक मिलता है जिसका आरंभिक बीज हम भारतेंदु में ढूँढ़ सकते हैं। प्रसाद के कृतित्व के आस्वादन और मूल्यांकन में यह बात बुनियादी महत्त्व की है और इसका थोड़ा खुलासा यहाँ ज़रूरी होगा।
प्रसाद का वैशिष्ट्य करुणा और आनन्द के अतिरिक्त जिन दो तत्वों से प्रेरित है, वे है उनका इतिहास-बोध और आत्म-बोध। पहली दृष्टि में परस्पर विरोधी लगते हुए भी ये दोनों चीज़ें उनके कृतित्व में इतने अविच्छेद्य रूप में जुड़ी हुई हैं कि लगता है, दोनों का विकास दो लगातार पास आती हुई और अंत में एक बिन्दु पर मिल जाने वाली रेखाओं की तरह हुआ। यह बिन्दु निश्चय ही ‘कामायनी’ है। किन्तु इस परिर्णात के काफ़ी पहले भी हम लगातार देख सकते है कि उनका कृतित्व अपने इतिहास-बोध के कारण ही अपनी उतनी ही विशिष्ट चारित्रिक पहचान बनाने लगा है, जितना कि अपने उत्कट आत्मबोध के कारण। प्रसाद के जीवन और कृत्तित्त का जो असली संघर्ष है, वह एक एकाकीकृत भावबोध की उपलब्धि का संघर्ष है। व्यक्तिगत विषाद से उन्मोचन विश्व-वेदना की प्रगाड़ अनुभूति में, और उस अनुभूति को अपनी सांस्कृतिक चेतना एवं इतिहास बोध के माध्यम से सर्वजनिक सार्थकता देने की प्रेरणा-इसी में से प्रसाद जी की रचनात्मक सिद्धि का वृत्त बनता है। एक ओर से पढ़ते हैं:-
‘‘वेदना-विकल यह चेतन
जड़ का पीड़ा से नर्तन
लय-सीमा में यह कम्पन
अभिनयमय है परिवर्तन
चल रहा कभी से यह कुढ़ंग’’
जड़ का पीड़ा से नर्तन
लय-सीमा में यह कम्पन
अभिनयमय है परिवर्तन
चल रहा कभी से यह कुढ़ंग’’
तो दूसरी ओर, ‘कामायनी’ तक आते-आते :
‘‘मैं की मेरी चेतनता
सबको ही स्पर्श किये-सी
सब भिन्न परिस्थितियों की
है मादक घूँट पिये-सी।’’
सबको ही स्पर्श किये-सी
सब भिन्न परिस्थितियों की
है मादक घूँट पिये-सी।’’
इन ‘भिन्न’ परिस्थियों पर भी एक नज़र डाल लेना यहाँ ठीक होगा। प्रसाद जी का जन्म मात शुल्क दशमी संवत् 1946 सन् 1889 के दिन काशी के एक सम्पन्न और यशस्वी घराने में हुआ था। चूँकी यह परिवार अपने विद्याप्रेम और औदार्य के लिए विख्यात था, अतः विद्धानों, कवियों, संगीतज्ञों का उनके यहाँ जमघट लगा रहता था। पाठकों और बलूची स्त्रियों से लगातार नेपाल, भूटान के कस्तूरीफ़रोशो तक, महापंडितों से लेकर जादू-टोने वालों तक, साधुओं से लेकर पाखंडियों तक, मानव-चरित्र का शायद ही कोई नमूना हो जो उस रंगमंच पर न उतरा हो। ऐसे में संवेदनशील बालक जयशंकर के चित्त पर जीवन-लीला का यह विराट वैविध्य अंकित होना ही था। यह परिवार शैव था। कहा जा सकता है कि शिवोपासना ही नहीं, शैव दर्शन के चिंतन-मनन की भी एक सुदीर्घ परम्परा प्रसाद के परिवेश में निहित थी। जब पिता का देहावसान हुआ, उस समय प्रसाद की अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी।
कुछ ही वर्षों के भीतर बड़े भाई भी परलोक सिधार गये और सोलह वर्षीय कवि पर समस्याओं का पहाड़ आ टूटा। आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह जर्जर हो चुकी एक संस्कारी कुल परिवार के लुप्त गौरव के पुनरुद्धार की चुनौती तो मुँह बाये सामने खड़ी ही थी, जिस परिवार पर अन्तहीन मुक़दमेबाज़ी, भारी क़र्ज़ का बोझ, स्वार्थी और अकारणद्रोही स्वजन, तथाकथित शुभचिन्तकों की खोखली सहानुभूति का व्यंग्य...सबकुछ विपरीत ही विपरीत था। कोई और होता तो अपनी सारी प्रतिभा को लेकर इस बोझ के नीचे चकनाचूर हो गया होता। किंतु इस प्रतिकूल परिस्थिति से जूझते हुए प्रसाद जी ने न केवल कुछ वर्षों के भीतर अपने कुटुम्ब की आर्थिक अवस्था सृदृढ़ कर ली, बल्कि अपनी बौद्धिक-मानसिक सम्पत्ति को भी इस वात्याचक्र से अक्षत उबार लिया।
कुछ ही वर्षों के भीतर बड़े भाई भी परलोक सिधार गये और सोलह वर्षीय कवि पर समस्याओं का पहाड़ आ टूटा। आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह जर्जर हो चुकी एक संस्कारी कुल परिवार के लुप्त गौरव के पुनरुद्धार की चुनौती तो मुँह बाये सामने खड़ी ही थी, जिस परिवार पर अन्तहीन मुक़दमेबाज़ी, भारी क़र्ज़ का बोझ, स्वार्थी और अकारणद्रोही स्वजन, तथाकथित शुभचिन्तकों की खोखली सहानुभूति का व्यंग्य...सबकुछ विपरीत ही विपरीत था। कोई और होता तो अपनी सारी प्रतिभा को लेकर इस बोझ के नीचे चकनाचूर हो गया होता। किंतु इस प्रतिकूल परिस्थिति से जूझते हुए प्रसाद जी ने न केवल कुछ वर्षों के भीतर अपने कुटुम्ब की आर्थिक अवस्था सृदृढ़ कर ली, बल्कि अपनी बौद्धिक-मानसिक सम्पत्ति को भी इस वात्याचक्र से अक्षत उबार लिया।
‘‘ये मानसिक विप्लव प्रभो, जो हो रहे दिन रात हैं
कुविचार कुरों के कठिन कैसे कुटिल आघात हैं
हे नाथ मेरे सारथी बन जाव मानस-युद्ध में
फिर तो ठहरने से बचेंगे एक भी न विरुद्ध में।’
कुविचार कुरों के कठिन कैसे कुटिल आघात हैं
हे नाथ मेरे सारथी बन जाव मानस-युद्ध में
फिर तो ठहरने से बचेंगे एक भी न विरुद्ध में।’
यही हुआ भी। जिस गहरे मनोविज्ञान यथार्थवाद की नींव पर प्रसाद के जीवन कृतित्व की पूरी इमारत खड़ी है, वह उनकी व्यक्तिगत जीवनी की भी बुनियाद है। घर-परिवार व्यवस्थित कर लेने के बाद हमारे कवि ने अपने अन्तर्जीवन की व्यवस्था भी उतनी ही दृढ़ता से सम्हाली और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के निरन्तर और अचूक विकास क्रम से उन्होंने साहित्य जगत को विस्मय में डाल दिया। धीरे-धीरे, लगभग नामालूम ढंग से उनकी रचनाएँ साहित्य जगत में गहरे भिदती गईं और क्या कविता, क्या कहानी, क्या नाटक, क्या-चिंतन हर क्षेत्र में खमीर की तरह रूपान्तरित सिद्ध होती चली गई।
किसी ने उनके बारे में लिखा है कि प्रसाद का जो आन्तरित व्यक्तित्व था, वह लीलापुरुष कृष्ण के दर्शन से प्रेरणा पाता था, और उनका जो सामाजिक व्यक्तित्व था, वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता था। निश्चित ही प्रसाद जी के काव्य के पीछे जो जीवन और व्यक्तित्व है, उसमें धैर्य और निस्संगता की विपुल क्षमता रही होनी चाहिए।
उनका आनन्दवाद महज़ आसानी से विरासत में मिल गई एक वस्तु ही नहीं है। इस दर्शन को उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और घोर मानसिक उत्पीड़न से जूझते हुए संकल्पपूर्वक अर्जित किया था। इसलिए उनमें एक विलक्षण मूल्यवत्ता है। जीवनी का जहाँ एक प्रश्न है, उसका आरंभ भी दुःखमय था और उपसंहार भी : जब प्रसाद जी अपनी सृजन सामर्थ्य के शिखर पर थे, तभी, कुल जमा सैंतालिस वर्ष की आयु में एक घातक रोग ने उन्हें आ ग्रसा और इलाज के लिए किसी ‘सेनेटोरियम’ में जा रहने की बजाए वहीं अपनी प्रिय काशी में ही उन्होंने अपनी इहलीला संवरण कर ली। प्रसाद की जीवनी और उससे जुड़ा कृतित्व हमारे मन में बरबस ही कवि कीट्स के बारे लिखी आधुनिक कवि येट्स की उस प्रसिद्ध पंक्ति को प्रतिध्वनि कर देता हैः ‘हिज़ आर्ट इज़ हैप्पी, बट हू नोज़ हिज़ माइण्ड’ (उसकी कला आनन्दमयी है, किन्तु उसके पीछे जो मन रहा होगा, उसकी कथा कौन जानता है !) अस्तु यहाँ तक प्रसादजी के मन का प्रश्न है, उसकी हमें अवश्य मिल सकती है, यदि हम उनकी आनन्दमयी काव्य-कला में ही नहीं, उनकी उन कथा-सृष्टियों और नाट्यकृतियों में भी गहरी डुबकी लगाएँ जिनमें विशुद्ध आनन्द और समरसता के अतिरिक्त भी बहुत कुछ समाया हुआ है। स्वयं उनकी कविता का अंतः साक्ष्य भी कम नहीं हैः उनके नाटक ‘विशाख’ का वह गीत याद आता है।
किसी ने उनके बारे में लिखा है कि प्रसाद का जो आन्तरित व्यक्तित्व था, वह लीलापुरुष कृष्ण के दर्शन से प्रेरणा पाता था, और उनका जो सामाजिक व्यक्तित्व था, वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता था। निश्चित ही प्रसाद जी के काव्य के पीछे जो जीवन और व्यक्तित्व है, उसमें धैर्य और निस्संगता की विपुल क्षमता रही होनी चाहिए।
उनका आनन्दवाद महज़ आसानी से विरासत में मिल गई एक वस्तु ही नहीं है। इस दर्शन को उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और घोर मानसिक उत्पीड़न से जूझते हुए संकल्पपूर्वक अर्जित किया था। इसलिए उनमें एक विलक्षण मूल्यवत्ता है। जीवनी का जहाँ एक प्रश्न है, उसका आरंभ भी दुःखमय था और उपसंहार भी : जब प्रसाद जी अपनी सृजन सामर्थ्य के शिखर पर थे, तभी, कुल जमा सैंतालिस वर्ष की आयु में एक घातक रोग ने उन्हें आ ग्रसा और इलाज के लिए किसी ‘सेनेटोरियम’ में जा रहने की बजाए वहीं अपनी प्रिय काशी में ही उन्होंने अपनी इहलीला संवरण कर ली। प्रसाद की जीवनी और उससे जुड़ा कृतित्व हमारे मन में बरबस ही कवि कीट्स के बारे लिखी आधुनिक कवि येट्स की उस प्रसिद्ध पंक्ति को प्रतिध्वनि कर देता हैः ‘हिज़ आर्ट इज़ हैप्पी, बट हू नोज़ हिज़ माइण्ड’ (उसकी कला आनन्दमयी है, किन्तु उसके पीछे जो मन रहा होगा, उसकी कथा कौन जानता है !) अस्तु यहाँ तक प्रसादजी के मन का प्रश्न है, उसकी हमें अवश्य मिल सकती है, यदि हम उनकी आनन्दमयी काव्य-कला में ही नहीं, उनकी उन कथा-सृष्टियों और नाट्यकृतियों में भी गहरी डुबकी लगाएँ जिनमें विशुद्ध आनन्द और समरसता के अतिरिक्त भी बहुत कुछ समाया हुआ है। स्वयं उनकी कविता का अंतः साक्ष्य भी कम नहीं हैः उनके नाटक ‘विशाख’ का वह गीत याद आता है।
‘‘आवृत हो अतीत सब मेरा
तूने देखा सब कुछ मेरा
परदा होने से......
तूने देखा सब कुछ मेरा
परदा होने से......
क्या यह परदा, कला के लिए ही नहीं, संवेदनशील ‘मन’ के लिए भी अपरिहार्य नहीं है ?.... क्या प्रसाद जी की ही एक और नाट्य-गीत भी हमें नहीं बताती कि......‘‘नृत्य करेगी नग्न विकलता परदे के उस पार ?’’ जीवन के गहन पीड़ा-बोध में से ही ‘आँसू’ का एक कवि जीवन की निराधार स्वीकृति का ऐसा गान रच सकता हैः
‘‘छलना थी फिर भी उसमें
मेरा विश्वास घना था।
उस माया की छाया में
कुछ सच्चा स्वयं बना था’’
मेरा विश्वास घना था।
उस माया की छाया में
कुछ सच्चा स्वयं बना था’’
कहने का तात्पर्य यही, कि प्रसाद जी का ‘आनन्दवाद’ भी उनके ‘नियतिवाद’ की तरह इकहरा और सरलीकृत नहीं है। वह सच्चे अर्थों में समत्व-बुद्धि, यानी ‘विज़्डम’ है। यह समत्व-बुद्धि उन्हें गहरे अन्तर्द्वन्द्व में से उपलब्ध हुई थी। जैनेन्द्र कुमार सरीखे कथाकार चिन्तक ने भी यदि प्रसाद की इस ज़ोखिम उठानेवाली बुद्धि का लोहा माना है; तो यह सर्वथा स्वाभाविक है। उन्हीं के शब्दों में-
‘‘मेरे भाव में वह पहले बड़े नास्तिक लेखक थे।.....हर मत-मन्यता को, सामाजिक हो कि नैतिक, धार्मिक हो कि राजनैतिक, उन्होंने प्रश्नवाचक के साथ लिया। किसी को अंतिम नहीं माना। ‘कंकाल’ इसी से कितना भयंकर हो उठा है मानों काया की कमयीता पर रीझने को तैयार नहीं है। शल्यक्रिया से भीतर के कदर्य और कुत्सिया को बाहर लाकर बिखेर देने में उन्हें हिचक नहीं है।.....नकार और निषेध को लेकर उठनेवालों दर्शन का उन्होंने प्राणपण से निराकरण किया और उस दर्शन को प्रतिष्ठित करना चाहा जो जीवन के प्रति निरपवाद स्वीकृति का निमंत्रण देता है। हिन्दुत्व की उनकी ऐसी ही धारणा थी। बौद्ध और जैन परम्पराओं में उन्होंने वर्जन पर बल देखा और वह उन्हें किसी रूप में मान्य नहीं था।....मुझे लगता है जैसे यही उनके साहित्य का मूलाभार, मूलकोण है।’’
यहाँ पर हमारे मन में शंका उठ सकती है कहाँ ‘पहला बड़ा नास्तिक लेखक और कहाँ ‘हिन्दुत्व’ ! इन दोनों के बीच क्या संगति है ? मगर जैनेन्द्र कुमार मानो हमारी शंका को भाँपते हुए ही, एक ऐसी गहरी बात आगे इसी सिलसिले कह गये हैं, जो प्रसाद के किसी अध्येता या आलोचक ने आज तक नहीं कही, और जो अकाटय लग उठती है। वे कहते है:-
‘‘प्रसाद की अतिशय सप्रश्नता और प्रखर बौद्धिकता, जैसा कि अनिवार्य है, उन्हें उस जगह तक ले गई जहाँ खुद बुद्धि पर टिके रहना व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहता। अपनी परिपक्व परिणति में बुद्धि यह दिखाए बिना नहीं रह सकती कि वह अपर्याप्त है और श्रद्धा में पूरी हो सकती है। इसका आशय यह नहीं, कि पहली वाली मेरी स्थापना सदोष है। बल्कि, यही कि श्रद्धा की स्वीकृति प्रसाद को बुद्धि द्वारा ही हो सकी है। जैसे बुद्धि माध्यम है, श्रद्धा बिना उसके अगम है।’’
यह अन्तर्दृष्टि हमारे विचार में कामायनी की सही समझ के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगी। यह उन आलोचकों को भी पर्याप्त प्रत्युत्तर है जिन्हें ‘कामायनी’ में बुद्धि तत्व की अवमानना अथवा श्रद्धा के पक्ष में एक तरह का भावुक सरलीकरण दिखाई दिया है।
सच पूछा जाए, तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जयशंकर प्रसाद का कृतित्व समवेत रूप में संसार का तिरस्कार करनेवाले फलसफ़े की सबसे ज़ोरदार काट प्रस्तुत करता है। करुणा क्या रवीन्द्रनाथ की कहानियों के वातावरण में गहरे रचीं हुई नहीं ? फिर भी कौन कह सकता है कि इस कारुण्य बोध के बावजूद रवीन्द्रनाथ का कवित्व और जीवन-दर्शन आनन्द प्रेरित ही नहीं ? जैसा कि हमने पहले भी देखा, इन दोनों दृष्टियों के बीच कोई अनिवार्य अन्तविरोध नहीं है। इन आनन्दवाद में तीव्र रागात्मक संसक्ति भर नहीं हैः उसमें आन्तरिक स्वातंत्र्य साधना और आत्मैक्य पर ज़ोर हैं। प्रसाद जी के उपन्यासों और नाटकों में संघर्ष और समाधान की एक विचित्र लीला दिखाई पड़ती हैः उनके चरित्र भी राग-विराग, आशा-निराशा रागाकुलता तथा दार्शनिक चिन्ताकुलता के बीच आन्दोलित होते रहते हैं। समाधान आशवस्त नहीं करता वहाँ; संघर्ष और अस्थिरता का ही तीखा अनुभव हमारे सिर चढ़कर बोलता है। किन्तु उनकी काव्य-रचनाओं में उत्तरोत्तर एक ऐसा संतुलन सध जाता प्रतीत होता है जो इस द्वन्द्वात्मक लीला को एक समरसता की अनुभूति में घुला देता है। वह ‘वह तुमुल कोलाहल’ है, तो यहाँ ‘हृदय की ‘बात’ है। कहना न होगा वह ‘तुमुल कोलाहल’ जिसे व्यापता है, वह कथाकार-नाटककार, तथा उच्च काव्य-भूमि पर एक प्रशान्त समरसता के बोध को सिद्ध करनेवाला कवि दोनों अंततः एक ही व्यक्तित्व और एक ही मनीषा के दो पहलू हैं। अन्ततः गाँधी जी के लिए भी तो अनासक्ति योग की सार्थकता जीवन और कर्म के पक्ष में ही प्रयुक्त होने में थी, न कि जीवन की चुनौती से पलायन करने में।
कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर महात्मा गाँधी ने इतिहास के इस मोड़ पर भारत की लोकचेतना को प्रवृत्ति मार्ग की ओर मोड़ते हुए उसके नैतिक पक्ष की सार-सँवार पर अधिक बल दिया, वहाँ, रवीन्द्रवनाथ ठाकुर और प्रसाद सरीखे सर्जकों ने उसी प्रवृत्ति के काव्यात्मक अर्थात् आनन्द मूलक पक्ष को पल्लावित किया। जीवन और जगत के संबंध में जो मौलिक अन्तदृष्टियाँ इस देश में अपनी सुदीर्घ लोकयात्रा के दौरान बार-बार कमाई और बार-बार गँवायी है, उन्हीं का नया संतुलन उपलब्ध करने की एक कठिन साधना प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व में भी हमें दिखाई देती है। प्रस्तुत संचयन से गुजरते हुए हम देख सकते है कि प्रसाद की काव्य कल्पना बराबर उनके प्रत्यक्ष जीवनानुभवों और पर्यवेक्षणों द्वारा प्रेरित और पुष्ट होती रही और उनका कथा-साहित्य भी एक गहरे मनोवैज्ञानिक यथार्थ को ही झलकाता चलता है- अपने सारे रोमान और सहस्य के बावजूद उनका काव्य अवश्य अपने स्वर और रंग में अधिक आदर्श प्रेरित है, किन्तु वह भी यथार्थ का उल्लंघन करने की किसी तरह की पलायनेच्छा का परिणाम नहीं। मानवीय नियति के प्रति उनका वही दायित्व बोध वहाँ और भी सारभूत और घनिष्ठ रूप में विद्यमान है।
‘‘मेरे भाव में वह पहले बड़े नास्तिक लेखक थे।.....हर मत-मन्यता को, सामाजिक हो कि नैतिक, धार्मिक हो कि राजनैतिक, उन्होंने प्रश्नवाचक के साथ लिया। किसी को अंतिम नहीं माना। ‘कंकाल’ इसी से कितना भयंकर हो उठा है मानों काया की कमयीता पर रीझने को तैयार नहीं है। शल्यक्रिया से भीतर के कदर्य और कुत्सिया को बाहर लाकर बिखेर देने में उन्हें हिचक नहीं है।.....नकार और निषेध को लेकर उठनेवालों दर्शन का उन्होंने प्राणपण से निराकरण किया और उस दर्शन को प्रतिष्ठित करना चाहा जो जीवन के प्रति निरपवाद स्वीकृति का निमंत्रण देता है। हिन्दुत्व की उनकी ऐसी ही धारणा थी। बौद्ध और जैन परम्पराओं में उन्होंने वर्जन पर बल देखा और वह उन्हें किसी रूप में मान्य नहीं था।....मुझे लगता है जैसे यही उनके साहित्य का मूलाभार, मूलकोण है।’’
यहाँ पर हमारे मन में शंका उठ सकती है कहाँ ‘पहला बड़ा नास्तिक लेखक और कहाँ ‘हिन्दुत्व’ ! इन दोनों के बीच क्या संगति है ? मगर जैनेन्द्र कुमार मानो हमारी शंका को भाँपते हुए ही, एक ऐसी गहरी बात आगे इसी सिलसिले कह गये हैं, जो प्रसाद के किसी अध्येता या आलोचक ने आज तक नहीं कही, और जो अकाटय लग उठती है। वे कहते है:-
‘‘प्रसाद की अतिशय सप्रश्नता और प्रखर बौद्धिकता, जैसा कि अनिवार्य है, उन्हें उस जगह तक ले गई जहाँ खुद बुद्धि पर टिके रहना व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहता। अपनी परिपक्व परिणति में बुद्धि यह दिखाए बिना नहीं रह सकती कि वह अपर्याप्त है और श्रद्धा में पूरी हो सकती है। इसका आशय यह नहीं, कि पहली वाली मेरी स्थापना सदोष है। बल्कि, यही कि श्रद्धा की स्वीकृति प्रसाद को बुद्धि द्वारा ही हो सकी है। जैसे बुद्धि माध्यम है, श्रद्धा बिना उसके अगम है।’’
यह अन्तर्दृष्टि हमारे विचार में कामायनी की सही समझ के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगी। यह उन आलोचकों को भी पर्याप्त प्रत्युत्तर है जिन्हें ‘कामायनी’ में बुद्धि तत्व की अवमानना अथवा श्रद्धा के पक्ष में एक तरह का भावुक सरलीकरण दिखाई दिया है।
सच पूछा जाए, तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जयशंकर प्रसाद का कृतित्व समवेत रूप में संसार का तिरस्कार करनेवाले फलसफ़े की सबसे ज़ोरदार काट प्रस्तुत करता है। करुणा क्या रवीन्द्रनाथ की कहानियों के वातावरण में गहरे रचीं हुई नहीं ? फिर भी कौन कह सकता है कि इस कारुण्य बोध के बावजूद रवीन्द्रनाथ का कवित्व और जीवन-दर्शन आनन्द प्रेरित ही नहीं ? जैसा कि हमने पहले भी देखा, इन दोनों दृष्टियों के बीच कोई अनिवार्य अन्तविरोध नहीं है। इन आनन्दवाद में तीव्र रागात्मक संसक्ति भर नहीं हैः उसमें आन्तरिक स्वातंत्र्य साधना और आत्मैक्य पर ज़ोर हैं। प्रसाद जी के उपन्यासों और नाटकों में संघर्ष और समाधान की एक विचित्र लीला दिखाई पड़ती हैः उनके चरित्र भी राग-विराग, आशा-निराशा रागाकुलता तथा दार्शनिक चिन्ताकुलता के बीच आन्दोलित होते रहते हैं। समाधान आशवस्त नहीं करता वहाँ; संघर्ष और अस्थिरता का ही तीखा अनुभव हमारे सिर चढ़कर बोलता है। किन्तु उनकी काव्य-रचनाओं में उत्तरोत्तर एक ऐसा संतुलन सध जाता प्रतीत होता है जो इस द्वन्द्वात्मक लीला को एक समरसता की अनुभूति में घुला देता है। वह ‘वह तुमुल कोलाहल’ है, तो यहाँ ‘हृदय की ‘बात’ है। कहना न होगा वह ‘तुमुल कोलाहल’ जिसे व्यापता है, वह कथाकार-नाटककार, तथा उच्च काव्य-भूमि पर एक प्रशान्त समरसता के बोध को सिद्ध करनेवाला कवि दोनों अंततः एक ही व्यक्तित्व और एक ही मनीषा के दो पहलू हैं। अन्ततः गाँधी जी के लिए भी तो अनासक्ति योग की सार्थकता जीवन और कर्म के पक्ष में ही प्रयुक्त होने में थी, न कि जीवन की चुनौती से पलायन करने में।
कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर महात्मा गाँधी ने इतिहास के इस मोड़ पर भारत की लोकचेतना को प्रवृत्ति मार्ग की ओर मोड़ते हुए उसके नैतिक पक्ष की सार-सँवार पर अधिक बल दिया, वहाँ, रवीन्द्रवनाथ ठाकुर और प्रसाद सरीखे सर्जकों ने उसी प्रवृत्ति के काव्यात्मक अर्थात् आनन्द मूलक पक्ष को पल्लावित किया। जीवन और जगत के संबंध में जो मौलिक अन्तदृष्टियाँ इस देश में अपनी सुदीर्घ लोकयात्रा के दौरान बार-बार कमाई और बार-बार गँवायी है, उन्हीं का नया संतुलन उपलब्ध करने की एक कठिन साधना प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व में भी हमें दिखाई देती है। प्रस्तुत संचयन से गुजरते हुए हम देख सकते है कि प्रसाद की काव्य कल्पना बराबर उनके प्रत्यक्ष जीवनानुभवों और पर्यवेक्षणों द्वारा प्रेरित और पुष्ट होती रही और उनका कथा-साहित्य भी एक गहरे मनोवैज्ञानिक यथार्थ को ही झलकाता चलता है- अपने सारे रोमान और सहस्य के बावजूद उनका काव्य अवश्य अपने स्वर और रंग में अधिक आदर्श प्रेरित है, किन्तु वह भी यथार्थ का उल्लंघन करने की किसी तरह की पलायनेच्छा का परिणाम नहीं। मानवीय नियति के प्रति उनका वही दायित्व बोध वहाँ और भी सारभूत और घनिष्ठ रूप में विद्यमान है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book