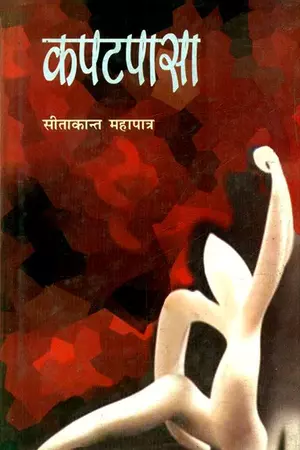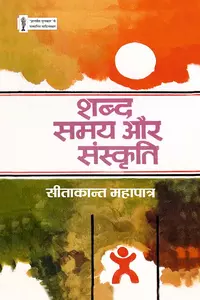|
कविता संग्रह >> कपटपासा कपटपासासीताकान्त महापात्र
|
111 पाठक हैं |
|||||||
**डॉ. सीताकांत महापात्र : 'कपटपासा' – मानव अस्तित्व और आधुनिक मूल्यों की गहराइयों में एक काव्यात्मक यात्रा**
Kapatpasa
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भीम भोइ
क्या तुम सचमुच अन्धे थे
जनम से ?
कभी-कभी मन करता है
तुम्हारा हाथ पकड़ कर
राह-बेराह न मान
लावारिस बच्चों की तरह
हम दोनों
घना अंधेरा हटा
बढ़ते चले जाते नक्षत्रों की ओर देख
एक के बाद एक
थकान भरे डग बढ़ाते हुए।
मैं वर्णन करता चलता
मुग्ध बातूनी-सा
सामने दृश्यमान जगत की एक-एक सम्पदा,
गहरी ख़ामोशी तोड़
सुनाई देता अँधेरे में तुम्हारा ही स्वर
हाँ सब कुछ दिख तो रहा चकमक
अभ्यन्तर अँधेरे में
कितनी सुन्दर उद्भासित है अमारात्रि
सहमा-सा मैं पूछ नहीं पाता
कौन-सा अभ्यन्तर ?
कौन-सी अमारात्रि है वह
गर्भगृह किस मन्दिर का ?
जनम से ?
कभी-कभी मन करता है
तुम्हारा हाथ पकड़ कर
राह-बेराह न मान
लावारिस बच्चों की तरह
हम दोनों
घना अंधेरा हटा
बढ़ते चले जाते नक्षत्रों की ओर देख
एक के बाद एक
थकान भरे डग बढ़ाते हुए।
मैं वर्णन करता चलता
मुग्ध बातूनी-सा
सामने दृश्यमान जगत की एक-एक सम्पदा,
गहरी ख़ामोशी तोड़
सुनाई देता अँधेरे में तुम्हारा ही स्वर
हाँ सब कुछ दिख तो रहा चकमक
अभ्यन्तर अँधेरे में
कितनी सुन्दर उद्भासित है अमारात्रि
सहमा-सा मैं पूछ नहीं पाता
कौन-सा अभ्यन्तर ?
कौन-सी अमारात्रि है वह
गर्भगृह किस मन्दिर का ?
नीबू का पेड़
जानता हूँ मैं तेरी साहसी जड़ों को
पहचानता हूँ उनकी भूख, क्षोभ, तपस्या।
पर सिर्फ़ इतना भर बता दे
एक नन्हे-से बीज में
कहाँ छुपा रखी थी
हरी साड़ी से सज्जित यह अनन्य शोभा
ऋषि मन को लुभावनी यह सरल छाया
प्रकाश पवन में मँडराती मृत्यु की माया।
कहा करते थे पिताजी
मिट्टी से उपजा अन्न खा कर
हम बालक से वृद्ध होते हैं
अन्त में मिट्टी हमें खा कर
पुन: हमारे बच्चों के लिए
अन्न, तरुलताएँ, पौधे उपजाती है।
मिट्टी के भीतर अँधेरी यात्रा में
क्या तेरी जड़ें अचानक जा मिलीं
मेरे परदादा की मजबूत घी-खाई हड्डियों से ?
क्या उसी राह से रास्ते के मोड़ पर दादाजी के सपनों
या दादी की आँखों के उज्जवल नक्षत्रों से ?
इसी मेल-मुलाकात से शायद उभरे हैं
पत्तों पर तेरे झिलिमिलाते चाँद और सितारे
फूल-फलों में तेरी बजती हैं संगीत की लहरें
टहनियों के माइक्रोफ़ोन में
पिताजी के गीता-पाठ का स्वर।
नीबू के पेड़, नीबू के पेड़ !
अगले जनम मेरे लौट कर आने तक
तू यहीं रहना, उखड़ कर चले न जाना
कह देना अपने भीतर के मृत्युदूतों से
किसी बच्चे ने किया है
अटपटा अनुरोध ऐसा
जो नहीं टाला जाता।
नीबू के पेड़, नीबू के पेड़ !
जानता हूँ मैं तेरे सीने में छिपे देवदूतों को
पहचानता हूँ समय और सपनों को ले कर
चुपचाप संगीत बुनते तेरे बुनकरपन को।
पहचानता हूँ उनकी भूख, क्षोभ, तपस्या।
पर सिर्फ़ इतना भर बता दे
एक नन्हे-से बीज में
कहाँ छुपा रखी थी
हरी साड़ी से सज्जित यह अनन्य शोभा
ऋषि मन को लुभावनी यह सरल छाया
प्रकाश पवन में मँडराती मृत्यु की माया।
कहा करते थे पिताजी
मिट्टी से उपजा अन्न खा कर
हम बालक से वृद्ध होते हैं
अन्त में मिट्टी हमें खा कर
पुन: हमारे बच्चों के लिए
अन्न, तरुलताएँ, पौधे उपजाती है।
मिट्टी के भीतर अँधेरी यात्रा में
क्या तेरी जड़ें अचानक जा मिलीं
मेरे परदादा की मजबूत घी-खाई हड्डियों से ?
क्या उसी राह से रास्ते के मोड़ पर दादाजी के सपनों
या दादी की आँखों के उज्जवल नक्षत्रों से ?
इसी मेल-मुलाकात से शायद उभरे हैं
पत्तों पर तेरे झिलिमिलाते चाँद और सितारे
फूल-फलों में तेरी बजती हैं संगीत की लहरें
टहनियों के माइक्रोफ़ोन में
पिताजी के गीता-पाठ का स्वर।
नीबू के पेड़, नीबू के पेड़ !
अगले जनम मेरे लौट कर आने तक
तू यहीं रहना, उखड़ कर चले न जाना
कह देना अपने भीतर के मृत्युदूतों से
किसी बच्चे ने किया है
अटपटा अनुरोध ऐसा
जो नहीं टाला जाता।
नीबू के पेड़, नीबू के पेड़ !
जानता हूँ मैं तेरे सीने में छिपे देवदूतों को
पहचानता हूँ समय और सपनों को ले कर
चुपचाप संगीत बुनते तेरे बुनकरपन को।
वृक्ष-सूक्त
बक्कल ढके रखता है अपने
सभी पितृ-पितामह के शवों को
ख़ामोश ताबूत में।
साहस बटोर कर बाहर झाँकता है
क्षमाशील सूर्य और चैती हवा को छू कर
किसी तरह जीवित रहता है;
हमेशा खड़ा रहता है, वृक्ष
महाश्मशान में
अपने भीतर मचे
लाखों मरण के हाहाकार के बीच।
कान लगा कर सुनता है चिड़ियों का कलरव
सिहर उठता है चैती हवा से
समझता है राहगीरों की छाया-तृष्णा
पहचानता है लकड़हारों की आँखों की प्राचीन क्षुधा;
पंक्तिबद्ध समाधियों के ख़ामोश सिरे पर
सुनाई पड़ता है स्वर कभी सोहर से रुलाई का कुआँ-कुआँ
कोई कली आँखें खोलती है।
भला कौन समझेगा उसकी
तपस्या का इतिवृत्त ;
चिडि़या ? सूर्य ? हवा ?
लकड़हारा या उदास राहगीर ?
सभी पितृ-पितामह के शवों को
ख़ामोश ताबूत में।
साहस बटोर कर बाहर झाँकता है
क्षमाशील सूर्य और चैती हवा को छू कर
किसी तरह जीवित रहता है;
हमेशा खड़ा रहता है, वृक्ष
महाश्मशान में
अपने भीतर मचे
लाखों मरण के हाहाकार के बीच।
कान लगा कर सुनता है चिड़ियों का कलरव
सिहर उठता है चैती हवा से
समझता है राहगीरों की छाया-तृष्णा
पहचानता है लकड़हारों की आँखों की प्राचीन क्षुधा;
पंक्तिबद्ध समाधियों के ख़ामोश सिरे पर
सुनाई पड़ता है स्वर कभी सोहर से रुलाई का कुआँ-कुआँ
कोई कली आँखें खोलती है।
भला कौन समझेगा उसकी
तपस्या का इतिवृत्त ;
चिडि़या ? सूर्य ? हवा ?
लकड़हारा या उदास राहगीर ?
चक्रव्यूह
उसका जीवन ही
उसका अपना रचा एक चक्रव्यूह है।
मन्दिर के देवता की आँखों से
माँ की मीठी बातों से
मास्टरजी की छड़ी-मार से
अनेक छपे अक्षरों
और अनछपे, अनजान सिहरन से
अनेक बातें सीख कर
उन्हीं को ढाल-तलवार बना पकड़ कर
चलता जाता है वह समय के कराल
अभ्यन्तर की ओर।
चलता चला जाता है, कितनी दूर चला जाता है
जान नहीं पाता
समय आने पर लगता है उसे
कुछ समझ नहीं पाता वह
न सुबह, न साँझ, न रात
लक्ष्यस्थल नहीं सूझता कोई
क्यों चलता चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है
याद नहीं आता कुछ।
पीछे लौट जाने को
सिर घुमा कर देखता है
राह अब नहीं सूझती
अँधेरा, परछाईं, सन्देह
मृत्यु के समस्त विभ्रम
घेर लेते हैं उसे।
उसका अपना रचा एक चक्रव्यूह है।
मन्दिर के देवता की आँखों से
माँ की मीठी बातों से
मास्टरजी की छड़ी-मार से
अनेक छपे अक्षरों
और अनछपे, अनजान सिहरन से
अनेक बातें सीख कर
उन्हीं को ढाल-तलवार बना पकड़ कर
चलता जाता है वह समय के कराल
अभ्यन्तर की ओर।
चलता चला जाता है, कितनी दूर चला जाता है
जान नहीं पाता
समय आने पर लगता है उसे
कुछ समझ नहीं पाता वह
न सुबह, न साँझ, न रात
लक्ष्यस्थल नहीं सूझता कोई
क्यों चलता चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है
याद नहीं आता कुछ।
पीछे लौट जाने को
सिर घुमा कर देखता है
राह अब नहीं सूझती
अँधेरा, परछाईं, सन्देह
मृत्यु के समस्त विभ्रम
घेर लेते हैं उसे।
मेरी भाषा
चिलचिलाती दुपहरी में
मन्त्री को फूलों की माला पहना
ड्रम बजा कर स्वागत करने वाले
ख़ुशामदकारियों के पीछे-पीछे
धूल और पसीने से सराबोर
एक-एक कर डग बढ़ाने वाले
दुबले-पतले अधनंगे लोगों के साथ-साथ
मार्च करती है, मेरी भाषा, काले स्वर्ग की ओर
सीने में छुपाए असंख्या क्षोभ।
गुनगुनाती है भाषा
संन्यासी की बन्द पलकों की कोर में
करुणा की पतली-सी नदी बह रही होती है
पलकों के नीचे।
तलाशती रहती है भाषा, कुछ पहले की तरह
स्वर और व्यंजन के उरोजों के बीच
प्रतिमा, प्रतीकों की अस्तव्यस्त सेज पलट कर
तुच्छ अस्मिता और आवेग भरे मोगरे का हार फेंक
मोह और आरती से बँधा जूड़ा खोल
तलाशती रहती है कहीं सबसे नीचे
आत्मा की सन्धि में छुपी
वाङ्मयी चुप्पी।
लिखती रहती है भाषा ख़ुद को पहले की तरह
लालटेन की रोशनी में झुकी
पुराने ताड़पत्रों में, पत्थरों में, आकाश में :
समाती चली जाती है भाषा माँड़ की महक में
अँधियारी रात में बाँस-वन की चिड़ियों के गीतों में।
तुरई लता कँटीली झाड़ियों पर अपना बोझ लादने की तरह
सहारा ले कर उठती है भाषा चित्रकल्प पर
ताकती रहती है अर्थ की ओर
आकुल तृष्णा से।
मन्त्री को फूलों की माला पहना
ड्रम बजा कर स्वागत करने वाले
ख़ुशामदकारियों के पीछे-पीछे
धूल और पसीने से सराबोर
एक-एक कर डग बढ़ाने वाले
दुबले-पतले अधनंगे लोगों के साथ-साथ
मार्च करती है, मेरी भाषा, काले स्वर्ग की ओर
सीने में छुपाए असंख्या क्षोभ।
गुनगुनाती है भाषा
संन्यासी की बन्द पलकों की कोर में
करुणा की पतली-सी नदी बह रही होती है
पलकों के नीचे।
तलाशती रहती है भाषा, कुछ पहले की तरह
स्वर और व्यंजन के उरोजों के बीच
प्रतिमा, प्रतीकों की अस्तव्यस्त सेज पलट कर
तुच्छ अस्मिता और आवेग भरे मोगरे का हार फेंक
मोह और आरती से बँधा जूड़ा खोल
तलाशती रहती है कहीं सबसे नीचे
आत्मा की सन्धि में छुपी
वाङ्मयी चुप्पी।
लिखती रहती है भाषा ख़ुद को पहले की तरह
लालटेन की रोशनी में झुकी
पुराने ताड़पत्रों में, पत्थरों में, आकाश में :
समाती चली जाती है भाषा माँड़ की महक में
अँधियारी रात में बाँस-वन की चिड़ियों के गीतों में।
तुरई लता कँटीली झाड़ियों पर अपना बोझ लादने की तरह
सहारा ले कर उठती है भाषा चित्रकल्प पर
ताकती रहती है अर्थ की ओर
आकुल तृष्णा से।
दादाजी
यहीं तुम्हें एक दिन छोड़ गये थे पिताजी
इसी खुले मैदान, सूर्यकिरण में
बहती चित्रोत्पला नदी के तट पर;
जिस तरह उस दिन उनको छोड़ आया
एकाकी, कुआखाई नदी किनारे।
बीच-बीच में यहाँ आ कर
देखा करता हूँ सब उसी तरह, पहले जैसा;
नदी किनारे सिर्फ़ कुछ पेड़ ही बड़े हुए हैं
लद गये हैं पेड़ पत्तों, फूलों और फलों से।
शुरू-शुरू में शायद यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता था
इसीलिए भाग आया करते थे
अकसर अँधेरी रातों में
हमारे सपनों में, अधिकतर दादी के सपनों में
फिर कुछ दिनों बाद आदत-सी जो पड़ गयी !
इसके अलावा स्कूल न जा कर रास्ते में
झड़बेरी खाने की तरह
तुम भी घूमा करते होगे नदी के टापुओं में।
आया हूँ आज यहाँ एक अरसे बाद
पहले-सी है सूर्यकिरण, वही खुला-खुला मैदान
बहती चित्रोत्पला
और अब बुढ़ा चुके, कुछ अधमरे पेड़।
इन सबके बीच
दिख जाता है तुम्हारा दढ़ियल चेहरा
सुनाई देती है तुम्हारी ठहाकेदार हँसी, दादाजी।
इसी खुले मैदान, सूर्यकिरण में
बहती चित्रोत्पला नदी के तट पर;
जिस तरह उस दिन उनको छोड़ आया
एकाकी, कुआखाई नदी किनारे।
बीच-बीच में यहाँ आ कर
देखा करता हूँ सब उसी तरह, पहले जैसा;
नदी किनारे सिर्फ़ कुछ पेड़ ही बड़े हुए हैं
लद गये हैं पेड़ पत्तों, फूलों और फलों से।
शुरू-शुरू में शायद यहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता था
इसीलिए भाग आया करते थे
अकसर अँधेरी रातों में
हमारे सपनों में, अधिकतर दादी के सपनों में
फिर कुछ दिनों बाद आदत-सी जो पड़ गयी !
इसके अलावा स्कूल न जा कर रास्ते में
झड़बेरी खाने की तरह
तुम भी घूमा करते होगे नदी के टापुओं में।
आया हूँ आज यहाँ एक अरसे बाद
पहले-सी है सूर्यकिरण, वही खुला-खुला मैदान
बहती चित्रोत्पला
और अब बुढ़ा चुके, कुछ अधमरे पेड़।
इन सबके बीच
दिख जाता है तुम्हारा दढ़ियल चेहरा
सुनाई देती है तुम्हारी ठहाकेदार हँसी, दादाजी।
तेरी अनुपस्थिति
तेरा न होना
हर जगह चाँदनी-फूलों से भरी चाँदनी रात-सा
बिखरा होता है !
सुबह कोमल उँगली से
चाय का कप छूकर ‘तत्ता’ के अनुभव से ले कर
चॉकलेट, हाजमोला के लिए ज़बर्दस्त माँग तक;
नन्हीं मुट्ठी में गमले से चुरा कर लाई
बैकुण्ठ की जादुई मिट्टी से ले कर
हम सबकी पोशाकों के रंगों के अनुसार
नामकरण करने तक,
जगन्नाथ महाप्रभु की गोल-गोल आँखों-सी आँखों वाले
कपटी उल्लू के वर्णन से ले कर
तिरछी नज़रों से देखना चतुर खरगोश तक।
टेलीफ़ोन में आवाज़ सुनाई देने पर लगता है
बहुत दूर, किसी अनजान कमरे में नहीं
यहीं दरवाज़े के पिछवाड़े
चुपचाप खड़ा है तू
प्रत्याशा से, निष्कपट आकांक्षा से, कुतूहल से
कुछ ही क्षणों में एक कोमल हाथ
मेरा हाथ थाम कर खींचता हुआ ले जाएगा
जिस ओर चाहेगा उस ओर।
डरता हूँ, कल कहीं तू समझ न जाए
न होना क्या है, खोने का अर्थ क्या है
जो टीसता रहता है सीने में;
शायद कल तू भी समझेगा
एक-एक इंच में अपने हृदय से जुड़ा घर
बन जाता है धीरे-धीरे सुदूर नक्षत्र कैसे,
तितलियाँ पकड़ने से ले कर पानी में खेलने तक
वस्तु, शब्द
उड़ जाते हैं कैसे नन्हीं चिड़ियों की तरह
आसमान की ओर, नक्षत्रों की ओर।
हर जगह चाँदनी-फूलों से भरी चाँदनी रात-सा
बिखरा होता है !
सुबह कोमल उँगली से
चाय का कप छूकर ‘तत्ता’ के अनुभव से ले कर
चॉकलेट, हाजमोला के लिए ज़बर्दस्त माँग तक;
नन्हीं मुट्ठी में गमले से चुरा कर लाई
बैकुण्ठ की जादुई मिट्टी से ले कर
हम सबकी पोशाकों के रंगों के अनुसार
नामकरण करने तक,
जगन्नाथ महाप्रभु की गोल-गोल आँखों-सी आँखों वाले
कपटी उल्लू के वर्णन से ले कर
तिरछी नज़रों से देखना चतुर खरगोश तक।
टेलीफ़ोन में आवाज़ सुनाई देने पर लगता है
बहुत दूर, किसी अनजान कमरे में नहीं
यहीं दरवाज़े के पिछवाड़े
चुपचाप खड़ा है तू
प्रत्याशा से, निष्कपट आकांक्षा से, कुतूहल से
कुछ ही क्षणों में एक कोमल हाथ
मेरा हाथ थाम कर खींचता हुआ ले जाएगा
जिस ओर चाहेगा उस ओर।
डरता हूँ, कल कहीं तू समझ न जाए
न होना क्या है, खोने का अर्थ क्या है
जो टीसता रहता है सीने में;
शायद कल तू भी समझेगा
एक-एक इंच में अपने हृदय से जुड़ा घर
बन जाता है धीरे-धीरे सुदूर नक्षत्र कैसे,
तितलियाँ पकड़ने से ले कर पानी में खेलने तक
वस्तु, शब्द
उड़ जाते हैं कैसे नन्हीं चिड़ियों की तरह
आसमान की ओर, नक्षत्रों की ओर।
उड़ीसा
इस छान-छप्पर के घर की
देहरी लाँघ जहाँ भी जाता हूँ मैं
दिल्ली, कि टोकियो, कि लेनिनग्राद
काम से, कविता के लिए, चेरीफूल की सभा में
या नेवा नदी,
साथ अपने ले जाता हूँ
पूरबी हवा से झुकता बौर से लदा
घर के सामने वाला आम का पेड़
जिस पर सपने की तरह सोन चिरैया
‘छिन में है, छिन में नहीं’ वाले खेल में
छिप जाती है, दिख जाती है,
फिर छिप जाती है, फिर दिख जाती है।
बस, इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
गलियों में लुकाछिपी खेलते
छोटे-छोटे बच्चों की
निष्पाप उदास आँखें;
टूटी कुर्सी को विकेट बना
चिलचिलाती दुपहरी में
क्रिकेट खेलने में मस्त
किशोरों की उज्जवल आँखें;
धान के खेत में कीचड़ में पैर गड़ाए झुके खड़े
कुशा डेरा, रघु मलिक के
अनिश्चित, अन्धकारमय भविष्य;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
पौ फटने से पहले
कजलपाखी कौआ या कोयल पुकारने से पहले
खण्डगिरि की गुफाओं से बह कर आते
जैन मुनियों के उदात्त प्रार्थना-स्वर;
रक्तरंजित दयानदी किनारे
पश्चाताप में डूबे
सम्राट के उनींदे प्रहर;
साथ ले जाता हूँ
दिन डूबे साँझ बप्पा से पहली बार मिले
उस किशोर द्वारा
मन्दिर का कँगूरा बिठा
समुद्र में छलाँग लगा कर आत्म-विसर्जन का
दिगन्तव्यापी करुण शोक-प्रहर;
चित्रोत्पला के घाट पर स्नान-तर्पण कर
खड़ाऊ खटखटाते लौटते दादाजी के
स्नेह-भरे सुबह के स्वर;
इतना ही है मेरे लिए उड़ासी।
साथ ले जाता हूँ
टूटे मन्दिर की दीवारों से
समय की परवाह किए बग़ैर
सबके अनजाने सुदूर ताकती
प्रोषितभर्तृका नायिकाओं को;
कुमुदिनी-भरे तालाब के स्नान-घाट पर
महावर लगे पाँव रगड़ते हुए
किसी दूर स्वप्नलोक में कोई किशोरियों से
बात-बात में मजाक़ करके
हँसते-हँसते लोटपोट होतीं
स्नेह-भरी भाभियों को;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
हल्दी की पत्तियों और मालपुए की महक
साँझ के अँधेरे में बरामदे से
टिकी बैठी देवी-सी दादी माँ
अल्पनाएँ, दशहरे की चहल-पहल
लक्ष्मी के चरण बाहरी द्वार से अन्दर कमरे तक;
ले जाता हूँ भागवत की छोटी-छोटी पंक्तियाँ
प्रसाद के कण और जगन्नाथ जी की दो गोल-गोल आँखों के
अभय वर;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
वही पुराना टेबल
जिस पर जमी धूल नज़रअन्दाज़ कर
इकट्ठी हो रहती हैं
मेरी किताबें-कॉपियाँ, ध्यान और धारणाएँ;
पिताजी के हाथ लग-लग कर आधी फटी
और तेल से चिकटी पुरानी गीता;
कमरे के चारों कोनों में भरे होते हैं
मेरे बेटा-बेटी के तमाम पुराने खिलौने
जिनकी ओर अब वे देखते तक नहीं
और उनके तरह-तरह के
नये-नये सपने, नये खिलौने, नयी कल्पनाएँ;
सिसकियाँ छिपाए मुस्कराहट बिखेरे
तुलसी चौरे में झुक कर
मत्था टेकती लक्ष्मी-प्रतिमा की नि:शब्द प्रार्थना।
देहरी लाँघ कहीं बाहर जाने पर
इतना मैं साथ ले जाता हूँ;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
देहरी लाँघ जहाँ भी जाता हूँ मैं
दिल्ली, कि टोकियो, कि लेनिनग्राद
काम से, कविता के लिए, चेरीफूल की सभा में
या नेवा नदी,
साथ अपने ले जाता हूँ
पूरबी हवा से झुकता बौर से लदा
घर के सामने वाला आम का पेड़
जिस पर सपने की तरह सोन चिरैया
‘छिन में है, छिन में नहीं’ वाले खेल में
छिप जाती है, दिख जाती है,
फिर छिप जाती है, फिर दिख जाती है।
बस, इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
गलियों में लुकाछिपी खेलते
छोटे-छोटे बच्चों की
निष्पाप उदास आँखें;
टूटी कुर्सी को विकेट बना
चिलचिलाती दुपहरी में
क्रिकेट खेलने में मस्त
किशोरों की उज्जवल आँखें;
धान के खेत में कीचड़ में पैर गड़ाए झुके खड़े
कुशा डेरा, रघु मलिक के
अनिश्चित, अन्धकारमय भविष्य;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
पौ फटने से पहले
कजलपाखी कौआ या कोयल पुकारने से पहले
खण्डगिरि की गुफाओं से बह कर आते
जैन मुनियों के उदात्त प्रार्थना-स्वर;
रक्तरंजित दयानदी किनारे
पश्चाताप में डूबे
सम्राट के उनींदे प्रहर;
साथ ले जाता हूँ
दिन डूबे साँझ बप्पा से पहली बार मिले
उस किशोर द्वारा
मन्दिर का कँगूरा बिठा
समुद्र में छलाँग लगा कर आत्म-विसर्जन का
दिगन्तव्यापी करुण शोक-प्रहर;
चित्रोत्पला के घाट पर स्नान-तर्पण कर
खड़ाऊ खटखटाते लौटते दादाजी के
स्नेह-भरे सुबह के स्वर;
इतना ही है मेरे लिए उड़ासी।
साथ ले जाता हूँ
टूटे मन्दिर की दीवारों से
समय की परवाह किए बग़ैर
सबके अनजाने सुदूर ताकती
प्रोषितभर्तृका नायिकाओं को;
कुमुदिनी-भरे तालाब के स्नान-घाट पर
महावर लगे पाँव रगड़ते हुए
किसी दूर स्वप्नलोक में कोई किशोरियों से
बात-बात में मजाक़ करके
हँसते-हँसते लोटपोट होतीं
स्नेह-भरी भाभियों को;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
हल्दी की पत्तियों और मालपुए की महक
साँझ के अँधेरे में बरामदे से
टिकी बैठी देवी-सी दादी माँ
अल्पनाएँ, दशहरे की चहल-पहल
लक्ष्मी के चरण बाहरी द्वार से अन्दर कमरे तक;
ले जाता हूँ भागवत की छोटी-छोटी पंक्तियाँ
प्रसाद के कण और जगन्नाथ जी की दो गोल-गोल आँखों के
अभय वर;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
साथ ले जाता हूँ
वही पुराना टेबल
जिस पर जमी धूल नज़रअन्दाज़ कर
इकट्ठी हो रहती हैं
मेरी किताबें-कॉपियाँ, ध्यान और धारणाएँ;
पिताजी के हाथ लग-लग कर आधी फटी
और तेल से चिकटी पुरानी गीता;
कमरे के चारों कोनों में भरे होते हैं
मेरे बेटा-बेटी के तमाम पुराने खिलौने
जिनकी ओर अब वे देखते तक नहीं
और उनके तरह-तरह के
नये-नये सपने, नये खिलौने, नयी कल्पनाएँ;
सिसकियाँ छिपाए मुस्कराहट बिखेरे
तुलसी चौरे में झुक कर
मत्था टेकती लक्ष्मी-प्रतिमा की नि:शब्द प्रार्थना।
देहरी लाँघ कहीं बाहर जाने पर
इतना मैं साथ ले जाता हूँ;
इतना ही है मेरे लिए उड़ीसा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book