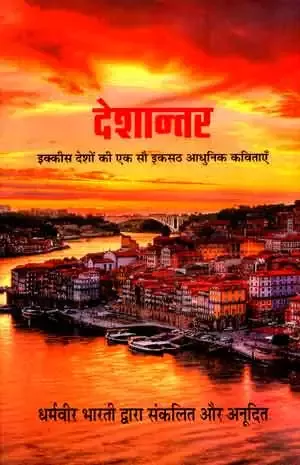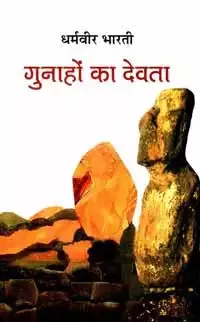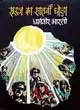|
कविता संग्रह >> देशान्तर देशान्तरधर्मवीर भारती
|
196 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत संकलन में यूरोप और अमेरिका (उत्तर और दक्षिण) के इक्कीस देशों की एक सौ इकसठ कविताओं की हिन्दी छायाएँ प्रस्तुत हैं।
Deshantar
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वक्तव्य
(प्रथम संस्करण से)
प्रस्तुत संकलन में यूरोप और अमेरिका (उत्तर और दक्षिण) के इक्कीस देशों की एक सौ इकसठ कविताओं की हिन्दी छायाएँ प्रस्तुत हैं। ये कविताएँ केवल उन कवियों की हैं जो 20 वीं शताब्दी में प्रख्यात हुए। आज जिसे हम आधुनिक काव्यबोध कहते हैं, उसे निर्मित करने में इन सबका हाथ रहा है। संकलित कवियों में से कुछ अपनी भाषा के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक कवि माने जाते हैं, कुछ को लेकर काफ़ी वाद-विवाद चलता रहा है, कुछ में सम्भावनाएँ हैं और अभी वे पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो पाये और कुछ की सम्भावनाएँ उनकी असमय मृत्यु के कारण पूर्णतया विकसित नहीं हो पायीं। कुछ कवि ऐसे भी हैं जो अपेक्षाकृत अल्पख्यात हैं किन्तु उनकी कतिपय कृतियाँ आधुनिक भावभूमि के किसी विशेष क्षेत्र का उद्घाटन करती हैं अतः वे संकलनीय नहीं। कुछ महत्त्वपूर्ण कवि ऐसे भी हैं। जिनका अनुवाद करना सम्भव नहीं प्रतीत हो सका, अतः उनकी कृतियाँ सम्मिलित नहीं की जा सकीं। यह संकलन समूचे आधुनिक काव्य का सर्वांग-सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, यह मेरा दावा क़तई नहीं है। यह केवल उसकी वैविध्य की बानगी प्रस्तुत करता है।
यों तो जब कभी दो सांस्कृतिक धाराओं में परस्पर सम्मिलन हुआ है, अनुवाद बराबर आदान-प्रदान का एक उपयोगी माध्यम रहा है। लेकिन आधुनिक सन्दर्भ में नये कवि के लिए काव्य का अनुवाद एक दूसरा महत्त्व भी रखता है। क्या कारण है कि एज़रा पाउण्ड से बोरिस पास्तरनाक तक किन्हीं विशेष स्थितियों में अनुवाद कार्य की ओर झुकते दीख पड़ते हैं।
इसका एक विशेष कारण है।
मध्य युग में कवि-कर्म का एक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग था-गुरुशिष्य परम्परा। प्रत्येक उदीयमान कवि किसी रससिद्ध कवि को गुरु के रूप में स्वीकारता था जिसे इस्लाह (परामर्श) देने, शिष्य के लेखन में संशोधन (तकमीन) करने का पूरा अधिकार रहता था। इन परामर्शों के अनुसार कवि अभ्यास करता था और परिपक्वता और प्रौढ़ता तक पहुँचते-पहुँचते स्वयं अपनी निजी शैली को खोजता और प्रतिष्ठित करता था।
आधुनिक कविता जिस क्रान्तिकारी भाव-भूमि में पनपी उसमें यह गुरु-निर्देशित अनुशासित अभ्यास की परम्परा न केवल अनावश्यक वरन् बाधक और हानिकार प्रतीत हुई और समाप्त हो गयी। यही नहीं वरन् काव्य-सम्प्रदाय जितनी तेज़ी से बदले उसमें गुरु शिष्य का तो प्रश्नदूर हर नयी पीढ़ी ने तो अनिवार्यतः अपने को पुरानी पीढ़ी से मनसा पृथक् पाया। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नया कवि कबीर की भाषा में न केवल ‘निगुरा’ रहा वरन् काव्य के क्षेत्र में अपने निगुरेपन को गर्व की वस्तु मानता रहा।
लेकिन ऊर्णनाभ की भाँति केवल अपने अन्दर से ही सारे अनुशासन बुन लेना, या तो मकड़ी ही के लिए सम्भव है या केवल ब्रह्म के लिए। प्रत्येक नये कवि को ( चाहे वह स्वीकार करे या न करे) निर्देश, अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता होती है और समय-समय पर वह इसे महसूस भी करता है। ऐसी अवस्था में अगर वह अपने तत्काल पूर्णवर्ती काव्य-सम्प्रदाय से निज को सहमत नहीं पाता तो उनसे भी और पहले के कवियों में अपनी प्रकृति के अनुकूल कवियों को चुनकर उनके काव्य का अवगाहन करता है, उनका अनुवाद कर अभ्यास करता है और इस तरह अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाता है। यह उसी की रचना प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। मसलन रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा पहले ब्रजबूलि के कवियों और बाद में कबीर तथा बाउलों की खोज। कभी कभी इस खोज के लिए कवि देश-देशान्तर के काव्य की ओर निगाह दौड़ाता है और उसमें से अपनी प्रकृति के अनुकूल काव्य कृतियों को खोजता है : मसलन एज़रा पाउण्ड द्वारा चीनी कविताओं की खोज।
किन्तु यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। आधुनिक प्रकृति उतने निष्क्रिय समर्पण की नहीं है कि जिस क्षण ‘भई रे पूता गुरू सौं भेंट’ उसी क्षण अपना दायित्व समाप्त समझ ले। आधुनिक प्रकृति के अनुसार यह खोज उन अर्थों में अब गुरु की खोज न होकर एक सफल और समर्थ ‘समानधर्मा’ की खोज होती है। यह समानधर्मी कृतित्व खोजता है, वह एक कवि में मिले या कई कवियों में, एक भाषा में मिले या कई भाषाओं में, एक काव्यधारा में मिले या कई काव्यधाराओं में।
जब कहीं किसी दूसरी भाषा में इस तरह के किसी कृतित्व की उपलब्धि नये कवि को होती है तो उसका सहज उत्साह उस कृतित्व को अपनी भाषा में पुनः प्रस्तुत करना चाहता है। उसको सहसा यह लगता है कि ‘अरे सचमुच बिलकुल यही बात तो वह कहना चाहता था पर कहने का इतना सटीक ढंग उसे नहीं आ पा रहा था।’ और वह काव्य-कृति स्वयं उसमें एक रचनात्मक उत्साह जगा देती है और अनुवाद उसी का परिणाम होता है। लेकिन यहीं पर एक कठिनाई भी आ खड़ी होती है। मूल कृति में और उसके अनुवाद के बीच में दीवारें बहुत बड़ी रहती हैं। पृथक् संस्कार, पृथक काव्य-रूढ़ियाँ पृथक् बिम्ब समूह। जोड़नेवाला तत्त्व बहुत क्षीण रहता है। और ऐसी स्थिति में सफल अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह शाब्दिक अनुवाद नहीं हो पाता और शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह सफल नहीं हो पाता। और काव्य-कला ऐसी कला है जिसमें शब्द बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
इस स्थिति को लक्षित कर एक अनुवादक ने कहा था कि ‘काव्यानुवाद की प्रकृति बिलकुल स्त्री-प्रकृति होती है। जितनी सुन्दर होगी उतनी ही अविश्वसनीय।’ स्त्री प्रकृति के बारे में तो इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ, पर अनुवादों के सम्बन्ध में मेरे ख़याल में एक बीच का रास्ता निकालने की गुंजायश है। मैंने भरसक कोशिश की है कि अनुवाद सुन्दर भी बनें और विश्वसनीय भी।
इन अनुवादों को प्रस्तुत करते समय स्वयं इन महान् कवियों की वाणी में डूबने की जो सुखद अनुभूति मिली है, जिस प्रकार कभी-कभी मेरे अन्दर कहीं कुछ जो बन्द था खुलता हुआ लगा है, जिस प्रकार मुझे आत्मीयता और समानधर्मी तत्त्व मिले हैं उनके लिए मेरा मन आदर और आभार से नत है।
यों तो जब कभी दो सांस्कृतिक धाराओं में परस्पर सम्मिलन हुआ है, अनुवाद बराबर आदान-प्रदान का एक उपयोगी माध्यम रहा है। लेकिन आधुनिक सन्दर्भ में नये कवि के लिए काव्य का अनुवाद एक दूसरा महत्त्व भी रखता है। क्या कारण है कि एज़रा पाउण्ड से बोरिस पास्तरनाक तक किन्हीं विशेष स्थितियों में अनुवाद कार्य की ओर झुकते दीख पड़ते हैं।
इसका एक विशेष कारण है।
मध्य युग में कवि-कर्म का एक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण अंग था-गुरुशिष्य परम्परा। प्रत्येक उदीयमान कवि किसी रससिद्ध कवि को गुरु के रूप में स्वीकारता था जिसे इस्लाह (परामर्श) देने, शिष्य के लेखन में संशोधन (तकमीन) करने का पूरा अधिकार रहता था। इन परामर्शों के अनुसार कवि अभ्यास करता था और परिपक्वता और प्रौढ़ता तक पहुँचते-पहुँचते स्वयं अपनी निजी शैली को खोजता और प्रतिष्ठित करता था।
आधुनिक कविता जिस क्रान्तिकारी भाव-भूमि में पनपी उसमें यह गुरु-निर्देशित अनुशासित अभ्यास की परम्परा न केवल अनावश्यक वरन् बाधक और हानिकार प्रतीत हुई और समाप्त हो गयी। यही नहीं वरन् काव्य-सम्प्रदाय जितनी तेज़ी से बदले उसमें गुरु शिष्य का तो प्रश्नदूर हर नयी पीढ़ी ने तो अनिवार्यतः अपने को पुरानी पीढ़ी से मनसा पृथक् पाया। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नया कवि कबीर की भाषा में न केवल ‘निगुरा’ रहा वरन् काव्य के क्षेत्र में अपने निगुरेपन को गर्व की वस्तु मानता रहा।
लेकिन ऊर्णनाभ की भाँति केवल अपने अन्दर से ही सारे अनुशासन बुन लेना, या तो मकड़ी ही के लिए सम्भव है या केवल ब्रह्म के लिए। प्रत्येक नये कवि को ( चाहे वह स्वीकार करे या न करे) निर्देश, अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता होती है और समय-समय पर वह इसे महसूस भी करता है। ऐसी अवस्था में अगर वह अपने तत्काल पूर्णवर्ती काव्य-सम्प्रदाय से निज को सहमत नहीं पाता तो उनसे भी और पहले के कवियों में अपनी प्रकृति के अनुकूल कवियों को चुनकर उनके काव्य का अवगाहन करता है, उनका अनुवाद कर अभ्यास करता है और इस तरह अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध बनाता है। यह उसी की रचना प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। मसलन रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा पहले ब्रजबूलि के कवियों और बाद में कबीर तथा बाउलों की खोज। कभी कभी इस खोज के लिए कवि देश-देशान्तर के काव्य की ओर निगाह दौड़ाता है और उसमें से अपनी प्रकृति के अनुकूल काव्य कृतियों को खोजता है : मसलन एज़रा पाउण्ड द्वारा चीनी कविताओं की खोज।
किन्तु यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। आधुनिक प्रकृति उतने निष्क्रिय समर्पण की नहीं है कि जिस क्षण ‘भई रे पूता गुरू सौं भेंट’ उसी क्षण अपना दायित्व समाप्त समझ ले। आधुनिक प्रकृति के अनुसार यह खोज उन अर्थों में अब गुरु की खोज न होकर एक सफल और समर्थ ‘समानधर्मा’ की खोज होती है। यह समानधर्मी कृतित्व खोजता है, वह एक कवि में मिले या कई कवियों में, एक भाषा में मिले या कई भाषाओं में, एक काव्यधारा में मिले या कई काव्यधाराओं में।
जब कहीं किसी दूसरी भाषा में इस तरह के किसी कृतित्व की उपलब्धि नये कवि को होती है तो उसका सहज उत्साह उस कृतित्व को अपनी भाषा में पुनः प्रस्तुत करना चाहता है। उसको सहसा यह लगता है कि ‘अरे सचमुच बिलकुल यही बात तो वह कहना चाहता था पर कहने का इतना सटीक ढंग उसे नहीं आ पा रहा था।’ और वह काव्य-कृति स्वयं उसमें एक रचनात्मक उत्साह जगा देती है और अनुवाद उसी का परिणाम होता है। लेकिन यहीं पर एक कठिनाई भी आ खड़ी होती है। मूल कृति में और उसके अनुवाद के बीच में दीवारें बहुत बड़ी रहती हैं। पृथक् संस्कार, पृथक काव्य-रूढ़ियाँ पृथक् बिम्ब समूह। जोड़नेवाला तत्त्व बहुत क्षीण रहता है। और ऐसी स्थिति में सफल अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह शाब्दिक अनुवाद नहीं हो पाता और शाब्दिक अनुवाद प्रस्तुत करें तो वह सफल नहीं हो पाता। और काव्य-कला ऐसी कला है जिसमें शब्द बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
इस स्थिति को लक्षित कर एक अनुवादक ने कहा था कि ‘काव्यानुवाद की प्रकृति बिलकुल स्त्री-प्रकृति होती है। जितनी सुन्दर होगी उतनी ही अविश्वसनीय।’ स्त्री प्रकृति के बारे में तो इस कथन से पूर्णतया सहमत हूँ, पर अनुवादों के सम्बन्ध में मेरे ख़याल में एक बीच का रास्ता निकालने की गुंजायश है। मैंने भरसक कोशिश की है कि अनुवाद सुन्दर भी बनें और विश्वसनीय भी।
इन अनुवादों को प्रस्तुत करते समय स्वयं इन महान् कवियों की वाणी में डूबने की जो सुखद अनुभूति मिली है, जिस प्रकार कभी-कभी मेरे अन्दर कहीं कुछ जो बन्द था खुलता हुआ लगा है, जिस प्रकार मुझे आत्मीयता और समानधर्मी तत्त्व मिले हैं उनके लिए मेरा मन आदर और आभार से नत है।
इलाहाबाद
16 जून, 1960
16 जून, 1960
धर्मवीर भारती
प्रस्तावना
जाँ स्टार अण्टर मेयेर
सृजन का शब्द
आरम्भ में केवल शब्द था
किन्तु उसकी सार्थकता थी श्रुति बनने में
कि वह किसी से कहा जाय
मौन को टूटना अनिवार्य था
शब्द का कहा जाना था
ताकि प्रलय का अराजक तिमिर
व्यवस्थित उजियाले में
रूपान्तरित हो
ताकि रेगिस्तान
गुलाबों की क्यारी बन जाय
शब्द का कहा जाना अनिवार्य था।
आदम की पसलियों के घाव से
इवा के मुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए
शब्द को कहा जाना था
चूँकि सत्य सदा सत्य है
आज भी अनिवार्य है
अतः आज के लिए भी शब्द है
और उसे कहा जाना अनिवार्य है।
किन्तु उसकी सार्थकता थी श्रुति बनने में
कि वह किसी से कहा जाय
मौन को टूटना अनिवार्य था
शब्द का कहा जाना था
ताकि प्रलय का अराजक तिमिर
व्यवस्थित उजियाले में
रूपान्तरित हो
ताकि रेगिस्तान
गुलाबों की क्यारी बन जाय
शब्द का कहा जाना अनिवार्य था।
आदम की पसलियों के घाव से
इवा के मुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए
शब्द को कहा जाना था
चूँकि सत्य सदा सत्य है
आज भी अनिवार्य है
अतः आज के लिए भी शब्द है
और उसे कहा जाना अनिवार्य है।
एज़रा पाउण्ड
एक लड़की
एक वृक्ष मेरे हाथों में समाविष्ट हो गया है
मेरी बाँहों में अन्दर-अन्दर वृक्ष रस चढ़ रहा है
वृक्ष मेरे वक्ष में उग गया है
अधोमुखी,
डालें मुझमें से उग रही हैं-बाँहों की तरह
वृक्ष वह तुम हो
तुम हो हरी काई
तुम हो वायलेट के फूल जिन पर हवा लहराती है
एक शिशु-और इतने ऊँचे-तुम हो
और देखो तो दुनिया के लिए यह मात्र नादानी है !
मेरी बाँहों में अन्दर-अन्दर वृक्ष रस चढ़ रहा है
वृक्ष मेरे वक्ष में उग गया है
अधोमुखी,
डालें मुझमें से उग रही हैं-बाँहों की तरह
वृक्ष वह तुम हो
तुम हो हरी काई
तुम हो वायलेट के फूल जिन पर हवा लहराती है
एक शिशु-और इतने ऊँचे-तुम हो
और देखो तो दुनिया के लिए यह मात्र नादानी है !
अक्र चहार का मक़बरा
मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, निकुपतिस्, मैंने निगरानी की है
पिछले पचास लाख वर्षों से, और तुम्हारी मुर्दा आँखें
हिलीं नहीं, न मेरे रति-संकेतों को समझ सकीं
और तुम्हारे कृश अंग, जिसमें मैं धधकती हुई चलती थी,
अब मेरे या अन्य किसी अग्निवर्णी वस्तु के स्पर्श से धधक नहीं उठते !
देखो तुम्हारे सिरहाने तकिया लगाने को घास उग आयी है
और चूमती है तुम्हें अपनी अगणित पल्लव-जिह्वाओं से
पर मैं तुम्हारे चुम्बनों से वंचित हूँ
मैं दीवार के स्वर्णाक्षर पढ़ चुकी हूँ
और उनके प्रतीकों पर अपनी चिन्तना थका चुकी हूँ
और इस मक़बरे में अब कोई भी नयापन शेष नहीं रहा
मैंने तुम्हारा बहुत ख़याल रक्खा है।
देखो मैंने मद्य-मंजूषाओं के
मोम-चिह्न नहीं तोड़े कि
तुम कहीं जागकर मदिरा की एक घूँट न पीना चाहो
और तुम्हारे समस्त वस्त्रों की शिक़नें मैं ठीक करती रही हूँ
मैं कैसे भूलूँ ओ निर्मोही !
कुछ ही दिनों पहले मैं नदी थी...
नहीं ?
हाँ; तुम कितने किशोर थे
और तुम पर तीन आत्माएँ मँडरा रही थीं,
और मैं आयी
और बहती हुई तुममें प्रविष्ट हो गयी,
उनको अपदस्थ करती हुई
मैं तुमसे एकमेक रही हूँ,
तुमको रत्ती-रत्ती जानती हूँ
क्या मैंने तुम्हारी हथेलियाँ और अँगुलियों के पोर नहीं छुए हैं ?
मैं तुममे आयी,
तुम्हारे आरपार गयी,
एड़ियों के आसपास तक
और आना जाना क्या ?
क्या मैं ही तुम नहीं थी ?
केवल तुम ?
और इस स्थान में कण-भर धूप भी
मुझे चैन देने नहीं आती
गहन तिमिर मुझे चीर रहा है
और मुझ पर ज्योति अवतरित नहीं होती,
और तुम भी एक शब्द नहीं कहते,
दिन-पर-दिन बीत जाते हैं।
ओह मैं मुक्त हो सकती हूँ, सील मुहर
और द्वार पर की गयी तमाम शिल्पकारी के बावजूद
हरे काँच से बाहर जा सकती हूँ...
किन्तु यहाँ शान्ति है
अतः कौन जाय ?
पिछले पचास लाख वर्षों से, और तुम्हारी मुर्दा आँखें
हिलीं नहीं, न मेरे रति-संकेतों को समझ सकीं
और तुम्हारे कृश अंग, जिसमें मैं धधकती हुई चलती थी,
अब मेरे या अन्य किसी अग्निवर्णी वस्तु के स्पर्श से धधक नहीं उठते !
देखो तुम्हारे सिरहाने तकिया लगाने को घास उग आयी है
और चूमती है तुम्हें अपनी अगणित पल्लव-जिह्वाओं से
पर मैं तुम्हारे चुम्बनों से वंचित हूँ
मैं दीवार के स्वर्णाक्षर पढ़ चुकी हूँ
और उनके प्रतीकों पर अपनी चिन्तना थका चुकी हूँ
और इस मक़बरे में अब कोई भी नयापन शेष नहीं रहा
मैंने तुम्हारा बहुत ख़याल रक्खा है।
देखो मैंने मद्य-मंजूषाओं के
मोम-चिह्न नहीं तोड़े कि
तुम कहीं जागकर मदिरा की एक घूँट न पीना चाहो
और तुम्हारे समस्त वस्त्रों की शिक़नें मैं ठीक करती रही हूँ
मैं कैसे भूलूँ ओ निर्मोही !
कुछ ही दिनों पहले मैं नदी थी...
नहीं ?
हाँ; तुम कितने किशोर थे
और तुम पर तीन आत्माएँ मँडरा रही थीं,
और मैं आयी
और बहती हुई तुममें प्रविष्ट हो गयी,
उनको अपदस्थ करती हुई
मैं तुमसे एकमेक रही हूँ,
तुमको रत्ती-रत्ती जानती हूँ
क्या मैंने तुम्हारी हथेलियाँ और अँगुलियों के पोर नहीं छुए हैं ?
मैं तुममे आयी,
तुम्हारे आरपार गयी,
एड़ियों के आसपास तक
और आना जाना क्या ?
क्या मैं ही तुम नहीं थी ?
केवल तुम ?
और इस स्थान में कण-भर धूप भी
मुझे चैन देने नहीं आती
गहन तिमिर मुझे चीर रहा है
और मुझ पर ज्योति अवतरित नहीं होती,
और तुम भी एक शब्द नहीं कहते,
दिन-पर-दिन बीत जाते हैं।
ओह मैं मुक्त हो सकती हूँ, सील मुहर
और द्वार पर की गयी तमाम शिल्पकारी के बावजूद
हरे काँच से बाहर जा सकती हूँ...
किन्तु यहाँ शान्ति है
अतः कौन जाय ?
समापन वाक्य
ओ मेरे गीतो
इतनी उत्कण्ठा और जिज्ञासा से क्यों देखते हो तुम लोगों के चेहरों में
क्या उनमें तुम्हें अपने गुज़रे खोये मिल जाएँगे ?
इतनी उत्कण्ठा और जिज्ञासा से क्यों देखते हो तुम लोगों के चेहरों में
क्या उनमें तुम्हें अपने गुज़रे खोये मिल जाएँगे ?
वालेस स्टीवेन्स
गोदना
रोशनी मकड़ी है
जल पर रेंगती है
बर्फ़ के किनारों पर
तुम्हारी पलकों के तले
और वहाँ अपना जाला बुनती है
अपने दो जाले
तुम्हारे नेत्रों के जाले
हिलगे हैं, तुम्हारे
माँस और अस्थियों से
जैसे छत की कड़ियों या घासों से
तुम्हारे नेत्रों के डोरे हैं
जल की सतह पर
बर्फ़ के छोरों पर।
जल पर रेंगती है
बर्फ़ के किनारों पर
तुम्हारी पलकों के तले
और वहाँ अपना जाला बुनती है
अपने दो जाले
तुम्हारे नेत्रों के जाले
हिलगे हैं, तुम्हारे
माँस और अस्थियों से
जैसे छत की कड़ियों या घासों से
तुम्हारे नेत्रों के डोरे हैं
जल की सतह पर
बर्फ़ के छोरों पर।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book