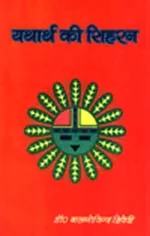|
गजलें और शायरी >> यथार्थ की सिहरन यथार्थ की सिहरनबाल गोविन्द द्विवेदी
|
98 पाठक हैं |
||||||
यथार्थ की सिहरन डॉ द्विवेदी की शताधिक हिन्दी-गजलों का संकलन है, जो कवि की जाग्रत, जीवन्त एवं ज्वलन्त काव्य-चेतना की विनम्र किन्तु आत्म-विश्वास से सम्पुट तथा प्रभावी प्रस्तुति है-
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
यथार्थ की सिहरन : विहंगावलोकन
‘‘समय के गीत को गाओ तो गज़ल होती है।
नेह सागर में नहाओ तो गजल होती है।’’
नेह सागर में नहाओ तो गजल होती है।’’
ग़ज़ल की उत्पत्ति-व्युत्पत्ति के संबंध में अनेकानेक अवधारणाएँ प्रचलित
हैं। अरबी के ‘तश्बीब’ के प्रारंभिक अंश ग़ज़ल के
नवांकुरण
हैं। प्रेम-संलाप, सौन्दर्य-परिदर्शन ग़ज़ल के व्यंजक अर्थ हैं। हिन्दी साहित्य
के प्रारम्भिक काल में ग़ज़ल लिखी गयी। प्रसाद, निराला, रामप्रसाद
‘बिस्मिल’ इस धारा में अवगाहित रहे। आगे इसकी सशक्त
धारा,
ओजस्विता होकर प्रभुविष्णुता के साथ प्रवाहित हुई।
ग़ज़ल के साथ एक युग ऐसा भी जुड़ा था, जो रीतिकालिक कवियों के सदृश्य दमित काम भावनाओं को उजागर करते थे; लेकिन प्रगति सोपान नूतन ग़ज़ल के पग बाँध न सके। पुरातन केंचुल को उतार फेंक वारांगना कुलवधू बनी। उसमें राष्ट्रीय चेतना के स्वर, प्रकृति-वर्णन, प्रेम का उदात्त स्वरूप, शोषण के विरुद्ध शंखनाद, सामाजिक विद्रूपताओं पर करारा प्रहार उसके वर्ण्य विषय बने।
दुष्यन्त की ग़ज़लों के साथ जिस नये युग की प्रस्तावना अंकित हुई, परवर्ती रचनाकारों ने अपनी-अपनी जीवन-दृष्टि, अनुभव की उष्मा और अभिव्यंजना के प्रभावी तेवरों के द्वारा उसे नये-नये आयामों के साथ अध्यायों से समृद्ध किया।
डॉ. बालगोविन्द द्विवेदी युवा पीढ़ी के उन समर्थ रचनाकारों में हैं; जिनके पास कारयित्री प्रतिभा नवोन्मेषी शक्तिमतता और जिनके हस्ताक्षर कविता की प्राची के क्षितिज पर उतरती अरुणिमा से आगे बढ़कर अब मध्याकाश को आलोकित कर रहे हैं।
‘यथार्थ की सिहरन’ डॉ. द्विवेदी की शताब्दी हिन्दी-ग़ज़लों का संकलन है, जो कवि की जागृत, जीवन्त एवं ज्वलन्त काव्य-चेतना की विनम्र किन्तु आत्म-विश्वास से सम्पुट तथा प्रभावी प्रस्तुति है-
ग़ज़ल के साथ एक युग ऐसा भी जुड़ा था, जो रीतिकालिक कवियों के सदृश्य दमित काम भावनाओं को उजागर करते थे; लेकिन प्रगति सोपान नूतन ग़ज़ल के पग बाँध न सके। पुरातन केंचुल को उतार फेंक वारांगना कुलवधू बनी। उसमें राष्ट्रीय चेतना के स्वर, प्रकृति-वर्णन, प्रेम का उदात्त स्वरूप, शोषण के विरुद्ध शंखनाद, सामाजिक विद्रूपताओं पर करारा प्रहार उसके वर्ण्य विषय बने।
दुष्यन्त की ग़ज़लों के साथ जिस नये युग की प्रस्तावना अंकित हुई, परवर्ती रचनाकारों ने अपनी-अपनी जीवन-दृष्टि, अनुभव की उष्मा और अभिव्यंजना के प्रभावी तेवरों के द्वारा उसे नये-नये आयामों के साथ अध्यायों से समृद्ध किया।
डॉ. बालगोविन्द द्विवेदी युवा पीढ़ी के उन समर्थ रचनाकारों में हैं; जिनके पास कारयित्री प्रतिभा नवोन्मेषी शक्तिमतता और जिनके हस्ताक्षर कविता की प्राची के क्षितिज पर उतरती अरुणिमा से आगे बढ़कर अब मध्याकाश को आलोकित कर रहे हैं।
‘यथार्थ की सिहरन’ डॉ. द्विवेदी की शताब्दी हिन्दी-ग़ज़लों का संकलन है, जो कवि की जागृत, जीवन्त एवं ज्वलन्त काव्य-चेतना की विनम्र किन्तु आत्म-विश्वास से सम्पुट तथा प्रभावी प्रस्तुति है-
‘‘सत्य में आस्था पाले वही सच्चा लगता
कर्म निष्काम जो करता, वही अच्छा लगता
जिन्दगी राख की ढेरी, प्रमाद-घन छाया
कर्म में स्वेद बहाये, वही अच्छा लगता।।’’
कर्म निष्काम जो करता, वही अच्छा लगता
जिन्दगी राख की ढेरी, प्रमाद-घन छाया
कर्म में स्वेद बहाये, वही अच्छा लगता।।’’
इसमें गीता के आर्ष छन्द ध्वनित होते हैं। वर्तमान परिवेश के प्रति कवि
सजग है, आज आम समस्या है रोजी-रोटी की। समस्याओं का प्रस्तुतीकरण ही रचना
को कालजयी बनाता है। देश की स्वतंत्रता का लाभ उठाने वाले नेता आम आदमी को
भय और भूख से मुक्ति नहीं दिला सके। यह बात कवि-मन को कचोटती है
‘‘दर-दर की ठोकरों में फंसा आदमी,
नेता मनायें जश्न, वही हो गये स्वतंत्र।’’
नेता मनायें जश्न, वही हो गये स्वतंत्र।’’
आजादी के साथ ही औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्ति मिल गई किन्तु अपनो ने उनसे
कहीं अधिक शोषण और दोहन का गुरुतर भार संभाल लिया। रक्षक ही भक्षक हो गये।
माली ही उपवन में आग लगाने को तत्पर रहने लगा-
‘‘चमन की पौध के विश्वास का मंदिर माली,
बागबाँ आग लगाये तो कहीं और चलें।’’
बागबाँ आग लगाये तो कहीं और चलें।’’
धर्म के ठेकेदार गरीबों को, धर्म की अफीम पिलाकर, अपने अनुसार अपने पीछे
चलने को मजबूर करते हैं। कवि का विरोध स्वाभाविक है-
‘‘शिवलिंग में दूध-पुष्प-मधु दिन में चढ़ा रहे,
महफिल सजी जो रात में, पीने लगे वो जाम।
श्रद्धा औ, भक्ति बिक रही, बाजार लग रहे,
बिकती हैं आस्थायें, बिकने लगे हैं धाम।’’
महफिल सजी जो रात में, पीने लगे वो जाम।
श्रद्धा औ, भक्ति बिक रही, बाजार लग रहे,
बिकती हैं आस्थायें, बिकने लगे हैं धाम।’’
महंत-मौलवी, पंडा-पुजारी आधुनिकतम् सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं।
भौतिकता से जन्मी विकृतियों का पोषण कर रहे हैं। उनको दान देने वाला आदमी
गरीबी, विवशता और अवसाद में जी रहा है। कवि का मन विद्रोह कर उठता है-
‘‘रंगाये वस्त्र सभी, मन रंगा नही पाये,
पाप के पंक में, दिन रात मौज करते हैं।
सुबह से शाम तक पूजा-नमाज की आदत,
स्वप्न में भी किसी पूजा की बात करते हैं।’’
पाप के पंक में, दिन रात मौज करते हैं।
सुबह से शाम तक पूजा-नमाज की आदत,
स्वप्न में भी किसी पूजा की बात करते हैं।’’
योगियों, गुरुओं, बापुओं और उपदेशकों की भीड़ बढ़ रही है। तथाकथित
महात्माओं के उद्योग-धंधे फल-फूल रहे हैं। उनके परिवारी-जन और संगी-साथी
वायुयानों, वातानुकूलित वाहनों और महलों के उपभोग का आनंद ले रहे हैं।
किन्तु उन्हें भगवान मानने वाले दरिद्रता के बोझ से पीड़ित हैं। कवि जन-मन
की पीड़ा का अनुभव करता है-
‘‘गुरुओं, पुजारियों की भीड़ बढ़ रही है नित,
चिर साधना के पंथ सभी रौंद रहे हैं।
माया के ब्यूह में फँसे उपदेश दे रहे,
गुमराह करके जग को, सब नोच रहे हैं।।’’
चिर साधना के पंथ सभी रौंद रहे हैं।
माया के ब्यूह में फँसे उपदेश दे रहे,
गुमराह करके जग को, सब नोच रहे हैं।।’’
इसीलिए कवि जन सामान्य से कहता है-
‘‘सर्वत्र सत्य व्याप्त है, कण-कण में विद्यमान,
तीरथ के पत्थरों को, सब पूज रहे हैं।
तुम ब्रह्म हो, स्वयं के ज्ञान-चक्षु खोल लो,
तम में फँसे आडम्बरों से जूझ रहे हैं।’’
तीरथ के पत्थरों को, सब पूज रहे हैं।
तुम ब्रह्म हो, स्वयं के ज्ञान-चक्षु खोल लो,
तम में फँसे आडम्बरों से जूझ रहे हैं।’’
उनको अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है-
‘‘कर्म निष्काम करो, दुनिया से डरते क्यों हो ?
कर्म पूजा है तो परिणाम से डरते क्यों हो ?
विषाद-ग्लानि, हीन-भावना मन से त्यागो,
अजातशत्रु हो, अंजाम से डरते क्यों हो ?’’
कर्म पूजा है तो परिणाम से डरते क्यों हो ?
विषाद-ग्लानि, हीन-भावना मन से त्यागो,
अजातशत्रु हो, अंजाम से डरते क्यों हो ?’’
समाज में दु:ख का मूल कारण नैतिक मूल्यों का क्षरण, ईर्ष्या-द्वेष-दंभ,
स्वार्थपरता और छल-कपट का बोलबाला। परिमाणत: वासना-पंक में डूबता मानव-मन।
कवि ठीक ही कहता है-
‘‘वासना-पंक में मन सतत फँस रहा,
ज्ञान की दिव्य-धारा बही जा रही।
प्रीति की संपदा लहलहाती फसल,
द्वेष की आग से सब जली जा रही।।’’
ज्ञान की दिव्य-धारा बही जा रही।
प्रीति की संपदा लहलहाती फसल,
द्वेष की आग से सब जली जा रही।।’’
विकृतियों को गले लगाने के फलस्वरूप-
‘‘कुंठित है चेतना की
धार, जी रहे हैं लोग,
चिंतन है तार-तार, गरल पी रहे हैं लोग।
विश्वास-चोट खा रहा, गिर-गिर के उठ रहा,
सिहरन है बेशुमार, अधर सी रहे हैं लोग।।
चिंतन है तार-तार, गरल पी रहे हैं लोग।
विश्वास-चोट खा रहा, गिर-गिर के उठ रहा,
सिहरन है बेशुमार, अधर सी रहे हैं लोग।।
इन परिस्थितियों में भी, भूखे इन्सान को पूजा के पंथ बाँट रहे हैं-
‘‘भूखा मनुष्य मर रहा, इन्सानियत मरी,
पूजा के पंथ, आदमी को बांट रहे हैं।’’
पूजा के पंथ, आदमी को बांट रहे हैं।’’
आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है, इसका परिहार्य अनिवार्य है। हिंसा की चरम
सीमा, चतुर्दिक, हाहाकार, चीत्कार फैलाए है, विध्वंस की लपटें प्रत्येक घर
को जला रही हैं-
‘‘सौहार्द-प्रेम-भाव का बहता था समीकरण
रिश्तों के बीच भर रहा, बारूद का धुआँ।’’
रिश्तों के बीच भर रहा, बारूद का धुआँ।’’
कवि उन्हें धैर्य बँधाता है-
‘‘धूम हो धुंध हो, दिखता नहीं कोई अपना,
समय का ज्वार है, धीरे से उतर जाने दो।।’’
समय का ज्वार है, धीरे से उतर जाने दो।।’’
सम्पूर्ण देश आतंक की छाया में जी रहा है। भय जन-सामान्य के मानस में गहरे
तक उतर आया है-
‘‘अधिकार छिन रहे थे, हम देखते रहे,
कलियों का रौंदना भी, हम देखते रहे।
नारी की लाज लुट रही थी राजमार्ग पर,
भय इस कदर बढ़ा कि हम देखते रहे।।’’
कलियों का रौंदना भी, हम देखते रहे।
नारी की लाज लुट रही थी राजमार्ग पर,
भय इस कदर बढ़ा कि हम देखते रहे।।’’
कवि आम आदमी की विपत्तियों में उसके साथ है। वह ज्ञान देता है कि यह
परिस्थितियाँ नयी नहीं हैं-
‘‘सदा धृतराष्ट्र-पुत्रों ने, अनय के बीज बोये हैं,
भटकते ही रहे पाण्डव, कहीं कुछ भी नहीं बदला।’’
भटकते ही रहे पाण्डव, कहीं कुछ भी नहीं बदला।’’
इसलिए,
‘‘नये संकल्प चुनना है, जगाओ कर्म पर आस्था,
बढ़ाओ मनन-चिंतन को, ज्ञान-गुण-सूक्त कुछ गुन लो।’’
बढ़ाओ मनन-चिंतन को, ज्ञान-गुण-सूक्त कुछ गुन लो।’’
कवि अभिजात्य वर्ग को हृदय-परिवर्तन का संदेश देता है-
‘‘अपना महल सजाने में सदियों गुजार दीं,
अंधेरों में कोई दीप, जलाकर तो देखिए।’’
अंधेरों में कोई दीप, जलाकर तो देखिए।’’
नेताओं से कहता है-
‘‘सद्भावना सिखा रहे, जनता को रात-दिन,
दीवार-दृढ़ अहं की, मिटाकर तो देखिए।’’
दीवार-दृढ़ अहं की, मिटाकर तो देखिए।’’
आजकल नेता, नेता कम अभिनेता ज्यादा हैं-
‘‘जनाकांक्षा रो रही, नेतृत्व की रंगीनियों से,
दिग्भ्रमित है लोक, नेता सत्व को झुठला रहा है।’’
दिग्भ्रमित है लोक, नेता सत्व को झुठला रहा है।’’
गाँव-गिराँव में भाईचारे, सौहार्द्र की परंपरा थी, भौतिकता की चमक-दमक
में; मात्र विद्वेष का धुँआ धुंधला रहा है। संकट में शत्रु की भी मदद करना
भारतीय संस्कृति थी; आज उसका विलोपन हो गया, जातिवाद-विष चतुर्दिक फैल
चुका है; इसका कारण कलुषित राजनीति है-
‘‘घुल गया विद्वेष का विष, गली-कूचे की पवन में
पंक में है गरल इतना, अब नहीं उगता कमल है’’
पंक में है गरल इतना, अब नहीं उगता कमल है’’
और-
‘‘गरल ईर्ष्या-द्वेष का वातावरण कलुषित हुआ
भ्रमित मन ऐसा, स्वयं को डस रहा है आदमी।।’’
भ्रमित मन ऐसा, स्वयं को डस रहा है आदमी।।’’
परिणामत:-
‘‘धर्मान्धता ने ही जलाये, आदमी-इन्सानियत,
जल गयी करुणा-दया-सद्भावना चित्कार कर।’’
जल गयी करुणा-दया-सद्भावना चित्कार कर।’’
और साथ ही-
‘‘गरीबों के साथ चल रही, साजिश बेगार की
सरकार पूछती है, क्या मर रहे हैं लोग।।’’
सरकार पूछती है, क्या मर रहे हैं लोग।।’’
मानव-जीवन के अन्य विभिन्न पहलुओं की भाँति डॉ. द्विवेदी जी ने राष्ट्रीय
भावनाओं को भी उदात्त अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने राष्ट्र-देवता शहीदों के
चरणों में अनेक श्रद्धाप्रवण वन्दनाओं एवं प्रेरक प्रशस्तियों के शब्द
सुमन भी अर्पित किये हैं-
‘‘हम नभग बन उड़ें, विश्व-आकाश में
राष्ट्र हित में जनम औ’ मरण चाहिए।’’
राष्ट्र हित में जनम औ’ मरण चाहिए।’’
और-
‘‘सर्वस्व लुटा हँसते रहे देश के लिए,
उनको भी याद कर न सके, कैसे हैं ये गीत।’’
उनको भी याद कर न सके, कैसे हैं ये गीत।’’
कवि के पास यदि अनुभूति की पूँजी है, तो स्वाध्याय का वैभव भी कम नहीं,
साथ ही उसके पास कलात्मक क्षमता भी है, जो अनुभूति और अध्ययन को समन्वित
करके परम्परा से प्राप्त प्रतीकों को युगानुरूप सन्दर्भों की उद्भावना
करके हमें चमत्कृत भी करती है, आनन्दित भी-
‘‘डोलियां नित खोजतीं कंधा कहारों का।
चिर प्रतीक्षा-रत रहा, पतझर बहारों का।।
चिर प्रतीक्षा-रत रहा, पतझर बहारों का।।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book