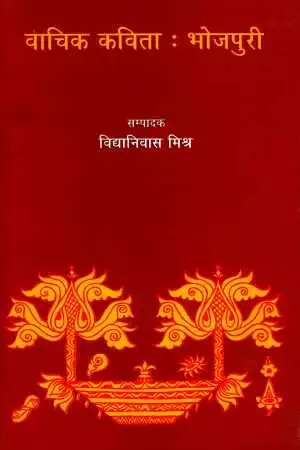|
कविता संग्रह >> वाचिक कविता भोजपुरी वाचिक कविता भोजपुरीविद्यानिवास मिश्र
|
377 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत हैं भोजपुरी कविताएँ.....
Vachik kavita bhojpuri
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय काव्य किसी न किसी रूप में वाचिक संस्कार से अभी तक सुवसित है। कविता की वाचिकता अभी भी है, और वह लोक में आदर भी पाती है। लेकिन साथ ही वाचिकता का जो सम्बन्ध अनुष्ठान की पवित्रता से था, वह कम भी हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो रस लेकर वाचिक काव्य को सुनते हैं। ऐसी स्थिति में ‘वाचिक कविताः भोजपुरी’ के प्रकाशन का एक विशेष अर्थ है।
प्रख्यात विद्वान डॉ. विद्यानिवास मिश्र द्वारा सम्पादित इस पुस्तक में अवधी की वाचिक परंपरा से जीवन्त-जाग्रत कविताएँ संकलित हैं। ये कविताएँ हृदयस्पर्शी तो हैं ही, अभिव्यक्ति के सलोनेपन के कारण अच्छी से अच्छी, बाँकी से बाँकी कविता के सामने एक चुनौती भी हैं। गीत की दृष्टि से समृद्ध अवधी की वाचिक परम्परा का यह संकलन सर्वथा प्रासंगिक है।
प्रख्यात विद्वान डॉ. विद्यानिवास मिश्र द्वारा सम्पादित इस पुस्तक में अवधी की वाचिक परंपरा से जीवन्त-जाग्रत कविताएँ संकलित हैं। ये कविताएँ हृदयस्पर्शी तो हैं ही, अभिव्यक्ति के सलोनेपन के कारण अच्छी से अच्छी, बाँकी से बाँकी कविता के सामने एक चुनौती भी हैं। गीत की दृष्टि से समृद्ध अवधी की वाचिक परम्परा का यह संकलन सर्वथा प्रासंगिक है।
भूमिका
यों तो भारतीय संस्कृति-मात्र वाचिक परम्परा की परिणित है, पर भारतीय काव्य किसी-न-किसी रूप में वाचिक संस्कार से अभी तक सुवासित है। कविता की वाचिकता किसी-न-किसी रूप में अभी भी है, लोक में आदर पाती है। यह अवश्य है कि वाचिकता का सम्बन्ध अनुष्ठान की पवित्रता से था वह काफ़ी-कुछ कम हो गया है। लोकगीतों को लोग अब अनुष्ठान के साथ सुनने के बजाय या तो कैसेट पर सुनना चाहते हैं या फिर उसकी सामाजिक शव-परीक्षा करना चाहते हैं। रस लेकर उन गीतों को तभी सुना जा सकता है जब उचित सन्दर्भ में रखकर देखें। वह होता नहीं इसलिए अधिक-से-अधिक हमारी दया-दृष्टि ही ऐसे साहित्य पर पड़ती है; थोड़े-से लोग हैं जिनकी कृपा-दृष्टि भी पड़ती है पर वे उसका उपयोग छिछली रूमानियत में ही करके सन्तुष्ट हो जाते हैं या फिर, उनमें अगर कोई करुण कथा है तो उसका उपयोग सामाजशास्त्रीय व्याख्या के लिए करने लगते हैं। बहुत कम लोग हैं जो लेकर इस वाचिक काव्य को सुनते हैं और सुनते हैं तो उनकी आँखें नम होती हैं। ऐसे ही लोगों पर भरोसा करके प्रस्तुत संकलन तैयार हुआ है।
हमारी कोशिश वाचिक परम्परा से जीवन्त-जाग्रत रचनाएं सुनने की रही है; अभिव्यक्ति के सलोनेपन से अच्छी-से-अच्छी, बाँकी-से-बाँकी कविता को पानी भरानेवाले हैं। कोई चाहे तो इन रचनाओं के शिल्प और बिम्ब-विधान में ही रमे, अभी तक उसमें भी रमने का कोई सिलसिला चला नहीं है। बरसों पहले मैंने सत्यव्रत अवस्थी की पुस्तक की भूमिका के रूप में शिल्प-विधान पर कुछ लिखा था, पर वह शास्त्र तो था नहीं वह लोक-साहित्य के अध्येताओं द्वारा भी अनदेखा ही रहा। आज हिन्दी क्षेत्र की लोकभाषाओं में गीत की दृष्टि से सबसे समृद्ध भोजपुरी की वाचिक परम्परा का संकलन तैयार करते हुए प्रासंगिक लगता है कि उस निबन्ध का एक बड़ा अंश यहां देखा जाए।
हम इतना मानकर तो चलें ही कि लोक-साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण्य-वस्तु लोक-जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों और प्रभावों तक सीमित है। यह तो लोक-साहित्य की पहली मर्यादा हुई। इसकी दूसरी मर्यादा है, उसकी रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का समावेत योगदान। यही कारण है कि लोक-साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है। शिल्प-विधान की बात करते समय हम जब इन दो मुख्य मर्यादाओं को सामने रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिल्प-विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि शिल्प का विधान यदि हमें दिखाता है तो वह सामाजिक समरसता की विवशता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही। वैसे प्रचलित अर्थ में शिल्प-विधान की बात यहाँ नहीं उठायी जा सकती है। लोग समझते यही हैं कि शिल्प के पीछे एक पूर्व-चिन्तित व्यापार अवश्य सन्निहित होता है और चूँकि लोक-साहित्य में ऐसा कोई व्यापार होने की सम्भावना नहीं है इसलिए उसके शिल्प-विधान की बात नहीं उठती। पर तात्त्विक दृष्टि से देखने पर शिल्प-विधान का अर्थ है अभिव्यक्ति को अभिव्यज्य से जोड़ना।
जो बात कही जा रही है, वह बात किसी रूप में कही जाए कि अभिप्रेत अर्थ ही द्योतित हो और न केवल द्योतित हो बल्कि प्रभावकारी रूप में द्योतित हो, यह उस बात से कम महत्त्व नहीं रखती और एक तरह से कहा जाय तो उस बात का अपरिहार्य अंग है। यह अंग ही शिल्प-विधान है। संस्कृति साहित्य-शास्त्र में जिसे रीति कहा गया वह शिल्प-विधान का एक अंश मात्र है। रीति की सैद्धान्तिक धारणा जो भी हो, उसका प्रायोगिक रूप मात्र वर्ण-संगठन ही है। शिल्प-विधान वर्ण-संघटना ही है। शिल्प-विधान वर्ण-संघटना के अलावा बिम्ब-विधान, लय और ताल का मेल, कथोपकथन शैली और प्रारम्भ और उपसंहार का विन्यास भी है। अँग्रेज़ी में जिसे टेकनीक कहा जाता है, और आलोचना में जिसे विधा संज्ञा दी जाती है, उससे भी शिल्प-विधान इस माने में आगे है कि टेकनीक या विधा अभिव्यक्ति की सतह पर ही रहते हैं, अभिव्यज्य की गहराई तक नहीं जाते। प्राचीन कला-शास्त्र में इसके लिए वर्तनी शब्द आया है उसका भी व्युत्पत्तिजन्य अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति का मोड़ कैसा होना चाहिए, यही वर्तनी है। शिल्प-विधान मात्र मोड़ नहीं है। यह अभिव्यक्ति का मर्म है। कला की भाषा में कहें तो यह रेखा है। इसलिए यह अभिव्यक्ति और अभिव्यज्य की सन्धि है। जैसे जोड़ का न दिखाई पड़ना ही उसकी सुन्दरता है वैसे ही इसका भी लक्षित न होना ही इसका चरम उत्कर्ष है। कला शब्द का अर्थ भी जोड़ना ही है और कला जितनी ही अलक्षित रहती है, उतनी ही प्रभावकारी हो पाती है।
इस दृष्टि से देखने से लोक-साहित्य में शिल्प-विधान अपने उत्कर्ष पर है, क्योंकि वह, सबसे अधिक यहीं पर निरभिमान, निर्व्याज और निसर्गोद्भूत है। कालिदास ने जिस ‘भ्रूविलासानभिज्ञ प्रीतिस्निग्ध-वधू-लोचन’ की छवि के द्वारा नीरद-राशि का पान कराया है, वह छवि ही इस शिल्प-विधान की जान है। बाँकपन से इसका परिचय नहीं विदग्धता का इसमें धैर्य नहीं और सँवार का इसे ध्यान नहीं। जो सौष्ठव है, वह ऐसा है कि भीतर की प्रीति से अपने-आप रच गया है और जो पानी है, वह ऐसा है, जो बिना पत्थर पर सान चढ़ाये अपने-आप के तेज से निखर गया है। कहा जा सकता है कि यह तो विषय-वस्तु की बात हुई, इसे शिल्प-विधान के अन्तर्गत क्यों लाया जा रहा है, तो उत्तर यह है कि शिल्प-विधान का अर्थ ही यह है कि वह विषय-वस्तु के साथ ऐसा मेल खाए कि विषय-वस्तु उसी के भीतर आकर रहे, उसके बाहर न जाए। अनुहार के लिए आभ्यन्तर प्रयत्न ही शिल्प-विधान है। यह आभ्यन्तर प्रयत्न लोक-साहित्य में कितने प्रकार का हो सकता है, इसकी आगे हम मीमांसा करेंगे।
लोक-साहित्य के मुख्यतः चार भेद कहे जाते हैं; लोक-गीत, लोक-गाथा, लोक-कथा और लोक-नाट्य। लोक-गाथा और लोत-कथा में भेद इतना ही है कि लोक-गाथा एक लम्बे आख्यान-गीत के रूप में चलती है और इसमें प्रबन्ध-योजना गाथा-प्रधान न होकर रस-प्रधान होती है, जबकि लोक-कथा गद्यात्मक होने के साथ-साथ कथा प्रधान या दूसरे शब्दों में घटना-प्रधान हुआ करती है। लोक-नाट्य जनसुलभ रंगमंच को दृष्टि में रखकर आंगिक और वाचिक अभिनय पर आधृत स्वांग या लीला तक सीमित रहता है। इसमें सामायिकता का विशेष ध्यान रहने के कारण स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता नहीं होती है। लोक-कथाओं और लोक-गाथाओं में कथा-शिल्प ही प्रमुख रहता है, केवल लोक-गान ऐसा प्रकार है, जिसमें अपने समग्र रूप में शिल्प-विधान विकसित हो सकता है, इन चारों प्रकार के रूपों में शिल्प-विधान के ये अंग समान रूप से अपेक्षित हैं।
पहला है शब्द या शब्द-समूहों की पुनरावृत्ति। ये शब्द या तो लोक-परम्परा में गृहीत मांगलिक विशेषणवाची होते हैं या केन्द्रभूत अर्थ के व्यंजक होते हैं। जब कोई पात्र किसी प्रश्न का उत्तर में अनुवाद देता है तो उस प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों का और उसके विशेषणों का ज्यों-का-त्यों उत्तर में अनुवाद करते हैं। जैसे प्रसंग है कि-
हमारी कोशिश वाचिक परम्परा से जीवन्त-जाग्रत रचनाएं सुनने की रही है; अभिव्यक्ति के सलोनेपन से अच्छी-से-अच्छी, बाँकी-से-बाँकी कविता को पानी भरानेवाले हैं। कोई चाहे तो इन रचनाओं के शिल्प और बिम्ब-विधान में ही रमे, अभी तक उसमें भी रमने का कोई सिलसिला चला नहीं है। बरसों पहले मैंने सत्यव्रत अवस्थी की पुस्तक की भूमिका के रूप में शिल्प-विधान पर कुछ लिखा था, पर वह शास्त्र तो था नहीं वह लोक-साहित्य के अध्येताओं द्वारा भी अनदेखा ही रहा। आज हिन्दी क्षेत्र की लोकभाषाओं में गीत की दृष्टि से सबसे समृद्ध भोजपुरी की वाचिक परम्परा का संकलन तैयार करते हुए प्रासंगिक लगता है कि उस निबन्ध का एक बड़ा अंश यहां देखा जाए।
हम इतना मानकर तो चलें ही कि लोक-साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा है और उसकी वर्ण्य-वस्तु लोक-जीवन में गृहीत चरित्रों, भावों और प्रभावों तक सीमित है। यह तो लोक-साहित्य की पहली मर्यादा हुई। इसकी दूसरी मर्यादा है, उसकी रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का समावेत योगदान। यही कारण है कि लोक-साहित्य पर व्यक्ति की छाप न होकर समग्र व्यक्ति-लोक की छाप होती है। शिल्प-विधान की बात करते समय हम जब इन दो मुख्य मर्यादाओं को सामने रखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें शिल्प-विधान के लिए कोई अभ्यास या कौशल परिलक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि शिल्प का विधान यदि हमें दिखाता है तो वह सामाजिक समरसता की विवशता के कारण अपने आप उद्भूत रूप में ही। वैसे प्रचलित अर्थ में शिल्प-विधान की बात यहाँ नहीं उठायी जा सकती है। लोग समझते यही हैं कि शिल्प के पीछे एक पूर्व-चिन्तित व्यापार अवश्य सन्निहित होता है और चूँकि लोक-साहित्य में ऐसा कोई व्यापार होने की सम्भावना नहीं है इसलिए उसके शिल्प-विधान की बात नहीं उठती। पर तात्त्विक दृष्टि से देखने पर शिल्प-विधान का अर्थ है अभिव्यक्ति को अभिव्यज्य से जोड़ना।
जो बात कही जा रही है, वह बात किसी रूप में कही जाए कि अभिप्रेत अर्थ ही द्योतित हो और न केवल द्योतित हो बल्कि प्रभावकारी रूप में द्योतित हो, यह उस बात से कम महत्त्व नहीं रखती और एक तरह से कहा जाय तो उस बात का अपरिहार्य अंग है। यह अंग ही शिल्प-विधान है। संस्कृति साहित्य-शास्त्र में जिसे रीति कहा गया वह शिल्प-विधान का एक अंश मात्र है। रीति की सैद्धान्तिक धारणा जो भी हो, उसका प्रायोगिक रूप मात्र वर्ण-संगठन ही है। शिल्प-विधान वर्ण-संघटना ही है। शिल्प-विधान वर्ण-संघटना के अलावा बिम्ब-विधान, लय और ताल का मेल, कथोपकथन शैली और प्रारम्भ और उपसंहार का विन्यास भी है। अँग्रेज़ी में जिसे टेकनीक कहा जाता है, और आलोचना में जिसे विधा संज्ञा दी जाती है, उससे भी शिल्प-विधान इस माने में आगे है कि टेकनीक या विधा अभिव्यक्ति की सतह पर ही रहते हैं, अभिव्यज्य की गहराई तक नहीं जाते। प्राचीन कला-शास्त्र में इसके लिए वर्तनी शब्द आया है उसका भी व्युत्पत्तिजन्य अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति का मोड़ कैसा होना चाहिए, यही वर्तनी है। शिल्प-विधान मात्र मोड़ नहीं है। यह अभिव्यक्ति का मर्म है। कला की भाषा में कहें तो यह रेखा है। इसलिए यह अभिव्यक्ति और अभिव्यज्य की सन्धि है। जैसे जोड़ का न दिखाई पड़ना ही उसकी सुन्दरता है वैसे ही इसका भी लक्षित न होना ही इसका चरम उत्कर्ष है। कला शब्द का अर्थ भी जोड़ना ही है और कला जितनी ही अलक्षित रहती है, उतनी ही प्रभावकारी हो पाती है।
इस दृष्टि से देखने से लोक-साहित्य में शिल्प-विधान अपने उत्कर्ष पर है, क्योंकि वह, सबसे अधिक यहीं पर निरभिमान, निर्व्याज और निसर्गोद्भूत है। कालिदास ने जिस ‘भ्रूविलासानभिज्ञ प्रीतिस्निग्ध-वधू-लोचन’ की छवि के द्वारा नीरद-राशि का पान कराया है, वह छवि ही इस शिल्प-विधान की जान है। बाँकपन से इसका परिचय नहीं विदग्धता का इसमें धैर्य नहीं और सँवार का इसे ध्यान नहीं। जो सौष्ठव है, वह ऐसा है कि भीतर की प्रीति से अपने-आप रच गया है और जो पानी है, वह ऐसा है, जो बिना पत्थर पर सान चढ़ाये अपने-आप के तेज से निखर गया है। कहा जा सकता है कि यह तो विषय-वस्तु की बात हुई, इसे शिल्प-विधान के अन्तर्गत क्यों लाया जा रहा है, तो उत्तर यह है कि शिल्प-विधान का अर्थ ही यह है कि वह विषय-वस्तु के साथ ऐसा मेल खाए कि विषय-वस्तु उसी के भीतर आकर रहे, उसके बाहर न जाए। अनुहार के लिए आभ्यन्तर प्रयत्न ही शिल्प-विधान है। यह आभ्यन्तर प्रयत्न लोक-साहित्य में कितने प्रकार का हो सकता है, इसकी आगे हम मीमांसा करेंगे।
लोक-साहित्य के मुख्यतः चार भेद कहे जाते हैं; लोक-गीत, लोक-गाथा, लोक-कथा और लोक-नाट्य। लोक-गाथा और लोत-कथा में भेद इतना ही है कि लोक-गाथा एक लम्बे आख्यान-गीत के रूप में चलती है और इसमें प्रबन्ध-योजना गाथा-प्रधान न होकर रस-प्रधान होती है, जबकि लोक-कथा गद्यात्मक होने के साथ-साथ कथा प्रधान या दूसरे शब्दों में घटना-प्रधान हुआ करती है। लोक-नाट्य जनसुलभ रंगमंच को दृष्टि में रखकर आंगिक और वाचिक अभिनय पर आधृत स्वांग या लीला तक सीमित रहता है। इसमें सामायिकता का विशेष ध्यान रहने के कारण स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता नहीं होती है। लोक-कथाओं और लोक-गाथाओं में कथा-शिल्प ही प्रमुख रहता है, केवल लोक-गान ऐसा प्रकार है, जिसमें अपने समग्र रूप में शिल्प-विधान विकसित हो सकता है, इन चारों प्रकार के रूपों में शिल्प-विधान के ये अंग समान रूप से अपेक्षित हैं।
पहला है शब्द या शब्द-समूहों की पुनरावृत्ति। ये शब्द या तो लोक-परम्परा में गृहीत मांगलिक विशेषणवाची होते हैं या केन्द्रभूत अर्थ के व्यंजक होते हैं। जब कोई पात्र किसी प्रश्न का उत्तर में अनुवाद देता है तो उस प्रश्न में प्रयुक्त शब्दों का और उसके विशेषणों का ज्यों-का-त्यों उत्तर में अनुवाद करते हैं। जैसे प्रसंग है कि-
के मोरा आगे पीछे बइठी, के लट छोरी
के मोरा जागी रयनिया के नरवा छिनाई
बन से निकरी बन तपसिन सितै समुझावैं
सीता, हम तोरा आगे-पीछे बइठब हम लट छोरब
हम तोरा जागबि रयनिया त नरवा छिनाइब
के मोरा जागी रयनिया के नरवा छिनाई
बन से निकरी बन तपसिन सितै समुझावैं
सीता, हम तोरा आगे-पीछे बइठब हम लट छोरब
हम तोरा जागबि रयनिया त नरवा छिनाइब
यह इसलिए किया जाता है कि अर्थ की प्रतीति में कोई व्यवधान न हो। इसी तरह थाली अगर हो तो सोने की ही हो, चौकी अगर हो तो चन्दन की ही हो, अटारी यदि हो तो ऊँची ही हो, बैठने की बात यदि आए तो मचिया जरूर आए, घोड़ा नीला ही हो, डोरी अगर हो तो रेशम की ही हो, सेज हो तो बेले की कलियाँ भी बिछी हों। ऐसा साहचर्य जो लोक-परम्परा में गृहीत है, लोक में कवि-समय की तरह ही अभिप्राय समझा जाता है, ऐसे जोड़ों की पुनरावृत्ति अर्थ की स्पष्टता और लोक-साहित्य की परम्परा की स्मृति के लिए की जाती है। तीसरे प्रकार की पुनरावृत्ति सामाजिक और आध्यात्मिक कारणों से होती है।
उदाहरण के लिए सात भाई के बीच में एक बहन का होना, प्रियतम के विदेश जाने पर बारह वर्ष तक एकतान प्रतीक्षा करना, ननद-भौजाई और सास-बहू के बीच विरसता की कल्पना, भाई-बहन के निश्छल स्नेह की रचना, पुत्र का पुत्री से अधिक महत्त्व होना और खरी बात कहने वाले को पहले दुःख भोगाकर समाज में विजयी बनाना-ये भारतीय लोक-साहित्य के ऐसे अभिमत तथ्य हैं कि जिन्हें सामाजिक अवस्था की परिणति ही कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीन की संख्या का महत्त्व अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, अपनी खुशी में जड़-चेतन सबको साझीदारी बनाने का उत्साह, और अपने दुख में प्रकृति को सहानुभूतिमय देखने की शक्ति-ये अभिप्राय भी ऐसे मर्मभूत सत्य के रूप में लोक-साहित्य गृहीत हुए हैं कि इनमें एक-एक-एक बात छिड़े बिना नहीं रहती। लोक, कथानकों में इन आध्यात्मिक अभिप्रायों की पुनरावृत्ति सबसे अधिक मिलती है, पुनरावृत्ति की परम्परा का स्रोत आरण्यकों और उपनिषदों में ढूँढ़ा जा सकता है। सत्य जिस रूप में समाज से परिचित होता है, उसी रूप में वह सत्य असन्दिग्ध रूप में समझा जा सकता है। दूसरे रूप में उसकी अन्यथा प्रतीत की अंशका रहती है।
इसलिए सत्य की अनुसन्धित्सा जहाँ मुख्य प्रतीति हो वहाँ सत्य को दस रंगों में रंगने की कोशिश करना उदेश्य में बाधक हो सकता है। बात कुछ अटपटी लगेगी पर उपनिषद् और लोक-साहित्य का स्वर इस माने में एक है कि समाज सत्य की उपलब्धि के लिए दोनों में समान रूप से बैचैनी है। उपनिषद् भी एक व्यक्ति की रचना नहीं, वरन् नाना प्रकार के विचारकों के चिन्तन और मनन में सहभागी, सहज-जीवन बिताने वाले समाज के द्वारा सत्य का साक्षात्कार है और लोक-साहित्य भी मंगल के लिए निरन्तर कर्मशील लोक-जीवन की चरम और सामूहिक उपलब्धि है।
दूसरा वैशिष्टय है अनपेक्षित कथांश का परिहार और केवल मर्मभूत कथांश का मर्म-विन्यास। लोक-मानस का कुतूहल किस अंश तक सीमित है इसकी ठीक-ठीक परख रखते हुए लोक-साहित्य बराबर उन अंशों को छोड़ते हुए चलता है, जो अंश अपने आप गम्य हो सकते हैं और जिसके बीच में जोड़ देने से कथा के रस में व्याघात उपस्थित हो सकता है। उदाहरण के लिए हरिणी वाला प्रसिद्ध सोहर ही ले लीजिए-
उदाहरण के लिए सात भाई के बीच में एक बहन का होना, प्रियतम के विदेश जाने पर बारह वर्ष तक एकतान प्रतीक्षा करना, ननद-भौजाई और सास-बहू के बीच विरसता की कल्पना, भाई-बहन के निश्छल स्नेह की रचना, पुत्र का पुत्री से अधिक महत्त्व होना और खरी बात कहने वाले को पहले दुःख भोगाकर समाज में विजयी बनाना-ये भारतीय लोक-साहित्य के ऐसे अभिमत तथ्य हैं कि जिन्हें सामाजिक अवस्था की परिणति ही कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तीन की संख्या का महत्त्व अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, अपनी खुशी में जड़-चेतन सबको साझीदारी बनाने का उत्साह, और अपने दुख में प्रकृति को सहानुभूतिमय देखने की शक्ति-ये अभिप्राय भी ऐसे मर्मभूत सत्य के रूप में लोक-साहित्य गृहीत हुए हैं कि इनमें एक-एक-एक बात छिड़े बिना नहीं रहती। लोक, कथानकों में इन आध्यात्मिक अभिप्रायों की पुनरावृत्ति सबसे अधिक मिलती है, पुनरावृत्ति की परम्परा का स्रोत आरण्यकों और उपनिषदों में ढूँढ़ा जा सकता है। सत्य जिस रूप में समाज से परिचित होता है, उसी रूप में वह सत्य असन्दिग्ध रूप में समझा जा सकता है। दूसरे रूप में उसकी अन्यथा प्रतीत की अंशका रहती है।
इसलिए सत्य की अनुसन्धित्सा जहाँ मुख्य प्रतीति हो वहाँ सत्य को दस रंगों में रंगने की कोशिश करना उदेश्य में बाधक हो सकता है। बात कुछ अटपटी लगेगी पर उपनिषद् और लोक-साहित्य का स्वर इस माने में एक है कि समाज सत्य की उपलब्धि के लिए दोनों में समान रूप से बैचैनी है। उपनिषद् भी एक व्यक्ति की रचना नहीं, वरन् नाना प्रकार के विचारकों के चिन्तन और मनन में सहभागी, सहज-जीवन बिताने वाले समाज के द्वारा सत्य का साक्षात्कार है और लोक-साहित्य भी मंगल के लिए निरन्तर कर्मशील लोक-जीवन की चरम और सामूहिक उपलब्धि है।
दूसरा वैशिष्टय है अनपेक्षित कथांश का परिहार और केवल मर्मभूत कथांश का मर्म-विन्यास। लोक-मानस का कुतूहल किस अंश तक सीमित है इसकी ठीक-ठीक परख रखते हुए लोक-साहित्य बराबर उन अंशों को छोड़ते हुए चलता है, जो अंश अपने आप गम्य हो सकते हैं और जिसके बीच में जोड़ देने से कथा के रस में व्याघात उपस्थित हो सकता है। उदाहरण के लिए हरिणी वाला प्रसिद्ध सोहर ही ले लीजिए-
छापक पेड़ छिउलिया त पतवन धनवन हो
तेहि तर ठाढ़ हिरिनिया त मन अति अनमन हो।।
चरतहिं चरत हरिनवा त हरिनी से पूछेले हो
हरिनी ! की तोर चरहा झुरान कि पानी बिनु मुरझेलु हो।।
नाहीं मोर चरहा झुरान ना पानी बिनु मुरझींले हो
हरिना ! आजु राजा के छठिहार तोहे मारि डरिहें हो।।
मचियहिं बइठल कोसिला रानी, हरिनी अरज करे हो
रानी ! मसुआ त सींझेला रसोइया खलरिया हमें दिहितू नू हो।।
पेड़वा से टाँगबो खलरिया त मनवा समुझाइबि हो
रानी ! हिरी-फिरी देखबि खलरिया जनुक हरिना जियतहिं हो
जाहु हरिनी घर अपना, खलरिया ना देइब हो
हरिनी ! खलरी के खँजड़ी मढ़ाइबि राम मोरा खेलिहेनू हो।।
जब-जब बाजेला खँजड़िया सबद सुनि अहँकेली हो
हरिनी ठाढि ढेकुलिया के नीचे हरिन के बिजूरेली हो।।
तेहि तर ठाढ़ हिरिनिया त मन अति अनमन हो।।
चरतहिं चरत हरिनवा त हरिनी से पूछेले हो
हरिनी ! की तोर चरहा झुरान कि पानी बिनु मुरझेलु हो।।
नाहीं मोर चरहा झुरान ना पानी बिनु मुरझींले हो
हरिना ! आजु राजा के छठिहार तोहे मारि डरिहें हो।।
मचियहिं बइठल कोसिला रानी, हरिनी अरज करे हो
रानी ! मसुआ त सींझेला रसोइया खलरिया हमें दिहितू नू हो।।
पेड़वा से टाँगबो खलरिया त मनवा समुझाइबि हो
रानी ! हिरी-फिरी देखबि खलरिया जनुक हरिना जियतहिं हो
जाहु हरिनी घर अपना, खलरिया ना देइब हो
हरिनी ! खलरी के खँजड़ी मढ़ाइबि राम मोरा खेलिहेनू हो।।
जब-जब बाजेला खँजड़िया सबद सुनि अहँकेली हो
हरिनी ठाढि ढेकुलिया के नीचे हरिन के बिजूरेली हो।।
वातावरण का चित्र है। हरिणी से हरिण एक प्रश्न पूछता है, बस इतना काफ़ी है, फिर यह कहने की ज़रूरत नहीं कि हरिण उत्तर दे रहा है और उत्तर से ही यह बात गम्य हो गयी कि हरिण छट्ठी के लिए मार डाला गया और इस कथाक्रम में हरिण का मारना नहीं कहा गया है। फिर हरिणी और कौसल्या का संवाद है और कौसल्या के उत्तर से ही यह बात गम्य हो जाती है कि हरिणी को निराश होकर लौटना पड़ा इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चित्र का सबसे मर्मस्पर्शी रूप सामने रखना अधिक आवश्यक है और वह रखा गया है। लोक-कथाओं में यह वैशिष्ट्य और अधिक महत्त्व रखता है। जहाँ एक ओर एक साभिप्राय बात बराबर दुहरायी जाएगी, वहाँ अभिप्राय से बहिर्भूत बात एकदम छोड़कर कथानक आगे चल देंगे। लोक-साहित्य ऐसे परिहार्य अंशों के वर्णन के लोभ में नहीं फंसता उसके लिए वातावरण का चित्र केवल प्रतीक है।
उपन्यासों में जैसे लम्बे वर्णन हमें मिलते हैं और यह कहा जाता है कि यह वर्णन चरित्र-चित्रण और कथा-निर्वाह के लिए अत्यन्त आवश्यक है, वैसी बात यहाँ नहीं है। उपन्यास में क्रम उलट-पलट दिया जाता है या कथा में अधिक रस-प्रकर्ष आने पर ध्यान दिया जाता है, पर लोक-कथा में या लोक-गाथा में कथा को उत्कर्ष पर पहुँचाकर छोड़ दिया जाता है और अन्त में केवल एक भरतवाक्य जैसी चीज़ ज़रूर जोड़ दी जाती है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरैं; या नेकी नेक राह, बदी बद राह, या अन्याय परिशोधित हुए बिना नहीं रहेगा, या ये सारे दुःख भूल गये, बधाई बजने लगी। गीतों में मंगल की कामना अत्यन्त सूक्ष्मता से व्यक्त होती है। कभी-कभी मंगल की बात लय की लहक में ही आकर रह जाती है। अधिकांश सोहरों की अन्तिम पंक्ति के आते-आते दुःख, लगता है, उमड़-घुमड़कर छा गया है और इतने ही में लय ऐसे मोड़ खाती है कि सारी उमड़न-घुमड़न तितर-बितर हो जाती है।
उपन्यासों में जैसे लम्बे वर्णन हमें मिलते हैं और यह कहा जाता है कि यह वर्णन चरित्र-चित्रण और कथा-निर्वाह के लिए अत्यन्त आवश्यक है, वैसी बात यहाँ नहीं है। उपन्यास में क्रम उलट-पलट दिया जाता है या कथा में अधिक रस-प्रकर्ष आने पर ध्यान दिया जाता है, पर लोक-कथा में या लोक-गाथा में कथा को उत्कर्ष पर पहुँचाकर छोड़ दिया जाता है और अन्त में केवल एक भरतवाक्य जैसी चीज़ ज़रूर जोड़ दी जाती है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरैं; या नेकी नेक राह, बदी बद राह, या अन्याय परिशोधित हुए बिना नहीं रहेगा, या ये सारे दुःख भूल गये, बधाई बजने लगी। गीतों में मंगल की कामना अत्यन्त सूक्ष्मता से व्यक्त होती है। कभी-कभी मंगल की बात लय की लहक में ही आकर रह जाती है। अधिकांश सोहरों की अन्तिम पंक्ति के आते-आते दुःख, लगता है, उमड़-घुमड़कर छा गया है और इतने ही में लय ऐसे मोड़ खाती है कि सारी उमड़न-घुमड़न तितर-बितर हो जाती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book