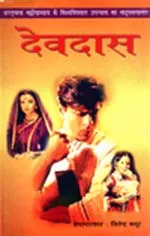|
नाटक-एकाँकी >> देवदास देवदासजितेन्द्र कपूर
|
442 पाठक हैं |
||||||
शरत् बाबू की अमर कृति ‘देवदास’ की कथा का नाट्यरूपान्तर........
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
शरत् बाबू की अमर कृति ‘देवदास’ की कथा में देवदास का
दर्द तो
मुखर था, सबने सुना और सबने देखा; किंतु पार्वती का क्या ? और चन्द्रमुखी
का क्या ? क्या उन्होंने कोई यातना नहीं भोगी ? क्या शरीर की कैद में उनकी
आत्मा किसी मौत से नहीं गुज़री ? वे दोनों भी अपने आँसुओं में उबलती रही
हैं; सिर्फ वे आँसूँ अन्तःस्रावी थे, शरत् बाबू की मनोभूमि पर न गिर पाये।
युगों की बर्फ़ तले दबे पार्वती और चन्द्रमुखी के
‘हिमालयी’
व्यक्तित्व को उजागर किया गया है प्रस्तुत कृत
‘देवदास’ में।
नाटक में दो अंक हैं जो परस्पर सन्नद्ध होते हुए भी स्वाश्रयी हैं यानी
उन्हें अलग-अलग एकांकियों के रूप में अभी अभिनीत किया जा सकता है। कामयाब
नाट्यरचयिता और नाट्यनिर्देशक श्री जितेन्द्र कपूर का यह प्रयास सामाजिक
जनों को रुचिकर एवं उपादेय लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
कुछ मन की....
दीर्घ काल से मेरी एक प्रबल इच्छा रही है कि शरत् चन्द्र का काम रंगमंच पर
प्रस्तुत हो।
मानव-मन की गहराइयों में उतर कर अन्दर सोए एक सम्पूर्णतः अपरिचित, अनचीन्हे व्यक्तित्व को जागरित करने, उसे उजागर करने की शरत् बाबू में अपूर्व क्षमता। यही कारण है कि उनके भोले-भाले, अनपढ़ ग्रामीण पात्र भी जब परिस्थितियों के भँवर में पड़ते हैं, तब वे डूब नहीं जाते अपितु अतल की गहराइयों को छूकर उसमें से वह अमृत-कलश ढूँढ़कर लाते हैं जिसकी एक बूंद भी यदि पाठक की आत्मा को छू ले तो उसी क्षण वह सम्पूर्ण क्षुद्रता, समस्त कलुष से मुक्त हो जाता है। यह विशेषता उनकी कृतियों के लगभग सब मुख्य पात्रों में है, किन्तु उनके नारी-पात्र तो इस धरती पर रहते हुए भी, इसकी मिट्टी से बने होने के उपरान्त भी धरती से कहीं ऊपर उठकर आकाश के नक्षत्र बन जाते हैं।
शरत् के कथानकों में पाई जानेवाली स्थितियाँ, उनके द्वान्द्वात्मक घर्षण तथा उनका अद्भूत चरित्र-चित्रण भी उन्हें नाटक की परिधि की ओर बार-बार आकर्षित करता है। किन्तु हाँ, नाटक एक तकनीकी कला है और किसी भी कृति को उसके साँचे में ढालने के लिए उसके तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है।
मैंने यह प्रयास किया है। आज के रंगमंच की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा है और विश्वास है कि आज के नाट्यकर्मी को उपलब्ध चाक्षुष और श्रव्य उपादनों की सहायता से इन नाटकों को भली प्रकार से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहें उन प्रस्तुतियों में थोड़ी-बहुत तकनीकी चुनौतियों का सामना भले ही करना पड़े।
रूपान्तरण के लिए मैंने शरत् बाबू के उपन्यास ‘देवदास’ को चुना है।
‘देवदास’ के चयन का प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रायः कथानक का केन्द्र-बिन्दु देवदास को ही माना जाता है और उपन्यास में पाठक की दृष्टि भी सदा देवदास पर ही ‘फोकस’ रही है। उपन्यास के फिल्मी संस्करणों में भी ‘लाइमलाइट’ देवदास ही केन्द्रित रही है। स्वयं शरत् चन्द्र उपन्यास का समापन करते हुए कहते हैं :
‘....अब, इतने दिनों में पार्वती का क्या हाल हुआ
कैसी है वह, नहीं जानता। खोज-पूछ को जी नहीं चाहा, सिर्फ़ देवदास के लिए बड़ा अफसोस होता है।..कभी, अगर देवदास जैसे बदनसीब, असंयमी और पापी से परिचय हो तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि और चाहे जो भी हो उसके जैसी मौत किसी की न हो..मरते वक्त वह किसी की आँखों में आँसू की एक बूँद देखकर मर सके।’
शायद देवदास से शरत् बाबू का तादात्म्य इस कारण भी विशेष रहा हो क्योंकि कहीं दूर-पार वह उनका स्वयं का प्रतिबिम्ब रहा हो और उसकी नियति में वे अपनी नियति देख रहे हों।
किन्तु, पार्वती का क्या ? और चन्द्रमुखी का क्या ? उन्होंने कोई यातना नहीं भोगी ? क्या शरीर में कैद उनकी आत्मा किसी मौत से नहीं गुज़री ?
देवदास का दर्द मुखर था, सबने सुना और सबने देखा, पर पारो और चन्द्रमुखी भी अपने आँसुओं में उबलती रही हैं; सिर्फ़ वे आँसू अन्तःस्रावी थे, शरत् चन्द्र की मनोभूमि पर न गिर पाए।
मुझे लगता है कि पारो और चन्द्रमुखी उपन्यास के कथानक में दो धुव हैं जिनके बीच देवदास दिशाहीन आँधी की तरह भटकता रहता है—खुद भी बिखरता है औरों को भी बिखराता है, किन्तु पारो और चन्द्रमुखी ? उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को उन्होंने हर स्थिति में निभाया है—शरत् के नारी-पात्र !
युगों की बर्फ़ के नीचे दबा पार्वती और चन्द्रमुखी का, ‘हिमालयी’ व्यक्तित्व कहीं मन को छू गया। मुझे लगा कि एक काम अधूरा रह गया जिसे मुझे पूरा करना है। इसलिए मैंने ‘देवदास’ पर कलम चलाने की धृष्टता की। नाटक को दो अंकों में बाँटा—‘पारो’ और ‘चन्द्रमुखी’। अंक परस्पर सन्नद्ध होते हुए भी स्वाश्रयी हैं और उन्हें अलग-अलग स्वतन्त्र एकांकियों के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
कथानक वही है, पात्र वे ही हैं, स्थितियाँ वे ही हैं। संवाद भी लगभग उपन्यास से ही लिये गए हैं। अपनी ओर से केवल उतना ही जोड़ा गया है जो नाटक के तारतम्य के वास्ते आवश्यक है।
नाटक का दृश्य-विधान विषम है। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं उसे एक या दो दृश्य-भूमियों पर न लगा सका, फिर भी चेष्टा रही है कि उसे सरलतम बनाया जाए। मेरे विचार से मंच-सज्जा करके भी काम चलाया जा सकता है। वैसे आज का ‘मंच’ इतना पंगु भी नहीं रहा। सलाइडों के प्रयोग, फ़िल्म-स्ट्रिप्स तथा कंप्यूटर इमेजिंग की सहायता से डिजिटल सीनोग्राफ़ी ने इसे अपूर्व सम्भावनाएँ प्रदान कर दी हैं। अब यह नाटक के निर्देशक एवं मंच-सज्जा सहायक पर निर्भर करता है कि वे कैसे समस्या से जूझते हैं। अपने लम्बे मंचीय आधार पर मैं कह सकता हूँ कि काम कठिन अवश्य है, पर असम्भाव्य नहीं। हो सकता है कि कोई सृजनशील निर्देशक अपनी उर्वर कल्पना द्वारा इसे चुटकियों में सुलझा ले।
इन शब्दों के साथ मेरा काम समाप्त होता है और रंगकर्मियों का शुरू। वे इस नाटक को उठाएँ, मंचित करें और सामाजिक-जन को ‘शरत् चन्द्र’ का चक्षुष अनुभव प्रदान करें।
मानव-मन की गहराइयों में उतर कर अन्दर सोए एक सम्पूर्णतः अपरिचित, अनचीन्हे व्यक्तित्व को जागरित करने, उसे उजागर करने की शरत् बाबू में अपूर्व क्षमता। यही कारण है कि उनके भोले-भाले, अनपढ़ ग्रामीण पात्र भी जब परिस्थितियों के भँवर में पड़ते हैं, तब वे डूब नहीं जाते अपितु अतल की गहराइयों को छूकर उसमें से वह अमृत-कलश ढूँढ़कर लाते हैं जिसकी एक बूंद भी यदि पाठक की आत्मा को छू ले तो उसी क्षण वह सम्पूर्ण क्षुद्रता, समस्त कलुष से मुक्त हो जाता है। यह विशेषता उनकी कृतियों के लगभग सब मुख्य पात्रों में है, किन्तु उनके नारी-पात्र तो इस धरती पर रहते हुए भी, इसकी मिट्टी से बने होने के उपरान्त भी धरती से कहीं ऊपर उठकर आकाश के नक्षत्र बन जाते हैं।
शरत् के कथानकों में पाई जानेवाली स्थितियाँ, उनके द्वान्द्वात्मक घर्षण तथा उनका अद्भूत चरित्र-चित्रण भी उन्हें नाटक की परिधि की ओर बार-बार आकर्षित करता है। किन्तु हाँ, नाटक एक तकनीकी कला है और किसी भी कृति को उसके साँचे में ढालने के लिए उसके तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है।
मैंने यह प्रयास किया है। आज के रंगमंच की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा है और विश्वास है कि आज के नाट्यकर्मी को उपलब्ध चाक्षुष और श्रव्य उपादनों की सहायता से इन नाटकों को भली प्रकार से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहें उन प्रस्तुतियों में थोड़ी-बहुत तकनीकी चुनौतियों का सामना भले ही करना पड़े।
रूपान्तरण के लिए मैंने शरत् बाबू के उपन्यास ‘देवदास’ को चुना है।
‘देवदास’ के चयन का प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रायः कथानक का केन्द्र-बिन्दु देवदास को ही माना जाता है और उपन्यास में पाठक की दृष्टि भी सदा देवदास पर ही ‘फोकस’ रही है। उपन्यास के फिल्मी संस्करणों में भी ‘लाइमलाइट’ देवदास ही केन्द्रित रही है। स्वयं शरत् चन्द्र उपन्यास का समापन करते हुए कहते हैं :
‘....अब, इतने दिनों में पार्वती का क्या हाल हुआ
कैसी है वह, नहीं जानता। खोज-पूछ को जी नहीं चाहा, सिर्फ़ देवदास के लिए बड़ा अफसोस होता है।..कभी, अगर देवदास जैसे बदनसीब, असंयमी और पापी से परिचय हो तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि और चाहे जो भी हो उसके जैसी मौत किसी की न हो..मरते वक्त वह किसी की आँखों में आँसू की एक बूँद देखकर मर सके।’
शायद देवदास से शरत् बाबू का तादात्म्य इस कारण भी विशेष रहा हो क्योंकि कहीं दूर-पार वह उनका स्वयं का प्रतिबिम्ब रहा हो और उसकी नियति में वे अपनी नियति देख रहे हों।
किन्तु, पार्वती का क्या ? और चन्द्रमुखी का क्या ? उन्होंने कोई यातना नहीं भोगी ? क्या शरीर में कैद उनकी आत्मा किसी मौत से नहीं गुज़री ?
देवदास का दर्द मुखर था, सबने सुना और सबने देखा, पर पारो और चन्द्रमुखी भी अपने आँसुओं में उबलती रही हैं; सिर्फ़ वे आँसू अन्तःस्रावी थे, शरत् चन्द्र की मनोभूमि पर न गिर पाए।
मुझे लगता है कि पारो और चन्द्रमुखी उपन्यास के कथानक में दो धुव हैं जिनके बीच देवदास दिशाहीन आँधी की तरह भटकता रहता है—खुद भी बिखरता है औरों को भी बिखराता है, किन्तु पारो और चन्द्रमुखी ? उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को उन्होंने हर स्थिति में निभाया है—शरत् के नारी-पात्र !
युगों की बर्फ़ के नीचे दबा पार्वती और चन्द्रमुखी का, ‘हिमालयी’ व्यक्तित्व कहीं मन को छू गया। मुझे लगा कि एक काम अधूरा रह गया जिसे मुझे पूरा करना है। इसलिए मैंने ‘देवदास’ पर कलम चलाने की धृष्टता की। नाटक को दो अंकों में बाँटा—‘पारो’ और ‘चन्द्रमुखी’। अंक परस्पर सन्नद्ध होते हुए भी स्वाश्रयी हैं और उन्हें अलग-अलग स्वतन्त्र एकांकियों के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
कथानक वही है, पात्र वे ही हैं, स्थितियाँ वे ही हैं। संवाद भी लगभग उपन्यास से ही लिये गए हैं। अपनी ओर से केवल उतना ही जोड़ा गया है जो नाटक के तारतम्य के वास्ते आवश्यक है।
नाटक का दृश्य-विधान विषम है। लाख प्रयत्न करने पर भी मैं उसे एक या दो दृश्य-भूमियों पर न लगा सका, फिर भी चेष्टा रही है कि उसे सरलतम बनाया जाए। मेरे विचार से मंच-सज्जा करके भी काम चलाया जा सकता है। वैसे आज का ‘मंच’ इतना पंगु भी नहीं रहा। सलाइडों के प्रयोग, फ़िल्म-स्ट्रिप्स तथा कंप्यूटर इमेजिंग की सहायता से डिजिटल सीनोग्राफ़ी ने इसे अपूर्व सम्भावनाएँ प्रदान कर दी हैं। अब यह नाटक के निर्देशक एवं मंच-सज्जा सहायक पर निर्भर करता है कि वे कैसे समस्या से जूझते हैं। अपने लम्बे मंचीय आधार पर मैं कह सकता हूँ कि काम कठिन अवश्य है, पर असम्भाव्य नहीं। हो सकता है कि कोई सृजनशील निर्देशक अपनी उर्वर कल्पना द्वारा इसे चुटकियों में सुलझा ले।
इन शब्दों के साथ मेरा काम समाप्त होता है और रंगकर्मियों का शुरू। वे इस नाटक को उठाएँ, मंचित करें और सामाजिक-जन को ‘शरत् चन्द्र’ का चक्षुष अनुभव प्रदान करें।
-जितेन्द्र कपूर
पात्र परिचय
बालिका पारो
: आयु लगभग बारह वर्ष, युवा
पारो : आयु लगभग
सोलह वर्ष
किशोर देवदास : आयु लगभग सोलह वर्ष, युवा देवदास : आयु लगभग बीस वर्ष
नीलकण्ठ चक्रवर्ती : पारो का पिता
अन्नपूर्णा देवी : पारो की माँ
नारायण मुखर्जी : देवदास का पिता, तालसोनापुर के ज़मींदार
हरिमति देवी : देवदास की माँ
मनोरमा : पारो की अन्तरंग सखी
भुवन चौधुरी : पारो के पति, हाथीपोता गाँव के ज़मींदार, आयु लगभग चालीस वर्ष
महेन्द्र : भुवन चौधुरी का युवा पुत्र
यशोदा : महेन्द्र की विवाहित छोटी बहन
धर्मदास : देवदास के परिवार का अधेड़ आयु का एक विश्वस्त अनुचर
निताई : देवदास के परिवार का एक अन्य अनुचर
रामचरन : पारो की श्वसुराल में एक किशोर अनुचर
एक देहाती : भुवन चौधुरी की ज़मींदारी में एक ग्रामीण
तीन वैष्णवियाँ : पद गाकर भिक्षा माँगने वाली तीन लोक-नायिकाएँ
किशोर देवदास : आयु लगभग सोलह वर्ष, युवा देवदास : आयु लगभग बीस वर्ष
नीलकण्ठ चक्रवर्ती : पारो का पिता
अन्नपूर्णा देवी : पारो की माँ
नारायण मुखर्जी : देवदास का पिता, तालसोनापुर के ज़मींदार
हरिमति देवी : देवदास की माँ
मनोरमा : पारो की अन्तरंग सखी
भुवन चौधुरी : पारो के पति, हाथीपोता गाँव के ज़मींदार, आयु लगभग चालीस वर्ष
महेन्द्र : भुवन चौधुरी का युवा पुत्र
यशोदा : महेन्द्र की विवाहित छोटी बहन
धर्मदास : देवदास के परिवार का अधेड़ आयु का एक विश्वस्त अनुचर
निताई : देवदास के परिवार का एक अन्य अनुचर
रामचरन : पारो की श्वसुराल में एक किशोर अनुचर
एक देहाती : भुवन चौधुरी की ज़मींदारी में एक ग्रामीण
तीन वैष्णवियाँ : पद गाकर भिक्षा माँगने वाली तीन लोक-नायिकाएँ
देवदास
यवनिका उठ रही है। वातावरण में बाँसुरी का कोमल आलाप गूँज रहा है।
सज्जाविहीन रंगमंच केवल काली ड्रेपरी से आच्छादित है। मंच के पृष्ठभाग में
साइक्लोरमा भी काले पर्दे से ढका हुआ है। मंच के बीचों-बीच पारो पत्थर की
प्रतिमा बनी निस्पंद खड़ी ऊपर शून्य में ताक रही है। पीले प्रकाश के एक
संकुचित वृत्त ने उसे आवृत्त कर रखा है। शेष मंच पर पूर्ण अन्धकार है।
बाँसुरी के स्वरों के अतिरिक्त वातावरण बिलकुल निश्शब्द है। यवनिका पूरी
तरह उठ जाने पर बाँसुरी मौन हो जाती है और नेपथ्य से नारी-स्वर में
माक्रोफोन पर आमुख आरम्भ होता है।
आमुख : मैं पारो हूँ !
आकाश की दूरियों में भटकता एक ऐसा धूमकेतु जिसकी नियति में जलकर मिट जाना भी नहीं। जीवन की तपती बालू पर चलते-चलते मेरे पैर संज्ञाशून्य हो गए हैं किन्तु राह का कोई अन्त दिखाई नहीं देता।
नारीत्व की गरिमा तले कहीं बहुत नीचे मेरा एहसास दब गया है।
मैं कैसे याद करूँ कि मेरा एक मन है, जो न स्त्री है, न पुरुष—वह केवल मन है !!
उस मन ने जिसे चाहा उसे भटकन की उन लहरों में ऊबता-डूबता छोड़कर आना पड़ा जो किसी तट को नहीं छूतीं।
आमुख : मैं पारो हूँ !
आकाश की दूरियों में भटकता एक ऐसा धूमकेतु जिसकी नियति में जलकर मिट जाना भी नहीं। जीवन की तपती बालू पर चलते-चलते मेरे पैर संज्ञाशून्य हो गए हैं किन्तु राह का कोई अन्त दिखाई नहीं देता।
नारीत्व की गरिमा तले कहीं बहुत नीचे मेरा एहसास दब गया है।
मैं कैसे याद करूँ कि मेरा एक मन है, जो न स्त्री है, न पुरुष—वह केवल मन है !!
उस मन ने जिसे चाहा उसे भटकन की उन लहरों में ऊबता-डूबता छोड़कर आना पड़ा जो किसी तट को नहीं छूतीं।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book