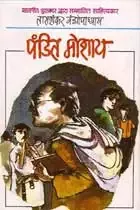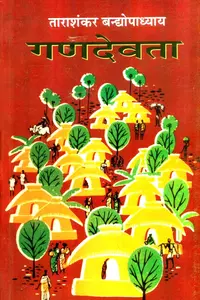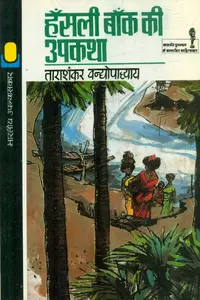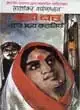|
कहानी संग्रह >> पंडित मोशाय पंडित मोशायताराशंकर वन्द्योपाध्याय
|
32 पाठक हैं |
||||||
इस संग्रह में ताराशंकर की सर्वकालिक कहानियां सम्मिलित हैं...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
साहित्य में लेखकों के दो प्रकार के वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में ऐसे
लेखक होते हैं जो आते ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाते हैं। बांग्ला
साहित्य में विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय ऐसे उदाहरण हैं। उनका पहला उपन्यास
‘पथेर पांचाली’ ही उनके जीवन का श्रेष्ठ उपन्यास
साबित हुआ।
बाद में उन्होंने ढेरों उच्चकोटि की कहानियां, उपन्यास आदि लिखे लेकिन
शायद अपनी बाद की लिखी हुई किसी भी कृति को अपनी सर्वप्रथम कृति से ज्यादा
महत्त्वपूर्ण नहीं बना पाये।
दूसरे वर्ग के लेखकों की शुरुआती रचनाएं सामान्य ही होती है। उनकी प्रतिभा को लोगों की नजरों में आने के लिए दीर्घकालीन कठोर साधना ही जरूरत पड़ती है। ताराशंकर इसी वर्ग के लेखक थे। उनकी पहले दौर की लिखी काफी रचनाएं औरत दर्जे की हैं। लंबे समय तक काफी कुछ देखने परखने के बाद, व्यर्थता की काफी ग्लानि और निराशा पार करके उन्होंने अपने लेखन की धाक जमायी थी। अपराजित आत्मविश्वास और ईश्वर भर्तिं ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया।
अपनी अभिव्यक्ति के उचित माध्यम की तलाश में भी उन्हें कम भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने पहले कविताएं लिखीं, फिर नाटक और सबसे अंत में कथा साहित्य लिखा। कहानियां और उपन्यास ही ताराशंकर को अपनी बात कहने के उपयुक्त माध्यम नजर आये।
ताराशंकर का साहित्यिक जीवन आठ वर्ष की उम्र में कविताओं से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत उन्होंने नाट्य लेखन में रुचि दिखायी। उनकी नियमित साहित्य साधना 28 वर्ष की उम्र में लामपुर से प्रकाशित पूर्णमा मासिक पत्रिका से शुरु हुई। कविता, कहानी आलोचना, सम्पादकीय के रूप में इस पत्रिका की ज्यादातर सामग्री उन्हीं की लिखी हुई होती थी। पूर्णिमा में ही ताराशंकर की पहली उल्लेखनीय कहानी ‘प्रवाह का तिनका’ प्रकाशित हुई थी।
कुछ दिन बाद ही ताराशंकर ने ‘रसकली’ नामक कहानी लिखी और ‘प्रवासी’ पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेज दी। कई महीनों तक बार बार –बार पत्र लिखने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार ताराशंकर खुद ‘प्रवासी’ ऑफिस में उपस्थिति हुए। जैसा अमूमन होता है, नये लेखक की रचना बिना पढ़े ही सम्पादकीय विभाग ने वापस लौटा दी। उस अस्वीकृत रचना को लेकर ताराशंकर पैदल ही मध्य कलकत्ता से दक्षिण कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे। उस दिन उनकी आंखें कई बार भर आई थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि साहित्य साधना की इच्छा को तिलांजलि देकर गंगा नहाकर घर लौट जायें एवं शांत गृहस्थ की तरह अपना जीवन खेती-खलिहानी करते हुए गुजार दें।
साहित्य क्षेत्र में अपने पराजय की बात सोचकर उनका चित्त व्यथित होने लगता था। सौभाग्य से एक दिन डाकघर में उन्हें एक पत्रिका नजर आ गई। उस पत्रिका का नाम था ‘कल्लोल।’ ताराशंकर ने ‘कल्लोल’ का पता नोट कर लिया और उसी पते पर उन्होंने रसकली कहानी भेज दी। जल्दी ही उन्हें कहानी के स्वीकृत होने की सूचना मिली। उत्साहित करने वाले पवित्र गंगोपाध्याय ने लिखा, आप इतने दिनों तक मौन क्यों बैठे हुए थे ? महानगरी के साहित्य क्षेत्र में ताराशंकर की वह पहली स्वीकृति थी।
विचारों का साम्य न होने पर भी नये लेखकों के लिए ‘कल्लोल’ का द्वार हमेशा खुला रहता था। आगे के दो वर्षों तक कल्लोल में ताराशंकर की कई कहानियां प्रकाशित हुईं। फिर ‘कालि कलम; ‘उपासना’ और ‘उत्तरा’ पत्रिकाओं में भी उन्होंने लिखा। श्मशान के पथ पर नामक कहानी ‘उपासना’ पत्रिका में छपी थी।
ताराशंकर ने लिखा है कि उनके साहित्य-जीवन का पहला अध्याय अवहेलना और अवज्ञा का काल था। उनकी पुत्री का देहान्त आठ वर्ष की उर्म में हो गया। कन्या वियोग से शोकाकुल कथाशिल्पी ने इस बार ‘संध्यामणि’ कहानी लिखी। सजनीकान्त द्वारा संपादित ‘बंगश्री’ पत्रिका के पहले अंक में यह कहानी ‘श्मशान घाट’ नाम से छपी थी। ‘संध्यामणि’ के पहले ताराशंकर अठारह उन्नीस कहानियां लिख चुके थे, जिनमें रसकली राईकलम और मालाचंदन जैसी कहानियां भी थीं। लेकिन संध्यामणि ऐसी पहली कहानी थी जिसे बांग्ला साहित्य में सिर्फ ताराशंकर ही लिख सकते थे।
‘संध्यामणि’ छपने के बाद अंतरंग साहित्यकारों के बीच इसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद ‘भारतवर्ष’ में छपी ‘डाईनीर बांशी’ (डाईन की बांसुरी) और ‘बंगश्री’ में प्रकाशित दूसरी कहानी मेला ने ताराशंकर को कथाकारों की पहली पंक्ति में ला बिठाया।
ताराशंकर ने अपनी साहित्य जीवन की बातों में जिस अपमान की घटना का जिक्र किया है। वह ‘देश’ पत्रिका के दफ्तर में घटा था। यह सन् 1934 की बात है। उसके पहले ‘देश’ के शारदीय विशेषांक में उनकी बहुचर्चित कहानी ‘नारी और नागिनी’ छप चुकी थी। देश के प्रभात गांगुली ने ‘नारी और नागिनी’ की बेहद प्रशंसा की थी। गांगुली महाशय बड़े मूड़ी आदमी थी। मिजाज ठीक रहता तो बेहद दिलदरिया थे और अगर मिजाज बिगड़ता तो चीखते-चिल्लाते हुए इस तरह इन्कार करते थे कि लेखक को बहुत अपमानजनक लगता। ताराशंकर की ‘मुसाफिरखाना’ जैसी कहानी उन्हें पसंद नहीं आयी। वे उसे लौटाते हुए बोले, यह (अर्थात् देश पत्रिका) कोई डस्टबिन नहीं है।
ताराशंकर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गयी थी कि कोई उन्हें खारिज नहीं कर सकता था। यदा कदा आलोचना करते हुए कोई कहता, ‘कहानियां अच्छी लिखते हैं, शैली भी अच्छी होती है। लेकिन कहानियां, बड़ी स्थूल होती हैं। उनमें सूक्ष्मता का अभाव है। जिज्ञासु ताराशंकर ने इस पर कविगुरु रवीन्द्रनाथ की राय जाननी चाही। उत्तर में रवीन्द्रनाथ ने लिखा, ‘तुम्हारी रचनाओं को स्थूल दृष्टि कहकर जिसने बदनाम किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तु्म्हारी रचनाओं में बड़ा सूक्ष्म स्पर्श होता है और तुम्हारी कलम से वास्तविकता सच बनकर नजर आती है, जिसमें यथार्थ को कोई नुकसान नहीं पहुचंता। कहानी लिखते वक्त कहानी न लिखने को ही जो लोग बहादुरी समझते हैं तुम ऐसे लोगों के दल में शामिल नहीं हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। रचना में यथार्थ की रक्षा करना ही सबसे कठिन होता है।’
यथार्थ लेखन के इस दुरुह मार्गपर ताराशंकर की जययात्रा बिना किसी रोक टोक के निरंतर आगे बढ़ती ही गयी।
ताराशंकर के रचनाकार के केन्द्रीय वृत्तभूमि में देहात का ब्राह्मण समाज था। लेकिन उनके जीवन बोध ने धीरे-धीरे फैलते हुए सामान्यजन को अपने दायरे में ले लिया। रवीन्द्रनाथ ने सबसे पहले अपनी कहानियों में गांव देहात के क्षुद्र मनुष्य को स्थान दिया था। लघु प्राण मामूली कथा छोटी छोटी दुख की बातें, जो बेहद सहज और सरल हैं। जिनका जीवन है, उन्हीं को लेकर कविगुरु ने अपनी छोटी कहानियों की मंजूषा सजाकर बांग्ला साहित्य में कहानियों की प्राण प्रतिष्ठा की। शरत् साहित्य में मुख्यतः देहातों के मध्यवित्त समाज को ही प्राथमिकता दी गयी है। ताराशंकर ने समाज के दीन हीन अछूत स्तर के लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनाकर अपने रचनालोक को पूर्णता प्रदान की। इस दृष्टि से ताराशंकर सम्पूर्ण समाज के जीवन बोध के सर्वप्रथम कलाकार हैं।
उनकी कहानियों में अपने समय का परिवेश उजागर हुआ है। माटी से बने मानव जीवन को ही उन्होंने आविष्कृत किया। इसी दृष्टि से उनके साहित्य को आंचलिक कहा जाता है। अंचल विशेष की प्रकृति और उसी के प्रभाव से नियंत्रित मनुष्य के सुख-दुख की यथार्थता को कहानियों को चिचित्र करने से जाहिर है उनमें आंचलिक विशेषताएं नजर आयेंगी ही। इस दृष्टि से यथार्थ जीवन पर जो भी लिखा जाए वही आंचलिक हो जाता है। लेकिन अपने समय और परिवेश की विशेषताओं को ग्रहण करके जो साहित्य चिरंतन मानव सत्य को उजागर करता है उस साहित्य को आंचलिक कहकर उसे संकीण बनाना उचित नहीं होगा। ताराशंकर के साहित्य का व्यक्ति अपनी आदिम प्रवृत्ति, युगों से संचित संस्कार और वंशानुगत आजीविका ढोने वाला परिचित इन्सान है। इसीलिए ताराशंकर बंगला के सार्वभौमिक जीवन -शिल्पी हैं।
‘पंडित मोशाय कहानी- संग्रह में ताराशंकर की सर्वकालिक कहानियां सम्मिलित की गई हैं। ‘डाक हरकारा’ ‘मंथर विष,’ ‘रंगीन चश्मा,’ ‘पंडित मोशाय’ ‘प्रतिध्वनि’, चंडी राय का संन्यास’, ‘इस्कापन’, ‘प्रतीक्षा,’ ‘रायबाड़ी’ और ‘मुकुंद की मजलिस’ सभी कहानियां अपने समय की बहुपठित एवं बहुप्रशंसित कहानियों में से रही हैं।
ताराशंकर जीवन से गहरे रूप से जुड़े हुए कथाकार थे। बंगाल के ग्राम्य जीवन की सच्ची तस्वीर उनकी रचनाओं में दिखायी देती है। आप ताराशंकर की कोई भी कहानी बस एक बार पढ़ने बैठ जायें। वह में शीघ्र ही आपको अपने सम्मोहन में बांध लेगी। ताराशंकर की कहानियां उबाऊ नहीं होती। आखिर से अंत में अंत तक मानो उनमें एक रस धार सी बहती रहती है। अत्यंज और अछूत निम्नवर्ग के लोगों के प्रति अभिजात भद्र समाज के पाशविक उत्पीड़न के वीभत्स चेहरे पर पड़ी नकाब को ताराशंकर ने अपनी कहानियों में बखूबी हटाया है। खुद अभिजात कुल के जमींदार संतान होते हुए भी ताराशंकर सहानुभूति और करुणा के संवाहक बनकर पीड़ित लोगों के जीवन में अपनी भागीदारी करना चाहते थे। बात और व्यवहार में धरतीपुत्रों के साथ धीरे-धीरे उनका आत्मिक संबंध बन गया था।
दूसरे वर्ग के लेखकों की शुरुआती रचनाएं सामान्य ही होती है। उनकी प्रतिभा को लोगों की नजरों में आने के लिए दीर्घकालीन कठोर साधना ही जरूरत पड़ती है। ताराशंकर इसी वर्ग के लेखक थे। उनकी पहले दौर की लिखी काफी रचनाएं औरत दर्जे की हैं। लंबे समय तक काफी कुछ देखने परखने के बाद, व्यर्थता की काफी ग्लानि और निराशा पार करके उन्होंने अपने लेखन की धाक जमायी थी। अपराजित आत्मविश्वास और ईश्वर भर्तिं ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया।
अपनी अभिव्यक्ति के उचित माध्यम की तलाश में भी उन्हें कम भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने पहले कविताएं लिखीं, फिर नाटक और सबसे अंत में कथा साहित्य लिखा। कहानियां और उपन्यास ही ताराशंकर को अपनी बात कहने के उपयुक्त माध्यम नजर आये।
ताराशंकर का साहित्यिक जीवन आठ वर्ष की उम्र में कविताओं से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत उन्होंने नाट्य लेखन में रुचि दिखायी। उनकी नियमित साहित्य साधना 28 वर्ष की उम्र में लामपुर से प्रकाशित पूर्णमा मासिक पत्रिका से शुरु हुई। कविता, कहानी आलोचना, सम्पादकीय के रूप में इस पत्रिका की ज्यादातर सामग्री उन्हीं की लिखी हुई होती थी। पूर्णिमा में ही ताराशंकर की पहली उल्लेखनीय कहानी ‘प्रवाह का तिनका’ प्रकाशित हुई थी।
कुछ दिन बाद ही ताराशंकर ने ‘रसकली’ नामक कहानी लिखी और ‘प्रवासी’ पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेज दी। कई महीनों तक बार बार –बार पत्र लिखने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार ताराशंकर खुद ‘प्रवासी’ ऑफिस में उपस्थिति हुए। जैसा अमूमन होता है, नये लेखक की रचना बिना पढ़े ही सम्पादकीय विभाग ने वापस लौटा दी। उस अस्वीकृत रचना को लेकर ताराशंकर पैदल ही मध्य कलकत्ता से दक्षिण कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे। उस दिन उनकी आंखें कई बार भर आई थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि साहित्य साधना की इच्छा को तिलांजलि देकर गंगा नहाकर घर लौट जायें एवं शांत गृहस्थ की तरह अपना जीवन खेती-खलिहानी करते हुए गुजार दें।
साहित्य क्षेत्र में अपने पराजय की बात सोचकर उनका चित्त व्यथित होने लगता था। सौभाग्य से एक दिन डाकघर में उन्हें एक पत्रिका नजर आ गई। उस पत्रिका का नाम था ‘कल्लोल।’ ताराशंकर ने ‘कल्लोल’ का पता नोट कर लिया और उसी पते पर उन्होंने रसकली कहानी भेज दी। जल्दी ही उन्हें कहानी के स्वीकृत होने की सूचना मिली। उत्साहित करने वाले पवित्र गंगोपाध्याय ने लिखा, आप इतने दिनों तक मौन क्यों बैठे हुए थे ? महानगरी के साहित्य क्षेत्र में ताराशंकर की वह पहली स्वीकृति थी।
विचारों का साम्य न होने पर भी नये लेखकों के लिए ‘कल्लोल’ का द्वार हमेशा खुला रहता था। आगे के दो वर्षों तक कल्लोल में ताराशंकर की कई कहानियां प्रकाशित हुईं। फिर ‘कालि कलम; ‘उपासना’ और ‘उत्तरा’ पत्रिकाओं में भी उन्होंने लिखा। श्मशान के पथ पर नामक कहानी ‘उपासना’ पत्रिका में छपी थी।
ताराशंकर ने लिखा है कि उनके साहित्य-जीवन का पहला अध्याय अवहेलना और अवज्ञा का काल था। उनकी पुत्री का देहान्त आठ वर्ष की उर्म में हो गया। कन्या वियोग से शोकाकुल कथाशिल्पी ने इस बार ‘संध्यामणि’ कहानी लिखी। सजनीकान्त द्वारा संपादित ‘बंगश्री’ पत्रिका के पहले अंक में यह कहानी ‘श्मशान घाट’ नाम से छपी थी। ‘संध्यामणि’ के पहले ताराशंकर अठारह उन्नीस कहानियां लिख चुके थे, जिनमें रसकली राईकलम और मालाचंदन जैसी कहानियां भी थीं। लेकिन संध्यामणि ऐसी पहली कहानी थी जिसे बांग्ला साहित्य में सिर्फ ताराशंकर ही लिख सकते थे।
‘संध्यामणि’ छपने के बाद अंतरंग साहित्यकारों के बीच इसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद ‘भारतवर्ष’ में छपी ‘डाईनीर बांशी’ (डाईन की बांसुरी) और ‘बंगश्री’ में प्रकाशित दूसरी कहानी मेला ने ताराशंकर को कथाकारों की पहली पंक्ति में ला बिठाया।
ताराशंकर ने अपनी साहित्य जीवन की बातों में जिस अपमान की घटना का जिक्र किया है। वह ‘देश’ पत्रिका के दफ्तर में घटा था। यह सन् 1934 की बात है। उसके पहले ‘देश’ के शारदीय विशेषांक में उनकी बहुचर्चित कहानी ‘नारी और नागिनी’ छप चुकी थी। देश के प्रभात गांगुली ने ‘नारी और नागिनी’ की बेहद प्रशंसा की थी। गांगुली महाशय बड़े मूड़ी आदमी थी। मिजाज ठीक रहता तो बेहद दिलदरिया थे और अगर मिजाज बिगड़ता तो चीखते-चिल्लाते हुए इस तरह इन्कार करते थे कि लेखक को बहुत अपमानजनक लगता। ताराशंकर की ‘मुसाफिरखाना’ जैसी कहानी उन्हें पसंद नहीं आयी। वे उसे लौटाते हुए बोले, यह (अर्थात् देश पत्रिका) कोई डस्टबिन नहीं है।
ताराशंकर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गयी थी कि कोई उन्हें खारिज नहीं कर सकता था। यदा कदा आलोचना करते हुए कोई कहता, ‘कहानियां अच्छी लिखते हैं, शैली भी अच्छी होती है। लेकिन कहानियां, बड़ी स्थूल होती हैं। उनमें सूक्ष्मता का अभाव है। जिज्ञासु ताराशंकर ने इस पर कविगुरु रवीन्द्रनाथ की राय जाननी चाही। उत्तर में रवीन्द्रनाथ ने लिखा, ‘तुम्हारी रचनाओं को स्थूल दृष्टि कहकर जिसने बदनाम किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तु्म्हारी रचनाओं में बड़ा सूक्ष्म स्पर्श होता है और तुम्हारी कलम से वास्तविकता सच बनकर नजर आती है, जिसमें यथार्थ को कोई नुकसान नहीं पहुचंता। कहानी लिखते वक्त कहानी न लिखने को ही जो लोग बहादुरी समझते हैं तुम ऐसे लोगों के दल में शामिल नहीं हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। रचना में यथार्थ की रक्षा करना ही सबसे कठिन होता है।’
यथार्थ लेखन के इस दुरुह मार्गपर ताराशंकर की जययात्रा बिना किसी रोक टोक के निरंतर आगे बढ़ती ही गयी।
ताराशंकर के रचनाकार के केन्द्रीय वृत्तभूमि में देहात का ब्राह्मण समाज था। लेकिन उनके जीवन बोध ने धीरे-धीरे फैलते हुए सामान्यजन को अपने दायरे में ले लिया। रवीन्द्रनाथ ने सबसे पहले अपनी कहानियों में गांव देहात के क्षुद्र मनुष्य को स्थान दिया था। लघु प्राण मामूली कथा छोटी छोटी दुख की बातें, जो बेहद सहज और सरल हैं। जिनका जीवन है, उन्हीं को लेकर कविगुरु ने अपनी छोटी कहानियों की मंजूषा सजाकर बांग्ला साहित्य में कहानियों की प्राण प्रतिष्ठा की। शरत् साहित्य में मुख्यतः देहातों के मध्यवित्त समाज को ही प्राथमिकता दी गयी है। ताराशंकर ने समाज के दीन हीन अछूत स्तर के लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनाकर अपने रचनालोक को पूर्णता प्रदान की। इस दृष्टि से ताराशंकर सम्पूर्ण समाज के जीवन बोध के सर्वप्रथम कलाकार हैं।
उनकी कहानियों में अपने समय का परिवेश उजागर हुआ है। माटी से बने मानव जीवन को ही उन्होंने आविष्कृत किया। इसी दृष्टि से उनके साहित्य को आंचलिक कहा जाता है। अंचल विशेष की प्रकृति और उसी के प्रभाव से नियंत्रित मनुष्य के सुख-दुख की यथार्थता को कहानियों को चिचित्र करने से जाहिर है उनमें आंचलिक विशेषताएं नजर आयेंगी ही। इस दृष्टि से यथार्थ जीवन पर जो भी लिखा जाए वही आंचलिक हो जाता है। लेकिन अपने समय और परिवेश की विशेषताओं को ग्रहण करके जो साहित्य चिरंतन मानव सत्य को उजागर करता है उस साहित्य को आंचलिक कहकर उसे संकीण बनाना उचित नहीं होगा। ताराशंकर के साहित्य का व्यक्ति अपनी आदिम प्रवृत्ति, युगों से संचित संस्कार और वंशानुगत आजीविका ढोने वाला परिचित इन्सान है। इसीलिए ताराशंकर बंगला के सार्वभौमिक जीवन -शिल्पी हैं।
‘पंडित मोशाय कहानी- संग्रह में ताराशंकर की सर्वकालिक कहानियां सम्मिलित की गई हैं। ‘डाक हरकारा’ ‘मंथर विष,’ ‘रंगीन चश्मा,’ ‘पंडित मोशाय’ ‘प्रतिध्वनि’, चंडी राय का संन्यास’, ‘इस्कापन’, ‘प्रतीक्षा,’ ‘रायबाड़ी’ और ‘मुकुंद की मजलिस’ सभी कहानियां अपने समय की बहुपठित एवं बहुप्रशंसित कहानियों में से रही हैं।
ताराशंकर जीवन से गहरे रूप से जुड़े हुए कथाकार थे। बंगाल के ग्राम्य जीवन की सच्ची तस्वीर उनकी रचनाओं में दिखायी देती है। आप ताराशंकर की कोई भी कहानी बस एक बार पढ़ने बैठ जायें। वह में शीघ्र ही आपको अपने सम्मोहन में बांध लेगी। ताराशंकर की कहानियां उबाऊ नहीं होती। आखिर से अंत में अंत तक मानो उनमें एक रस धार सी बहती रहती है। अत्यंज और अछूत निम्नवर्ग के लोगों के प्रति अभिजात भद्र समाज के पाशविक उत्पीड़न के वीभत्स चेहरे पर पड़ी नकाब को ताराशंकर ने अपनी कहानियों में बखूबी हटाया है। खुद अभिजात कुल के जमींदार संतान होते हुए भी ताराशंकर सहानुभूति और करुणा के संवाहक बनकर पीड़ित लोगों के जीवन में अपनी भागीदारी करना चाहते थे। बात और व्यवहार में धरतीपुत्रों के साथ धीरे-धीरे उनका आत्मिक संबंध बन गया था।
अनुवादक
डाक हरकारा
डॉक्टरबाबू बुलावे पर जा रहे थे।
सावन के महीने की कृष्णपक्ष की रात थी। उस पर मौसम भी खराब था। बादलों से भरे आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। सामान्यतः अंधेरे में भी जो एक हल्का उजाला रहता है, वह भी नहीं था। घने बादलों की काली छाया के घने अंधेरे में पृथ्वी जैसे खो गयी थी। बस चारों तरफ फैले असंख्य जुगनुओं की ज्योति टिमटिमा रही थी-जैसे असीम अनंत मृत्यु के घेरे में क्षणभंगुर जीवन दीप्ति जन्म जन्मांतरों के माध्यम से चलती रहती है।
अचानक रास्ते के एक कीचड़ भरे गढ्ढे में बैलगाड़ी का एक पहिया पड़ जाने के कारण हुए झटके से डॉक्टर की सोच पर असर पड़ा। चारों तरफ पानी से भरे खेत थे जिनमें मेढ़क टर्रा रहे थे, आस पास के पेड़ों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। उसी के साथ गाड़ी के पहियों की किसी के एकसुर में रोने वाली आवाज की तरह ही एक करुण दीर्घ शब्द उन आवाजों के साथ बड़े सहज रुप से एकाकार हो गयी थी। सड़क के बगल के पेड़ों के पत्तों से टुपटाप टुपटाप करके पानी गिर रहा था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पक्की सड़क के सख्त पत्थर के टुकड़ों पर से वह बैलगाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। डॉक्टर अपने सामने के अंधेरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। दूर जैसे एक जुगनू अक्षय दीप्ति से जलते हुए बड़ी तेजी से इस तरफ ही आ रहा था।
डॉक्टर ने गाड़ीवान से पूछा, ‘अटल यह कैसी रोशनी है ?’
बरसात की रात में अटल नींद में ऊंघ रहा था, उसने एक बार जबर्दस्ती अपनी आंखें खोलकर देखते हुए कहा, पता नहीं बाबू ऐ ऐ इस बैल को क्या कहना चाहिए जरा बता तो ! यह कहकर वह उन दोनों बैलों को कोंचकर फिर ऊंघने लगा।
हां, वह रोशनी ही थी, उसकी रोशनी क्रमशः तेज होती जा रही थी, उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह रोशनी तेजी से इधर ही बढ़ती आ रही थी। डॉक्टर उद्गिग्न हो गया। ऐसे बुरे मौसम में कौन इस तरह दौड़ते हुए आ रहा था। रोगी के घर का कोई आदमी है क्या ?
झुन- झुन- झुन ! धीमी घंटियों की आवाज डॉक्टर के कानों में पड़ने लगी। डॉक्टर ने आवाज लगायी, कौन है ? कौन आ रहा है ?’
जवाब मिला, ‘डाक सरकार बहादुर की डाक। मैं डाक हरकारा हूं। कहते कहते वह आदमी नजदीक आ गया। घंटियों की आवाज अब साफ सुनायी पड़ने लगी। उस आदमी के हाथ में रोशनी। डॉक्टर ने देखा, एक नाटे कद का काला, अधेड़ आदमी कंधे पर डाक का थैला लटकाकर एक समान गति से दौड़ते हुए जा रहा था। उसके सिर पर एक फटी पगड़ी थी, एक हाथ में बल्लम था; उसी बल्लम के फाल के साथ झूलती हुई घंटी रुनझुन करती हुई बज रही थी।
डॉक्टर ने पूछा, तू दीन है न ?’
दीनू डोम डाक हरकारा था-मेल रनर। सात मील दूर आदमपुर स्टेशन से डाक लेकर हरिपुर पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा था। दीनू ने उसी तरह दौड़ते हुए जवाब दिया, हां।’
कितनी रात हुई, बता सकता है दीनू ?’
जी रात खत्म होने को ही आ रही है। तीन पहर बीत चुके हैं। दीनू की बात के अंतिम शब्द गाड़ी के पीछे से आये। मेल रनर समान गति से दौड़ रहा था। बात कहते कहते वह गाड़ी पार करके आगे बढ़ गया। घंटी की आवाज क्रमशः धीमी पड़ने लगी थी। रोशनी की शिखा क्रमशः परिधि से छोटी होते होते बिन्दु में बदल गयी थी।
अटल इस बीच जाग गया था। उसन अचानक पूछा, अच्छा डॉक्टरबाबू, इस बस्ते के अंदर क्या रहता है ?’
डॉक्टर ने हंसकर कहा, ‘चिट्ठी है रे चिट्ठी ! न जाने कितने देश देशांतरों की खबरें समझा ? एक सौ, दो सौ, पांच सौ कोस दूर जो कुछ घट रहा है, वही सब खबरें इस बैग में रहती है।’
अटल खामोश होकर कुछ सोचने लगा। देश देशांतरों की खबरें। लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर वह बोला ओह यूं ही नहीं कहते, हवा से भी ज्यादा तेज खबर भागती है।
सावन के महीने की कृष्णपक्ष की रात थी। उस पर मौसम भी खराब था। बादलों से भरे आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। सामान्यतः अंधेरे में भी जो एक हल्का उजाला रहता है, वह भी नहीं था। घने बादलों की काली छाया के घने अंधेरे में पृथ्वी जैसे खो गयी थी। बस चारों तरफ फैले असंख्य जुगनुओं की ज्योति टिमटिमा रही थी-जैसे असीम अनंत मृत्यु के घेरे में क्षणभंगुर जीवन दीप्ति जन्म जन्मांतरों के माध्यम से चलती रहती है।
अचानक रास्ते के एक कीचड़ भरे गढ्ढे में बैलगाड़ी का एक पहिया पड़ जाने के कारण हुए झटके से डॉक्टर की सोच पर असर पड़ा। चारों तरफ पानी से भरे खेत थे जिनमें मेढ़क टर्रा रहे थे, आस पास के पेड़ों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। उसी के साथ गाड़ी के पहियों की किसी के एकसुर में रोने वाली आवाज की तरह ही एक करुण दीर्घ शब्द उन आवाजों के साथ बड़े सहज रुप से एकाकार हो गयी थी। सड़क के बगल के पेड़ों के पत्तों से टुपटाप टुपटाप करके पानी गिर रहा था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पक्की सड़क के सख्त पत्थर के टुकड़ों पर से वह बैलगाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। डॉक्टर अपने सामने के अंधेरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। दूर जैसे एक जुगनू अक्षय दीप्ति से जलते हुए बड़ी तेजी से इस तरफ ही आ रहा था।
डॉक्टर ने गाड़ीवान से पूछा, ‘अटल यह कैसी रोशनी है ?’
बरसात की रात में अटल नींद में ऊंघ रहा था, उसने एक बार जबर्दस्ती अपनी आंखें खोलकर देखते हुए कहा, पता नहीं बाबू ऐ ऐ इस बैल को क्या कहना चाहिए जरा बता तो ! यह कहकर वह उन दोनों बैलों को कोंचकर फिर ऊंघने लगा।
हां, वह रोशनी ही थी, उसकी रोशनी क्रमशः तेज होती जा रही थी, उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह रोशनी तेजी से इधर ही बढ़ती आ रही थी। डॉक्टर उद्गिग्न हो गया। ऐसे बुरे मौसम में कौन इस तरह दौड़ते हुए आ रहा था। रोगी के घर का कोई आदमी है क्या ?
झुन- झुन- झुन ! धीमी घंटियों की आवाज डॉक्टर के कानों में पड़ने लगी। डॉक्टर ने आवाज लगायी, कौन है ? कौन आ रहा है ?’
जवाब मिला, ‘डाक सरकार बहादुर की डाक। मैं डाक हरकारा हूं। कहते कहते वह आदमी नजदीक आ गया। घंटियों की आवाज अब साफ सुनायी पड़ने लगी। उस आदमी के हाथ में रोशनी। डॉक्टर ने देखा, एक नाटे कद का काला, अधेड़ आदमी कंधे पर डाक का थैला लटकाकर एक समान गति से दौड़ते हुए जा रहा था। उसके सिर पर एक फटी पगड़ी थी, एक हाथ में बल्लम था; उसी बल्लम के फाल के साथ झूलती हुई घंटी रुनझुन करती हुई बज रही थी।
डॉक्टर ने पूछा, तू दीन है न ?’
दीनू डोम डाक हरकारा था-मेल रनर। सात मील दूर आदमपुर स्टेशन से डाक लेकर हरिपुर पोस्ट ऑफिस की ओर जा रहा था। दीनू ने उसी तरह दौड़ते हुए जवाब दिया, हां।’
कितनी रात हुई, बता सकता है दीनू ?’
जी रात खत्म होने को ही आ रही है। तीन पहर बीत चुके हैं। दीनू की बात के अंतिम शब्द गाड़ी के पीछे से आये। मेल रनर समान गति से दौड़ रहा था। बात कहते कहते वह गाड़ी पार करके आगे बढ़ गया। घंटी की आवाज क्रमशः धीमी पड़ने लगी थी। रोशनी की शिखा क्रमशः परिधि से छोटी होते होते बिन्दु में बदल गयी थी।
अटल इस बीच जाग गया था। उसन अचानक पूछा, अच्छा डॉक्टरबाबू, इस बस्ते के अंदर क्या रहता है ?’
डॉक्टर ने हंसकर कहा, ‘चिट्ठी है रे चिट्ठी ! न जाने कितने देश देशांतरों की खबरें समझा ? एक सौ, दो सौ, पांच सौ कोस दूर जो कुछ घट रहा है, वही सब खबरें इस बैग में रहती है।’
अटल खामोश होकर कुछ सोचने लगा। देश देशांतरों की खबरें। लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। आखिरकार एक गहरी सांस लेकर वह बोला ओह यूं ही नहीं कहते, हवा से भी ज्यादा तेज खबर भागती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book