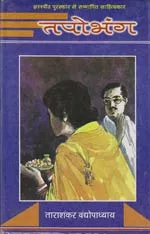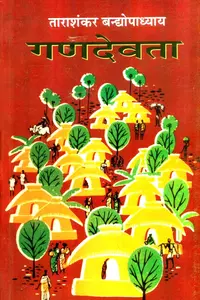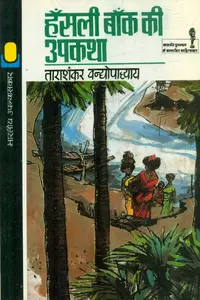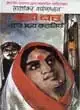|
कहानी संग्रह >> तपोभंग तपोभंगताराशंकर वन्द्योपाध्याय
|
222 पाठक हैं |
||||||
‘तपोभंग’ में निम्न कहानियां संकलित की गई हैं—अधेला और पैसा’, ‘रायबाड़ी’, तपोभंग’, ‘मधु मास्टर’, ‘मिट्टी’, ‘इन्सान का मन’, ‘व्याधि’ तथा ‘प्रतिध्वनि’।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित ताराशंकर वंद्योपाध्याय,
रवीन्द्रनाथ टैगोर और शरतचन्द्र के बाद बंगाल के प्रमुख लेखकों में से एक
हैं। उनका नाम विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय और मणिक वंद्योपाध्याय के साथ
लिया जाता है।
ताराशंकर का समग्र साहित्य स्वाधीनता की लड़ाई की पृष्ठभूमि में मनुष्य का जीवन संगीत मात्र ही नहीं है। कथा-साहित्य के तीन प्रमुख उपादानों स्थान, काल और पात्र की नींव पर जिन अविस्मरणीय कहानियों और उपन्यासों की उन्होंने रचना की है, वह जनता का सार्वकालिक जीवन संगीत है।
रवीन्द्रनाथ ने एक बार कहा था, ‘बहुसंख्यक गांवों से भरपूर हमारा जो देश है उस देश को देखने की दृष्टि हमने खो दी है। हमारे साहित्य क्षेत्र में जिन लोगों ने इस संकीर्ण सीमाबद्ध दृष्टि को पूरे देश में व्यापकता से प्रसारित किया है उनमें ताराशंकर का स्थान सबसे आगे है।’
खासकर रवीन्द्रनाथ ने जिन्हें ‘अंत्यज’ ‘मंत्रवर्जित’ कहा है, उस अवज्ञात अनार्य लोगों के सुख-दुख, सुगति-दुर्गति को ताराशंकर ने जिस रसदृष्टि से देखा था वैसा दृष्टि बांग्ला साहित्य में विरल ही है। इस दृष्टि से उनके उपन्यासों की तुलना में उनकी कहानियां बांग्ला साहित्य की अविस्मरणीय संपदा हैं। उनकी कहानियों ने विचित्र रस के उपादान से हमारे कथा-साहित्य को समृद्ध किया है।
बंगाल के गांवों पर लिखते हुए ताराशंकर ने कोई नई जमीन नहीं तोड़ी थी, क्योंकि शरतचन्द्र तथा कुछ अन्य लेखक ग्रामीणजनों के बारे में लिख चुके थे, पर उनके पास ताराशंकर जैसा ज्ञान, विशाल दृष्टि और इतिहास बोध नहीं था।
वस्तुतः बंगाल के ग्रामीण समाज को ऐसी समग्र और सार्वभौम दृष्टि से ताराशंकर से पहले किसी और ने नहीं देखा।
ताराशंकर का समग्र साहित्य स्वाधीनता की लड़ाई की पृष्ठभूमि में मनुष्य का जीवन संगीत मात्र ही नहीं है। कथा-साहित्य के तीन प्रमुख उपादानों स्थान, काल और पात्र की नींव पर जिन अविस्मरणीय कहानियों और उपन्यासों की उन्होंने रचना की है, वह जनता का सार्वकालिक जीवन संगीत है।
रवीन्द्रनाथ ने एक बार कहा था, ‘बहुसंख्यक गांवों से भरपूर हमारा जो देश है उस देश को देखने की दृष्टि हमने खो दी है। हमारे साहित्य क्षेत्र में जिन लोगों ने इस संकीर्ण सीमाबद्ध दृष्टि को पूरे देश में व्यापकता से प्रसारित किया है उनमें ताराशंकर का स्थान सबसे आगे है।’
खासकर रवीन्द्रनाथ ने जिन्हें ‘अंत्यज’ ‘मंत्रवर्जित’ कहा है, उस अवज्ञात अनार्य लोगों के सुख-दुख, सुगति-दुर्गति को ताराशंकर ने जिस रसदृष्टि से देखा था वैसा दृष्टि बांग्ला साहित्य में विरल ही है। इस दृष्टि से उनके उपन्यासों की तुलना में उनकी कहानियां बांग्ला साहित्य की अविस्मरणीय संपदा हैं। उनकी कहानियों ने विचित्र रस के उपादान से हमारे कथा-साहित्य को समृद्ध किया है।
बंगाल के गांवों पर लिखते हुए ताराशंकर ने कोई नई जमीन नहीं तोड़ी थी, क्योंकि शरतचन्द्र तथा कुछ अन्य लेखक ग्रामीणजनों के बारे में लिख चुके थे, पर उनके पास ताराशंकर जैसा ज्ञान, विशाल दृष्टि और इतिहास बोध नहीं था।
वस्तुतः बंगाल के ग्रामीण समाज को ऐसी समग्र और सार्वभौम दृष्टि से ताराशंकर से पहले किसी और ने नहीं देखा।
भूमिका
साहित्य में लेखकों के दो प्रकार के वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में ऐसे
लेखक होते हैं जो आते ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाते हैं। बांग्ला
साहित्य में विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय ऐसे उदाहरण हैं। उनका पहला उपन्यास
‘पथेर पांचाली’ ही उनके जीवन का श्रेष्ठ उपन्यास
साबित हुआ।
बाद में उन्होंने ढेरों उच्चकोटि की कहानियां, उपन्यास आदि लिखे लेकिन
शायद अपनी बाद की लिखी हुई किसी भी कृति को अपनी सर्वप्रथम कृति से ज्यादा
महत्त्वपूर्ण नहीं बना पाये।
दूसरे वर्ग के लेखकों की शुरुआती रचनाएं सामान्य ही होती है। उनकी प्रतिभा को लोगों की नजरों में आने के लिए दीर्घकालीन कठोर साधना ही जरूरत पड़ती है। ताराशंकर इसी वर्ग के लेखक थे। उनकी पहले दौर की लिखी काफी रचनाएं औरत दर्जे की हैं। लंबे समय तक काफी कुछ देखने परखने के बाद, व्यर्थता की काफी ग्लानि और निराशा पार करके उन्होंने अपने लेखन की धाक जमायी थी। अपराजित आत्मविश्वास और ईश्वर भर्तिं ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया।
अपनी अभिव्यक्ति के उचित माध्यम की तलाश में भी उन्हें कम भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने पहले कविताएं लिखीं, फिर नाटक और सबसे अंत में कथा साहित्य लिखा। कहानियां और उपन्यास ही ताराशंकर को अपनी बात कहने के उपयुक्त माध्यम नजर आये।
ताराशंकर का साहित्यिक जीवन आठ वर्ष की उम्र में कविताओं से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत उन्होंने नाट्य लेखन में रुचि दिखायी। उनकी नियमित साहित्य साधना 28 वर्ष की उम्र में लामपुर से प्रकाशित पूर्णमा मासिक पत्रिका से शुरु हुई। कविता, कहानी आलोचना, सम्पादकीय के रूप में इस पत्रिका की ज्यादातर सामग्री उन्हीं की लिखी हुई होती थी। पूर्णिमा में ही ताराशंकर की पहली उल्लेखनीय कहानी ‘प्रवाह का तिनका’ प्रकाशित हुई थी।
कुछ दिन बाद ही ताराशंकर ने ‘रसकली’ नामक कहानी लिखी और ‘प्रवासी’ पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेज दी। कई महीनों तक बार बार –बार पत्र लिखने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार ताराशंकर खुद ‘प्रवासी’ ऑफिस में उपस्थिति हुए। जैसा अमूमन होता है, नये लेखक की रचना बिना पढ़े ही सम्पादकीय विभाग ने वापस लौटा दी। उस अस्वीकृत रचना को लेकर ताराशंकर पैदल ही मध्य कलकत्ता से दक्षिण कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे। उस दिन उनकी आंखें कई बार भर आई थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि साहित्य साधना की इच्छा को तिलांजलि देकर गंगा नहाकर घर लौट जायें एवं शांत गृहस्थ की तरह अपना जीवन खेती-खलिहानी करते हुए गुजार दें।
साहित्य क्षेत्र में अपने पराजय की बात सोचकर उनका चित्त व्यथित होने लगता था। सौभाग्य से एक दिन डाकघर में उन्हें एक पत्रिका नजर आ गई। उस पत्रिका का नाम था ‘कल्लोल।’ ताराशंकर ने ‘कल्लोल’ का पता नोट कर लिया और उसी पते पर उन्होंने रसकली कहानी भेज दी। जल्दी ही उन्हें कहानी के स्वीकृत होने की सूचना मिली। उत्साहित करने वाले पवित्र गंगोपाध्याय ने लिखा, आप इतने दिनों तक मौन क्यों बैठे हुए थे ? महानगरी के साहित्य क्षेत्र में ताराशंकर की वह पहली स्वीकृति थी।
विचारों का साम्य न होने पर भी नये लेखकों के लिए ‘कल्लोल’ का द्वार हमेशा खुला रहता था। आगे के दो वर्षों तक कल्लोल में ताराशंकर की कई कहानियां प्रकाशित हुईं। फिर ‘कालि कलम; ‘उपासना’ और ‘उत्तरा’ पत्रिकाओं में भी उन्होंने लिखा। श्मशान के पथ पर नामक कहानी ‘उपासना’ पत्रिका में छपी थी।
ताराशंकर ने लिखा है कि उनके साहित्य-जीवन का पहला अध्याय अवहेलना और अवज्ञा का काल था। उनकी पुत्री का देहान्त आठ वर्ष की उर्म में हो गया। कन्या वियोग से शोकाकुल कथाशिल्पी ने इस बार ‘संध्यामणि’ कहानी लिखी। सजनीकान्त द्वारा संपादित ‘बंगश्री’ पत्रिका के पहले अंक में यह कहानी ‘श्मशान घाट’ नाम से छपी थी। ‘संध्यामणि’ के पहले ताराशंकर अठारह उन्नीस कहानियां लिख चुके थे, जिनमें रसकली राईकलम और मालाचंदन जैसी कहानियां भी थीं। लेकिन संध्यामणि ऐसी पहली कहानी थी जिसे बांग्ला साहित्य में सिर्फ ताराशंकर ही लिख सकते थे।
‘संध्यामणि’ छपने के बाद अंतरंग साहित्यकारों के बीच इसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद ‘भारतवर्ष’ में छपी ‘डाईनीर बांशी’ (डाईन की बांसुरी) और ‘बंगश्री’ में प्रकाशित दूसरी कहानी मेला ने ताराशंकर को कथाकारों की पहली पंक्ति में ला बिठाया।
ताराशंकर ने अपनी साहित्य जीवन की बातों में जिस अपमान की घटना का जिक्र किया है। वह ‘देश’ पत्रिका के दफ्तर में घटा था। यह सन् 1934 की बात है। उसके पहले ‘देश’ के शारदीय विशेषांक में उनकी बहुचर्चित कहानी ‘नारी और नागिनी’ छप चुकी थी। देश के प्रभात गांगुली ने ‘नारी और नागिनी’ की बेहद प्रशंसा की थी। गांगुली महाशय बड़े मूड़ी आदमी थी। मिजाज ठीक रहता तो बेहद दिलदरिया थे और अगर मिजाज बिगड़ता तो चीखते-चिल्लाते हुए इस तरह इन्कार करते थे कि लेखक को बहुत अपमानजनक लगता। ताराशंकर की ‘मुसाफिरखाना’ जैसी कहानी उन्हें पसंद नहीं आयी। वे उसे लौटाते हुए बोले, यह (अर्थात् देश पत्रिका) कोई डस्टबिन नहीं है।
ताराशंकर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गयी थी कि कोई उन्हें खारिज नहीं कर सकता था। यदा कदा आलोचना करते हुए कोई कहता, ‘कहानियां अच्छी लिखते हैं, शैली भी अच्छी होती है। लेकिन कहानियां, बड़ी स्थूल होती हैं। उनमें सूक्ष्मता का अभाव है। जिज्ञासु ताराशंकर ने इस पर कविगुरु रवीन्द्रनाथ की राय जाननी चाही। उत्तर में रवीन्द्रनाथ ने लिखा, ‘तुम्हारी रचनाओं को स्थूल दृष्टि कहकर जिसने बदनाम किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तु्म्हारी रचनाओं में बड़ा सूक्ष्म स्पर्श होता है और तुम्हारी कलम से वास्तविकता सच बनकर नजर आती है, जिसमें यथार्थ को कोई नुकसान नहीं पहुचंता। कहानी लिखते वक्त कहानी न लिखने को ही जो लोग बहादुरी समझते हैं तुम ऐसे लोगों के दल में शामिल नहीं हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। रचना में यथार्थ की रक्षा करना ही सबसे कठिन होता है।’
यथार्थ लेखन के इस दुरुह मार्गपर ताराशंकर की जययात्रा बिना किसी रोक टोक के निरंतर आगे बढ़ती ही गयी।
ताराशंकर के रचनाकार के केन्द्रीय वृत्तभूमि में देहात का ब्राह्मण समाज था। लेकिन उनके जीवन बोध ने धीरे-धीरे फैलते हुए सामान्यजन को अपने दायरे में ले लिया। रवीन्द्रनाथ ने सबसे पहले अपनी कहानियों में गांव देहात के क्षुद्र मनुष्य को स्थान दिया था। लघु प्राण मामूली कथा छोटी छोटी दुख की बातें, जो बेहद सहज और सरल हैं। जिनका जीवन है, उन्हीं को लेकर कविगुरु ने अपनी छोटी कहानियों की मंजूषा सजाकर बांग्ला साहित्य में कहानियों की प्राण प्रतिष्ठा की। शरत् साहित्य में मुख्यतः देहातों के मध्यवित्त समाज को ही प्राथमिकता दी गयी है। ताराशंकर ने समाज के दीन हीन अछूत स्तर के लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनाकर अपने रचनालोक को पूर्णता प्रदान की। इस दृष्टि से ताराशंकर सम्पूर्ण समाज के जीवन बोध के सर्वप्रथम कलाकार हैं। उनकी कहानियों में अपने समय का परिवेश उजागर हुआ है। माटी से बने मानव जीवन को ही उन्होंने आविष्कृत किया। इसी दृष्टि से उनके साहित्य को आंचलिक कहा जाता है। अंचल विशेष की प्रकृति और उसी के प्रभाव से नियंत्रित मनुष्य के सुख-दुख की यथार्थता को कहानियों को चिचित्र करने से जाहिर है उनमें आंचलिक विशेषताएं नजर आयेंगी ही। इस दृष्टि से यथार्थ जीवन पर जो भी लिखा जाए वही आंचलिक हो जाता है। लेकिन अपने समय और परिवेश की विशेषताओं को ग्रहण करके जो साहित्य चिरंतन मानव सत्य को उजागर करता है उस साहित्य को आंचलिक कहकर उसे संकीण बनाना उचित नहीं होगा। ताराशंकर के साहित्य का व्यक्ति अपनी आदिम प्रवृत्ति, युगों से संचित संस्कार और वंशानुगत आजीविका ढोने वाला परिचित इन्सान है। इसीलिए ताराशंकर बंगला के सार्वभौमिक जीवन -शिल्पी हैं।
ताराशंकर की कहानियों की मुख्य विशेषता है समाज के अज्ञात कुलशील क्षुद्र समझे जाने वाले लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना और अंतरंगता। भारतीय मानव समाज के आदि स्तर के निर्माता थे, परवर्ती का के आर्य सभ्यता के प्रसार और प्रतिष्ठा के फलस्वरूप वे लोग समाज की सीमारेखा के बाहर अवज्ञात और अवहेलित होकर पढ़ रहे; शिक्षित और सभ्यताभिमानी तथा अपने को ऊंचा समझने वाले लोगों ने जिनकी ओर मुंह उठाकर नहीं देखा, ताराशंकर उन्हीं पतितों-अवहेलितों के कथाकार थे।
‘तपोभंग’ कथा-संकलन में ताराशंकर वंद्योपाध्याय की निम्म कहानियां संकलित की गई हैं—अधेला और पैसा’, ‘रायबाड़ी’, ‘तपोभंग’, ‘मधु मास्टर’, ‘मिट्टी’, ‘इन्सान का मन’, ‘व्याधि’ तथा ‘प्रतिध्वनि’।
ये कहानियां ताराशंकर की कथा-यात्रा के विभिन्न पड़ावों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके कथा-लेखन की विविधता को दर्शाती हैं।
दूसरे वर्ग के लेखकों की शुरुआती रचनाएं सामान्य ही होती है। उनकी प्रतिभा को लोगों की नजरों में आने के लिए दीर्घकालीन कठोर साधना ही जरूरत पड़ती है। ताराशंकर इसी वर्ग के लेखक थे। उनकी पहले दौर की लिखी काफी रचनाएं औरत दर्जे की हैं। लंबे समय तक काफी कुछ देखने परखने के बाद, व्यर्थता की काफी ग्लानि और निराशा पार करके उन्होंने अपने लेखन की धाक जमायी थी। अपराजित आत्मविश्वास और ईश्वर भर्तिं ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया।
अपनी अभिव्यक्ति के उचित माध्यम की तलाश में भी उन्हें कम भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने पहले कविताएं लिखीं, फिर नाटक और सबसे अंत में कथा साहित्य लिखा। कहानियां और उपन्यास ही ताराशंकर को अपनी बात कहने के उपयुक्त माध्यम नजर आये।
ताराशंकर का साहित्यिक जीवन आठ वर्ष की उम्र में कविताओं से प्रारंभ हुआ। तदुपरांत उन्होंने नाट्य लेखन में रुचि दिखायी। उनकी नियमित साहित्य साधना 28 वर्ष की उम्र में लामपुर से प्रकाशित पूर्णमा मासिक पत्रिका से शुरु हुई। कविता, कहानी आलोचना, सम्पादकीय के रूप में इस पत्रिका की ज्यादातर सामग्री उन्हीं की लिखी हुई होती थी। पूर्णिमा में ही ताराशंकर की पहली उल्लेखनीय कहानी ‘प्रवाह का तिनका’ प्रकाशित हुई थी।
कुछ दिन बाद ही ताराशंकर ने ‘रसकली’ नामक कहानी लिखी और ‘प्रवासी’ पत्रिका को प्रकाशनार्थ भेज दी। कई महीनों तक बार बार –बार पत्र लिखने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार ताराशंकर खुद ‘प्रवासी’ ऑफिस में उपस्थिति हुए। जैसा अमूमन होता है, नये लेखक की रचना बिना पढ़े ही सम्पादकीय विभाग ने वापस लौटा दी। उस अस्वीकृत रचना को लेकर ताराशंकर पैदल ही मध्य कलकत्ता से दक्षिण कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचे। उस दिन उनकी आंखें कई बार भर आई थीं। एक बार उन्होंने सोचा कि साहित्य साधना की इच्छा को तिलांजलि देकर गंगा नहाकर घर लौट जायें एवं शांत गृहस्थ की तरह अपना जीवन खेती-खलिहानी करते हुए गुजार दें।
साहित्य क्षेत्र में अपने पराजय की बात सोचकर उनका चित्त व्यथित होने लगता था। सौभाग्य से एक दिन डाकघर में उन्हें एक पत्रिका नजर आ गई। उस पत्रिका का नाम था ‘कल्लोल।’ ताराशंकर ने ‘कल्लोल’ का पता नोट कर लिया और उसी पते पर उन्होंने रसकली कहानी भेज दी। जल्दी ही उन्हें कहानी के स्वीकृत होने की सूचना मिली। उत्साहित करने वाले पवित्र गंगोपाध्याय ने लिखा, आप इतने दिनों तक मौन क्यों बैठे हुए थे ? महानगरी के साहित्य क्षेत्र में ताराशंकर की वह पहली स्वीकृति थी।
विचारों का साम्य न होने पर भी नये लेखकों के लिए ‘कल्लोल’ का द्वार हमेशा खुला रहता था। आगे के दो वर्षों तक कल्लोल में ताराशंकर की कई कहानियां प्रकाशित हुईं। फिर ‘कालि कलम; ‘उपासना’ और ‘उत्तरा’ पत्रिकाओं में भी उन्होंने लिखा। श्मशान के पथ पर नामक कहानी ‘उपासना’ पत्रिका में छपी थी।
ताराशंकर ने लिखा है कि उनके साहित्य-जीवन का पहला अध्याय अवहेलना और अवज्ञा का काल था। उनकी पुत्री का देहान्त आठ वर्ष की उर्म में हो गया। कन्या वियोग से शोकाकुल कथाशिल्पी ने इस बार ‘संध्यामणि’ कहानी लिखी। सजनीकान्त द्वारा संपादित ‘बंगश्री’ पत्रिका के पहले अंक में यह कहानी ‘श्मशान घाट’ नाम से छपी थी। ‘संध्यामणि’ के पहले ताराशंकर अठारह उन्नीस कहानियां लिख चुके थे, जिनमें रसकली राईकलम और मालाचंदन जैसी कहानियां भी थीं। लेकिन संध्यामणि ऐसी पहली कहानी थी जिसे बांग्ला साहित्य में सिर्फ ताराशंकर ही लिख सकते थे।
‘संध्यामणि’ छपने के बाद अंतरंग साहित्यकारों के बीच इसकी व्यापक चर्चा हुई। इसके बाद ‘भारतवर्ष’ में छपी ‘डाईनीर बांशी’ (डाईन की बांसुरी) और ‘बंगश्री’ में प्रकाशित दूसरी कहानी मेला ने ताराशंकर को कथाकारों की पहली पंक्ति में ला बिठाया।
ताराशंकर ने अपनी साहित्य जीवन की बातों में जिस अपमान की घटना का जिक्र किया है। वह ‘देश’ पत्रिका के दफ्तर में घटा था। यह सन् 1934 की बात है। उसके पहले ‘देश’ के शारदीय विशेषांक में उनकी बहुचर्चित कहानी ‘नारी और नागिनी’ छप चुकी थी। देश के प्रभात गांगुली ने ‘नारी और नागिनी’ की बेहद प्रशंसा की थी। गांगुली महाशय बड़े मूड़ी आदमी थी। मिजाज ठीक रहता तो बेहद दिलदरिया थे और अगर मिजाज बिगड़ता तो चीखते-चिल्लाते हुए इस तरह इन्कार करते थे कि लेखक को बहुत अपमानजनक लगता। ताराशंकर की ‘मुसाफिरखाना’ जैसी कहानी उन्हें पसंद नहीं आयी। वे उसे लौटाते हुए बोले, यह (अर्थात् देश पत्रिका) कोई डस्टबिन नहीं है।
ताराशंकर की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन गयी थी कि कोई उन्हें खारिज नहीं कर सकता था। यदा कदा आलोचना करते हुए कोई कहता, ‘कहानियां अच्छी लिखते हैं, शैली भी अच्छी होती है। लेकिन कहानियां, बड़ी स्थूल होती हैं। उनमें सूक्ष्मता का अभाव है। जिज्ञासु ताराशंकर ने इस पर कविगुरु रवीन्द्रनाथ की राय जाननी चाही। उत्तर में रवीन्द्रनाथ ने लिखा, ‘तुम्हारी रचनाओं को स्थूल दृष्टि कहकर जिसने बदनाम किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि तु्म्हारी रचनाओं में बड़ा सूक्ष्म स्पर्श होता है और तुम्हारी कलम से वास्तविकता सच बनकर नजर आती है, जिसमें यथार्थ को कोई नुकसान नहीं पहुचंता। कहानी लिखते वक्त कहानी न लिखने को ही जो लोग बहादुरी समझते हैं तुम ऐसे लोगों के दल में शामिल नहीं हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। रचना में यथार्थ की रक्षा करना ही सबसे कठिन होता है।’
यथार्थ लेखन के इस दुरुह मार्गपर ताराशंकर की जययात्रा बिना किसी रोक टोक के निरंतर आगे बढ़ती ही गयी।
ताराशंकर के रचनाकार के केन्द्रीय वृत्तभूमि में देहात का ब्राह्मण समाज था। लेकिन उनके जीवन बोध ने धीरे-धीरे फैलते हुए सामान्यजन को अपने दायरे में ले लिया। रवीन्द्रनाथ ने सबसे पहले अपनी कहानियों में गांव देहात के क्षुद्र मनुष्य को स्थान दिया था। लघु प्राण मामूली कथा छोटी छोटी दुख की बातें, जो बेहद सहज और सरल हैं। जिनका जीवन है, उन्हीं को लेकर कविगुरु ने अपनी छोटी कहानियों की मंजूषा सजाकर बांग्ला साहित्य में कहानियों की प्राण प्रतिष्ठा की। शरत् साहित्य में मुख्यतः देहातों के मध्यवित्त समाज को ही प्राथमिकता दी गयी है। ताराशंकर ने समाज के दीन हीन अछूत स्तर के लोगों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपनाकर अपने रचनालोक को पूर्णता प्रदान की। इस दृष्टि से ताराशंकर सम्पूर्ण समाज के जीवन बोध के सर्वप्रथम कलाकार हैं। उनकी कहानियों में अपने समय का परिवेश उजागर हुआ है। माटी से बने मानव जीवन को ही उन्होंने आविष्कृत किया। इसी दृष्टि से उनके साहित्य को आंचलिक कहा जाता है। अंचल विशेष की प्रकृति और उसी के प्रभाव से नियंत्रित मनुष्य के सुख-दुख की यथार्थता को कहानियों को चिचित्र करने से जाहिर है उनमें आंचलिक विशेषताएं नजर आयेंगी ही। इस दृष्टि से यथार्थ जीवन पर जो भी लिखा जाए वही आंचलिक हो जाता है। लेकिन अपने समय और परिवेश की विशेषताओं को ग्रहण करके जो साहित्य चिरंतन मानव सत्य को उजागर करता है उस साहित्य को आंचलिक कहकर उसे संकीण बनाना उचित नहीं होगा। ताराशंकर के साहित्य का व्यक्ति अपनी आदिम प्रवृत्ति, युगों से संचित संस्कार और वंशानुगत आजीविका ढोने वाला परिचित इन्सान है। इसीलिए ताराशंकर बंगला के सार्वभौमिक जीवन -शिल्पी हैं।
ताराशंकर की कहानियों की मुख्य विशेषता है समाज के अज्ञात कुलशील क्षुद्र समझे जाने वाले लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना और अंतरंगता। भारतीय मानव समाज के आदि स्तर के निर्माता थे, परवर्ती का के आर्य सभ्यता के प्रसार और प्रतिष्ठा के फलस्वरूप वे लोग समाज की सीमारेखा के बाहर अवज्ञात और अवहेलित होकर पढ़ रहे; शिक्षित और सभ्यताभिमानी तथा अपने को ऊंचा समझने वाले लोगों ने जिनकी ओर मुंह उठाकर नहीं देखा, ताराशंकर उन्हीं पतितों-अवहेलितों के कथाकार थे।
‘तपोभंग’ कथा-संकलन में ताराशंकर वंद्योपाध्याय की निम्म कहानियां संकलित की गई हैं—अधेला और पैसा’, ‘रायबाड़ी’, ‘तपोभंग’, ‘मधु मास्टर’, ‘मिट्टी’, ‘इन्सान का मन’, ‘व्याधि’ तथा ‘प्रतिध्वनि’।
ये कहानियां ताराशंकर की कथा-यात्रा के विभिन्न पड़ावों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके कथा-लेखन की विविधता को दर्शाती हैं।
अनुवादक
अधेला और पैसा
दियासलाई के बाजार में आग लग गयी। आग दियासलाई के कारखाने या गोदाम में
नहीं बल्कि उसके दाम में लगी थी। आधे पैसे की दियासलाई का दाम बढ़कर एक
पैसा हो गया। दियासलाई के डिब्बे पर लिखा रहता ‘चालीस
तीलियां’, मगर तीस तीलियों से ज्यादा नहीं होता था। इसके अलावा
पांच
तीलियों पर मसाला भी नहीं चिपका रहता था। इसके अतिरिक्त पांच तीलियां टूटी
भी रहती थीं। शहर में तो एक बार सिगरेट लाइटर की अचानक बिक्री बढ़ गयी।
जेबकतरे खीझने लगे। जब जेब काटने में उनके हाथ में लाइटर ही पड़ती। गांव
में लोग पीठ दिखाने लगे मतलब वे पीछे चले गये। वहां पर पुरातन का
पुनराविर्भाव हुआ, नये सिरे से चकमक पत्थर व्यवहार होने लगा। महू ग्राम का
मदन कर्मकार कुछ दिन से लगातार चकमक के लिए लोहे की बेंकी तैयार कर रहा
था, मगर वह सफल नहीं हो पा रहा था।
भूलूदत्त के यहां तीन पुरखों से महाजनी चली आ रही थी। वह व्यवसायी भी भी था। उसने दियासलाई का कारोबार बंद कर दिया। हालांकि बेचना बंद नहीं किया। मगर खुद इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मदन से वह चार बेंकी खरीद लाया। एक उसने दुकान पर रखा, एक घर में, एक अपनी जेब में और आखिरी को उसने अपने बेटे मरीराम को देते हुए कहा, ‘ले, इसे रख ले।’’
मरीराम अपने बाप को देखने लगा, वह समझ नहीं पाया, इसे कहां रखना था। भूलूदत्त् खीझकर बोला, ‘जेब में। जेब में रख नवाबजादा। एक पत्थर ले लेना और बांस के चोंगे के भीतर थोड़े से पीले रंग का कस्ता। समझ गये ?’
मरीराम खीझकर बोला, ‘‘इससे जेब फट जायेगी।’
बेहद खीझते हुए अपने बेटे की ओर कुछ देर तक देखने के बाद दत्त न कहा, ‘अरे सूअर, अपने कपड़े मुझे देना, मैं मजबूत कपड़े की जेब लगवा दूंगा।’
मरीराम बड़बड़ता हुआ बाहर निकल गया।
दत्त ने कहा, ‘‘ससुरा जंगली है, मामूली सूअर नहीं।’
दत्त के किराने की दुकान के बगल में ही मरीराम ने तस्वीरों और आईनों की दुकान खोली थी। उसी दिन दत्त ने देखा कि एक मोरीराम दस मोरीराम बनकर माचिस से दस तीलियों के एक साथ जलाकर अपनी बीड़ी सुलगा रहा था। यह देखकर सलाई की तीलियों की तरह वह भी भक् से जल उठा। बोला, ‘मोरे, अरे ओ सूअर ! इतनी तीलियां एक साथ जलाकर क्या लक्ष्मी माई की चिता सजा रहा है ?’’
उत्तेजना से वह भूल गया कि उसने जो दस मरीराम को दस तीलियां जलाते हुए देखा था। वह वहां लगे आईनों का कमाल था।
मरीराम भी खीझ गया। अपने नयी उम्र में अपने पिता की ऐसी कंजूसी उसे पसंद नहीं थी। उसने कहा, ‘मैंने दस तीलियां कहां से जला लीं ? एक ही तो जलायी है।’
‘मगर वही क्यों जलायी ? पता है, इस एक ही तीली में पूरा गाव जलकर राख हो सकता है।’
‘तब क्या ‘यह’ मैं नहीं पी सकता ?’
मरीराम बहुत नाराज हो गया था। फिर भी उसने पिता का सम्मान करने के लिए ‘बीड़ी’ न कहकर ‘यह’ कहा।
दत्त ने कहा, ‘यह’ जरूर पियो। मगर तीली जलाकर क्यों ? तेरा, चकमक पत्थर कहां गया ?’
मरीराम बड़बड़ाते हुए बोला, ‘बीस बार ठोकने पर एक बार चिनगारी निकलती है। वह मैं.....।’
दत्त ने टोकते हुए कहा, ‘अरे सूअर, जरा तलाश करके एक ‘घोड़ाखुरे (घोड़े की नाल के आकार वाला) पत्थर ले आ।’
मरीराम छिपकर पिता को मुंह बिराकर दोनों अंगूठा दिखाते हुए चुप हो रहा। कुछ देर रुककर दत्त बोला, ‘जरा दुकान की देखभाल करना। मैं तगादे पर गोपालपुर जा रहा हूं।’
गोपालपुर वहां से कोसभर दूर था। वहां लाल मिट्टी पथरीले रास्ते से जाना पड़ता था। जाते समय दत्त ने रास्ते से चकमक पत्थर उठाते हुए अपनी जेब में भर ली। तगादा करने के बाद भी उसकी दूसरी जेब सूनी ही रह गयी, एक भी तांबे का टुकड़ा उसमें नहीं आया। खीझकर लौटते समय उसने वह खाली जेब भी चकमक पत्थरों से भर ली।
अब रखने की जगह नहीं थी मगर चकमक पत्थरों पर उसकी नजर थी।
आखिरकार दत्त को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसकी निगाह रह-रहकर उन पत्थरों पर पड़ रही थी, हर पत्थर उसे उठाने लायक लगता था। उसकी नजर एक थोड़े बड़े और आकर्षक लगने वाले एक पत्थर पर पड़ी। साधारणतः ऐसा पत्थर नजर नहीं आता। दत्त ने उसे उठा लिया। रखने की जगह न रखने के कारण सारे रास्ते वह उसे हाथ में लिये रहा।
भूलूदत्त के यहां तीन पुरखों से महाजनी चली आ रही थी। वह व्यवसायी भी भी था। उसने दियासलाई का कारोबार बंद कर दिया। हालांकि बेचना बंद नहीं किया। मगर खुद इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मदन से वह चार बेंकी खरीद लाया। एक उसने दुकान पर रखा, एक घर में, एक अपनी जेब में और आखिरी को उसने अपने बेटे मरीराम को देते हुए कहा, ‘ले, इसे रख ले।’’
मरीराम अपने बाप को देखने लगा, वह समझ नहीं पाया, इसे कहां रखना था। भूलूदत्त् खीझकर बोला, ‘जेब में। जेब में रख नवाबजादा। एक पत्थर ले लेना और बांस के चोंगे के भीतर थोड़े से पीले रंग का कस्ता। समझ गये ?’
मरीराम खीझकर बोला, ‘‘इससे जेब फट जायेगी।’
बेहद खीझते हुए अपने बेटे की ओर कुछ देर तक देखने के बाद दत्त न कहा, ‘अरे सूअर, अपने कपड़े मुझे देना, मैं मजबूत कपड़े की जेब लगवा दूंगा।’
मरीराम बड़बड़ता हुआ बाहर निकल गया।
दत्त ने कहा, ‘‘ससुरा जंगली है, मामूली सूअर नहीं।’
दत्त के किराने की दुकान के बगल में ही मरीराम ने तस्वीरों और आईनों की दुकान खोली थी। उसी दिन दत्त ने देखा कि एक मोरीराम दस मोरीराम बनकर माचिस से दस तीलियों के एक साथ जलाकर अपनी बीड़ी सुलगा रहा था। यह देखकर सलाई की तीलियों की तरह वह भी भक् से जल उठा। बोला, ‘मोरे, अरे ओ सूअर ! इतनी तीलियां एक साथ जलाकर क्या लक्ष्मी माई की चिता सजा रहा है ?’’
उत्तेजना से वह भूल गया कि उसने जो दस मरीराम को दस तीलियां जलाते हुए देखा था। वह वहां लगे आईनों का कमाल था।
मरीराम भी खीझ गया। अपने नयी उम्र में अपने पिता की ऐसी कंजूसी उसे पसंद नहीं थी। उसने कहा, ‘मैंने दस तीलियां कहां से जला लीं ? एक ही तो जलायी है।’
‘मगर वही क्यों जलायी ? पता है, इस एक ही तीली में पूरा गाव जलकर राख हो सकता है।’
‘तब क्या ‘यह’ मैं नहीं पी सकता ?’
मरीराम बहुत नाराज हो गया था। फिर भी उसने पिता का सम्मान करने के लिए ‘बीड़ी’ न कहकर ‘यह’ कहा।
दत्त ने कहा, ‘यह’ जरूर पियो। मगर तीली जलाकर क्यों ? तेरा, चकमक पत्थर कहां गया ?’
मरीराम बड़बड़ाते हुए बोला, ‘बीस बार ठोकने पर एक बार चिनगारी निकलती है। वह मैं.....।’
दत्त ने टोकते हुए कहा, ‘अरे सूअर, जरा तलाश करके एक ‘घोड़ाखुरे (घोड़े की नाल के आकार वाला) पत्थर ले आ।’
मरीराम छिपकर पिता को मुंह बिराकर दोनों अंगूठा दिखाते हुए चुप हो रहा। कुछ देर रुककर दत्त बोला, ‘जरा दुकान की देखभाल करना। मैं तगादे पर गोपालपुर जा रहा हूं।’
गोपालपुर वहां से कोसभर दूर था। वहां लाल मिट्टी पथरीले रास्ते से जाना पड़ता था। जाते समय दत्त ने रास्ते से चकमक पत्थर उठाते हुए अपनी जेब में भर ली। तगादा करने के बाद भी उसकी दूसरी जेब सूनी ही रह गयी, एक भी तांबे का टुकड़ा उसमें नहीं आया। खीझकर लौटते समय उसने वह खाली जेब भी चकमक पत्थरों से भर ली।
अब रखने की जगह नहीं थी मगर चकमक पत्थरों पर उसकी नजर थी।
आखिरकार दत्त को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसकी निगाह रह-रहकर उन पत्थरों पर पड़ रही थी, हर पत्थर उसे उठाने लायक लगता था। उसकी नजर एक थोड़े बड़े और आकर्षक लगने वाले एक पत्थर पर पड़ी। साधारणतः ऐसा पत्थर नजर नहीं आता। दत्त ने उसे उठा लिया। रखने की जगह न रखने के कारण सारे रास्ते वह उसे हाथ में लिये रहा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book