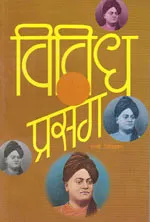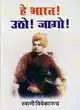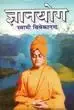|
विवेकानन्द साहित्य >> विविध प्रसंग विविध प्रसंगस्वामी विवेकानन्द
|
73 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है किताब विविध प्रसंग...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
दो शब्द
प्रथम संस्करण
स्वामी विवेकानन्द एक अपूर्व प्रतिभाशाली मनीषी थे। हमें केवल आध्यात्मिक
क्षेत्र में ही उनकी इस अलौकिक प्रखर प्रतिभा का परिचय नहीं, मिलता वरन्
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में—मानव-जीवन के घनिष्ठ सम्बन्ध रखने
वाले प्रत्येक विषय में भी हम उनकी दिव्य झाँकी देखते हैं। यही कारण था कि
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर मि.जे.एच. राइट ने उनकी
प्रतिभा से प्रभावित हो कहा था, ‘‘आपसे परिचय-पत्र के
लिए
पूछना मानो सूर्य से यह पूछना है कि तुम्हारा चमकने का क्या अधिकार है
!’’ उन्होंने यह भी लिखा, ‘‘मेरा
विश्वास है कि
यह अज्ञात हिन्दू संन्यासी हमारे सभी विद्वानों को एकत्रित करने पर जो कुछ
हो सकता है, उससे भी अधिक विद्वान् है।’’
प्रस्तुत पुस्तक स्वामीजी द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिए गए व्याख्यानों की टिप्पणियों का संग्रह है। इन व्याख्यानों में उन्होंने विविध महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर अपने मौलिक विचार प्रकट किये हैं; उदाहरणार्थ—भक्तियोग, कर्मयोग, कला, ज्ञानयोग, भाषा, संन्यासी और गृहस्थ, नियम और मुक्ति, आदि-आदि। यदि भारत स्वामीजी के इन जीवनप्रद विचारों द्वारा अपने को अनुप्राणित कर सके तो निश्चय ही वह अपनी अतीत गौरव-गरिमा का पुनर्लाभ कर सकेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं।
हम डॉ. महादेवप्रसादजी शर्मा, एम.ए., डी. लिट्., के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने मूल अंग्रेजी से प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद किया है। भाषा एवं भाव दोनों ही दृष्टिकोण से उनका यह कार्य सफल रहा है।
हमारा पूर्ण विश्वास है कि आज, जब हम नव-भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए कमर कसे हुए हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर स्वामीजी के ये उद्बोधक एवं रचनात्मक विचार अत्यन्त उपादेय सिद्ध होंगे।
प्रस्तुत पुस्तक स्वामीजी द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिए गए व्याख्यानों की टिप्पणियों का संग्रह है। इन व्याख्यानों में उन्होंने विविध महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर अपने मौलिक विचार प्रकट किये हैं; उदाहरणार्थ—भक्तियोग, कर्मयोग, कला, ज्ञानयोग, भाषा, संन्यासी और गृहस्थ, नियम और मुक्ति, आदि-आदि। यदि भारत स्वामीजी के इन जीवनप्रद विचारों द्वारा अपने को अनुप्राणित कर सके तो निश्चय ही वह अपनी अतीत गौरव-गरिमा का पुनर्लाभ कर सकेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं।
हम डॉ. महादेवप्रसादजी शर्मा, एम.ए., डी. लिट्., के बड़े आभारी हैं, जिन्होंने मूल अंग्रेजी से प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद किया है। भाषा एवं भाव दोनों ही दृष्टिकोण से उनका यह कार्य सफल रहा है।
हमारा पूर्ण विश्वास है कि आज, जब हम नव-भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए कमर कसे हुए हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर स्वामीजी के ये उद्बोधक एवं रचनात्मक विचार अत्यन्त उपादेय सिद्ध होंगे।
प्रकाशक
विविध प्रसंग
1
कर्मयोग
मानसिक और भौतिक सभी विषयों से आत्मा को प्रथक कर लेना ही हमारा लक्ष्य
है। इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आत्मा देखती है कि वह सर्वदा ही
एकाकी है और उसे सुखी बनाने के लिये अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। जब तक
अपने को सुखी बनाने के लिये हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है, तब तक हम
गुलाम है। जब ‘पुरुष’ जान लेता है कि वह मुक्त है,
उसे अपनी
पूर्णता के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं एवं यह प्रकृति नितान्त
अनावश्यक है, तब कैवल्य लाभ हो जाता है।
मनुष्य चाँदी के चन्द टुकड़ों के पीछे दौड़ता रहता है और उनकी प्राप्ति के लिए अपने एक सजातीय को भी धोखा देने में नहीं हिचकता; पर यदि वह स्वयं पर नियंत्रण रखे तो कुछ ही वर्षों में अपने चरित्र का ऐसा सुन्दर विकास कर सकता है कि यदि वह चाहे तो लाखों रुपये उसके पास आ जाएँ। तब वह अपनी इच्छा-शक्ति से जगत् का परिचालन कर सकता है। किन्तु हम कितने निर्बुद्ध हैं !
अपनी भूलों को संसार को बतलाते फिरने से क्या लाभ ? इस तरह उनमें सुधार तो हो नहीं सकता। अपनी करनी का फल तो सब को भुगतना ही पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं कि भविष्य में अधिक अच्छा काम करें। बली और शक्तिमान के साथ ही संसार की सहानुभूति रहती है।
केवल वही कर्म, जो निष्काम लोक-कल्याण की भावना से किया जाता है, बन्धन का कारण नहीं होता।
किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या नीचा काम करता है, वह केवल इसी कारण ऊँचा काम करने वाले की अपेक्षा छोटा या हीन नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए, पर यह देखना चाहिए कि वह कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्यों को करने की उसकी शक्ति और तरीके में होती है। एक मोची, जो कि कम से कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो दिन भर थोथी बकवास किया करता है।
प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य—निष्ठा भगवत्पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है; बुद्ध जीवों की भ्रान्त अज्ञानतिमिराच्छन्न आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति दिलाने में यह कर्तव्य-निष्ठा निश्चय ही एक बड़ी सहायक है।
जो कर्तव्य हमारे निकटतम हैं, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारु रूप से सम्पन्न करने से हमारी कार्य-शक्ति बढ़ती है; और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते है जब हमें जीवन और समाज के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।
प्रकृति का न्याय समान रूप से निर्मम और कठोर होता है। व्यवहार-कुशल व्यक्ति जीवन को न तो भला कहेगा और न बुरा।
प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं-न-कहीं एक विशाल ईमानदारी और सच्चाई छिपी रहती है, और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है। वह पूर्णतया स्वार्थहीन न रहा हो, पर वह उसकी ओर अग्रसर होता रहा था। यदि वह सम्पूर्ण रूप से स्वार्थहीन होता; तो उसकी सफलता वैसी ही महान् होती, जैसी बुद्ध या ईसा की। सर्वत्र निःस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर रहती है।
मानवजाति के महान् नेतागण उन लोगों की अपेक्षा, जो केवल मंच पर से व्याख्यान झाड़ा करते हैं, अधिक उच्च कोटि के हुआ करते हैं।
यदि हमें पवित्रता या अपवित्रता का अर्थ अहिंसा या हिंसा के रूप में लें, तब हम चाहे जितना प्रयत्न करें, हमारा कोई भी कार्य सम्पूर्णतया पवित्र या अपवित्र नहीं हो सकता। हम बिना किसी की हिंसा किये साँस तक नहीं ले सकते। भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी-न-किसी के मुँह से छीनकर खाते हैं; हमारा जीवन ही अन्य कुछ प्राणियों का अस्तित्व मिटा दे रहा है। चाहे मनुष्य हों या पशु अथवा छोटे-छोटे पौधे, पर कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी को हमारे लिये मिटना ही पड़ता है। ऐसा होने का कारण यह स्पष्ट ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। हम अनन्तकाल तक कर्म करते रहें, पर इस दुर्भेद्य जाल के बाहर न आ सकते। हम कर्म पर कर्म करते रहें, परन्तु कर्मों का कहीं अन्त न होगा।
जो मनुष्य प्रेम से अभिभूत होकर बिना किसी बन्धन के कार्य करता है, उसे कार्य-फल की कोई परवाह नहीं रहती। परन्तु जो गुलाम है, वह बिना कोड़ों की मार के कार्य नहीं कर सकता, और न नौकर, बिना वेतन के। ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक जीवन को ले लो। सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियाँ चाहता है या विरोध-प्रदर्शन है। यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी न दो, तो उसका उत्साह जाता रहता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। यही दास की तरह काम करना कहलाता है।
ऐसी परिस्थिति में, बदले में कुछ चाह रखना हमारा दूसरा स्वभाव-सा बन जाता है। इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है; ‘मैं तुम्हें यह देता हूँ और तुम मुझे वह दो’ यह भाव। ‘मैं कार्य के लिए ही कार्य करता हूँ’ यह कहना तो बहुत सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना बहुत कठिन है। मैं कर्म ही के लिए कर्म करनेवाले मनुष्य को देखने के लिए बीसों कोस सिर के बल जाने को तैयार हूँ। लोगों के काम में कहीं –न-कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। कहीं उसका रूप धन-प्राप्ति का होता है, तो कहीं आधिकार-प्राप्ति का और कहीं अन्य कोई लाभ। कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में स्वार्थ रहता अवश्य है। तुम मेरे मित्र हो, और मैं तुम्हारे साथ रह कर काम करना चाहता हूँ। यह सब दिखने में बड़ा अच्छा है; और प्रतिपल मैं अपनी सच्चाई की दुहाई भी दे सकता हूँ। पर ध्यान रखो, तुम्हें मेरे मत से मत मिलाकर काम करना होगा। यदि तुम मुझसे सहमत नहीं होते, तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता ! स्वार्थ के लिए सिद्धि के लिए इस प्रकार का काम दुःखदायी होता है। जहाँ हम अपने मन के स्वामी होकर कार्य करते हैं, केवल वही कर्म हमें अनाशक्ति और आनन्द प्रदान करता है।
एक बड़ा पाठ सीखने का यह है कि समस्त विश्व का मूल्य आँकने के लिए मैं ही मापदण्ड नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने भावों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जाति एवं देश के आदर्शों और रीति-रिवाजों की जाँच उन्हीं के विचारों, उन्हीं के मापदण्ड के अनुसार होनी चाहिए। अमेरिकावासी जिस वातावरण में रहते हैं, वही उनके रीतिरिवाजों का कारण है, और भारतीय प्रथाएँ भारतीयों के वातावरण की फलोत्पत्ति हैं; और इसी प्रकार चीन, जापान, इंग्लैण्ड तथा अन्य सब देशों के सम्बन्ध में भी यही बात है।
हम जिस स्थिति के योग्य हैं, वही हमें मिलती है।
मनुष्य चाँदी के चन्द टुकड़ों के पीछे दौड़ता रहता है और उनकी प्राप्ति के लिए अपने एक सजातीय को भी धोखा देने में नहीं हिचकता; पर यदि वह स्वयं पर नियंत्रण रखे तो कुछ ही वर्षों में अपने चरित्र का ऐसा सुन्दर विकास कर सकता है कि यदि वह चाहे तो लाखों रुपये उसके पास आ जाएँ। तब वह अपनी इच्छा-शक्ति से जगत् का परिचालन कर सकता है। किन्तु हम कितने निर्बुद्ध हैं !
अपनी भूलों को संसार को बतलाते फिरने से क्या लाभ ? इस तरह उनमें सुधार तो हो नहीं सकता। अपनी करनी का फल तो सब को भुगतना ही पड़ेगा। हम यही कर सकते हैं कि भविष्य में अधिक अच्छा काम करें। बली और शक्तिमान के साथ ही संसार की सहानुभूति रहती है।
केवल वही कर्म, जो निष्काम लोक-कल्याण की भावना से किया जाता है, बन्धन का कारण नहीं होता।
किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई छोटा या नीचा काम करता है, वह केवल इसी कारण ऊँचा काम करने वाले की अपेक्षा छोटा या हीन नहीं हो जाता। मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए, पर यह देखना चाहिए कि वह कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है। मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्यों को करने की उसकी शक्ति और तरीके में होती है। एक मोची, जो कि कम से कम समय में बढ़िया और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है, अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो दिन भर थोथी बकवास किया करता है।
प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य—निष्ठा भगवत्पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है; बुद्ध जीवों की भ्रान्त अज्ञानतिमिराच्छन्न आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति दिलाने में यह कर्तव्य-निष्ठा निश्चय ही एक बड़ी सहायक है।
जो कर्तव्य हमारे निकटतम हैं, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारु रूप से सम्पन्न करने से हमारी कार्य-शक्ति बढ़ती है; और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था की भी प्राप्ति कर सकते है जब हमें जीवन और समाज के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।
प्रकृति का न्याय समान रूप से निर्मम और कठोर होता है। व्यवहार-कुशल व्यक्ति जीवन को न तो भला कहेगा और न बुरा।
प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं-न-कहीं एक विशाल ईमानदारी और सच्चाई छिपी रहती है, और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है। वह पूर्णतया स्वार्थहीन न रहा हो, पर वह उसकी ओर अग्रसर होता रहा था। यदि वह सम्पूर्ण रूप से स्वार्थहीन होता; तो उसकी सफलता वैसी ही महान् होती, जैसी बुद्ध या ईसा की। सर्वत्र निःस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर रहती है।
मानवजाति के महान् नेतागण उन लोगों की अपेक्षा, जो केवल मंच पर से व्याख्यान झाड़ा करते हैं, अधिक उच्च कोटि के हुआ करते हैं।
यदि हमें पवित्रता या अपवित्रता का अर्थ अहिंसा या हिंसा के रूप में लें, तब हम चाहे जितना प्रयत्न करें, हमारा कोई भी कार्य सम्पूर्णतया पवित्र या अपवित्र नहीं हो सकता। हम बिना किसी की हिंसा किये साँस तक नहीं ले सकते। भोजन का प्रत्येक ग्रास हम किसी-न-किसी के मुँह से छीनकर खाते हैं; हमारा जीवन ही अन्य कुछ प्राणियों का अस्तित्व मिटा दे रहा है। चाहे मनुष्य हों या पशु अथवा छोटे-छोटे पौधे, पर कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी को हमारे लिये मिटना ही पड़ता है। ऐसा होने का कारण यह स्पष्ट ही है कि कर्म द्वारा पूर्णता कभी नहीं प्राप्त की जा सकती। हम अनन्तकाल तक कर्म करते रहें, पर इस दुर्भेद्य जाल के बाहर न आ सकते। हम कर्म पर कर्म करते रहें, परन्तु कर्मों का कहीं अन्त न होगा।
जो मनुष्य प्रेम से अभिभूत होकर बिना किसी बन्धन के कार्य करता है, उसे कार्य-फल की कोई परवाह नहीं रहती। परन्तु जो गुलाम है, वह बिना कोड़ों की मार के कार्य नहीं कर सकता, और न नौकर, बिना वेतन के। ऐसा ही समस्त जीवन में है। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक जीवन को ले लो। सार्वजनिक सभा में भाषण देने वाला या तो कुछ तालियाँ चाहता है या विरोध-प्रदर्शन है। यदि तुम इन दोनों में से उसे कुछ भी न दो, तो उसका उत्साह जाता रहता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। यही दास की तरह काम करना कहलाता है।
ऐसी परिस्थिति में, बदले में कुछ चाह रखना हमारा दूसरा स्वभाव-सा बन जाता है। इसके बाद है नौकर का काम, जो किसी वेतन की अपेक्षा करता है; ‘मैं तुम्हें यह देता हूँ और तुम मुझे वह दो’ यह भाव। ‘मैं कार्य के लिए ही कार्य करता हूँ’ यह कहना तो बहुत सरल है, पर इसे पूरा कर दिखाना बहुत कठिन है। मैं कर्म ही के लिए कर्म करनेवाले मनुष्य को देखने के लिए बीसों कोस सिर के बल जाने को तैयार हूँ। लोगों के काम में कहीं –न-कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। कहीं उसका रूप धन-प्राप्ति का होता है, तो कहीं आधिकार-प्राप्ति का और कहीं अन्य कोई लाभ। कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में स्वार्थ रहता अवश्य है। तुम मेरे मित्र हो, और मैं तुम्हारे साथ रह कर काम करना चाहता हूँ। यह सब दिखने में बड़ा अच्छा है; और प्रतिपल मैं अपनी सच्चाई की दुहाई भी दे सकता हूँ। पर ध्यान रखो, तुम्हें मेरे मत से मत मिलाकर काम करना होगा। यदि तुम मुझसे सहमत नहीं होते, तो मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता ! स्वार्थ के लिए सिद्धि के लिए इस प्रकार का काम दुःखदायी होता है। जहाँ हम अपने मन के स्वामी होकर कार्य करते हैं, केवल वही कर्म हमें अनाशक्ति और आनन्द प्रदान करता है।
एक बड़ा पाठ सीखने का यह है कि समस्त विश्व का मूल्य आँकने के लिए मैं ही मापदण्ड नहीं हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने भावों के अनुसार होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक जाति एवं देश के आदर्शों और रीति-रिवाजों की जाँच उन्हीं के विचारों, उन्हीं के मापदण्ड के अनुसार होनी चाहिए। अमेरिकावासी जिस वातावरण में रहते हैं, वही उनके रीतिरिवाजों का कारण है, और भारतीय प्रथाएँ भारतीयों के वातावरण की फलोत्पत्ति हैं; और इसी प्रकार चीन, जापान, इंग्लैण्ड तथा अन्य सब देशों के सम्बन्ध में भी यही बात है।
हम जिस स्थिति के योग्य हैं, वही हमें मिलती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book