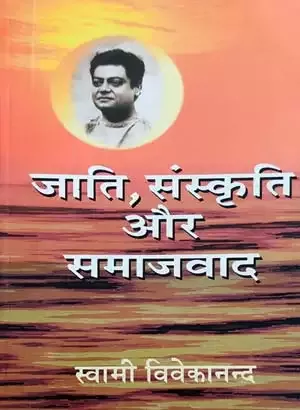|
विवेकानन्द साहित्य >> जाति संस्कृति और समाजवाद जाति संस्कृति और समाजवादस्वामी विवेकानन्द
|
333 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक जाति, संस्कृति और समाजवाद...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
(प्रथम संस्करण)
प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानन्द जी के, ‘जाति, संस्कृति और
समाजवाद’ पर मौलिक एवं उद्धोधक विचारों का संकलन है ये सब
स्वामी जी
के विभिन्न ग्रन्थों से चुनकर संग्रहित किये गये है इसमें स्वामीजी ने
हिन्दू जाति का सामाजिक व्यवस्थाओं की पाश्चात्यों की सामाजिक व्यवस्था के
साथ तुलना करते हुए उन्नति के रहस्य पर प्रकाश डाला है।
हमारी इस महान हिन्दू जाति का एक आदर्श रहा है और उस आदर्श की बुनियाद पर ही उसने अपनी समस्त जाति-व्यवस्था की तुलना की थी। यह पुराकाल में एक अत्यंत गौरवशाली संस्था रही है। पर आज हम देखते हैं कि वह नष्टगौरव हो धूल में मिली जा रही है। उसका वह आदर्श क्या था। जिसके बल पर वह युगों तक समस्त राष्ट्रों की अग्रणी बना रही है ? उसका पतन कैसे हुआ और आज की इस हीन दशा में कैसे पहुँची, इसका चित्र स्वामी जी ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अपनी मर्मस्पर्शी भाषा में अंकित किया है।
साथ ही स्वामी जी ने उस आदर्श तक पुनः उन्नति करने के उपायों का भी निर्देश किया है। स्वामीजी समाजवाद के प्रेमी थे पर वे चाहते थे कि उसका आधार यावत् अस्तित्व का आध्यात्मिक एकत्व हो। वे समाज में क्रान्ति चाहते थे, पर यह उसकी इच्छा नहीं थी कि वह हिंसात्मक हो अथवा विप्लव का रूप धारण करे वरन उनकी बुनियाद पारस्परिक प्रेम एवं अपनी संस्कृति की यथार्थ जानकारी हो। वे इससे सहमत नहीं थे कि समाज में समता स्थापित करने के लिए हम पाश्चात्यों का अनुसन्धान करें वरन् वे चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिकता द्वारा परिचालित हो विकास सदैव भीतर से ही होना चाहिए हमें जिसकी आवश्यकता है वह है भारत के महान आध्यात्मिक आदर्शवाद के साथ पाश्चात्यों के सामाजिक उन्नति विषय विचारों का संयोग।
हम पं. द्वारकानाथजी तिवारी, बी. ए. एल्.एल्.बी. के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अँगरेजी ग्रंथ से प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद किया है।
हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि आज, जब हिन्दू समाज के विभिन्न अंगों के बीच विवाद और कलह का ताण्डव नृत्य देख रहे हैं, स्वामीजी की भारत की जाति एवं संस्कृति सम्बन्धी यह गम्भीर विवेचना बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।
हमारी इस महान हिन्दू जाति का एक आदर्श रहा है और उस आदर्श की बुनियाद पर ही उसने अपनी समस्त जाति-व्यवस्था की तुलना की थी। यह पुराकाल में एक अत्यंत गौरवशाली संस्था रही है। पर आज हम देखते हैं कि वह नष्टगौरव हो धूल में मिली जा रही है। उसका वह आदर्श क्या था। जिसके बल पर वह युगों तक समस्त राष्ट्रों की अग्रणी बना रही है ? उसका पतन कैसे हुआ और आज की इस हीन दशा में कैसे पहुँची, इसका चित्र स्वामी जी ने अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अपनी मर्मस्पर्शी भाषा में अंकित किया है।
साथ ही स्वामी जी ने उस आदर्श तक पुनः उन्नति करने के उपायों का भी निर्देश किया है। स्वामीजी समाजवाद के प्रेमी थे पर वे चाहते थे कि उसका आधार यावत् अस्तित्व का आध्यात्मिक एकत्व हो। वे समाज में क्रान्ति चाहते थे, पर यह उसकी इच्छा नहीं थी कि वह हिंसात्मक हो अथवा विप्लव का रूप धारण करे वरन उनकी बुनियाद पारस्परिक प्रेम एवं अपनी संस्कृति की यथार्थ जानकारी हो। वे इससे सहमत नहीं थे कि समाज में समता स्थापित करने के लिए हम पाश्चात्यों का अनुसन्धान करें वरन् वे चाहते थे कि हम अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिकता द्वारा परिचालित हो विकास सदैव भीतर से ही होना चाहिए हमें जिसकी आवश्यकता है वह है भारत के महान आध्यात्मिक आदर्शवाद के साथ पाश्चात्यों के सामाजिक उन्नति विषय विचारों का संयोग।
हम पं. द्वारकानाथजी तिवारी, बी. ए. एल्.एल्.बी. के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक अँगरेजी ग्रंथ से प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद किया है।
हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि आज, जब हिन्दू समाज के विभिन्न अंगों के बीच विवाद और कलह का ताण्डव नृत्य देख रहे हैं, स्वामीजी की भारत की जाति एवं संस्कृति सम्बन्धी यह गम्भीर विवेचना बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।
प्रकाशक
जाति, संस्कृति और समाजवाद
1
पृष्ठभूमि
गिरिराज हिमालय के चिरशुभ्र हिमाच्छादित शिखरों से तीव्र वेग से फूटकर
निकलनेवाले कितने झरने एवं गरजते हुए जल-प्रपात, कितने बरफीले नाले और
सततप्रवाही नदियाँ एक साथ मिलकर विशाल सुर-सरिता गंगाजी के रूप में
प्रवाहित होती हुई समुद्र की ओर भंयकर वेग से दौड़ती हैं ! इसी प्रकार,
अगणित सन्तों के हृदय से तथा विभिन्न भू-भागों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों
के मस्तिष्क से उत्पन्न हुए कितने प्रकार के भावों तथा विचारों एवं
शक्तिप्रवाहों से उच्चतर मानवी कार्यों के प्रदर्शित क्षेत्र, कर्मभूमि
भारत को पहले से ही व्याप्त कर रखा है !
सचमुच, भारत विभिन्न मानववंशों का मानो एक संग्राहालय ही है ! नर और वानर में सम्बन्ध स्थापित करनेवाला जो एक अस्थि-कंकाल हाल ही में सुमात्रा में पाया गया है, वह शोध करने पर सम्भवताः, यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ प्रागैतिहासिक के पाषाण-निर्मित द्वार-प्रकारों (Dolmens) का अभाव नहीं। चकमक के औजार तो प्रायः कहीं भी खोदकर निकाले जा सकते हैं. ....फिर, ऐतिहासिक काल के नेग्रिटोकोलेरियन (Negrito-Kolarian), द्राविड़ तथा आर्य मानववंश भी यहां पाये जाते हैं। इनके साथ समय-समय पर प्रायः समस्त ज्ञान एवं बहुत से आज भी अज्ञात मानव-वंशों का किसी अंश में सम्मिश्रण होता रहा है। .....उफनती उबलती, संघर्ष करती और सतत रूप बदलती हुई तथा ऊपरी सतह तक उठकर, फैलकर, छोटी-छोटी लहरों को मिलाकर पुनः शान्त हुई इन विभिन्न मानव-वंशरूपी तरंगों से बना हुआ मानवता का महासागर-यही है भारतवर्ष का इतिहास।
इन भिन्न-भिन्न मानव–वंशों के संयोग से हमारे वर्तंमान समाजों, रीतियों और रूढ़ियों का विकास होना प्रारम्भ हुआ। नये विचार उत्पन्न होते गये और नये विज्ञानों का बीजारोपण होने लगा। एक श्रेणी के मनुष्य हस्तकौशल या बौद्धिक श्रम द्वारा उपयोग और आराम की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनाने लगे, तथा दूसरे वर्ग के मनुष्यों ने उनके संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया, और वे सब इन वस्तुओं का विनिमय करने लगे। तब ऐसा हुआ कि जो लोग बहुत चतुर थे, उन्होंने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य अपने ऊपर ले लिया, और वे इस कार्य में पारिश्रमिक शुल्क के बहाने लाभ का अधिकांश स्वयं ही लेने लगे। एक ने भूमि को जोतकर खेती की, दूसरे ने उसकी पैदावारी को लूट-पाट से बचाने के लिए उसकी रखवाली की, तीसरे ने उस पैदावारी को दूसरी जगह पहुँचाया और चौथे ने उसे खरीद लिया। खेती करनेवाले को लगभग कुछ नहीं मिला; ऱखवाली करनेवाला जितना ले सका, बलपूर्वक ले गया, बाजार में लानेवाले व्यापारी ने उसमें से प्रमुख भाग ले लिया और खरीददार को उन वस्तुओं के लिए बेहिसाब दाम देना पड़ा, जिसके भार के कारण उसे कष्ट भुगतना पड़ा ! रखवाली करनेवाला राजा कहाने लगा; वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जानेवाला व्यापारी बना। इन दोनों ने उत्पन्न तो कुछ भी नहीं किया, पर तो भी उन्होंने उन वस्तुओं का उत्तमांश छीन लिया। कृषक के श्रम और मजदूरी के फलों का अत्यधिक लाभ उठाकर वे स्वयं तो मोटे-ताजे बन गये, और बेचारा कृषक, जिसने सब वस्तुओं को उत्पन्न किया, भूखों मरने लगा और ईश्वर से सहायता माँगने लगा।
अब, कालक्रम से समस्याएँ जटिल होती चलीं और ग्रन्थियों पर ग्रन्थियों की वृद्धि हो गयी। बस इसी उलझन और गुत्थियों के जाल से हमारे वर्तमान जटिल समाज का विकास हुआ है। अतीत आचार के चिन्ह आज भी बने हुए हैं, और पूर्णतया मिटते नहीं है।
एशिया की सम्पूर्ण सभ्यता का विकास प्रथमतः बड़ी नदियों के समीप के मैदानों और उपजाऊ भूमियों में-गंगा, यांगसीकियांग और यूफ्रेटिज नदियों के कछारों में-हुआ। इन सभ्यताओं का मूल आधार कृषिकर्म ही है, और इन सब में दैवी प्रकृति की प्रधानता है। एतद्विपरीत, अधिकांश यूरोपीय सभ्यता का उद्भव पर्वत-प्रदेशों या समुद्र-तटों में हुआ है-जल और स्थल में लूटमार ही सभ्यता का आधार है; उसमें आसुरी प्रकृति की प्रधानता है।
यूरोपीय सभ्यता की तुलना उस वस्त्र खण्ड से की जा सकती है, जो इन उपादानों से बना है–उसे बुनने का ‘करघा’ समुद्रतट का विस्तृत समशीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश है; उसकी ‘रूई’ विभिन्न जातियों की वर्णसंकरता से उत्पन्न प्रबल युद्धप्रिय जाति है; ताना अपने शरीर और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध. है,.... और उसका ‘बाना’ वाणिज्य हैं उस सभ्यता का साधन तलवार है; उसके सहायक और शक्ति; और उसका उद्देश्य ऐहिक और पारलौकिक सुखोपभोग है।
सचमुच, भारत विभिन्न मानववंशों का मानो एक संग्राहालय ही है ! नर और वानर में सम्बन्ध स्थापित करनेवाला जो एक अस्थि-कंकाल हाल ही में सुमात्रा में पाया गया है, वह शोध करने पर सम्भवताः, यहाँ भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ प्रागैतिहासिक के पाषाण-निर्मित द्वार-प्रकारों (Dolmens) का अभाव नहीं। चकमक के औजार तो प्रायः कहीं भी खोदकर निकाले जा सकते हैं. ....फिर, ऐतिहासिक काल के नेग्रिटोकोलेरियन (Negrito-Kolarian), द्राविड़ तथा आर्य मानववंश भी यहां पाये जाते हैं। इनके साथ समय-समय पर प्रायः समस्त ज्ञान एवं बहुत से आज भी अज्ञात मानव-वंशों का किसी अंश में सम्मिश्रण होता रहा है। .....उफनती उबलती, संघर्ष करती और सतत रूप बदलती हुई तथा ऊपरी सतह तक उठकर, फैलकर, छोटी-छोटी लहरों को मिलाकर पुनः शान्त हुई इन विभिन्न मानव-वंशरूपी तरंगों से बना हुआ मानवता का महासागर-यही है भारतवर्ष का इतिहास।
इन भिन्न-भिन्न मानव–वंशों के संयोग से हमारे वर्तंमान समाजों, रीतियों और रूढ़ियों का विकास होना प्रारम्भ हुआ। नये विचार उत्पन्न होते गये और नये विज्ञानों का बीजारोपण होने लगा। एक श्रेणी के मनुष्य हस्तकौशल या बौद्धिक श्रम द्वारा उपयोग और आराम की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनाने लगे, तथा दूसरे वर्ग के मनुष्यों ने उनके संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया, और वे सब इन वस्तुओं का विनिमय करने लगे। तब ऐसा हुआ कि जो लोग बहुत चतुर थे, उन्होंने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य अपने ऊपर ले लिया, और वे इस कार्य में पारिश्रमिक शुल्क के बहाने लाभ का अधिकांश स्वयं ही लेने लगे। एक ने भूमि को जोतकर खेती की, दूसरे ने उसकी पैदावारी को लूट-पाट से बचाने के लिए उसकी रखवाली की, तीसरे ने उस पैदावारी को दूसरी जगह पहुँचाया और चौथे ने उसे खरीद लिया। खेती करनेवाले को लगभग कुछ नहीं मिला; ऱखवाली करनेवाला जितना ले सका, बलपूर्वक ले गया, बाजार में लानेवाले व्यापारी ने उसमें से प्रमुख भाग ले लिया और खरीददार को उन वस्तुओं के लिए बेहिसाब दाम देना पड़ा, जिसके भार के कारण उसे कष्ट भुगतना पड़ा ! रखवाली करनेवाला राजा कहाने लगा; वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जानेवाला व्यापारी बना। इन दोनों ने उत्पन्न तो कुछ भी नहीं किया, पर तो भी उन्होंने उन वस्तुओं का उत्तमांश छीन लिया। कृषक के श्रम और मजदूरी के फलों का अत्यधिक लाभ उठाकर वे स्वयं तो मोटे-ताजे बन गये, और बेचारा कृषक, जिसने सब वस्तुओं को उत्पन्न किया, भूखों मरने लगा और ईश्वर से सहायता माँगने लगा।
अब, कालक्रम से समस्याएँ जटिल होती चलीं और ग्रन्थियों पर ग्रन्थियों की वृद्धि हो गयी। बस इसी उलझन और गुत्थियों के जाल से हमारे वर्तमान जटिल समाज का विकास हुआ है। अतीत आचार के चिन्ह आज भी बने हुए हैं, और पूर्णतया मिटते नहीं है।
एशिया की सम्पूर्ण सभ्यता का विकास प्रथमतः बड़ी नदियों के समीप के मैदानों और उपजाऊ भूमियों में-गंगा, यांगसीकियांग और यूफ्रेटिज नदियों के कछारों में-हुआ। इन सभ्यताओं का मूल आधार कृषिकर्म ही है, और इन सब में दैवी प्रकृति की प्रधानता है। एतद्विपरीत, अधिकांश यूरोपीय सभ्यता का उद्भव पर्वत-प्रदेशों या समुद्र-तटों में हुआ है-जल और स्थल में लूटमार ही सभ्यता का आधार है; उसमें आसुरी प्रकृति की प्रधानता है।
यूरोपीय सभ्यता की तुलना उस वस्त्र खण्ड से की जा सकती है, जो इन उपादानों से बना है–उसे बुनने का ‘करघा’ समुद्रतट का विस्तृत समशीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश है; उसकी ‘रूई’ विभिन्न जातियों की वर्णसंकरता से उत्पन्न प्रबल युद्धप्रिय जाति है; ताना अपने शरीर और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध. है,.... और उसका ‘बाना’ वाणिज्य हैं उस सभ्यता का साधन तलवार है; उसके सहायक और शक्ति; और उसका उद्देश्य ऐहिक और पारलौकिक सुखोपभोग है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book