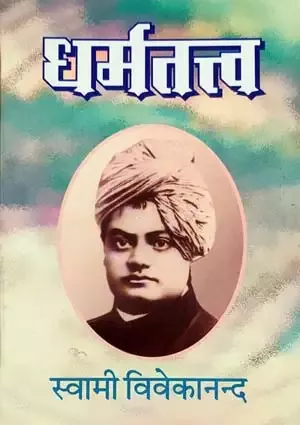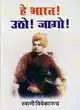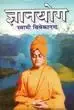|
विवेकानन्द साहित्य >> धर्मतत्त्व धर्मतत्त्वस्वामी विवेकानन्द
|
143 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है पुस्तक धर्मतत्त्व...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्राक्कथन
‘धर्मतत्त्व’ यह पुस्तक प्रकाशित करते हमें आनन्द हो रहा है
प्रस्तुत पुस्तक में स्वामी विवेकानन्द जी के कुछ चुने हुए व्याख्यानों
एवं प्रवचनों का संग्रह पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया गया है। धर्म के
अन्तिम लक्ष्य आत्मज्ञान में स्वयं प्रतिष्ठित हो स्वामीजी ने जो धर्म
सम्बन्धी वक्तृताएँ दी, वे स्वतः सिद्ध दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति पर
आधारित थीं और इसलिए उनके शब्दों का साधारण महत्त्व है। प्रस्तुत पुस्तक
में स्वामी जी का कथन है कि मोक्ष अथवा भगवत्प्राप्ति ही समस्त धर्मों का
एकमात्र अन्तिम ध्येय है तथा विधि-अनुष्ठान, ग्रन्थ, मतमान्तर आदि धर्म के
गौण अंग हैं।
अतः केवल इन्हीं में न उलझकर उनकी सहायता से धर्म के अन्तिम लक्ष्य पर पहुंचना ही धर्म का सारतत्त्व है। ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान- ये इस लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न उपाय हैं। इन सभी उपायों का विवेचन करते हुए प्रस्तुत पुस्तक में स्वामीजी ने दर्शाया है कि साधक को किन गुणों को आत्मसात् करना अनिवार्य है, साथ ही अत्यन्त युक्तियक्त शब्दों द्वारा यह भी बतलाया है कि समस्त विभिन्न धर्म उसी एकमात्र ध्येय, आत्मज्ञान अथवा ईश्वरप्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यही तथ्य ध्यान में रखते हुए यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार वास्तविक आन्तरिकता से धर्मसाधना करे तो संसार के सभी धार्मिक एवं साम्प्रदायिक द्वन्द्व मिट जाएँगे। पुस्तक के अध्ययन के उपरान्त पाठकगण स्वयं यह देखेंगे कि यथार्थ धर्मतत्त्व को जानकर तदनुसार जीवन को ढालना ही व्यक्ति के अपने निजी जीवन में, साथ विश्व में, शान्ति स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है।
पुस्तक में संगृहीत व्याख्यान एवं प्रवचन अद्वैत आश्रम, मायावती द्वारा प्रकाशित ‘विवेकानन्द-साहित्य’ से संकलित किये गये हैं।
अतः केवल इन्हीं में न उलझकर उनकी सहायता से धर्म के अन्तिम लक्ष्य पर पहुंचना ही धर्म का सारतत्त्व है। ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान- ये इस लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न उपाय हैं। इन सभी उपायों का विवेचन करते हुए प्रस्तुत पुस्तक में स्वामीजी ने दर्शाया है कि साधक को किन गुणों को आत्मसात् करना अनिवार्य है, साथ ही अत्यन्त युक्तियक्त शब्दों द्वारा यह भी बतलाया है कि समस्त विभिन्न धर्म उसी एकमात्र ध्येय, आत्मज्ञान अथवा ईश्वरप्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यही तथ्य ध्यान में रखते हुए यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार वास्तविक आन्तरिकता से धर्मसाधना करे तो संसार के सभी धार्मिक एवं साम्प्रदायिक द्वन्द्व मिट जाएँगे। पुस्तक के अध्ययन के उपरान्त पाठकगण स्वयं यह देखेंगे कि यथार्थ धर्मतत्त्व को जानकर तदनुसार जीवन को ढालना ही व्यक्ति के अपने निजी जीवन में, साथ विश्व में, शान्ति स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है।
पुस्तक में संगृहीत व्याख्यान एवं प्रवचन अद्वैत आश्रम, मायावती द्वारा प्रकाशित ‘विवेकानन्द-साहित्य’ से संकलित किये गये हैं।
प्रकाशक
धर्मतत्व
धर्म की आवश्यकता
(लन्दन में दिया हुआ व्याख्यान)
मानवजाति के भाग्यनिर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही
हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होनेवाली शक्ति से अधिक
महत्त्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं न कहीं
यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है, तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को
संगठित करनेवाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी
जानते हैं कि धार्मिक एकता का सम्बन्ध प्रायः जातिगत, जलवायुगत तथा
वंशानुगति एकता के सम्बन्धों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह सर्वविदित
तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजनेवाले तथा धर्म में विश्वास करनेवाले लोग जिस
दृढ़ता और शक्ति से एक–दूसरे का साथ देते हैं, वह एक ही वंश
के लोगों की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता।
धर्म
के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। अब हमें जितने
प्राचीन धर्मों का ज्ञान है वे सब एक यह दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक
हैं, मानो उनका उद्भव मानव-मस्तिष्क से नहीं बल्कि उस स्रोत से हुआ है, जो
उनके बाहर है।
आधुनिक विद्वान दो सिद्धान्तों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मामूलक सिद्धान्त और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धान्त। पहले सिद्धान्त के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ; दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत सम्बन्धियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है, और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ।
मिस्र, बेबिलोन, चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मसम्बन्धी धारणा द्वित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव-शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है। किन्तु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है, जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा है कि इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुँची, तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्टतः पितर-पूजा है।
बेबिलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिन्दुओं में भी इस पितर-पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनमें धर्म का आधार पितर-पूजा ही है और यह सब अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई भी धर्म प्रचलित माना जा सकता है, तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर-पूजा से विकसित माननेवालों का आधार काफी सुदृढ़ है।
किन्तु कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जो प्राचीन आर्य-साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर-पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रन्थों में इसकी किंचित् चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान् उसमें प्रकृति-पूजा के ही चिन्ह पाते हैं। जो प्रस्तुत दृश्य के परे हैं, इसकी एक झाँकी पाने के लिए मानव-मन आकुल प्रतीत होता है। ऊषा, सन्ध्या, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियाँ, उसका सौन्दर्य-इन सब मानव-मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा।
इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में वैयक्तिक गुणों का आरोपण करना शुरू किया। उन्होंने उनमें आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की, जो कभी सुन्दर और कभी इन्द्रियातीत होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्तिगतरूप दिया गया, या नहीं दिया गया, किन्तु उनका अन्त उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के सम्बन्ध में भी हुई, उनके तो सम्पूर्ण पुराणोपाख्यान अमूर्त प्रकृति-पूजा ही है। और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैन्डिनेविया के निवासियों एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत माननेवालों का भी पक्ष काफी प्रबल हो जाता है।
यद्यपि ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी लगते हैं, किन्तु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं ‘इन्द्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष’ मानता हूँ। एक ओर मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है। मृतकों की प्रेतात्माओं को ढ़ूँढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर जो भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इन्द्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इन्द्रियों से सन्तुष्ट नहीं है वह इनसे परे भी जाना चाहता है।
इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिलकुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झाँकी स्वप्न में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था ! हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले स्वप्न और जाग्रत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वप्नवास्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं !
अतः इसमें क्या आश्चर्य यदि मनुष्य हठात् यह निष्कर्ष निकाल ले कि शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी ? मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित हुआ मनुष्य ऊँचे से ऊँचे विचारों तक पहुँच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृतावस्था से सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्नावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृतावस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है।
आधुनिक विद्वान दो सिद्धान्तों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मामूलक सिद्धान्त और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धान्त। पहले सिद्धान्त के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ; दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म का प्रारम्भ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत सम्बन्धियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है, और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ।
मिस्र, बेबिलोन, चीन तथा अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से ऐसे स्पष्ट चिन्हों का पता चलता है, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवासियों की आत्मसम्बन्धी धारणा द्वित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव-शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है। किन्तु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है, जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मिस्रवासियों में मृत शरीर सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया, मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा है कि इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुँची, तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्टतः पितर-पूजा है।
बेबिलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिन्दुओं में भी इस पितर-पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के सम्बन्ध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनमें धर्म का आधार पितर-पूजा ही है और यह सब अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई भी धर्म प्रचलित माना जा सकता है, तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर-पूजा से विकसित माननेवालों का आधार काफी सुदृढ़ है।
किन्तु कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जो प्राचीन आर्य-साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर-पूजा के उदाहरण सर्वत्र ही देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रन्थों में इसकी किंचित् चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सब से प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान् उसमें प्रकृति-पूजा के ही चिन्ह पाते हैं। जो प्रस्तुत दृश्य के परे हैं, इसकी एक झाँकी पाने के लिए मानव-मन आकुल प्रतीत होता है। ऊषा, सन्ध्या, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियाँ, उसका सौन्दर्य-इन सब मानव-मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा।
इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में वैयक्तिक गुणों का आरोपण करना शुरू किया। उन्होंने उनमें आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की, जो कभी सुन्दर और कभी इन्द्रियातीत होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्तिगतरूप दिया गया, या नहीं दिया गया, किन्तु उनका अन्त उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के सम्बन्ध में भी हुई, उनके तो सम्पूर्ण पुराणोपाख्यान अमूर्त प्रकृति-पूजा ही है। और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैन्डिनेविया के निवासियों एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत माननेवालों का भी पक्ष काफी प्रबल हो जाता है।
यद्यपि ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी लगते हैं, किन्तु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं ‘इन्द्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष’ मानता हूँ। एक ओर मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है। मृतकों की प्रेतात्माओं को ढ़ूँढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर जो भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इन्द्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इन्द्रियों से सन्तुष्ट नहीं है वह इनसे परे भी जाना चाहता है।
इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिलकुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झाँकी स्वप्न में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था ! हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले स्वप्न और जाग्रत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वप्नवास्था में भी जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं !
अतः इसमें क्या आश्चर्य यदि मनुष्य हठात् यह निष्कर्ष निकाल ले कि शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी ? मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित हुआ मनुष्य ऊँचे से ऊँचे विचारों तक पहुँच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृतावस्था से सत्य सिद्ध नहीं होते और स्वप्नावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृतावस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book