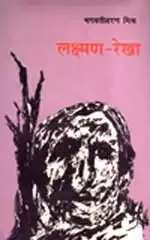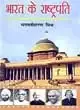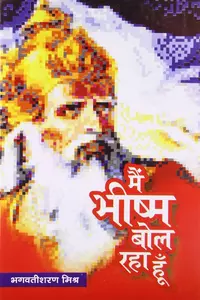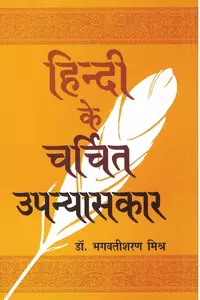|
पर्यावरणीय >> लक्ष्मण-रेखा लक्ष्मण-रेखाभगवतीशरण मिश्र
|
448 पाठक हैं |
||||||
प्रतिष्ठित उपन्यासकार भगवतीशरण मिश्र का यह ‘लक्ष्मण-रेखा’ उपन्यास ‘पर्यावरण’ की समस्या पर केन्द्रित है : सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
झील, नदी, पेड़, पहाड़ी, वन, समाज, राजनीति, जीवन; और इन सब पर तना हुआ
प्रदूषण का काला साया-लगभग इन सब-कुछ की कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई
लक्ष्मण-रेखा तो होती ही है। प्रेम की भी होती है, शायद मानवीय मूल्यों के
दायरे में सबसे ज्यादा।—और जब कोई समर्थ कथाकार इन तमाम रेखाओं
को
बार-बार उकेरता है, उनका जीवंत साक्षात्कार कराता है और तेज धारदार
प्रश्न-चिहन् भी लगाता है, तब एक मर्मस्पर्शी औपन्यासिक कृति की रचना सहज
ही हो जाती है—जैसे यह उपन्यास
‘लक्ष्मण-रेखा’ जो आज के
बेचैन और संवेदनहीन समाज के सामने स्वयं एक प्रश्न-चिह्न है।
प्रतिष्ठित उपन्यासकार भगवतीशरण मिश्र का यह ‘लक्ष्मण-रेखा’ उपन्यास कहने को तो ‘पर्यावरण’ की समस्या पर केन्द्रित है। लेकिन उपन्यास में प्रतिपाद्य यह पर्यावरण जितनी बाहरी है उतना ही भीतरी—बहुत भीतरी भी है। जाहिर है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण से मुक्ति पाने की आकांक्षा और जीवन के रंग-राग के तलाश की इस कथात्मक प्रक्रिया में ‘लक्ष्मण-रेखा’ उपन्यास का पाठक भी गम्भीर रूप से भागीदार बनेगा।
प्रतिष्ठित उपन्यासकार भगवतीशरण मिश्र का यह ‘लक्ष्मण-रेखा’ उपन्यास कहने को तो ‘पर्यावरण’ की समस्या पर केन्द्रित है। लेकिन उपन्यास में प्रतिपाद्य यह पर्यावरण जितनी बाहरी है उतना ही भीतरी—बहुत भीतरी भी है। जाहिर है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण से मुक्ति पाने की आकांक्षा और जीवन के रंग-राग के तलाश की इस कथात्मक प्रक्रिया में ‘लक्ष्मण-रेखा’ उपन्यास का पाठक भी गम्भीर रूप से भागीदार बनेगा।
अपनी बात
उपन्यास और कहानी के लिए किसी भूमिका की अनिवार्यता नहीं। वस्तुतः बिना
भूमिका के ही ये कृतियाँ भलीं क्योंकि कहीं भूल से मूल कथा की ओर इंगित भी
हो गया तो पुस्तक पढ़ने का सारा उत्साह ही समाप्त।
तो मैं यह गलती करने नहीं जा रहा। कथा रही अपनी जगह पर, यह भूमिका अपनी जगह।
वस्तुतः मुझे कथा को लेकर कुछ लेना-देना भी नहीं। उसकी वकालत करने मैं क्यों बैठूँ—मैं उसका स्रष्टा ? बोलना होगा तो वह स्वयं बोलेगी। अपनी पहचान गढ़ लेगी। हर पिता की यही आकांक्षा होती है कि उसकी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाय। पिता नामक जीवनधारी के नाम-यश की बैसाखी वह घुमा फेंके। हर कृति लेखक की संतान ही होती है। उसे वह बैसाखी नहीं थमाना चाहता।
तो यह व्याख्या नहीं है इस बात की कि यह कथा क्यों और कैसे लिखी गई, साथ ही इसकी भी कि यह क्यों और कैसे अत्यंत सरस, उपयोगी और उपन्यास की सारी विशेषताओं से संपन्न है। यह ऐसी होगी तो पाठक स्वयं उसके साक्षी बनकर खड़े हो जाएँगे जैसे वे अब तक मेरी सारी कृतियों के साथ करते रहे हैं। अतः एक तरह से यह उपक्रम पाठकों को साधुवाद देने का भी हुआ क्योंकि लेखक और पाठक अक्सर आमने-सामने नहीं हो पाते।
पाठकों के लिए अपने कृतज्ञता-ज्ञापन के पश्चात् मैं अपनी बात पर आऊँ जिसके लिए यह भूमिका गढ़नी पड़ी। मैं पुस्तक को लेकर नहीं, उसके नाम को लेकर कुछ अवश्य कहना चाहता हूँ।
पुस्तक में यह शब्द लक्ष्मण-रेखा कई बार आया है पर मात्र यही घटना इस शब्द को शीर्ष स्थान नहीं दिला देती, इसे शीर्षक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर देती।
शीर्षक वह, जो पुस्तक के मूल स्वर को पकड़ सके। उसके कथ्य की संपूर्णता को एक-दो शब्दों में ही समेट ले। अतः शीर्षक का चयन मेरे लिए सदा कृति के प्रस्तुतीकरण से अधिक कठिन रहा है। पुस्तक का मूल विषय अथवा यदि शास्त्रीय शब्दावली का सहारा लूँ तो प्रतिपाद्य, ‘पर्यावरण’ है। पर्यावरण की रक्षा की ओर, उसके प्रदूषण को नियंत्रित करने की ओर, विश्व के सभी बुद्धिजीवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।
यहीं पर आती है मेरी लक्ष्मण-रेखा। इतिहास-पुराण साक्षी हैं कि जब-जब मनुष्य ने इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास किया है, अनर्थ घटा है। लंकेश रावण ने इस रेखा को अतिक्रमित करने की भूल नहीं की होती तो एक स्वर्ण-नगरी भस्म नहीं हुई होती। एक घोर नर-संहार नहीं हुआ होता जिसमें लंका से नृ-वंश कुछ दिनों के लिए प्रायः निर्मूल ही नहीं हो गया होता।
द्रौपदी का चीर-हरण करने का दुस्साहस कर दुःशासन और दुर्योध्न ने इस लक्ष्मण-रेखा को पैरों तले रौंदने का प्रयास नहीं किया होता तो महाभारत नहीं घटता और यह राष्ट्र कुछ दिनों के लिए मरघट नहीं बन जाता।
औरंगजेब ने लक्ष्मण-रेखा की ऐसी-तैसी न की होती और हिंदुओं के मंदिरों, पूजा-घरों की ईंट-से-ईंट नहीं बजा दी होती, उन पर ‘जजिया’ नहीं लाद दी होती तो यमुना की धारा में सांप्रदायिक विद्वेष का वह विष नहीं घोल पाया होता जिसने आज तक दो संप्रदायों के मध्य एक स्वस्थ संबंध-बेली को कभी पनपने नहीं दिया।
अगर अंग्रेजों ने 1857 और 1942 में इस लक्ष्मण-रेखा को अपने बूटों के नीचे बुरी तरह मसली नहीं होती तो शायद न तो उनका प्रस्थान ही इस भूमि से इतना शीघ्र हुआ होता, न वे जाते-जाते हमारे मन–प्राणों में इतनी कड़वाहट ही भर जाते, जिससे हम अपने लाखों प्रयासों के बाद भी अब तक मुक्त होने में सफल नहीं हो पा रहे।
जनरल डायर ने अगर इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा की रक्षा की होती तो न होता ‘जलियाँवाला बाग कांड’ और न हो धोने पड़ते उसे अपने प्राणों से अपनी ही धरती पर हाथ।
आधुनिक इतिहास के पृष्ठ भी ऐसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं जिनका उल्लेख कर मैं स्वयं किसी लक्ष्मण-रेखा के अतिक्रमण की भूल नहीं करने जा रहा।
तो यह लक्ष्मण-रेखा आवश्यक है हर जगह खींचोगे, एक सीमा बाँधोगे जिसके आगे जाने का अर्थ, अनर्थ की संज्ञा पा सकता है ? समरों की सृष्टि कर सकता है, प्रदूषण का जनक हो सकता है, संबंधों को व्यर्थ और विषाक्त कर सकता है ?
व्यक्तिगत जीवन में यह अतिक्रमित रेखा मनुष्य को पशु की श्रेणी में ला पटक सकती है। आज के किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों ने अपने पारस्परिक संबंधों में इस लक्ष्मण-रेखा को धत्ता बताया है तो पूरा समाज ही सांस्कृतिक अवमूल्यन का आखेट हुआ है। उनका क्या बना-बिगड़ा है इसका लेखा-जोखा वे स्वयं कर लें। घोर प्रदूषण यहाँ भी पैदा हुआ है और हर प्रकार के प्रदूषण पर प्रश्न चिह्न लगाना ही इस पुस्तक का लक्ष्य होने के कारण, ‘लक्ष्मण-रेखा’ शीर्षक की सार्थकता को इस सर्वाधिक निद्यं प्रदूषण ने सार्थकता ही प्रदान की है। मानवीय मूल्यों को विघटन से बचाने का सर्वाधिक दायित्व नई पीढ़ी का ही है, अतः लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा-रक्षा उसका ही प्रथम दायित्व बनता है।
लक्ष्मण-रेखा का यही उल्लंघन पर्यावर्णीय-प्रदूषण का भी कारण बना है। कितना धुआँ उगलोगे अपने वाहनों से, फैक्ट्रियों से, रॉकेटों से ? यहाँ भी तो कोई लक्ष्मण-रेखा होनी चाहिए कि नहीं ?
कितने गंदे नालों का मुँह खोलोगे, कितना कचड़ा उगलोगे अपने कारखानों से गंगा-यमुना और अन्य नदियों के पेट में ? कितना अपेय बनाओगे पेय जल को ? कोई लक्ष्मण-रेखा तो होनी चाहिए यहाँ भी ?
और वन ? तुम्हारे प्राण-रक्षक ? तुम्हारे फेफड़ों में निरंतर प्राण-वायु फूँकने वाले ? तुम्हें शीतलता और शरणस्थली से लेकर फल-फूल के रूप में उदर-पूर्ति का साधन बनने वाले ? आदिवासियों, बनवासियों, गिरिजनों के अस्तित्व तो अस्तित्व उनकी संस्कृति के भी पोषक और प्रतीक ? कब तक काटोंगे इन्हें, कितना और कहाँ तक ? कोई लक्ष्मण-रेखा खीचोंगे कि नहीं जो प्रकृति के साथ तुम्हारे इस विवेकहीन व्यवहार पर अंकुश दे ?
तो यही है मेरी लक्ष्मण-रेखा। चाहे जातीय प्रदूषण हो, सामाजिक और सांस्कृतिक हो अथवा हो पर्यावर्णीय। इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा की रक्षा हो सके तो अब भी बहुत कुछ है जिसे विनष्ट होने से रोका जा सकता है।
पाठकों के प्रति आरंभ में ही आभार प्रकट किया। मेरी रचनाधर्मिता को जो निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं, इस अवसर पर उन्हें स्मरण नहीं करना कृतघ्नता होगी।
अंततः वाणी प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री अरुण माहेश्वरी को इसलिये प्रचुर साधुवाद कि बिना उनकी तत्परता के न तो यह पुस्तक इतना शीघ्र लिख पाती, न छप पाती।
अपने सभी जाने-अनजाने शुभेच्छुओं के प्रति एक बार पुनः श्रद्धा-निवेदन के साथ—
तो मैं यह गलती करने नहीं जा रहा। कथा रही अपनी जगह पर, यह भूमिका अपनी जगह।
वस्तुतः मुझे कथा को लेकर कुछ लेना-देना भी नहीं। उसकी वकालत करने मैं क्यों बैठूँ—मैं उसका स्रष्टा ? बोलना होगा तो वह स्वयं बोलेगी। अपनी पहचान गढ़ लेगी। हर पिता की यही आकांक्षा होती है कि उसकी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाय। पिता नामक जीवनधारी के नाम-यश की बैसाखी वह घुमा फेंके। हर कृति लेखक की संतान ही होती है। उसे वह बैसाखी नहीं थमाना चाहता।
तो यह व्याख्या नहीं है इस बात की कि यह कथा क्यों और कैसे लिखी गई, साथ ही इसकी भी कि यह क्यों और कैसे अत्यंत सरस, उपयोगी और उपन्यास की सारी विशेषताओं से संपन्न है। यह ऐसी होगी तो पाठक स्वयं उसके साक्षी बनकर खड़े हो जाएँगे जैसे वे अब तक मेरी सारी कृतियों के साथ करते रहे हैं। अतः एक तरह से यह उपक्रम पाठकों को साधुवाद देने का भी हुआ क्योंकि लेखक और पाठक अक्सर आमने-सामने नहीं हो पाते।
पाठकों के लिए अपने कृतज्ञता-ज्ञापन के पश्चात् मैं अपनी बात पर आऊँ जिसके लिए यह भूमिका गढ़नी पड़ी। मैं पुस्तक को लेकर नहीं, उसके नाम को लेकर कुछ अवश्य कहना चाहता हूँ।
पुस्तक में यह शब्द लक्ष्मण-रेखा कई बार आया है पर मात्र यही घटना इस शब्द को शीर्ष स्थान नहीं दिला देती, इसे शीर्षक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर देती।
शीर्षक वह, जो पुस्तक के मूल स्वर को पकड़ सके। उसके कथ्य की संपूर्णता को एक-दो शब्दों में ही समेट ले। अतः शीर्षक का चयन मेरे लिए सदा कृति के प्रस्तुतीकरण से अधिक कठिन रहा है। पुस्तक का मूल विषय अथवा यदि शास्त्रीय शब्दावली का सहारा लूँ तो प्रतिपाद्य, ‘पर्यावरण’ है। पर्यावरण की रक्षा की ओर, उसके प्रदूषण को नियंत्रित करने की ओर, विश्व के सभी बुद्धिजीवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।
यहीं पर आती है मेरी लक्ष्मण-रेखा। इतिहास-पुराण साक्षी हैं कि जब-जब मनुष्य ने इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रयास किया है, अनर्थ घटा है। लंकेश रावण ने इस रेखा को अतिक्रमित करने की भूल नहीं की होती तो एक स्वर्ण-नगरी भस्म नहीं हुई होती। एक घोर नर-संहार नहीं हुआ होता जिसमें लंका से नृ-वंश कुछ दिनों के लिए प्रायः निर्मूल ही नहीं हो गया होता।
द्रौपदी का चीर-हरण करने का दुस्साहस कर दुःशासन और दुर्योध्न ने इस लक्ष्मण-रेखा को पैरों तले रौंदने का प्रयास नहीं किया होता तो महाभारत नहीं घटता और यह राष्ट्र कुछ दिनों के लिए मरघट नहीं बन जाता।
औरंगजेब ने लक्ष्मण-रेखा की ऐसी-तैसी न की होती और हिंदुओं के मंदिरों, पूजा-घरों की ईंट-से-ईंट नहीं बजा दी होती, उन पर ‘जजिया’ नहीं लाद दी होती तो यमुना की धारा में सांप्रदायिक विद्वेष का वह विष नहीं घोल पाया होता जिसने आज तक दो संप्रदायों के मध्य एक स्वस्थ संबंध-बेली को कभी पनपने नहीं दिया।
अगर अंग्रेजों ने 1857 और 1942 में इस लक्ष्मण-रेखा को अपने बूटों के नीचे बुरी तरह मसली नहीं होती तो शायद न तो उनका प्रस्थान ही इस भूमि से इतना शीघ्र हुआ होता, न वे जाते-जाते हमारे मन–प्राणों में इतनी कड़वाहट ही भर जाते, जिससे हम अपने लाखों प्रयासों के बाद भी अब तक मुक्त होने में सफल नहीं हो पा रहे।
जनरल डायर ने अगर इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा की रक्षा की होती तो न होता ‘जलियाँवाला बाग कांड’ और न हो धोने पड़ते उसे अपने प्राणों से अपनी ही धरती पर हाथ।
आधुनिक इतिहास के पृष्ठ भी ऐसे असंख्य प्रमाणों से भरे हैं जिनका उल्लेख कर मैं स्वयं किसी लक्ष्मण-रेखा के अतिक्रमण की भूल नहीं करने जा रहा।
तो यह लक्ष्मण-रेखा आवश्यक है हर जगह खींचोगे, एक सीमा बाँधोगे जिसके आगे जाने का अर्थ, अनर्थ की संज्ञा पा सकता है ? समरों की सृष्टि कर सकता है, प्रदूषण का जनक हो सकता है, संबंधों को व्यर्थ और विषाक्त कर सकता है ?
व्यक्तिगत जीवन में यह अतिक्रमित रेखा मनुष्य को पशु की श्रेणी में ला पटक सकती है। आज के किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों ने अपने पारस्परिक संबंधों में इस लक्ष्मण-रेखा को धत्ता बताया है तो पूरा समाज ही सांस्कृतिक अवमूल्यन का आखेट हुआ है। उनका क्या बना-बिगड़ा है इसका लेखा-जोखा वे स्वयं कर लें। घोर प्रदूषण यहाँ भी पैदा हुआ है और हर प्रकार के प्रदूषण पर प्रश्न चिह्न लगाना ही इस पुस्तक का लक्ष्य होने के कारण, ‘लक्ष्मण-रेखा’ शीर्षक की सार्थकता को इस सर्वाधिक निद्यं प्रदूषण ने सार्थकता ही प्रदान की है। मानवीय मूल्यों को विघटन से बचाने का सर्वाधिक दायित्व नई पीढ़ी का ही है, अतः लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा-रक्षा उसका ही प्रथम दायित्व बनता है।
लक्ष्मण-रेखा का यही उल्लंघन पर्यावर्णीय-प्रदूषण का भी कारण बना है। कितना धुआँ उगलोगे अपने वाहनों से, फैक्ट्रियों से, रॉकेटों से ? यहाँ भी तो कोई लक्ष्मण-रेखा होनी चाहिए कि नहीं ?
कितने गंदे नालों का मुँह खोलोगे, कितना कचड़ा उगलोगे अपने कारखानों से गंगा-यमुना और अन्य नदियों के पेट में ? कितना अपेय बनाओगे पेय जल को ? कोई लक्ष्मण-रेखा तो होनी चाहिए यहाँ भी ?
और वन ? तुम्हारे प्राण-रक्षक ? तुम्हारे फेफड़ों में निरंतर प्राण-वायु फूँकने वाले ? तुम्हें शीतलता और शरणस्थली से लेकर फल-फूल के रूप में उदर-पूर्ति का साधन बनने वाले ? आदिवासियों, बनवासियों, गिरिजनों के अस्तित्व तो अस्तित्व उनकी संस्कृति के भी पोषक और प्रतीक ? कब तक काटोंगे इन्हें, कितना और कहाँ तक ? कोई लक्ष्मण-रेखा खीचोंगे कि नहीं जो प्रकृति के साथ तुम्हारे इस विवेकहीन व्यवहार पर अंकुश दे ?
तो यही है मेरी लक्ष्मण-रेखा। चाहे जातीय प्रदूषण हो, सामाजिक और सांस्कृतिक हो अथवा हो पर्यावर्णीय। इस लक्ष्मण-रेखा की मर्यादा की रक्षा हो सके तो अब भी बहुत कुछ है जिसे विनष्ट होने से रोका जा सकता है।
पाठकों के प्रति आरंभ में ही आभार प्रकट किया। मेरी रचनाधर्मिता को जो निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं, इस अवसर पर उन्हें स्मरण नहीं करना कृतघ्नता होगी।
अंततः वाणी प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री अरुण माहेश्वरी को इसलिये प्रचुर साधुवाद कि बिना उनकी तत्परता के न तो यह पुस्तक इतना शीघ्र लिख पाती, न छप पाती।
अपने सभी जाने-अनजाने शुभेच्छुओं के प्रति एक बार पुनः श्रद्धा-निवेदन के साथ—
भगवतीशरण मिश्र
लक्ष्मण-रेखा
एक
‘‘तुम्हारे जीवन में सूर्योदय हुआ
है।’’
—गीतिका विश्वम्भर की इस आकस्मिक उक्ति में उलझकर रह गई। जब
आसमान
में पूर्णिमा का चाँद सोलहों कलाओं से खिलखिलाता अपनी धवल रश्मियों से
नीचे की उपत्यका और वनस्पति-बोझिल पहाड़ियों को स्नात करता-इठलाता, आकाश
की ऊँचाइयों को एक अनुपम आश्वस्ति और आत्मविश्वास के साथ मापता जा रहा हो
उस समय सूर्योदय की बात बेतुकी नहीं थी क्या ?
‘‘तुमने सुना नहीं ?’’ विश्वम्भर उसके समीप आ गया था, ऐसा कि उसके शरीर से निस्सृत गंध गीतिका के कुछ अधिक ही संवेदनशील नासापुट आसानी से पकड़ सकते थे।
‘‘आज यह कैसी मोहक गंध तुम्हारे तन से निस्सृत हो रही है ?’’ उसने पूछा था और उसका मन किया था उसकी चाँदनी-भीगे हाथों को वह अपने दोनों हाथों में कस ले। पर वह ऐसा नहीं कर सकी। जानती थी, इसका वह बुरा मानेगा और सूर्योंदय से ही सही आरंभ उसकी बातचीत किसी असमय के सूर्यास्त-सी समाप्त हो जाएगी—जैसे भरी दोपहरी में सूर्य ग्रहण-ग्रस्त हो जाए।
‘‘आज फूलों की वादियों से जो लौटा हूँ। मेरा कार्य मुझे किन-किन वादियों-वनों में ले जाता है तुम्हें क्या पता ? वनैले फूलों की गंध है यह —अनछुई, अननुभूत।’’ विश्वम्भर ने उत्तर दिया।
नैनीताल था यह। नहीं, झील का अछोर विस्तार सामने नहीं था। एक पहाड़ी की चोटी पर ही खड़े थे वे। पास के एक डाकबंगले में जगह मिली थी। झील का पुराना आकर्षण तो अब वर्षों से तिरोहित होने लगा था। इसका पानी दिनों-दिन अपनी स्वच्छता खोता जा रहा था। एक हरीतिमा-सी उसमें घुलने लगी थी। यह अगल-बगल की पहाड़ियों का प्रभाव था क्या कि झील भी अपना रंग बदलने लगी थी ? नहीं, ऐसा कुछ नही था, गीतिका ने अपने इस प्रवास के दौरान एक बार अकेली ही झील के किनारे खड़ी-खड़ी सोचा था। उस दिन वह चाह कर भी विश्वम्भर को झील के किनारे तक नहीं खीच सकी थी।
‘‘तुम्हीं जाओ वहाँ, उस झील के पानी से मुझे अब उबकाई आती है। और जानती हो इसकी झील से पूरे नैनीताल को पानी पिलाते हैं और उसके लिए जल-शोधन के क्रम में पड़ने वाली क्रोमीन की मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। अब तो यह पानी इस दवा से इतना प्रदूषित हो गया है कि हम समतल-वासियों को यह रास ही नहीं आता।’’ उस दिन विश्वम्भर का पेट सचमुच खराब था। उसी दिन क्या, वह इस बार जब से नैनीताल आया है ‘आंटिबाइटिक्स’ की बैसाखियों के सहारे ही अपने अनियंत्रित हो आए उदर को नियंत्रित करता रहा है।
हाँ, उस दिन नैना देवी के मंदिर के सामने खड़ी झील के पानी को देखते हुए उसने सोचा था, क्योंकि दिनों-दिन ऐसा होता जा रहा है उसका रूप ? क्यों घुलता जा रहा है वनस्पतियों का रंग इसमें ? पर वनस्पतियाँ तो प्रायः निर्दोष होती है....जीवनदायिनी। इन्हीं में कोई संजीवनी भी कहीं होगी। इसी हिमालय से हनुमान ले गए थे उसे, लक्ष्मण की प्राण-रक्षा के लिए। यह पानी मात्र वनस्पतियों का रंग ही ग्रहण कर सका है, उनका गुण नहीं। इस पानी के रंग बदलने के कारण कुछ और हैं। उसकी दृष्टि उठी थी झील की दूसरी ओर की पहाड़ी से गिरते कई नालों की तरह जो अपनी गंदगी अबाध रूप से उड़ेलते जा रहे थे। नैनी में। बरसाती दिनों में तो हाहाकार करते ये कृतिम-अकृतमि नाले इसमें पता नहीं कितना काली-पीला मिट्टी और सड़े-गले पत्ते ला परोसते हैं ? और नैनीताल की बरसात भी क्या कुछ कम दिनों की होती है ? कभी-कभी मई के आरंभ में ही शुरु हो गई तो अगस्त के मध्य तक खिंची चली जाती है।
विश्म्भर ‘क्रोमीन’ द्वारा उसके जल के प्रदूषण की बात कर रहा था। वह कैसे भूल गया कि ‘क्रोमीन’ तो बाद में प्रदूषित करती है, इस नैनी के जल को वास्तविक प्रदूषण तो इसे हमारी उदासीनता ही प्रदान करती है। नालों से गिरते पानी को छोड़ भी दें तो ‘सीजन’ के दिनों में ताल के वक्ष पर तैरती अनेक नौकाओं में आसीतन अनेक हाथों से खाद्य सामग्रियों को वेष्टित करने वाले पोलथीन तथा कागज और पत्तों के दोनों का ही इतना विसर्जन इसमें नाविकों के लाख-माना करने पर भी होता है कि नैनी इस सबको गलाने-पचाने के बाद कब तक अपने अमृत-जल को गरल में परिवर्तित होने से रोक सकती है ?
‘‘यह नैना देवी ही साक्षी हैं।’’ उनकी नौका को एक दिन अलमस्ती में झील के इस छोर से उस छोर तक ले जाता हुआ बूढ़ा मुहम्मद इस्माइल बोला था, ‘‘यह ताल न जाने कितनी जानो के लिए कब्र बन आया। लैला –मजनू आज भी पैदा होते रहते हैं हुजूर। और न जाने कितनी लैलाओं और कितने मजनुओं ने कभी झील की सड़क वाली दीवार से तो कभी किसी आभागे नाविक की नौका से ही इस मनहूस पानी में छलांग लगाकर अपनी मुहब्बत पर इल्हामी मुहर लगा दी, नहीं कहा जा सकता।’’
‘‘तब तो यह पानी आदमी की लाशों का स्वाद भी सँजोए हुए है ? सड़ी-गली लाशें इस पानी को सड़ाती ही तो रहती हैं।’’ विश्वम्भर बोल गया था।
‘‘यह क्या आज से हो रहा है हुजूर ?’’ अपनी सत्तर की उम्र के बावजूद पूर्णतया झुर्री-रहित अपने चेहरे पर एक अनाम चमक लाते हुए मुहम्मद बोला था।
‘‘तुमने सुना नहीं ?’’ विश्वम्भर उसके समीप आ गया था, ऐसा कि उसके शरीर से निस्सृत गंध गीतिका के कुछ अधिक ही संवेदनशील नासापुट आसानी से पकड़ सकते थे।
‘‘आज यह कैसी मोहक गंध तुम्हारे तन से निस्सृत हो रही है ?’’ उसने पूछा था और उसका मन किया था उसकी चाँदनी-भीगे हाथों को वह अपने दोनों हाथों में कस ले। पर वह ऐसा नहीं कर सकी। जानती थी, इसका वह बुरा मानेगा और सूर्योंदय से ही सही आरंभ उसकी बातचीत किसी असमय के सूर्यास्त-सी समाप्त हो जाएगी—जैसे भरी दोपहरी में सूर्य ग्रहण-ग्रस्त हो जाए।
‘‘आज फूलों की वादियों से जो लौटा हूँ। मेरा कार्य मुझे किन-किन वादियों-वनों में ले जाता है तुम्हें क्या पता ? वनैले फूलों की गंध है यह —अनछुई, अननुभूत।’’ विश्वम्भर ने उत्तर दिया।
नैनीताल था यह। नहीं, झील का अछोर विस्तार सामने नहीं था। एक पहाड़ी की चोटी पर ही खड़े थे वे। पास के एक डाकबंगले में जगह मिली थी। झील का पुराना आकर्षण तो अब वर्षों से तिरोहित होने लगा था। इसका पानी दिनों-दिन अपनी स्वच्छता खोता जा रहा था। एक हरीतिमा-सी उसमें घुलने लगी थी। यह अगल-बगल की पहाड़ियों का प्रभाव था क्या कि झील भी अपना रंग बदलने लगी थी ? नहीं, ऐसा कुछ नही था, गीतिका ने अपने इस प्रवास के दौरान एक बार अकेली ही झील के किनारे खड़ी-खड़ी सोचा था। उस दिन वह चाह कर भी विश्वम्भर को झील के किनारे तक नहीं खीच सकी थी।
‘‘तुम्हीं जाओ वहाँ, उस झील के पानी से मुझे अब उबकाई आती है। और जानती हो इसकी झील से पूरे नैनीताल को पानी पिलाते हैं और उसके लिए जल-शोधन के क्रम में पड़ने वाली क्रोमीन की मात्रा वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। अब तो यह पानी इस दवा से इतना प्रदूषित हो गया है कि हम समतल-वासियों को यह रास ही नहीं आता।’’ उस दिन विश्वम्भर का पेट सचमुच खराब था। उसी दिन क्या, वह इस बार जब से नैनीताल आया है ‘आंटिबाइटिक्स’ की बैसाखियों के सहारे ही अपने अनियंत्रित हो आए उदर को नियंत्रित करता रहा है।
हाँ, उस दिन नैना देवी के मंदिर के सामने खड़ी झील के पानी को देखते हुए उसने सोचा था, क्योंकि दिनों-दिन ऐसा होता जा रहा है उसका रूप ? क्यों घुलता जा रहा है वनस्पतियों का रंग इसमें ? पर वनस्पतियाँ तो प्रायः निर्दोष होती है....जीवनदायिनी। इन्हीं में कोई संजीवनी भी कहीं होगी। इसी हिमालय से हनुमान ले गए थे उसे, लक्ष्मण की प्राण-रक्षा के लिए। यह पानी मात्र वनस्पतियों का रंग ही ग्रहण कर सका है, उनका गुण नहीं। इस पानी के रंग बदलने के कारण कुछ और हैं। उसकी दृष्टि उठी थी झील की दूसरी ओर की पहाड़ी से गिरते कई नालों की तरह जो अपनी गंदगी अबाध रूप से उड़ेलते जा रहे थे। नैनी में। बरसाती दिनों में तो हाहाकार करते ये कृतिम-अकृतमि नाले इसमें पता नहीं कितना काली-पीला मिट्टी और सड़े-गले पत्ते ला परोसते हैं ? और नैनीताल की बरसात भी क्या कुछ कम दिनों की होती है ? कभी-कभी मई के आरंभ में ही शुरु हो गई तो अगस्त के मध्य तक खिंची चली जाती है।
विश्म्भर ‘क्रोमीन’ द्वारा उसके जल के प्रदूषण की बात कर रहा था। वह कैसे भूल गया कि ‘क्रोमीन’ तो बाद में प्रदूषित करती है, इस नैनी के जल को वास्तविक प्रदूषण तो इसे हमारी उदासीनता ही प्रदान करती है। नालों से गिरते पानी को छोड़ भी दें तो ‘सीजन’ के दिनों में ताल के वक्ष पर तैरती अनेक नौकाओं में आसीतन अनेक हाथों से खाद्य सामग्रियों को वेष्टित करने वाले पोलथीन तथा कागज और पत्तों के दोनों का ही इतना विसर्जन इसमें नाविकों के लाख-माना करने पर भी होता है कि नैनी इस सबको गलाने-पचाने के बाद कब तक अपने अमृत-जल को गरल में परिवर्तित होने से रोक सकती है ?
‘‘यह नैना देवी ही साक्षी हैं।’’ उनकी नौका को एक दिन अलमस्ती में झील के इस छोर से उस छोर तक ले जाता हुआ बूढ़ा मुहम्मद इस्माइल बोला था, ‘‘यह ताल न जाने कितनी जानो के लिए कब्र बन आया। लैला –मजनू आज भी पैदा होते रहते हैं हुजूर। और न जाने कितनी लैलाओं और कितने मजनुओं ने कभी झील की सड़क वाली दीवार से तो कभी किसी आभागे नाविक की नौका से ही इस मनहूस पानी में छलांग लगाकर अपनी मुहब्बत पर इल्हामी मुहर लगा दी, नहीं कहा जा सकता।’’
‘‘तब तो यह पानी आदमी की लाशों का स्वाद भी सँजोए हुए है ? सड़ी-गली लाशें इस पानी को सड़ाती ही तो रहती हैं।’’ विश्वम्भर बोल गया था।
‘‘यह क्या आज से हो रहा है हुजूर ?’’ अपनी सत्तर की उम्र के बावजूद पूर्णतया झुर्री-रहित अपने चेहरे पर एक अनाम चमक लाते हुए मुहम्मद बोला था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book