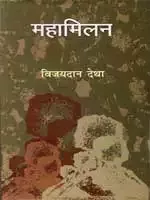|
उपन्यास >> महामिलन महामिलनविजयदान देथा
|
98 पाठक हैं |
||||||
विजयदान देथा की जानी-पहचानी और विशिष्ट कथा शैली में बुना गया उपन्यास है- ‘महामिलन’
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
विजयदान देथा की जानी-पहचानी और विशिष्ट कथा शैली में बुना गया उपन्यास
है- ‘महामिलन’। गाँव इसकी कथा-भूमि है, गौतम नाम का अनाथ हो
गया बालक कथा-नायक है। अफीमची पिता और डरी हुई माता की इस सन्तान का
रिश्ता बहुत बचपन में हो जाता है। मगर रिश्ता किसी मुकाम तक पहुँचे, उसके
पहले माता-पिता जीवन का ही रिश्ता तोड़कर दूसरे लोक चले जाते हैं।
दुर्भाग्य इस बालक को बन्धक बनने पर मजबूर करता है।
मगर असल कथा वहाँ शुरू होती है, जहाँ गौतम-पिता द्वारा किए गए रिश्ते का सूत्र नये सिरे से थामने निकलता है। वह सूत्र उसकी पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा तोड़ा जा चुका है। लेकिन गौतम कटिबद्ध है, प्राण देने का संकल्प भी उसके साथ है। पत्नी उससे मिलती है, मगर वह उसे पहचानता नहीं। वह पहचान लेती है, ठिठोली करती है या परीक्षा लेती है, पता नहीं, मगर उसे पता है कि आनेवाले दिनों में कई परीक्षाएँ बाकी हैं। यहाँ से विजयदान देथा की कलम का कौशल अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। जीवन में निहित विडम्बनाओं का ऐसा अंकन करते हैं कि पाठक ठगा -सा रह जाता है। उसे भावनाओं के की संघर्ष देखने को मिलते हैं, वह सरलता को दुनियादारी से लोहा लेता हुआ देखता है, सैद्धान्तिकता और नैतिकता को व्यावहारिकता और अनैतिकता से लड़ता हुआ पाता है। पूरे उपन्यास में एक आस्था झिलमिलाती रहती है, गौतम के जीतने का विश्वास, जो पाठक का भी विश्वास बन जाता है।
एक पुरातन लगती कथा जञ्जीर से आधुनिक समय को बाँधने का यह साहस विजयदान देथा ही दिखा सकते हैं उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लेखकीय कौशल से एक बड़े फलक में पसर जाता है। ‘महामिलन’ में एक तरह की बहुफलकीयता भी है जिसके विभिन्न कोणों को समझने में पाठक को जरा भी मुश्किल नहीं होती है।
मगर असल कथा वहाँ शुरू होती है, जहाँ गौतम-पिता द्वारा किए गए रिश्ते का सूत्र नये सिरे से थामने निकलता है। वह सूत्र उसकी पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा तोड़ा जा चुका है। लेकिन गौतम कटिबद्ध है, प्राण देने का संकल्प भी उसके साथ है। पत्नी उससे मिलती है, मगर वह उसे पहचानता नहीं। वह पहचान लेती है, ठिठोली करती है या परीक्षा लेती है, पता नहीं, मगर उसे पता है कि आनेवाले दिनों में कई परीक्षाएँ बाकी हैं। यहाँ से विजयदान देथा की कलम का कौशल अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। जीवन में निहित विडम्बनाओं का ऐसा अंकन करते हैं कि पाठक ठगा -सा रह जाता है। उसे भावनाओं के की संघर्ष देखने को मिलते हैं, वह सरलता को दुनियादारी से लोहा लेता हुआ देखता है, सैद्धान्तिकता और नैतिकता को व्यावहारिकता और अनैतिकता से लड़ता हुआ पाता है। पूरे उपन्यास में एक आस्था झिलमिलाती रहती है, गौतम के जीतने का विश्वास, जो पाठक का भी विश्वास बन जाता है।
एक पुरातन लगती कथा जञ्जीर से आधुनिक समय को बाँधने का यह साहस विजयदान देथा ही दिखा सकते हैं उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लेखकीय कौशल से एक बड़े फलक में पसर जाता है। ‘महामिलन’ में एक तरह की बहुफलकीयता भी है जिसके विभिन्न कोणों को समझने में पाठक को जरा भी मुश्किल नहीं होती है।
-प्रियदर्शन
अन्तरपुट
काबुलीवाले ! ओ काबुलीवाले !
16 जुलाई, 1998, बुधवार
बोरुन्दा
प्रिय शिवप्रसाद ,
पाठ्यक्रम के अलावा जब से अन्य पुस्तकें पढ़ने की गहरी अभिरुचि जाग्रत हुई है। तब से जाने क्यों बिना मुखबन्द की पुस्तक देखकर ऐसा महसूस होता है कि पुस्तक सम्पूर्ण नहीं है। पहिनावे में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मेरे द्वारा प्रकाशित या सम्पादित कोई भी पुस्तक भूमिका के बगैर नहीं छपी। मेरी हर पुस्तक मेरी देखरेख में आँखों के सामने ही छपती रही है। जैसे छपाई भी किसी-न-किसी रूप में लेखन से जुड़ी हो। जिस तरह दूसरे के खाने से अपना पेट नहीं भरता, ठीक इसी तरह सामने छपाई न होने पर मुझे तृप्ति नहीं होती, शिव ! कुछ-न-कुछ अभाव खटकता है। मानों मेरी सन्तान उघड़े बदन है। पहली बार मेरी देखरेख के बिना, मेरी नजरों से परे ‘दुविधा’ और ‘उलझन’ का प्रकाशन हुआ। जब भी इन्हें देखता हूँ तो दिल में एक चुभन-सी महसूस होती है। कहीं अपने ही शरीर का कोई अंग पीछे तो नहीं छूट गया ?
‘सपनप्रिया’ की भूमिका से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ और लिखते-लिखते ही यह बात समझ में आई कि प्राक्कथन, सम्बन्धित पुस्तक के बारे में ही हो, यह जरूरी नहीं है। रचनाओं की तरह वह भी एक स्वतन्त्र विधा हो, जिससे लेखक के हाड़-मांस और उसके अन्तस् की पहिचान अपने पाठकों से हो सके। और उस पहिचान से रचनाओं को समझने में एक दृष्टि मिले। लेखक हवा में साँस जरूर लेता है, पर उसके अधिकांश कार्य-कलाप धरती से, परिवार से मित्रों से, परंपरा से, अपने प्रिय लेखक और पाठकों से जुड़े रहते हैं। अपनी रचनाओं के साथ लेखक का मिजाज भी प्रस्तुत रहे तभी रचना पूर्ण बनती है। अब मैं ऐसा सोचने लगा हूँ। किसी भी विशाल-से-विशाल और छोटे-से-छोटे पेड़-पौधे की ऊपरी छाल के नीचे एक झीनी-सी अन्तरचाल होता है न, उसके प्राणों की सुरक्षा के लिए चारों ओर आवेष्टित। समझ गए न शिव ? रचनाओं और लेखक के बीच ऐसी ही एक अदीठ अन्तरछाल या अन्तर पुट अवस्थित रहता है। यदि अधिकृत रूप से उसका तनिक आभास पाठकों को मिल जाए तो निस्सन्देह अपनत्व की अनुभूति होती है। अपनी आसन्न मनःस्थित और अपना सोच रचनाओं के साथ-साथ दर्ज हो तो एक अलग ही अनुगूँज सुनाई देती है।
इसलिए अपने प्रिय लेखकों के पत्र, उनकी जीवनी से उनके आत्मकथ्य, उनके संस्मरण और उनकी डायरियाँ पढ़ने की मुझे बड़ी ‘हवस’ रहती है। इनसे फकत मेरी मानसिक प्यास ही नहीं बुझती, शारारिक प्यास भी बुझ जाती है, जो पानी जितनी ही अपरिहार्य है। ऐन मौके पर मेरी धूमिल स्मृति ने बड़ा साथ दिया रे शिव ! श्रीमती शीला सन्धु ने सुमित्रानन्दन पन्त के बारे में एक अविस्मरणीय संस्मरण सुनाया, जब वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से समादृत हुए थे। शीलाजी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गईं तो पन्तजी ने एक लिफफा उनके सामने किया। शीलाजी ने बाल-विस्मय से पूछा, ‘क्या है ?’ तब उन्होंने झीने स्वर में सहज भाव से कहा, ‘आपने कुछ वर्ष पहिले राजकमल के लिए एक प्रेस लगाने की बात कही थी न। इसमें ज्ञानपीठ का चेक है। थोड़ी मदद मिलेगी।’ सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। पन्तजी की कविताएँ मेरे मन को छूती नहीं थीं। यह किस्सा सुनते ही पन्तजी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। पुराने पछतावे का भी पार नहीं रहा। दुबारा पढ़ने पर उनकी रचनाओं का स्वाद ही कुछ और लगेगा।
अन्तोन चेखोव और तॉलस्तॉय के संस्मरण जो मैक्सिम गोर्की ने अपनी सधी कलम से चित्रित किए हैं, वे मुझे उनकी फोटुओं की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित करते हैं। द्रवित करते हैं। तस्वीर में तो बाहर की बनावट और क्षणिक मुद्रा टंक्कित हो जाती है और हमेशा के लिए व्यक्ति के चेहरे पर चिपक जाती है। लेकिन पत्र, डायरी व संस्मरणों से आत्मिक छवि झलकती है। संस्मरण और अपनी आत्मकथा के सीगे में गोर्की लाजवाब है रे शिव, जिन्हें पढ़कर बाहर का हुलिया तो भीतर सिमटने लगता है और भीतर का तमाम अदृष्ट बाहर प्रकट होने लगता है। कृतियों के साथ-साथ यदि कृतिकार का व्यक्तित्व किसी भी रूप में उजागर होता रहे तो कृतियों में अन्तर्निहित व्यञजना अपना अलग ही सुर गुनगुनाने लगती है। अगली बार मिलते ही मैक्सिम गोर्की के संस्मरण लाऊँगा, और तुम्हारे मुँह से मैं सुनूँगा।
अब तक तो फकत उन्हें पढ़ता रहा हूँ। तुम बड़े भाव-विभोर होकर सुनाते हो। मैं इतना अच्छा नहीं सुना पाऊँगा। जिस तरह तुम्हारे ईश्वर की माया का कोई पार नहीं है, उसी तरह शिव की श्रेष्ठतम कृतियों की माया का भी कोई पार नहीं है। तुम्हारे खयाल से आराध्य को एक बार सुमरना ही पर्याप्त नहीं है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कृतियों को फकत एक बार पढ़ना ही काफी नहीं है। अनन्त रहस्यमयी इन कृतियों का रहस्य केवल आँखों से ही दिखलाई नहीं पड़ता। क्षण-क्षण बदलती प्रकृति का परिवेश और उससे प्रभावित मनः स्थित के माहौल में परायण करते समय रचना भी अपने रंग बदलती रहती है। कलियों की नईं सिमटे-बँधे ‘सबद’ शनैः-शनैः खुलते जाते हैं और उनमें घुले मर्म की महक एक ऐसी सुवास फैलाने लगती है, जो किसी भी प्राकृतिक या लौकिक सौरभ से नहीं मिलता। नासा-रन्ध्रों के बजाय शरीर का रोम-रोम उसे सूँघने के लिए आतुर हो उठता है।
एक अन्तरंग बात कहूँ, दूसरे विश्वास करें न करें तुम आँख मीच कर विश्वास करोगे। अभी परसों का ही ताजातरीन अनुभव है, उससे पहले किसी भी रचना को पढ़कर ऐसी अपूर्व अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई, दृष्टान्त का सहारा लूँ, उससे कम खुशी मुझे रवि बाबू की अद्वितीय कहानी ‘काबुलीवाला’ पढ़ते समय हुई। साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन द्वारा ‘रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ’ इतनी बार पढ़ चुका कि ‘काबुलीवाला’, ‘पोस्टमास्टर’, ‘एक रात’, ‘क्षुधित पाषाण’ और ‘आधी रात में’ अब कहीं निशान लगाने और टिप्पणी लिखने की कोई गुञ्जाइश नहीं बची है। रात के दो बजे पानी पीने के लिए उठा। मद्धिम चाँदनी से चौक हलका-हलका आलोकित हो रहा था। ऊपर देखा-बादलों से मुक्त सप्तमी का चाँद आधा खण्डित होते हुए भी मुस्करा रहा था। एक दिन पहले तो आकाश में घटनाएँ इस कदर उमड़-घुमड़ रही थीं कि जैसे अब ये कभी बेदखल होंगी नहीं, इसी तरह चारों ओर डेरा जमाए रहेंगी। पर एक ही दिन में किसी की जादुई शक्ति ने ऐसा सफाया किया कि बादल का नाम-निशान तक कहीं नजर नहीं आया।
शायद तुम्हारे आराध्य के उन्हीं आगोचर हाथों ने उन्हें बेदखल किया, जिन्होंने आठ-दस रोज से प्रतिष्ठित कर रखा था। मेरे अपने गाँव से तो वे मामूली बूँदाबूँदी करके ही ओझल हो गए। किन्तु कोटा, बूँदी, जयपुर और अजमेर में जरूरत से ज्यादा बरस रहे हैं। तेरा ईश्वर भी बड़ा मन-मौजी है रे शिव ! तेरी कुछ चलती हो जो सूखें गाँवों में बारिश करने के लिए अरदास करना। बड़ा तन्मय होकर उसे याद करता है न। कुछ-न-कुछ बड़े बिना वापस नींद आती नहीं। सिरहाने गुरुदेव की गुरुवाणी और सीसा पेंसिल रखकर सोया था। काबुलीवाला से स्नेह-मिलन की इच्छा हुई तो वही कहानी शुरू कर दी। पढ़ते-पढ़ते नहीं ही तो लेनी है शीर्षक पढ़कर बाईं बाजू पश्चिम दिशा में खुलने वाली खिड़की से झाँका-बबूल पर हल्की-हल्की चाँदनी का घोल छितरा हुआ था।
धुँधली-धुँधली हरियाली और पतली-पतली डालियों का ऐसा अप्रतिम नजारा दिखलाई पड़ा कि आँखे वहीं अटक कर रही गईं। खुले सीने पर पोथी धर दी। एक दी एक ही ठौर गड़ा यही बबूल का गाछ कितने-कितने रंग बदलता है सवेरे उषा की वेला इसकी हरियाली का रंग गी दूसरा है। दमकती धूप फैली हो तो वही हरियाली एकदम प्रगाढ़ और गहरी हो जाती है। फिर साँझ की वेला झीना घूँघट पहिने सलज्ज हरियाली की रौनक ही बदल जाती है। तेरा या पूनम की चाँदनी में इसका हरा-भरा रंग कैसा प्रदीप्त हो उठता है और अँधेरी रात में चलो हरियाली का अभाव-मात्र दिखलाई पड़ता है। तब इसके कौन से रूप को सही मानू, शिव कुछ समझ में नहीं आता। लगता है इस रहस्य को समझने का प्रयास अधिक उपादेय साबित नहीं होगा। इसके सभी रूप सही हैं। रंग-द्वेष से विकृत का प्रत्यक्ष स्वरूप भी एकदम सही है।
उस अद्भुत दृश्य से आँखें, मन और आत्मा तृप्त हो गई तो काबुलीवाला शीर्षक भी बड़ा रहस्यमय लगा। ‘मेरी पाँच बरस की छोटी बेटी मिनी बोले पलभर भी नहीं रह सकती।’ यह वाक्य पूरा होते ही विश्व-जगत् की समस्त ‘मुन्नियों’ का बचपन चश्में से ढकीं मात्र दो पुतलियों में ही समा गया। ‘सुबह मैंने अपने उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद में हाथ लगाया था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी, पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौआ कहता था, वह कुछ नहीं जानता हैं न ?’ पानी की बूँद में असंख्य कीटाणु समाये रहते हैं।
उसी प्रकार एक ही मिनी में मुझे उस उम्र की अनगिनत बच्चियों के रूप मे दिखाई पड़ने लगी। पिताजी में समूची दुनिया के शालीन मनीषा के पिता, माँ की एक काया में संसार की समस्त माताएँ और काबुलीवाले के ढीले-ढीले लिबास में अफगानिस्तान के तमाम पठान अपनी कद्दावर कद-काठी सहित समा गए। गुरुदेव की कलम का करिश्मा कुछ ऐसा ही ऐन्द्रियजालिक है तुम हमेशा नहाने के बाद पद्मानशन की मुद्रा में रामचरितमानस का पाठ गाकर करते हो। गीता और शंकराचार्य के श्लोकों को सुमधुर उच्चारण करते हो। साहित्य में भी परिष्कृत रुचि है तुम्हारी। पर मेरे कहने से रवि बाबू, शरत् बाबू, चेखोव, तॉलस्तॉय, दॉस्तोयवस्की, स्टीफन ज्वाइग, हावर्ड फास्ट, कजान जाकिस इत्यादि श्रेष्ठतम् लेखों की कृतियों का भी नियमित पाठ करो। जिन्हें पाने की तुम्हारे मन में अदम्य लालसा है वे राम-रहीम, कृष्ण, ब्रह्म, खुदा या ईसू इन सबको ऐसे विलक्ष्ण ग्रन्थों में पा सकोगे। ये केवल लेखक ही नहीं, स्रष्टा हैं-स्रष्टा। सृष्टिकर्ता के अचराचर से इनकी सृष्टि कम नहीं है।
काबुलीवाला की घटनाएँ याद न हों तो फिर से बता दूँ-पाँच बरस की छोटी मिनी अपनी उम्र के अनुसार सब बच्चों की तरह जिज्ञासु है। बाह्य-जगत् को जानने की इच्छुक है। अपने मिनी, पिता से तरह-तरह के प्रश्न पूछती है। एक दिन संयोग से काबुलीवाला की हँक सुनकर उसे आवाज देती है। पहली मुलाकात से बच्ची का डर मिटने के पश्चात् दोनों में अच्छी-खासी दोस्ती हो जाती है। प्रतिदिन रहमत की हाँक सुनकर जोर-जोर से पुकारती है। काबुलीवाले बड़े स्नेह-दुलार से मिनी को बादाम-पिस्ते व काजू इत्यादि मेवे देता है और परस्पर हँसी-टट्टे के संवाद भी चलते रहते हैं। काबुलीवाला प्रतिवर्ष माघ के महीने देश जाने से पहले अपनी उधार वसूल करता है। एक सिरफिरे ग्राहक से तू-तड़ाक के दौरान पठान-भाई आवेश में आकर उसे छुरा मार देता है। परिणाम-स्वरूप उसे आठ साल की सख्त सजा हो जाती है। पूरी सजा काटने के बाद वह मिनी के घर उससे मिलने आता है। संयोग से उसी साँझ मिनी का ब्याह है। काबुलीवाले करी उत्कट लालसा देखकर, सहृदय पिता मिनी को बुलाकर दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। पिता के आग्रह करने पर काबुलीवाला किराये के रुपये लेकर अपने देश लौट जाता है। मिनी की हम उम्र बिटिया और उसकी माँ से मिलने की खातिर।
उपरोक्त घटनाओं के इस एक ही कथानक से अनेक लेखक बहुतेरी कहानियाँ लिख सकते हैं। किन्तु गुरुदेव ने इस कथानक को बादलों की ऊँचाई से उठाते हुए कहानी कला को जिस अज्ञात लोक तक उड़ाया है, मैं तो आज भी वैसी कल्पना नहीं कर सकता। कहानी के क्रमिक विकास में सारी घटनाएँ इस कलात्मक ताने-बाने से गुम्फित हुई हैं कि जिन्हें कहानी से अलग किया ही नहीं जा सकता। संवाद, प्रतिसंवाद, वर्णन प्रतिक्रिया, अन्तर्द्वन्द्व, कल्पना और सूक्ष्म अनुभूतियों का ऐसा आनुपातिक चित्रण हुआ है कि निर्जीव घटनाओं में प्राणों का सञ्चार हो गया। लगता है यह कहानी लिखी नहीं गई, रची गई है। उकेरी गई है।
तभी पौरुषेय के बहाने अपौरुषेय की श्रेणी में प्रवेश पा गई है। अनुदित कहानी के सारे शब्द अपने वर्णानुक्रम से कोश के भीतर बरसों से बन्दी पड़े हैं, सामने दिए अर्थों के साथ। ससुराल का अर्थ—ससुर का घर। पति के पिता का निवास कारागृह और जेलखाना भी लिखा है। लेकिन कहानी में बदलते प्रसंगों के अनुसार जिस-जिस वाक्य के बीच ससुराल का प्रयोग हुआ है, उसे बाँचते हुए कलेजे पर जो चोट लगती है, वह सौन्दर्यानुभूति के चरम-आनन्द की मानो पराकाष्ठा हो। गुरुदेव की कलम का परस पाकर ससुराल का समूचा हर्ष-विषाद, द्वेष-प्रताड़ना, पति का सहवास, गर्भ की आशा, प्रसव पीड़ा से उत्पन्न मधुर उमंग, शिशु का दुग्धपान, बेटी की विदाई, बहू का गृह-प्रवेश इत्यादि सब-कुछ भरा-पूरा परिवेश आँखो के सामने झिलमिलाने लगता है और ससुराल की यही संज्ञा जब मिनी के प्रसंग से हटकर दो सिपाहियों के साथ भीड़-भभ्भड़ से घिरे रहमत के सन्दर्भ में प्रयुक्त होती है तो उसका सारा मर्म ही बदल जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँवों में बेड़ियाँ हैं। कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा है। अबोध मिनी उससे पूछती है, ‘तुम ससुराल जाओगे ?’‘’
‘रहमत ने हँस कर कहा, वहीं जा रहा हूँ।’’
‘देखा, उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा, तब हाथ दिखाकर बोला, ‘‘ससुर को मारता, पर क्या करूँ-हाथ बँधे हैं।’
पाठ्यक्रम के अलावा जब से अन्य पुस्तकें पढ़ने की गहरी अभिरुचि जाग्रत हुई है। तब से जाने क्यों बिना मुखबन्द की पुस्तक देखकर ऐसा महसूस होता है कि पुस्तक सम्पूर्ण नहीं है। पहिनावे में कुछ कमी रह गई है, इसलिए मेरे द्वारा प्रकाशित या सम्पादित कोई भी पुस्तक भूमिका के बगैर नहीं छपी। मेरी हर पुस्तक मेरी देखरेख में आँखों के सामने ही छपती रही है। जैसे छपाई भी किसी-न-किसी रूप में लेखन से जुड़ी हो। जिस तरह दूसरे के खाने से अपना पेट नहीं भरता, ठीक इसी तरह सामने छपाई न होने पर मुझे तृप्ति नहीं होती, शिव ! कुछ-न-कुछ अभाव खटकता है। मानों मेरी सन्तान उघड़े बदन है। पहली बार मेरी देखरेख के बिना, मेरी नजरों से परे ‘दुविधा’ और ‘उलझन’ का प्रकाशन हुआ। जब भी इन्हें देखता हूँ तो दिल में एक चुभन-सी महसूस होती है। कहीं अपने ही शरीर का कोई अंग पीछे तो नहीं छूट गया ?
‘सपनप्रिया’ की भूमिका से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ और लिखते-लिखते ही यह बात समझ में आई कि प्राक्कथन, सम्बन्धित पुस्तक के बारे में ही हो, यह जरूरी नहीं है। रचनाओं की तरह वह भी एक स्वतन्त्र विधा हो, जिससे लेखक के हाड़-मांस और उसके अन्तस् की पहिचान अपने पाठकों से हो सके। और उस पहिचान से रचनाओं को समझने में एक दृष्टि मिले। लेखक हवा में साँस जरूर लेता है, पर उसके अधिकांश कार्य-कलाप धरती से, परिवार से मित्रों से, परंपरा से, अपने प्रिय लेखक और पाठकों से जुड़े रहते हैं। अपनी रचनाओं के साथ लेखक का मिजाज भी प्रस्तुत रहे तभी रचना पूर्ण बनती है। अब मैं ऐसा सोचने लगा हूँ। किसी भी विशाल-से-विशाल और छोटे-से-छोटे पेड़-पौधे की ऊपरी छाल के नीचे एक झीनी-सी अन्तरचाल होता है न, उसके प्राणों की सुरक्षा के लिए चारों ओर आवेष्टित। समझ गए न शिव ? रचनाओं और लेखक के बीच ऐसी ही एक अदीठ अन्तरछाल या अन्तर पुट अवस्थित रहता है। यदि अधिकृत रूप से उसका तनिक आभास पाठकों को मिल जाए तो निस्सन्देह अपनत्व की अनुभूति होती है। अपनी आसन्न मनःस्थित और अपना सोच रचनाओं के साथ-साथ दर्ज हो तो एक अलग ही अनुगूँज सुनाई देती है।
इसलिए अपने प्रिय लेखकों के पत्र, उनकी जीवनी से उनके आत्मकथ्य, उनके संस्मरण और उनकी डायरियाँ पढ़ने की मुझे बड़ी ‘हवस’ रहती है। इनसे फकत मेरी मानसिक प्यास ही नहीं बुझती, शारारिक प्यास भी बुझ जाती है, जो पानी जितनी ही अपरिहार्य है। ऐन मौके पर मेरी धूमिल स्मृति ने बड़ा साथ दिया रे शिव ! श्रीमती शीला सन्धु ने सुमित्रानन्दन पन्त के बारे में एक अविस्मरणीय संस्मरण सुनाया, जब वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से समादृत हुए थे। शीलाजी उन्हें स्टेशन पर छोड़ने गईं तो पन्तजी ने एक लिफफा उनके सामने किया। शीलाजी ने बाल-विस्मय से पूछा, ‘क्या है ?’ तब उन्होंने झीने स्वर में सहज भाव से कहा, ‘आपने कुछ वर्ष पहिले राजकमल के लिए एक प्रेस लगाने की बात कही थी न। इसमें ज्ञानपीठ का चेक है। थोड़ी मदद मिलेगी।’ सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। पन्तजी की कविताएँ मेरे मन को छूती नहीं थीं। यह किस्सा सुनते ही पन्तजी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। पुराने पछतावे का भी पार नहीं रहा। दुबारा पढ़ने पर उनकी रचनाओं का स्वाद ही कुछ और लगेगा।
अन्तोन चेखोव और तॉलस्तॉय के संस्मरण जो मैक्सिम गोर्की ने अपनी सधी कलम से चित्रित किए हैं, वे मुझे उनकी फोटुओं की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित करते हैं। द्रवित करते हैं। तस्वीर में तो बाहर की बनावट और क्षणिक मुद्रा टंक्कित हो जाती है और हमेशा के लिए व्यक्ति के चेहरे पर चिपक जाती है। लेकिन पत्र, डायरी व संस्मरणों से आत्मिक छवि झलकती है। संस्मरण और अपनी आत्मकथा के सीगे में गोर्की लाजवाब है रे शिव, जिन्हें पढ़कर बाहर का हुलिया तो भीतर सिमटने लगता है और भीतर का तमाम अदृष्ट बाहर प्रकट होने लगता है। कृतियों के साथ-साथ यदि कृतिकार का व्यक्तित्व किसी भी रूप में उजागर होता रहे तो कृतियों में अन्तर्निहित व्यञजना अपना अलग ही सुर गुनगुनाने लगती है। अगली बार मिलते ही मैक्सिम गोर्की के संस्मरण लाऊँगा, और तुम्हारे मुँह से मैं सुनूँगा।
अब तक तो फकत उन्हें पढ़ता रहा हूँ। तुम बड़े भाव-विभोर होकर सुनाते हो। मैं इतना अच्छा नहीं सुना पाऊँगा। जिस तरह तुम्हारे ईश्वर की माया का कोई पार नहीं है, उसी तरह शिव की श्रेष्ठतम कृतियों की माया का भी कोई पार नहीं है। तुम्हारे खयाल से आराध्य को एक बार सुमरना ही पर्याप्त नहीं है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कृतियों को फकत एक बार पढ़ना ही काफी नहीं है। अनन्त रहस्यमयी इन कृतियों का रहस्य केवल आँखों से ही दिखलाई नहीं पड़ता। क्षण-क्षण बदलती प्रकृति का परिवेश और उससे प्रभावित मनः स्थित के माहौल में परायण करते समय रचना भी अपने रंग बदलती रहती है। कलियों की नईं सिमटे-बँधे ‘सबद’ शनैः-शनैः खुलते जाते हैं और उनमें घुले मर्म की महक एक ऐसी सुवास फैलाने लगती है, जो किसी भी प्राकृतिक या लौकिक सौरभ से नहीं मिलता। नासा-रन्ध्रों के बजाय शरीर का रोम-रोम उसे सूँघने के लिए आतुर हो उठता है।
एक अन्तरंग बात कहूँ, दूसरे विश्वास करें न करें तुम आँख मीच कर विश्वास करोगे। अभी परसों का ही ताजातरीन अनुभव है, उससे पहले किसी भी रचना को पढ़कर ऐसी अपूर्व अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई, दृष्टान्त का सहारा लूँ, उससे कम खुशी मुझे रवि बाबू की अद्वितीय कहानी ‘काबुलीवाला’ पढ़ते समय हुई। साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन द्वारा ‘रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ’ इतनी बार पढ़ चुका कि ‘काबुलीवाला’, ‘पोस्टमास्टर’, ‘एक रात’, ‘क्षुधित पाषाण’ और ‘आधी रात में’ अब कहीं निशान लगाने और टिप्पणी लिखने की कोई गुञ्जाइश नहीं बची है। रात के दो बजे पानी पीने के लिए उठा। मद्धिम चाँदनी से चौक हलका-हलका आलोकित हो रहा था। ऊपर देखा-बादलों से मुक्त सप्तमी का चाँद आधा खण्डित होते हुए भी मुस्करा रहा था। एक दिन पहले तो आकाश में घटनाएँ इस कदर उमड़-घुमड़ रही थीं कि जैसे अब ये कभी बेदखल होंगी नहीं, इसी तरह चारों ओर डेरा जमाए रहेंगी। पर एक ही दिन में किसी की जादुई शक्ति ने ऐसा सफाया किया कि बादल का नाम-निशान तक कहीं नजर नहीं आया।
शायद तुम्हारे आराध्य के उन्हीं आगोचर हाथों ने उन्हें बेदखल किया, जिन्होंने आठ-दस रोज से प्रतिष्ठित कर रखा था। मेरे अपने गाँव से तो वे मामूली बूँदाबूँदी करके ही ओझल हो गए। किन्तु कोटा, बूँदी, जयपुर और अजमेर में जरूरत से ज्यादा बरस रहे हैं। तेरा ईश्वर भी बड़ा मन-मौजी है रे शिव ! तेरी कुछ चलती हो जो सूखें गाँवों में बारिश करने के लिए अरदास करना। बड़ा तन्मय होकर उसे याद करता है न। कुछ-न-कुछ बड़े बिना वापस नींद आती नहीं। सिरहाने गुरुदेव की गुरुवाणी और सीसा पेंसिल रखकर सोया था। काबुलीवाला से स्नेह-मिलन की इच्छा हुई तो वही कहानी शुरू कर दी। पढ़ते-पढ़ते नहीं ही तो लेनी है शीर्षक पढ़कर बाईं बाजू पश्चिम दिशा में खुलने वाली खिड़की से झाँका-बबूल पर हल्की-हल्की चाँदनी का घोल छितरा हुआ था।
धुँधली-धुँधली हरियाली और पतली-पतली डालियों का ऐसा अप्रतिम नजारा दिखलाई पड़ा कि आँखे वहीं अटक कर रही गईं। खुले सीने पर पोथी धर दी। एक दी एक ही ठौर गड़ा यही बबूल का गाछ कितने-कितने रंग बदलता है सवेरे उषा की वेला इसकी हरियाली का रंग गी दूसरा है। दमकती धूप फैली हो तो वही हरियाली एकदम प्रगाढ़ और गहरी हो जाती है। फिर साँझ की वेला झीना घूँघट पहिने सलज्ज हरियाली की रौनक ही बदल जाती है। तेरा या पूनम की चाँदनी में इसका हरा-भरा रंग कैसा प्रदीप्त हो उठता है और अँधेरी रात में चलो हरियाली का अभाव-मात्र दिखलाई पड़ता है। तब इसके कौन से रूप को सही मानू, शिव कुछ समझ में नहीं आता। लगता है इस रहस्य को समझने का प्रयास अधिक उपादेय साबित नहीं होगा। इसके सभी रूप सही हैं। रंग-द्वेष से विकृत का प्रत्यक्ष स्वरूप भी एकदम सही है।
उस अद्भुत दृश्य से आँखें, मन और आत्मा तृप्त हो गई तो काबुलीवाला शीर्षक भी बड़ा रहस्यमय लगा। ‘मेरी पाँच बरस की छोटी बेटी मिनी बोले पलभर भी नहीं रह सकती।’ यह वाक्य पूरा होते ही विश्व-जगत् की समस्त ‘मुन्नियों’ का बचपन चश्में से ढकीं मात्र दो पुतलियों में ही समा गया। ‘सुबह मैंने अपने उपन्यास के सत्रहवें परिच्छेद में हाथ लगाया था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी, पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौआ कहता था, वह कुछ नहीं जानता हैं न ?’ पानी की बूँद में असंख्य कीटाणु समाये रहते हैं।
उसी प्रकार एक ही मिनी में मुझे उस उम्र की अनगिनत बच्चियों के रूप मे दिखाई पड़ने लगी। पिताजी में समूची दुनिया के शालीन मनीषा के पिता, माँ की एक काया में संसार की समस्त माताएँ और काबुलीवाले के ढीले-ढीले लिबास में अफगानिस्तान के तमाम पठान अपनी कद्दावर कद-काठी सहित समा गए। गुरुदेव की कलम का करिश्मा कुछ ऐसा ही ऐन्द्रियजालिक है तुम हमेशा नहाने के बाद पद्मानशन की मुद्रा में रामचरितमानस का पाठ गाकर करते हो। गीता और शंकराचार्य के श्लोकों को सुमधुर उच्चारण करते हो। साहित्य में भी परिष्कृत रुचि है तुम्हारी। पर मेरे कहने से रवि बाबू, शरत् बाबू, चेखोव, तॉलस्तॉय, दॉस्तोयवस्की, स्टीफन ज्वाइग, हावर्ड फास्ट, कजान जाकिस इत्यादि श्रेष्ठतम् लेखों की कृतियों का भी नियमित पाठ करो। जिन्हें पाने की तुम्हारे मन में अदम्य लालसा है वे राम-रहीम, कृष्ण, ब्रह्म, खुदा या ईसू इन सबको ऐसे विलक्ष्ण ग्रन्थों में पा सकोगे। ये केवल लेखक ही नहीं, स्रष्टा हैं-स्रष्टा। सृष्टिकर्ता के अचराचर से इनकी सृष्टि कम नहीं है।
काबुलीवाला की घटनाएँ याद न हों तो फिर से बता दूँ-पाँच बरस की छोटी मिनी अपनी उम्र के अनुसार सब बच्चों की तरह जिज्ञासु है। बाह्य-जगत् को जानने की इच्छुक है। अपने मिनी, पिता से तरह-तरह के प्रश्न पूछती है। एक दिन संयोग से काबुलीवाला की हँक सुनकर उसे आवाज देती है। पहली मुलाकात से बच्ची का डर मिटने के पश्चात् दोनों में अच्छी-खासी दोस्ती हो जाती है। प्रतिदिन रहमत की हाँक सुनकर जोर-जोर से पुकारती है। काबुलीवाले बड़े स्नेह-दुलार से मिनी को बादाम-पिस्ते व काजू इत्यादि मेवे देता है और परस्पर हँसी-टट्टे के संवाद भी चलते रहते हैं। काबुलीवाला प्रतिवर्ष माघ के महीने देश जाने से पहले अपनी उधार वसूल करता है। एक सिरफिरे ग्राहक से तू-तड़ाक के दौरान पठान-भाई आवेश में आकर उसे छुरा मार देता है। परिणाम-स्वरूप उसे आठ साल की सख्त सजा हो जाती है। पूरी सजा काटने के बाद वह मिनी के घर उससे मिलने आता है। संयोग से उसी साँझ मिनी का ब्याह है। काबुलीवाले करी उत्कट लालसा देखकर, सहृदय पिता मिनी को बुलाकर दोनों की मुलाकात करवा देते हैं। पिता के आग्रह करने पर काबुलीवाला किराये के रुपये लेकर अपने देश लौट जाता है। मिनी की हम उम्र बिटिया और उसकी माँ से मिलने की खातिर।
उपरोक्त घटनाओं के इस एक ही कथानक से अनेक लेखक बहुतेरी कहानियाँ लिख सकते हैं। किन्तु गुरुदेव ने इस कथानक को बादलों की ऊँचाई से उठाते हुए कहानी कला को जिस अज्ञात लोक तक उड़ाया है, मैं तो आज भी वैसी कल्पना नहीं कर सकता। कहानी के क्रमिक विकास में सारी घटनाएँ इस कलात्मक ताने-बाने से गुम्फित हुई हैं कि जिन्हें कहानी से अलग किया ही नहीं जा सकता। संवाद, प्रतिसंवाद, वर्णन प्रतिक्रिया, अन्तर्द्वन्द्व, कल्पना और सूक्ष्म अनुभूतियों का ऐसा आनुपातिक चित्रण हुआ है कि निर्जीव घटनाओं में प्राणों का सञ्चार हो गया। लगता है यह कहानी लिखी नहीं गई, रची गई है। उकेरी गई है।
तभी पौरुषेय के बहाने अपौरुषेय की श्रेणी में प्रवेश पा गई है। अनुदित कहानी के सारे शब्द अपने वर्णानुक्रम से कोश के भीतर बरसों से बन्दी पड़े हैं, सामने दिए अर्थों के साथ। ससुराल का अर्थ—ससुर का घर। पति के पिता का निवास कारागृह और जेलखाना भी लिखा है। लेकिन कहानी में बदलते प्रसंगों के अनुसार जिस-जिस वाक्य के बीच ससुराल का प्रयोग हुआ है, उसे बाँचते हुए कलेजे पर जो चोट लगती है, वह सौन्दर्यानुभूति के चरम-आनन्द की मानो पराकाष्ठा हो। गुरुदेव की कलम का परस पाकर ससुराल का समूचा हर्ष-विषाद, द्वेष-प्रताड़ना, पति का सहवास, गर्भ की आशा, प्रसव पीड़ा से उत्पन्न मधुर उमंग, शिशु का दुग्धपान, बेटी की विदाई, बहू का गृह-प्रवेश इत्यादि सब-कुछ भरा-पूरा परिवेश आँखो के सामने झिलमिलाने लगता है और ससुराल की यही संज्ञा जब मिनी के प्रसंग से हटकर दो सिपाहियों के साथ भीड़-भभ्भड़ से घिरे रहमत के सन्दर्भ में प्रयुक्त होती है तो उसका सारा मर्म ही बदल जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँवों में बेड़ियाँ हैं। कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक सिपाही के हाथ में खून से सना छुरा है। अबोध मिनी उससे पूछती है, ‘तुम ससुराल जाओगे ?’‘’
‘रहमत ने हँस कर कहा, वहीं जा रहा हूँ।’’
‘देखा, उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा, तब हाथ दिखाकर बोला, ‘‘ससुर को मारता, पर क्या करूँ-हाथ बँधे हैं।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book