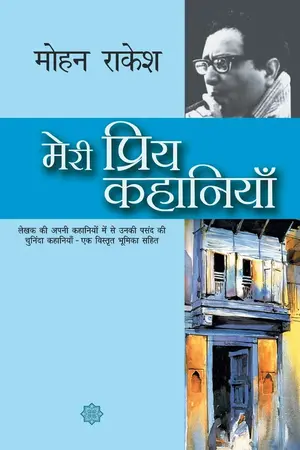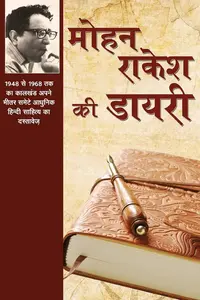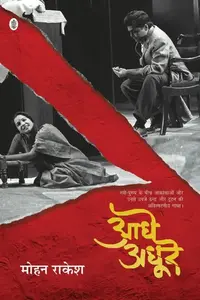|
कहानी संग्रह >> मेरी प्रिय कहानियाँ : मोहन राकेश मेरी प्रिय कहानियाँ : मोहन राकेशमोहन राकेश
|
91 पाठक हैं |
|||||||
"व्यक्ति और समाज के अंतर्द्वंद्व का आईना : मोहन राकेश की कालजयी कहानियाँ"
Meri prira kahaniyan by Mohan rakesh
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी कहानी को कथा और शैली दोनों ही दृष्टियों से नई दिशा देनेवाले लेखकों में मोहन राकेश का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कम ही लिखा परन्तु उनकी अनेक कहानियाँ साहित्य की अमर निधि बन गईं। प्रस्तुत संकलन में उनकी अपने ही द्वारा चुनी हुई कहानियाँ हैं। तथा अपने लेखन व रचना प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप में लिखी गई भूमिका भी है।
नये दौर की मेरी अधिकांश कहानियां
संबंधों की यंत्रणा को
अपने अकेलेपन में
झेलते लोगों की कहानियां हैं
जिनमें हर इकाई के माध्यम से
उसके परिवेश को अंकित करने का प्रयत्न है
यह अकेलापन समाज से कटकर
व्यक्ति का अकेलापन नहीं
समाज के बीच होने का अकेलापन है
और उसकी परणति भी
किसी तरह के सिनिसिज़्म में नहीं,
झेलने की निष्ठा में है
व्यक्ति और समाज को परस्पर-विरोधी
एक दूसरे से भिन्न और आपस में कटी हुई इकाइयां
न मानकर यहां उन्हें एक ऐसी अभिन्नता में देखने का
प्रयत्न है जहां व्यक्ति समाज की विडम्बनाओं का
और समाज व्यक्ति की यन्त्रणाओं का आईना है
नये दौर की मेरी अधिकांश कहानियां
संबंधों की यंत्रणा को
अपने अकेलेपन में
झेलते लोगों की कहानियां हैं
जिनमें हर इकाई के माध्यम से
उसके परिवेश को अंकित करने का प्रयत्न है
यह अकेलापन समाज से कटकर
व्यक्ति का अकेलापन नहीं
समाज के बीच होने का अकेलापन है
और उसकी परणति भी
किसी तरह के सिनिसिज़्म में नहीं,
झेलने की निष्ठा में है
व्यक्ति और समाज को परस्पर-विरोधी
एक दूसरे से भिन्न और आपस में कटी हुई इकाइयां
न मानकर यहां उन्हें एक ऐसी अभिन्नता में देखने का
प्रयत्न है जहां व्यक्ति समाज की विडम्बनाओं का
और समाज व्यक्ति की यन्त्रणाओं का आईना है
भूमिका
अपनी लिखी कहानियों में से कुछ एक को अलग छांटना काफी दुविधा का काम है। लिखते समय एक रचना के साथ जो निकटता रहती है, वर्ष बीतने के साथ किसी भी व्यतीत संबंध की तरह वह धुँधलाने लगती है। जिन प्रभावों में एक रचना होती है, उनसे हटकर किसी दूसरे प्रभावों में जीता व्यक्ति उस पहले की रचना के समय की आत्मीयता नहीं बनाए रह सकता। एक रचना से उबरकर ही वह पूरी रचना में प्रवृत्त होता है। और अन्तराल जब कई-कई रचनाओं का हो, तब तो आत्मीयता की भूमि पर किसी रचना की ओर लौटना असम्भव हो जाता है।
इसलिये जो कहानियां मैंने इस संग्रह के लिए चुनी हैं, उनके चुनाव का कोई कारण दे सकना मेरे लिए बहुत कठिन है। कहना नहीं हो, तो केवल इतना कहा जा सकता है कि इस बार अपनी कहानियों में से गुजरते हुए इन कहानियों पर उंगली ठहरती गई। ‘आर्द्रा’, ‘मिस पाल’ तथा ‘एक और ज़िंदगी’ जैसी कुछ अधिक प्रसिद्ध कहानियां आज मेरे समर्थन की अपेक्षा नहीं रखतीं।
चुनाव करने में मेरी एक दृष्टि अवश्य रही है कि संग्रह की कहानियां मेरी आज की कथायात्रा के प्राय: सभी पड़ावों का प्रतिनिधित्व कर सकें। केवल ‘इंसान के खंडहर’ शीर्षक संग्रह से मेरे बाद के प्रयोगों के साथ एक कड़ी के रूप में ठीक से जुड़ नहीं पाती। उनके शिल्प और कथ्य दोनों में एक तरह की ‘कोशिश’ है, एक निश्चित तलाश का कच्चापन ! यूं पाठकों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे आज भी मेरी वही कहानियां सबसे अधिक पसंद हैं।
यह आवश्यक नहीं कि एक लेखक के साथ-साथ उसके सभी पाठक उसकी बदलती मानसिकता के सब पड़ावों से गुजरते रहें। हर पड़ाव पर किन्हीं पाठकों के साथ उसके एक लेखक का संबंध टूट जाता है, और वहीं से एक नये वर्ग के साथ उसके संबंध की शुरुआत हो जाती है। ऐसा न होना एक लेखक की जड़ता का प्रमाण होगा। जीवन-भर एक ही मानसिक भूमि पर रहकर रचना करते जाना केवल शब्दों का व्यवसाय है,
और कुछ नहीं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत पाठकों का एक दूसरा वर्ग भी हैं, जो न केवल लेखक की पूरी रचनायात्रा में उसके साथ रहता है बल्कि कई बार अपनी नई अपेक्षाएं सामने लाकर उसे प्रयोग की नई दिशा में अग्रसर होने के लिए बाध्य भी करता है। एक लेख और उसके पाठक वर्ग की यह सहयात्रा यदि जीवन-भर बनी रहे,
तो काफी सुखद हो सकती है। परन्तु संभावना यह भी है कि एक मुकाम ऐसा आ जाए, जहां मनोवेगों की प्रक्रिया बिलकुल अलग हो जाने से लेखक एकदम अकेला पड़ जाए। यह अकेलापन आगे चलकर उसे एक नये पाठक समुदाय से जोड़ भी सकता है और अपने तक सीमित रहकर टूट जाने के लिए विवश भी कर सकता है। परन्तु रचना के समय इस इतिहास-संदर्भ की बात सोचना ग़लत है।
मैंने अपनी शुरू-शुरू की कहानियां जिन दिनों लिखीं- उनमें से कई एक इन्सान के खंडहर में भी संकलित नहीं हैं- उन दिनों कई कारणों से मैं अपने को अपने तब तक के परिवेश से बहुत कटा हुआ महसूस करता था। जिन व्यक्तियों और संस्कारों के बीच पलकर बड़ा हुआ था, उनके खोखलेपन को लेकर मन में गहरी कटुता और वितृष्णा थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सिर पर होने से उसे निभाने की मजबूरी से मन छटपटाता था। मैं किसी तरह अपने को विरासत के सब संबंधों से मुक्त कर लेना चाहता था परन्तु मुक्ति का कोई उपाय नहीं था।
छोटा भाई इतना छोटा था, बड़ा बहिन इतनी संस्कार-ग्रस्त और मां इतनी असहाय कि मेरी ‘स्वतन्त्रता’ की भूख कोरी मानसिक उड़ान के सिवा कुछ नहीं रखती थी। मेरी शुरू की कहानियां इसी मानसिकता की उपज थीं। एक छोटा-सा दायरा था, तीन-चार दोस्तों का। वे सब भी किसी-न-किसी रूप में अपने-अपने परिवेश से ऊबे या कटे हुए लोग थे। किसी भी रचना की सार्थकता इसी में थी कि कहां तक उससे उस दायरे की मानसिक अपेक्षाओं की पूर्ति होती है।
हममें से दो आदमी, मैं और मेरा एक साथी, संस्कृत में एम.ए. कर चुके थे; एक अंग्रेजी में एम.ए. कर रहा था और दो-एक लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। मेरे संस्कृत के सहपाठी को छोड़कर हम सबके लिए लाहौर की ज़िन्दगी नई चीज़ थी और हम लोग ज़्यादा-से-ज़्यादा समय घर से बाहर रहने के लिए पूरा-पूरा दिन माल पर काफी़ हाउस और चेन्नीज़ लंच होम से लेकर स्टौंडर्स और लारेंस बार के बीच बिता दिया करते थे।
हमें इस ‘जीवन-बोध’ में दीक्षित करने वाला व्यक्ति मेरा सहपाठी ही था जो पंजाब मंत्रिमण्डल के एक सदस्य का दत्तक पुत्र होने के नाते हम सबसे अधिक साधन-सम्पन्न था और पहले से माल रोड की बार-रेस्तरां दुनिया से घनिष्ठता रखता था। क्योंकि जुमलेबाजी उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, इसलिए हम सब उससे प्रभावित होने के कारण काफ़ी हाउस से लेकर साहित्य तक हर जगह को सिर्फ़ ज़ुमलेबाजी का अखाड़ा मानते थे।
‘एक अच्छे जुमले के सामने दोस्त भी बहुत छोटी चीज़ है’- इस दृष्टि को लेकर चलनेवाले हम चार-पांच ‘जीनियस’ एक तो हर मिलने वाले पर अपनी कला अज़माते रहते थे, दूसरे उस सारे साहित्य को बेकार समझते थे, जिसमें ज़ुमलेबाजी का चटखारा न हो। अगर हमें मंटो जैसे लेखक की कहानियां पसंद आती थीं तो अपनी शिल्प या कथ्य के कारण नहीं बल्कि उस ज़ुमलेबाजी की वजह से ही जो मंटो की भी खासी कमजोरी थी। इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं था कि अपने ढंग से हम भी अपनी कहानियों में ज़ुमलेबाज़ी का अभ्यास करते।
पर उसी शब्द के अतिरिक्त मोह के कारण आज उस समय की रचनाएँ इतनी बेगाना लगती हैं कि उनमें से किसी एक को यहां केवल उदाहरण के रूप में रख लेने को भी मन नहीं हुआ।
‘इन्सान का खंडहर’ के बाद मेरा दूसरा कहानी-संग्रह था- ‘नए बादल’। दोनों के प्रकाशन में सात साल का अन्तर है। ‘इंसान के खंडहर’ सन् पचास में प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, ‘नए बादल’ सन् सत्तावन में भारतीय ज्ञानपीठ से। उसके कुछ ही महीने बाद सन् अट्ठावन के आरंभ में, ‘राजकमल प्रकाशन’ से ‘जानवर और जानवर’ का कहानियां दो अलग-अलग संग्रहों में संकलित होने पर भी मेरे कहानी-लेखन के एक ही दौर की कहानियां हैं
जिसका आरम्भ सन् चौवन से होता है। सन् पचास से सन् चौवन के बीच एक लंबे अरसे तक मैंने कहानियां लगभग नहीं लिखीं। केवल दो कहानियां लिखीं। केवल दो कहानियां लिखीं थीं शायद- एक ‘पंखयुक्त ट्रेजड़ी’ और एक ‘छोटी-सी चीज़’ जो दोनों प्रतीकों में प्रकाशित हुई थीं। एक और कहानी, जो उस समय ‘सरगम’ में छपी, वह सन् पचास में लिखी जा चुकी थी।
सन् पचास से सन् चौवन के बीच का समय मेरे लिए काफी उथल-पुथल का समय था। विभाजन के बाद काफ़ी दिनों तक बेकारी की मार सहने के बाद मुम्बई के शिक्षा विभाग में जो लेक्चररशिप मिली थी, वह सन् उनचास में छिन गई थी, कारण था आँखों का निर्धारित सीमा से अधिक कमज़ोर होना।
उसके बाद बेरोज़गारी के कुछ दिन दिल्ला में कटे फिर जालंधर के डी.ए.वी. कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई। लेकिन छ: महीने बाद, सन् पचास से शुरू में, बिना कन्फर्म किए उस नौकरी से भी हटा दिया गया। इस बार कारण था, टीचर्ज़ यूनियन की गतिविधि में सक्रिय भाग लेना। जिन साथियों के भरोसे अधिकारियों की दमन-नीति का विरोध किया था, उनके बिदक जाने से खासा मोह-भंग हुआ।
बेरोज़गारी का आतंक नये सिर से सिर पर आ जाने से काफी़ दौड़-धूप करके शिमला के बिशप काटन स्कूल में नौकरी कर ली, परन्तु उत्तरोत्तर मोहभंग की प्रक्रिया उसके वर्षों तक चलती रही। जीवन के उखड़ेपन को समेटने के इरादे से सन् पचास के अन्त में विवाह कर लिया, पर वह भी एक और स्तर पर मोह-भंग की शुरूआत थी। सन् बावन तक आते-आते परिस्थितियों की पकड़ इस तरह कसने लगी थी कि आखिर नौकरी छोड़ दी। तय किया कि जैसे भी हो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए, केवल लेखन पर निर्भर रहकर न्यूनतम साधनों में से ग़ुजारा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह अभियान भी ज्यादा दिन नहीं चल सका।
सन् तिरेपन के शरू के कुछ महीने तो किसी तरह निकल गए पर उसके बाद नए सिरे से नौकरी की तलाश में जुट जाना पड़ा। कई जगह कोशिश कर चुकने के बाद जब मन लगभग हारने लगा, तो एक व्यंग्यत्मक स्थिति सामने आई। जालंधर के डी.ए.वी. कॉलेज में, जहाँ तीन साल पहले हिन्दी विभाग में पाँचवी जगह पर कन्फर्म नहीं किया गया था, वहीं अब विभागाध्यक्ष के रूप में में बुला लिया गया।
जिन साथियों के बीच सो गया था, उनमें से कोई-एक अब भी वहां थे। मुझे नौकरी मिल गई, पर मोह-भंग की वह प्रक्रिया, जो वहां से जाने के समय शुरू हुई थी, तब तक वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कई-कई स्तरों पर अपने चरम तक पहुंचने लगी थी।
दूसरी बार जालंधर नौकरी करने से पहले ख़ानाबदोशी के दौरे में कहानियां नहीं लिखी गई। बिशप काटन स्कूल से नौकरी छोड़ने और डी.ए.वी. कालेज, जालंधर में वापस आने के बीच केवल पश्चिमी समुद्र-तट का यात्रा-विवरण लिखा जो ‘आख़िरी चट्टान तक’ शीर्षक से ‘प्रगति प्रकाशन’ से ही प्रकाशित हुआ।
लम्बे अरसे के बाद जो पहली कहानी लिखी उसका शीर्षक था, ‘सौदा’ यह कहानी, जो कि कहानी में प्रकाशित हुई, मेरी पहले की कहानियों से इतनी अलग थी कि एक तरह से उसे मेरे लेखन के उस दौर की शुरुआत माना जा सकता है जिसमें आगे चलकर ‘उसकी रोटी’, ‘मंदी’, ‘मलवे का मालिक’ और ‘जानवर और जानवर’ जैसी कहानियां लिखी गई। ‘इंसान के खंडहर’ से इस दौर तक आते-आते ओढ़ी हुई बौद्धिकता के कोने काफी झड़ गये थे।
इसलिये जो कहानियां मैंने इस संग्रह के लिए चुनी हैं, उनके चुनाव का कोई कारण दे सकना मेरे लिए बहुत कठिन है। कहना नहीं हो, तो केवल इतना कहा जा सकता है कि इस बार अपनी कहानियों में से गुजरते हुए इन कहानियों पर उंगली ठहरती गई। ‘आर्द्रा’, ‘मिस पाल’ तथा ‘एक और ज़िंदगी’ जैसी कुछ अधिक प्रसिद्ध कहानियां आज मेरे समर्थन की अपेक्षा नहीं रखतीं।
चुनाव करने में मेरी एक दृष्टि अवश्य रही है कि संग्रह की कहानियां मेरी आज की कथायात्रा के प्राय: सभी पड़ावों का प्रतिनिधित्व कर सकें। केवल ‘इंसान के खंडहर’ शीर्षक संग्रह से मेरे बाद के प्रयोगों के साथ एक कड़ी के रूप में ठीक से जुड़ नहीं पाती। उनके शिल्प और कथ्य दोनों में एक तरह की ‘कोशिश’ है, एक निश्चित तलाश का कच्चापन ! यूं पाठकों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे आज भी मेरी वही कहानियां सबसे अधिक पसंद हैं।
यह आवश्यक नहीं कि एक लेखक के साथ-साथ उसके सभी पाठक उसकी बदलती मानसिकता के सब पड़ावों से गुजरते रहें। हर पड़ाव पर किन्हीं पाठकों के साथ उसके एक लेखक का संबंध टूट जाता है, और वहीं से एक नये वर्ग के साथ उसके संबंध की शुरुआत हो जाती है। ऐसा न होना एक लेखक की जड़ता का प्रमाण होगा। जीवन-भर एक ही मानसिक भूमि पर रहकर रचना करते जाना केवल शब्दों का व्यवसाय है,
और कुछ नहीं। लेकिन इस स्थिति के विपरीत पाठकों का एक दूसरा वर्ग भी हैं, जो न केवल लेखक की पूरी रचनायात्रा में उसके साथ रहता है बल्कि कई बार अपनी नई अपेक्षाएं सामने लाकर उसे प्रयोग की नई दिशा में अग्रसर होने के लिए बाध्य भी करता है। एक लेख और उसके पाठक वर्ग की यह सहयात्रा यदि जीवन-भर बनी रहे,
तो काफी सुखद हो सकती है। परन्तु संभावना यह भी है कि एक मुकाम ऐसा आ जाए, जहां मनोवेगों की प्रक्रिया बिलकुल अलग हो जाने से लेखक एकदम अकेला पड़ जाए। यह अकेलापन आगे चलकर उसे एक नये पाठक समुदाय से जोड़ भी सकता है और अपने तक सीमित रहकर टूट जाने के लिए विवश भी कर सकता है। परन्तु रचना के समय इस इतिहास-संदर्भ की बात सोचना ग़लत है।
मैंने अपनी शुरू-शुरू की कहानियां जिन दिनों लिखीं- उनमें से कई एक इन्सान के खंडहर में भी संकलित नहीं हैं- उन दिनों कई कारणों से मैं अपने को अपने तब तक के परिवेश से बहुत कटा हुआ महसूस करता था। जिन व्यक्तियों और संस्कारों के बीच पलकर बड़ा हुआ था, उनके खोखलेपन को लेकर मन में गहरी कटुता और वितृष्णा थी। घर की पूरी जिम्मेदारी सिर पर होने से उसे निभाने की मजबूरी से मन छटपटाता था। मैं किसी तरह अपने को विरासत के सब संबंधों से मुक्त कर लेना चाहता था परन्तु मुक्ति का कोई उपाय नहीं था।
छोटा भाई इतना छोटा था, बड़ा बहिन इतनी संस्कार-ग्रस्त और मां इतनी असहाय कि मेरी ‘स्वतन्त्रता’ की भूख कोरी मानसिक उड़ान के सिवा कुछ नहीं रखती थी। मेरी शुरू की कहानियां इसी मानसिकता की उपज थीं। एक छोटा-सा दायरा था, तीन-चार दोस्तों का। वे सब भी किसी-न-किसी रूप में अपने-अपने परिवेश से ऊबे या कटे हुए लोग थे। किसी भी रचना की सार्थकता इसी में थी कि कहां तक उससे उस दायरे की मानसिक अपेक्षाओं की पूर्ति होती है।
हममें से दो आदमी, मैं और मेरा एक साथी, संस्कृत में एम.ए. कर चुके थे; एक अंग्रेजी में एम.ए. कर रहा था और दो-एक लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। मेरे संस्कृत के सहपाठी को छोड़कर हम सबके लिए लाहौर की ज़िन्दगी नई चीज़ थी और हम लोग ज़्यादा-से-ज़्यादा समय घर से बाहर रहने के लिए पूरा-पूरा दिन माल पर काफी़ हाउस और चेन्नीज़ लंच होम से लेकर स्टौंडर्स और लारेंस बार के बीच बिता दिया करते थे।
हमें इस ‘जीवन-बोध’ में दीक्षित करने वाला व्यक्ति मेरा सहपाठी ही था जो पंजाब मंत्रिमण्डल के एक सदस्य का दत्तक पुत्र होने के नाते हम सबसे अधिक साधन-सम्पन्न था और पहले से माल रोड की बार-रेस्तरां दुनिया से घनिष्ठता रखता था। क्योंकि जुमलेबाजी उसकी बहुत बड़ी विशेषता थी, इसलिए हम सब उससे प्रभावित होने के कारण काफ़ी हाउस से लेकर साहित्य तक हर जगह को सिर्फ़ ज़ुमलेबाजी का अखाड़ा मानते थे।
‘एक अच्छे जुमले के सामने दोस्त भी बहुत छोटी चीज़ है’- इस दृष्टि को लेकर चलनेवाले हम चार-पांच ‘जीनियस’ एक तो हर मिलने वाले पर अपनी कला अज़माते रहते थे, दूसरे उस सारे साहित्य को बेकार समझते थे, जिसमें ज़ुमलेबाजी का चटखारा न हो। अगर हमें मंटो जैसे लेखक की कहानियां पसंद आती थीं तो अपनी शिल्प या कथ्य के कारण नहीं बल्कि उस ज़ुमलेबाजी की वजह से ही जो मंटो की भी खासी कमजोरी थी। इसलिए यह अस्वाभाविक नहीं था कि अपने ढंग से हम भी अपनी कहानियों में ज़ुमलेबाज़ी का अभ्यास करते।
पर उसी शब्द के अतिरिक्त मोह के कारण आज उस समय की रचनाएँ इतनी बेगाना लगती हैं कि उनमें से किसी एक को यहां केवल उदाहरण के रूप में रख लेने को भी मन नहीं हुआ।
‘इन्सान का खंडहर’ के बाद मेरा दूसरा कहानी-संग्रह था- ‘नए बादल’। दोनों के प्रकाशन में सात साल का अन्तर है। ‘इंसान के खंडहर’ सन् पचास में प्रगति प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, ‘नए बादल’ सन् सत्तावन में भारतीय ज्ञानपीठ से। उसके कुछ ही महीने बाद सन् अट्ठावन के आरंभ में, ‘राजकमल प्रकाशन’ से ‘जानवर और जानवर’ का कहानियां दो अलग-अलग संग्रहों में संकलित होने पर भी मेरे कहानी-लेखन के एक ही दौर की कहानियां हैं
जिसका आरम्भ सन् चौवन से होता है। सन् पचास से सन् चौवन के बीच एक लंबे अरसे तक मैंने कहानियां लगभग नहीं लिखीं। केवल दो कहानियां लिखीं। केवल दो कहानियां लिखीं थीं शायद- एक ‘पंखयुक्त ट्रेजड़ी’ और एक ‘छोटी-सी चीज़’ जो दोनों प्रतीकों में प्रकाशित हुई थीं। एक और कहानी, जो उस समय ‘सरगम’ में छपी, वह सन् पचास में लिखी जा चुकी थी।
सन् पचास से सन् चौवन के बीच का समय मेरे लिए काफी उथल-पुथल का समय था। विभाजन के बाद काफ़ी दिनों तक बेकारी की मार सहने के बाद मुम्बई के शिक्षा विभाग में जो लेक्चररशिप मिली थी, वह सन् उनचास में छिन गई थी, कारण था आँखों का निर्धारित सीमा से अधिक कमज़ोर होना।
उसके बाद बेरोज़गारी के कुछ दिन दिल्ला में कटे फिर जालंधर के डी.ए.वी. कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई। लेकिन छ: महीने बाद, सन् पचास से शुरू में, बिना कन्फर्म किए उस नौकरी से भी हटा दिया गया। इस बार कारण था, टीचर्ज़ यूनियन की गतिविधि में सक्रिय भाग लेना। जिन साथियों के भरोसे अधिकारियों की दमन-नीति का विरोध किया था, उनके बिदक जाने से खासा मोह-भंग हुआ।
बेरोज़गारी का आतंक नये सिर से सिर पर आ जाने से काफी़ दौड़-धूप करके शिमला के बिशप काटन स्कूल में नौकरी कर ली, परन्तु उत्तरोत्तर मोहभंग की प्रक्रिया उसके वर्षों तक चलती रही। जीवन के उखड़ेपन को समेटने के इरादे से सन् पचास के अन्त में विवाह कर लिया, पर वह भी एक और स्तर पर मोह-भंग की शुरूआत थी। सन् बावन तक आते-आते परिस्थितियों की पकड़ इस तरह कसने लगी थी कि आखिर नौकरी छोड़ दी। तय किया कि जैसे भी हो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए, केवल लेखन पर निर्भर रहकर न्यूनतम साधनों में से ग़ुजारा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यह अभियान भी ज्यादा दिन नहीं चल सका।
सन् तिरेपन के शरू के कुछ महीने तो किसी तरह निकल गए पर उसके बाद नए सिरे से नौकरी की तलाश में जुट जाना पड़ा। कई जगह कोशिश कर चुकने के बाद जब मन लगभग हारने लगा, तो एक व्यंग्यत्मक स्थिति सामने आई। जालंधर के डी.ए.वी. कॉलेज में, जहाँ तीन साल पहले हिन्दी विभाग में पाँचवी जगह पर कन्फर्म नहीं किया गया था, वहीं अब विभागाध्यक्ष के रूप में में बुला लिया गया।
जिन साथियों के बीच सो गया था, उनमें से कोई-एक अब भी वहां थे। मुझे नौकरी मिल गई, पर मोह-भंग की वह प्रक्रिया, जो वहां से जाने के समय शुरू हुई थी, तब तक वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कई-कई स्तरों पर अपने चरम तक पहुंचने लगी थी।
दूसरी बार जालंधर नौकरी करने से पहले ख़ानाबदोशी के दौरे में कहानियां नहीं लिखी गई। बिशप काटन स्कूल से नौकरी छोड़ने और डी.ए.वी. कालेज, जालंधर में वापस आने के बीच केवल पश्चिमी समुद्र-तट का यात्रा-विवरण लिखा जो ‘आख़िरी चट्टान तक’ शीर्षक से ‘प्रगति प्रकाशन’ से ही प्रकाशित हुआ।
लम्बे अरसे के बाद जो पहली कहानी लिखी उसका शीर्षक था, ‘सौदा’ यह कहानी, जो कि कहानी में प्रकाशित हुई, मेरी पहले की कहानियों से इतनी अलग थी कि एक तरह से उसे मेरे लेखन के उस दौर की शुरुआत माना जा सकता है जिसमें आगे चलकर ‘उसकी रोटी’, ‘मंदी’, ‘मलवे का मालिक’ और ‘जानवर और जानवर’ जैसी कहानियां लिखी गई। ‘इंसान के खंडहर’ से इस दौर तक आते-आते ओढ़ी हुई बौद्धिकता के कोने काफी झड़ गये थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book