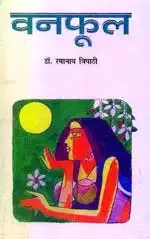|
जीवनी/आत्मकथा >> वनफूल वनफूलरमानाथ त्रिपाठी
|
84 पाठक हैं |
||||||
लेखक की आत्मकथा के इस प्रथम खण्ड ‘वनफूल’ में उपन्यास जैसी सरसता, कविता-जैसी भाव प्रणवता और शोध जैसी प्रबुद्धता है।
Vanphool - A hindi Book by - Ramnath Tripathi वनफूल - रमानाथ त्रिपाठी
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
वनफूल में उपन्यास जैसी सरसता, कविता-जैसी भाव प्रणवता और शोध जैसी प्रबुद्धता है। माँ ने शिशु को घुट्टी में रामकथा प्रेम दिया था। शैशव से ही वे क्रांतिकारियों की देशभक्ति से प्रभावित हुए। उन्हें सरकारी कोप भी सहना पड़ा। छात्र-जीवन में उन्हें कहीं से आर्थिक सहायता नहीं मिली। केवल एक जून भोजन करते हुए ट्यूशन और छात्र-वृत्ति के बल पर उन्होंने शिक्षा पूरी की। आत्मकथा में ऐसे लोकतत्त्वों का भी समावेश है जो आधुनिक सभ्यता की तड़क-भड़क में लुप्त होते जा रहे हैं। वनफूल के माध्यम से ये लोकतत्त्व इतिहास के दस्तावेज बन जायंगे। विभिन्न स्थितियों का चित्रात्मक वर्णन भी इस आत्मकथा की विशेषता है। वनफूल नारी प्रसंगों में भी अनूठी शुचिता है। हिन्दी की आत्मकथात्मक परम्परा में इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है।
एक आत्मकथा रचना जिसमें लेखक के बचपन से प्रारम्भ होकर उसके जीवन के उतार-चढ़ाव, संघर्ष का बहुत ही सजीव, सरस चित्रण है।
एक पिछड़े ग्राम का साधारण व्यक्ति कैसे अपनी ईमानदारी और श्रम से जीवन में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। एक जीवंत आत्मकथा जो उपन्यास से भी अधिक रोचक है।
एक आत्मकथा रचना जिसमें लेखक के बचपन से प्रारम्भ होकर उसके जीवन के उतार-चढ़ाव, संघर्ष का बहुत ही सजीव, सरस चित्रण है।
एक पिछड़े ग्राम का साधारण व्यक्ति कैसे अपनी ईमानदारी और श्रम से जीवन में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। एक जीवंत आत्मकथा जो उपन्यास से भी अधिक रोचक है।
प्राक्क्थन
मेरे जीवन का अधिकांश समय शोध-कार्य में बीत गया। मूलत: मैं कोमल मन का कवि और कथाकार हूँ। अब वृद्धावस्था में न गंभीर शोध का सामर्थ्य है और न गंभीर लेखन का। निष्क्रिय होकर चुप बैठते भी नहीं बनता। मेरे प्रिय शिष्य-शिष्याओं ने प्रेरित किया कि मैं आत्मकथा लिखूँ। मैंने भी सोचा कि जब गंभीर लेखन नहीं हो सकता तो ऐसा ही सही। आत्मकथा लिखने में मेरे भीतर बैठे रचनाकार को भी परितोष मिलेगा।
कहा जाता है कि आत्मकथा लिखना एक दुष्कर कार्य है। इसे तटस्थ होकर लिखा जाना चाहिए। महान् लेखकों के लिए दुष्कर कार्य होगा, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। सारी घटनाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के (और मेरे अपने भी) उज्ज्वल और कृष्ण पक्ष होते हैं। पाठक के मन पर उज्ज्वल पक्ष छाए या न छाए कृष्ण-पक्ष अवश्य ही छा जाता है। मुझे यहाँ सावधान होना पड़ा है। कई कृष्ण-पक्षों को मैं टाल गया हूँ। कई नाम ज्यों के त्यों हैं और कई नाम बदल दिए हैं। जो सत्य नाम हैं उनके कृष्ण-पक्ष छिपा गया हूँ।
मैंने तटस्थ होकर लिखने की चेष्टा तो की है, किन्तु स्वभाव का आवेशी हूँ, अत: कई स्थलों पर तटस्थ नहीं रह सका रहूँ। मैंने कभी डायरियाँ लिखना प्रारम्भ किया था, फिर सारी पुरानी डायरियाँ नष्ट कर दीं। अब मुझे जो याद आता गया वही लिखते गया। मैंने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे सही हैं, क्रम आगे-पीछे का हो गया है।
मेरे जीवन के कई ऐसे अंश हैं जिन्हें बारीकी के साथ व्यक्त किया जाता है तो उपन्यास जैसा आनन्द आता है और आत्मकथा बहुत ही धारदार हो जाती, किन्तु तब इसका आकार तिगुना बड़ा हो जाता। आज पाठक के पास इतना समय कहाँ है कि वह किसी की आत्मकथा में अपना सिर खपाए।
आत्मकथा के इस प्रथम खण्ड ‘वनफूल’ में मेरे जन्म-स्थान क्योंटरा से लेकर कानपुर तक के संस्मरण होंगे। मैंने कहीं-कहीं पर कोष्ठक (ब्रैकेट) का प्रयग किया है, विशेषत: वहाँ जहाँ किसी तथ्य का वर्णन करते-करते क्रम तोड़कर आगे की बात कही है।
मैं तन-मन-धन से राष्ट्र के लिए समर्पित कहा हूँ। तुच्छ स्वार्थों के लिए मैंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। साहित्कार भी गुट बनाकर आगे बढ़ते हैं, मैं निपट अकेला हूँ। समाज, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में कोई भी समर्थ व्यक्ति मेरा पक्षधर या पृष्ठ-पोषक नहीं। मेरा एक छोटा-सा संसार अवश्य है, जिसमें प्रबुद्ध विनीत छात्र, कुछ प्रिय जन और अपनत्व देने वाला पाठक-समुदाय। प्रत्येक व्यक्ति ही समाज और परम्परा से बहुत-कुछ पाता है, मैंने भी पाया है। मैं भले ही गोटें बिठाकर लाभकारी ऊँचें पदों पर आसीन नहीं हो सका हूँ, तथापि मैंने आगे की पीढी़ को कुछ संस्कार दिए है। मुझे पूर्ववर्ती जनों से प्रकाश मिला है। मैंने भी मिट्टी के छोटे-छोटे दीप जलाए हैं। मुझे पूर्ववर्ती जनों से प्रकाश मिला है। मैंने भी मिट्टी के छोटे-छोटे दीप जलाए हैं, जो आगे तक प्रकाश-परम्परा को जीवन्त रखेंगे।
संस्मरण लिखने में मेरी सबसे बड़ी बाधा हैं पत्नी हेम पुत्र अजय, इनके डर से मुझे आत्मकथा से कई तथ्य हटाने पड़े हैं। इससे कई वर्णन फीके पड़ गए होंगे।
मेरे प्रिय जन-प्रो. एस. तंकमणि अम्मा (तिरुअनन्तपुरम्), प्रो.टी. राजेश्वरानन्द शर्मा (तिरुपति), डा. रमेशचन्द्र शर्मा (कानपुर), डा. रामपत यादव (कुरुक्षेत्र) और डा. रामनिवास शर्मा (पटियाला) मुझे आत्मकथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए उत्साहित करते रहे, ताकि मेरे साहित्य पर शोध-कार्य करने वाले उनके छात्र लाभान्वित हो सकें। बन्धुवर डॉ. हर गुलाल गुप्त ने पाण्डुलिपि पढ़कर विस्तृत समीक्षा लिखी है और उपयोगी सुझाव भी दिए हैं।
आत्मकथा के कुछ अंश ‘साहित्य अमृत’, ‘साहित्य परिक्रमा’, ‘कादम्बिनी’ (दिल्ली), ‘तुलसी मानस भारती’ (भोपाल),
‘तुलसी-प्रभा’ (जमशेदपुर), ‘गुर्जर राष्ट्रवीणा’ (अहमदाबाद), ‘वीणा’ (इन्दौर), ‘संयोग साहित्य’ (मुम्बई) और ‘वसन्त’ (मारीशस) में प्रकाशित हुए हैं। इन्हें पढ़कर दद्दा विष्णु प्रभाकर जी, प्राचार्य डॉ. अरुणा सीतेश, प्रो. सियाराम तिवारी (पटना) प्रो. भूपेन्द्र रायचौधरी (गुवाहाटी), प्रो. प्रभात कुमार पाण्डेय (काशी), डॉ. गोपाल बाबू शर्मा (अलीगढ़), डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी और श्री जुगल कुशोर जैथलिया (कोलकाता) ने प्रशंसा भरे पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहित किया है।
इसी प्रकाशन से मेरे दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं-‘शंख सिन्दूर’ और ‘रामगाथा’, प्रथम उपन्यास बांगलादेशीय गाथा-गीतों पर आधारित ऐतिहासिक और आंचलिक कृति है। ‘रामगाथा’ उपन्यास मुख्यत: वाल्मीकि–रामायण के आधार पर लिखा गया है। मैंने इसे जन-जीवन से भी जोड़ा है। यो दोनों कृतियाँ चर्चित, अन्य भाषाओं में अनुदित और पुरस्कृत हुई हैं।
अब यह तुच्छ कृति पाठकों के कर-कमलों में समर्पित है। पता नहीं जंगल से घिरे क्योंटरा में उगा यह वनफूल उन्हें अपने खटमिट्ठे अनुभवों से प्रभावित कर भी पाएगा !
कहा जाता है कि आत्मकथा लिखना एक दुष्कर कार्य है। इसे तटस्थ होकर लिखा जाना चाहिए। महान् लेखकों के लिए दुष्कर कार्य होगा, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। सारी घटनाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के (और मेरे अपने भी) उज्ज्वल और कृष्ण पक्ष होते हैं। पाठक के मन पर उज्ज्वल पक्ष छाए या न छाए कृष्ण-पक्ष अवश्य ही छा जाता है। मुझे यहाँ सावधान होना पड़ा है। कई कृष्ण-पक्षों को मैं टाल गया हूँ। कई नाम ज्यों के त्यों हैं और कई नाम बदल दिए हैं। जो सत्य नाम हैं उनके कृष्ण-पक्ष छिपा गया हूँ।
मैंने तटस्थ होकर लिखने की चेष्टा तो की है, किन्तु स्वभाव का आवेशी हूँ, अत: कई स्थलों पर तटस्थ नहीं रह सका रहूँ। मैंने कभी डायरियाँ लिखना प्रारम्भ किया था, फिर सारी पुरानी डायरियाँ नष्ट कर दीं। अब मुझे जो याद आता गया वही लिखते गया। मैंने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे सही हैं, क्रम आगे-पीछे का हो गया है।
मेरे जीवन के कई ऐसे अंश हैं जिन्हें बारीकी के साथ व्यक्त किया जाता है तो उपन्यास जैसा आनन्द आता है और आत्मकथा बहुत ही धारदार हो जाती, किन्तु तब इसका आकार तिगुना बड़ा हो जाता। आज पाठक के पास इतना समय कहाँ है कि वह किसी की आत्मकथा में अपना सिर खपाए।
आत्मकथा के इस प्रथम खण्ड ‘वनफूल’ में मेरे जन्म-स्थान क्योंटरा से लेकर कानपुर तक के संस्मरण होंगे। मैंने कहीं-कहीं पर कोष्ठक (ब्रैकेट) का प्रयग किया है, विशेषत: वहाँ जहाँ किसी तथ्य का वर्णन करते-करते क्रम तोड़कर आगे की बात कही है।
मैं तन-मन-धन से राष्ट्र के लिए समर्पित कहा हूँ। तुच्छ स्वार्थों के लिए मैंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। साहित्कार भी गुट बनाकर आगे बढ़ते हैं, मैं निपट अकेला हूँ। समाज, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में कोई भी समर्थ व्यक्ति मेरा पक्षधर या पृष्ठ-पोषक नहीं। मेरा एक छोटा-सा संसार अवश्य है, जिसमें प्रबुद्ध विनीत छात्र, कुछ प्रिय जन और अपनत्व देने वाला पाठक-समुदाय। प्रत्येक व्यक्ति ही समाज और परम्परा से बहुत-कुछ पाता है, मैंने भी पाया है। मैं भले ही गोटें बिठाकर लाभकारी ऊँचें पदों पर आसीन नहीं हो सका हूँ, तथापि मैंने आगे की पीढी़ को कुछ संस्कार दिए है। मुझे पूर्ववर्ती जनों से प्रकाश मिला है। मैंने भी मिट्टी के छोटे-छोटे दीप जलाए हैं। मुझे पूर्ववर्ती जनों से प्रकाश मिला है। मैंने भी मिट्टी के छोटे-छोटे दीप जलाए हैं, जो आगे तक प्रकाश-परम्परा को जीवन्त रखेंगे।
संस्मरण लिखने में मेरी सबसे बड़ी बाधा हैं पत्नी हेम पुत्र अजय, इनके डर से मुझे आत्मकथा से कई तथ्य हटाने पड़े हैं। इससे कई वर्णन फीके पड़ गए होंगे।
मेरे प्रिय जन-प्रो. एस. तंकमणि अम्मा (तिरुअनन्तपुरम्), प्रो.टी. राजेश्वरानन्द शर्मा (तिरुपति), डा. रमेशचन्द्र शर्मा (कानपुर), डा. रामपत यादव (कुरुक्षेत्र) और डा. रामनिवास शर्मा (पटियाला) मुझे आत्मकथा शीघ्र पूर्ण करने के लिए उत्साहित करते रहे, ताकि मेरे साहित्य पर शोध-कार्य करने वाले उनके छात्र लाभान्वित हो सकें। बन्धुवर डॉ. हर गुलाल गुप्त ने पाण्डुलिपि पढ़कर विस्तृत समीक्षा लिखी है और उपयोगी सुझाव भी दिए हैं।
आत्मकथा के कुछ अंश ‘साहित्य अमृत’, ‘साहित्य परिक्रमा’, ‘कादम्बिनी’ (दिल्ली), ‘तुलसी मानस भारती’ (भोपाल),
‘तुलसी-प्रभा’ (जमशेदपुर), ‘गुर्जर राष्ट्रवीणा’ (अहमदाबाद), ‘वीणा’ (इन्दौर), ‘संयोग साहित्य’ (मुम्बई) और ‘वसन्त’ (मारीशस) में प्रकाशित हुए हैं। इन्हें पढ़कर दद्दा विष्णु प्रभाकर जी, प्राचार्य डॉ. अरुणा सीतेश, प्रो. सियाराम तिवारी (पटना) प्रो. भूपेन्द्र रायचौधरी (गुवाहाटी), प्रो. प्रभात कुमार पाण्डेय (काशी), डॉ. गोपाल बाबू शर्मा (अलीगढ़), डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी और श्री जुगल कुशोर जैथलिया (कोलकाता) ने प्रशंसा भरे पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहित किया है।
इसी प्रकाशन से मेरे दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं-‘शंख सिन्दूर’ और ‘रामगाथा’, प्रथम उपन्यास बांगलादेशीय गाथा-गीतों पर आधारित ऐतिहासिक और आंचलिक कृति है। ‘रामगाथा’ उपन्यास मुख्यत: वाल्मीकि–रामायण के आधार पर लिखा गया है। मैंने इसे जन-जीवन से भी जोड़ा है। यो दोनों कृतियाँ चर्चित, अन्य भाषाओं में अनुदित और पुरस्कृत हुई हैं।
अब यह तुच्छ कृति पाठकों के कर-कमलों में समर्पित है। पता नहीं जंगल से घिरे क्योंटरा में उगा यह वनफूल उन्हें अपने खटमिट्ठे अनुभवों से प्रभावित कर भी पाएगा !
26 वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली, 110088
रमानाथ त्रिपाठी
वनफूल
बीहड़ से घिरा मेरा क्योंटरा गाँव यमुना के किनारे बसा है। क्योंटरा-केवटरा-केवटों के रहने का स्थान। संस्कृत पाठशाला के बाहर टँगे नामपट पर लिखा रहता है कैवर्तनगर, इष्टिकापुरी। इष्टिकापुरी अर्थात् इटावा। अब यह गाँव इटावा नहीं, औरेया जिला के अन्तर्गत है। मेरे गाँव में ककइया ईंटों की बनी कई हवेलियाँ, अनेक कुएँ और अनेक विचित्र प्रकार के मन्दिर हैं।
गाँव के पूरब और पश्चिम में बीहड़ है, दक्षिण की ओर यमुना नदी है। उत्तर की ओर कुछ खेत और कुछ बीहड़ हैं। इस ओर से ही यह जनपद के अंश से जुड़ा है। पूरब में गढ़ी थी, अर्थात् छोटा किला। कायस्थ लोग तोंपे लेकर आए। उन्होंने यह गढ़ी ध्वस्त कर दी और गाँव बसाया। उन्होंने पाठक, मिश्र और पाण्डेय वंश के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बसाकर उन्हें जमीन दे दी। कायस्थ लोग अपने पुरोहित ब्राह्मणों को पालागन करते और ब्राह्मण लोग उन्हें अपना छोटा-सा राजा मानकर सम्मान देते। कायस्थों की कई हवेलियाँ हैं। अब इनमें चमगादड़ और अबाबील अड्डा जमाए हुए हैं। गाँव के ब्राह्मणों ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, स्थान कायस्थ जमींदारों ने दिया था। इसके पास पत्थर की पेटियों का शिव-मन्दिर है, इसमें ईंट और लोहा का प्रयोग नहीं है। खेतों की ओर कुँआ स्थित है, इसके लंबे हौज में चमड़े के पुर से खींचकर पानी भरा जाता है। इस प्रकार गर्मी में पशुओं की प्याऊ तैयार की जाती है। यमुना मील भर दूर है, सभी पशु वहाँ नहीं पहुँच पाते। गर्मी में तलैयाँ सूख जाती हैं। यह प्याऊ पशुओं के जीवन का आधार है।
पूरब के बीहड़ के ढूह (टीले) के ऊपर दो खम्बे आज भी दिखाई देते हैं। ये बहुत ही मजबूत हैं। इनके चारों ओर छोटे-छोटे कई ढूँह हैं जो मेरी झरबेरी, करील, छयोंकर, बबूल आदि के पेड़-पौधों से आच्छादित रहते हैं। पेड़-पौधों को बकरियाँ खा जाती हैं और इन्हें बढ़ने नहीं देतीं। जंगल के बीच-बीच कुछ पुरानी ईंटें और चूड़ी के टुकड़े आदि पड़े रहते हैं। विश्वास नहीं होता कि यह बीहड़ कभी जीते-जागते मानवों से भरी गढ़ी थी। ध्वस्त गढ़ी से दूर हटकर एक शिवलिंग है। खेतों की ओर कुँआ है, जिसके पास विशाल बरगद है। ये सभी किसी समय गढ़ी की सीमा के भीतर ही रहे होंगे।
दक्षिण की ओर खेत पारकर हम यमुना की कगार पर पहुँच जाते हैं। खूब नीचे यमुना लेटी दिखाई देती है। यहाँ का करमुखा घाट स्नान-घाट है तो श्मशान घाट भी हैं। घाट के पास ऊँचे टीले पर बसा छोटा-सा गौहानी गाँव है। यह केवटों की बस्ती है, कुछ कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी रहते हैं। पहले यो केवट क्योंटरा रहते होंगे, इसीलिए हमारा गाँव क्योंटरा-केवटों के रहने का स्थान कहलाया। हमारा गाँव-गौहानी-वासियों के लिए शहर है। दस्यु फूलन देई का प्रेमी विक्रम मल्लाह गौहानी का ही था। गाँव के चम्बल जैसे खारों में फूलन देई राईफल और लाउड़ स्पीकर लिए घूमी है।
गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर भदौरा घाट है। यहाँ पहुंचने के लिए लगभग एक किलोमीटर का बीहड़ी रास्ता भी पार करना पड़ता है। भदौरा घाट का लम्बा-चौड़ा विशाल भाग चट्टानी कठोर मिट्टी का बना है। बरसात में भी उफनती यमुना हजारों वर्षों से इसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करती रही है, किन्तु यह अभी भी सलामत है। इस पत्थरी कठोर घाट ने यमुना को धनुषाकार मोड़ दिया है। यहाँ से ही यह मुड़कर करमुखा घाट की ओर चली जाती है। नदी-तट पर कई शिलाएँ पड़ी हुई हैं। इन पर बैठकर कपड़े धोए हैं। वर्षा ऋतु में यमुना भयानक रूप धारण कर लेती है। भदौरा में एक दो ब्राह्मण परिवार और चार-पाँच मल्लाह परिवार (केवट) परिवार रहते हैं। वर्षा ऋतु में मल्लाह देखते हैं कि कोई मरा पशु या पेड़ बहता आ रहा है तो ये एक विशाल रस्सा किसी पेड़ में बाँध देते हैं, उसका दूसरा छोर अपनी कमर में। ये हनुमान की तरह छलांग लगाकर प्रलयंकारी यमुना में कूंद पड़ते हैं और बहती हुई वस्तु को रस्सी से बाँध देते हैं। ऊँचे तट पर खड़े इनके साथी इन्हें पानी से बाहर खींच लेते हैं। यमुना इन वरुण पुत्रों की जीविका का साधन है। गर्मी में तट पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि उपजाए जाते हैं। तट की बलुही धरती में गड्डा खोदकर कछुए अण्डे दे जाते हैं। ये मल्लाह इन्हें खोदकर खाने के लिए ले जाते हैं।
करमुखा घाट की ओर यमुना इतनी निचाई पर बहती है कि सिंचाई के लिए इसका उपयोग नहीं हो पाता। मेरे यौवन-काल तक सिंचाई का कोई साधन नहीं था, अत: एक ही फसल बोई जाती थी। खरीफ में ज्वार या बाजरा और इसके बीच में उड़द तथा ग्वार बो दिए जाते थे। ग्वार को दर्हारी कहते हैं और इसकी छियाँ (फलियाँ) बैलों को खिलाई जाती हैं। शहर में इसे शाक-सब्जी के रूप में लिया जाता है। ज्वार-बाजरा के बीच कोई-कोई अरहर भी बो देते हैं। फसल कट जाने के बाद भी यह खड़ी रहती है। यह दो फसलों तक चलती हैं। बिहारी का दोहा याद आता है-
गाँव के पूरब और पश्चिम में बीहड़ है, दक्षिण की ओर यमुना नदी है। उत्तर की ओर कुछ खेत और कुछ बीहड़ हैं। इस ओर से ही यह जनपद के अंश से जुड़ा है। पूरब में गढ़ी थी, अर्थात् छोटा किला। कायस्थ लोग तोंपे लेकर आए। उन्होंने यह गढ़ी ध्वस्त कर दी और गाँव बसाया। उन्होंने पाठक, मिश्र और पाण्डेय वंश के कान्यकुब्ज ब्राह्मणों को बसाकर उन्हें जमीन दे दी। कायस्थ लोग अपने पुरोहित ब्राह्मणों को पालागन करते और ब्राह्मण लोग उन्हें अपना छोटा-सा राजा मानकर सम्मान देते। कायस्थों की कई हवेलियाँ हैं। अब इनमें चमगादड़ और अबाबील अड्डा जमाए हुए हैं। गाँव के ब्राह्मणों ने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, स्थान कायस्थ जमींदारों ने दिया था। इसके पास पत्थर की पेटियों का शिव-मन्दिर है, इसमें ईंट और लोहा का प्रयोग नहीं है। खेतों की ओर कुँआ स्थित है, इसके लंबे हौज में चमड़े के पुर से खींचकर पानी भरा जाता है। इस प्रकार गर्मी में पशुओं की प्याऊ तैयार की जाती है। यमुना मील भर दूर है, सभी पशु वहाँ नहीं पहुँच पाते। गर्मी में तलैयाँ सूख जाती हैं। यह प्याऊ पशुओं के जीवन का आधार है।
पूरब के बीहड़ के ढूह (टीले) के ऊपर दो खम्बे आज भी दिखाई देते हैं। ये बहुत ही मजबूत हैं। इनके चारों ओर छोटे-छोटे कई ढूँह हैं जो मेरी झरबेरी, करील, छयोंकर, बबूल आदि के पेड़-पौधों से आच्छादित रहते हैं। पेड़-पौधों को बकरियाँ खा जाती हैं और इन्हें बढ़ने नहीं देतीं। जंगल के बीच-बीच कुछ पुरानी ईंटें और चूड़ी के टुकड़े आदि पड़े रहते हैं। विश्वास नहीं होता कि यह बीहड़ कभी जीते-जागते मानवों से भरी गढ़ी थी। ध्वस्त गढ़ी से दूर हटकर एक शिवलिंग है। खेतों की ओर कुँआ है, जिसके पास विशाल बरगद है। ये सभी किसी समय गढ़ी की सीमा के भीतर ही रहे होंगे।
दक्षिण की ओर खेत पारकर हम यमुना की कगार पर पहुँच जाते हैं। खूब नीचे यमुना लेटी दिखाई देती है। यहाँ का करमुखा घाट स्नान-घाट है तो श्मशान घाट भी हैं। घाट के पास ऊँचे टीले पर बसा छोटा-सा गौहानी गाँव है। यह केवटों की बस्ती है, कुछ कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी रहते हैं। पहले यो केवट क्योंटरा रहते होंगे, इसीलिए हमारा गाँव क्योंटरा-केवटों के रहने का स्थान कहलाया। हमारा गाँव-गौहानी-वासियों के लिए शहर है। दस्यु फूलन देई का प्रेमी विक्रम मल्लाह गौहानी का ही था। गाँव के चम्बल जैसे खारों में फूलन देई राईफल और लाउड़ स्पीकर लिए घूमी है।
गाँव के दक्षिण-पश्चिम की ओर भदौरा घाट है। यहाँ पहुंचने के लिए लगभग एक किलोमीटर का बीहड़ी रास्ता भी पार करना पड़ता है। भदौरा घाट का लम्बा-चौड़ा विशाल भाग चट्टानी कठोर मिट्टी का बना है। बरसात में भी उफनती यमुना हजारों वर्षों से इसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करती रही है, किन्तु यह अभी भी सलामत है। इस पत्थरी कठोर घाट ने यमुना को धनुषाकार मोड़ दिया है। यहाँ से ही यह मुड़कर करमुखा घाट की ओर चली जाती है। नदी-तट पर कई शिलाएँ पड़ी हुई हैं। इन पर बैठकर कपड़े धोए हैं। वर्षा ऋतु में यमुना भयानक रूप धारण कर लेती है। भदौरा में एक दो ब्राह्मण परिवार और चार-पाँच मल्लाह परिवार (केवट) परिवार रहते हैं। वर्षा ऋतु में मल्लाह देखते हैं कि कोई मरा पशु या पेड़ बहता आ रहा है तो ये एक विशाल रस्सा किसी पेड़ में बाँध देते हैं, उसका दूसरा छोर अपनी कमर में। ये हनुमान की तरह छलांग लगाकर प्रलयंकारी यमुना में कूंद पड़ते हैं और बहती हुई वस्तु को रस्सी से बाँध देते हैं। ऊँचे तट पर खड़े इनके साथी इन्हें पानी से बाहर खींच लेते हैं। यमुना इन वरुण पुत्रों की जीविका का साधन है। गर्मी में तट पर ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि उपजाए जाते हैं। तट की बलुही धरती में गड्डा खोदकर कछुए अण्डे दे जाते हैं। ये मल्लाह इन्हें खोदकर खाने के लिए ले जाते हैं।
करमुखा घाट की ओर यमुना इतनी निचाई पर बहती है कि सिंचाई के लिए इसका उपयोग नहीं हो पाता। मेरे यौवन-काल तक सिंचाई का कोई साधन नहीं था, अत: एक ही फसल बोई जाती थी। खरीफ में ज्वार या बाजरा और इसके बीच में उड़द तथा ग्वार बो दिए जाते थे। ग्वार को दर्हारी कहते हैं और इसकी छियाँ (फलियाँ) बैलों को खिलाई जाती हैं। शहर में इसे शाक-सब्जी के रूप में लिया जाता है। ज्वार-बाजरा के बीच कोई-कोई अरहर भी बो देते हैं। फसल कट जाने के बाद भी यह खड़ी रहती है। यह दो फसलों तक चलती हैं। बिहारी का दोहा याद आता है-
सब सूक्यौ बीत्यौ बनौ, ऊखौ लई उखारि।
हरी-हरी अरहरि अजैं, धरि धरहरि जिय नारि।। 135
हरी-हरी अरहरि अजैं, धरि धरहरि जिय नारि।। 135
अरहर के सूखे पौधे (खाडू) कई काम आते हैं। इनमें बराँछा (झाडू) बनता है। ईंधन के भी रूप में इसका प्रयोग होता है। छत बनाने के लिए धन्न (शहतीर) पर खाड़ू बिछाकर अडूस के पत्ते रखे जाते हैं, इन पर मिट्टी बिछाकर कूट दिया जाता है। बस, बन गई वाटर प्रूफ छत। खाडू का एक और उपयोग है। छप्पर छाने के समय बाँसों का या अरण्ड के डंठलों का ढाँचा बनाकर उसे खाडू का खूब मोटा-रस्सा-सा बनाकर जोड़ा जाता है। खाड़ू की खूब पतली टहनियाँ पानी में कई घण्टे डुबाई जाती हैं। ये खूब नरम हो जाती हैं। ढाँचे के ऊपर फूस रखकर इन्हीं भीगी टहनियों से उसे बाँधा जाता है। ये सूखकर कड़ी हो जाती हैं और कई-कई बरसातें झेलकर भी नहीं गलती, जबकि सन की बनी रस्सियाँ गल जाती हैं।
रबी की फसल में चना बोया जाता है, कभी-कभी जौ भी। खेत जोतते समय पठारी धरती पर बड़े-बड़े ढेले उभर आते हैं। इनके बीच चने का पौधा हवा पीता हुआ खूब छिछलता है। यह बिना सिंचाई के भी जिन्दा रहता है। मैंने पाया कि इसी पठारी चने के समान मेरा व्यक्तित्व रहा है। विषम परिस्थितियों के बीच संघर्ष करता हुआ मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे किसी समर्थ या सत्ताधारी व्यक्ति का सहारा प्राय: नहीं ही मिला।
जौ-चना सत्तू बनाने के काम भी आते हैं। चने की रोटी गरीब खाते हैं। यह गेहूँ की तुलना में बहुत सस्ता था। अब तो चना सभी अन्नों का ताऊ हो गया है।
रबी की फसल में चना बोया जाता है, कभी-कभी जौ भी। खेत जोतते समय पठारी धरती पर बड़े-बड़े ढेले उभर आते हैं। इनके बीच चने का पौधा हवा पीता हुआ खूब छिछलता है। यह बिना सिंचाई के भी जिन्दा रहता है। मैंने पाया कि इसी पठारी चने के समान मेरा व्यक्तित्व रहा है। विषम परिस्थितियों के बीच संघर्ष करता हुआ मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे किसी समर्थ या सत्ताधारी व्यक्ति का सहारा प्राय: नहीं ही मिला।
जौ-चना सत्तू बनाने के काम भी आते हैं। चने की रोटी गरीब खाते हैं। यह गेहूँ की तुलना में बहुत सस्ता था। अब तो चना सभी अन्नों का ताऊ हो गया है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book