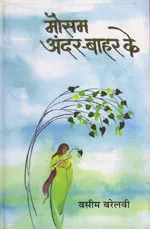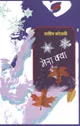|
गजलें और शायरी >> मौसम अंदर-बाहर के मौसम अंदर-बाहर केवसीम बरेलवी
|
444 पाठक हैं |
||||||
वशीम बरेलवी की शायरी में वो रचनात्मकता है, जो इन्सानी ज़िन्दगी के त्रासद पहलू को भरपूर आनन्द के साथ पेश करने में समर्थ है......
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ग़म की मानी हुई हक़ीक़त को मीर तक़ी मीर से लेकर आज तक के शायरों ने साहित्य की विषय-वस्तु बनाया है। हमारी शायरी में इस ग़म की परछाइयाँ मिलती चली आयी हैं, लेकिन हमारे कालखण्ड का विचारक वसीम बरेलवी इस आन्तरिक व्यथा से समाजी और इन्सानी ग़मों का आनन्ददायक उपचार तलाश करता है। उसके यहाँ वह रचनात्मक है, जो इन्सानी ज़िन्दगी के त्रासद पहलू को भरपूर अनुभूति के साथ रेश करने में समर्थ है और उसके आनन्द और उत्साहवर्द्धक भविष्य को जन्म देने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने प्रयास किया है कि वह इस धरती पर बसने वाले तमाम इन्सानों की छोटी-बड़ी समस्याओं को सिर्फ पेश करके न छोड़ दे, बल्कि ऐसा रास्ता भी दे जिस पर चल कर इन्सान स्थायी आनन्द और आसमान की रोशनी बुलनदियों को छू ले।
शमीम करहानी
ग़ज़ल और ग़ज़सख़ोरों की तारीख़, कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये शब्द और एहसास का ही रिश्ता न होकर हमारे आँसुओं की एक लकीर है जो थोड़े-थोड़े अर्से के बाह हर युग में झिलमिला उठती है और इस झिलमिलाहट में जब-तब देखा गया है कि किसी बड़े शायर का चेहरा उभर आता है। इस चमक का नाम कभी फ़ैज़ था, कभी फ़िराक़ था, कोई चेहरा दुष्यन्त के नाम से पहचाना गया, किसी को जिगर कहा गया। हमारे आज के दौर में आँसुओं की ये लकीर ज़हाँ दमकी है, वहीं वसीम बरेलवी का चेहरा उभरा है। इन्होंने अपने शायरा में जिस तरह दिल की धड़कन और दिमाग़ की करवटों को शब्दों के परिधान दिये गये हैं वह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। आँसू को दामन तक, जज़्बातों को एहसास तक और ख़्वाबों के ताबीर तक पहुँचाने में जितना वक्त लगता है उससे भी कम समय में वसीम साहब की ग़ज़लें वक्त के माथे की तहरीर बन जाती हैं। ख़ुदा करे वसीम साहब इसी तरह अपने चाहने वालों और सुनने वालों को अपनी तन्हाइयों को सजाने के लिए उसी तरह किताबों के तोहफ़ें देते रहें।
मंसूर उस्मानी
मौसम अंदर-बाहर के
तन-मन और आत्मा को तृप्त करने वाले जादूगर हैं श्री वसीम बरेलवी जी के ये गीतकविता हृदय के महासागर में, उसकी उत्ताल तरंगों पर तैरनेवाले जहाज़ की तरफ है और गीत इसी समुद्र में भीतर-भीतर चलनेवाली पनडुब्बी का प्रचलन है। आशय यह है कि गीत थोड़ी भीतरी विधा है। गीत लिखते समय रचनाकार को अपने भीतर-भीतर एक ही दिशा में चलना पड़ता है। जैसा पनडुब्बी में पारदर्शी शीशों के माध्यम से समुद्र में व्याप्त संसार को देखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार गीत भी हृदय-जगत में जो कुछ है, उसको देखने और उसको काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने की अद्भुत कला है। काव्यात्मक ढंग कहने का आशय यह है कि उसमें भाव, बुद्धि और कल्पना का समावेश कुछ इस तरह से रहता है कि उसमें लयात्मकता, तान और नाद को एक साथ प्रस्तुत करने की सहज प्रक्रिया स्वयमेव मिल जाती है। इसी कारण गीत में एकात्मकता अर्थात एक ही बिन्दु को देखने या उसी को एक साथ प्रस्तुत करने की सहज प्रक्रिया स्वयमेव मिल जाती है। इसी कारण गीत में एकात्मकता अर्थात् एक ही बिन्दु को देखते रहने या उसी पर वृत्त बनाने का कार्य होता रहता है। एकात्मकता अर्थात् एक ही बिन्दु को देखते रहने या उसी पर वृत्त बनाने का कार्य होता रहता है। एकात्मकता से एक पल को भी हटने का अर्थ है गीत को कमज़ोर करना या मार्ग से हट जाना। गीत में एक केन्द्रीय भाव होता है जो पूरे गीत में रचनाकार की अपनी निजी भाषा और शैली में इस प्रकार अभिव्यक्त होता है जिससे पाठक या श्रोता के हृदय में लगभग उसी भाव को जगा सके जो रचनाकार के मन में है। दूसरे शब्दों में कहाँ जाये तो गीत रचनाकार के हृदय से श्रोता या पाठक के हृदय तक की यात्रा है। और यह हृदय-से-हृदय की यात्रा भी कुछ ऐसी कि जो गीत को एक के होंटों से दूसरे तक ले जाती है। शायद यही कारण है कि हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आज गीतों को दूर से चली आती हुई समृद्ध मौखिक परम्परा का प्रतिफलन माना है। जहाँ तक मौखिक परम्परा का सवाल है, वह भारत के लोक जीवन में रचे-बसे लोकगीतों में ही सर्वाधिक निहित और सुरक्षित रही है। कारण यह है लोकगीतों में लोकजीवन, लोकसंस्कृति, लोकभाषा और लोकधुनों का ऐसा आत्मिक मिलन रहता है कि श्रोताओं का अनायास ही अपनी भाव-भूमि पर ले आता है। यदि उसमें उल्लास है तो श्रोता उल्लसित हो उठता है, यदि उसमें वेदना है तो श्रोता आँसू बहाने पर विवश हो जाता है। लोकगीतों का हृदय से सीधा संबंध है। हम अपने जीवन को तीन तलों पर जीते हैं- शरीर का तल, मन का तल और आत्मा या रूह का तल। कविता इन तीनों हृदय तलों का उत्सव है। और लोकगीत तो केवल उत्सव ही नहीं महोत्सव है। हृदय के तलों से ही हम आत्मा के तल की ओर मुड़ सकते हैं, इसलिए लोकगीत अधिक आत्मिक है।
ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय उर्दू साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले विश्वविख्यात शायर वसीम बरेलवी जी के गीतों को पढ़ रहा हूँ। उनको गीतों में मुझे भारतीय समाज में व्याप्त उसी लोकतत्व की प्रधानता मिली है। वह लोकतत्व जो वसीम जी के गीतों को हिन्दी परम्परा की उस कड़ी से जोड़ने में सक्रिय हो रहा है जो लोकगीतों के नाम से जानी जाती है और सदैव सम्मान पाती रही है। उनके गीतों में जो भावाभिव्यक्ति हुई है, उसका अधिकांश ऐसा है जो प्रेम करनेवाली एक ग्रामीण भोली-भाली लड़की के मन को दर्शाता है। यह नहीं, उसकी भाषा और अभिव्यक्ति शिल्प की बनावट में बहुत दूर, सहज और सरल है। सरलता और सहजता युगों-युगों से व्याप्त आकर्षण और आनन्द का विषय रही है। वसीम जी के ये गीत इसी कारण हृदय में छूने वाले मर्मस्पर्शी गीत हैं। वे प्यारे हैं, क्योंकि वे सरल हैं। उनमें सम्मोहन है, क्योंकि वे सहज हैं।
अब बात ज़रा दूसरे रुख पे मोड़ते हैं। और वह बात यह है कि इन दिनों एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साहित्य और उसकी प्रमुख विधाओं से न केवल परिचित हो रहा है, वरन् उसे आत्मसात भी कर रहा है। हिन्दी में इन दिनों ग़ज़ल विधा इसकी साक्षी है। उर्दू के ग़जलकार जितनी ग़ज़लें कह रहे हैं, कमोबेश हिन्दी में प्रमुख विधाओं-गीत और दोहे- को भी अपना लिया है दोहे का प्रचलन तो इन दिनों पाकिस्तान में भी प्रचुर मात्रा में है। इन दिनों ही ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं, वरन् हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल और मध्यकाल में भी ऐसा हुआ। तेरहवीं शताब्दी के अमीर ख़ुसरों ने भी, जो भारत में ग़ज़ल को लाने वाले पहले कवि कहे जाते हैं, ग़ज़लों के साथ-साथ दोहे, चतुष्पादियाँ और मुकरियाँ लिखीं। अर्ब्दुहीम ख़ानख़ाना ने दोहे की विधा को समृद्ध किया इसे कौन नहीं जानता। रसखान के सवैये आज भी भारतीय समाज के व्यक्ति-व्यक्ति के होटों पर हैं। नज़ीन ने भी लोकजीवन से जुड़ी कविताएँ लिखीं। सच तो यह है कि भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव और समन्वय का काम जितना कवियों और शायरों ने किया उतना हमारे राजनीतिज्ञ भी नहीं कर सके। इस गौरवशाली परम्परा में उर्दू के प्रमुख शायर श्री वसीम बरेलवी ने गीत लिख कर अपना नाम शामिल कर लिया है और यह सम्मिलन साधारण नहीं है, वरन विशेष बन गया है। विशेष इसलिए, क्योंकि इनके गीत लोकजीवन से जुड़े हैं।
आइए, हम फिर वसीम जी के गीतों की ओर मुड़ते हैं। मेरे सामने उनके अट्ठारह गीत हैं, गीतों के अट्ठारह अध्यायों की तरह। जैसा कि मैंने पहले भी इस तथ्य को रेखांकित किया है, वसीम जी के इन गीतों में एक ऐसी अल्हड़, भोली नायिका है जो तरह-तरह से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। वह प्रेम करना जानती है। प्रेमनुभूतियाँ उसे भाँति-भाँति की भाव-मुद्राओं एवं शारीरिक प्रक्रियाओं से गुज़ारती हैं। प्रेमी से मिलना चाहती है, मिल नहीं पाती। कुछ तो उसकी अपनी ही लाज शर्म उसका रास्ता रोकती है और कुछ सामाजिक मर्यादाएँ हैं जो उसको उन्मुक्त नहीं रहने देती। अनेक लक्ष्मण रेखाएँ हैं जो उसे देहरी पार करने से रोकती हैं। यह वह नायिका है जिसे उसके अपने नायक की एक नज़र ही ‘धूप से छाव’ कर गयी है, क्योंकि उसे तन की तपती रेत पर प्रिय की प्रेम-भरी निगाह ‘शबनम की बूँदों’ का स्पर्श दे जाती है। प्रेम में यदि कोई पड़ जाय तो फिर उसे सारी दुनिया नयी नज़र आती हैं। इसीलिए इस नायिका को भी ‘रोज़ के देखे-भाले मंज़र कुछ और ही’ नज़र आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर की नदियाँ उसके साथ-साथ चल रही हैं, और जैसे ही किनारा हाथ में आता है वैसे ही वह डूब-सी जाती हैं। प्रेम की नदी सचमुच है ही ऐसी। जब लक्ष्य मिलने वाला होता है कि हाथ से निकल जाता है। यह बात अलग रही कि उसका ‘मैं’ अब ‘मैं’ नहीं रहा है। वह ‘तू’ में परिवर्तित हो गया है। और यह तन ही होता है जब एक को दूसरे में तादात्मय हो जब कोई भेद नहीं रहा, सब अभेद हो गया तभी तो वह कहती है-
ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय उर्दू साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले विश्वविख्यात शायर वसीम बरेलवी जी के गीतों को पढ़ रहा हूँ। उनको गीतों में मुझे भारतीय समाज में व्याप्त उसी लोकतत्व की प्रधानता मिली है। वह लोकतत्व जो वसीम जी के गीतों को हिन्दी परम्परा की उस कड़ी से जोड़ने में सक्रिय हो रहा है जो लोकगीतों के नाम से जानी जाती है और सदैव सम्मान पाती रही है। उनके गीतों में जो भावाभिव्यक्ति हुई है, उसका अधिकांश ऐसा है जो प्रेम करनेवाली एक ग्रामीण भोली-भाली लड़की के मन को दर्शाता है। यह नहीं, उसकी भाषा और अभिव्यक्ति शिल्प की बनावट में बहुत दूर, सहज और सरल है। सरलता और सहजता युगों-युगों से व्याप्त आकर्षण और आनन्द का विषय रही है। वसीम जी के ये गीत इसी कारण हृदय में छूने वाले मर्मस्पर्शी गीत हैं। वे प्यारे हैं, क्योंकि वे सरल हैं। उनमें सम्मोहन है, क्योंकि वे सहज हैं।
अब बात ज़रा दूसरे रुख पे मोड़ते हैं। और वह बात यह है कि इन दिनों एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साहित्य और उसकी प्रमुख विधाओं से न केवल परिचित हो रहा है, वरन् उसे आत्मसात भी कर रहा है। हिन्दी में इन दिनों ग़ज़ल विधा इसकी साक्षी है। उर्दू के ग़जलकार जितनी ग़ज़लें कह रहे हैं, कमोबेश हिन्दी में प्रमुख विधाओं-गीत और दोहे- को भी अपना लिया है दोहे का प्रचलन तो इन दिनों पाकिस्तान में भी प्रचुर मात्रा में है। इन दिनों ही ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं, वरन् हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल और मध्यकाल में भी ऐसा हुआ। तेरहवीं शताब्दी के अमीर ख़ुसरों ने भी, जो भारत में ग़ज़ल को लाने वाले पहले कवि कहे जाते हैं, ग़ज़लों के साथ-साथ दोहे, चतुष्पादियाँ और मुकरियाँ लिखीं। अर्ब्दुहीम ख़ानख़ाना ने दोहे की विधा को समृद्ध किया इसे कौन नहीं जानता। रसखान के सवैये आज भी भारतीय समाज के व्यक्ति-व्यक्ति के होटों पर हैं। नज़ीन ने भी लोकजीवन से जुड़ी कविताएँ लिखीं। सच तो यह है कि भारत में साम्प्रदायिक सद्भाव और समन्वय का काम जितना कवियों और शायरों ने किया उतना हमारे राजनीतिज्ञ भी नहीं कर सके। इस गौरवशाली परम्परा में उर्दू के प्रमुख शायर श्री वसीम बरेलवी ने गीत लिख कर अपना नाम शामिल कर लिया है और यह सम्मिलन साधारण नहीं है, वरन विशेष बन गया है। विशेष इसलिए, क्योंकि इनके गीत लोकजीवन से जुड़े हैं।
आइए, हम फिर वसीम जी के गीतों की ओर मुड़ते हैं। मेरे सामने उनके अट्ठारह गीत हैं, गीतों के अट्ठारह अध्यायों की तरह। जैसा कि मैंने पहले भी इस तथ्य को रेखांकित किया है, वसीम जी के इन गीतों में एक ऐसी अल्हड़, भोली नायिका है जो तरह-तरह से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। वह प्रेम करना जानती है। प्रेमनुभूतियाँ उसे भाँति-भाँति की भाव-मुद्राओं एवं शारीरिक प्रक्रियाओं से गुज़ारती हैं। प्रेमी से मिलना चाहती है, मिल नहीं पाती। कुछ तो उसकी अपनी ही लाज शर्म उसका रास्ता रोकती है और कुछ सामाजिक मर्यादाएँ हैं जो उसको उन्मुक्त नहीं रहने देती। अनेक लक्ष्मण रेखाएँ हैं जो उसे देहरी पार करने से रोकती हैं। यह वह नायिका है जिसे उसके अपने नायक की एक नज़र ही ‘धूप से छाव’ कर गयी है, क्योंकि उसे तन की तपती रेत पर प्रिय की प्रेम-भरी निगाह ‘शबनम की बूँदों’ का स्पर्श दे जाती है। प्रेम में यदि कोई पड़ जाय तो फिर उसे सारी दुनिया नयी नज़र आती हैं। इसीलिए इस नायिका को भी ‘रोज़ के देखे-भाले मंज़र कुछ और ही’ नज़र आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर की नदियाँ उसके साथ-साथ चल रही हैं, और जैसे ही किनारा हाथ में आता है वैसे ही वह डूब-सी जाती हैं। प्रेम की नदी सचमुच है ही ऐसी। जब लक्ष्य मिलने वाला होता है कि हाथ से निकल जाता है। यह बात अलग रही कि उसका ‘मैं’ अब ‘मैं’ नहीं रहा है। वह ‘तू’ में परिवर्तित हो गया है। और यह तन ही होता है जब एक को दूसरे में तादात्मय हो जब कोई भेद नहीं रहा, सब अभेद हो गया तभी तो वह कहती है-
कल तक जिस दरपन में थी और मेरे वीराने
आज उसी दरपन में तू ही तू है क्या जाने
अन्दर चोर छुपा है जाने कब चुर जाऊँ
सजन,यह बात किसे बतलाऊँ
आज उसी दरपन में तू ही तू है क्या जाने
अन्दर चोर छुपा है जाने कब चुर जाऊँ
सजन,यह बात किसे बतलाऊँ
किन्तु इस स्थिति में आना कोई यूँ ही हो गया है। कितना प्रयास करना पड़ा
है। प्रिय तो बहुत ऊँचाई पर है। उसे छूना, उसे पाना क्या सरल है ? वह तो
‘अम्बर की आँख का तारा’ और प्रेमिका के हाथ तो बहुत
छोटे हैं, प्रेमी तो ‘भरी बरसात’ है और प्रेमिका
‘पानी की एक बूँद है। यदि इस बूँद ने अपने प्रिय की ओर बढ़ना चाहा तो पाँव में
‘लक्ष्मन रेखा’ लिपट गयी। अनेक मर्यादाएँ आ गयीं, फिर
भी उसकी एक चाहत तो जनम-जनम रहेगी:-
जनम-जनम माँगूंगी तुझको, तू मुझको ठुकराना
मैं माटी में मिल जाऊँगी तू माटी हो जाना
लहर के आगे क्या इक तिनके की औक़ात
सजन, मैं भूल गयी यह बात
मैं माटी में मिल जाऊँगी तू माटी हो जाना
लहर के आगे क्या इक तिनके की औक़ात
सजन, मैं भूल गयी यह बात
वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपने प्रिय को शीघ्र ही पा लेते है। अन्यथा
मिलन की राह विरह में बदल जाती है। जब बादल के संग-संग मन बढ़ता है और तन
में बिजुरी-सी लहराती है तभी न जाने क्या हो जाता है कि यह नायिका
‘चुनना तो फूल चाहती है किन्तु काँटा चुभ जाता है।’
यह सबसे
अपने मन का भेद, मन का रहस्य छुपाना चाहती है, किन्तु ‘हवा का
एक ही
झोंका’ सारे भेदों को खोल देता है। उसका उसके पास कुछ नहीं
रहता।
यहीं झोका उस सब कुछ ले जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो खेतों की
हरियाली उसे ताने मारती है और हँसी उड़ाती है, सारी प्रकृति ही उससे साजन
की दूरी का लाभ उठाती है। जो भी हैं, प्रिय से मिलन की राह में रोड़ा
अटकाने वाले ही हैं। फिर भी पिया मिलन री आस उसे हैं-
मस्त हवा चुनरी से खेले बेशर्मी सिखलाये
प्रकृति भी साजन की दूरी का लाभ उठाये
इतने हिम्मत तोड़ने वाले और मिरी इक आस
न जाने मुझ बिरहिन की प्यास
प्रकृति भी साजन की दूरी का लाभ उठाये
इतने हिम्मत तोड़ने वाले और मिरी इक आस
न जाने मुझ बिरहिन की प्यास
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book