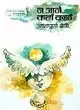|
नारी विमर्श >> खरीदा हुआ दुख खरीदा हुआ दुखआशापूर्णा देवी
|
24 पाठक हैं |
||||||
आशापूर्णा जी के उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं। सृजन की श्रेष्ठ सहभागी होते हुए भी नारी का पुरुष के समान मूल्यांकन नहीं है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका आशापूर्णा देवी का एक नया उपन्यास
आशापूर्णा देवी का लेखन उनका निजी संसार नहीं है वे हमारे आस-पास फैले संसार का विस्तारमात्र है। इनके उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं। सृजन की श्रेष्ठ सहभागी होते हुए भी नारी का पुरुष के समान मूल्यांकन नहीं? पुरुष की बड़ी सी कमजोरी पर समाज में कोई हलचल नहीं, लेकिन नारी की थोड़ी सी चूक उसके जीवन को रसातल में डाल देती है। यह है एक असहाय विडम्बना ! बंकिम, रवीन्द्र, शरत् के पश्चात् आशा पूर्णा देवी हिन्दी भाषी आँचल में एक सुपरिचित नाम है—जिसकी हर कृति एक नयी अपेक्षा के साथ पढ़ी जाती है।
आशापूर्णा देवी का लेखन उनका निजी संसार नहीं है वे हमारे आस-पास फैले संसार का विस्तारमात्र है। इनके उपन्यास मूलतः नारी केन्द्रित होते हैं। सृजन की श्रेष्ठ सहभागी होते हुए भी नारी का पुरुष के समान मूल्यांकन नहीं? पुरुष की बड़ी सी कमजोरी पर समाज में कोई हलचल नहीं, लेकिन नारी की थोड़ी सी चूक उसके जीवन को रसातल में डाल देती है। यह है एक असहाय विडम्बना ! बंकिम, रवीन्द्र, शरत् के पश्चात् आशा पूर्णा देवी हिन्दी भाषी आँचल में एक सुपरिचित नाम है—जिसकी हर कृति एक नयी अपेक्षा के साथ पढ़ी जाती है।
खरीदा हुआ दुख
पैसे दे तुमने गरीबी खरीदी !
पैसे दे तुमने गरीबी खरीदी !
पैसे दे तुमने—
सुबह से शुरू हो दिन भर दिलोदिमाग पर इन्हीं शब्दों का हथौड़ा पाँच-पाँच चोट कर रहा है। लग रहा है कि शहर के तमाम कोलाहल से भी यही शब्द उठ रहे हैं। चलती बस के पहियों की घरघराहट से भी यही शब्द निकल रहे हैं।
पीयूषकान्ति को अब यह नहीं लग रहा कि यह जहर-भरा वाक्य, जो उसके मन में सुबह से घुमड़ रहा है, सुरमा के मुख से निकला व्यंग्यमय वाक्य है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य, जो उसकी चेतना के हर स्तर पर गूँज रहा है, किसी नेत्रविहीन बर्रैये की गुनगुनाहट है। पैसे दे तुमने गरीबी खरीदी !
नेत्रविहीन बर्रैया या घिसा हुआ ग्रामोफोन रिकार्ड ?
आये दिन सुरमा का व्यंग्य और असन्तोष हर कदम पर ही छिटक-छिटक कर बिखर रहा है। घर पर पीयूषकान्ति की निर्बुद्धिता की समालोचना का तो समझिये खेत में हल ही चल गया। मगर, फिर भी, यह मानना ही पड़ेगा कि इतना स्पष्ट, इतना तीखा मन्तव्य इसके पहले कभी सुना न गया था। सुबह जब वह चलने लगा तब मन्तव्य की यह कटार सुरमा ने उस पर फेंक मारी। चौंक उठा था पियूषकान्ति और शायद अपने अनजाने ही बोल पड़ा था, ‘‘पैसों से मैंने क्या खरीदा ?’
सुरमा ने अपनी कथनी को दोहराना जरूरी नहीं समझा। इतना ही बोली, ‘जो खरीदा है, उसकी करतूत तो रोम-रोम में अनुभव कर रहे हो। पैसों से तुमने....’
बात को असमाप्त ही छोड़ उसके सामने हट गई थी सुरमा। यह सुरमा की पुरानी आदत है, जब बहुत उत्तेजित हो उठती है, तब बात पूरी नहीं कर पाती।
पीयूष के पास उस समय रुकने की फुर्सत न थी, वह जल्दी-जल्दी निकल पड़ा था, मगर सुरमा का यह श्लेषवाक्य सारा दिन उसका पीछा करता रहा, किसी भी तरह वह उसे अपने मन से हटा नहीं पा रहा था।
किस परिस्थिति में सुरमा ने यह बात कही थी ?
जिस समय पीयूष ने बाजार से थैला ला कर उसके सामने रखा था। गोलियों जैसे आलू, छोटे-छोटे परवल, और छोटी-छोटी मछली थी उसमें। क्या तब, या तब, जब, पीयूष को बनियान पहने थ्ज्ञा उसकी पीठ पर झाँकते छेदों को देख कर जब उसने कहा था, ‘‘वाह !’
लेकिन वह तो बहुत पहले की बात है।
यह तो दफ्तर जाने के समय की बात नहीं है।
सुबह, बाजार से लाये सामना को देखकर जो आँधी उठी थी उसे तो पीयूष ने यहाँ के बाजार की बुराई कह कर सम्भाल ही लिया था। कहाँ था, ‘सोचा था मैंने यहाँ और कुछ मिले न मिले, सब्जी वगैरह तो ताजी मिलेगी ही लेकिन क्या सड़ियल बाजार है यहाँ का ! राम करो।’
शीतल छुरी-सी बोली थी सुरमा, ‘जब हाथ के बगल में बढ़िया बाजार था, तब तो वहाँ कभी झाँकने भी नहीं गये। अब इस सड़ियल बाजार में कीड़े भरे बैंगने और सड़ी मछली छानते फिर रहे हो !’
सड़ी मछली वाला आरोप सुरमा ने तो सिर्फ कुढ़न के मारे कहा था ! मगर उसका पहला वाक्य बिलकुल सच है। ‘गड़ियाहाट’ जैसे मशहूर बाजार के बिलकुल करीब जब रहता था तब पीयूषकान्ति ने कभी बाजार के भीतर कदम नहीं रखा था।
श्याम बाजार से बहुत दूर छिटक कर जब वह इधर आया, तब, पहले ही दिन पीयूषकान्ति इस मुहल्ले का बाजार देखने गया था। गया जरूर था, पर लौटते ही उसने सिर पर हाथ रख कर कहा था, ‘कौन जाये बाजार ? बाजार ? बाजार में सामान तो कुछ दिखता ही नहीं, दिखाई पड़ती हैं सिर्फ साड़ियाँ।’
साड़ियाँ ? क्या मतलब है तुम्हारा साड़ियों से ? मछली-सब्जी की दुकानों में आज-कल साड़ियों की दुकानें....।’
यह कहा था उसके बेटे टू टू ने।
‘दुकान ? हाँ ऐसा कहा जा सकता है। चलती-फिरती दुकानें। शादी-ब्याह में पहनी जाने वाली साड़ियाँ पहनकर, हाथों में एक एक रंगी बैग व डोलची झुलाती महिलायें सारा बाजार छाने डाल रही हैं।’
‘छानने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है ?’ सुरमा बोली, ‘तुम भी टेरिकॉट-टेरिलिन का सूट डाँटकर रंग-बिरंगा बैग लटकाये बाजार के चक्कर काटो न !’
‘माफ करो। मुझसे यह नहीं होगा।’ कहा था पीयूषकान्ति ने, ‘इस मुहल्ले में आने के बाद, गृहस्थी का सबसे झंझट वाला काम तुम्हारे ही पल्ले पड़ गया, देखता हूँ।’
‘तुम कहना चाहते हो, कि आगे से मुझे बाजार जाना पड़ेगा ?’
‘ले-दे कर इसी नतीजे पर तो पहुँचा हूँ। क्या तुम्हारे पास भारी, कामदार आँचल की दो-चार साड़ियाँ भी नहीं हैं ?’ उत्तर दिया था पीयूषकान्ति ने !
सुरमा ने कहा था, ‘दक्षिण-कलकत्ता में औरतें तो बहुत दिन पहले से ही बाजार-हाट जाती रही हैं। तुम्हारा उत्तर-कलकत्ता ही अभी तक उसी पुरानी लकीर को पीटता चला आ रहा है। एक दिन की घटना सुनाऊँ तुम्हें, वह जो मौसी जी अपने मकान के बगल वाले मकान में रहती हैं, दक्षिण कलकत्ते में रहने वालियों की क्या थुक्का-फजीहत की उन्होंने ! बोलीं, ‘अन्धेर है, घर की बहू-बेटियाँ नौकरानियों की तरह हाथ में थैला लटकाये बाजार जाती हैं—साग, मांस, मछली, आलू, परवल खरीदने ! छिः छिः छिः ! आधुनिक जीवन से परिचित होने में तुम्हारे उत्तर कलकत्ते—को अभी बहुत दिन लगेंगे।’
गड़ियाहाट जाने के बाद से ही सुरमा स्यामबाजार को ‘’तुम्हारा’ मुहल्ला कहने लगी है। पीयूष ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। मालूम होता है, पहली रात को बिल्ली मरने वाली बात उसे किसी ने बतायी न थी।
ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो सीधे-सादे पीयूषकान्ति को मालूम नहीं। लेकिन सुरमा यह जानती थी कि अगर नाव को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला काम जो करना है, वह है उसकी रस्सी को काट देना।
जो भी हो पीयूषकान्ति का प्रस्ताव सुरमा ने बड़ी खुशी से अपना लिया था। गृहस्थी के सबसे झंझट वाले काम’ को बिना ना-नुकुर किये उसने अपने ऊपर ले लिया था। बिलकुल अकेले जाने की आदत डालने में कुछ वक्त जरूर लगा था उसे। कीमती और भारी साड़ियाँ पहन, उल्टे पल्ले से, छोटी बेटी को साथ ले बाजार जाने लगी वह।
और पीयूषकान्ति ने सोचा, ‘चलो बाबा, अच्छा हुआ, जान छूटी।’
तब से जाने छूटने के अनुच्छेद ही चल रहा था। इधर मुहल्ला बदलने के साथ ही फिर उसकी बारी आ गई।
इस मुहल्ले के गंदे, गँवई, गरीब बाजार में पीयूषकान्ति के अलावा जायेगा कौन ? सुरमा ? उसका बेटा या बेटियाँ ? उन्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है।
उतनी सुबह जाने में पीयूषकान्ति को दिक्कत होती है तो करना क्या है।
अपने ही घर तक नाला काट कर अगर कोई घड़ियाल को घर में बुलायेगा तो घड़ियाल के दाँतों की धार से उसे अवश्य ही परिचित होना पड़ेगा।
असल बात यह नहीं कि बाजार दीन-हीन है, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं। असल बात तो यह है कि आये दिन पीयूषकान्ति की जेब में हर वक्त नोटों का बण्डल न रहने से चैन नहीं पड़ती थी, वही पीयूषकान्ति आज बजट के अनुसार गिन-गिनकर पैसे ले बाजार जाता है। कहीं, पास पैसा रहने से यदि मन ललक जाये, ज्यादा खर्च हो जाये, इस डर के कारण ज्यादा पैसा लेकर वह बाजार जाता ही नहीं। यह सीख उसके वर्तमान गुरू से मिली है।
यह तो मानी हुई बात है कि इन गुरुदेव के दरशाये पथ पर चल कर, जो सौदा बाजार से आयेगा, उससे पीयूषकान्ति की पत्नी और परिवार गदगद तो नहीं हो उठेंगे, अवश्य ही उन्हें गुस्सा आयेगा।
जब उन्होंने पीयूषकान्ति के लाये सामान को देख जली-कटी सुनाई, तब पीयूष ने आत्म-रक्षा के उद्देश्य से कहा था, ‘क्या करूँ, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। मैं तो बहुत-बहुत ढूँढ़ा हूँ कि कोई अच्छी चीज मिले, और तुम कहती हो कि मैं सड़ी-गली बासी चीजें ही खोजता रहता हूँ।
पीयूष ने कहा तो जरूर था, मगर उसके स्वर में आत्म-विश्वास नहीं फूटा था।
उसकी बात का सीधा जवाब न दिया था सुरमा ने। तीर से भी ज्यादा चुभने वाली पैनी मुस्कराहट से उसका स्वागत कर उसने थैला उठाया और चौके में जाती-जाती ‘यहाँ’ आकर रहने के विषय में कुछ और जहर छिड़क गई।
उस वक्त तो पीयूष ने चैन की साँस ली। चलो भई, फिलहाल के लिये तो जान छूटी। लेकिन उसके बाद ?
फिर ?
ठीक दफ्तर जाने के समय ?
हाँ, याद आया। दफ्तर जाते समय एक अप्रिय घटना फिर घट गई। बुलू ने कहा था कि उसे एक किताब चाहिये, इकनामिक्स की। चाहिए का मतलब था ‘अवश्य ही चाहिए’ और ‘फौरन चाहिए।’ क्योंकि उसकी जरूरतें कल तक रुकना नहीं जानतीं। मतलब यह हुआ कि ऑफिस जाने से पहले पापा चालीस रुपये उसे दें। सुन कर पीयूष ने कहा था —यही उसका अपराध है। हाँ, कहाँ था पीयूष ने, ‘तुम लोगों की पढ़ाई का खर्च भरते-भरते तो दिवाला ही निकला जा रहा है। अभी तो चार-पाँच दिन पहले अट्ठाइस रुपये लिये थे किताब खरीदने के लिए। कालेज की फीस और बस का इतना-इतना किराया ऊपर से।’
बुलू क्षण भर चुप रही, फिर एक एड़ी पर खड़ी हो एक चक्कर घूम, कमरे से बाहर हो गई। जाते-जाते कह गई, ‘ठीक है, अगले महीने से मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं भरना पड़ेगा तुम्हें, मैं खुद ही इन्तजाम कर लूँगी। लेकिन, बस के किराये का ताना देने के पहले, एक बार सोच लेते तो अच्छा होता।’
बुलू, यानी पीयूषकान्ति की छोटी बेटी, जो अभी कुछ ही दिन पहले गड़ियाहाट में रहते समय, जब-तब पापा के गले में बाहें डाल कर झूल पड़ती और कहती, ‘‘पापा, ओ पापा, कितने स्वीट हो पापा। किसी का पापा ऐसा नहीं। बहुत-बहुत-बहुत ही स्वीट हो तुम।’
पैसे दे तुमने गरीबी खरीदी !
पैसे दे तुमने—
सुबह से शुरू हो दिन भर दिलोदिमाग पर इन्हीं शब्दों का हथौड़ा पाँच-पाँच चोट कर रहा है। लग रहा है कि शहर के तमाम कोलाहल से भी यही शब्द उठ रहे हैं। चलती बस के पहियों की घरघराहट से भी यही शब्द निकल रहे हैं।
पीयूषकान्ति को अब यह नहीं लग रहा कि यह जहर-भरा वाक्य, जो उसके मन में सुबह से घुमड़ रहा है, सुरमा के मुख से निकला व्यंग्यमय वाक्य है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य, जो उसकी चेतना के हर स्तर पर गूँज रहा है, किसी नेत्रविहीन बर्रैये की गुनगुनाहट है। पैसे दे तुमने गरीबी खरीदी !
नेत्रविहीन बर्रैया या घिसा हुआ ग्रामोफोन रिकार्ड ?
आये दिन सुरमा का व्यंग्य और असन्तोष हर कदम पर ही छिटक-छिटक कर बिखर रहा है। घर पर पीयूषकान्ति की निर्बुद्धिता की समालोचना का तो समझिये खेत में हल ही चल गया। मगर, फिर भी, यह मानना ही पड़ेगा कि इतना स्पष्ट, इतना तीखा मन्तव्य इसके पहले कभी सुना न गया था। सुबह जब वह चलने लगा तब मन्तव्य की यह कटार सुरमा ने उस पर फेंक मारी। चौंक उठा था पियूषकान्ति और शायद अपने अनजाने ही बोल पड़ा था, ‘‘पैसों से मैंने क्या खरीदा ?’
सुरमा ने अपनी कथनी को दोहराना जरूरी नहीं समझा। इतना ही बोली, ‘जो खरीदा है, उसकी करतूत तो रोम-रोम में अनुभव कर रहे हो। पैसों से तुमने....’
बात को असमाप्त ही छोड़ उसके सामने हट गई थी सुरमा। यह सुरमा की पुरानी आदत है, जब बहुत उत्तेजित हो उठती है, तब बात पूरी नहीं कर पाती।
पीयूष के पास उस समय रुकने की फुर्सत न थी, वह जल्दी-जल्दी निकल पड़ा था, मगर सुरमा का यह श्लेषवाक्य सारा दिन उसका पीछा करता रहा, किसी भी तरह वह उसे अपने मन से हटा नहीं पा रहा था।
किस परिस्थिति में सुरमा ने यह बात कही थी ?
जिस समय पीयूष ने बाजार से थैला ला कर उसके सामने रखा था। गोलियों जैसे आलू, छोटे-छोटे परवल, और छोटी-छोटी मछली थी उसमें। क्या तब, या तब, जब, पीयूष को बनियान पहने थ्ज्ञा उसकी पीठ पर झाँकते छेदों को देख कर जब उसने कहा था, ‘‘वाह !’
लेकिन वह तो बहुत पहले की बात है।
यह तो दफ्तर जाने के समय की बात नहीं है।
सुबह, बाजार से लाये सामना को देखकर जो आँधी उठी थी उसे तो पीयूष ने यहाँ के बाजार की बुराई कह कर सम्भाल ही लिया था। कहाँ था, ‘सोचा था मैंने यहाँ और कुछ मिले न मिले, सब्जी वगैरह तो ताजी मिलेगी ही लेकिन क्या सड़ियल बाजार है यहाँ का ! राम करो।’
शीतल छुरी-सी बोली थी सुरमा, ‘जब हाथ के बगल में बढ़िया बाजार था, तब तो वहाँ कभी झाँकने भी नहीं गये। अब इस सड़ियल बाजार में कीड़े भरे बैंगने और सड़ी मछली छानते फिर रहे हो !’
सड़ी मछली वाला आरोप सुरमा ने तो सिर्फ कुढ़न के मारे कहा था ! मगर उसका पहला वाक्य बिलकुल सच है। ‘गड़ियाहाट’ जैसे मशहूर बाजार के बिलकुल करीब जब रहता था तब पीयूषकान्ति ने कभी बाजार के भीतर कदम नहीं रखा था।
श्याम बाजार से बहुत दूर छिटक कर जब वह इधर आया, तब, पहले ही दिन पीयूषकान्ति इस मुहल्ले का बाजार देखने गया था। गया जरूर था, पर लौटते ही उसने सिर पर हाथ रख कर कहा था, ‘कौन जाये बाजार ? बाजार ? बाजार में सामान तो कुछ दिखता ही नहीं, दिखाई पड़ती हैं सिर्फ साड़ियाँ।’
साड़ियाँ ? क्या मतलब है तुम्हारा साड़ियों से ? मछली-सब्जी की दुकानों में आज-कल साड़ियों की दुकानें....।’
यह कहा था उसके बेटे टू टू ने।
‘दुकान ? हाँ ऐसा कहा जा सकता है। चलती-फिरती दुकानें। शादी-ब्याह में पहनी जाने वाली साड़ियाँ पहनकर, हाथों में एक एक रंगी बैग व डोलची झुलाती महिलायें सारा बाजार छाने डाल रही हैं।’
‘छानने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है ?’ सुरमा बोली, ‘तुम भी टेरिकॉट-टेरिलिन का सूट डाँटकर रंग-बिरंगा बैग लटकाये बाजार के चक्कर काटो न !’
‘माफ करो। मुझसे यह नहीं होगा।’ कहा था पीयूषकान्ति ने, ‘इस मुहल्ले में आने के बाद, गृहस्थी का सबसे झंझट वाला काम तुम्हारे ही पल्ले पड़ गया, देखता हूँ।’
‘तुम कहना चाहते हो, कि आगे से मुझे बाजार जाना पड़ेगा ?’
‘ले-दे कर इसी नतीजे पर तो पहुँचा हूँ। क्या तुम्हारे पास भारी, कामदार आँचल की दो-चार साड़ियाँ भी नहीं हैं ?’ उत्तर दिया था पीयूषकान्ति ने !
सुरमा ने कहा था, ‘दक्षिण-कलकत्ता में औरतें तो बहुत दिन पहले से ही बाजार-हाट जाती रही हैं। तुम्हारा उत्तर-कलकत्ता ही अभी तक उसी पुरानी लकीर को पीटता चला आ रहा है। एक दिन की घटना सुनाऊँ तुम्हें, वह जो मौसी जी अपने मकान के बगल वाले मकान में रहती हैं, दक्षिण कलकत्ते में रहने वालियों की क्या थुक्का-फजीहत की उन्होंने ! बोलीं, ‘अन्धेर है, घर की बहू-बेटियाँ नौकरानियों की तरह हाथ में थैला लटकाये बाजार जाती हैं—साग, मांस, मछली, आलू, परवल खरीदने ! छिः छिः छिः ! आधुनिक जीवन से परिचित होने में तुम्हारे उत्तर कलकत्ते—को अभी बहुत दिन लगेंगे।’
गड़ियाहाट जाने के बाद से ही सुरमा स्यामबाजार को ‘’तुम्हारा’ मुहल्ला कहने लगी है। पीयूष ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। मालूम होता है, पहली रात को बिल्ली मरने वाली बात उसे किसी ने बतायी न थी।
ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो सीधे-सादे पीयूषकान्ति को मालूम नहीं। लेकिन सुरमा यह जानती थी कि अगर नाव को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहला काम जो करना है, वह है उसकी रस्सी को काट देना।
जो भी हो पीयूषकान्ति का प्रस्ताव सुरमा ने बड़ी खुशी से अपना लिया था। गृहस्थी के सबसे झंझट वाले काम’ को बिना ना-नुकुर किये उसने अपने ऊपर ले लिया था। बिलकुल अकेले जाने की आदत डालने में कुछ वक्त जरूर लगा था उसे। कीमती और भारी साड़ियाँ पहन, उल्टे पल्ले से, छोटी बेटी को साथ ले बाजार जाने लगी वह।
और पीयूषकान्ति ने सोचा, ‘चलो बाबा, अच्छा हुआ, जान छूटी।’
तब से जाने छूटने के अनुच्छेद ही चल रहा था। इधर मुहल्ला बदलने के साथ ही फिर उसकी बारी आ गई।
इस मुहल्ले के गंदे, गँवई, गरीब बाजार में पीयूषकान्ति के अलावा जायेगा कौन ? सुरमा ? उसका बेटा या बेटियाँ ? उन्हें पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है।
उतनी सुबह जाने में पीयूषकान्ति को दिक्कत होती है तो करना क्या है।
अपने ही घर तक नाला काट कर अगर कोई घड़ियाल को घर में बुलायेगा तो घड़ियाल के दाँतों की धार से उसे अवश्य ही परिचित होना पड़ेगा।
असल बात यह नहीं कि बाजार दीन-हीन है, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं। असल बात तो यह है कि आये दिन पीयूषकान्ति की जेब में हर वक्त नोटों का बण्डल न रहने से चैन नहीं पड़ती थी, वही पीयूषकान्ति आज बजट के अनुसार गिन-गिनकर पैसे ले बाजार जाता है। कहीं, पास पैसा रहने से यदि मन ललक जाये, ज्यादा खर्च हो जाये, इस डर के कारण ज्यादा पैसा लेकर वह बाजार जाता ही नहीं। यह सीख उसके वर्तमान गुरू से मिली है।
यह तो मानी हुई बात है कि इन गुरुदेव के दरशाये पथ पर चल कर, जो सौदा बाजार से आयेगा, उससे पीयूषकान्ति की पत्नी और परिवार गदगद तो नहीं हो उठेंगे, अवश्य ही उन्हें गुस्सा आयेगा।
जब उन्होंने पीयूषकान्ति के लाये सामान को देख जली-कटी सुनाई, तब पीयूष ने आत्म-रक्षा के उद्देश्य से कहा था, ‘क्या करूँ, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। मैं तो बहुत-बहुत ढूँढ़ा हूँ कि कोई अच्छी चीज मिले, और तुम कहती हो कि मैं सड़ी-गली बासी चीजें ही खोजता रहता हूँ।
पीयूष ने कहा तो जरूर था, मगर उसके स्वर में आत्म-विश्वास नहीं फूटा था।
उसकी बात का सीधा जवाब न दिया था सुरमा ने। तीर से भी ज्यादा चुभने वाली पैनी मुस्कराहट से उसका स्वागत कर उसने थैला उठाया और चौके में जाती-जाती ‘यहाँ’ आकर रहने के विषय में कुछ और जहर छिड़क गई।
उस वक्त तो पीयूष ने चैन की साँस ली। चलो भई, फिलहाल के लिये तो जान छूटी। लेकिन उसके बाद ?
फिर ?
ठीक दफ्तर जाने के समय ?
हाँ, याद आया। दफ्तर जाते समय एक अप्रिय घटना फिर घट गई। बुलू ने कहा था कि उसे एक किताब चाहिये, इकनामिक्स की। चाहिए का मतलब था ‘अवश्य ही चाहिए’ और ‘फौरन चाहिए।’ क्योंकि उसकी जरूरतें कल तक रुकना नहीं जानतीं। मतलब यह हुआ कि ऑफिस जाने से पहले पापा चालीस रुपये उसे दें। सुन कर पीयूष ने कहा था —यही उसका अपराध है। हाँ, कहाँ था पीयूष ने, ‘तुम लोगों की पढ़ाई का खर्च भरते-भरते तो दिवाला ही निकला जा रहा है। अभी तो चार-पाँच दिन पहले अट्ठाइस रुपये लिये थे किताब खरीदने के लिए। कालेज की फीस और बस का इतना-इतना किराया ऊपर से।’
बुलू क्षण भर चुप रही, फिर एक एड़ी पर खड़ी हो एक चक्कर घूम, कमरे से बाहर हो गई। जाते-जाते कह गई, ‘ठीक है, अगले महीने से मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं भरना पड़ेगा तुम्हें, मैं खुद ही इन्तजाम कर लूँगी। लेकिन, बस के किराये का ताना देने के पहले, एक बार सोच लेते तो अच्छा होता।’
बुलू, यानी पीयूषकान्ति की छोटी बेटी, जो अभी कुछ ही दिन पहले गड़ियाहाट में रहते समय, जब-तब पापा के गले में बाहें डाल कर झूल पड़ती और कहती, ‘‘पापा, ओ पापा, कितने स्वीट हो पापा। किसी का पापा ऐसा नहीं। बहुत-बहुत-बहुत ही स्वीट हो तुम।’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book