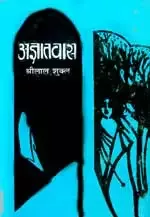|
विविध उपन्यास >> अज्ञातवास अज्ञातवासश्रीलाल शुक्ल
|
467 पाठक हैं |
||||||
अज्ञातवास एक ऐसी ही अफसर श्रेणी के इंजीनियर की कहानी है जिसकी स्मृतियां एक चित्र को देखकर जाग उठती हैं और जो अपने स्वयं के मित्रों के जिस गांव में उसका डेरा है वहाँ के निवासियों के और अपनी बेटी के भी जीवन की घटनाओं को पर्त-दर-पर्त सामने रखती चली जाती हैं।
प्रस्तुत है पुस्तक के कुछ अंश
गाँव और शहर दोनों की कहानियाँ और एक साथ कहने में श्रीलाल शुक्ल माहिर है। और बहुत कम पृष्ठों में कहानी के भीतर कहानी इस तरह पिरोते चले जाते हैं कि पूरा पढ़े बिना पाठक चैन नहीं लेता। अज्ञातवास एक ऐसी ही अफसर श्रेणी के इंजीनियर की कहानी है जिसकी स्मृतियां एक चित्र को देखकर जाग उठती हैं और जो अपने स्वयं के मित्रों के जिस गांव में उसका डेरा है वहाँ के निवासियों के और अपनी बेटी के भी जीवन की घटनाओं को पर्त-दर-पर्त सामने रखती चली जाती हैं। उसकी पत्नी और उपपत्नी की कथा उपन्यास का चरम बिन्दु है जो बिलकुल अंत में जाकर स्पष्ट होता है। अज्ञातवास निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ,पठनीय उपन्यास है।
प्रस्तावना
‘अज्ञातवास’ 1956-60 में लिखा गया था। यदि 1961 में श्री स.ही. वात्स्यायन की मुझे सहज कृपा न मिली होती और राजपाल एण्ड सन्ज़ एक अपेक्षाकृत नये लेखक के लिए कुछ ख़तरा-उठाने के लिए तैयार न हुए होते, तो शायद इसका उस वर्ष भी छपना मुश्किल होता।
उन दिनों पत्र-पत्रिकाओं में निकलनेवाली इसकी समीक्षाओं से मैं उतना ही प्रोत्साहित हुआ था जितना इसकी धीमी बिक्री से प्रकाशकों को निरुत्साहित होना चाहिए था। पर निश्चय ही उनका उत्साह संदेह से परे है। वे इस उपन्यास का अब नया संस्करण निकाल रहे हैं। मैं आभारी हूं।
इस संस्करण में-एक अपवाद छोड़कर-मूल पुस्तक को यथावत् रहने दिया गया है। अपवाद मूल पुस्तक के अंग्रेज़ी अनुच्छेदों के विषय में है। अपने आरम्भिक रचनाकाल में भाषा के, और विशेषतया कथा-साहित्य में पात्रों के वार्तालाप की भाषा के बारे में मैं उतना सचेत न था। इससे अज्ञातवास के कुछ स्थलों में अंग्रेज़ी का बेहिचक प्रयोग हुआ था। इस संस्करण में मैंने अंग्रेज़ी के अधिकांश अनुच्छेदों को हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया है। पर कहीं-कहीं अंग्रेज़ी के वाक्य और टुकड़े पूर्ववत् मौजूद हैं। अपने हिन्दी लेखन में अंग्रेजी का स्वच्छन्द प्रयोग करने वाले कई रचनाकारों की तरह किसी समय मैं भी रचना-प्रक्रिया की गहनता से जूझे बिना, दिमाग पर ज़रा-सा दबाव पड़ते ही, किस तरह अंग्रेज़ी की ओर लपकता था, इसका आभास अब भी इस पुस्तक से मिल जाएगा।
उन दिनों पत्र-पत्रिकाओं में निकलनेवाली इसकी समीक्षाओं से मैं उतना ही प्रोत्साहित हुआ था जितना इसकी धीमी बिक्री से प्रकाशकों को निरुत्साहित होना चाहिए था। पर निश्चय ही उनका उत्साह संदेह से परे है। वे इस उपन्यास का अब नया संस्करण निकाल रहे हैं। मैं आभारी हूं।
इस संस्करण में-एक अपवाद छोड़कर-मूल पुस्तक को यथावत् रहने दिया गया है। अपवाद मूल पुस्तक के अंग्रेज़ी अनुच्छेदों के विषय में है। अपने आरम्भिक रचनाकाल में भाषा के, और विशेषतया कथा-साहित्य में पात्रों के वार्तालाप की भाषा के बारे में मैं उतना सचेत न था। इससे अज्ञातवास के कुछ स्थलों में अंग्रेज़ी का बेहिचक प्रयोग हुआ था। इस संस्करण में मैंने अंग्रेज़ी के अधिकांश अनुच्छेदों को हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया है। पर कहीं-कहीं अंग्रेज़ी के वाक्य और टुकड़े पूर्ववत् मौजूद हैं। अपने हिन्दी लेखन में अंग्रेजी का स्वच्छन्द प्रयोग करने वाले कई रचनाकारों की तरह किसी समय मैं भी रचना-प्रक्रिया की गहनता से जूझे बिना, दिमाग पर ज़रा-सा दबाव पड़ते ही, किस तरह अंग्रेज़ी की ओर लपकता था, इसका आभास अब भी इस पुस्तक से मिल जाएगा।
समर्पण
इस उपन्यास में रजनीकांत गाँव के होकर भी वहां की आंतरिकता से अपरिचित रहे। कच्ची झोपड़ियां और पक्के बंगले, तुलसी ओर क्रोटन इनके अन्तर की तुच्छता में ही वे उलझे रहे। इनसे ऊपर उठकर जीवन के बृहत्तर परिवेश में वे अपने को नहीं पहचान सके।
ठीक इसके विपरीत श्रीमती गिरिजा शुक्ल के साथ हुआ। उन्होंने पहले कभी गांव न देखा था। शादी होने के बाद ही वे पहली बार एक गांव में आईं। तब बरसात शुरू हो गई थी और ग्राम्यगीतों और सौम्य कविताओं के सम्मिलित षड़्यंत्र के बावजूद रास्तों और मकानों में सीलन, कीचड़, मच्छर, मलेरिया और सांप-बिच्छू का ही आकर्षण था। पर कीचड़ से लथपथ और मलेरिया से जर्जर गाँव की संक्रामक आत्मा ने उन्हें अपनी ओर खींचा और दोनों ने एक-दूसरे को अपना लिया।
जीवन के प्रति एक शांत, सम्यक् दृष्टि का परिचय देते हुए बाहरी वातावरण से ऊपर उठकर उन्होंने वहाँ की मानवीय स्थिति को आत्मसात् करने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने यथार्थ के सहज और आंतरिक सौंदर्यका वरण किया।
पति होकर भी आज तक मैं उनकी इस प्रवृत्ति को छोटा बनाकर नहीं देख पाया।
विवाहित जीवन के उन प्रारम्भिक दिनों का स्मरण करते हुए अपनी यह कृति उन्हें ही अर्पित करता हूं।
ठीक इसके विपरीत श्रीमती गिरिजा शुक्ल के साथ हुआ। उन्होंने पहले कभी गांव न देखा था। शादी होने के बाद ही वे पहली बार एक गांव में आईं। तब बरसात शुरू हो गई थी और ग्राम्यगीतों और सौम्य कविताओं के सम्मिलित षड़्यंत्र के बावजूद रास्तों और मकानों में सीलन, कीचड़, मच्छर, मलेरिया और सांप-बिच्छू का ही आकर्षण था। पर कीचड़ से लथपथ और मलेरिया से जर्जर गाँव की संक्रामक आत्मा ने उन्हें अपनी ओर खींचा और दोनों ने एक-दूसरे को अपना लिया।
जीवन के प्रति एक शांत, सम्यक् दृष्टि का परिचय देते हुए बाहरी वातावरण से ऊपर उठकर उन्होंने वहाँ की मानवीय स्थिति को आत्मसात् करने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने यथार्थ के सहज और आंतरिक सौंदर्यका वरण किया।
पति होकर भी आज तक मैं उनकी इस प्रवृत्ति को छोटा बनाकर नहीं देख पाया।
विवाहित जीवन के उन प्रारम्भिक दिनों का स्मरण करते हुए अपनी यह कृति उन्हें ही अर्पित करता हूं।
श्रीलाल शुक्ल
चित्र की ओर कुछ देर बराबर देखते रहने के बाद रजनीकान्त ने पूछा, और इसका नाम क्या है ?’’ राजेश्वर सरलता से हंसा; बोला, नाम के ही मामले में मैं कमज़ोर पड़ता हूं। मेरे मन में कुछ बिम्ब उभरते हैं, उन्हीं के सहारे चित्र बनता जाता है। चित्र बन जाता है, पर मैं नाम नहीं खोज पाता। नाम ढूँढ़ने के लिए चित्रकार नहीं, कवि होना पड़ता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘क्या हर्ज है, थोड़ देर के लिए कवि ही सही....’’ राजेश्वर फिर वैसे ही हंसा। कहने लगा, ‘‘मैं कवि नहीं हो सकता, मेरे शब्द कमज़ोर हैं। तभी तो रंगों और रेखाओं का सहारा लिया है।’’
रजनीकान्त के मन में आया, कुछ देर उससे शब्दों की कविता और रेखाओं की कविता की अभिन्नता पर बहस की जाय। पर उन्होंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया।
हर साल इंजीनियरिंग कॉलिज से निकले हुए कुछ तेज़ विद्यार्थी उनकी मातहती में इन्जीनियर होकर आते हैं। उस समय माहवारी तनख्वाह पानेवालों की उनमें परम्परागत विनम्रता नहीं होती। हर बात में वे अपनी राय देते हैं, हर बात पर बहस कर सकते हैं। उनको चुप करने के लिए रजनीकान्त ने एक गम्भीर मुस्कराहट का आविष्कार किया है, जिसके सहारे वे बिना कुछ कहे ही बहुत से तर्कों का जवाब दे देते हैं। इस समय उसी मुस्कराहट को अपने चेहरे पर फैलाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी, चित्र का कुछ नाम तो रखा ही होगा।’’
राजेश्वर ने कुछ हिचकते हुए कहा, ‘‘जी, कोई नाम रखना जरूरी ही हो तो इसे ‘अज्ञातवास’ कह सकते हैं। आपकी क्या राय है ?’’ कहकर उसने प्रभा की ओर देखा।
प्रभा की निगाह भी चित्र पर ही लगी थी। कुछ सोचकर रजनीकान्त से बोली, ‘‘इससे अच्छा शीर्षक और हो ही क्या सकता है पापा ?’’
सामाजिक जीवन की यह नाटकीय मुस्कराहट उनके चेहरे पर धुंधली पड़ गई। बिना किसी को लक्ष्य किए, धीरे से प्रश्न-सा करते हुए बोले, ‘‘अज्ञातवास ?’’
जिस चित्र को लेकर ये बातें हो रही थीं उसमें कोई भारी विशेषता न थी। केवल गझनार के पेड़ों का एक घना जंगल था।
वे पेड़ गहरे हरे थे और पीछे काले होते चले गए थे। सामने के दो-तीन पेड़ों के बीच छुटी हुई गोलाकार जगह में शाम की फैलती हुई कालिख पहले की लोहित आभाओं को घेरती चली आ रही थी। पर उसके पीछे छायाएं न थीं। छाया की जगह क्रम से काले पड़ते हुए घने पेड़ों का अनियमित विस्तार-भर था। और कुछ न था।
इस चित्र को देखते-देखते कुछ खो देने की, कुछ भूल जाने की, कहीं भटक जाने की-सी उदासी उनके मन में फैल गई थी। जैसे वे क्लब में व्हिस्की पी रहे हों और बिलियर्ड खेल रहे हों, और पड़ोस के कमरे से कह-कहे और नाच की धुनें कानों में आ रही हों, तभी उन्हें कोई बाहर बुलाकर ले आए, रोशनी, गर्मी, मस्ती और ठहाकों से दूर ले जाकर किसी वीरान और ठिठुरन-भरी सड़क पर अकेला छोड़ दे और वे हाथ में क्यू लिए हुए, आस्तीन की बांहें समेटे, समझ न सकें कि क्या हो रहा है।
उन्हें खुद नहीं मालूम कि वह चित्र देखकर उन्हें कैसा लगा। जैसे किसी ने बन्द कमरे के झरोखे से रात के पिछले पहर खुले स्वतंत्र आकाश में शुक्रतारा देखा हो, किसी ने थके मन से जोड़-बाकी का हिसाब लगाते समय दूर से बहक आती हुई किसी रागिनी के अधखुले स्वर सुने हों। जैसे दफ्तर की फाइलों से दबे हुए मन में बहुत दिन पहले सुनी हुई कविता की कोई विश्रृंखल पंक्ति अचानक ही कहीं से उभर आई हो ! ऐसा ? शायद ऐसा नहीं। यह अनुभव कुछ दूसरी ही तरह का था।
राजेश्वर शहर से यहां तक अपनी पेंटिंग बेचने के लिए लाया था। चित्र बनाने के पहले उसके मन में रंगों के चाहे जितने ही इन्द्रधनुष क्यों न खिंचे हों, पर उसके खत्म होते ही उसने अनुभव किया कि उसकी जेब और उसके साथ ही साथ उसका दिमाग खाली है। परिणाम यह हुआ कि जिसमें अपने चित्र का नामकरण तक करने की व्यावहारिकता न थी, उसे विवशतः अपने प्रशंसक रजनीकांत की तलाश में उनकी कोठी पर जाना पड़ा। फिर पता लगाते-लगाते वह घोर देहात में नहर से लगे हुए इस डाक बँगले तक चला आया।
शाम होनेवाली थी। राजेश्वर ने कहा, ‘‘मुझे आज्ञा हो तो जाऊं। रात दस बजे वाली गाड़ी से वापस लौट जाऊंगा।’’
उन्होंने एक चेक लिखकर उसके हाथ में दिया। बोले, ‘‘इसे अपने चित्र की कीमत मत समझना। मैं इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, यह इसी मजबूरी की सनद है।’’ कहकर उन्होंने हंसने की कोशिश की।
फिर प्रभा को बुलाकर कहा, ‘‘प्रभा बेटी, गंगाधर के लिए कार स्टेशन जा रही होगी, राजेश्वरजी उसी से क्यों नहीं चले जाते ?’’
राजेश्वर के चले जाने के बाद वे उस चित्र को बरामदे से उठाकर कमरे में ले आए। उसे एक कोने में, छोटी-सी मेज के ऊपर दीवाल के सहारे टिका दिया। फिर एक बड़ी आरामकुर्सी पर लेट गए। उसका शीर्षक बार-बार उनके मन की दीवालों से, बन्द कमरे में भटकनेवाली मधुमक्खी की तरह, टकराता रहा।
सोचते रहे :
आज कोई इन घने होते हुए जंगलों में खो गया है। आज यह जीवन दिशा खोकर भटक रहा है, निरुद्देश्य बीत रहा है।
पहले भी ऐसा था। पर तब वह इसी कारण किसी किशोरी-सा आकर्षक था। जिसे लगाव की उंगलियों ने छुआ नहीं, जिसके वर्तमान में कौतूहल है, भविष्य में अस्पष्ट मादकता है। तब प्रत्येक भाव इसे छेड़ने आता। इसे अपनाना चाहता। आकर्षक दिखने के लिए सिद्धान्त का चेहरा लगाकर आता। पर अब धीरे-धीरे वह भीड़ भी छंट रही है। दूर पड़ते हुए को पकड़ने के लिए यह उद्देश्यहीनता पागल-सी दौड़ रही है। या, चुपचाप बैठकर अपने आप पर खीझ रही है, प्रौढ़ा अविवाहिता-सी।
इस कमरे की खिड़की खुली है और अगहन की हवा बहकर अन्दर आ रही है। पछुआ हवा। अलसी और मटर के नीले-बैंगनी फूलों को छेड़ती हुई। बांसों के झुरमुट में सीटी-सी बजाती। मुरझाते कमल-वनों पर उसांस-सी छोड़ती। डाक्टर करते हैं, इस हवा से बचो। मैं खिड़की बन्द करना चाहता हूं। पर उठना नहीं चाहता, किसी को पुकार भी नहीं सकता।
मैं यूं ही रहा हूं। बहुत कुछ करना चाहता हूं। करने में कोई बाधा नहीं है, पर नहीं करता। वैसे जब कुछ कर लेता हूं तब सोचता हूं कि यही करना चाहता था। जो किया नहीं, उसके लिए सोचना चाहता हूं कि उसे कभी चाहा नहीं। अपने कृतित्व की तुष्टि के लिए अतीत की अंधेरी गुफाओं से न जाने कितने नगण्य, उपेक्षित कृतियाँ ढूंढ़कर लाता हूं, स्मृति की उपलब्धियां !
फिर भी कहीं कुछ चुभता-सा रहता है।
कभी-कभी जान पड़ता है, चारों ओर से फंस गया हूं। सामने उजाला था। उसे छोड़कर जहाँ आ गया हूं, वहां अंधेरा है, चारों ओर पेड़ों के घने झुरमुट हैं जो राह रोकते हैं, और अब सोचने की जगह भी नहीं। वहां भी काले जंगल हैं। सोचने की जो जगह पहले घेर चुका था, वे जंगल उस पर भी हमलावार हो रहे थे। कुछ झाड़ियाँ से उग आई हैं। कंटीली घास पनप रही है।
सोचते-सोचते वे उद्विग्न हो गए। फिर और सोचने लगे। जैसे कभी-कभी अपने ही मांस में अपना नाखून गड़ाते रहते पर खाल की तीखी जलन में भी जो कुछ मिलता-सा है, जैसे कोई अपनी ही हथेली पर बेंत-सा लगाता है....।
‘‘पापा, आज शिकार नहीं होगा क्या ? आपने कपड़े तक नहीं बदले ?’’
उनके मन में घने काले पेड़ों के झुरमुट एक धब्बा-सा बना रहे थे, जिन पर मिले-जुले, घने, अचल पत्ते थे। चिड़ियां नहीं थीं। बोले, ‘‘नहीं, आज मैं यहीं रहूंगा। गंगाधर एण्ड कम्पनी आनेवाली है। दो-एक घण्टे में वे लोग आ जाएंगे।’’
रेशमी, सुगन्धित, रूखे बालों के गुच्छे। पछुवा में उड़ते हुए। सुनहले मत्थे और एक आंख पर तैरते-से, एक उंगली से उन्हें बालों की असंख्यता में समेटते हुए उसने धीरे से दोहराया, ‘‘गंगाधर एऽऽण्ड कऽऽम्पनी।’’ हलकी लिपिस्टिक में खिले हुए होंठ। उनपर एक हलकी वक्रता-सी फैली।
शायद उन्होंने सुना नहीं। एक असभ्य-सी अंगड़ाई लेते हुए थकी आवाज में बोले, ‘‘चिड़ियां मारते-मारते जी भर गया !’’
इस आवाज़ में कुछ है। पापा की आवाज़ ऐसी नहीं है : उसके मन में आया। ढीले-ढाले गाउन में वे सोफे पर पड़े सिगार पी रहे थे। पी कहाँ रहे थे, वह होंठों में दबा हुआ था। न जाने कब बुझ गया था। वह आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। कन्धे पर धीरे से हाथ रखकर बोली, ‘‘क्यों पापा ? गंगाधर एण्ड कम्पनी के लिए भी दो-एक काज़ें न मारिएगा ?’’ पर उन्होंने सिर हिलाया। उसी थकान के साथ कहा, ‘‘नहीं प्रभा, किसी के भी लिए नहीं !’’ कहकर वे संभलकर सोफे पर बैठ गए। पास की मेज़ से सिगार जलाने के लिए लाइटर उठा लिया।
तो, यह थकान कैसी है ? जो दिन-भर के आराम के बाद, स्वस्थ शरीर की वेगवती दृढ़ता में भी नहीं बह पाती ? उन्होंने लाइटर फिर वैसे ही मेज़ पर रख दिया। सिगार बुझा हुआ है।
सामने आकर प्रभा ने लाइटर जलाया, वे मुस्कराए। धीरे-धीरे उन्होंने सिगार जलाया। धीरे से ही उसका धुआं होठों के कोने से फूटकर बाहर निकल आया।
प्रभा उनके पास बैठ गई। गाउन की बांह पर हाथ फेरते हुए बोली, ‘‘क्या हुआ पापा ?’’
सामने एक बड़ी खिड़की थी। उसके पीछे साफ-सुथरा मखमली दूब का लॉन, फिर पतली सड़क, फिर चौड़ी रविशें। उसके बाद डाकबंगले की चहारदीवारी। गुड़हल की हरी-भरी, घनी, करीने से कटी हुई ऊंची हेज, उसके पार जो है वह दिखाई नहीं देता। कुछ दूर आगे बांसों के घने झाड़ों के पास धुएं की एक क्षीण रेखा पृथ्वी के समानान्तर फैली हुई। उस पार कोई गाँव होगा।
वे देखते रहे। प्रभा का सवाल धीरे से पचाकर, कुछ रुककर, बोले, ‘‘कुछ भी तो नहीं हुआ, प्रभा बेटी।’’
वे बेटी कह रहे हैं। उनके मन में कहीं कुछ कुरेदता है। तभी यह प्यार होंठों पर उभर रहा है। वह स्नेह की आवेग में हंसी। बाईस वर्ष की युवती। ऐसी हंसी दस साल पहले तन-मन को ढके रहती थी। अब यह हंसी कभी-कभी ही आती है। किसी पुराने परिचय की बन्धुता में मन को समेटती हुई, हंसती हुई बोली, ‘‘काज़ें झील में पड़ी हुई हैं। गंगाधर एण्ड कम्पनी आनेवाली है। कारतूसों के नये डिब्बे सवेरे ही आ चुके हैं और आप गुमसुम बैठे हुए हैं ? यह कुछ हुआ ही नहीं ? बताते क्यों नहीं, पापा, बात क्या है ?’’
सहसा उनके मन में बात करते रहने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। बोले, ‘‘बताऊं क्या बात है ? तुम समझ लोगी न ?’’
वे खड़े हो गए। खिड़की के पास जाकर उन्होंने अपने शरीर को सीधा किया—लगभग अड़तालीस वर्ष की अवस्था का पुष्ट शरीर। गोरा रंग। आंखों पर फ्रेम का चश्मा। कभी आकर्षक, कभी डरावनी-सी लगने वाली बड़ी आंखें चश्मे के अन्दर से और भी बड़ी दीख पड़ती हुईं। कनपटियों में और कानों के ऊपर बाल सफेद होने लगे हैं, मत्थे पर दो-तीन शिकनें खिंचती हैं, मिटती हैं। फिर भी लगता है, यौवन को इस आकार में बहुत कुछ मिल गया है। जेल में अपने किसी प्रियजन से मिलने आए हुए भावुक व्यक्ति-सा यौवन ! समय हो जाने पर भी जाना नहीं चाहता !
प्रभा देखती रही। उनकी पीठ का बहुत-सा भाग, चेहरे के किनारे चश्मे के फ्रेम की झलक, वह देखती रही। सिगार का धुआं दो-तीन लहरों में बहता हुआ आया। धीरे-धीरे गुंजलकों में ऊपर की ओर उठ गया।
उनकी आंखों के आगे असाढ़ की एक सांझ अपनी स्वर्णाभा में डूब-उतरा रही थी। लगभग अट्ठाईस साल पहले की शाम।
वे इंजीनिरियरिंग कॉलिज में प्रवेश पा चुके थे। दूसरे दिन उन्हें जाना था, नीचे मां उनके जाने की तैयारी में लगी थी। वे छत पर एक किनारे खड़े गांव की पूर्वी सीमा की ओर देख रहे थे। खेत थे, खेतों के पार पलाश-वन था।
अचानक उन्हें एक खनक सुन पड़ी। चांदी, सोना, आकांक्षा, ऐश्वर्य, कविता—सबका मिला-जुला अस्फुट स्वर। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जीने की आखिरी सीढ़ी पर दरवाजे की ओट खड़ी हुई रानी उन्हें हाथ के इशारे से बुला रही थी।
वे जाकर उसके पास खड़े हो गए। बड़े स्नेह से पूछा, ‘‘क्या बात है ?’’
उसने उन्हें देखा। फिर लजाकर दूसरी ओर देखने लगी। हंसी के बहाव को रोकते हुए बोली, ‘‘कुछ भी तो नहीं।’’
अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को दोनों ओर से घेरकर उन्होंने फिर पूछा, ‘‘क्या बात है रानी, बोलो न ?’’ लाज और उसी के साथ भीतर न दब पानेवाले आवेग-उल्लास के कारण उसका तेहरा तमतमाया जा रहा था। उन्होंने उसके मुँह को अपने पास, अपने सामने खींच लिया था, फिर भी चंचल आंखें किसी असंभव दिशा में भागकर छिपना चाहती थीं। धीरे से उन्होंने रानी को अपनी ओर समेटा। इस बार बिना किसी विरोध के वह और भी पास आ गई। अपने सिर को रजनीकांत के कन्धे के सहारे टिकाकर, आंखें मूंद एक क्षण चुपचाप खड़ी रही। वे उसकी उद्धत, उतप्त सांसें सुनते रहे। उसके मत्थे पर घिरे असंयत बालों को संवारते रहे।
फिर उसने आंखें खोलीं। पूछा, ‘‘वहां अकेले क्यों खड़े थे ?’’
उन्होंने कहा, ‘‘चलो, वहीं चलकर देखें, तब मालूम होगा मैं वहां क्यों खड़ा था।’’
बच्चों की तरह घबराहट से सिर हिलाकर वह बोली, ‘‘न, न ! मैं वहां कैसे जा सकती हूं। दूर-दूर से लोग देखेंगे नहीं, मैं छत पर खड़ी हूं। क्या कहेंगे, बताओ ?’’
वे हँसने लगे। बनावटी सरलता के साथ पूछा, ‘‘क्या कहेंगे, बताओ न ?’’
रानी ने कहा, ‘‘मैं कुछ नहीं जानती। यहीं से बताओ, वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे थे ?’’
रजनीकांत पूर्व की ओर फैली हुई निर्बाध हरियाली को देखते रहे। फिर हाथ उठाकर इशारा करते हुए बोले, ‘‘वह देखो रानी, मैं यही देख रहा था।’’
एक मचलती हुई आवारा शाम। पागल हवाएं। ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की मजबूरी में बंधी, क्षितिज को पल्लवों से छूने के लिए चारों ओर उड़ती हुई बेसब्र टहनियां। हाथ-पैर पटकती हुई रूठी लताएँ। पूर्व के आकाश में एक-दूसरे को ज़ोर-ज़ोर से ठेलते हुए, बदमस्त, मटमैले बादल। शोरगुल और गरज। सहमकर भागती, छिपती हुई बिजलियां। गिरते हुए सूरज को नीचे ढकेलकर, काले मेघों के बन्धनों को तोड़कर, बेकाबू बढ़ती हुई, टीलों को चूमती, पेड़ों के गले लिपटती बेशर्म किरणें। ढलानें और कछारों, बागों और मैदानों में बेतक्कलुफी से लेटती अस्थिर परछाइयां।
सब कुछ अनियंत्रित, असंयत।
कुछ ही क्षणों में इन रक्त-श्याम मेघों का मायालोक मिटनेवाला था। किरणें उसी तिमिर-लोक में वापस लौट जाने वाली थीं। पर अभी पूर्व का पलाश-वन साफ दिख रहा था। वर्षा के प्रथम आसार से धुली हुई, लहर लेती हुई हरियाली। यह वन कितनी दूर तक फैला चला गया है ! इसके उस पार फिर घनी बागें मिलेंगी, खेत होंगे....पर रजनीकांत के घर की छत से यही लगता था कि उसके पार भी एक और वन होगा, कुछ और घना, कुछ और रहस्यमय। फैलती हुई छायाएं, मिटती हुई रक्तिम आभा, चमकती हुई हरियाली—इस सबका निस्सीम सघन विस्तार वे देखते रहे। बोले, ‘‘रानी तुम देख रही हो न ? मैं कल जा रहा हूँ। मेरा यह हरा-भरा संसार कुछ दिनों के लिए पीछे छूट जाएगा।’’
उन्हें लगा, रानी की निगाह उनके चेहरे पर गड़-सी गई है। शायद वह उनकी ओर उसी आग्रह से, आसन्न वियोग की उसी उत्कटता से देख रही थी, जिस तरह वे इस पलाश-वन को देखते रहे थे। फिर बड़े प्यार से, हलके व्यंग्य से बोली, ‘‘हां, तुम्हारे पीछे छूटनेवाले तो यह ऊसर जंगल ही हैं। इनके साथ तुम्हारा कोई और भी पीछे छूट रहा है, कभी यह भी सोचोगे ?’’
कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपने-आपको भुला दिया। अपनी इस नवपरिणीता पत्नी के दबे आवेग ने उनके उस पूरे आवेग को उभार दिया जिसे वे जान-बूझकर दिन-भर दबाते रहे थे। आषाढ़ की उस डूबती-उतराती शाम की निरंकुशता उसके मन को झकझोरने लगी। अपने को रानी के आगे पूरी तरह अर्पित करते हुए उन्होंने अस्पष्ट स्वरों में कहा, ‘‘रानी, तुम कुछ नहीं समझतीं। मेरा अपना संसार क्या है—तुम यह कुछ नहीं समझतीं।’’
आज सब कुछ बदल चुका है। केवल उन वनों का लैंडस्केप सामने है।
पर इस लैंडस्केप में उजाले पर काले जंगलों का आक्रमण हो रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘क्या हर्ज है, थोड़ देर के लिए कवि ही सही....’’ राजेश्वर फिर वैसे ही हंसा। कहने लगा, ‘‘मैं कवि नहीं हो सकता, मेरे शब्द कमज़ोर हैं। तभी तो रंगों और रेखाओं का सहारा लिया है।’’
रजनीकान्त के मन में आया, कुछ देर उससे शब्दों की कविता और रेखाओं की कविता की अभिन्नता पर बहस की जाय। पर उन्होंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया।
हर साल इंजीनियरिंग कॉलिज से निकले हुए कुछ तेज़ विद्यार्थी उनकी मातहती में इन्जीनियर होकर आते हैं। उस समय माहवारी तनख्वाह पानेवालों की उनमें परम्परागत विनम्रता नहीं होती। हर बात में वे अपनी राय देते हैं, हर बात पर बहस कर सकते हैं। उनको चुप करने के लिए रजनीकान्त ने एक गम्भीर मुस्कराहट का आविष्कार किया है, जिसके सहारे वे बिना कुछ कहे ही बहुत से तर्कों का जवाब दे देते हैं। इस समय उसी मुस्कराहट को अपने चेहरे पर फैलाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी, चित्र का कुछ नाम तो रखा ही होगा।’’
राजेश्वर ने कुछ हिचकते हुए कहा, ‘‘जी, कोई नाम रखना जरूरी ही हो तो इसे ‘अज्ञातवास’ कह सकते हैं। आपकी क्या राय है ?’’ कहकर उसने प्रभा की ओर देखा।
प्रभा की निगाह भी चित्र पर ही लगी थी। कुछ सोचकर रजनीकान्त से बोली, ‘‘इससे अच्छा शीर्षक और हो ही क्या सकता है पापा ?’’
सामाजिक जीवन की यह नाटकीय मुस्कराहट उनके चेहरे पर धुंधली पड़ गई। बिना किसी को लक्ष्य किए, धीरे से प्रश्न-सा करते हुए बोले, ‘‘अज्ञातवास ?’’
जिस चित्र को लेकर ये बातें हो रही थीं उसमें कोई भारी विशेषता न थी। केवल गझनार के पेड़ों का एक घना जंगल था।
वे पेड़ गहरे हरे थे और पीछे काले होते चले गए थे। सामने के दो-तीन पेड़ों के बीच छुटी हुई गोलाकार जगह में शाम की फैलती हुई कालिख पहले की लोहित आभाओं को घेरती चली आ रही थी। पर उसके पीछे छायाएं न थीं। छाया की जगह क्रम से काले पड़ते हुए घने पेड़ों का अनियमित विस्तार-भर था। और कुछ न था।
इस चित्र को देखते-देखते कुछ खो देने की, कुछ भूल जाने की, कहीं भटक जाने की-सी उदासी उनके मन में फैल गई थी। जैसे वे क्लब में व्हिस्की पी रहे हों और बिलियर्ड खेल रहे हों, और पड़ोस के कमरे से कह-कहे और नाच की धुनें कानों में आ रही हों, तभी उन्हें कोई बाहर बुलाकर ले आए, रोशनी, गर्मी, मस्ती और ठहाकों से दूर ले जाकर किसी वीरान और ठिठुरन-भरी सड़क पर अकेला छोड़ दे और वे हाथ में क्यू लिए हुए, आस्तीन की बांहें समेटे, समझ न सकें कि क्या हो रहा है।
उन्हें खुद नहीं मालूम कि वह चित्र देखकर उन्हें कैसा लगा। जैसे किसी ने बन्द कमरे के झरोखे से रात के पिछले पहर खुले स्वतंत्र आकाश में शुक्रतारा देखा हो, किसी ने थके मन से जोड़-बाकी का हिसाब लगाते समय दूर से बहक आती हुई किसी रागिनी के अधखुले स्वर सुने हों। जैसे दफ्तर की फाइलों से दबे हुए मन में बहुत दिन पहले सुनी हुई कविता की कोई विश्रृंखल पंक्ति अचानक ही कहीं से उभर आई हो ! ऐसा ? शायद ऐसा नहीं। यह अनुभव कुछ दूसरी ही तरह का था।
राजेश्वर शहर से यहां तक अपनी पेंटिंग बेचने के लिए लाया था। चित्र बनाने के पहले उसके मन में रंगों के चाहे जितने ही इन्द्रधनुष क्यों न खिंचे हों, पर उसके खत्म होते ही उसने अनुभव किया कि उसकी जेब और उसके साथ ही साथ उसका दिमाग खाली है। परिणाम यह हुआ कि जिसमें अपने चित्र का नामकरण तक करने की व्यावहारिकता न थी, उसे विवशतः अपने प्रशंसक रजनीकांत की तलाश में उनकी कोठी पर जाना पड़ा। फिर पता लगाते-लगाते वह घोर देहात में नहर से लगे हुए इस डाक बँगले तक चला आया।
शाम होनेवाली थी। राजेश्वर ने कहा, ‘‘मुझे आज्ञा हो तो जाऊं। रात दस बजे वाली गाड़ी से वापस लौट जाऊंगा।’’
उन्होंने एक चेक लिखकर उसके हाथ में दिया। बोले, ‘‘इसे अपने चित्र की कीमत मत समझना। मैं इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, यह इसी मजबूरी की सनद है।’’ कहकर उन्होंने हंसने की कोशिश की।
फिर प्रभा को बुलाकर कहा, ‘‘प्रभा बेटी, गंगाधर के लिए कार स्टेशन जा रही होगी, राजेश्वरजी उसी से क्यों नहीं चले जाते ?’’
राजेश्वर के चले जाने के बाद वे उस चित्र को बरामदे से उठाकर कमरे में ले आए। उसे एक कोने में, छोटी-सी मेज के ऊपर दीवाल के सहारे टिका दिया। फिर एक बड़ी आरामकुर्सी पर लेट गए। उसका शीर्षक बार-बार उनके मन की दीवालों से, बन्द कमरे में भटकनेवाली मधुमक्खी की तरह, टकराता रहा।
सोचते रहे :
आज कोई इन घने होते हुए जंगलों में खो गया है। आज यह जीवन दिशा खोकर भटक रहा है, निरुद्देश्य बीत रहा है।
पहले भी ऐसा था। पर तब वह इसी कारण किसी किशोरी-सा आकर्षक था। जिसे लगाव की उंगलियों ने छुआ नहीं, जिसके वर्तमान में कौतूहल है, भविष्य में अस्पष्ट मादकता है। तब प्रत्येक भाव इसे छेड़ने आता। इसे अपनाना चाहता। आकर्षक दिखने के लिए सिद्धान्त का चेहरा लगाकर आता। पर अब धीरे-धीरे वह भीड़ भी छंट रही है। दूर पड़ते हुए को पकड़ने के लिए यह उद्देश्यहीनता पागल-सी दौड़ रही है। या, चुपचाप बैठकर अपने आप पर खीझ रही है, प्रौढ़ा अविवाहिता-सी।
इस कमरे की खिड़की खुली है और अगहन की हवा बहकर अन्दर आ रही है। पछुआ हवा। अलसी और मटर के नीले-बैंगनी फूलों को छेड़ती हुई। बांसों के झुरमुट में सीटी-सी बजाती। मुरझाते कमल-वनों पर उसांस-सी छोड़ती। डाक्टर करते हैं, इस हवा से बचो। मैं खिड़की बन्द करना चाहता हूं। पर उठना नहीं चाहता, किसी को पुकार भी नहीं सकता।
मैं यूं ही रहा हूं। बहुत कुछ करना चाहता हूं। करने में कोई बाधा नहीं है, पर नहीं करता। वैसे जब कुछ कर लेता हूं तब सोचता हूं कि यही करना चाहता था। जो किया नहीं, उसके लिए सोचना चाहता हूं कि उसे कभी चाहा नहीं। अपने कृतित्व की तुष्टि के लिए अतीत की अंधेरी गुफाओं से न जाने कितने नगण्य, उपेक्षित कृतियाँ ढूंढ़कर लाता हूं, स्मृति की उपलब्धियां !
फिर भी कहीं कुछ चुभता-सा रहता है।
कभी-कभी जान पड़ता है, चारों ओर से फंस गया हूं। सामने उजाला था। उसे छोड़कर जहाँ आ गया हूं, वहां अंधेरा है, चारों ओर पेड़ों के घने झुरमुट हैं जो राह रोकते हैं, और अब सोचने की जगह भी नहीं। वहां भी काले जंगल हैं। सोचने की जो जगह पहले घेर चुका था, वे जंगल उस पर भी हमलावार हो रहे थे। कुछ झाड़ियाँ से उग आई हैं। कंटीली घास पनप रही है।
सोचते-सोचते वे उद्विग्न हो गए। फिर और सोचने लगे। जैसे कभी-कभी अपने ही मांस में अपना नाखून गड़ाते रहते पर खाल की तीखी जलन में भी जो कुछ मिलता-सा है, जैसे कोई अपनी ही हथेली पर बेंत-सा लगाता है....।
‘‘पापा, आज शिकार नहीं होगा क्या ? आपने कपड़े तक नहीं बदले ?’’
उनके मन में घने काले पेड़ों के झुरमुट एक धब्बा-सा बना रहे थे, जिन पर मिले-जुले, घने, अचल पत्ते थे। चिड़ियां नहीं थीं। बोले, ‘‘नहीं, आज मैं यहीं रहूंगा। गंगाधर एण्ड कम्पनी आनेवाली है। दो-एक घण्टे में वे लोग आ जाएंगे।’’
रेशमी, सुगन्धित, रूखे बालों के गुच्छे। पछुवा में उड़ते हुए। सुनहले मत्थे और एक आंख पर तैरते-से, एक उंगली से उन्हें बालों की असंख्यता में समेटते हुए उसने धीरे से दोहराया, ‘‘गंगाधर एऽऽण्ड कऽऽम्पनी।’’ हलकी लिपिस्टिक में खिले हुए होंठ। उनपर एक हलकी वक्रता-सी फैली।
शायद उन्होंने सुना नहीं। एक असभ्य-सी अंगड़ाई लेते हुए थकी आवाज में बोले, ‘‘चिड़ियां मारते-मारते जी भर गया !’’
इस आवाज़ में कुछ है। पापा की आवाज़ ऐसी नहीं है : उसके मन में आया। ढीले-ढाले गाउन में वे सोफे पर पड़े सिगार पी रहे थे। पी कहाँ रहे थे, वह होंठों में दबा हुआ था। न जाने कब बुझ गया था। वह आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। कन्धे पर धीरे से हाथ रखकर बोली, ‘‘क्यों पापा ? गंगाधर एण्ड कम्पनी के लिए भी दो-एक काज़ें न मारिएगा ?’’ पर उन्होंने सिर हिलाया। उसी थकान के साथ कहा, ‘‘नहीं प्रभा, किसी के भी लिए नहीं !’’ कहकर वे संभलकर सोफे पर बैठ गए। पास की मेज़ से सिगार जलाने के लिए लाइटर उठा लिया।
तो, यह थकान कैसी है ? जो दिन-भर के आराम के बाद, स्वस्थ शरीर की वेगवती दृढ़ता में भी नहीं बह पाती ? उन्होंने लाइटर फिर वैसे ही मेज़ पर रख दिया। सिगार बुझा हुआ है।
सामने आकर प्रभा ने लाइटर जलाया, वे मुस्कराए। धीरे-धीरे उन्होंने सिगार जलाया। धीरे से ही उसका धुआं होठों के कोने से फूटकर बाहर निकल आया।
प्रभा उनके पास बैठ गई। गाउन की बांह पर हाथ फेरते हुए बोली, ‘‘क्या हुआ पापा ?’’
सामने एक बड़ी खिड़की थी। उसके पीछे साफ-सुथरा मखमली दूब का लॉन, फिर पतली सड़क, फिर चौड़ी रविशें। उसके बाद डाकबंगले की चहारदीवारी। गुड़हल की हरी-भरी, घनी, करीने से कटी हुई ऊंची हेज, उसके पार जो है वह दिखाई नहीं देता। कुछ दूर आगे बांसों के घने झाड़ों के पास धुएं की एक क्षीण रेखा पृथ्वी के समानान्तर फैली हुई। उस पार कोई गाँव होगा।
वे देखते रहे। प्रभा का सवाल धीरे से पचाकर, कुछ रुककर, बोले, ‘‘कुछ भी तो नहीं हुआ, प्रभा बेटी।’’
वे बेटी कह रहे हैं। उनके मन में कहीं कुछ कुरेदता है। तभी यह प्यार होंठों पर उभर रहा है। वह स्नेह की आवेग में हंसी। बाईस वर्ष की युवती। ऐसी हंसी दस साल पहले तन-मन को ढके रहती थी। अब यह हंसी कभी-कभी ही आती है। किसी पुराने परिचय की बन्धुता में मन को समेटती हुई, हंसती हुई बोली, ‘‘काज़ें झील में पड़ी हुई हैं। गंगाधर एण्ड कम्पनी आनेवाली है। कारतूसों के नये डिब्बे सवेरे ही आ चुके हैं और आप गुमसुम बैठे हुए हैं ? यह कुछ हुआ ही नहीं ? बताते क्यों नहीं, पापा, बात क्या है ?’’
सहसा उनके मन में बात करते रहने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। बोले, ‘‘बताऊं क्या बात है ? तुम समझ लोगी न ?’’
वे खड़े हो गए। खिड़की के पास जाकर उन्होंने अपने शरीर को सीधा किया—लगभग अड़तालीस वर्ष की अवस्था का पुष्ट शरीर। गोरा रंग। आंखों पर फ्रेम का चश्मा। कभी आकर्षक, कभी डरावनी-सी लगने वाली बड़ी आंखें चश्मे के अन्दर से और भी बड़ी दीख पड़ती हुईं। कनपटियों में और कानों के ऊपर बाल सफेद होने लगे हैं, मत्थे पर दो-तीन शिकनें खिंचती हैं, मिटती हैं। फिर भी लगता है, यौवन को इस आकार में बहुत कुछ मिल गया है। जेल में अपने किसी प्रियजन से मिलने आए हुए भावुक व्यक्ति-सा यौवन ! समय हो जाने पर भी जाना नहीं चाहता !
प्रभा देखती रही। उनकी पीठ का बहुत-सा भाग, चेहरे के किनारे चश्मे के फ्रेम की झलक, वह देखती रही। सिगार का धुआं दो-तीन लहरों में बहता हुआ आया। धीरे-धीरे गुंजलकों में ऊपर की ओर उठ गया।
उनकी आंखों के आगे असाढ़ की एक सांझ अपनी स्वर्णाभा में डूब-उतरा रही थी। लगभग अट्ठाईस साल पहले की शाम।
वे इंजीनिरियरिंग कॉलिज में प्रवेश पा चुके थे। दूसरे दिन उन्हें जाना था, नीचे मां उनके जाने की तैयारी में लगी थी। वे छत पर एक किनारे खड़े गांव की पूर्वी सीमा की ओर देख रहे थे। खेत थे, खेतों के पार पलाश-वन था।
अचानक उन्हें एक खनक सुन पड़ी। चांदी, सोना, आकांक्षा, ऐश्वर्य, कविता—सबका मिला-जुला अस्फुट स्वर। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जीने की आखिरी सीढ़ी पर दरवाजे की ओट खड़ी हुई रानी उन्हें हाथ के इशारे से बुला रही थी।
वे जाकर उसके पास खड़े हो गए। बड़े स्नेह से पूछा, ‘‘क्या बात है ?’’
उसने उन्हें देखा। फिर लजाकर दूसरी ओर देखने लगी। हंसी के बहाव को रोकते हुए बोली, ‘‘कुछ भी तो नहीं।’’
अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को दोनों ओर से घेरकर उन्होंने फिर पूछा, ‘‘क्या बात है रानी, बोलो न ?’’ लाज और उसी के साथ भीतर न दब पानेवाले आवेग-उल्लास के कारण उसका तेहरा तमतमाया जा रहा था। उन्होंने उसके मुँह को अपने पास, अपने सामने खींच लिया था, फिर भी चंचल आंखें किसी असंभव दिशा में भागकर छिपना चाहती थीं। धीरे से उन्होंने रानी को अपनी ओर समेटा। इस बार बिना किसी विरोध के वह और भी पास आ गई। अपने सिर को रजनीकांत के कन्धे के सहारे टिकाकर, आंखें मूंद एक क्षण चुपचाप खड़ी रही। वे उसकी उद्धत, उतप्त सांसें सुनते रहे। उसके मत्थे पर घिरे असंयत बालों को संवारते रहे।
फिर उसने आंखें खोलीं। पूछा, ‘‘वहां अकेले क्यों खड़े थे ?’’
उन्होंने कहा, ‘‘चलो, वहीं चलकर देखें, तब मालूम होगा मैं वहां क्यों खड़ा था।’’
बच्चों की तरह घबराहट से सिर हिलाकर वह बोली, ‘‘न, न ! मैं वहां कैसे जा सकती हूं। दूर-दूर से लोग देखेंगे नहीं, मैं छत पर खड़ी हूं। क्या कहेंगे, बताओ ?’’
वे हँसने लगे। बनावटी सरलता के साथ पूछा, ‘‘क्या कहेंगे, बताओ न ?’’
रानी ने कहा, ‘‘मैं कुछ नहीं जानती। यहीं से बताओ, वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे थे ?’’
रजनीकांत पूर्व की ओर फैली हुई निर्बाध हरियाली को देखते रहे। फिर हाथ उठाकर इशारा करते हुए बोले, ‘‘वह देखो रानी, मैं यही देख रहा था।’’
एक मचलती हुई आवारा शाम। पागल हवाएं। ऊँचे-ऊँचे पेड़ों की मजबूरी में बंधी, क्षितिज को पल्लवों से छूने के लिए चारों ओर उड़ती हुई बेसब्र टहनियां। हाथ-पैर पटकती हुई रूठी लताएँ। पूर्व के आकाश में एक-दूसरे को ज़ोर-ज़ोर से ठेलते हुए, बदमस्त, मटमैले बादल। शोरगुल और गरज। सहमकर भागती, छिपती हुई बिजलियां। गिरते हुए सूरज को नीचे ढकेलकर, काले मेघों के बन्धनों को तोड़कर, बेकाबू बढ़ती हुई, टीलों को चूमती, पेड़ों के गले लिपटती बेशर्म किरणें। ढलानें और कछारों, बागों और मैदानों में बेतक्कलुफी से लेटती अस्थिर परछाइयां।
सब कुछ अनियंत्रित, असंयत।
कुछ ही क्षणों में इन रक्त-श्याम मेघों का मायालोक मिटनेवाला था। किरणें उसी तिमिर-लोक में वापस लौट जाने वाली थीं। पर अभी पूर्व का पलाश-वन साफ दिख रहा था। वर्षा के प्रथम आसार से धुली हुई, लहर लेती हुई हरियाली। यह वन कितनी दूर तक फैला चला गया है ! इसके उस पार फिर घनी बागें मिलेंगी, खेत होंगे....पर रजनीकांत के घर की छत से यही लगता था कि उसके पार भी एक और वन होगा, कुछ और घना, कुछ और रहस्यमय। फैलती हुई छायाएं, मिटती हुई रक्तिम आभा, चमकती हुई हरियाली—इस सबका निस्सीम सघन विस्तार वे देखते रहे। बोले, ‘‘रानी तुम देख रही हो न ? मैं कल जा रहा हूँ। मेरा यह हरा-भरा संसार कुछ दिनों के लिए पीछे छूट जाएगा।’’
उन्हें लगा, रानी की निगाह उनके चेहरे पर गड़-सी गई है। शायद वह उनकी ओर उसी आग्रह से, आसन्न वियोग की उसी उत्कटता से देख रही थी, जिस तरह वे इस पलाश-वन को देखते रहे थे। फिर बड़े प्यार से, हलके व्यंग्य से बोली, ‘‘हां, तुम्हारे पीछे छूटनेवाले तो यह ऊसर जंगल ही हैं। इनके साथ तुम्हारा कोई और भी पीछे छूट रहा है, कभी यह भी सोचोगे ?’’
कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपने-आपको भुला दिया। अपनी इस नवपरिणीता पत्नी के दबे आवेग ने उनके उस पूरे आवेग को उभार दिया जिसे वे जान-बूझकर दिन-भर दबाते रहे थे। आषाढ़ की उस डूबती-उतराती शाम की निरंकुशता उसके मन को झकझोरने लगी। अपने को रानी के आगे पूरी तरह अर्पित करते हुए उन्होंने अस्पष्ट स्वरों में कहा, ‘‘रानी, तुम कुछ नहीं समझतीं। मेरा अपना संसार क्या है—तुम यह कुछ नहीं समझतीं।’’
आज सब कुछ बदल चुका है। केवल उन वनों का लैंडस्केप सामने है।
पर इस लैंडस्केप में उजाले पर काले जंगलों का आक्रमण हो रहा है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book