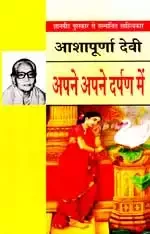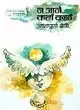|
नारी विमर्श >> अपने अपने दर्पण में अपने अपने दर्पण मेंआशापूर्णा देवी
|
375 पाठक हैं |
||||||
इस उपन्यास की पटभूमि एक बंगाली समाज है जो एक बदलाव के मोड़ से गुज़र रहा है। यहाँ प्राचीन धारणाओं, प्राचीन आदर्शों तथा मूल्यबोध पर आधारित मानव जीवन नवीन सभ्यता की चकाचौंध से कुछ विभ्रांत-सा हो गया है।...
भले ही गृहिणी हों, थी तो इसी परिवार की वधू-'कुल-वधू।' उनका अकेले सड़क
किनारे दलान पर बैठना शोभा नहीं देता। हालाँकि बीच में पड़ी खाली बंजर जमीन से
रास्ता दूर ही पड़ जाता था, फिर भी लोग तो देखेंगे राय-परिवार की गृहिणी बैठी
हैं!
और अब?
बीच-बीच में जब शक्तिनाथ सोचते हैं तो एक अजीब कौतुक का अनुभव होता है
उन्हें।
हालाँकि घर बिल्कुल वैसा ही है। वही दलान, सामने की खाली जमीन। केवल सड़क में
बदलाव आया है।
ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क के बदले 'पीचरोड' बन गया है।
पुराने नियम से आज भी सोम और शुक्रवार को हाट बैठती है। परंतु उसी से सटकर एक
बाजार लगता है रोज, वहाँ भी हाट जैसी भीड़ लगी रहती है। क्योंकि आदमी की
संख्या बढ़ गई है। बहुत अधिक बढ़ गई है। कब किस तरह बढ़ गई, पता नहीं चला।
पहले इस मंडल विष्णुपुर गाँव में राह चलते ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता था जिसे
गाँव का कोई न पहचानता हो। कोई चेहरा अनजाना-सा लगा तो तुरंत टोक देते थे,
'तुमको तो ठीक से पहचानते नहीं भाई?' पूछ-ताछ करके निश्चिंत होते थे-जब वह
किसी का कुटुम्ब या भांजा या नाती लगता था। जो कभी-कभार आते हैं, रत्ती-भर से
छ: फीट के होकर, उन्हें पहचानने में कठिनाई तो होती ही है।
अब तो अनजाने लोगों से रास्ते, दुकान-बाजार सब भर गये हैं! अब तो कोई किसी को
पुकार कर नहीं पूछता, 'किस घर के कुटुम्ब हो भाई?.....पहचान में नहीं आ रहे
हो!'
अब तो घर के परिचित लोग भी उस अनजानी भीड़ में खो जाते हैं। कोई घर से बाहर
निकलता है तो सूना-सा लगता है, जैसे कहीं खो गया हो।
अब तो सुबह सात-पैंतालीस की लोकल ट्रेन से निकल कर, फिर रात के आठ-बारह वाले
'लोकल' से लौट कर आने की भी निश्चयता नहीं है। साढ़े आठ, नौ, दस कुछ भी हो
सकता है। निश्चयता नहीं है, इसी कारण निश्चिंतता भी नहीं है।
जबकि शक्तिनाथ के जमाने में कैसा अचूक था आठ-बारह का वह 'लोकल'! स्टेशन से घर
पैदल आने में शक्तिनाथ को अट्ठारह मिनट के करीब लगते थे, अत: साढ़े आठ
बजते-बजते खेतू चाय का पानी चढ़ा देती थी। हालाँकि बाद में यह काम मुक्ति की
पत्नी रमोला करने लगी थी।
ट्रेन का भी इधर-उधर नहीं था, कदमों का भी नहीं। डेली पैसेंजरों की गतिविधि
चाँद-सूरज की तरह ही अटूट नियम से बँधी रहती थी।
आज के लोगों को इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जा सकता है। क्योंकि 'नियम'
शब्द ही आज शब्दकोष से निकल गया है। आजकल घर-भर के प्राय: सभी डेली-पैसेंजरी
करते हैं, स्त्री-पुरुष सभी। 'डेली पैसेंजर' शब्द का कोई स्त्रीलिंग
शब्द नहीं है। कम-से-कम शक्तिनाथ की जानकारी में नहीं है। लेकिन स्त्री-पुरुष
बराबर कदमों से यह डेली-पैसेंजरी किये जा रहे हैं।
क्या योगनाथ कभी दुःस्वप्न में भी कल्पना कर सकते थे कि उन्हीं के घर की
बहू-बेटियाँ डेली-पैसेंजरी करेंगी!
योगनाथ ही क्यों? क्या शक्तिनाथ ही कल्पना कर सकते थे, जब वह खुद जाते थे?
नहीं। अंग्रेजों के जमाने में किसी महिला ने डेली-पैसेंजर नहीं देखा।
कर्मकेंद्र कलकत्ते के दो बड़े-बड़े स्टेशन ऑफिस-टाइम पर सीना बिछाकर बैठे रहते
थे, हर घंटे धोती-शर्ट, शर्ट-कोट, कोट-दुशाला और जूते पहने लोग नयी-नयी
तरंगों की तरह उस पर से निकल जाते थे।
साड़ी-ब्लाउज, जूड़े-चोटी, काजल-बिंदी के कोमल स्पर्श उन्हें नसीब नहीं होते
थे।
केवल नीरस गद्य, केवल नीरस कठिन पुरुष के पदचाप।
शक्तिनाथ भी उन्हीं में से एक थे। स्वभाव से शौकीन थे इसलिए कभी भी सिर्फ
धोती-कमीज या जैसे-तैसे मोजे के बिना ही जूते में पाँव डाल कर नहीं भागते थे।
मुहल्ले के सारे 'लोकल' पकड़ने वालों में शक्तिनाथ सबसे जल्दी नींद से उठते थे
क्योंकि उनकी वेश-भूषा त्रुटिहीन होती थी, भोजन भी आडम्बर के साथ होता था और
हमेशा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के कारण कभी भी खाना खाकर दौड़ नहीं लगाते
थे। तेज कदमों से ही सही, पर आराम से चलकर जाते थे।
साफ-सुथरी चूनट वाली धोती, उसके ऊपर डबल काफ सिल्क टुईल की कमीज और उसके भी
ऊपर कीमती कोट पहनते थे। चैक वाले मोजे और पॉलिश से चकाचक फीते बँधे शू पहन
कर जब शक्तिनाथ पान का डब्बा हाथ में लेकर चमकाते हुए स्टेशन का रास्ता नापते
थे तो देखकर लगता था कोई राजपुरुष जा रहे हैं।
लगता था जब तक शक्तिनाथ पहुँचेंगे नहीं, उनके साहब लोग अनाथ होकर पड़े रहेंगे।
शक्तिनाथ के नाम के साथ उनकी प्रकृति का कोई विरोध नहीं था। वास्तविक रूप से
शक्तिमान थे वह। डेढ़-पौने दो मील का रास्ता चुटकी में तय कर लेते थे।
खैर, जाते तो मुहल्ले के सभी थे। घोष-परिवार का अभिलाष, दत्ता के घर का वह
सदा-बीमार लड़का-नंद या कुछ नाम था जिसका, अट्ठारह साल का पोचा जिसे मैट्रिक
पास करते ही नौकरी लग गई थी, पैदल कौन नहीं जाता था? कितनों के पास साइकिल थी
ही? मगर एक है दनदना कर जाना और एक है मर-मर कर जाना। अधिक उम्र में शौक से
एक साईकिल खरीदी थी शक्तिनाथ ने, मगर वह उनकी किस्मत में अधिक दिन रही नहीं।
उनका बड़ा भतीजा मुक्तिनाथ बारह-तेरह वर्ष की उम्र से ही उस साइकिल का भागीदार
बन बैठा था। 'देख तेरा है कि मेरा' बस साइकिल लेकर नौ-दो-ग्यारह हो जाता था।
अत: शक्तिनाथ दयालु होकर कहने लगे, मुझे उसमें आराम नहीं मिलता है, घुटनों
में दर्द होता है। तू ही चला उसे।
अर्थात् अब मुक्तिनाथ के लज्जित या कुंठित होने का सवाल नहीं रहा। मझले चाचा
को साईकिल चलाने से घुटने में दर्द होता है, साईकिल में पड़े-पड़े जंग लग
जाएगा, तभी न वह इसे चालू रखता है?
मन-ही-मन लेह-भरी हँसी हँसकर शक्तिनाथ ने सोचा-'तुझे इतना अच्छा लगता है, तू
ही ले ले,' कहने से कहीं शरमा जाय इसीलिए न यह कौशल करना पड़ा।
अच्छा, स्नेह-ममता यह सब क्या धीरे-धीरे मानव-मन से लुप्त होता जा रहा है?
शक्तिनाथ सोचने लगे-मुक्ति के बच्चों से भक्ति का तो उतना लगाव दिखाई नहीं
देता? मुक्ति का भी तो भक्ति के बच्चों पर, ब्रतीनाथ की बेटी के ऊपर कोई
स्नेह दिखाई नहीं देता है। ये उनके सगे ताऊ-चाचा हैं, यह तो पता ही नहीं चलता
है, जैसे दूर के रिश्तेदार हों। मानो एक घर में रहते हैं केवल इसीलिए बातचीत
करते हैं।
यह सब देखकर कभी-कभी खेतू बहुत क्रोधित होकर कहती है, 'जा ही तो रहा है!
बिल्कुल गायब होता जा रहा है! क्यों नहीं होगा? आदमी के तन में कोई
'स्नेह' पदार्थ जा भी रहा है क्या? तन में नहीं जाएगा तो मन में कहाँ से
आएगा? तन से ही मन है। किसने पहले सोचा था भैया कि इस मंडल विष्णुपुर के
लोगों को दूध नसीब नहीं होगा, घी का नाम भूल जाएँगे? हमलोग इस दुनिया में आये
ही हैं कितने दिन? दो सौ बरस भी नहीं, सौ बरस भी नहीं, सत्तर से नीचे ही हैं
अभी! इसी बीच कितनी बार यह दुनिया पलट गई, बोलो? क्या देख चुके हैं और क्या
देख रहे हैं! तब तो दिन-रात कहते थे, अंगरेज लोग हमारा सब लूटकर खा रहे हैं,
मगर वह खाना 'गिरस्थ' लोग की नज़र में नहीं पड़ता था। उनका तो सबकुछ ठीक-ठाक
चलता था।
हमहीं लोगों को ले लो। दूध-घी, दही, मक्सन, छेना, खोवा सब खाते थे कि नहीं?
और अब क्या हो रहा है? अब कौन लूटकर खा रहा है इस देश को?'
खेतू गृहस्थी चलाने में कुशल होते हुए भी बाहरी दुनिया के विषय में बिल्कुल
अनभिज्ञ है और अपनी इस कमी को बिना सोचे-समझे सबके सामने खोलकर रख देती है।
आजकल के बच्चों के सामने अपनी खिल्ली भी उड़वाती है। खेतू अगर जोरदार आवाज़
में घोषित करे, पेट में 'स्नेह पदार्थ' की कमी के कारण मन में स्नेह का अभाव
हो रहा है, अमरीका के गेहूँ खा-खाकर ही इस युग के बच्चे अमरीकियों की तरह
लापरवाह, मस्तान होते जा रहे हैं, या मछली-भात की जगह रोटी-गोश्त खाकर ही
बंगालियों का स्वभाव अड़ियल, रूखा-सूखा होता जा रहा है, तो क्या हँसेंगे नहीं
ये लोग?
|
|||||