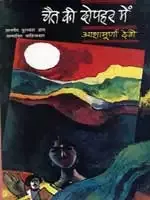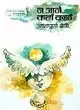|
नारी विमर्श >> चैत की दोपहर में चैत की दोपहर मेंआशापूर्णा देवी
|
162 पाठक हैं |
||||||
चैत की दोपहर में नारी की ईर्ष्या भावना, अधिकार लिप्सा तथा नैसर्गिक संवेदना का चित्रण है।...
वक्तव्य
बांग्ला लेखिका श्रीमती आशापूर्णा देवी का जन्म 8 जनवरी, सन् 1910 को हुआ।
पिछले साठ वर्षों में अपनी 175 औपन्यासिक तथा कथा कृतियों के माध्यम से आपने
मानव स्वभाव के अनेक पक्षों को उजागर किया। बंकिम, रवीन्द्र और शरतचन्द्र के
पश्चात् आशापूर्णा ही ऐसा सुपरिचित नाम है, जिसकी प्रत्येक कृति पिछली आधी
शताब्दी में बांग्ला और अन्य भाषाओं में एक नई उपेक्षा से पढ़ी जाती रही है।आशापूर्णा देवी का बचपन और कैशोर्य कलकत्ता में ही बीता। उनके पिता एक कलाकार थे और मां साहित्य की जबरदस्त पाठिका। उनके पास अपने कहने को एक छोटा-भोटा पुस्तकालय भी था। एक कट्टरपंथी परिवार के नाते आशापूर्णा को उनकी दूसरी बहनों के साथ स्कूली पढ़ाई की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन परिवार में उपलब्ध पुस्तकों को पढ़ने की कोई रोक-टोक न थी। मां के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रभाव आशापूर्णा के कृतित्व पर सबसे अधिक पड़ा।
आशापूर्णा देवी की आरम्भिक रचनाएं द्वितीय महायुद्ध के दौरान लिखी गई थीं। उनकी कहानियां किशोरवय के पाठकों के लिए होती थीं। पाठकों के लिए उनकी पहली कहानी ''पत्नी ओ प्रेयसी'' (1937) ई० मे प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर आज तक पिछले साठ वर्षो से, नारी के तन और मन के दो अनिवार्य ध्रुवान्तों के बीच उठने वाले कई शाश्वत प्रश्नों को पारिवारिक मर्यादा और बदलते किसी साहित्यकार ने नहीं रखा।
आशापूर्णा देवी का पहला कहानी-संकलन ''जल और आगुन'' (1940) ई. में प्रकाशित हुआ था तब यह कोई नहीं जानता था कि भारतीय कथा-साहित्य के मंच पर एक ऐसी कथानेत्री व्यक्तित्व का आगमन हो चुका है जो समाज की कुंठा और कुत्सा, संकट और संघर्ष, जुगुप्सा और लिप्सा को अपने पात्र-संसार के माध्यम से एक नया प्रस्थान और मुक्त आकाश प्रदान करेगी।
इसके साथ, अन्य असंख्य नारौ पात्रों-मां, बहन, दीदी, मौसी, दादी, बुआँ, तथा घर के और भी सदस्य, नाते और रिश्तेदार यहाँ तक नौकर-चाकर की मनोदशा का भी जितनी सहजता और विशिष्टता से प्रामाणिक अंकन उनके कथा-साहित्य में हुआ है। वह अन्यत्र दुर्लभ है।
आशापूर्णा जब 13 वर्ष की थीं तब प्रबल उमंग में उन्होंने एक कविता की रचना की तथा एक सुपरिचित बाल पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेज दी वह कविता प्रकाशित ही नहीं हुई वरन् संपादक की ओर से और रचनाओं के लिए अनुरोध भी प्राप्त हुआ। यही अनुरोध आशापूर्णा देवी के साहित्यिक उभार का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना। 15 वर्ष की आयु में उन्हें साहित्यिक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला जिससे उनके उत्साह में और अभिवृद्धि हुई। सौभाग्य के पश्चात उनकी कोई रचना संपादकों से कभी लौटाई नहीं गई। इस प्रकार उनका लेखन तभी से अविराम गति जीवन का एक अंग बन गया।
आशापूर्णा की विश्वविद्यालय की औपचारिक पढ़ाई नहीं मिली। अपने बाल्य-काल से ही वे जिज्ञासा और कौतूहल से भरी दुनिया का साक्षात्कार करती रहीं। यह ठोस दुनिया रोज किसी-न-किसी रूप में नये वातायन और वातावरण के साथ उनके सामने उपस्थित हो जाती थीं और अपने अनौखे और अजूबे पात्रों का संसार उनके लिए जुटा देती थी। एक स्त्री होने के नाते उन्होंने स्त्री-पात्रों की मानसिकता, उनके नारी सुलभ स्वभाव की दुर्बलताओं-दर्प, दंभ, द्वंद्व, दासता और अन्यमनस्कता का चित्रण भी अपनी रचनाओं में खूब किया। अनगिनत नारी पात्राओं के पारदर्शी संसार द्वारा इन रचनाओं में सामान्य किन्तु अविस्मरणीय पात्रों का एक ऐसा अविराम एवं जीवन्त संसार मुखरित अबाध और जटिल यात्रा का पथ भले ही गरीबी, शोषण, अभाव, कोलाहल, उन्माद, प्रेम-घृणा और अवसाद से परिपूर्ण हो लेकिन उनकी रचनाओं में जीवन और परिवेश के बीच एक अटूट और सार्थक संवाद चलता रहता है।
'प्रेम और प्रयोजन'' (1945) आशापूर्णा देवी की पहली औपन्यासिक कृति थी। आज से लगभग 48 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। लेकिन इसके सारे सवाल और सन्दर्भ आज भी प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। पिछले पचास-साठ बर्षों में स्वाधीनता-आन्दोलन की प्रेरणाओं, स्वतन्त्रता प्राप्ति, नई-पुरानी सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, नारी शिक्षा स्वातन्त्र्य, कामकाजी महिलाएं, नगरों का अभिशप्त जीवन, मूल्यों संकट जैसे तमाम विषयों से अलग रही हैं वे तमाम समस्याओं, छोटे-बड़े आन्दोलनों को सड़कों पर नहीं, घर की चारदीवारी के अन्दर रखकर उनका समाधान प्रस्तुत करती है। पात्रों के आस-पास घटित होने वाली घटनाओ का सूक्ष्म अंकन कर विवरण प्रस्तुत करती हैं तभी किसी निष्कर्ष पर पहुँचती हैं। उनके पात्र हमारे साथ चल रहे जीवन के अनखुले पृष्ठों और अनचीन्हे संदर्भों को इस तरह खुलकर व्याख्यातित करती हैं। अचानक सामने पाकर यही प्रतीत होता है कि इस जानी-पहचानी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा हमारी नज़रों से अब तक ओझल क्योंकर रहा? उनकी सारी स्थापनाएँ भारतीय परिवेश, मर्यादा और स्वीकृत तथा प्रदत्त पारिवारिक ढांचे के अनुरूप होती हैं। नारी के आत्मनिर्णय और आत्मगौरव को सर्वाधिक महत्त्व देती हैं। नारी के आत्मनिर्णय और सामाजिक अन्याय के सिलाफ उन्होंने भरपूर वकालत की है।
आशापूर्णा भारतीय नारी के आधुनिका होने के नाम पर उच्छृ खल या पारिवारिक मर्यादाओं की अनदेखी करने का न तो प्रस्साव रखती हैं और न ही उसकी ऐसी कोई पैरवी करती हैं जिससे कि अपनी किसी बात को एक जिद्दी दलील के तौर पर उद्धृत किया जाये।
उन्होंने समाज के विभिन्न स्तरों पर ऐसे असंख्य पात्रों की मनोदशाओं का चित्रण किया है जो अबोले हैं, या जो खुद नहीं बोलते-भले ही दूसरे लोग उनके बारे में हजार तरह की बातें करें।
आशापूर्णा समाजशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या दार्शनिक की मुद्रा ओढ़कर था आधुनिक या प्रगतिशील लेखिका होने का मुखौटा नहीं लगातीं। वे अपनी जमीन और अपने सन्दर्भ को खूब अच्छी तरह देखती-परखती हैं। आशापूर्णा ने अपने स्त्री पात्रों को अनजाने और अपरिचित कोने से उठाया और सबके बीच और सबके साथ रखा। उसे रसोईघर की दुनिया से बाहर निकालकर बृहत्तर परिवेश देना चाहा। जहाँ नारी का माता-पत्नी और बेटी वाला शाश्वत रूप सुरक्षित रहा, वहाँ सामाजिक बदलाव की भूमिका में भी उसके सक्रिय और वांछित, योगदान को अंकित किया गया।
आशापूर्णा का मानना है कि भारतीय नारी का सारा जीवन सामाजिक अवरोधों और वंचनाओं में ही कट जाता है जिसे उसकी तपस्या कहकर हमारा समाज गौरवान्वित होता आया है। नारी जाति की असहायता को ही वाणी देने में उनकी सृजनात्मकता सुकारथ हुई है।
लेखिका ने उच्चवर्गीय या धनी-मानी परिवारों की स्त्रियों की विवशता या दयनीयता का भी चित्रण किया है, जहाँ अब भी वे कोई निर्णय नहीं ले सकतीं।
चैत की दोपहर में आशापूर्णा देवी ने एक ऐसी ही स्त्री की विवशता को दर्शाया है। उपन्यास की नायिका-अवंती सादी के पहले अरण्य को प्यार करती थी। अवंती सम्पन्न घर लड़की थी और अरण्य साधारण परिवार का युवक। अरण्य अवंती से शादी करने का आग्रह करता है पर अवंती उसे कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करते को कहती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book