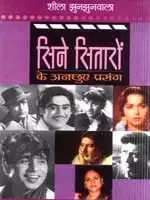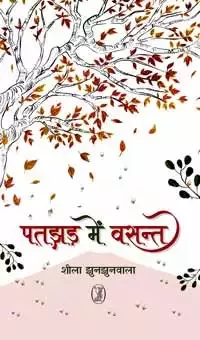|
सिनेमा एवं मनोरंजन >> सिने सितारों के अनछुए प्रसंग सिने सितारों के अनछुए प्रसंगशीला झुनझुनवाला
|
41 पाठक हैं |
||||||
पुस्तक में कुछ सशक्त सिने सितारों की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को बहुत ही नजदीक से, अंतरंगता के साथ उभारने का प्रयत्न किया गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
लेखिका ने इस पुस्तक में कुछ सशक्त सिने सितारों की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को बहुत ही नजदीक से, अन्यतम अंतरंगता के साथ उभारने का प्रयत्न किया है। अशोक कुमार एकमात्र अभिनेता थे, जिन्होंने
पूरे सात दशक फिल्म जगत् में बिताए और इस दौर के गौऱवशाली इतिहास व
उत्थान-पतन के चश्मदीद गवाह रहे। दिलीप कुमार,
राजकपूर एवं देव आनंद इस कड़ी के दूसरी पीढ़ी के सशक्त एवं
संवेदनशील अभिनेता रहे जिन्होंने अपनी मौलिक एवं सर्वग्राह्य अभिनय-शैली
द्वारा अलग-अलग अभिनय स्कूल कायम किए, जिसकी नकल अनेक अभिनेताओं ने की।
तीसरी पीढ़ी के अभिनेता अभिताभ बच्चन ने ‘दीवार’ व ‘शोले’ से फिल्म-निर्माण की शैली व दिशा एकदम से बदल देने तथा आर्थिक पतन के कगार पर खड़े फिल्म उद्योग में अपनी एक्शन फिल्मों के जरिए नए प्राण फूँकने व उसे नवस्फूर्ति प्रदान करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
इस पुस्तक में किशोर कुमार, जया बच्चन और वहीदा रहमान भी अहम किरदार हैं। आशा है, फिल्म जगत् के 92 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए इस पुस्तक की अहम भूमिका होगी।
तीसरी पीढ़ी के अभिनेता अभिताभ बच्चन ने ‘दीवार’ व ‘शोले’ से फिल्म-निर्माण की शैली व दिशा एकदम से बदल देने तथा आर्थिक पतन के कगार पर खड़े फिल्म उद्योग में अपनी एक्शन फिल्मों के जरिए नए प्राण फूँकने व उसे नवस्फूर्ति प्रदान करने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
इस पुस्तक में किशोर कुमार, जया बच्चन और वहीदा रहमान भी अहम किरदार हैं। आशा है, फिल्म जगत् के 92 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए इस पुस्तक की अहम भूमिका होगी।
92 वर्ष भारतीय सिनेमा के
उन्नीस सौ
अस्सी के दशक में अंतराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध जापानी फिल्म
निर्देशक अकीरा कुरूसोवा ने मुझसे भारतीय सिनेमा, खासकर हिंन्दी सिनेमा की
मौजूदा समस्याओं पर बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय सिनेमा, खासकर आपका
हिंदी सिनेमा कभी भी नहीं मर सकता, लाख उस पर विपत्तियाँ आएँ, भले ही वह
इससे कुछ समय के लिए डाँवाडोल हो जाए, समस्याओं के चक्रव्यूह में फँस जाए
और उसे अपनी नींव डगमगाती-डोलती दिखलाई दे, तब भी उस पर असर नहीं होगा।
हॉलीवुड की तरह ही भारतीय सिनेमा में शुरू से ही समय-समय पर बुद्धि जीवी,
प्रतिभाशाली एंव समर्पित ऐसे फिल्मकार होते हैं, और होते रहेंगे दो आपके
सिनेमा की मँझधार में फँसी नाव को आसानी से किनारे ले आएँगे। सबसे
महत्त्वपूर्ण बात यह हुई है कि भारतीय सिनेमा समय और दर्शकों की बदलती
अभिरूचियों व माँग के तरह खुद में परिवर्तन करता रहा है।
हॉलीवुड के
जीवंत रहने का भी यही कारण है और परिवर्तनशीलता की यह प्रवृत्ति ही भारतीय
सिनेमा के हमेशा अक्षुण्ण रहने का भी कारण है। जापान, पोलैंड, रूस,
फ्रासं, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया आदि तमाम देशों में सिनेमा
इसलिए
मरणासन्न की राह पर है क्योंकि वे समय की माँग के अनुसार खुद को बदलने की
चाह नहीं रखते। इसीलिए इन देशों के फिल्म-निर्माण में भारी गिरावट तेजी से
आती जा रही है। इन्होंने खुद भी नहीं बदला तो खुद अपनी मौत मर जाएँगे,
क्योंकि सिनेमा एवं टेलीविजन तकनीक में बहुत शीघ्र ही क्रांति होने वाली
है बल्कि इस क्रांति का श्रीगणेश हो गया है। कई देशों में टेलीविजन फिल्म
उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरने लगा है।
अकीरा कुरूसोवा ने सही ही कहा था। आने वाले दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, पोलैंड में सिनेमा सचमुच न केवल मौत की कगार पर पहुँच गया, बल्कि उसकी दिन-ब-दिन घुटती साँस पर टेलीविजन पर प्रदर्शित टी० वी० धारावाहिकों एवं टेलीफिल्मों ने एक के बाद एक सलीब टाँगने भी शुरू कर दिए थे। अगर जापानी व चीनी सिनेमा में अचानक ब्रुस ली और उनके मार्शल आर्ट का पदार्पण नहीं हुआ होता तो जापानी व चीनी सिनेमा अपने ही बनाए हुए ताबूतों में कभी के दफन हो गए होते। जिस समय कुरुसोवा ने यह बात कही थी, जापान में जहाँ प्रतिवर्ष 200 से 300 फिल्में बनती थीं, उनकी संख्या घटकर 50-60 ही रह गई थी। जब हमारी अकीरा कुरूसोवा से बातचीत हुई थी, तब भारत में भी टेलीविजन धीरे-धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। किंतु तब भी नए टी० वी० चैनलों के सामने बैठकर धारावाहिकों एवं टेलीफिल्मों को देखने की बात लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। केबल एवं वीडियो पायरेसी के खतरे की बातें भी तब किसी के जेहन में नहीं थीं। तब फिल्म उद्योग सेंसर बोर्ड के कहर, संगीत की धुनों की नकल और 16 एम० एम० के प्रोजेक्टर वाले उन छोटे-छोटे तथाकथित सिनेमाघरों की मार सह रहा था जहाँ फिल्म रिलीज के पहले या रिलीज होते ही नई फिल्मों को प्रदर्शित कर दिया जाता था। ये फिल्में फिल्म लेबोरेटरीज या सिनेमाघरों के प्रोजेक्टरों द्वारा गैरकानूनी ढंग से 16 एम० एम० पर ट्रांसफर कर ली जाती थीं औऱ ये सिनेमाघर घनी बस्तियों, चालों, झोपड़पट्टियों में एक छोटे-से बंद कमरे में दीवार पर 16 एम० एम० का पर्दा या सफेद चादर अथवा दीवार पर सफेद पेंट करवाकर मिनी थियेटर के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते थे। तब फिल्म-निर्माताओं की एकमात्र संस्था ‘इम्पा’ इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हर उपाय कर रही थी, लेकिन सिनेमा तकनीक, वीडियो सी०डी० तथा टेलीविजन की क्रांतिकारी आँधी के बावजूद न तो तब भारतीय सिनेमा मरा और न ही अब जब उसके सामने समस्याओं के असंख्य पहाड़ ढेर सारे सिनेमाघर बंद कर दिए गए, राज्यों में मनोरंजन कर आसमान की ऊँचाइयाँ छूने लगा, टी०वी० धारावाहिकों व वीडियो पायरेसी के निरंतर प्रहार उस पर होते रहे, लेकिन इसके बावजूद विश्व सिनेमा में हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड (भारतीय सिनेमा) का स्थान दूसरे नंबर पर है।
ऐसा कैसे हुआ ? अकीरा कुरूसोवा की भविष्यवाणी सही कैसे साबित हुई ? इसका जवाब भी तब उन्होंने दिया था-समय और माँग के अनुराग भारतीय सिनेमा में परिवर्तन का उसका लचीला रूख और नई-नई प्रतिभाओं का उदय इसका कारण है।’ दादा साहब फालके से लेकर आज के युवा निर्देशक करण जौहर और अन्य युवा पीढ़ी के फिल्मकारों का उदय, ‘राजा हरिश्चंद’ से लेकर अब तक की प्रदर्शित सुपरहिट फिल्में, सालुंके से लेकर आमिर खान, शाहरूख खान, हतिक रोशन जैसे सितारों के उदय का 92 वर्ष का अंतराल-भारतीय सिनेमा के अमरत्व का अक्षुण्ण महाकाव्य जो है। इस दौरान फिल्मों में, उनकी निर्माण-तकनीक, अभिनय-परंपरा व नृत्य-संगीत ने हजारों-हजार करवटें जो ली हैं। 92 वर्ष पहले सन् 1912 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फालके घुंडीराज गोविंद फालके-ने अगर लाइट ऑफ क्राइस्ट’ फिल्म नहीं देखी होती और क्राइस्ट की ही तरह कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को सेल्युलाइड पर उतारने की कल्पना न पिरोई होती तो शायद भारत में सिनेमा का श्रीगणेश ही नहीं हुआ होता। यह बात अलग है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म कृष्ण-चरित्र पर बनाने के बजाय 1912 के अंत में राजा हरिश्चंद्र के चरित्र पर ’राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जिसका प्रदर्शन 1913 में हुआ था। एक पारंपारिक पुजारी-परिवार में 30 अप्रैल,1870 को त्र्यंबकेश्वर (नासिक) में जन्मे घुंडीराज गोविंद फालके को उनके पिता अपनी ही तरह संस्कृत-पंडित बनाना चाहते थे। बचपन से ही उनकी रूचि पेंटिंग, नाटक, अभिनय और जादूगरी आदि विविध कलाओं की तरफ ज्यादा थी। इसीलिए जब पिता गोविंद फालके मुंबई के प्रख्यात एलफिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होकर मुंबई आए तो उन्होंने बेटे की रूचि को ध्यान में रखकर उनका एडमिशन जे०जे० स्कूल आँफ आर्ट्रस में करा दिया, जो आज भी भारत ही नहीं, समूचे एशिया में प्रथम श्रेणी का आर्ट्रस कॉलेज माना जाता है। यहाँ उन्होंने आर्ट्रस की अन्य विधाओं के साथ-साथ फोटोग्राफी भी सीखी। इसके बाद कला भवन व गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कुछ समय रहकर फोटोग्राफी व अन्य विधाओं में महारत हासिल की। उनकी फोटोग्राफी प्रतिभा से प्रभावित हो उन्हें एक फोटोग्राफी कंपनी ने इस शर्त पर फोटोग्राफी प्रिंटिंग की विकसित तकनीक का अध्ययन करने के लिए जर्मनी भेजा कि वहाँ से वापस लौटने पर उन्हें अनुबंध के मुताबिक निर्धारित अवधि तक उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। वापस लौटने के कुछ समय बाद 1910 में उनकी एक आँख खराब हो गई और काफी इलाज के बाद ही उससें रोशनी आ सकी।
उस कंपनी की नौकरी संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद वे अपने कैरियर की योजना बना ही रहे थे कि एक दिन उन्होंने लाइट ऑफ क्राइस्ट’ फिल्म देखी और उनके दिमाग में क्राइस्ट के चरित्र की ही तरह कृष्ण के चरित्र को लेकर फिल्म बनाने की कल्पना घर कर गई, लेकिन फिल्म-निर्माण संबंधी उपकरण तब भारत मे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख तथा दोस्तों से उधार ले वे फिल्म-निर्माण संबंधी उपकरण खरीदने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ वे प्रख्यात फिल्म-निर्माता सेसिल हेपबर्थ से भी मिले। उनसे फिल्म-निर्माण संबंधी तमाम जानकारियाँ प्राप्त कीं और वापस लौटकर फिल्म-निर्माण की योजना पर जुट गए। इसी बीच कृष्ण-चरित्र पर फिल्म बनाने की योजना रोककर राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फाइनेंस की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जब तारामती की भूमिका निभाने के लिए कोई वेश्या भी तैयार नहीं हुई तब एक रेस्तराँ में रसोइए का काम करने वाले सालुंसे को 15 रूपए पारिश्रमिक पर तारामती बनने के लिए राजी किया। पंद्रह हजार रूपय की लागत से 1912 में निर्मित 3700 फुट लंबी राजा हरिश्चंद’ 3 मई,1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो उसके विज्ञापन में छपा था-‘राजा हरिश्चंद-75 हजार चित्रों का नजारा। सिर्फ तीन आने में दो मील लंबी फिल्म का आनंद।’ सिनेमाघर में ‘राजा हरिश्चंद्र’ देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। हिंदी भाषा में प्रस्तुत यह चलती-फिरती फिल्म लोगों के लिए अचंभा भी थी और उत्सुकता-भरी अकूत जिज्ञासाओं का समंदर भी। इस सफलता ने घुंडिराज गोविंद फालके को दूसरी फिल्में बनाने, अपनी फिल्म यूनिट तैयार करने और एक बंद व ओपन स्टूडियो के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने ‘भस्मासुर-मोहिनी’ (1913), ‘सत्यवान-सावित्री’ (1914), ‘लंका दहन’, ‘कृष्ण जन्म’ आदि फिल्मों के निर्माण के साथ अपनी एक फिल्म यूनिट भी बनाई जिसके सदस्यों की संख्या बढ़ते-बढ़ते सौ से भी अधिक हो गई। ‘राजा हरिश्चंद्र’ की वाराणसी में शूटिंग कर उन्होंने जहाँ आउटडोर शूटिंग की शुरूआत की, वहीं नासिक में एक ऐसे स्थान पर स्टूडियो बनाया जिसके चारों तरफ पहाड़, नदीं, खेत-खलिहान थे ताकि एक ही जगह वे पूरी फिल्म की शूटिंग कर सकें। सालुंसे ने ‘राजा हरिश्चंद्र’ में नारी-वेश में जहाँ तारामती की भूमिका की थी वहीं ‘लंका दहन’ में उन्होंने राम और सीता दोनों की भूमिकाएँ निभाकर दोहरी भूमिका (डबल रोल) निभाने की परंपरा की भी शुरूआत की थी। दादा साहेब फालके ‘वन मैन शो’ थे-अपनी यूनिट के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, एडिटर, मेकअप मैन के साथ-साथ अभिनेता भी थे। बचपन व किशोरावस्था में सीखी जादू की कला का प्रदर्शन उन्होंन ‘प्रोफेसर खलीफा’ में जादूगर का रोल खुद निभाकर किया था। एक तरफ वे स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर थे तो दूसरी तरफ सुपर इंपोजिशन कला के महारथी। जब फिल्म ’कृष्ण जन्म’ में भगवान् श्रीकृष्ण के रूप में कलाकार पर्दें पर आया तो दर्शकों ने खड़े होकर हाथ जो़ड़े तथा पर्दें पर पैसे भी फेंके।
हिन्दी फिल्म-निर्माण की जो शुरूआत मराठी-भाषी महाराष्ट्रीयन घुंडिराज गोविंद फालके ने 1912 में की थी, उस कड़ी में जुड़ने के लिए और भी निर्माता-निर्देशक मैदान में आ गए। उनमें धीरेन गांगुली (इंग्लैंड रिटर्नः 1913) तथा बाबूराम पेंटर (सावकरी पाशः 1925) आदि प्रमुख थे। 1913 से 1937 तक मूक फिल्मों का दौर जारी रहा और हर तरह की फिल्मों का निर्माण हुआ। एक तरफ धार्मिक फिल्मों का बोलबोला रहा तो दूसरी तरफ सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांटिक व समसामयिक फिल्मों का निर्माण भी काफी हुआ। सती विषय पर बनी पहली मूक फिल्म ‘सती पार्वती’ (1920), मॉडर्न जमाने की समस्याओं पर पहली फिल्म ‘इंग्लैंड रिटर्न’ (1921), प्रथम ऐतिहासिक फिल्म ‘अशोक’(1922), प्रथम रोमानी फिल्म ’लैला मजनू’ (1922), प्रथम सामाजिक फिल्म ’ले़डी टीचर’ व ‘तारा डांसर’ (सभी 1922) ने भी इन विषयों पर बनने वाली फिल्मों के लिए नए द्वार खोले। हालाँकि घुंडिराज गोविंद फालके ने पोस्ट सिंक्रोनाइजिंग संवादों के जरिए सवाक (बोलती) फिल्में बनाने की कोशिश की, ढेर सारे प्रयोग भी किए, लेकिन नाकामयाब रहे। सवाक फिल्मों का श्रीगणेश एक ईरानी(अर्देशिर ईरानी) ने 1930-31 में प्रथम बोलती फिल्म ‘आलमआरा’ बनाकर किया। पुणे में जन्में खान बहादुर अर्देशिर एम० ईरानी अध्यापक से मिट्टी तेल इंस्पेक्टर, फिर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के बाद संगीत न फोटाग्राफी उपकरण के विक्रेता बने। छात्र-जीवन से ही फोटोग्राफी के प्रति दीवानदी ने उन्हें सिनेमा की तरफ प्रेरित किया। पहले वे हॉलीवुड की प्रख्यात निर्माण संस्था ‘युनिवर्सल पिक्चर्स’ के भारत में (मुंबई में) प्रतिनिधि बने, फिर मुंबई में ही मैजेस्टिक सिनेमाघर का निर्माण किया और एलैक्जैंडर सिनेमाघऱ में भागीदारी भी की। 1926 में उन्होंन इंपीरियल सिनेमा की स्थापना की और इस बैनर के अंतर्गत प्रथम सवाक फिल्म में गानों का भी पिक्चराइजेशन किया। 1939 में उन्होंने ज्योति स्टूडियो का निर्माण किया जहाँ 20वीं शती तक फिल्मों की शूर्टिंग होती रही।
अकीरा कुरूसोवा ने सही ही कहा था। आने वाले दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, पोलैंड में सिनेमा सचमुच न केवल मौत की कगार पर पहुँच गया, बल्कि उसकी दिन-ब-दिन घुटती साँस पर टेलीविजन पर प्रदर्शित टी० वी० धारावाहिकों एवं टेलीफिल्मों ने एक के बाद एक सलीब टाँगने भी शुरू कर दिए थे। अगर जापानी व चीनी सिनेमा में अचानक ब्रुस ली और उनके मार्शल आर्ट का पदार्पण नहीं हुआ होता तो जापानी व चीनी सिनेमा अपने ही बनाए हुए ताबूतों में कभी के दफन हो गए होते। जिस समय कुरुसोवा ने यह बात कही थी, जापान में जहाँ प्रतिवर्ष 200 से 300 फिल्में बनती थीं, उनकी संख्या घटकर 50-60 ही रह गई थी। जब हमारी अकीरा कुरूसोवा से बातचीत हुई थी, तब भारत में भी टेलीविजन धीरे-धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। किंतु तब भी नए टी० वी० चैनलों के सामने बैठकर धारावाहिकों एवं टेलीफिल्मों को देखने की बात लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। केबल एवं वीडियो पायरेसी के खतरे की बातें भी तब किसी के जेहन में नहीं थीं। तब फिल्म उद्योग सेंसर बोर्ड के कहर, संगीत की धुनों की नकल और 16 एम० एम० के प्रोजेक्टर वाले उन छोटे-छोटे तथाकथित सिनेमाघरों की मार सह रहा था जहाँ फिल्म रिलीज के पहले या रिलीज होते ही नई फिल्मों को प्रदर्शित कर दिया जाता था। ये फिल्में फिल्म लेबोरेटरीज या सिनेमाघरों के प्रोजेक्टरों द्वारा गैरकानूनी ढंग से 16 एम० एम० पर ट्रांसफर कर ली जाती थीं औऱ ये सिनेमाघर घनी बस्तियों, चालों, झोपड़पट्टियों में एक छोटे-से बंद कमरे में दीवार पर 16 एम० एम० का पर्दा या सफेद चादर अथवा दीवार पर सफेद पेंट करवाकर मिनी थियेटर के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते थे। तब फिल्म-निर्माताओं की एकमात्र संस्था ‘इम्पा’ इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हर उपाय कर रही थी, लेकिन सिनेमा तकनीक, वीडियो सी०डी० तथा टेलीविजन की क्रांतिकारी आँधी के बावजूद न तो तब भारतीय सिनेमा मरा और न ही अब जब उसके सामने समस्याओं के असंख्य पहाड़ ढेर सारे सिनेमाघर बंद कर दिए गए, राज्यों में मनोरंजन कर आसमान की ऊँचाइयाँ छूने लगा, टी०वी० धारावाहिकों व वीडियो पायरेसी के निरंतर प्रहार उस पर होते रहे, लेकिन इसके बावजूद विश्व सिनेमा में हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड (भारतीय सिनेमा) का स्थान दूसरे नंबर पर है।
ऐसा कैसे हुआ ? अकीरा कुरूसोवा की भविष्यवाणी सही कैसे साबित हुई ? इसका जवाब भी तब उन्होंने दिया था-समय और माँग के अनुराग भारतीय सिनेमा में परिवर्तन का उसका लचीला रूख और नई-नई प्रतिभाओं का उदय इसका कारण है।’ दादा साहब फालके से लेकर आज के युवा निर्देशक करण जौहर और अन्य युवा पीढ़ी के फिल्मकारों का उदय, ‘राजा हरिश्चंद’ से लेकर अब तक की प्रदर्शित सुपरहिट फिल्में, सालुंके से लेकर आमिर खान, शाहरूख खान, हतिक रोशन जैसे सितारों के उदय का 92 वर्ष का अंतराल-भारतीय सिनेमा के अमरत्व का अक्षुण्ण महाकाव्य जो है। इस दौरान फिल्मों में, उनकी निर्माण-तकनीक, अभिनय-परंपरा व नृत्य-संगीत ने हजारों-हजार करवटें जो ली हैं। 92 वर्ष पहले सन् 1912 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फालके घुंडीराज गोविंद फालके-ने अगर लाइट ऑफ क्राइस्ट’ फिल्म नहीं देखी होती और क्राइस्ट की ही तरह कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को सेल्युलाइड पर उतारने की कल्पना न पिरोई होती तो शायद भारत में सिनेमा का श्रीगणेश ही नहीं हुआ होता। यह बात अलग है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म कृष्ण-चरित्र पर बनाने के बजाय 1912 के अंत में राजा हरिश्चंद्र के चरित्र पर ’राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जिसका प्रदर्शन 1913 में हुआ था। एक पारंपारिक पुजारी-परिवार में 30 अप्रैल,1870 को त्र्यंबकेश्वर (नासिक) में जन्मे घुंडीराज गोविंद फालके को उनके पिता अपनी ही तरह संस्कृत-पंडित बनाना चाहते थे। बचपन से ही उनकी रूचि पेंटिंग, नाटक, अभिनय और जादूगरी आदि विविध कलाओं की तरफ ज्यादा थी। इसीलिए जब पिता गोविंद फालके मुंबई के प्रख्यात एलफिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होकर मुंबई आए तो उन्होंने बेटे की रूचि को ध्यान में रखकर उनका एडमिशन जे०जे० स्कूल आँफ आर्ट्रस में करा दिया, जो आज भी भारत ही नहीं, समूचे एशिया में प्रथम श्रेणी का आर्ट्रस कॉलेज माना जाता है। यहाँ उन्होंने आर्ट्रस की अन्य विधाओं के साथ-साथ फोटोग्राफी भी सीखी। इसके बाद कला भवन व गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कुछ समय रहकर फोटोग्राफी व अन्य विधाओं में महारत हासिल की। उनकी फोटोग्राफी प्रतिभा से प्रभावित हो उन्हें एक फोटोग्राफी कंपनी ने इस शर्त पर फोटोग्राफी प्रिंटिंग की विकसित तकनीक का अध्ययन करने के लिए जर्मनी भेजा कि वहाँ से वापस लौटने पर उन्हें अनुबंध के मुताबिक निर्धारित अवधि तक उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। वापस लौटने के कुछ समय बाद 1910 में उनकी एक आँख खराब हो गई और काफी इलाज के बाद ही उससें रोशनी आ सकी।
उस कंपनी की नौकरी संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद वे अपने कैरियर की योजना बना ही रहे थे कि एक दिन उन्होंने लाइट ऑफ क्राइस्ट’ फिल्म देखी और उनके दिमाग में क्राइस्ट के चरित्र की ही तरह कृष्ण के चरित्र को लेकर फिल्म बनाने की कल्पना घर कर गई, लेकिन फिल्म-निर्माण संबंधी उपकरण तब भारत मे उपलब्ध नहीं थे। इसलिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख तथा दोस्तों से उधार ले वे फिल्म-निर्माण संबंधी उपकरण खरीदने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ वे प्रख्यात फिल्म-निर्माता सेसिल हेपबर्थ से भी मिले। उनसे फिल्म-निर्माण संबंधी तमाम जानकारियाँ प्राप्त कीं और वापस लौटकर फिल्म-निर्माण की योजना पर जुट गए। इसी बीच कृष्ण-चरित्र पर फिल्म बनाने की योजना रोककर राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फाइनेंस की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जब तारामती की भूमिका निभाने के लिए कोई वेश्या भी तैयार नहीं हुई तब एक रेस्तराँ में रसोइए का काम करने वाले सालुंसे को 15 रूपए पारिश्रमिक पर तारामती बनने के लिए राजी किया। पंद्रह हजार रूपय की लागत से 1912 में निर्मित 3700 फुट लंबी राजा हरिश्चंद’ 3 मई,1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो उसके विज्ञापन में छपा था-‘राजा हरिश्चंद-75 हजार चित्रों का नजारा। सिर्फ तीन आने में दो मील लंबी फिल्म का आनंद।’ सिनेमाघर में ‘राजा हरिश्चंद्र’ देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। हिंदी भाषा में प्रस्तुत यह चलती-फिरती फिल्म लोगों के लिए अचंभा भी थी और उत्सुकता-भरी अकूत जिज्ञासाओं का समंदर भी। इस सफलता ने घुंडिराज गोविंद फालके को दूसरी फिल्में बनाने, अपनी फिल्म यूनिट तैयार करने और एक बंद व ओपन स्टूडियो के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने ‘भस्मासुर-मोहिनी’ (1913), ‘सत्यवान-सावित्री’ (1914), ‘लंका दहन’, ‘कृष्ण जन्म’ आदि फिल्मों के निर्माण के साथ अपनी एक फिल्म यूनिट भी बनाई जिसके सदस्यों की संख्या बढ़ते-बढ़ते सौ से भी अधिक हो गई। ‘राजा हरिश्चंद्र’ की वाराणसी में शूटिंग कर उन्होंने जहाँ आउटडोर शूटिंग की शुरूआत की, वहीं नासिक में एक ऐसे स्थान पर स्टूडियो बनाया जिसके चारों तरफ पहाड़, नदीं, खेत-खलिहान थे ताकि एक ही जगह वे पूरी फिल्म की शूटिंग कर सकें। सालुंसे ने ‘राजा हरिश्चंद्र’ में नारी-वेश में जहाँ तारामती की भूमिका की थी वहीं ‘लंका दहन’ में उन्होंने राम और सीता दोनों की भूमिकाएँ निभाकर दोहरी भूमिका (डबल रोल) निभाने की परंपरा की भी शुरूआत की थी। दादा साहेब फालके ‘वन मैन शो’ थे-अपनी यूनिट के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, एडिटर, मेकअप मैन के साथ-साथ अभिनेता भी थे। बचपन व किशोरावस्था में सीखी जादू की कला का प्रदर्शन उन्होंन ‘प्रोफेसर खलीफा’ में जादूगर का रोल खुद निभाकर किया था। एक तरफ वे स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर थे तो दूसरी तरफ सुपर इंपोजिशन कला के महारथी। जब फिल्म ’कृष्ण जन्म’ में भगवान् श्रीकृष्ण के रूप में कलाकार पर्दें पर आया तो दर्शकों ने खड़े होकर हाथ जो़ड़े तथा पर्दें पर पैसे भी फेंके।
हिन्दी फिल्म-निर्माण की जो शुरूआत मराठी-भाषी महाराष्ट्रीयन घुंडिराज गोविंद फालके ने 1912 में की थी, उस कड़ी में जुड़ने के लिए और भी निर्माता-निर्देशक मैदान में आ गए। उनमें धीरेन गांगुली (इंग्लैंड रिटर्नः 1913) तथा बाबूराम पेंटर (सावकरी पाशः 1925) आदि प्रमुख थे। 1913 से 1937 तक मूक फिल्मों का दौर जारी रहा और हर तरह की फिल्मों का निर्माण हुआ। एक तरफ धार्मिक फिल्मों का बोलबोला रहा तो दूसरी तरफ सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांटिक व समसामयिक फिल्मों का निर्माण भी काफी हुआ। सती विषय पर बनी पहली मूक फिल्म ‘सती पार्वती’ (1920), मॉडर्न जमाने की समस्याओं पर पहली फिल्म ‘इंग्लैंड रिटर्न’ (1921), प्रथम ऐतिहासिक फिल्म ‘अशोक’(1922), प्रथम रोमानी फिल्म ’लैला मजनू’ (1922), प्रथम सामाजिक फिल्म ’ले़डी टीचर’ व ‘तारा डांसर’ (सभी 1922) ने भी इन विषयों पर बनने वाली फिल्मों के लिए नए द्वार खोले। हालाँकि घुंडिराज गोविंद फालके ने पोस्ट सिंक्रोनाइजिंग संवादों के जरिए सवाक (बोलती) फिल्में बनाने की कोशिश की, ढेर सारे प्रयोग भी किए, लेकिन नाकामयाब रहे। सवाक फिल्मों का श्रीगणेश एक ईरानी(अर्देशिर ईरानी) ने 1930-31 में प्रथम बोलती फिल्म ‘आलमआरा’ बनाकर किया। पुणे में जन्में खान बहादुर अर्देशिर एम० ईरानी अध्यापक से मिट्टी तेल इंस्पेक्टर, फिर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के बाद संगीत न फोटाग्राफी उपकरण के विक्रेता बने। छात्र-जीवन से ही फोटोग्राफी के प्रति दीवानदी ने उन्हें सिनेमा की तरफ प्रेरित किया। पहले वे हॉलीवुड की प्रख्यात निर्माण संस्था ‘युनिवर्सल पिक्चर्स’ के भारत में (मुंबई में) प्रतिनिधि बने, फिर मुंबई में ही मैजेस्टिक सिनेमाघर का निर्माण किया और एलैक्जैंडर सिनेमाघऱ में भागीदारी भी की। 1926 में उन्होंन इंपीरियल सिनेमा की स्थापना की और इस बैनर के अंतर्गत प्रथम सवाक फिल्म में गानों का भी पिक्चराइजेशन किया। 1939 में उन्होंने ज्योति स्टूडियो का निर्माण किया जहाँ 20वीं शती तक फिल्मों की शूर्टिंग होती रही।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book