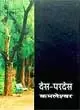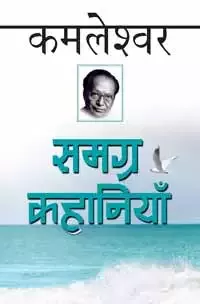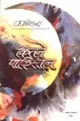|
गजलें और शायरी >> हिन्दुस्तानी गजलें हिन्दुस्तानी गजलेंकमलेश्वर
|
441 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है उर्दू-हिन्दी के शायरों की श्रेष्ठ गजलें....
Hindustani Gazalein
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दुस्तानी ग़ज़लें
ग़ज़ल के इतिहास में जाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। साहित्य की हर विधा अपनी बात और उसे कहने के ढब से, संस्कारों से फौ़रन पहचानी जाती है। ग़ज़ल की तो यह ख़ास ख़ासियत है। आप उर्दू जाने या न जानें, पर ग़ज़ल को जान भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जब 13 वीं सदी में, आज से सात सौ साल पहले हिन्दी खड़ी बोली के बाबा आदम अमीर खुसरों ने खड़ी बोली हिन्दी की ग़ज़ल लिखी :
जब यार देखा नयन भर गिल की गई चिंता उतर,
ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाय कर।
जब आँख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया,
हक्का इलाही क्या किया, आँसू चले भर लाय कर।
तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है,
तुझे दोस्ती बिसियार है इक शब मिलो तुम आय कर।
जाना तलब तेरी करूं दीगर तलब किसकी करूं,
तेरी ही चिंता दिल धरूं इक दिन मिलो तुम आय कर !
ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाय कर।
जब आँख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया,
हक्का इलाही क्या किया, आँसू चले भर लाय कर।
तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है,
तुझे दोस्ती बिसियार है इक शब मिलो तुम आय कर।
जाना तलब तेरी करूं दीगर तलब किसकी करूं,
तेरी ही चिंता दिल धरूं इक दिन मिलो तुम आय कर !
तो ग़ज़ल का इतिहास जानने की जरूरत नहीं थी। अमीर खुसरों के सात सौ साल बाद बीसवीं सदी बीतते बरसों में जब दुष्यंत ने ग़ज़ल लिखी :
कहाँ तो तय था चिराँगा हरेक घर के लिए,
कहाँ चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए।
कहाँ चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए।
तब भी इतिहास को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बात कही गई, वह सीधे लोगों के दिलों-दिमाग़ तक पहुँच गई। और जब ‘अदम’ गोंडवी कहते हैं :
ग़ज़ल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में,
मुसलसल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इरादों में।
मुसलसल फ़न का दम घुटता है इन अदबी इरादों में।
तब भी इस कथन को समझने के लिए इतिहास को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग़ज़ल एक मात्र ऐसी विधा है जो किसी ख़ास भाषा के बन्धन में बँधने से इनकार करती है। इतिहास को ग़ज़ल की जरूरत है, ग़ज़ल को इतिहास की नहीं !
अरबी-फारसी से लेकर उर्दू और हिन्दी तक इसने अब तक जो सदियों का सफ़र तय किया है वह इंसानी सफ़र की सोच है। वह चाहे दिली सोच रही हो या अपने समय की। इसीलिए ग़ज़ल कभी भी देशों या मजहबों की सरहदों में कै़द नहीं हो पाई। इसे ज़बरदस्ती रुहानी या आध्यात्मिक लिबास नहीं पहनाया जा सका। यह हमेशा इंसानी भावनाओं, उसकी सांसारिक सोच की ऊंचाइयों-गहराइयों और दु:ख-सुख का साथ देती रही। ग़ज़ल ने दिल की कुदरती ख़लिश और दर्द को तराश कर और दिमाग़ी सोच की बेचैनियों को अल्फ़ाज़ का अमली जामा पहनाकर वह तहज़ीब पैदा की जो दिलो-दिमाग़ की सरहदों पर होने वाले हमलों का मुकाबला सदियों से करती रही है और आज भी उसकी पहरेदारी कर रही है। ग़ज़ल एक साँस लेती, जीती-जागती तहज़ीब है ! इसी तहज़ीब को हिन्दी और उर्दू ने अपनाया। यह विधा या तो सौन्दर्य की इबादत करती रही या सौन्दर्य को विकृत किए जाने के खिलाफ़ जद्दों में जुटी रही। इसने हर समय हर तरह, हमेशा इन्सान के सपनों का साथ दिया। जब-जब मनुष्य के सपनों को साहित्य ने उलझाया, ग़ज़ल ने उसे सुलझाया। इसीलिए दुष्यन्त को कहना पड़ा :
‘मैं बराबर महसूस करता रहा हूँ कि कविता में आधुनिकता छद्म, कविता को बराबर पाठकों से दूर करता चला गया है। कविता और पाठकों के बीच इतना फासला कभी नहीं था, जितना आज है, इससे ज्यादा दु:खद बात यह है कि कविता धीरे-धीरे अपनी पहचान और कवि एक ही शैली और शब्दावली में एक ही कविता लिख रहे हैं। और इस कविता के बारे में कहा जाता है कि यह सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति की भूमिका तैयार कर रही है। मेरी समझ में यह दलील खादी और वक्तव्य भ्रामक है। जो कविता लोगों तक पहुँचती ही नहीं, वह भली क्रांति की संवाहक कैसे हो सकती हैं ?’
कोई सृजनात्मक लेखक-कवि साहित्य की ठहरी हुई या गलत सोच के कठघरों में कैद नहीं हो पाता। ग़ज़ल तो और भी आज़ाद है। यह तो बहुत से शायरों में नहीं आती। यह बड़ी फरार किस्म की विधा है। पकड़ में नहीं आती। आ जाती है तो ता-ज़िन्दगी साथ निभाती है और शायर से ज़्यादा अपने समय और अपने इन्सान के काम आती है। सच पूछो तो ग़ज़ल एक याद की तरह है। सदियों की इंसानी सोच और सदमों से साँस लेने वाली विधा, जो यादों की तरह बार-बार लौट आती है। यही इसकी रचनात्मकता और तहज़ीब है।
याद ! यानी स्मृति की यह परम्परा ही इन्सानी ज़िन्दगी के तमाम हादसों, सदमों और ओस जैसे आँसुओं को सँभालती है। स्मृति की परम्परा धर्म की परम्परा से ज़्यादा प्रगाढ़ है। साहित्य यह बताता है कि सीधे-सीधे तो नहीं, फिर भी धर्म के अच्छे पहलुओं को मंजूर करते हुए भी, धर्म के नाम पर वह अपनी स्मृति की परम्परा से अलग नहीं हो सकता। इसी स्मृति की परम्परा का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग हैं भूगोल। व्यक्ति का धर्म, जाति, वर्ण या वंश कोई भी हो, वह अपना जन्म-स्थान यानी अपने नितांत निजी भूगोल को कभी नहीं भूल पाता। दुनिया का कोई ऐसा लेखक शायर नहीं है जो अपनी जन्मभूमि की स्मृति को भुला सका हो। इस स्मृति का धर्म के साथ कोई नाता नहीं होता। बड़े-से-बड़े लेखक-कवि का बचपन देख जाइए, उसमें धर्म नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो अपना घर, छप्पर, पेड-पौधे, नदी-पोखर, टूटी या कच्ची धूल भरी सड़क या पगडंडी, खेल-खलिहान या अपने मोहल्ले की बस्ती, दोस्त और साथी, पशु-पक्षी, मौसम और उनकी खट्टी-मीठी यादें शायरी में तो दिल अंदरूनी भूगोल के अक़्स और नक़्श उभरने लगते हैं।
राही मासूम रज़ा के क्लैसिक उपन्यास ‘आधा गांव’ का ही एक अंश उठा लीजिए। फ़ौज में गया उसका एक पात्र जब युद्ध के मोर्चे से वापस लौटता है तो मज़हबी बहस के दौरान वह बड़ी तल्ख़ी, पर शत-प्रतिशत सच्चाई और ईमानदारी से लगभग इन शब्दों में कहता है : ‘मोर्चे पर जब मौत सामने होती है तो मुझे (आदतन) अल्लाह तो याद आता है पर सबसे ज़्य़ादा मुझे अपना गंगौली गाँव और घर याद आता है....मुझे काबा याद नहीं आता होगा....मुझे तो सिर्फ गंगौली का अपना घर याद आता है।’
सोचिए, आख़िर इन्सान की यह कौन सी बड़ी सच्चाई है जो धर्म-मज़हब की सच्चाई से भी बहुत ऊँची उठ जाती है ! और वह तब, जब मौत जैसी खूँखार सच्चाई उसके सामने खड़ी होती है। आख़िर मौत के आगे तो कुछ नहीं है, यदि धर्म या मज़हब ही अन्तिम सत्य होता तो ‘आधा गाँव’ के उस मुसलमान पात्र को ‘काबा’ याद आना चाहिए था या किसी हिन्दू पात्र को बद्री-केदार, राम जी या कृष्ण जी के मन्दिर याद आने ही चाहिए, पर ऐसा निश्चय ही होता है। अब मृतकों की गवाही तो एकत्रित नहीं की जा सकती, पर रामजन्मभूमि अभियान में जो कारसेवक अयोध्या गए थे, माना जा सकता है कि धर्म से अधिकतम जुड़े हुए लोग थे।
उन पर गोली चली थी। उन्नीस रामसेवक वहीं अयोध्या से अस्थायी मन्दिर के सामने मारे गए थे। वे तो अब नहीं है, पर उन्हीं के साथ गोलियों की आकस्मिक मौत से जो बच गए थे, उन्हें वहीं मौजूद ‘रामलला’ की याद नहीं आई थी ! नहीं तो मौत से बचने के बाद वे रामभक्त सबसे पहले ‘रामलला’ के आगे माथा नवाते या ईश्वर को याद करते हुए वे किसी तीर्थ स्थान या मन्दिर में जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे मौत से बचकर सीधे अपने घरों की ओर भागे थे। जेहादी मुस्लिम आतंकवादियों को ही ले लीजिए। वे तो धर्म के लिए धर्म के नाम पर ही बेगुनाहों या ‘गुनहगारों’ को मारते हैं। उनके संगठनों के नाम भी विशुद्ध रूप से धार्मिक हैं। जैसे जैश-ए-मुहम्मद अर्थात् पैगंबर मुहम्मद की सेना, या कि लश्करे-तय्यबा मज़हब की पवित्र फौज़ ! अब इनसे ज्यादा मज़हब में आस्था रखने वाला कौन होगा ? लेकिन जब यह मज़हबी-जेहादी मारे जाते हैं तो इनकी जेहबों से मक्का-मदीने की तस्वीरें नहीं निकलतीं, इनकी जेबों से अपने घरों, शादियों और घरवालों की तस्वीरें निकलती हैं। यह तस्वीर यादों के सिवा क्या हैं ? खूँखार से खूँखार आदमी भी अपनी यादों से मुक्त नहीं हो पाता।
मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो धर्म, वर्ण, नस्ल या जाति पूछ कर दोस्ती करता हो या जिसकी दोस्ती का दायरा सिर्फ अपने धर्मवालों तक सीमित हो। इसे आप क्या कहेंगे ? यह सच्चाई बताती है कि धर्म या मज़हब से पहले अपने आस-पास और जन्म की जगह वाली कुदरत से व्यक्ति का रिश्ता होता है। यह रिश्ता धर्म नहीं तय करता, उस दौर का अनुभव और बाद में उसकी स्मृतियाँ तय करती हैं। धर्म जब धीरे-धीरे मनुष्य के मन में जगह बनाता है, तब भी वह इन स्मृतियों को खंडित नहीं करता, धर्म और स्मृति में कोई स्पर्धा और वैमनस्य भी नहीं होता, धर्म का अपना विधि विधान होता है। स्मृति का कोई विधि-विधान या कर्मकांड नहीं होता, इसीलिए संस्कृति के निर्माण में धर्म से अधिक स्मृति का अंशदान और योगदान होता है।
संस्कृति लिखी नहीं जाती, वह स्व-निर्मित होती रहती है। संस्कृति का लिखित रूप ही साहित्य होता है। ग़ज़ल संस्कृति के इसी घराने की सदस्य और सबसे सुन्दर सौगात है ! साहित्य अपने इन्सानी अनुभव और संवेदना से सांस्कृतिक सोच और मूल्यों को उदात्त और वृहत्तर बनता रहता है। संस्कृति मनुष्य की सामाजिक चेतना है। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर धर्म नितांत व्यक्तिगत हो जाता है। एक ही धर्म के दो व्यक्तियों का धर्म एक दूसरे के काम नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति तब अपनी-अपनी स्मृतियों के बल पर सिर्फ़ अपनी मुक्ति की कामना करता है। वह एक धर्म के अनुसार एक धर्म कामना या मोक्ष की कामना नहीं करता। इसीलीए मैं स्मृति की परम्परा, जो कि सांस्कृतिक आधार भूमि है, बेहद महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। भारतीय सभ्यता को स्मृति की इसी परम्परा ने जीवित रखा है, धर्म और धर्म के स्वरूप, सिद्धान्त और उनकी व्याख्याएँ आती-जाती, स्थापित और तिरोहित होती रहीं, इनमें से जो कुछ शुभ था, उसके अंशों को हमारी यह सभ्यता और संस्कृति अंगीकर करती रही, पर सभ्यता और संस्कृति का अधिकांश स्मृति और उसकी मानवीय चिन्ताओं के यथार्थ और उसके सपनों से ही निर्मित होता रहा। कोई भी संस्कृति हो, पाश्चात्य या पौर्वात्य, उसकी धमनियों में सांस्कृतिक का रक्त ही प्रवाहित है।
एक उदाहरण दूँ ! मेरे ही नहीं, बहुतों के मित्र थे, एक तेग इलाहाबादी साहब। उनका असली नाम था मुस्तफ़ा ज़ैदी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे मुझसे एक साल आगे थे। भारत के दो अल्पकालीन प्रधानमंत्रियों वी.पी.सिंह और चन्द्रशेखर के वे सहपाठी थे। तेग इलाहाबादी उर्फ़ मुस्तफ़ा ज़ैदी की ज़िन्दगी में क्या हादसा हुआ कि विभाजन के दस साल बाद वे भारत को गालियाँ देते हुए पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्हें हाथों-हाथ लिया गया और वे पाकिस्तानी सिविल सर्विस के एक आला अफ़सर, कराची के कमिश्नर बन कर घनघोर भारत विरोधी बन गए। लेकिन कराची का यह कमिश्नर मुस्तफ़ा ज़ैदी आखिर एक शायर भी था, जिसका नाम था तेग इलाहाबादी।
अरबी-फारसी से लेकर उर्दू और हिन्दी तक इसने अब तक जो सदियों का सफ़र तय किया है वह इंसानी सफ़र की सोच है। वह चाहे दिली सोच रही हो या अपने समय की। इसीलिए ग़ज़ल कभी भी देशों या मजहबों की सरहदों में कै़द नहीं हो पाई। इसे ज़बरदस्ती रुहानी या आध्यात्मिक लिबास नहीं पहनाया जा सका। यह हमेशा इंसानी भावनाओं, उसकी सांसारिक सोच की ऊंचाइयों-गहराइयों और दु:ख-सुख का साथ देती रही। ग़ज़ल ने दिल की कुदरती ख़लिश और दर्द को तराश कर और दिमाग़ी सोच की बेचैनियों को अल्फ़ाज़ का अमली जामा पहनाकर वह तहज़ीब पैदा की जो दिलो-दिमाग़ की सरहदों पर होने वाले हमलों का मुकाबला सदियों से करती रही है और आज भी उसकी पहरेदारी कर रही है। ग़ज़ल एक साँस लेती, जीती-जागती तहज़ीब है ! इसी तहज़ीब को हिन्दी और उर्दू ने अपनाया। यह विधा या तो सौन्दर्य की इबादत करती रही या सौन्दर्य को विकृत किए जाने के खिलाफ़ जद्दों में जुटी रही। इसने हर समय हर तरह, हमेशा इन्सान के सपनों का साथ दिया। जब-जब मनुष्य के सपनों को साहित्य ने उलझाया, ग़ज़ल ने उसे सुलझाया। इसीलिए दुष्यन्त को कहना पड़ा :
‘मैं बराबर महसूस करता रहा हूँ कि कविता में आधुनिकता छद्म, कविता को बराबर पाठकों से दूर करता चला गया है। कविता और पाठकों के बीच इतना फासला कभी नहीं था, जितना आज है, इससे ज्यादा दु:खद बात यह है कि कविता धीरे-धीरे अपनी पहचान और कवि एक ही शैली और शब्दावली में एक ही कविता लिख रहे हैं। और इस कविता के बारे में कहा जाता है कि यह सामाजिक और राजनीतिक क्रान्ति की भूमिका तैयार कर रही है। मेरी समझ में यह दलील खादी और वक्तव्य भ्रामक है। जो कविता लोगों तक पहुँचती ही नहीं, वह भली क्रांति की संवाहक कैसे हो सकती हैं ?’
कोई सृजनात्मक लेखक-कवि साहित्य की ठहरी हुई या गलत सोच के कठघरों में कैद नहीं हो पाता। ग़ज़ल तो और भी आज़ाद है। यह तो बहुत से शायरों में नहीं आती। यह बड़ी फरार किस्म की विधा है। पकड़ में नहीं आती। आ जाती है तो ता-ज़िन्दगी साथ निभाती है और शायर से ज़्यादा अपने समय और अपने इन्सान के काम आती है। सच पूछो तो ग़ज़ल एक याद की तरह है। सदियों की इंसानी सोच और सदमों से साँस लेने वाली विधा, जो यादों की तरह बार-बार लौट आती है। यही इसकी रचनात्मकता और तहज़ीब है।
याद ! यानी स्मृति की यह परम्परा ही इन्सानी ज़िन्दगी के तमाम हादसों, सदमों और ओस जैसे आँसुओं को सँभालती है। स्मृति की परम्परा धर्म की परम्परा से ज़्यादा प्रगाढ़ है। साहित्य यह बताता है कि सीधे-सीधे तो नहीं, फिर भी धर्म के अच्छे पहलुओं को मंजूर करते हुए भी, धर्म के नाम पर वह अपनी स्मृति की परम्परा से अलग नहीं हो सकता। इसी स्मृति की परम्परा का एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग हैं भूगोल। व्यक्ति का धर्म, जाति, वर्ण या वंश कोई भी हो, वह अपना जन्म-स्थान यानी अपने नितांत निजी भूगोल को कभी नहीं भूल पाता। दुनिया का कोई ऐसा लेखक शायर नहीं है जो अपनी जन्मभूमि की स्मृति को भुला सका हो। इस स्मृति का धर्म के साथ कोई नाता नहीं होता। बड़े-से-बड़े लेखक-कवि का बचपन देख जाइए, उसमें धर्म नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो अपना घर, छप्पर, पेड-पौधे, नदी-पोखर, टूटी या कच्ची धूल भरी सड़क या पगडंडी, खेल-खलिहान या अपने मोहल्ले की बस्ती, दोस्त और साथी, पशु-पक्षी, मौसम और उनकी खट्टी-मीठी यादें शायरी में तो दिल अंदरूनी भूगोल के अक़्स और नक़्श उभरने लगते हैं।
राही मासूम रज़ा के क्लैसिक उपन्यास ‘आधा गांव’ का ही एक अंश उठा लीजिए। फ़ौज में गया उसका एक पात्र जब युद्ध के मोर्चे से वापस लौटता है तो मज़हबी बहस के दौरान वह बड़ी तल्ख़ी, पर शत-प्रतिशत सच्चाई और ईमानदारी से लगभग इन शब्दों में कहता है : ‘मोर्चे पर जब मौत सामने होती है तो मुझे (आदतन) अल्लाह तो याद आता है पर सबसे ज़्य़ादा मुझे अपना गंगौली गाँव और घर याद आता है....मुझे काबा याद नहीं आता होगा....मुझे तो सिर्फ गंगौली का अपना घर याद आता है।’
सोचिए, आख़िर इन्सान की यह कौन सी बड़ी सच्चाई है जो धर्म-मज़हब की सच्चाई से भी बहुत ऊँची उठ जाती है ! और वह तब, जब मौत जैसी खूँखार सच्चाई उसके सामने खड़ी होती है। आख़िर मौत के आगे तो कुछ नहीं है, यदि धर्म या मज़हब ही अन्तिम सत्य होता तो ‘आधा गाँव’ के उस मुसलमान पात्र को ‘काबा’ याद आना चाहिए था या किसी हिन्दू पात्र को बद्री-केदार, राम जी या कृष्ण जी के मन्दिर याद आने ही चाहिए, पर ऐसा निश्चय ही होता है। अब मृतकों की गवाही तो एकत्रित नहीं की जा सकती, पर रामजन्मभूमि अभियान में जो कारसेवक अयोध्या गए थे, माना जा सकता है कि धर्म से अधिकतम जुड़े हुए लोग थे।
उन पर गोली चली थी। उन्नीस रामसेवक वहीं अयोध्या से अस्थायी मन्दिर के सामने मारे गए थे। वे तो अब नहीं है, पर उन्हीं के साथ गोलियों की आकस्मिक मौत से जो बच गए थे, उन्हें वहीं मौजूद ‘रामलला’ की याद नहीं आई थी ! नहीं तो मौत से बचने के बाद वे रामभक्त सबसे पहले ‘रामलला’ के आगे माथा नवाते या ईश्वर को याद करते हुए वे किसी तीर्थ स्थान या मन्दिर में जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे मौत से बचकर सीधे अपने घरों की ओर भागे थे। जेहादी मुस्लिम आतंकवादियों को ही ले लीजिए। वे तो धर्म के लिए धर्म के नाम पर ही बेगुनाहों या ‘गुनहगारों’ को मारते हैं। उनके संगठनों के नाम भी विशुद्ध रूप से धार्मिक हैं। जैसे जैश-ए-मुहम्मद अर्थात् पैगंबर मुहम्मद की सेना, या कि लश्करे-तय्यबा मज़हब की पवित्र फौज़ ! अब इनसे ज्यादा मज़हब में आस्था रखने वाला कौन होगा ? लेकिन जब यह मज़हबी-जेहादी मारे जाते हैं तो इनकी जेहबों से मक्का-मदीने की तस्वीरें नहीं निकलतीं, इनकी जेबों से अपने घरों, शादियों और घरवालों की तस्वीरें निकलती हैं। यह तस्वीर यादों के सिवा क्या हैं ? खूँखार से खूँखार आदमी भी अपनी यादों से मुक्त नहीं हो पाता।
मैंने आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो धर्म, वर्ण, नस्ल या जाति पूछ कर दोस्ती करता हो या जिसकी दोस्ती का दायरा सिर्फ अपने धर्मवालों तक सीमित हो। इसे आप क्या कहेंगे ? यह सच्चाई बताती है कि धर्म या मज़हब से पहले अपने आस-पास और जन्म की जगह वाली कुदरत से व्यक्ति का रिश्ता होता है। यह रिश्ता धर्म नहीं तय करता, उस दौर का अनुभव और बाद में उसकी स्मृतियाँ तय करती हैं। धर्म जब धीरे-धीरे मनुष्य के मन में जगह बनाता है, तब भी वह इन स्मृतियों को खंडित नहीं करता, धर्म और स्मृति में कोई स्पर्धा और वैमनस्य भी नहीं होता, धर्म का अपना विधि विधान होता है। स्मृति का कोई विधि-विधान या कर्मकांड नहीं होता, इसीलिए संस्कृति के निर्माण में धर्म से अधिक स्मृति का अंशदान और योगदान होता है।
संस्कृति लिखी नहीं जाती, वह स्व-निर्मित होती रहती है। संस्कृति का लिखित रूप ही साहित्य होता है। ग़ज़ल संस्कृति के इसी घराने की सदस्य और सबसे सुन्दर सौगात है ! साहित्य अपने इन्सानी अनुभव और संवेदना से सांस्कृतिक सोच और मूल्यों को उदात्त और वृहत्तर बनता रहता है। संस्कृति मनुष्य की सामाजिक चेतना है। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर धर्म नितांत व्यक्तिगत हो जाता है। एक ही धर्म के दो व्यक्तियों का धर्म एक दूसरे के काम नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति तब अपनी-अपनी स्मृतियों के बल पर सिर्फ़ अपनी मुक्ति की कामना करता है। वह एक धर्म के अनुसार एक धर्म कामना या मोक्ष की कामना नहीं करता। इसीलीए मैं स्मृति की परम्परा, जो कि सांस्कृतिक आधार भूमि है, बेहद महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। भारतीय सभ्यता को स्मृति की इसी परम्परा ने जीवित रखा है, धर्म और धर्म के स्वरूप, सिद्धान्त और उनकी व्याख्याएँ आती-जाती, स्थापित और तिरोहित होती रहीं, इनमें से जो कुछ शुभ था, उसके अंशों को हमारी यह सभ्यता और संस्कृति अंगीकर करती रही, पर सभ्यता और संस्कृति का अधिकांश स्मृति और उसकी मानवीय चिन्ताओं के यथार्थ और उसके सपनों से ही निर्मित होता रहा। कोई भी संस्कृति हो, पाश्चात्य या पौर्वात्य, उसकी धमनियों में सांस्कृतिक का रक्त ही प्रवाहित है।
एक उदाहरण दूँ ! मेरे ही नहीं, बहुतों के मित्र थे, एक तेग इलाहाबादी साहब। उनका असली नाम था मुस्तफ़ा ज़ैदी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वे मुझसे एक साल आगे थे। भारत के दो अल्पकालीन प्रधानमंत्रियों वी.पी.सिंह और चन्द्रशेखर के वे सहपाठी थे। तेग इलाहाबादी उर्फ़ मुस्तफ़ा ज़ैदी की ज़िन्दगी में क्या हादसा हुआ कि विभाजन के दस साल बाद वे भारत को गालियाँ देते हुए पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्हें हाथों-हाथ लिया गया और वे पाकिस्तानी सिविल सर्विस के एक आला अफ़सर, कराची के कमिश्नर बन कर घनघोर भारत विरोधी बन गए। लेकिन कराची का यह कमिश्नर मुस्तफ़ा ज़ैदी आखिर एक शायर भी था, जिसका नाम था तेग इलाहाबादी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book