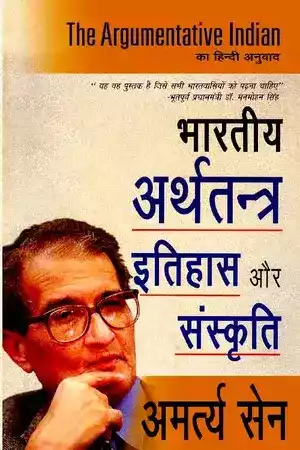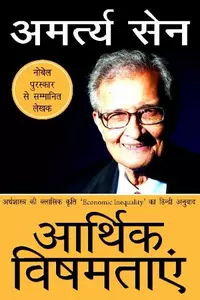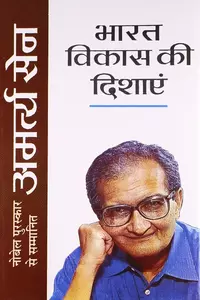|
अर्थशास्त्र >> भारतीय अर्थतन्त्र इतिहास और संस्कृति भारतीय अर्थतन्त्र इतिहास और संस्कृतिअमर्त्य सेन
|
91 पाठक हैं |
|||||||
"भारतीय वाद-संवाद की परंपरा : इतिहास, संस्कृति और सामाजिक न्याय का नया दृष्टिकोण"
Bhartiya Arthashastra Itihas Aur Sanskriti a hindi book by Amartya sen - भारतीय अर्थतन्त्र इतिहास और संस्कृति - अमर्त्य सेन
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री, भारतरत्न अमर्त्य सेन की नवीनतम महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए पाठनीय।
प्राक्कथन
ये लेख पिछले दशक में लिखे गए थे—आधे तो पिछले एक ही दो वर्षों में लिखे गए हैं। पहले चार लेख जो इस संकलन का प्रथम भाग भी हैं इस पुस्तक की मुख्य धारा का परिचय दे रहे हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध भारत की सुदीर्घ वाद-संवाद परंपरा से है।
भारत एक बहुत ही विविधता सम्पन्न देश है, इसमें अनेक अध्यावसायों का अनुसरण होता है, बहुत ही अलग-अलग मान्यताएँ है, लोगों के रिवाज और दृष्टिकोणों का तो बहुत ही रंग-बिरंगा चित्र यहाँ सजा है। देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और समकालीन राजनीति के विषय में चर्चा करते हुए किसी भी व्यक्ति को अपने विषयों का चयन तो करना ही पड़ेगा। सभी आयाम-पक्षों पर विचार कर पाना इतना सहज नहीं होगा। अतः यह बताने की अवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भारत की वाद-संवाद परम्परा पर ध्यान केन्द्रण इसी चयन प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि भारत के इतिहास, संस्कृति या राजनीति पर विचार का यही सर्वोपयुक्त साधन है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि और अनेक तरीकों से यह व्याख्या हो सकती है। मेरा यह केन्द्रण चयन तीन कारणों से प्रभावित रहा है— भारत के वाद-संवाद की परम्परा का लम्बा इतिहास, इसकी समकालीन प्रासंगिकता और इस समय संस्कृति विषयक परिचर्चाओं में इसकी सापेक्ष अनदेखी। यह भी कहा जा सकता है कि भारत में इतने अधिक विचार दृष्टिकोण केवल इसी कारण फल-फूल पाए हैं कि यहाँ वैचारिक विविधता और वाद-संवाद को प्रायः सर्व सहमति प्राप्त रही है। भारत की इस विविधता का प्रसार और गहनता अपने आप में बहुत विलक्षण है।
आज के भारत को समझने के लिए अतीत में झाँकने की बात आज एक उत्तेजक राजनीतिक रूप धारण कर गई है। अतीत के प्रति यह उत्साह आज की हिन्दुत्वादी राजनीति अधिक दिखा रही है, ये भारतीय सभ्यता को संकीर्ण दृष्टियों से देखते हुए उसे मुसलिम पूर्व एवं पश्चात की दो अवधियों में विभाजित करने के अभ्यस्त हो चले हैं। पहली अवधि ईसापूर्व तीसरी सहस्राब्दी से लेकर द्वितीय ईसवी सहस्राब्दी के आरम्भ तक चली है। किन्तु भारतीय संस्कृति को एकात्मकतावादी दृष्टिकोण से देखनेवालों को यह प्राचीन युग पर आग्रह बड़ा संदेह भरा दिखता है। ये हिन्दुत्ववादी भारत की वास्तविक धरोहर द्वितीय सहस्राब्दी (ई.पू.) में रचे गए ‘पवित्र ग्रन्थ’ वेदों को मानते हैं। ये हिन्दू विचारों की कसौटी के रूप में महाकाव्य रामायण को भी उद्धृत करते हैं—और उसके आधार पर किसी पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करना उचित ठहराते हैं कि राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। किन्तु एकात्मकतावादियों को वर्तमान धर्मनिरपेक्ष जीवन में वेदों और रामायण का यह अतिक्रमण रास नहीं आता।
एकात्मावादियों को भारत के लम्बे इतिहास में से केवल कुछ एक हिन्दू शास्त्रों के चयन में पक्षपात की गन्ध आती है। आज के भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुधर्मी जीवन में इस प्रकार के पक्षपाती रवैय्ये के हानिकारक प्रभावों की ओर सभी ये एकात्मकतावादी संकेत कर रहे हैं। भले ही भारत की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या हिन्दू हो पर, यहाँ मुस्लिम संख्या भी विश्व में तीसरे क्रम पर और ब्रिटेन तथा फ्रांस की सारी जनसंख्याओं के योगफल से भी अधिक है। फिर ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, आदि धर्मों के अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं।
एकात्मकता तथा बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी हम इस बात से इन्कार नहीं कर पाएँगे कि इन पुरातन ग्रन्थों और कथानकों का भारत ही साहित्यिक तथा विचार परम्पराओं पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इन्होंने एक ओर साहित्यक और दार्शनिक रचनाओं को प्रभावित किया है तो दूसरी ओर कथा वाचन की लोकशैलियों और आलोचनात्मक द्वन्द्वात्मकता पर भी इनके प्रभाव रहे हैं। बंगाल के मुस्लिम पठान शासकों ने ग्रन्थों के अच्छे बंगाली अनुवाद भी कराए थे। उनका प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के प्रति लगाव संस्कृति प्रेम था, हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने की इच्छा नहीं। भारतीय संस्कृति में उनके महत्त्व को नकारने का संकीर्ण धर्मनिरपेक्षतावादी आधार भी हिन्दू धार्मिकता के संकीर्ण चश्मों से कम घातक नहीं होगा।
वेदों में मन्त्र और धार्मिक कृत्य तो हैं, पर कथाएं भी हैं, विश्व की रचना के बारे में अनुमान भी हैं और पूर्व चर्चित वाद संवाद परम्परा के अनुसार कुछ मुश्किल प्रश्न भी उठाए गए हैं। एक मौलिक शंका तो विश्व के निर्माण को लेकर ही उठाई गई है— क्या किसी ने इसे रचा था— या यह स्वमेव ही अनायास पैदा हो गया ? क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो ये जानता हो कि क्या हुआ था ? ऋग्वेद तो इन शंकाओं के बारे में बड़े प्रश्न उठाता है— इस बात को कौन जानता है ? कौन इसकी उद्घोषणा करेगा ? ये कब रचा गया था ? इसकी रचना कैसे हुई थी ?... सम्भवतः यह स्वमेव ही बन गया हो...या नहीं भी...जो ऊँचे स्वर्ग में बैठा सब कुछ देख रहा है वही जानता होगा...सम्भवतः उसे भी नहीं पता हो। भारत की वादी संवादी इतिहास की परंपरा की व्याख्या में ये चार हजार वर्ष पुराने प्रश्न बार-बार उठेंगे, इनके साथ ही मीमांसा व नीतिशास्त्र के अनेक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी विचार गहन धार्मिक आस्था, अति सम्मानपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ-साथ वेदों में समाए रहे हैं।
भले ही अन्य धर्म स्थानों का विध्वंस करने को उत्साहित हिन्दू राजनीतिवादी राम को ईश्वर को अवतार मान रहे हों पर प्रायः सारे रामायण महाकाव्य में तो राम को कथा का नायक ही माना गया है— ऐसा नायक जिसमें अनेक सद्गुण हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी हैं। उसे अपनी ही पत्नी पर सन्देह बना रहता है। रामायण में जाबालि नामक ब्राह्मण को काफी स्थानों पर सम्मान मिला है। वह भी राम को भगवान नहीं मानता और उनके कुछ कामों को किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कृत्य कह डालता है। अन्ततः जाबालि को अपना आरोप वापस लेने को सहमत कर लिया जाता है पर रामायणकार उसे अपने विचारों की विस्तार से व्याख्या का भी पूरा अवसर देते हैं। जाबालि का कहना था— कोई उहलोक नहीं है, उसे पाने का कोई धार्मिक विधान भी नहीं है, शास्त्रों में देव पूजन, बलि, कर्म, दान, व्रतअनुष्ठान आदि की बातें तो कुछ चतुर व्यक्तियों द्वारा अन्यों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए भर दी हैं। रामायण का किसी संकीर्ण धार्मिक संदेश के प्रचार के लिए प्रयोग तो इसके किन्हीं विशेष अंशों को अपनाने और शेष को छिपा जाने के चातुर्य से ही सम्भव हो पा रहा है। अन्यथा, रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में यह तो एक अद्भुत कथानक है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का बहुत ही रोचक अंश है।
भारत में संशयवादी परम्परा भी बहुत पुरानी है और इसका परित्याग कर भारत की संस्कृति के इतिहास को समझ पाना सम्भव नहीं रहेगा। भले ही युद्धों संघर्षों में व्यपाक हिंसा भी होती रही है पर भारत के समूचे इतिहास में द्वन्द्ववादी परम्परा की गहरी पैठ सदा बनी रही है। भारत में तो शस्त्र संग्रामों के साथ-साथ ही शास्त्रीय संग्राम भी चलते रहे हैं। केवल शस्त्र संग्राम पर ही ध्यान देने से तो ऐसा बहुत कुछ लुप्त हो जाएगा जिसका हमारे समाज और संस्कृति की रचनाओं में बहुत महत्त्व रहा है।
भारत की वैचारिक विविधता की सर्वस्वीकृति परम्परा को अवश्य समझा जाना चाहिए। हिन्दुत्ववादी सारे ही प्राचीन भारत पर अपना एकछत्र अधिकार स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं और इसे ही ‘भारतीय संस्कृति के पलने’ का नाम दे रहे हैं। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि भारत में अनेक संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। यह बताना भी जरूरी ही कि प्रारम्भ से ही व्यापक वैचारिक अन्तर भी यहाँ विद्यामान रहे हैं। जिसे अब हिन्दू धार्मिकता का नाम दिया जा रहा है उसी के साथ बौद्ध, जैन, अनास्था और अनैश्वरवादी मत भी यहाँ फलते-फूलते रहे हैं।
यही नहीं एक हजार साल पहले तक तो यहाँ बौद्धमत ही सबसे प्रबल रहा है। प्रथम सहस्राब्दी के चीनी तो भारत को ‘बौद्धराज्य’ ही कहते थे। प्राचीन भारत को ऐसे किसी तंग डिब्बे में बन्द नहीं किया जा सकता है जिसमें रखने का प्रयास संकीर्ण हिन्दुत्ववादी कर रहे हैं।
भारत के बौद्ध सम्राट अशोक ने ई. पू. तीसरी शती में सहिष्णुता और समृद्ध वैचारिक बहुलता की आवश्यकता पर बल दिया था और विश्व की सबसे पुरानी संवाद द्वारा विवाद निपटाने की आचार संहिता की भी रचना की थी। उसके अनुसार विरोधी का भी सदैव पूर्ण सम्मान होना चाहिए। यही राजनीतिक सिद्धान्त बाद में भारत में हुई चर्चाओं में बार-बार दिखाई दिया है। पर सहिष्णुता और सभी धर्मों से राजनीति का समान अन्तर बनाए रखने की बात को सबसे स्पष्ट रूप से भारत के मुगल सम्राट अकबर ने ही उठाया था। 1990 में जहाँ भारत में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्त रचे जा रहे थे वहीं यूरोप तो उन दिनों धर्म-अभियोग चला ‘अपराधियों’ को जिन्दा जलाने के जुनून का शिकार था।
आज के युग में उस वाद संवाद तथा बाहुलता की स्वीकारोक्ति की परम्परा का बहुत ही महत्त्व है। लोकतन्त्र और जनसंवाद में चर्चा और तर्कों का निर्णायक महत्त्व होता है। ये धर्म निरपेक्षता तथा सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति सम्यक व्यवहार का आधार हैं। इन संरचनात्मक वरीयताओं से आगे निकलकर यह बाहुलतावादी परम्परा, यदि ठीक से उसका उपयोग हो तो, सामाजिक विषमताओं के विरोध, तथा गरीबी और अभावों के निर्मूलन में भी सहायक हो सकती है। सामाजिक न्याय के लिए प्रयास में आवाज उठाने का अपना निर्णायक महत्व होता है !
कई बार कहा जाता है कि द्वन्द्वात्मकता का प्रयोग तो केवल अमीरों और अधिक शिक्षितों तक सीमित रहता है और सामान्य जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। इस विचार में भरा कुलीनतावाद न केवल विचित्र है वरन् ये जिस प्रकार की राजनीतिक निष्क्रियता को बढ़ाता है उस दृष्टि से तो बहुत ही धिक्कार योग्य भी होता है। आलोचनात्मक स्वर कभी से दुखी का सहारा रहे हैं तथा वाद-संवाद में भागीदारी एक सामान्य अवसर है और इसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती।
भारत एक बहुत ही विविधता सम्पन्न देश है, इसमें अनेक अध्यावसायों का अनुसरण होता है, बहुत ही अलग-अलग मान्यताएँ है, लोगों के रिवाज और दृष्टिकोणों का तो बहुत ही रंग-बिरंगा चित्र यहाँ सजा है। देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और समकालीन राजनीति के विषय में चर्चा करते हुए किसी भी व्यक्ति को अपने विषयों का चयन तो करना ही पड़ेगा। सभी आयाम-पक्षों पर विचार कर पाना इतना सहज नहीं होगा। अतः यह बताने की अवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि भारत की वाद-संवाद परम्परा पर ध्यान केन्द्रण इसी चयन प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि भारत के इतिहास, संस्कृति या राजनीति पर विचार का यही सर्वोपयुक्त साधन है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि और अनेक तरीकों से यह व्याख्या हो सकती है। मेरा यह केन्द्रण चयन तीन कारणों से प्रभावित रहा है— भारत के वाद-संवाद की परम्परा का लम्बा इतिहास, इसकी समकालीन प्रासंगिकता और इस समय संस्कृति विषयक परिचर्चाओं में इसकी सापेक्ष अनदेखी। यह भी कहा जा सकता है कि भारत में इतने अधिक विचार दृष्टिकोण केवल इसी कारण फल-फूल पाए हैं कि यहाँ वैचारिक विविधता और वाद-संवाद को प्रायः सर्व सहमति प्राप्त रही है। भारत की इस विविधता का प्रसार और गहनता अपने आप में बहुत विलक्षण है।
आज के भारत को समझने के लिए अतीत में झाँकने की बात आज एक उत्तेजक राजनीतिक रूप धारण कर गई है। अतीत के प्रति यह उत्साह आज की हिन्दुत्वादी राजनीति अधिक दिखा रही है, ये भारतीय सभ्यता को संकीर्ण दृष्टियों से देखते हुए उसे मुसलिम पूर्व एवं पश्चात की दो अवधियों में विभाजित करने के अभ्यस्त हो चले हैं। पहली अवधि ईसापूर्व तीसरी सहस्राब्दी से लेकर द्वितीय ईसवी सहस्राब्दी के आरम्भ तक चली है। किन्तु भारतीय संस्कृति को एकात्मकतावादी दृष्टिकोण से देखनेवालों को यह प्राचीन युग पर आग्रह बड़ा संदेह भरा दिखता है। ये हिन्दुत्ववादी भारत की वास्तविक धरोहर द्वितीय सहस्राब्दी (ई.पू.) में रचे गए ‘पवित्र ग्रन्थ’ वेदों को मानते हैं। ये हिन्दू विचारों की कसौटी के रूप में महाकाव्य रामायण को भी उद्धृत करते हैं—और उसके आधार पर किसी पुरानी मस्जिद को ध्वस्त करना उचित ठहराते हैं कि राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। किन्तु एकात्मकतावादियों को वर्तमान धर्मनिरपेक्ष जीवन में वेदों और रामायण का यह अतिक्रमण रास नहीं आता।
एकात्मावादियों को भारत के लम्बे इतिहास में से केवल कुछ एक हिन्दू शास्त्रों के चयन में पक्षपात की गन्ध आती है। आज के भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुधर्मी जीवन में इस प्रकार के पक्षपाती रवैय्ये के हानिकारक प्रभावों की ओर सभी ये एकात्मकतावादी संकेत कर रहे हैं। भले ही भारत की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या हिन्दू हो पर, यहाँ मुस्लिम संख्या भी विश्व में तीसरे क्रम पर और ब्रिटेन तथा फ्रांस की सारी जनसंख्याओं के योगफल से भी अधिक है। फिर ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, आदि धर्मों के अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं।
एकात्मकता तथा बहुसांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी हम इस बात से इन्कार नहीं कर पाएँगे कि इन पुरातन ग्रन्थों और कथानकों का भारत ही साहित्यिक तथा विचार परम्पराओं पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इन्होंने एक ओर साहित्यक और दार्शनिक रचनाओं को प्रभावित किया है तो दूसरी ओर कथा वाचन की लोकशैलियों और आलोचनात्मक द्वन्द्वात्मकता पर भी इनके प्रभाव रहे हैं। बंगाल के मुस्लिम पठान शासकों ने ग्रन्थों के अच्छे बंगाली अनुवाद भी कराए थे। उनका प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के प्रति लगाव संस्कृति प्रेम था, हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने की इच्छा नहीं। भारतीय संस्कृति में उनके महत्त्व को नकारने का संकीर्ण धर्मनिरपेक्षतावादी आधार भी हिन्दू धार्मिकता के संकीर्ण चश्मों से कम घातक नहीं होगा।
वेदों में मन्त्र और धार्मिक कृत्य तो हैं, पर कथाएं भी हैं, विश्व की रचना के बारे में अनुमान भी हैं और पूर्व चर्चित वाद संवाद परम्परा के अनुसार कुछ मुश्किल प्रश्न भी उठाए गए हैं। एक मौलिक शंका तो विश्व के निर्माण को लेकर ही उठाई गई है— क्या किसी ने इसे रचा था— या यह स्वमेव ही अनायास पैदा हो गया ? क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो ये जानता हो कि क्या हुआ था ? ऋग्वेद तो इन शंकाओं के बारे में बड़े प्रश्न उठाता है— इस बात को कौन जानता है ? कौन इसकी उद्घोषणा करेगा ? ये कब रचा गया था ? इसकी रचना कैसे हुई थी ?... सम्भवतः यह स्वमेव ही बन गया हो...या नहीं भी...जो ऊँचे स्वर्ग में बैठा सब कुछ देख रहा है वही जानता होगा...सम्भवतः उसे भी नहीं पता हो। भारत की वादी संवादी इतिहास की परंपरा की व्याख्या में ये चार हजार वर्ष पुराने प्रश्न बार-बार उठेंगे, इनके साथ ही मीमांसा व नीतिशास्त्र के अनेक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी विचार गहन धार्मिक आस्था, अति सम्मानपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ-साथ वेदों में समाए रहे हैं।
भले ही अन्य धर्म स्थानों का विध्वंस करने को उत्साहित हिन्दू राजनीतिवादी राम को ईश्वर को अवतार मान रहे हों पर प्रायः सारे रामायण महाकाव्य में तो राम को कथा का नायक ही माना गया है— ऐसा नायक जिसमें अनेक सद्गुण हैं तो कुछ कमजोरियाँ भी हैं। उसे अपनी ही पत्नी पर सन्देह बना रहता है। रामायण में जाबालि नामक ब्राह्मण को काफी स्थानों पर सम्मान मिला है। वह भी राम को भगवान नहीं मानता और उनके कुछ कामों को किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कृत्य कह डालता है। अन्ततः जाबालि को अपना आरोप वापस लेने को सहमत कर लिया जाता है पर रामायणकार उसे अपने विचारों की विस्तार से व्याख्या का भी पूरा अवसर देते हैं। जाबालि का कहना था— कोई उहलोक नहीं है, उसे पाने का कोई धार्मिक विधान भी नहीं है, शास्त्रों में देव पूजन, बलि, कर्म, दान, व्रतअनुष्ठान आदि की बातें तो कुछ चतुर व्यक्तियों द्वारा अन्यों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए भर दी हैं। रामायण का किसी संकीर्ण धार्मिक संदेश के प्रचार के लिए प्रयोग तो इसके किन्हीं विशेष अंशों को अपनाने और शेष को छिपा जाने के चातुर्य से ही सम्भव हो पा रहा है। अन्यथा, रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में यह तो एक अद्भुत कथानक है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का बहुत ही रोचक अंश है।
भारत में संशयवादी परम्परा भी बहुत पुरानी है और इसका परित्याग कर भारत की संस्कृति के इतिहास को समझ पाना सम्भव नहीं रहेगा। भले ही युद्धों संघर्षों में व्यपाक हिंसा भी होती रही है पर भारत के समूचे इतिहास में द्वन्द्ववादी परम्परा की गहरी पैठ सदा बनी रही है। भारत में तो शस्त्र संग्रामों के साथ-साथ ही शास्त्रीय संग्राम भी चलते रहे हैं। केवल शस्त्र संग्राम पर ही ध्यान देने से तो ऐसा बहुत कुछ लुप्त हो जाएगा जिसका हमारे समाज और संस्कृति की रचनाओं में बहुत महत्त्व रहा है।
भारत की वैचारिक विविधता की सर्वस्वीकृति परम्परा को अवश्य समझा जाना चाहिए। हिन्दुत्ववादी सारे ही प्राचीन भारत पर अपना एकछत्र अधिकार स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं और इसे ही ‘भारतीय संस्कृति के पलने’ का नाम दे रहे हैं। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि भारत में अनेक संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। यह बताना भी जरूरी ही कि प्रारम्भ से ही व्यापक वैचारिक अन्तर भी यहाँ विद्यामान रहे हैं। जिसे अब हिन्दू धार्मिकता का नाम दिया जा रहा है उसी के साथ बौद्ध, जैन, अनास्था और अनैश्वरवादी मत भी यहाँ फलते-फूलते रहे हैं।
यही नहीं एक हजार साल पहले तक तो यहाँ बौद्धमत ही सबसे प्रबल रहा है। प्रथम सहस्राब्दी के चीनी तो भारत को ‘बौद्धराज्य’ ही कहते थे। प्राचीन भारत को ऐसे किसी तंग डिब्बे में बन्द नहीं किया जा सकता है जिसमें रखने का प्रयास संकीर्ण हिन्दुत्ववादी कर रहे हैं।
भारत के बौद्ध सम्राट अशोक ने ई. पू. तीसरी शती में सहिष्णुता और समृद्ध वैचारिक बहुलता की आवश्यकता पर बल दिया था और विश्व की सबसे पुरानी संवाद द्वारा विवाद निपटाने की आचार संहिता की भी रचना की थी। उसके अनुसार विरोधी का भी सदैव पूर्ण सम्मान होना चाहिए। यही राजनीतिक सिद्धान्त बाद में भारत में हुई चर्चाओं में बार-बार दिखाई दिया है। पर सहिष्णुता और सभी धर्मों से राजनीति का समान अन्तर बनाए रखने की बात को सबसे स्पष्ट रूप से भारत के मुगल सम्राट अकबर ने ही उठाया था। 1990 में जहाँ भारत में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्त रचे जा रहे थे वहीं यूरोप तो उन दिनों धर्म-अभियोग चला ‘अपराधियों’ को जिन्दा जलाने के जुनून का शिकार था।
आज के युग में उस वाद संवाद तथा बाहुलता की स्वीकारोक्ति की परम्परा का बहुत ही महत्त्व है। लोकतन्त्र और जनसंवाद में चर्चा और तर्कों का निर्णायक महत्त्व होता है। ये धर्म निरपेक्षता तथा सभी धर्मों के अनुयायियों के प्रति सम्यक व्यवहार का आधार हैं। इन संरचनात्मक वरीयताओं से आगे निकलकर यह बाहुलतावादी परम्परा, यदि ठीक से उसका उपयोग हो तो, सामाजिक विषमताओं के विरोध, तथा गरीबी और अभावों के निर्मूलन में भी सहायक हो सकती है। सामाजिक न्याय के लिए प्रयास में आवाज उठाने का अपना निर्णायक महत्व होता है !
कई बार कहा जाता है कि द्वन्द्वात्मकता का प्रयोग तो केवल अमीरों और अधिक शिक्षितों तक सीमित रहता है और सामान्य जनता के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। इस विचार में भरा कुलीनतावाद न केवल विचित्र है वरन् ये जिस प्रकार की राजनीतिक निष्क्रियता को बढ़ाता है उस दृष्टि से तो बहुत ही धिक्कार योग्य भी होता है। आलोचनात्मक स्वर कभी से दुखी का सहारा रहे हैं तथा वाद-संवाद में भागीदारी एक सामान्य अवसर है और इसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book