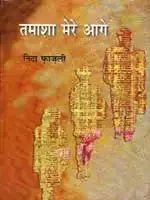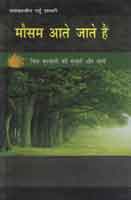|
गजलें और शायरी >> तमाशा मेरे आगे तमाशा मेरे आगेनिदा फाजली
|
33 पाठक हैं |
||||||
निदा फॉज़ली की रचना तमाशा मेरे आगे...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मुम्बई में पेडर रोड में सोफिया कालेज के पास एक बिल्डिंग है, नाम है
पुष्प विला, इस की तीसरी फ्लोर पर कई कमरों का एक फ्लेट है। इस फ्लेट में
एक कमरा पिछले कई सालों से बन्द है। हर रोज सुबह सिर्फ सफाई और एक बड़ी-सी
मुस्कुराते हुए नौजवान की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने के लिए थोड़ी देर
को खुलता है और फिर बन्द हो जाता है। यह कमरा आज से कई वर्षों पहले भी एक
रात को जैसा था आज भी वैसा ही है। डबल बैड पर आड़े-तिरछे तकिये,
सिमटी-सुकड़ी चादर, ड्रेसिंग मेज पर रखा चश्मा, हैंगर पर सूट, फर्श पर
पड़े जूते, मेज पर बिखरी रेजगारी, इन्तिजार करता नाइट सूट, वक्त को
नापते-नापते न जाने कब की बन्द घड़ी ऐसा लगता है, जैसे कोई जल्दी लौटने के
लिये अभी-अभी बाहर गया है, जाने वाला उस रात के बाद अपने कमरे का रास्ता
भूल गया लेकिन उसका कमरा उसकी तस्वीर और बिखरी हुई चीजों के साथ, आज भी
उसके इन्तजार में है।
इस कमरे में रहने वाले का नाम विवेक सिंह था, और मृत को जीवित रखने वाले का नाम मशहूर ग़ज़ल सिंगर जगजीत सिंह है जो विवेक के पिता हैं। यह कमरा इन्सान और भगवान के बीच निरंतर लड़ाई का प्रतीकात्मक रूप हैं। भगवान बना कर मिटा रहा है, और इन्सान मिटे हुए को मुस्कुराती तस्वीर में, अगरबत्ती जलाकर, मुसलसल साँसे जगा रहा है। मौत और जिन्दगी की इसी लड़ाई का नाम इतिहास है। इतिहास दो तरह के होते हैं। एक वह जो राजाओं और बादमाशों के हार-जीत के किस्से दोहराता हैं और दूसरा वह जो उस आदमी के दुख-दर्द का साथ निभाता है जो हर युग में राजनीति का ईधन बनाया जाता है, और अनबूझ कर भुलाया जाता है।
इस कमरे में रहने वाले का नाम विवेक सिंह था, और मृत को जीवित रखने वाले का नाम मशहूर ग़ज़ल सिंगर जगजीत सिंह है जो विवेक के पिता हैं। यह कमरा इन्सान और भगवान के बीच निरंतर लड़ाई का प्रतीकात्मक रूप हैं। भगवान बना कर मिटा रहा है, और इन्सान मिटे हुए को मुस्कुराती तस्वीर में, अगरबत्ती जलाकर, मुसलसल साँसे जगा रहा है। मौत और जिन्दगी की इसी लड़ाई का नाम इतिहास है। इतिहास दो तरह के होते हैं। एक वह जो राजाओं और बादमाशों के हार-जीत के किस्से दोहराता हैं और दूसरा वह जो उस आदमी के दुख-दर्द का साथ निभाता है जो हर युग में राजनीति का ईधन बनाया जाता है, और अनबूझ कर भुलाया जाता है।
तारीख में महल भी हैं, हाकिम भी तख्त भी
गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर
गुमनाम जो हुए हैं वो लश्कर तलाश कर
मैंने ऐसे ही ‘गुमनामों’ को नाम और चेहरे देने की
कोशिश की
है, मैंने अपने अतीत को वर्तमान में जिया है। और पुष्प विला की तीसरी
मंजिल के हर कमरे की तरह अकीदत की अगरबत्तियाँ जलाकर ‘तमाशा
मेरे
आगे’ को रौशन किया है। फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ एक तस्वीर थी
और
मेरे साथ बहुत सी यादों के गम शामिल हैं। बीते हुए का फिर से जीने में
बहुत कुछ अपना भी दूसरों में शरीक हो जाता है, यह बीते हुए को याद करने
वाले की मजबूरी भी है। समय गुज़र कर ठहर जाता है और उसे याद करने वाले
लगातार बदलते जाते हैं, यह बदलाव उसी वक्त थमता है जब वह स्वयं दूसरों की
याद बन जाता है। इन्सान और भगवान के युद्ध में मेरी हिस्सेदारी इतनी ही है।
खुदा के हाथों में मत सौंप सारे कामों को
बदलते वक्त पर कुछ अपना इख्तियार भी रख-
बदलते वक्त पर कुछ अपना इख्तियार भी रख-
इस किताब को लिखा है मैंने लेकिन लिखवाया है राजकुमार केसवानी ने जिसके
लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
फ्लाबियर ने अपने चर्चित उपन्यास मैडम बॉवेरी के प्रकाशन के बारे में कहा था...काश मेरे पास इतना पैसा होता कि सारी किताबें खरीद लेता और इसे फिर से लिखता....समय का अभाव नहीं होता तो मैं भी ऐसा ही करता मेरा एक शेर है-
फ्लाबियर ने अपने चर्चित उपन्यास मैडम बॉवेरी के प्रकाशन के बारे में कहा था...काश मेरे पास इतना पैसा होता कि सारी किताबें खरीद लेता और इसे फिर से लिखता....समय का अभाव नहीं होता तो मैं भी ऐसा ही करता मेरा एक शेर है-
कोशिश के बावजूद यह उल्लास रह गया
हर काम में हमेशा कोई काम रह गया
हर काम में हमेशा कोई काम रह गया
जिंदगी हिसाबों से जी नहीं जाती
एक थे फजल ताबिश। आज से तीस-चालीस साल पहले का भोपाल आज जैसा भोपाल नहीं
था। जगह-जगह मुशायरों की महफिलें सजाता था, शेर सुनाता था और दाद पाता था।
जवान, अधेड़ और बुजुर्ग, वह एक साथ कई चेहरों में नज़र आता था। कहीं तो
कच्चे दालानों में गाव-तकियों से पीठ टिकाए गज़ल के इतिहास को दोहराता था,
कहीं अधेड़ बनकर छोटे-बड़े चायखानों में ग़ज़ल और राजनीति के रिश्तों पर
नई-नई बहसें जगाता था और कहीं नौजवानों जैसी नई शायरी सुनाता था और रात को
देर तक पान की गिलौरियाँ चबाता था।
फ़ज़ल ताबिश उस भोपाल के नौजवान प्रतिनिधि थे। मुँह में होठों को लाल करता पान, उँगली पर चूने का चुटकी-भर निशान, पठानी आनबान और बात-बात पर गूँजते क़हक़हों की उड़ान उनकी पहचान थी। वह बहुत हँसते थे। अपने हम उम्रों में उनके पास सबसे ज्यादा हँसी का भंडार था, जिसे वह जी खोलकर खर्च करते थे। किसी परिचित की परेशानियाँ या किसी अजनबी की हैरानी के अलावा हर घटना या विषय उनके लिए क़हक़हे का कारण था। उन दिनों उनका क़हक़हा ताज और दुष्यंत की ग़ज़ल शेरी भोपाली की शेरवानी, कैफ भोपाली के फक्कड़पन की तरह भोपाल में मशहूर था। फ़र्क केवल इतना था, ताज, शेरी, कैफ़ और दुष्यंत भोपाल के बाहर भी जाने जाते थे और फ़ज़ल के क़हक़हे अभी सिर्फ तालाबों के इर्द-गिर्द ही पहचाने जाते थे। लगातार हँसने ने फ़ज़ल के चेहरे की शादाबी में इज़ाफ़ा किया था। उनका एक शेर है-
फ़ज़ल ताबिश उस भोपाल के नौजवान प्रतिनिधि थे। मुँह में होठों को लाल करता पान, उँगली पर चूने का चुटकी-भर निशान, पठानी आनबान और बात-बात पर गूँजते क़हक़हों की उड़ान उनकी पहचान थी। वह बहुत हँसते थे। अपने हम उम्रों में उनके पास सबसे ज्यादा हँसी का भंडार था, जिसे वह जी खोलकर खर्च करते थे। किसी परिचित की परेशानियाँ या किसी अजनबी की हैरानी के अलावा हर घटना या विषय उनके लिए क़हक़हे का कारण था। उन दिनों उनका क़हक़हा ताज और दुष्यंत की ग़ज़ल शेरी भोपाली की शेरवानी, कैफ भोपाली के फक्कड़पन की तरह भोपाल में मशहूर था। फ़र्क केवल इतना था, ताज, शेरी, कैफ़ और दुष्यंत भोपाल के बाहर भी जाने जाते थे और फ़ज़ल के क़हक़हे अभी सिर्फ तालाबों के इर्द-गिर्द ही पहचाने जाते थे। लगातार हँसने ने फ़ज़ल के चेहरे की शादाबी में इज़ाफ़ा किया था। उनका एक शेर है-
न कर शुमार कि हर शै गिना नहीं जाती
ये जिंदगी है हिसाबों से जी नहीं जाती
ये जिंदगी है हिसाबों से जी नहीं जाती
मिर्ज़ा ग़ालिब ने बुढ़ापे में अपनी महबूबा के हुस्न को याद किया था,
जिसके बारे में सबने उनके ख़तों के संग्रह में पढ़ा। फ़ज़ल ताबिश को मैंने
आँखों से देखा था। उनके व्यक्तित्व में काबुल के सुर्ख सेबों की तरुणाई और
वहाँ के बर्फपोश पहाड़ों की ऊँचाइयों का आकर्षण था। शादी से पहले वह
बहुत-सी आँखों के सपने थे, लेकिन शादी के बाद सिर्फ ताहिरा खाँ के अपने
थे। ताहिरा खाँ, उनकी बेगम थीं। इस संबंध में उनका एक शेर है-
फिर हमने एक प्यार किया, फिर वही हुआ
वो दिलबर भी ताहिरा खाँ से हार गया
वो दिलबर भी ताहिरा खाँ से हार गया
बात-बात पर घड़ी-घड़ी हँसने वाले शायर फ़ज़ल ताबिश एक नाराज़ जेहन, के
फ़नकार थे। उनकी नाराज़गी सियासत से थी, धार्मिक भेदभाव की लानत से थी,
इंसान के हाथों इंसान की शहादत से थी, उनकी कविता नेकी और बदी की लड़ाई
में क्रियात्मक साझेदारी की फ़नकारी थी। वह आधुनिक प्रगतिशील शायर थे।
उनका संग्रह ‘रोशनी किस जगह से काली है’ 1944 में
प्रकाशित
हुआ था। उनका एक शेर, जिसकी एक पंक्ति उनके संग्रह का नाम है, उनके काव्य
चरित्र का बयान भी है-
रेशा-रेशा उधेड़कर देखो
रोशनी किस जगह से काली है
रोशनी किस जगह से काली है
फ़ज़ल का जन्म 15 अगस्त 1933 में हुआ। भोपाल के एक पुराने ख़ानदान के
चिराग़ थे। घर का माहौल मज़हबी था और घर के बाहर वह कम्युनिस्ट थे। उन
दिनों भोपाल के लोकप्रिय कम्युनिस्ट, कॉमरेड शाकिर अली ख़ाँ थे। वह पाँचों
वक्त खुदा के दरबार में सिर झुकाते थे और नमाज़ों के बाद सामाजिक
नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सुर्ख परचम उठाते थे। फ़ज़ल ताबिश के स्वभाव का
संतुलन भी इसी इलाक़ाई माहौल और भोपाली कम्युनिज्म की देन था। वह मुसलमान
थे, लेकिन उनकी मुसलमानियत में दूसरे धर्मों की इंसानियत की थी इज्जत
शामिल थी।
फ़ज़ल ताबिश के साथ शुरू में ज़िंदगी का सुलूक कुछ अच्छा नहीं रहा। अभी वह प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे कि अचानक सारा घर बोझ बनकर उनके कंधों पर आ गिरा। घर में सबसे बड़ा होने की सज़ा उन्होंने स्वीकार की और अपनी शिक्षा रोक कर एक कार्यालय में बाबूगिरी करने लगे। निरंतर 15 बरस घर की जिम्मेदारियों में ख़र्च होने के बाद जो थोड़ा-बहुत बचे थे, उससे उर्दू में एम.ए. किया और हमीदिया कॉलेज में लेक्चरर हो गए। जिंदगी की इस लंबी दौड़-धूप में साहित्य भी साथ-साथ चलता रहा। शायरी के अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी रचे और मणि कौल और कुमार शहानी की फिल्मों में अभिनय भी किया।
उनकी आमदनी सिर्फ अपने लिए नहीं थी। उसमें बहुत-सों की भागीदारी थी। इसमें ताज भोपाली का नशा था, एक दोस्त की बेटी की पढ़ाई थी, रात में यार-दोस्तों की मेहमानवाजी थी और पार्टी व सामाजिक सम्मेलनों के लिए चंदा भी था। उनका घर भोपाल के इक़बाल मैदान के सामने शीशमहल की ऊपरी मंजिल में था। नवाबी दौर में यह इमारत खई पहरों की निगरानी में थी, जब से फ़ज़ल ताबिश का निवास बनी, शहर-भर के साहित्यकरों और पार्टी वर्करों की हुक्मरानी में थी। ताला-कुंडी से आज़ाद यह घर सबके लिए खुला था। फ़ज़ल घर में हों या न हों, ताहिरा खाँ, हों उनके दोस्तों में कोई भी किसी भी वक्त भी इसमें जा सकता था, रसोई में खाना खा सकता था, चाय बना सकता था, खा-पीकर आराम फ़रमा सकता था और तरो-ताज़ा होकर वापस जा सकता था।
फ़ज़ल ताबिश के साथ शुरू में ज़िंदगी का सुलूक कुछ अच्छा नहीं रहा। अभी वह प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे कि अचानक सारा घर बोझ बनकर उनके कंधों पर आ गिरा। घर में सबसे बड़ा होने की सज़ा उन्होंने स्वीकार की और अपनी शिक्षा रोक कर एक कार्यालय में बाबूगिरी करने लगे। निरंतर 15 बरस घर की जिम्मेदारियों में ख़र्च होने के बाद जो थोड़ा-बहुत बचे थे, उससे उर्दू में एम.ए. किया और हमीदिया कॉलेज में लेक्चरर हो गए। जिंदगी की इस लंबी दौड़-धूप में साहित्य भी साथ-साथ चलता रहा। शायरी के अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी रचे और मणि कौल और कुमार शहानी की फिल्मों में अभिनय भी किया।
उनकी आमदनी सिर्फ अपने लिए नहीं थी। उसमें बहुत-सों की भागीदारी थी। इसमें ताज भोपाली का नशा था, एक दोस्त की बेटी की पढ़ाई थी, रात में यार-दोस्तों की मेहमानवाजी थी और पार्टी व सामाजिक सम्मेलनों के लिए चंदा भी था। उनका घर भोपाल के इक़बाल मैदान के सामने शीशमहल की ऊपरी मंजिल में था। नवाबी दौर में यह इमारत खई पहरों की निगरानी में थी, जब से फ़ज़ल ताबिश का निवास बनी, शहर-भर के साहित्यकरों और पार्टी वर्करों की हुक्मरानी में थी। ताला-कुंडी से आज़ाद यह घर सबके लिए खुला था। फ़ज़ल घर में हों या न हों, ताहिरा खाँ, हों उनके दोस्तों में कोई भी किसी भी वक्त भी इसमें जा सकता था, रसोई में खाना खा सकता था, चाय बना सकता था, खा-पीकर आराम फ़रमा सकता था और तरो-ताज़ा होकर वापस जा सकता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book