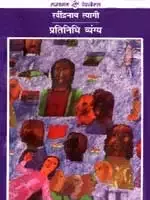|
लेख-निबंध >> प्रतिनिधि व्यंग्य प्रतिनिधि व्यंग्यरवीन्द्रनाथ त्यागी
|
50 पाठक हैं |
||||||
रवीन्द्रनाथ त्यागी के चुने हुए व्यंग्य निबंधों को संग्रह....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रवीन्द्रनाथ त्यागी समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण
व्यंग्य-लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी व्यंग्य-रचनाओं में घटनाओं
और चरित्रों के बजाय परिवेश और स्थितियों का चित्रण मिलता है, जिसके
माध्यम से वे अपने समय और समाज के विभिन्न अंतर्विरोधों को रेखांकित करते
हैं। इस प्रक्रिया में उनके लिए इतिहास, पुराण, साहित्य, संस्कृति,
राजनीति और प्रशासन-कुछ भी निषिद्ध नहीं है। सब कुछ जैसे उनके लेखकीय
अनुभव में शामिल हैं। वे बिना अपना बचाव किए हर जगह चोट करते हैं और बेहद
सहज भाव से, मानों हँसते-हँसते जीवन के गंभीर और बुनियादी सवालों तक जा
पहुँचते हैं। ‘पूज्य’ कही जानेवाली नारी उनके व्यंग्यों में
सब कहीं मौज़ूद है जो कहीं सामंती तो कहीं पूँजीवादी अप-संस्कृति से उपजी
पुरुष-कुंठाओं और विकृतियों की शिकार नज़र आती है। कहना न होगा कि यह कृति
अपने समय की बहुत-सी अशिष्टताओं पर बहुत ही शिष्टता से विचार करती है।
जब मैं दौरे पर गया
जैसा कि आप में से समझदार लोग जानते होंगे, दौरे जो होते हैं वे कई तरह के
होते हैं। एक दौरा तो बीमारी की किस्म का होता है जैसे कि मिरगी का दौरा
और एक दौरा वह होता है जो किसी शायर के तन्हा दिल में अपनी तन्हा ग़ज़ल
दूसरों तक पहुँचाने के लिए उठता है वह भी-कभी काफी ज़बर्दस्त किस्म का
होता है और हालत यह होती है कि उस दौरे के दौरान जो कुछ भी हो जाए वह कम
है। कभी शायर का गरेबाँ चाक किया जाता है तो कभी उसके चाँद जैसे मुखड़े पर
जूते चप्पल फेंके जाते हैं जो कि महबूबा की निगाहों की अपेक्षा कहीं
ज्य़ादा तीखे, वफ़ादार और पुरअसर साबित होते हैं। कवि की प्रेयसि तो सिर्फ
उसके दिल की ही देखभाल करती है जब कि ये भौतिक पदार्थ शरीर के शेष अंगों
की सेवा भी उसी तत्परता के साथ करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक
मुशायरे में अपनी एक आँख खोने के बाद एक बुज़ुर्गवार शायर ने अपनी दूसरी
आँख की सेहत का खयाल रखते हुए कविता करना ही छोड़ दिया था। कविता और आँख
से मुक्ति पाने के बाद वे समीक्षा लिखने लगे क्योंकि समीक्षक को दो तो
क्या, एक आँख की भी जरूरत कभी नहीं पड़ी। एक और शायर थे जो एक मुशायरे में
इतने घायल हुए थे कि उस दिन से उन्होंने अपना उपन्यास ही
‘घायल’ रख लिया। खैर, अंत में चलकर एक दौरा वह भी
होता है जो
कि सरकार के आला अफ़सर गाहे-बगाहे करते रहते हैं। गर्मियों में वे पहाड़
जाते हैं और सर्दियों में दक्षिण। जिस दौरे की चर्चा मैं कर रहा था, वह इस
आखिरी किस्म का ही था।
गर्मी ज्यादा होने के कारण मैंने पहाड़ों पर ही जाना तय किया। कई छोटे-मोटे दफ्तर थे। जिनका निरीक्षण न जाने कब से नहीं हुआ था। जहाँ मैं जा रहा था, उसी क्षेत्र में एक संन्यासी भी रहते थे जो न जाने कब से मौन व्रत धारण किए हुए थे। उनकी आयु का पता किसी को नहीं था। एक बार बहुत आग्रह करने पर बाबा ने स्वयं ही यह सूचना दी थी कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो भंडारा किया था, उसमें वे गए थे और इसके अलावा उन बेचारों को खुद भी कुछ पता नहीं था। इतना बताते के बाद बाबा फिर से मौन हो गए थे, जैसा कि वह पिछले सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे। एक मित्र ने बताया कि पर्वतों पर कभी-कभी काफी ठंड हो जाती है। बहरहाल, सारी बातें मद्दे-नज़र रखते हुए मैंने बीवी को भी अपने साथ ले लिया।
स्टेशन तक छोड़ने दफ्तर के लोग गए। उन्होंने डिब्बा तलाश किया, सीट तलाश की, बिस्तर खोले, सुराही भरी और उसके बाद गाड़ी चलने तक हाथ बाँधें वे लोग वहीं प्लेटफार्म पर ही खड़े रहे। काफ़ी खुश दिखाई देते थे। सोच रहे होंगे कि चलो, इस नामाकूल के बाहर जाने से अब हफ़्ता-दस दिन तो आराम से कटेगा। मैंने उनसे चले जाने के लिए कई बार कहा, मगर वे थे कि मैंने वाकई स्टेशन छोड़ दिया। वे वहीं अपने पिछले पैरों के सहारे खड़े रहे और सिगनल की दिशा में देखते रहे। गाड़ी जो थी वह भी काफ़ी नियमित आदतों की थी; बाकी दिन भी लगभग एक घंटा लेट चलती थी, आज भी लगभग एक घंटा लेट चली। और क्योंकि यह डाकगाड़ी थी, इसकी गति तीस किलोमीटर से कम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता, बड़े स्टेशनों पर इस गरीब को भी रुकना पड़ा। मजबूरी जो ठहरी। और जब रुक गई तो फिर आधा घंटे से पहले चलना भी क्या ? प्रेमिका चाहे कैसी भी हो, अपने पुराने प्रेमियों को पूरी तरह कभी नहीं भूल सकती। और इस गाड़ी की तो उन स्टेशनों से बरसों पुरानी जान-पहचान थी। एक परिचित स्टेशन पर तो यह पतिव्रता गाड़ी कोई एक घंटा रुकी। ठीक आधी रात का समय, हल्की-सी बूँदाबाँदी और बत्तियाँ एकदम गुल। ऐसे वातावरण में तो इसे विद्यापति या जयदेव की अभिसारिका बनना ही था।
मेरे डिब्बे में चार बर्थ थीं। दो हमारी थीं और दो सामने वाले प्राणियों की। इन प्राणियों में से एक पुल्लिंग था और एक स्त्रीलिंग। पुरुष जो थे वे काफ़ी अधेड़ थे और सेहत की स्थिति यह थी कि बिना किसी संकोच के एक स्वस्थ हाथी की छटा देते थे। अंतर बस इतना ही था कि जहाँ हाथी के केवल दो दाँत ही मुँह के बाहर निकले होते हैं, वहाँ इनके कोई पंद्रह दाँत बाहर निकले हुए थे और इस चराचर सृष्टि की शोभा निहार रहे थे। जहाँ तक स्त्री-रत्न का प्रश्न है, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल था। वे उस अधेड़ सज्जन की बहन भी तो हो सकती थी, कन्या भी और पत्नी भी। बहरहाल वे उनकी अम्मा हरगिज़ नहीं थी। उन्होंने अपने उस हाथी रूपधारी साथी को बहुत कम देखा; वे या तो खिड़की के बार पीछे भागता फूलों-भरा क्षितिज ही देखती रहीं या फिर अपने ओठ और लिपस्टिक ही ठीक करती रहीं। उनका मुखड़ा यदि सेर-भर का था तो पाउडर उस पर इतना पुता हुआ था। कि सेर पर सवा सेर वाली कहावत एकदम मज़ा दे जाती थी। वैसे मज़ा उस वक्त भी कम नहीं आया जब कि वे स्थूलकाय सज्जन डिब्बे से बाहर जाते समय फिसले और अपने पंद्रह दातों के साथ काफ़ी तबीयत के साथ धराशायी हो गए। मैं तो सोचता था कि अब कोई क्रेन वगैरह ही आकर इन्हें सीधा करेगी, पर डिब्बे में कुछ सर्वोदयी किस्म के यात्रियों के सामूहिक प्रयत्नों से वे उठ गए। उनको उठाने की उस प्रक्रिया में डिब्बे के दो-चार यात्री जो फिसल गए-वह एक दीगर बात ठहरी।
मैं उस मनुष्य-रूपी हाथी को देखता रहा और मन-ही-मन प्रणाम करता रहा। इतिहास साक्षी है कि पोरस, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान, इब्राहीम लोदी और दाराशिकोह-इन सबका पतन मात्र हाथियों के कारण ही हुआ था। मगर यह महान् आत्मा थी कि गजगामी और गजानन होने के बावजूद सिर्फ अपना ही पतन करती थी, किसी दूसरे का नहीं। और हाँ, इनके पतित होने का उस रूपवती स्त्री पर कोई असर नहीं पड़ा। वे उसी भाँति बैठी रहीं और रूप सँवारती रहीं। हम लोगों को तो वे इस भाँति देखती रहीं जैसे कि फिसलना तो उन हज़रत का खानदानी शौक था और हम तो उसमें बिना बात दखल दे रहे थे। कभी-कभी तो वे इस अंदाज में देखती थीं कि सीधा करना है तो मुझे करो: इस गरीब और बूढ़े इंसान से छेड़छाड़ करने से क्या फायदा ?
रेल से उतरकर हम दोनों ने सरकारी गाड़ी में सफ़र किया। कोई पचास कर्मचारी हमारे स्वागत को आए थे। किसी के हाथ में फूलमाला थी तो किसी के साथ ताजा अखबार और ताजे फल। फूलमालाएँ मेरे गले में पड़ी और फल वगैरह मेरी पत्नी को दिए गए। एक होनहार नौजवान मेरी पत्नी के गले में भी फूलमाला डालना चाहते थे पर पता नहीं क्यों, मुझे देखकर सहसा सहम गए। मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब मैं भी अपनी पत्नी के गले में माला डालना चाहता था पर उनके अब्बाजान को देखकर सहसा सहम गया था। यादों की शहनाई बजनी शुरू हुई ही थी कि हमारा अगला सफर शुरू हो गया थ और ‘बिसमिल्ला’ खान जो थे, वे अपने शहनाई के साथ चुप हो गए। एक राजपवित्र अधिकारी और एक चपरासी हमारे साथ गाड़ी में बैठे और बाकी लोग पता नहीं कैसे वापस लौटे। पत्नी जो थी वह रास्ते-भर फल खाती रही। आज उसका व्रत का दिन था : आज तो फल क्या, यदि फूलों का वृक्ष भी मिल जाता तो उसकी भी खैरियत नहीं थी। आर्य-ललनाएँ व्रतों के संदर्भ में सदा से चरित्रवती होती आई।
कोई चार घंटे में हम लोग अपने मंजिले-मकसूद तक पहुँच गए। काफी जनसंख्या हमें रिसीव करने को खड़ी थी। डाकबँगले का एक कक्ष हमारे लिए सजाया गया था और चंद चपरासी गुलदस्तों की अदा में अपनी वर्दी में हाजिर थे। चपरासी तमीज़दार किस्म के थे: उन्होंने मेरी पत्नी को भी ‘सर’ ही कहकर पुकारा, जिसे सुनकर अपना तो कलेजा ही दहल गया। इस उम्र में पत्नी यदि यौन-परिवर्तन कर जाए तो काफी दिक्कत पड़ती है। कमरे के भीतर ढेर सारी पत्र-पत्रिकाएँ रखी थीं-खासकर वे जिनमें कि मेरी रचनाएँ छपी थीं। साबुन, सिगरेट और मेवे का प्रबन्ध था। कुछ लोगों की बीवियाँ भी बरामदे में खड़ी थीं। सारा माहौल कुछ ऐसा था कि मेरी बीवी को भी रोब लेने का मूड़ आना शुरू हो गया। इसी मूड़ के दौरान एक बार उसने मुझे भी इडियट कहा, जो इत्तफ़ाक से मेरे अतिरिक्त किसी गैर ने नहीं सुना।
इसके बाद मैं वहाँ कोई हफ़्ता-भर दफ़्तर की फाइलें देखता रहा, वाउचर लिंक करता रहा, संबंधित अधिकारियों से मुलाकातें करता रहा और बीवी की आँख बचाकर डाँकबँगले में ठहरी एक मेम साहब के सौंदर्य को भी निहारता रहा। इस दौरान मेरी बीवी जो थी वह सरकार के खर्चे पर आसपास के पर्वतों की सैर करती रही, मौन रहनेवाले उन बाबा के आश्रम में जाती रही और दावतें खाती रही। उस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान अगर कुछ वक्त मिला तो उसमें कुछ तोहफें बटोर लिए। हफ्ते-भर बाद जब हम लौटे तो महसूस हुआ कि उन तोहफ़ों की वजह से सामान जो था वह कई गुना बढ़ गया था। मेरी भावुक पत्नी ने बताया कि इन तोहफों को अस्वीकार करने से छोटे कर्मचारियों की पत्नियों के हृदय को ठेस पहुँचती। इसके अतिरिक्त स्थानीय हस्तशिल्प-कला को यदि हम लोग ही प्रोत्साहन न देंगे तो फिर कौन देगा ? आखिर इन लोगों को कुछ अतिरिक्त आय होती ही होगी जो इतने तोहफे दे रहे हें वरना तंगी के दिनों में कौन इतनी हिम्मत करता ? मैंने पत्नी की कद्र की और डाकबँगले के बिल के भुगतान का भार भी अपने एक नायब पर ही छोड़ दिया। और हाँ, डाकबँगले की चम्मचें बहुत बढ़िया थीं : खानसामा की निगाह बचाकर हम लोग दो अदद चम्मच भी उठा लाए। वैदिकी हिंसा न भवति। मैं तो खैर एक ही चम्मच से संतुष्ट था पर पत्नी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहा कि लेना है तो जोड़ी ही लो; अकेली चम्मच को विरह सताएगा।
हम लोगों के वापसी टिकट भी वहीं के लोगों ने खरीदे। लौटते वक्त शानदार विदाई दी गई। बेवकूफ होने के नाते मैं बराबर यही सोचता रहा कि अधीन कर्मचारियों के साथ समाधि तब टूटी, जब कि गाड़ी ने गति ले ली और स्टेशन काफी पीछे छूट गया। मैंने नेत्र खोले। फूलमालाओं और तोहफों के डिब्बों से दबी मेरी पत्नी ने बड़ी मासूममियत के साथ मुझे अरसे बाद देखा और एक निहायत ईमानदार मुसकराहट के साथ पूछा कि हे आर्यपुत्र, तुम दौरे पर हर महीने क्यों नहीं जाते ?
गर्मी ज्यादा होने के कारण मैंने पहाड़ों पर ही जाना तय किया। कई छोटे-मोटे दफ्तर थे। जिनका निरीक्षण न जाने कब से नहीं हुआ था। जहाँ मैं जा रहा था, उसी क्षेत्र में एक संन्यासी भी रहते थे जो न जाने कब से मौन व्रत धारण किए हुए थे। उनकी आयु का पता किसी को नहीं था। एक बार बहुत आग्रह करने पर बाबा ने स्वयं ही यह सूचना दी थी कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो भंडारा किया था, उसमें वे गए थे और इसके अलावा उन बेचारों को खुद भी कुछ पता नहीं था। इतना बताते के बाद बाबा फिर से मौन हो गए थे, जैसा कि वह पिछले सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे। एक मित्र ने बताया कि पर्वतों पर कभी-कभी काफी ठंड हो जाती है। बहरहाल, सारी बातें मद्दे-नज़र रखते हुए मैंने बीवी को भी अपने साथ ले लिया।
स्टेशन तक छोड़ने दफ्तर के लोग गए। उन्होंने डिब्बा तलाश किया, सीट तलाश की, बिस्तर खोले, सुराही भरी और उसके बाद गाड़ी चलने तक हाथ बाँधें वे लोग वहीं प्लेटफार्म पर ही खड़े रहे। काफ़ी खुश दिखाई देते थे। सोच रहे होंगे कि चलो, इस नामाकूल के बाहर जाने से अब हफ़्ता-दस दिन तो आराम से कटेगा। मैंने उनसे चले जाने के लिए कई बार कहा, मगर वे थे कि मैंने वाकई स्टेशन छोड़ दिया। वे वहीं अपने पिछले पैरों के सहारे खड़े रहे और सिगनल की दिशा में देखते रहे। गाड़ी जो थी वह भी काफ़ी नियमित आदतों की थी; बाकी दिन भी लगभग एक घंटा लेट चलती थी, आज भी लगभग एक घंटा लेट चली। और क्योंकि यह डाकगाड़ी थी, इसकी गति तीस किलोमीटर से कम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता, बड़े स्टेशनों पर इस गरीब को भी रुकना पड़ा। मजबूरी जो ठहरी। और जब रुक गई तो फिर आधा घंटे से पहले चलना भी क्या ? प्रेमिका चाहे कैसी भी हो, अपने पुराने प्रेमियों को पूरी तरह कभी नहीं भूल सकती। और इस गाड़ी की तो उन स्टेशनों से बरसों पुरानी जान-पहचान थी। एक परिचित स्टेशन पर तो यह पतिव्रता गाड़ी कोई एक घंटा रुकी। ठीक आधी रात का समय, हल्की-सी बूँदाबाँदी और बत्तियाँ एकदम गुल। ऐसे वातावरण में तो इसे विद्यापति या जयदेव की अभिसारिका बनना ही था।
मेरे डिब्बे में चार बर्थ थीं। दो हमारी थीं और दो सामने वाले प्राणियों की। इन प्राणियों में से एक पुल्लिंग था और एक स्त्रीलिंग। पुरुष जो थे वे काफ़ी अधेड़ थे और सेहत की स्थिति यह थी कि बिना किसी संकोच के एक स्वस्थ हाथी की छटा देते थे। अंतर बस इतना ही था कि जहाँ हाथी के केवल दो दाँत ही मुँह के बाहर निकले होते हैं, वहाँ इनके कोई पंद्रह दाँत बाहर निकले हुए थे और इस चराचर सृष्टि की शोभा निहार रहे थे। जहाँ तक स्त्री-रत्न का प्रश्न है, उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल था। वे उस अधेड़ सज्जन की बहन भी तो हो सकती थी, कन्या भी और पत्नी भी। बहरहाल वे उनकी अम्मा हरगिज़ नहीं थी। उन्होंने अपने उस हाथी रूपधारी साथी को बहुत कम देखा; वे या तो खिड़की के बार पीछे भागता फूलों-भरा क्षितिज ही देखती रहीं या फिर अपने ओठ और लिपस्टिक ही ठीक करती रहीं। उनका मुखड़ा यदि सेर-भर का था तो पाउडर उस पर इतना पुता हुआ था। कि सेर पर सवा सेर वाली कहावत एकदम मज़ा दे जाती थी। वैसे मज़ा उस वक्त भी कम नहीं आया जब कि वे स्थूलकाय सज्जन डिब्बे से बाहर जाते समय फिसले और अपने पंद्रह दातों के साथ काफ़ी तबीयत के साथ धराशायी हो गए। मैं तो सोचता था कि अब कोई क्रेन वगैरह ही आकर इन्हें सीधा करेगी, पर डिब्बे में कुछ सर्वोदयी किस्म के यात्रियों के सामूहिक प्रयत्नों से वे उठ गए। उनको उठाने की उस प्रक्रिया में डिब्बे के दो-चार यात्री जो फिसल गए-वह एक दीगर बात ठहरी।
मैं उस मनुष्य-रूपी हाथी को देखता रहा और मन-ही-मन प्रणाम करता रहा। इतिहास साक्षी है कि पोरस, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान, इब्राहीम लोदी और दाराशिकोह-इन सबका पतन मात्र हाथियों के कारण ही हुआ था। मगर यह महान् आत्मा थी कि गजगामी और गजानन होने के बावजूद सिर्फ अपना ही पतन करती थी, किसी दूसरे का नहीं। और हाँ, इनके पतित होने का उस रूपवती स्त्री पर कोई असर नहीं पड़ा। वे उसी भाँति बैठी रहीं और रूप सँवारती रहीं। हम लोगों को तो वे इस भाँति देखती रहीं जैसे कि फिसलना तो उन हज़रत का खानदानी शौक था और हम तो उसमें बिना बात दखल दे रहे थे। कभी-कभी तो वे इस अंदाज में देखती थीं कि सीधा करना है तो मुझे करो: इस गरीब और बूढ़े इंसान से छेड़छाड़ करने से क्या फायदा ?
रेल से उतरकर हम दोनों ने सरकारी गाड़ी में सफ़र किया। कोई पचास कर्मचारी हमारे स्वागत को आए थे। किसी के हाथ में फूलमाला थी तो किसी के साथ ताजा अखबार और ताजे फल। फूलमालाएँ मेरे गले में पड़ी और फल वगैरह मेरी पत्नी को दिए गए। एक होनहार नौजवान मेरी पत्नी के गले में भी फूलमाला डालना चाहते थे पर पता नहीं क्यों, मुझे देखकर सहसा सहम गए। मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब मैं भी अपनी पत्नी के गले में माला डालना चाहता था पर उनके अब्बाजान को देखकर सहसा सहम गया था। यादों की शहनाई बजनी शुरू हुई ही थी कि हमारा अगला सफर शुरू हो गया थ और ‘बिसमिल्ला’ खान जो थे, वे अपने शहनाई के साथ चुप हो गए। एक राजपवित्र अधिकारी और एक चपरासी हमारे साथ गाड़ी में बैठे और बाकी लोग पता नहीं कैसे वापस लौटे। पत्नी जो थी वह रास्ते-भर फल खाती रही। आज उसका व्रत का दिन था : आज तो फल क्या, यदि फूलों का वृक्ष भी मिल जाता तो उसकी भी खैरियत नहीं थी। आर्य-ललनाएँ व्रतों के संदर्भ में सदा से चरित्रवती होती आई।
कोई चार घंटे में हम लोग अपने मंजिले-मकसूद तक पहुँच गए। काफी जनसंख्या हमें रिसीव करने को खड़ी थी। डाकबँगले का एक कक्ष हमारे लिए सजाया गया था और चंद चपरासी गुलदस्तों की अदा में अपनी वर्दी में हाजिर थे। चपरासी तमीज़दार किस्म के थे: उन्होंने मेरी पत्नी को भी ‘सर’ ही कहकर पुकारा, जिसे सुनकर अपना तो कलेजा ही दहल गया। इस उम्र में पत्नी यदि यौन-परिवर्तन कर जाए तो काफी दिक्कत पड़ती है। कमरे के भीतर ढेर सारी पत्र-पत्रिकाएँ रखी थीं-खासकर वे जिनमें कि मेरी रचनाएँ छपी थीं। साबुन, सिगरेट और मेवे का प्रबन्ध था। कुछ लोगों की बीवियाँ भी बरामदे में खड़ी थीं। सारा माहौल कुछ ऐसा था कि मेरी बीवी को भी रोब लेने का मूड़ आना शुरू हो गया। इसी मूड़ के दौरान एक बार उसने मुझे भी इडियट कहा, जो इत्तफ़ाक से मेरे अतिरिक्त किसी गैर ने नहीं सुना।
इसके बाद मैं वहाँ कोई हफ़्ता-भर दफ़्तर की फाइलें देखता रहा, वाउचर लिंक करता रहा, संबंधित अधिकारियों से मुलाकातें करता रहा और बीवी की आँख बचाकर डाँकबँगले में ठहरी एक मेम साहब के सौंदर्य को भी निहारता रहा। इस दौरान मेरी बीवी जो थी वह सरकार के खर्चे पर आसपास के पर्वतों की सैर करती रही, मौन रहनेवाले उन बाबा के आश्रम में जाती रही और दावतें खाती रही। उस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान अगर कुछ वक्त मिला तो उसमें कुछ तोहफें बटोर लिए। हफ्ते-भर बाद जब हम लौटे तो महसूस हुआ कि उन तोहफ़ों की वजह से सामान जो था वह कई गुना बढ़ गया था। मेरी भावुक पत्नी ने बताया कि इन तोहफों को अस्वीकार करने से छोटे कर्मचारियों की पत्नियों के हृदय को ठेस पहुँचती। इसके अतिरिक्त स्थानीय हस्तशिल्प-कला को यदि हम लोग ही प्रोत्साहन न देंगे तो फिर कौन देगा ? आखिर इन लोगों को कुछ अतिरिक्त आय होती ही होगी जो इतने तोहफे दे रहे हें वरना तंगी के दिनों में कौन इतनी हिम्मत करता ? मैंने पत्नी की कद्र की और डाकबँगले के बिल के भुगतान का भार भी अपने एक नायब पर ही छोड़ दिया। और हाँ, डाकबँगले की चम्मचें बहुत बढ़िया थीं : खानसामा की निगाह बचाकर हम लोग दो अदद चम्मच भी उठा लाए। वैदिकी हिंसा न भवति। मैं तो खैर एक ही चम्मच से संतुष्ट था पर पत्नी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहा कि लेना है तो जोड़ी ही लो; अकेली चम्मच को विरह सताएगा।
हम लोगों के वापसी टिकट भी वहीं के लोगों ने खरीदे। लौटते वक्त शानदार विदाई दी गई। बेवकूफ होने के नाते मैं बराबर यही सोचता रहा कि अधीन कर्मचारियों के साथ समाधि तब टूटी, जब कि गाड़ी ने गति ले ली और स्टेशन काफी पीछे छूट गया। मैंने नेत्र खोले। फूलमालाओं और तोहफों के डिब्बों से दबी मेरी पत्नी ने बड़ी मासूममियत के साथ मुझे अरसे बाद देखा और एक निहायत ईमानदार मुसकराहट के साथ पूछा कि हे आर्यपुत्र, तुम दौरे पर हर महीने क्यों नहीं जाते ?
मेरी पहली किताब
किसी ने कहा है कि कवि जो होते हैं वे बनाएँ नहीं जाते, पैदा होते हैं।
खाकसार पर ठीक यही बात लागू होती है। बचपन में मैं जब रोता भी था तो भी
अनुप्रास, द्रवविलंबित छंद और लय का प्रय़ोग करता था। पूत के पाँव पालने
में क्या, उससे पहले ही दीखने प्रारंभ हो गए थे। सच्चाई तो यह है कि मेरे
पाँव दाई ने पैदा होते ही देख लिए थे और उसने लोगों को बताया था कि पूत के
एक नहीं, बल्कि दो पाँव हैं। एक दायाँ पाँव, दूसरा बायाँ पाँव। यह स्थिति
अब तक वैसे ही चली आ रही है। हाईस्कूल पहुँचते-पहुँचते मैंने कोई पचास
कविताएँ लिख ली थीं। जिनमें से कुछ ‘प्रिय-प्रवास’ की
तर्ज़
पर थी और कुछ ‘जयद्रथ-वध’ के अंदाज पर। ये दोनों
पोथियाँ
मैंने स्कूल की लाइब्रेरी से ही चुराई थीं। स्कूल में मेरी काव्य-प्रतिभा
का लोहा लाइब्रेरियन से लेकर ड्रिल मास्टर तक पूरी जगह मानते थे।
इंटरमीडिएट में आते-आते स्थिति यह हो गई कि मेरी कुछ कविताएँ स्थानीय फर्नीचर पत्रिकाओं व कालेज की मैगजीनों में छपने लगीं। मेरे उर्दू-अध्यापक मुझे महाकवि कहने लगे, क्योंकि शुद्ध हिन्दी में होने के कारण मेरी कविताएँ उनकी समझ में नहीं आती थीं और उनका निश्चित मत था कि जिस शायर का कलाम उनकी पकड़ में नहीं आता था, वह जरूर महान् होता था। ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरे उन उर्दू के अध्यापक की मृत्यु केवल पचहत्तर वर्ष की आयु में ही सम्पन्न हो गई थी। शायरी से जो भी वक्त बचता था, वह नियमित रूप से शराब को दिया जाता था। इतना प्रतिभावान नशा करने वाला शराब से लेकर शायरी तक कोई नशा ऐसा नहीं बचा था, जिसे वे नहीं करते थे। भगवान् उनकी आत्मा को शांति दे।
इंटरमीडिएट में आते-आते स्थिति यह हो गई कि मेरी कुछ कविताएँ स्थानीय फर्नीचर पत्रिकाओं व कालेज की मैगजीनों में छपने लगीं। मेरे उर्दू-अध्यापक मुझे महाकवि कहने लगे, क्योंकि शुद्ध हिन्दी में होने के कारण मेरी कविताएँ उनकी समझ में नहीं आती थीं और उनका निश्चित मत था कि जिस शायर का कलाम उनकी पकड़ में नहीं आता था, वह जरूर महान् होता था। ज्यादा शराब पीने की वजह से मेरे उन उर्दू के अध्यापक की मृत्यु केवल पचहत्तर वर्ष की आयु में ही सम्पन्न हो गई थी। शायरी से जो भी वक्त बचता था, वह नियमित रूप से शराब को दिया जाता था। इतना प्रतिभावान नशा करने वाला शराब से लेकर शायरी तक कोई नशा ऐसा नहीं बचा था, जिसे वे नहीं करते थे। भगवान् उनकी आत्मा को शांति दे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book