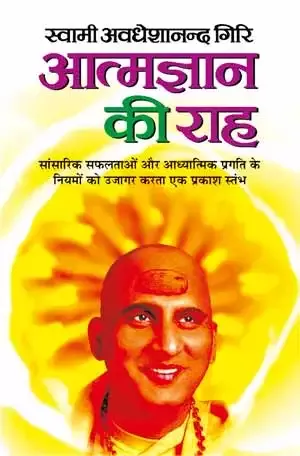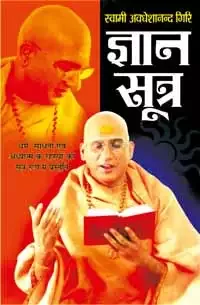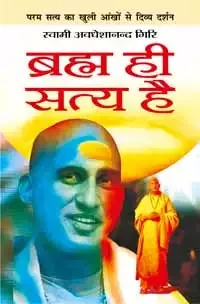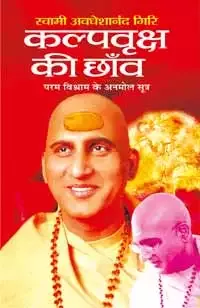|
धर्म एवं दर्शन >> आत्मज्ञान की राह आत्मज्ञान की राहस्वामी अवधेशानन्द गिरि
|
170 पाठक हैं |
||||||
आत्मज्ञान की राह
Atmagyan Ki Rah - A Hindi Book - by Swami Avdheshanand Giri
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सभी की मंजिल एक है, राहें जरूर अलग-अलग हैं— यह वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन कुछ अनुभवी संतों का कहना है कि ऐसा अधिकारी भेद से कहा-सुना जाता है, क्योंकि अध्यात्म के अनुभव सभी को एक से होते हैं। इसके अनुसार यह भिन्नता बिल्कुल ऐसी ही है, जैसे ज्योति का प्रकाश विभिन्न रंग के कांच से अलग-अलग दिखाई देता है। इस प्रकार जो दिख रहा है, वह भी सत्य है—व्यावहारिक सत्य और जो सभी में एक-सा है—वह भी सत्य है अर्थात् पारमार्थिक सत्य।
जब कभी भी साधनों की अनेकता के बारे में भ्रमित हों तो ध्यान रखें कि विभिन्न महापुरुषों द्वारा बताए गए सत्य में कोई भिन्नता नहीं है। लक्ष्य के रूप में ही नहीं, यात्रा की आंतरिक प्रक्रिया के रूप में भी अभेद है।
जब कभी भी साधनों की अनेकता के बारे में भ्रमित हों तो ध्यान रखें कि विभिन्न महापुरुषों द्वारा बताए गए सत्य में कोई भिन्नता नहीं है। लक्ष्य के रूप में ही नहीं, यात्रा की आंतरिक प्रक्रिया के रूप में भी अभेद है।
1
आंतरिक शून्यता ही है परम सिद्धि
किसी समय महर्षि रमण से पश्चिमी विचारक पॉल बर्टन ने पूछा था, ‘मनुष्य की महत्वाकांक्षा की जड़ क्या है ?’ महर्षि रमण हंस कर बोले, ‘हीनता का भाव।’ बात थोड़ी अटपटी-सी लगती है। हीनता का भाव और महत्वाकांक्षी चेतना परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे वस्तुतः विरोधी हैं नहीं। बल्कि एक ही भावदशा के दो छोर हैं। एक छोर से जो हीनता है, वही दूसरे छोर से महत्वाकांक्षा है। हीनता स्वयं से छुटकारा पाने की कोशिश में महत्वाकांक्षा बन जाती है। इसे सुसज्जित हीनता कहना भी गलत नहीं है। हालांकि बहुमूल्य से बहुमूल्य साज-सज्जा के बावजूद न तो वह मिटती है और न नष्ट होती है थोड़ी देर के लिए यह हो सकता है कि दूसरों की दृष्टि से वह छिप जाए लेकिन अपने आपको लगातार उसके दर्शन होते रहते हैं। वस्तुतः जब भी किसी जीवन-समस्या को गलत ढंग से पकड़ा जाता है, तो परिणाम यही होता है।
इस संबंध में एक सच्चाई और भी है। व्यक्ति जब अपनी असलियत से भागना चाहता है, तो उसे किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षा का बुखार जकड़ ही लेता है। अपने आपसे अन्य होने की चाहत में वह स्वयं जैसा है, उसे ढकता है, लेकिन किसी तथ्य का ढक जाना और उससे मुक्त हो जाना एक बात नहीं है। हीनता की विस्मृति, हीनता का विसर्जन नहीं है। यह तो बहुत अविवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इसीलिए ज्यों-ज्यों दवा दी जाती है, त्यों-त्यों रोग बढ़ता है। महत्वाकांक्षी मन की प्रत्येक सफलता आत्मघाती है, क्योंकि वह अग्नि में घृत का काम करती है, सफलता तो आ जाती है, पर हीनता नहीं मिटती, इसीलिए और बड़ी सफलताएं जरूर लगने लगती हैं। इतिहास ऐसे ही बीमार लोगों से भरा पड़ा है। प्रायः सभी इस रोग से संक्रमति हैं।
महत्वादांक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वह विध्वंस, हिंसा, रुग्ण चित्त से निकली घृणा और ईर्ष्या है। मनुष्य-मनुष्य के बीच सांसारिक संघर्ष यही तो है। युद्ध इसी का व्यापक रूप है। यह सांसारिक होती है, तो इससे पर-हिंसा जन्म लेती है। यदि यह आध्यात्मिक है तो आत्महिंसा पर उतारू हो जाती है। अध्यात्म कहीं कुछ पाने की लालसा नहीं, बल्कि स्वयं को सही ढंग से जानने-पहचानने का विज्ञान है। यह सृजनात्मक चेतना में ही संभव है और केवल यही चेतना सृजनात्मक हो सकती है, जो महत्वाकांक्षा हो सकती है। स्वस्थ चित्त केन्द्रीय अभाव है, जिससे सारी हीनताओं का आविर्भाव होता है। आत्मज्ञानी के अतिरिक्त इस अभाव से और कोई मुक्त नहीं है। व्यक्ति के लिए चित्त से सभी महत्वाकांक्षाओं की विदाई अत्यंत आवश्यक है। इनके रहते तो जीवन की दशा और दिशा औंधी और उलटी ही रहेगी।
मनुष्य जब स्वयं में किसी भी तरह की हीनता पाकर उससे भागने लगता है, तो उसकी दिशा अपने आप से विपरीत हो जाती है। वह इस विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ने लगती है। बस यही भूल जाती है। मनोवैज्ञानिक एच. गिब्सन ने अपने शोध पत्र ‘एबीशनः एन इंटरोगेशन टु हेल्थ’ में इस भूल का खुलासा किया है। उनका निष्कर्ष है कि सब हीनताएं गहरे आंतरिक अभाव की सूचनाओं के अतिरिक्त रिक्तता को बाह्य उपलब्धियों से भरने की कोशिश चलती रहती है।
भला आंतरिक रिक्तता के गड्ढे को बाहरी उपलब्धियों से भरना कैसे संभव है, क्योंकि जो बाह्य है। धन, पद और भी ऐसी बहुत-सी चीजें बाहरी ही हैं। पूछा जा सकता है, तब आंतरिक क्या है ? उस अभाव, शून्यता को छोड़कर कुछ भी आंतरिक नहीं। उससे भागना स्वयं से भागना है। उससे पलायन स्वयं की सत्ता से पलायन है। उससे भागने से नहीं, वरन् उसमें जीने और जागने में ही कल्याण है। जो व्यक्ति उसमें जीने और जागने का साहस करता है, उसके समक्ष यह शून्य ही पूर्ण बन जाता है। इसके लिए वह रिक्तता ही परम मुक्ति सिद्ध होती है। वह सत्ता ही परमात्मा है, जिसकी एक झलक में ही सभी अभाव पूरे हो जाते हैं, सभी हीनताएं विलीन हो जाती हैं।
इस संबंध में एक सच्चाई और भी है। व्यक्ति जब अपनी असलियत से भागना चाहता है, तो उसे किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षा का बुखार जकड़ ही लेता है। अपने आपसे अन्य होने की चाहत में वह स्वयं जैसा है, उसे ढकता है, लेकिन किसी तथ्य का ढक जाना और उससे मुक्त हो जाना एक बात नहीं है। हीनता की विस्मृति, हीनता का विसर्जन नहीं है। यह तो बहुत अविवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इसीलिए ज्यों-ज्यों दवा दी जाती है, त्यों-त्यों रोग बढ़ता है। महत्वाकांक्षी मन की प्रत्येक सफलता आत्मघाती है, क्योंकि वह अग्नि में घृत का काम करती है, सफलता तो आ जाती है, पर हीनता नहीं मिटती, इसीलिए और बड़ी सफलताएं जरूर लगने लगती हैं। इतिहास ऐसे ही बीमार लोगों से भरा पड़ा है। प्रायः सभी इस रोग से संक्रमति हैं।
महत्वादांक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वह विध्वंस, हिंसा, रुग्ण चित्त से निकली घृणा और ईर्ष्या है। मनुष्य-मनुष्य के बीच सांसारिक संघर्ष यही तो है। युद्ध इसी का व्यापक रूप है। यह सांसारिक होती है, तो इससे पर-हिंसा जन्म लेती है। यदि यह आध्यात्मिक है तो आत्महिंसा पर उतारू हो जाती है। अध्यात्म कहीं कुछ पाने की लालसा नहीं, बल्कि स्वयं को सही ढंग से जानने-पहचानने का विज्ञान है। यह सृजनात्मक चेतना में ही संभव है और केवल यही चेतना सृजनात्मक हो सकती है, जो महत्वाकांक्षा हो सकती है। स्वस्थ चित्त केन्द्रीय अभाव है, जिससे सारी हीनताओं का आविर्भाव होता है। आत्मज्ञानी के अतिरिक्त इस अभाव से और कोई मुक्त नहीं है। व्यक्ति के लिए चित्त से सभी महत्वाकांक्षाओं की विदाई अत्यंत आवश्यक है। इनके रहते तो जीवन की दशा और दिशा औंधी और उलटी ही रहेगी।
मनुष्य जब स्वयं में किसी भी तरह की हीनता पाकर उससे भागने लगता है, तो उसकी दिशा अपने आप से विपरीत हो जाती है। वह इस विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ने लगती है। बस यही भूल जाती है। मनोवैज्ञानिक एच. गिब्सन ने अपने शोध पत्र ‘एबीशनः एन इंटरोगेशन टु हेल्थ’ में इस भूल का खुलासा किया है। उनका निष्कर्ष है कि सब हीनताएं गहरे आंतरिक अभाव की सूचनाओं के अतिरिक्त रिक्तता को बाह्य उपलब्धियों से भरने की कोशिश चलती रहती है।
भला आंतरिक रिक्तता के गड्ढे को बाहरी उपलब्धियों से भरना कैसे संभव है, क्योंकि जो बाह्य है। धन, पद और भी ऐसी बहुत-सी चीजें बाहरी ही हैं। पूछा जा सकता है, तब आंतरिक क्या है ? उस अभाव, शून्यता को छोड़कर कुछ भी आंतरिक नहीं। उससे भागना स्वयं से भागना है। उससे पलायन स्वयं की सत्ता से पलायन है। उससे भागने से नहीं, वरन् उसमें जीने और जागने में ही कल्याण है। जो व्यक्ति उसमें जीने और जागने का साहस करता है, उसके समक्ष यह शून्य ही पूर्ण बन जाता है। इसके लिए वह रिक्तता ही परम मुक्ति सिद्ध होती है। वह सत्ता ही परमात्मा है, जिसकी एक झलक में ही सभी अभाव पूरे हो जाते हैं, सभी हीनताएं विलीन हो जाती हैं।
2
विनम्र बनाने वाला त्याग ही श्रेष्ठ
कहा गया है कि संतोष ही परम धर्म है। पर कई बार देखा जाता है कि कोई भी उतने भर से संतुष्ट नहीं होता, जितना उसे मिलता है। हरेक के मन में अधिक पाने की लालसा रहती है। इस इच्छा के चलते किसी के पास त्याग और दूसरों की भलाई के बारे में कुछ सोचने का वक्त नहीं रहा। आज समाज में दुखों और कष्टों की भरमार इसीलिए है कि कोई भी गिरते हुए को सहारा देने को तैयार नहीं होता। दूसरों की पीड़ा को दूर करना तो दूर, उसके बारे में जानना तक नहीं चाहता है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book