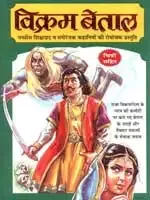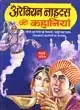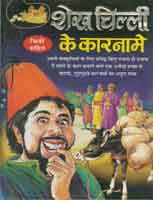|
बाल एवं युवा साहित्य >> विक्रम बेताल विक्रम बेतालधरमपाल बारिया
|
140 पाठक हैं |
||||||
किस्सागोई की अनूठी मिसाल हैं विक्रम-बेताल की ये कहानियां...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
किस्सागोई की अनूठी मिसाल हैं विक्रम-बेताल की ये कहानियां ! ये कहानियां
जहां जिन्दगी के उलझे पहलुओं को सुलझाती हैं, वहीं महाराज विक्रमादित्य की
न्यायप्रियता की ओर भी संकेत करती हैं।
अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए एक योगी विक्रमादित्य को सम्मोहित करता है और उन्हें भेज देता है बेताल पर काबू पाने के लिए। बेताल को काबू कर अपने कंधे पर डाल लेता है विक्रम और चल देता है अपने लक्ष्य की ओर। रास्ते में बेताल एक-एक करके पच्चीस कथाएं सुनाता है और पूछता है कि कौन हैं दोषी। इस तरह रहस्य-रोमांच से भरी हैं ये सभी कहानियां !
कैसी हैं ये कहानियां ? कैसे हैं सवाल और कैसे हैं जवाब ? क्या बेताल को योगी के पास ले जा सका विक्रम ? क्या हुआ योगी की साधना का ? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ें रहस्य-रोमांच से भरी शिक्षाप्रद और मनोरंजन से सराबोर अनूठी कहानियों की इस सचित्र प्रस्तुति को !
अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए एक योगी विक्रमादित्य को सम्मोहित करता है और उन्हें भेज देता है बेताल पर काबू पाने के लिए। बेताल को काबू कर अपने कंधे पर डाल लेता है विक्रम और चल देता है अपने लक्ष्य की ओर। रास्ते में बेताल एक-एक करके पच्चीस कथाएं सुनाता है और पूछता है कि कौन हैं दोषी। इस तरह रहस्य-रोमांच से भरी हैं ये सभी कहानियां !
कैसी हैं ये कहानियां ? कैसे हैं सवाल और कैसे हैं जवाब ? क्या बेताल को योगी के पास ले जा सका विक्रम ? क्या हुआ योगी की साधना का ? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ें रहस्य-रोमांच से भरी शिक्षाप्रद और मनोरंजन से सराबोर अनूठी कहानियों की इस सचित्र प्रस्तुति को !
कौन था सम्राट विक्रमादित्य
‘कथा सरित सागर’ ‘सोमदेव’ द्वारा
संस्कृत भाषा
में लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वास्तव में यह कहना अधिक उचित होगा कि
‘वृहत् कथा’, जो कि ‘बड़ कहा’ का
अनुवाद है, के
आधार पर ‘सोमदेव’ ने ‘कथा सागर’
का पुनर्लेखन
किया। ‘बड़ कहा’ ‘गुणाढ्य’
द्वारा पौशाची प्राकृत
भाषा में लिखी गई थी। ‘गुणाढ्य’ आंध्रवंश के राजा
सातवाहन के
दरबार में मंत्री थे (495 ईं.पू.)। ‘गुणाढ्य’ के बारे
में ऐसा
कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक ‘बड़ा कहा’ में
सात
वर्षों में सात लाख छन्दों की रचना की थी। सबसे पहले इस पुस्तक का अनुवाद
‘वहत् कथा’ के रूप में संस्कृत भाषा में राजा
दुर्विनीत
द्वारा किया गया; परन्तु दुर्भाग्यवश ‘बड़ा कहा’ और
‘वृहत् कथा’ दोनों में से अब एक भी उपलब्ध नहीं है।
‘सोमदेव’, जो कि कश्मीर के राजा अनंत देव के समकालीन (1029-1064 ई.) थे, ने ‘वृहत् कथा’ को संस्कृत भाषा में ‘कथा सरित सागर’ के नाम से पुनः लिखा, इसमें 21, 388 छन्द्र हैं। ‘वेताल पंचिविंशति’ या ‘बेताल पच्चीसी’ और ‘सिंहासन द्वत्रिंशिका’ या ‘सिंहासन बत्तीसी’ ‘कथा सरित सागर’ के ही दो भाग हैं। ‘बेताल पच्चीसी’ में कवि ने बेताल द्वारा राजा विक्रमादित्य को पच्चीस अर्थपूर्ण कहानियां सुनवाईं हैं और ‘सिंहासन बत्तीसी’ में कवि ने बत्तीस पुतलियों द्वारा एक-एक करके बत्तीस कहानियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य का विस्तारपूर्वक परिचय करवाया है।
तत्पश्चात् काफी समय के उपरान्त जब लोगों के मन में ‘कथा सरित सागर’ के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब मुहम्मद शाह, जो एक मुगल शासक था, ने सवाई राजा जय सिंह के दरबार में एक दरबारी कवि ‘सोरठ’ द्वारा ब्रज भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद करवाया। इसके बाद इस रचना को अधिक सरल बनाने में योगदान रहा कैप्टन मार्ट का। तारिनीचरण मिश्र के सहयोग से इस रचना को और अधिक सरल तथा ग्राह्य रूप दे कर कैप्टन मार्ट ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान बंगाल के स्कूलों में इसका परिचय करवाया। इस पुस्तक में वैताल द्वारा सम्राट विक्रमादित्य को सुनाई गई पच्चीस कथाओं का संकलन है। सम्राट विक्रमादित्य कौन था तथा इतिहास में उसका क्या स्थान था, यह आज भी विवाद का विषय है। कारण है सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्य आदि उपलब्ध न होना। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्राट ने कहीं न कहीं इतिहास में अपना योगदान अवश्य दिया है। इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में लगभग बारह विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने किसी प्रकार के सफल अभियान के बाद ‘सम्राट विक्रमादित्य’ की पदवी ग्रहण कर ली। यहां तक कि चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य (ई. 375-415) ने भी गुजरात तथा काठियावाड़ा की महान विजय के पश्चात् यह पदवी ग्रहण की। यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित ‘नवरत्न’ थे —1. कालिदास, 2. धनवन्तरि, 3. क्षपणक, 4. अमर सिंह. 5. शंकु, 6. घटकर्पर, 7. वाराहमिहिर, 8. वररुचि और 9. वैताल भट्ट।
‘वैताल भट्ट’, जो कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ‘विक्रमादित्य’ के नवरत्नों में से एक थे, का ‘बेताल’, जिसे ‘वैताल पंचविंशति’ में प्रेत के रूप में दर्शाया गया है, से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि ‘बड़ कहा’ की रचना क्राइस्ट के जन्म से कुछ शताब्दी पूर्व की है जबकि ‘वैताल भट्ट’ का जन्म क्राइस्ट के जन्म से कुछ शताब्दी बाद में हुआ था। इसी प्रकार ‘वेताल पंचविंशति’ के विक्रमादित्य से भी चन्द्रगुप्त द्वीतीय विक्रमादित्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यह कहना तर्कसंगत होगा कि जिन्होंने भी ‘विक्रमादित्य’ की पदवी ग्रहण की, उन्होंने ऐसा केवल अपनी सफलताओं को मान्यता देने तथा ‘विक्रमादित्य’ की महानता का अनुसरण करने के लिए किया। इसका यह अर्थ हुआ कि ये सभी सम्राट ‘विक्रमादित्य’ से अत्यन्त प्रभावित थे और यह भी हुआ कि पुस्तक में नायक की भूमिक निभाने वाले सम्राट विक्रमादित्य का जन्म बहुत समय पहले हुआ था तथा उसका समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त (द्वीतीय) विक्रमादित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता का प्रमाण नहीं मिला है, विक्रमादित्य का काल्पनिक कथाओं में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्थान है।
कुछ कहानीकारों ने इस सम्बन्ध में प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर रचनाएं की हैं। इस सम्बन्ध में एक रुचिकर कहानी कुछ इस प्रकार है—
किसी गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह अपने साथियों के संग अपनी भेड़ें चराने चरागाह जाया करता था। जब भेंड़ें चारागाह में चरने लगतीं तो चारावाह बालक अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता। खेलते समय यह चरवाहा बालक प्रतिदिनम मिट्टी के एक टीले पर बैठ जाता तथा अपने को राजा कहने लगता। उसके मित्रों को भी इस खेल में मजा आता। वे उसकी प्रजा बनकर फरियादें लेकर आते और अपने ‘राजा’ से न्याय की मांग करते। चरवाहा बालक भी किसी राजा की भांति ही अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सुनाता। धीरे-धीरे गांववासियों को भी इस मेधावी बालक की प्रतिभा का पता चला। जब भी उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद होता, जिसका निपटारा वे स्वयं नहीं कर पाते, वे उस विवाह को लेकर उस चरवाहे बालक के पास न्याय के लिए जाते। चरवाहा बालक उसी मिट्टी के टीले पर बैठकर गांववासियों की समस्या ध्यान से सुनता तथा उस पर अपना निर्णय देता। उसका निर्णय दोनों दलों को मान्य होता तथा वे सन्तुष्ट होकर वापस लौटते।
धीरे-धीरे यह बात आग की भांति चारों ओर फैल गई तथा उस समय के शासक राजा भोज देव को भी इसकी सूचना मिली। उसने उस चरवाये बालक को राजदरबार में बुलाकर उसकी न्याय प्रतिभा की परीक्षा की तथा इस निर्णय पर पहुंचा कि वह एक साधारण बालक के समान ही था।
‘‘मैंने तो तुम्हारी न्याय प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ सुना था परन्तु तुम तो एक साधारण बालक निकले,’’ राजा भोज देव ने कहा राजा भोज देव की बात सुनकर चरवाहा बालक बोला, ‘‘महाराज, मैं एक अशिक्षित साधारण बालक ही हूं। परन्तु महाराज आपके राज्य के उत्तर-पश्चिम सूबे के पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का एक टीला है। जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो न्याय प्रतिभा स्वयं ही मुझमें आने लगती है। मैं स्वयं को राजा अनुभव करने लगता हूं।’’
राजा भोज देव को बालक की बातों का अर्थ समझते देर नहीं लगी। उसने उस बालक से वह मिट्टी का टीला दिखाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उसने चरवाहे बालक से मिट्टी के टीले पर बैठने के लिए कहा और उसके सम्मुख एक अत्यन्त पेचीदा मसला निर्णय के लिए रखा। यह एक ऐसा मसला था जिसकी उसने स्वयं कई बार सुनवाई की थी, परन्तु कोई निर्णय देना सम्भव नहीं हो पा रहा था। वह यह देखकर भौचक्का रह गया कि बालक ने उस मसले को बहुत सरल ढंग से सुलझा दिया।
अन्त में राजा भोज देव इस नतीजे पर पहुंचा कि बालक में नहीं बल्कि उस मिट्टी के टीले में ही कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है
अतः उसने अपने मन्त्रियों को उस स्थान की खुदाई करवाने का आदेश जारी किया। तुरन्त मजदूर बुलाए गए। उन्होंने उस स्थान की खुदाई करनी आरम्भ कर दी। एक घंटे की ताबड़-तोड़ खुदाई के बाद एक मजदूर की कुदाल किसी धातु से जा टकरायी। धातु से टकराने की ध्वनि ने राजा भोज देव को चौकन्नाकर दिया, क्योंकि वह स्वयं अपनी निगरानी में उस स्थान की खुदाई करवा रहा था। उसने अपने मन्त्रियों से कहा कि वे मजदूरों को उस स्थान की बहुत धीरे और सावधानीपूर्वक खुदाई करने का आदेश दें। लगभग एक घंटे की खुदाई के बाद उस स्थान से एक भव्य स्वर्ण सिंहासन निकला। राजा भोज देव तो सिंहासन की चकाचौंध को ठगा-सा देखता रह गया। ‘हे भगवान ! जब अभी इस सिंहासन का ऐसा भव्य रूप है तो जब इसे साफ करके चमका दिया जाएगा तब तो इसकी छटा देखते ही बनेगी—’ राजा भोज देव ने सोचा।
सूर्य ढलने वाला था। स्वर्ण सिंहासन को साफ कर चमका दिया गया था। सिंहासन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उसे स्वर्णिम छटा प्रदान कर रही थीं। सिंहासन को अत्यन्त सावधानीपूर्वक राजाभोज देव के दरबार में लाया गया।
सभी दरबारी सिंहासन के इर्द-गिर्द जमा होकर सिंहासन की छटा देखने लगे। सिंहासन सोने का बना हुआ था तथा उसमें विभिन्न आकारों के विभिन्न प्रकार के हीरे-जवाहरात जड़े हुए थे। सभी दरबारी यह देखकर एक स्वर में बोले कि यह तो इन्द्र देवता का सिंहासन लगता है।
राजा भोज देव ने अपने ज्योतिषियों से कहा कि वे उसके सिंहासनारूढ़ होने का शुभ दिन तथा समय निकालें। ज्योतिषियों ने तारों तथा ग्रहों का अध्ययन कर हिसाब लगाया था अन्ततः यह बताया सम्राट मंगलवार को पूर्णमासी की रात के प्रथम प्रहर में सिंहासन पर बैठें।
अब राजा भोज देव बहुत बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। पूर्णमासी की रात के प्रथम प्रहर में पूजा तथा यज्ञ कर राजा स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए अग्रसर हुआ, परन्तु उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने नारी स्वर में एक साथ कुछ स्त्रियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनी। सम्राट ने मुड़करर राजदरबार में उपस्थित लोगों पर नजर डाली। प्रत्येक चकित था।
राजा भोज देव ने आगे बढ़कर स्वर्ण सिंहासन का नजदीक से मुआयाना किया और जो कुछ उसने देखा उस पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़ सकी थी। सिंहासन के दोनों हाथों पर कठपुतलियां बैठी थीं। सम्राट ने गिना, प्रत्येक हत्थे पर सोलह कठपुतलियां थीं। इसके पश्चात् सम्राट ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया, खनकती हुई हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार सम्राट सिंहासन के बहुत निकट पहुंच चुका था। उसने कठपुतलियों को हिलते-डुलते तथा खिलखिलाते देखा तो आतंकित हो उठा। उसने कहा, ‘‘तुम सब कौन हो ? क्यों हंस रही हो ? तुम सब नहीं जानतीं कि मैं राजा भोज देव हूं ? मुझे देखकर हंसना अपराध है। तुम्हारी हंसी में तिरस्कार है। चाहूं तो तुम सबको दंड दे सकता हूं।’’
‘‘नहीं, महाराज नहीं। कृपया आप ऐसा न सोचें। हमने आपका कभी अनादर नहीं करना चाहा। हां, हम आपको एक बात जरूर स्पष्ट रूप से बताना चाहती हैं कि इस सिंहासन पर, जो कभी हमारे सम्राट विक्रमादित्य का था, आप बैठने के अधिकारी नहीं है।’’ दाएं हत्थे पर बैठी प्रथम कठपुतली ने कहा।
राजा भोज देव पर कठपुतली की बात वज्र के समान गिरी। उसने अपने को सम्भालते हुए कहा, ‘‘मैं तुम्हारी बात सुनकर सचमुच विस्मित हूं। परन्तु इससे पहले कि तुम मुझे महान सम्राट् विक्रमादित्य के विषय में विस्तार से बताओ, मैं तुम सबका परिचय चाहता हूं।’’
‘‘अवश्य महाराज ! मेरा नाम मंजरी है। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें।’’
उसके पश्चात् उसने धीरे-धीरे अन्य कठपुतलियों का भी परिचय करवाया, जिनके नाम थे—
1. मंजरी, 2. चित्ररेखा, 3. रतिभामा, 4. चन्द्रकला, 5. लीलावती, 6. काम कंदला, 7. कामदा, 8. पुष्पावती, 9. मधुमालती, 10. प्रेमावती, 11. पद्मावती, 12. कीर्तिमती, 13. त्रिलोचनी, 14. रुद्रावती, 15. अनूपवती, 16. सुन्दरवती, 18 सत्यवती, 19. तारा, 20, चन्द्रज्योति, 21. अनुराधा, 22. अनूपरेखा, 23 करूपावती, 24 चित्रकला, 25. जयलक्ष्मी, 26. विद्यावती, 27 जगज्योति, 28. मनमोहिनी, 29. वैदेही, 30. रूपवती, 31. कौशल्या और 32. मैनावती।
सभी कठपुतलियों का परिचय करवाने के पश्चात् मंजरी ने राजा भोज देव से सम्राट विक्रमादित्य की कथा सुनने का आग्रह किया—
‘‘महाराज, धारा नगरी में भर्तृहरि नामक राजा का शासन था। भर्तृहरि एक ऐयाश राजा था। यही कारण था कि उसका भाई विक्रमादित्य राज्य छोड़कर चला गया। अब तो राजा भर्तृहरि पहले से अधिक स्वचन्द हो गया। राजा भर्तृहरि की छः रानियां थीं जिनमें सबसे छोटी थी रानी पिंगला। राजा भर्तृहरि पिंगला से अथाह प्रेम करता था। परन्तु राजा अपनी इन्द्रियों से अत्यधिक विवश होने के कारण रानियों के अतिरिक्त वेश्याओं के पास भी आया-जाया करता था। उन्हीं वेश्याओं में एक थी चित्रसेना, जिसे भर्तृहरि बहुत प्रेम करता था। वह चित्रसेना के प्रेमपाश में ऐसा बंधा हुआ था कि उसने अपने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों पर छोड रखा था तथा उसके साथ दिन-रात रंगरलियां मनाता रहता था।’’
मंजरी ने एक क्षण रुक राजा भोज देव की ओर ध्यान से देखा और उसे तल्लीनता से कहानी सुनता देख आगे बोली, ‘‘समय धीरे-धीरे बीत रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के दरबार में उपस्थिति हुआ। उसने राजा को एक फल देते हुए कहा कि इस फल का सेवन करने वाला दीर्घजीवी तथा निरोगी होगा। राजा भर्तृहरि फल पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, परन्तु उसने फल स्वयं खाने के बजाय रानी पिंगला को दे दिया ताकि पिंगला लम्बे समय तक अपना यौवन कायम रख सके। परन्तु रानी पिंगला भी राजा भर्तृहरि की भांति ऐयाशी का जीवन व्यतीत करती थी तथा चुपुके-चुपके राजा के रथ के चालक से प्रेम करती थी। उसने वह फल रथवान को दे दिया। रथ चालक ने उस फल को चित्रसेना को भेंट कर दिया—वह भी भर्तृहरि की भांति चित्रसेना के पास लुक-छिपकर जाया करता था।
चित्रसेना थी तो वेश्या किंतु उसके मन में अपने निकृष्ट जीवन से घृणा थी। उसका मानना था कि समाज और देश के लिए उसका जीवन व्यर्थ है। अतः अपने अन्तःकरण के धिक्कारने पर उसने वह फल राजा को यह सोचकर दिया कि राजा भर्तृहरि उस फल का सेवन कर लम्बे समय तक युवा एवं नीरोगी रहेगा तथा देश की अधिकाधिक सेवा कर सकेगा। परन्तु उसे उस समय घोर आश्चर्य हुआ जब राजा भर्तृहरि उस फल को उसके पास देखते ही क्रोधित हो उठे।
राजा भर्तृहरि ने चित्रसेना के पास फल होने के कारणों की जांच करवाई और जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसने चित्रसेना तथा रथचालक दोनों को अपने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। परन्तु इन सभी घटनाओं से उसको भारी आघात पहुंचा और उसने संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया।
जब विक्रमादित्य को भर्तृहरि के संन्यास लेने की सूचना मिली तो वह तुरन्त वापस लौट आया विक्रमादित्य को राज्य की कोई लालसा नहीं थी। उसने तो राज्य की बाग़डोर केवल इसलिए सम्भाली कि कहीं राजा की अनुपस्थिति में प्रजा विद्रोह न कर दे या शत्रु आक्रमण न करे दे।
चूंकि राजा विक्रमादित्य अपने भाई के समान स्वभाव वाला नहीं था तथा ऐसे कार्यों से बहुत दूर रहता था जो निकृष्ट या अनैतिक समझे जाते हों, इसीलिए शीघ्र ही वह मन्त्रियों तथा अपनी प्रजा में लोकप्रिय हो गया। राजा विक्रमादित्य अपनी निष्पक्षता तथा न्याय-विवेक के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में देश की बहुत उन्नति हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उसकी विशेष रूप से रचना की थी। यही कारण था कि उसके शासनकाल में कभी देश पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आईं—जैसे सूखा या बाढ़ आदि। देश की जनता सुखी थी। राजा ने ऐसा प्रबन्ध कर रखा था कि राज्य में दूध मक्खन तथा अनाज की कोई कमी नहीं थी। राज्य का गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखा नहीं रहता था।
‘सोमदेव’, जो कि कश्मीर के राजा अनंत देव के समकालीन (1029-1064 ई.) थे, ने ‘वृहत् कथा’ को संस्कृत भाषा में ‘कथा सरित सागर’ के नाम से पुनः लिखा, इसमें 21, 388 छन्द्र हैं। ‘वेताल पंचिविंशति’ या ‘बेताल पच्चीसी’ और ‘सिंहासन द्वत्रिंशिका’ या ‘सिंहासन बत्तीसी’ ‘कथा सरित सागर’ के ही दो भाग हैं। ‘बेताल पच्चीसी’ में कवि ने बेताल द्वारा राजा विक्रमादित्य को पच्चीस अर्थपूर्ण कहानियां सुनवाईं हैं और ‘सिंहासन बत्तीसी’ में कवि ने बत्तीस पुतलियों द्वारा एक-एक करके बत्तीस कहानियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य का विस्तारपूर्वक परिचय करवाया है।
तत्पश्चात् काफी समय के उपरान्त जब लोगों के मन में ‘कथा सरित सागर’ के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब मुहम्मद शाह, जो एक मुगल शासक था, ने सवाई राजा जय सिंह के दरबार में एक दरबारी कवि ‘सोरठ’ द्वारा ब्रज भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद करवाया। इसके बाद इस रचना को अधिक सरल बनाने में योगदान रहा कैप्टन मार्ट का। तारिनीचरण मिश्र के सहयोग से इस रचना को और अधिक सरल तथा ग्राह्य रूप दे कर कैप्टन मार्ट ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान बंगाल के स्कूलों में इसका परिचय करवाया। इस पुस्तक में वैताल द्वारा सम्राट विक्रमादित्य को सुनाई गई पच्चीस कथाओं का संकलन है। सम्राट विक्रमादित्य कौन था तथा इतिहास में उसका क्या स्थान था, यह आज भी विवाद का विषय है। कारण है सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के लिए कोई ऐतिहासिक तथ्य आदि उपलब्ध न होना। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्राट ने कहीं न कहीं इतिहास में अपना योगदान अवश्य दिया है। इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में लगभग बारह विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने किसी प्रकार के सफल अभियान के बाद ‘सम्राट विक्रमादित्य’ की पदवी ग्रहण कर ली। यहां तक कि चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य (ई. 375-415) ने भी गुजरात तथा काठियावाड़ा की महान विजय के पश्चात् यह पदवी ग्रहण की। यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित ‘नवरत्न’ थे —1. कालिदास, 2. धनवन्तरि, 3. क्षपणक, 4. अमर सिंह. 5. शंकु, 6. घटकर्पर, 7. वाराहमिहिर, 8. वररुचि और 9. वैताल भट्ट।
‘वैताल भट्ट’, जो कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ‘विक्रमादित्य’ के नवरत्नों में से एक थे, का ‘बेताल’, जिसे ‘वैताल पंचविंशति’ में प्रेत के रूप में दर्शाया गया है, से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि ‘बड़ कहा’ की रचना क्राइस्ट के जन्म से कुछ शताब्दी पूर्व की है जबकि ‘वैताल भट्ट’ का जन्म क्राइस्ट के जन्म से कुछ शताब्दी बाद में हुआ था। इसी प्रकार ‘वेताल पंचविंशति’ के विक्रमादित्य से भी चन्द्रगुप्त द्वीतीय विक्रमादित्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी यह कहना तर्कसंगत होगा कि जिन्होंने भी ‘विक्रमादित्य’ की पदवी ग्रहण की, उन्होंने ऐसा केवल अपनी सफलताओं को मान्यता देने तथा ‘विक्रमादित्य’ की महानता का अनुसरण करने के लिए किया। इसका यह अर्थ हुआ कि ये सभी सम्राट ‘विक्रमादित्य’ से अत्यन्त प्रभावित थे और यह भी हुआ कि पुस्तक में नायक की भूमिक निभाने वाले सम्राट विक्रमादित्य का जन्म बहुत समय पहले हुआ था तथा उसका समुद्रगुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त (द्वीतीय) विक्रमादित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता का प्रमाण नहीं मिला है, विक्रमादित्य का काल्पनिक कथाओं में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्थान है।
कुछ कहानीकारों ने इस सम्बन्ध में प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर रचनाएं की हैं। इस सम्बन्ध में एक रुचिकर कहानी कुछ इस प्रकार है—
किसी गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह अपने साथियों के संग अपनी भेड़ें चराने चरागाह जाया करता था। जब भेंड़ें चारागाह में चरने लगतीं तो चारावाह बालक अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता। खेलते समय यह चरवाहा बालक प्रतिदिनम मिट्टी के एक टीले पर बैठ जाता तथा अपने को राजा कहने लगता। उसके मित्रों को भी इस खेल में मजा आता। वे उसकी प्रजा बनकर फरियादें लेकर आते और अपने ‘राजा’ से न्याय की मांग करते। चरवाहा बालक भी किसी राजा की भांति ही अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय सुनाता। धीरे-धीरे गांववासियों को भी इस मेधावी बालक की प्रतिभा का पता चला। जब भी उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद होता, जिसका निपटारा वे स्वयं नहीं कर पाते, वे उस विवाह को लेकर उस चरवाहे बालक के पास न्याय के लिए जाते। चरवाहा बालक उसी मिट्टी के टीले पर बैठकर गांववासियों की समस्या ध्यान से सुनता तथा उस पर अपना निर्णय देता। उसका निर्णय दोनों दलों को मान्य होता तथा वे सन्तुष्ट होकर वापस लौटते।
धीरे-धीरे यह बात आग की भांति चारों ओर फैल गई तथा उस समय के शासक राजा भोज देव को भी इसकी सूचना मिली। उसने उस चरवाये बालक को राजदरबार में बुलाकर उसकी न्याय प्रतिभा की परीक्षा की तथा इस निर्णय पर पहुंचा कि वह एक साधारण बालक के समान ही था।
‘‘मैंने तो तुम्हारी न्याय प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ सुना था परन्तु तुम तो एक साधारण बालक निकले,’’ राजा भोज देव ने कहा राजा भोज देव की बात सुनकर चरवाहा बालक बोला, ‘‘महाराज, मैं एक अशिक्षित साधारण बालक ही हूं। परन्तु महाराज आपके राज्य के उत्तर-पश्चिम सूबे के पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का एक टीला है। जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो न्याय प्रतिभा स्वयं ही मुझमें आने लगती है। मैं स्वयं को राजा अनुभव करने लगता हूं।’’
राजा भोज देव को बालक की बातों का अर्थ समझते देर नहीं लगी। उसने उस बालक से वह मिट्टी का टीला दिखाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उसने चरवाहे बालक से मिट्टी के टीले पर बैठने के लिए कहा और उसके सम्मुख एक अत्यन्त पेचीदा मसला निर्णय के लिए रखा। यह एक ऐसा मसला था जिसकी उसने स्वयं कई बार सुनवाई की थी, परन्तु कोई निर्णय देना सम्भव नहीं हो पा रहा था। वह यह देखकर भौचक्का रह गया कि बालक ने उस मसले को बहुत सरल ढंग से सुलझा दिया।
अन्त में राजा भोज देव इस नतीजे पर पहुंचा कि बालक में नहीं बल्कि उस मिट्टी के टीले में ही कोई अदृश्य शक्ति छिपी हुई है
अतः उसने अपने मन्त्रियों को उस स्थान की खुदाई करवाने का आदेश जारी किया। तुरन्त मजदूर बुलाए गए। उन्होंने उस स्थान की खुदाई करनी आरम्भ कर दी। एक घंटे की ताबड़-तोड़ खुदाई के बाद एक मजदूर की कुदाल किसी धातु से जा टकरायी। धातु से टकराने की ध्वनि ने राजा भोज देव को चौकन्नाकर दिया, क्योंकि वह स्वयं अपनी निगरानी में उस स्थान की खुदाई करवा रहा था। उसने अपने मन्त्रियों से कहा कि वे मजदूरों को उस स्थान की बहुत धीरे और सावधानीपूर्वक खुदाई करने का आदेश दें। लगभग एक घंटे की खुदाई के बाद उस स्थान से एक भव्य स्वर्ण सिंहासन निकला। राजा भोज देव तो सिंहासन की चकाचौंध को ठगा-सा देखता रह गया। ‘हे भगवान ! जब अभी इस सिंहासन का ऐसा भव्य रूप है तो जब इसे साफ करके चमका दिया जाएगा तब तो इसकी छटा देखते ही बनेगी—’ राजा भोज देव ने सोचा।
सूर्य ढलने वाला था। स्वर्ण सिंहासन को साफ कर चमका दिया गया था। सिंहासन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उसे स्वर्णिम छटा प्रदान कर रही थीं। सिंहासन को अत्यन्त सावधानीपूर्वक राजाभोज देव के दरबार में लाया गया।
सभी दरबारी सिंहासन के इर्द-गिर्द जमा होकर सिंहासन की छटा देखने लगे। सिंहासन सोने का बना हुआ था तथा उसमें विभिन्न आकारों के विभिन्न प्रकार के हीरे-जवाहरात जड़े हुए थे। सभी दरबारी यह देखकर एक स्वर में बोले कि यह तो इन्द्र देवता का सिंहासन लगता है।
राजा भोज देव ने अपने ज्योतिषियों से कहा कि वे उसके सिंहासनारूढ़ होने का शुभ दिन तथा समय निकालें। ज्योतिषियों ने तारों तथा ग्रहों का अध्ययन कर हिसाब लगाया था अन्ततः यह बताया सम्राट मंगलवार को पूर्णमासी की रात के प्रथम प्रहर में सिंहासन पर बैठें।
अब राजा भोज देव बहुत बेसब्री से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। पूर्णमासी की रात के प्रथम प्रहर में पूजा तथा यज्ञ कर राजा स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए अग्रसर हुआ, परन्तु उस समय उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने नारी स्वर में एक साथ कुछ स्त्रियों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनी। सम्राट ने मुड़करर राजदरबार में उपस्थित लोगों पर नजर डाली। प्रत्येक चकित था।
राजा भोज देव ने आगे बढ़कर स्वर्ण सिंहासन का नजदीक से मुआयाना किया और जो कुछ उसने देखा उस पर किसी अन्य की दृष्टि नहीं पड़ सकी थी। सिंहासन के दोनों हाथों पर कठपुतलियां बैठी थीं। सम्राट ने गिना, प्रत्येक हत्थे पर सोलह कठपुतलियां थीं। इसके पश्चात् सम्राट ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया, खनकती हुई हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार सम्राट सिंहासन के बहुत निकट पहुंच चुका था। उसने कठपुतलियों को हिलते-डुलते तथा खिलखिलाते देखा तो आतंकित हो उठा। उसने कहा, ‘‘तुम सब कौन हो ? क्यों हंस रही हो ? तुम सब नहीं जानतीं कि मैं राजा भोज देव हूं ? मुझे देखकर हंसना अपराध है। तुम्हारी हंसी में तिरस्कार है। चाहूं तो तुम सबको दंड दे सकता हूं।’’
‘‘नहीं, महाराज नहीं। कृपया आप ऐसा न सोचें। हमने आपका कभी अनादर नहीं करना चाहा। हां, हम आपको एक बात जरूर स्पष्ट रूप से बताना चाहती हैं कि इस सिंहासन पर, जो कभी हमारे सम्राट विक्रमादित्य का था, आप बैठने के अधिकारी नहीं है।’’ दाएं हत्थे पर बैठी प्रथम कठपुतली ने कहा।
राजा भोज देव पर कठपुतली की बात वज्र के समान गिरी। उसने अपने को सम्भालते हुए कहा, ‘‘मैं तुम्हारी बात सुनकर सचमुच विस्मित हूं। परन्तु इससे पहले कि तुम मुझे महान सम्राट् विक्रमादित्य के विषय में विस्तार से बताओ, मैं तुम सबका परिचय चाहता हूं।’’
‘‘अवश्य महाराज ! मेरा नाम मंजरी है। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें।’’
उसके पश्चात् उसने धीरे-धीरे अन्य कठपुतलियों का भी परिचय करवाया, जिनके नाम थे—
1. मंजरी, 2. चित्ररेखा, 3. रतिभामा, 4. चन्द्रकला, 5. लीलावती, 6. काम कंदला, 7. कामदा, 8. पुष्पावती, 9. मधुमालती, 10. प्रेमावती, 11. पद्मावती, 12. कीर्तिमती, 13. त्रिलोचनी, 14. रुद्रावती, 15. अनूपवती, 16. सुन्दरवती, 18 सत्यवती, 19. तारा, 20, चन्द्रज्योति, 21. अनुराधा, 22. अनूपरेखा, 23 करूपावती, 24 चित्रकला, 25. जयलक्ष्मी, 26. विद्यावती, 27 जगज्योति, 28. मनमोहिनी, 29. वैदेही, 30. रूपवती, 31. कौशल्या और 32. मैनावती।
सभी कठपुतलियों का परिचय करवाने के पश्चात् मंजरी ने राजा भोज देव से सम्राट विक्रमादित्य की कथा सुनने का आग्रह किया—
‘‘महाराज, धारा नगरी में भर्तृहरि नामक राजा का शासन था। भर्तृहरि एक ऐयाश राजा था। यही कारण था कि उसका भाई विक्रमादित्य राज्य छोड़कर चला गया। अब तो राजा भर्तृहरि पहले से अधिक स्वचन्द हो गया। राजा भर्तृहरि की छः रानियां थीं जिनमें सबसे छोटी थी रानी पिंगला। राजा भर्तृहरि पिंगला से अथाह प्रेम करता था। परन्तु राजा अपनी इन्द्रियों से अत्यधिक विवश होने के कारण रानियों के अतिरिक्त वेश्याओं के पास भी आया-जाया करता था। उन्हीं वेश्याओं में एक थी चित्रसेना, जिसे भर्तृहरि बहुत प्रेम करता था। वह चित्रसेना के प्रेमपाश में ऐसा बंधा हुआ था कि उसने अपने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों पर छोड रखा था तथा उसके साथ दिन-रात रंगरलियां मनाता रहता था।’’
मंजरी ने एक क्षण रुक राजा भोज देव की ओर ध्यान से देखा और उसे तल्लीनता से कहानी सुनता देख आगे बोली, ‘‘समय धीरे-धीरे बीत रहा था। एक दिन एक ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के दरबार में उपस्थिति हुआ। उसने राजा को एक फल देते हुए कहा कि इस फल का सेवन करने वाला दीर्घजीवी तथा निरोगी होगा। राजा भर्तृहरि फल पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, परन्तु उसने फल स्वयं खाने के बजाय रानी पिंगला को दे दिया ताकि पिंगला लम्बे समय तक अपना यौवन कायम रख सके। परन्तु रानी पिंगला भी राजा भर्तृहरि की भांति ऐयाशी का जीवन व्यतीत करती थी तथा चुपुके-चुपके राजा के रथ के चालक से प्रेम करती थी। उसने वह फल रथवान को दे दिया। रथ चालक ने उस फल को चित्रसेना को भेंट कर दिया—वह भी भर्तृहरि की भांति चित्रसेना के पास लुक-छिपकर जाया करता था।
चित्रसेना थी तो वेश्या किंतु उसके मन में अपने निकृष्ट जीवन से घृणा थी। उसका मानना था कि समाज और देश के लिए उसका जीवन व्यर्थ है। अतः अपने अन्तःकरण के धिक्कारने पर उसने वह फल राजा को यह सोचकर दिया कि राजा भर्तृहरि उस फल का सेवन कर लम्बे समय तक युवा एवं नीरोगी रहेगा तथा देश की अधिकाधिक सेवा कर सकेगा। परन्तु उसे उस समय घोर आश्चर्य हुआ जब राजा भर्तृहरि उस फल को उसके पास देखते ही क्रोधित हो उठे।
राजा भर्तृहरि ने चित्रसेना के पास फल होने के कारणों की जांच करवाई और जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसने चित्रसेना तथा रथचालक दोनों को अपने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। परन्तु इन सभी घटनाओं से उसको भारी आघात पहुंचा और उसने संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया।
जब विक्रमादित्य को भर्तृहरि के संन्यास लेने की सूचना मिली तो वह तुरन्त वापस लौट आया विक्रमादित्य को राज्य की कोई लालसा नहीं थी। उसने तो राज्य की बाग़डोर केवल इसलिए सम्भाली कि कहीं राजा की अनुपस्थिति में प्रजा विद्रोह न कर दे या शत्रु आक्रमण न करे दे।
चूंकि राजा विक्रमादित्य अपने भाई के समान स्वभाव वाला नहीं था तथा ऐसे कार्यों से बहुत दूर रहता था जो निकृष्ट या अनैतिक समझे जाते हों, इसीलिए शीघ्र ही वह मन्त्रियों तथा अपनी प्रजा में लोकप्रिय हो गया। राजा विक्रमादित्य अपनी निष्पक्षता तथा न्याय-विवेक के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में देश की बहुत उन्नति हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उसकी विशेष रूप से रचना की थी। यही कारण था कि उसके शासनकाल में कभी देश पर प्राकृतिक आपदाएं नहीं आईं—जैसे सूखा या बाढ़ आदि। देश की जनता सुखी थी। राजा ने ऐसा प्रबन्ध कर रखा था कि राज्य में दूध मक्खन तथा अनाज की कोई कमी नहीं थी। राज्य का गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखा नहीं रहता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book