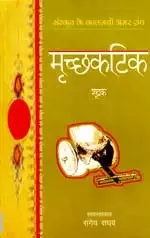|
नाटक-एकाँकी >> मृच्छकटिक मृच्छकटिकशूद्रक
|
110 पाठक हैं |
||||||
महाकवि शूद्रक द्वारा रचित एक यथार्थवादी नाटक...
Mrichchkatik - A Hindi Book - by Shudrak
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मृच्छकटिक का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। आधुनिक साहित्य में भी पुस्तक का ऐसा शीर्षक रखा जाता है। ‘मृच्छकटिक’ संस्कृत नाटक है। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग है, जैसा कि प्रायः संस्कृत के और नाटकों में है। राजा, ब्राह्मण और पढ़े-लिखे लोग संस्कृत बोलते हैं, और स्त्रियां और निचले तबके के लोग प्राकृत। इससे प्रकट होता है कि जब ये नाटक लिखे गए थे तब संस्कृत जनभाषा नहीं थी, ऊँचे तबके के लोगों की भाषा रह गई थी, लेकिन उसे सब लोग आसानी से समझ लेते थे। अगर यह माना जाए कि ये नाटक केवल राजदरबारों में होते थे, तो वहाँ पढ़े-लिखे लोगों में खाली संस्कृत से ही काम चल सकता था। वे फिर प्राकृत का प्रयोग ही न करते। ‘मृच्छकटिक’ एक पुराना नाटक है। बाद के युग में भी कवियों, नाटककारों ने पुरानी परंपरा को ही चलाया।
‘मृच्छकटिक’ को राजा शूद्रक ने लिखा था। वह बड़ा कवि था। कुछ लोग कहते हैं, शूद्रक कोई था ही नहीं, एक कल्पित पात्र है। परन्तु पुराने समय में शूद्रक कोई राजा था इसका उल्लेख हमें स्कन्दपुराण में मिलता है। भास नामक कवि ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम ‘दरिद्र चारुदत्त’ है। ‘दरिद्र चारुदत्त’ भाषा और कला की दृष्टि से ‘मृच्छकटिक’ से पुराना नाटक है। निश्चयपूर्वक शूद्रक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाण ने अपनी ‘कादम्बरी’ में राजा शूद्रक को अपना पात्र बनाया है, पर यह नहीं कहा कि वह कवि भी था। बाण का समय छठी शती है। मेरा मत है कि शूद्रक कोई कवि था, जो राजा भी था। वह बहुत पुराना था। परन्तु कालिदास के समय तक उसे प्रधानता नहीं दी गई थी, या कहें कि जिस कालिदास ने सौमिल्ल, भास और कविपुत्र का नाम अपने से पहले बड़े लेखकों में गिनाया है, उसने सबकी सूची नहीं दी थी। शूद्रक का बनाया नाटक पुराना था, जो निरन्तर सम्पादित होता रहा और बाद में प्रसिद्ध हो गया। हो सकता है वह भास के बाद हुआ हो। भास का समय ईसा की पहली या दूसरी शती माना जाता है। ‘मृच्छकटिक’ में दो कथाएँ हैं। एक चारुदत्त की, दूसरी आर्यक की। गुणाढ्य की बृहत्कथा में गोपाल दारक आर्यक के विद्रोह की कथा है। बृहत्कथा अपने मूल रूप में पैशाची भाषा में ‘बड्डकहा’ के नाम से लिखी गई थी। इससे प्रकट होता है कि यह नाटक ईस्वी पहली शती या दूसरी शती का है।
यह नाटक संस्कृत साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इसमें–
(१) गणिका का प्रेम है। विशुद्ध प्रेम, धन के लिए नहीं; क्योंकि वसंतसेना दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करती है। गणिका कलाएँ जानने वाली ऊँचे दर्जे की वेश्याएँ होती थीं, जिनका समाज में आदर होता था। ग्रीक लोगों में ऐसी ही ‘हितायरा’ हुआ करती थीं।
(२) गणिका गृहस्थी और प्रेम की अधिकारिणी बनती है, वधू बनती है, और कवि उसे समाज के सम्मान्य पुरुष ब्राह्मण चारुदत्त से ब्याहता है। ब्याह कराता है, रखैल नहीं बनाता। स्त्री-विद्रोह के प्रति कवि की सहानुभूति है। पाँचवें अंक में ही चारुदत्त और वसंतसेना मिल जाते हैं, परन्तु लेखक का उद्देश्य वहीं पूरा नहीं होता। वह दसवें अंक तक कथा बढ़ाकर राजा की सम्मति दिलवाकर प्रेमपात्र नहीं, विवाह कराता है। वसंतसेना अन्तःपुर में पहुँचना चाहती है और पहुँच जाती है। लेखक ने इरादतन यह नतीजा अपने सामने रखा है।
(३) इस नाटक में कचहरी में होने वाले पाप और राजकाज की पोल का बड़ा यथार्थवादी चित्रण है, जनता के विद्रोह की कथा है।
(४) इस नाटक का नायक राजा नहीं है, व्यापारी है, जो व्यापारी-वर्ग के उत्थान का प्रतीक है।
ये इसकी विशेषताएँ हैं। राजनीतिक विशेषता यह है कि इसमें क्षत्रिय राजा बुरा बताया गया है। गोप-पुत्र आर्यक–एक ग्वाला है, जिसे कवि राजा बनाता है। यद्यपि कवि वर्णाश्रम को मानता है, पर वह गोप को ही राजा बनाता है। मेरा मत है कि यह मूलकथा पुरानी है और सम्भवतः यह घटना कोई वास्तविक घटना है जो किंवदन्ती में रह गई। दासप्रथा के लड़खड़ाते समाज का चित्रण बहुत सुन्दर हुआ है, और यह हमें चाणक्य के समय में मिलता है, जब ‘आर्य’ शब्द ‘नागरिक’ (Roman Citizen) के रुप में प्रयुक्त मिलता है। हो सकता है, कोई पुरानी किंवदन्ती चाणक्य के बाद के समय में इस कथा में उतर आई हो। बुद्ध के समय में व्यापारियों का उत्कर्ष भी काफी हुआ था। तब उज्जयिनी का राज्य अलग था, कोसल का अलग। यहाँ भी उज्जयिनी का वर्णन है। एक जगह लगता है कि उस समय भी भारत की एकता का आभास था, जब कहा गया है कि सारी पृथ्वी आर्यक ने जीत ली–वह पृथ्वी जिसकी कैलास पताका है।
देखा जाए तो कवि यथार्थवादी था और निष्पक्ष था। उसने सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाई हैं। और बड़ी गहराई से चित्रण किया है। यही उसकी सफलता का कारण है।
‘मृच्छकटिक’ की कथा का स्थान उज्जयिनी है, हमें इसमें चातुर्वर्ण्य का समाज मिलता है–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का मुख्य काम पुरोहिताई था। पर वे राजकाज में भी दिलचस्पी लेते थे और मुझे जो इस कथा में एक बड़ी गम्भीर बात मिलती है वह यह है कि यहाँ ब्राह्मण, व्यापारी और निम्नवर्ण मिलकर मदान्ध क्षत्रिय राज्य को उखाड़ फेंकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। और फिर सोचने की बात यह है कि इस कथा का लेखक राजा शूद्रक माना जाता है जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा गया है। यह क्या प्रकट करता है ? यह तो स्पष्ट ही है कि प्रस्तावना शूद्रक की मौत के बाद लिखी गई है, क्योंकि स्वयं उसके जलकर मरने का वर्णन हमें मिलता है। इसका मतलब है कि यह नाटक लेखक के मरने के बाद प्रसिद्ध हुआ था, पहले नहीं। इससे प्रकट होता है कि नाटक की मूलकथा उस समय की है जब आभीर जैसी विदेशी जाति बाहर से आकर भारत में बस चुकी थी और आभीर और गोप भारत में हिलमिल गए थे। महाभारत से प्रकट होता है कि गोप–ग्वाले भारत में पहले भी थे। श्रीकृष्ण के अन्तिम काल में आभीरों ने आक्रमण किया था। उन्होंने यादवगण जीता था। यादवगण द्वारका की तरफ था। द्वारका गुजरात की ओर थी। ये आभीर उसी तरफ आकर बस गए थे। वहीं आभीर गोपों से मिलमिला गए। इन्हींको बाद में अहीर कहा गया। मैं तो कहता हूँ कि यह गोप शब्द आभीर के लिए आया है, इसका कारण यही है कि गोप तब तक ‘क्षत्रिय’ नहीं माने गए थे। बाद में सम्भवतः मान लिए गए थे, क्योंकि आर्यक के राजा हो जाने के बाद ऐसा हो जाना कठिन नहीं था। मूल क्षत्रिय मदान्ध थे और ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करते थे। यह तो निस्सन्देह सत्य है कि मूल क्षत्रियों के ‘गणतन्त्रवाद’, ‘बाह्मण-विरोधी स्वभाव’ के कारण जनता और प्रायः ब्राह्मणगण–(सिवाय यज्ञ की दक्षिणा लेनेवालों को छोड़कर)–विरुद्ध थे। उन्होंने कई बाहरी जातियों को मान्यता दी थी। ऐसा ही विद्रोह कृष्ण ने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के विरुद्ध गोवर्धन-पूजा करा कर कंस के विरुद्ध किया था। स्पष्ट ही हम गोप-पुत्र आर्यक को राजा बनते देखते हैं और ब्राह्मण शर्विलक उसे राजा बनाने को तख्ता पलटता है। चारुदत्त भी उसका सहायक है। राजा पालक अत्याचारी है। सब उससे अप्रसन्न हैं। आर्यक उसे उखाड़ता है तो उसकी इन्द्र से तुलना की जाती है। वह कुल और मान का रक्षक माना जाता है। वह ब्राह्मणों को अनुष्ठान में लगनेवाली शासन-व्यवस्था स्थापित करता है। शूद्रक सम्भवतः कोई गोप राजा ही था, जिसने चारुदत्त ब्राह्मण और आर्यक की कथा मिला दी थी। भास ने केवल ब्राह्मणकथा को लिखा था। शूद्रक ने गोप-उत्थान भी लिखा। परन्तु उसके मरने के बाद ही नाटक प्रसिद्ध हुआ। गोप था अतः नाम शूद्रक था। बाद में क्योंकि गोप क्षत्रिय भी माने गए, वह भी क्षत्रिय मान लिया गया। आज भी सारे अहीर अपने को यादव क्षत्रिय ही मानते हैं। अर्थात् यह सोचना कि गोप क्षत्रिय बनने के प्रयत्न में थे, नितान्त संगत है और अभी तक भारत में उच्च वर्ण बनने के प्रयत्न में हमें कई निम्नवर्ण मिलते हैं। प्राचीन समय में भी यह बराबर चलता था। धन्धा बदल जाने से गणों के क्षत्रिय अग्रवाल, जैसवाल बनकर बनिए बन गए। परवर्ती हूण राजा अपने को क्षत्रिय कहने लगे। रुद्रदमन जैसे शक अपने को क्षत्रिय मानते थे। मेरी बात पर विचार करते समय कथा के मूल समय और कथा के लिखे जाने के समय का भेद नहीं भूलिए। एक पुराना है, दूसरा बाद का। बाद के में भी पुराने के कई चिह्न हैं, जैसे वैष्णवों द्वारा बाद में सम्पादित महाभारत में मूल महाभारत के कई चिह्न रह गए हैं। पुरानी कथा का केन्द्र है उज्जयिनी। वह इतना बड़ा नगर है कि पाटलिपुत्र का संवाहक उसकी प्रसिद्धि सुनकर बसने को, धन्धा प्राप्त करने को, आता है। उस समय वह पाटलिपुत्र को महानगर नहीं कहता। इसका मतलब है कि उस समय पाटलिपुत्र से अधिक महत्व उज्जयिनी का था। स्पष्ट ही पाटलिपुत्र बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र (ग्राम) था, जबकि उज्जयिनी में महासेन चण्ड प्रद्योत का समृद्ध राज्य था। दूसरी प्राचीनता है कि इसमें दास प्रथा बहुत है। दास-दासी धन देकर आज़ाद कर लिए जाते थे। उस समाज में गणिका भी वधू बन जाती थी। यह सब बातें ऐसे समाज की हैं, जहाँ ज़्यादा कड़ाई नहीं मिलती, जो बाद में चालू हुई थी। बल्कि कवि ने गणिका को वधू बनाकर समाज में एक नया आदर्श रखा है। उसमें विद्रोह की भावना है। अत्याचारी को वह पशु की तरह मरवाता है, स्त्री को ऊँचा उठाता तथा दास स्थावरक को आज़ाद करता है। यों कह सकते हैं कि यह नाटक जोकि शास्त्रीय शब्दों में प्रकरण है–बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कौन जानता है, ऐसे न जाने कितने सामाजिक नाटक काल के गाल में खो गए। हूणों से लेकर तुर्कों तक के विध्वंसों ने न जाने कितने ग्रन्थ-रत्न जला डाले !
तो हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं वे हमें एक नये प्रकाश की ओर ले जाते हैं और इस दृष्टिकोण से हमें इस नाटक का महत्त्व कहीं अधिक लगता है।
इस प्रकार लेखक, रचनाकाल सामाजिक परिस्थिति आदि को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि मृच्छकटिक नाटक प्राचीन और परवर्ती सम्पादन का फल है। बाद के युग में नाटक का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं रहा, और सामाजिक बन्धन तोड़ने में उसका स्वर भी इतना स्पष्ट और मुखर नहीं रहा। आगे के नाटकों में हमें ब्राह्मणों का सम्मान अधिक मिलता है, जबकि ‘मृच्छकटिक’ में हम ब्राह्मण मैत्रेय को गणिका वसंतसेना को पहले नमस्कार करते देखते हैं। परवर्ती सामाजिक चित्रणों में यदि हमें ब्राह्मण की पोल मिलती है, तो उसका दर्जा कुछ अधिक उठा हुआ पाते हैं।
‘मृच्छकटिक’ को राजा शूद्रक ने लिखा था। वह बड़ा कवि था। कुछ लोग कहते हैं, शूद्रक कोई था ही नहीं, एक कल्पित पात्र है। परन्तु पुराने समय में शूद्रक कोई राजा था इसका उल्लेख हमें स्कन्दपुराण में मिलता है। भास नामक कवि ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम ‘दरिद्र चारुदत्त’ है। ‘दरिद्र चारुदत्त’ भाषा और कला की दृष्टि से ‘मृच्छकटिक’ से पुराना नाटक है। निश्चयपूर्वक शूद्रक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाण ने अपनी ‘कादम्बरी’ में राजा शूद्रक को अपना पात्र बनाया है, पर यह नहीं कहा कि वह कवि भी था। बाण का समय छठी शती है। मेरा मत है कि शूद्रक कोई कवि था, जो राजा भी था। वह बहुत पुराना था। परन्तु कालिदास के समय तक उसे प्रधानता नहीं दी गई थी, या कहें कि जिस कालिदास ने सौमिल्ल, भास और कविपुत्र का नाम अपने से पहले बड़े लेखकों में गिनाया है, उसने सबकी सूची नहीं दी थी। शूद्रक का बनाया नाटक पुराना था, जो निरन्तर सम्पादित होता रहा और बाद में प्रसिद्ध हो गया। हो सकता है वह भास के बाद हुआ हो। भास का समय ईसा की पहली या दूसरी शती माना जाता है। ‘मृच्छकटिक’ में दो कथाएँ हैं। एक चारुदत्त की, दूसरी आर्यक की। गुणाढ्य की बृहत्कथा में गोपाल दारक आर्यक के विद्रोह की कथा है। बृहत्कथा अपने मूल रूप में पैशाची भाषा में ‘बड्डकहा’ के नाम से लिखी गई थी। इससे प्रकट होता है कि यह नाटक ईस्वी पहली शती या दूसरी शती का है।
यह नाटक संस्कृत साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इसमें–
(१) गणिका का प्रेम है। विशुद्ध प्रेम, धन के लिए नहीं; क्योंकि वसंतसेना दरिद्र चारुदत्त से प्रेम करती है। गणिका कलाएँ जानने वाली ऊँचे दर्जे की वेश्याएँ होती थीं, जिनका समाज में आदर होता था। ग्रीक लोगों में ऐसी ही ‘हितायरा’ हुआ करती थीं।
(२) गणिका गृहस्थी और प्रेम की अधिकारिणी बनती है, वधू बनती है, और कवि उसे समाज के सम्मान्य पुरुष ब्राह्मण चारुदत्त से ब्याहता है। ब्याह कराता है, रखैल नहीं बनाता। स्त्री-विद्रोह के प्रति कवि की सहानुभूति है। पाँचवें अंक में ही चारुदत्त और वसंतसेना मिल जाते हैं, परन्तु लेखक का उद्देश्य वहीं पूरा नहीं होता। वह दसवें अंक तक कथा बढ़ाकर राजा की सम्मति दिलवाकर प्रेमपात्र नहीं, विवाह कराता है। वसंतसेना अन्तःपुर में पहुँचना चाहती है और पहुँच जाती है। लेखक ने इरादतन यह नतीजा अपने सामने रखा है।
(३) इस नाटक में कचहरी में होने वाले पाप और राजकाज की पोल का बड़ा यथार्थवादी चित्रण है, जनता के विद्रोह की कथा है।
(४) इस नाटक का नायक राजा नहीं है, व्यापारी है, जो व्यापारी-वर्ग के उत्थान का प्रतीक है।
ये इसकी विशेषताएँ हैं। राजनीतिक विशेषता यह है कि इसमें क्षत्रिय राजा बुरा बताया गया है। गोप-पुत्र आर्यक–एक ग्वाला है, जिसे कवि राजा बनाता है। यद्यपि कवि वर्णाश्रम को मानता है, पर वह गोप को ही राजा बनाता है। मेरा मत है कि यह मूलकथा पुरानी है और सम्भवतः यह घटना कोई वास्तविक घटना है जो किंवदन्ती में रह गई। दासप्रथा के लड़खड़ाते समाज का चित्रण बहुत सुन्दर हुआ है, और यह हमें चाणक्य के समय में मिलता है, जब ‘आर्य’ शब्द ‘नागरिक’ (Roman Citizen) के रुप में प्रयुक्त मिलता है। हो सकता है, कोई पुरानी किंवदन्ती चाणक्य के बाद के समय में इस कथा में उतर आई हो। बुद्ध के समय में व्यापारियों का उत्कर्ष भी काफी हुआ था। तब उज्जयिनी का राज्य अलग था, कोसल का अलग। यहाँ भी उज्जयिनी का वर्णन है। एक जगह लगता है कि उस समय भी भारत की एकता का आभास था, जब कहा गया है कि सारी पृथ्वी आर्यक ने जीत ली–वह पृथ्वी जिसकी कैलास पताका है।
देखा जाए तो कवि यथार्थवादी था और निष्पक्ष था। उसने सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाई हैं। और बड़ी गहराई से चित्रण किया है। यही उसकी सफलता का कारण है।
‘मृच्छकटिक’ की कथा का स्थान उज्जयिनी है, हमें इसमें चातुर्वर्ण्य का समाज मिलता है–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का मुख्य काम पुरोहिताई था। पर वे राजकाज में भी दिलचस्पी लेते थे और मुझे जो इस कथा में एक बड़ी गम्भीर बात मिलती है वह यह है कि यहाँ ब्राह्मण, व्यापारी और निम्नवर्ण मिलकर मदान्ध क्षत्रिय राज्य को उखाड़ फेंकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। और फिर सोचने की बात यह है कि इस कथा का लेखक राजा शूद्रक माना जाता है जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा गया है। यह क्या प्रकट करता है ? यह तो स्पष्ट ही है कि प्रस्तावना शूद्रक की मौत के बाद लिखी गई है, क्योंकि स्वयं उसके जलकर मरने का वर्णन हमें मिलता है। इसका मतलब है कि यह नाटक लेखक के मरने के बाद प्रसिद्ध हुआ था, पहले नहीं। इससे प्रकट होता है कि नाटक की मूलकथा उस समय की है जब आभीर जैसी विदेशी जाति बाहर से आकर भारत में बस चुकी थी और आभीर और गोप भारत में हिलमिल गए थे। महाभारत से प्रकट होता है कि गोप–ग्वाले भारत में पहले भी थे। श्रीकृष्ण के अन्तिम काल में आभीरों ने आक्रमण किया था। उन्होंने यादवगण जीता था। यादवगण द्वारका की तरफ था। द्वारका गुजरात की ओर थी। ये आभीर उसी तरफ आकर बस गए थे। वहीं आभीर गोपों से मिलमिला गए। इन्हींको बाद में अहीर कहा गया। मैं तो कहता हूँ कि यह गोप शब्द आभीर के लिए आया है, इसका कारण यही है कि गोप तब तक ‘क्षत्रिय’ नहीं माने गए थे। बाद में सम्भवतः मान लिए गए थे, क्योंकि आर्यक के राजा हो जाने के बाद ऐसा हो जाना कठिन नहीं था। मूल क्षत्रिय मदान्ध थे और ब्राह्मणों पर भी अत्याचार करते थे। यह तो निस्सन्देह सत्य है कि मूल क्षत्रियों के ‘गणतन्त्रवाद’, ‘बाह्मण-विरोधी स्वभाव’ के कारण जनता और प्रायः ब्राह्मणगण–(सिवाय यज्ञ की दक्षिणा लेनेवालों को छोड़कर)–विरुद्ध थे। उन्होंने कई बाहरी जातियों को मान्यता दी थी। ऐसा ही विद्रोह कृष्ण ने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के विरुद्ध गोवर्धन-पूजा करा कर कंस के विरुद्ध किया था। स्पष्ट ही हम गोप-पुत्र आर्यक को राजा बनते देखते हैं और ब्राह्मण शर्विलक उसे राजा बनाने को तख्ता पलटता है। चारुदत्त भी उसका सहायक है। राजा पालक अत्याचारी है। सब उससे अप्रसन्न हैं। आर्यक उसे उखाड़ता है तो उसकी इन्द्र से तुलना की जाती है। वह कुल और मान का रक्षक माना जाता है। वह ब्राह्मणों को अनुष्ठान में लगनेवाली शासन-व्यवस्था स्थापित करता है। शूद्रक सम्भवतः कोई गोप राजा ही था, जिसने चारुदत्त ब्राह्मण और आर्यक की कथा मिला दी थी। भास ने केवल ब्राह्मणकथा को लिखा था। शूद्रक ने गोप-उत्थान भी लिखा। परन्तु उसके मरने के बाद ही नाटक प्रसिद्ध हुआ। गोप था अतः नाम शूद्रक था। बाद में क्योंकि गोप क्षत्रिय भी माने गए, वह भी क्षत्रिय मान लिया गया। आज भी सारे अहीर अपने को यादव क्षत्रिय ही मानते हैं। अर्थात् यह सोचना कि गोप क्षत्रिय बनने के प्रयत्न में थे, नितान्त संगत है और अभी तक भारत में उच्च वर्ण बनने के प्रयत्न में हमें कई निम्नवर्ण मिलते हैं। प्राचीन समय में भी यह बराबर चलता था। धन्धा बदल जाने से गणों के क्षत्रिय अग्रवाल, जैसवाल बनकर बनिए बन गए। परवर्ती हूण राजा अपने को क्षत्रिय कहने लगे। रुद्रदमन जैसे शक अपने को क्षत्रिय मानते थे। मेरी बात पर विचार करते समय कथा के मूल समय और कथा के लिखे जाने के समय का भेद नहीं भूलिए। एक पुराना है, दूसरा बाद का। बाद के में भी पुराने के कई चिह्न हैं, जैसे वैष्णवों द्वारा बाद में सम्पादित महाभारत में मूल महाभारत के कई चिह्न रह गए हैं। पुरानी कथा का केन्द्र है उज्जयिनी। वह इतना बड़ा नगर है कि पाटलिपुत्र का संवाहक उसकी प्रसिद्धि सुनकर बसने को, धन्धा प्राप्त करने को, आता है। उस समय वह पाटलिपुत्र को महानगर नहीं कहता। इसका मतलब है कि उस समय पाटलिपुत्र से अधिक महत्व उज्जयिनी का था। स्पष्ट ही पाटलिपुत्र बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र (ग्राम) था, जबकि उज्जयिनी में महासेन चण्ड प्रद्योत का समृद्ध राज्य था। दूसरी प्राचीनता है कि इसमें दास प्रथा बहुत है। दास-दासी धन देकर आज़ाद कर लिए जाते थे। उस समाज में गणिका भी वधू बन जाती थी। यह सब बातें ऐसे समाज की हैं, जहाँ ज़्यादा कड़ाई नहीं मिलती, जो बाद में चालू हुई थी। बल्कि कवि ने गणिका को वधू बनाकर समाज में एक नया आदर्श रखा है। उसमें विद्रोह की भावना है। अत्याचारी को वह पशु की तरह मरवाता है, स्त्री को ऊँचा उठाता तथा दास स्थावरक को आज़ाद करता है। यों कह सकते हैं कि यह नाटक जोकि शास्त्रीय शब्दों में प्रकरण है–बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कौन जानता है, ऐसे न जाने कितने सामाजिक नाटक काल के गाल में खो गए। हूणों से लेकर तुर्कों तक के विध्वंसों ने न जाने कितने ग्रन्थ-रत्न जला डाले !
तो हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं वे हमें एक नये प्रकाश की ओर ले जाते हैं और इस दृष्टिकोण से हमें इस नाटक का महत्त्व कहीं अधिक लगता है।
इस प्रकार लेखक, रचनाकाल सामाजिक परिस्थिति आदि को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि मृच्छकटिक नाटक प्राचीन और परवर्ती सम्पादन का फल है। बाद के युग में नाटक का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं रहा, और सामाजिक बन्धन तोड़ने में उसका स्वर भी इतना स्पष्ट और मुखर नहीं रहा। आगे के नाटकों में हमें ब्राह्मणों का सम्मान अधिक मिलता है, जबकि ‘मृच्छकटिक’ में हम ब्राह्मण मैत्रेय को गणिका वसंतसेना को पहले नमस्कार करते देखते हैं। परवर्ती सामाजिक चित्रणों में यदि हमें ब्राह्मण की पोल मिलती है, तो उसका दर्जा कुछ अधिक उठा हुआ पाते हैं।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book