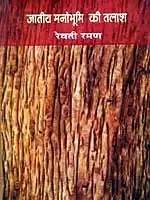|
भाषा एवं साहित्य >> जातीय मनोभूमि की तलाश जातीय मनोभूमि की तलाशरेवती रमण
|
54 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है लेखक के जीवन की उत्कृष्ट समालोचना.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘जातीय मनोभूमि की तलाश’
रचना के भीतर आलोचक की अपनी
भी तलाश है। नयी-पुरानी कृतियों से संवाद की आतुरता आत्म को तजकर नहीं हो
सकती। इस वेदना-विकलता को सिर्फ भावक या अभिभावक के हवाले नहीं किया जा
सकता। ‘हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे
अभी’-ये सवाल सदैव उन्हीं के मन में नहीं उठते जो
पुनरुत्थानवादी हैं या गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं। जातीय
अस्मिता के लिए संकट की घड़ी में सार्थक लेखन जातीय मनोभूमि को समझे बिना
मुश्किल है। सर्जक हों, आलोचक हों या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं-तब
भी क्या द्वन्द्व रहित हुआ जा सकता है, संशयरहित हुआ जा सकता है ? मुक्ति
की चाहत अग्रसर है और शायद यही वह तत्व है जो शुरू से अन्त तक व्याप्त है।
इस एक तत्व की प्रधानता ने शिक्षित-अशिक्षित सबको बिना किसी भेद-भाव के
जातीय साहित्य में जगह दी है। विचलन से वितर्क व्यर्थ नहीं है, न इससे
छुटकारा ही सम्भव है तथापि जातीय साहित्य की मनोभूमि व्यापक है, उर्वर है।
वह हर बार लीलावादी ही नहीं हैं, संश्लिष्ट ही नहीं हैं। कल्पना और यथार्थ
के द्वन्द्व में एक समय कल्पना अधिक कारगार हो सकती है तो दूसरे समय में
यथार्थ की पारदर्शिता प्रबल हो सकती है।
ईमान की बात कहूँ तो कोई एक पक्ष चुन लेना मेरे लिए सदैव दुष्कर रहा है। एक जिद या संकेत पर इधर या उधर पंक्ति में खड़ा हो जाना मुझे स्वीकार्य नहीं हुआ है। क्या यही स्वाधीन मन की गतिविधि है ? या स्वेच्छाचारी अराजक उपक्रम ?
समीक्षक स्वभाववश अन्य के अँधेरे में खास दिलचस्पी रखते हैं। जबकि मौका निकाल उन्हें चिराग तले अँघेरे की शिनाख्त करनी चाहिए। पीछे मुड़कर देखना हर बार कुछ मूल्यवान देखने या वहाँ से ले आने के लिए नहीं हुआ है। आदान-प्रदान में आस्था के बावजूद जब एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से टकराती है तो आलोचना की भाषा में एक खास तरह की चमक आ जाती है। भाषिक विशिष्टता अक्सर मानवीय समृद्धि का उदाहरण होती हैं।
ये समीक्षाएँ साक्षी हैं कि मैने आत्म-समर्पण नहीं किया है न तटस्थ के दबाव में निश्छल भावुकता का अनादर ही। व्यक्ति हो या संस्था-उससे टकराने मात्र के लिए टकराना मेरा इरादा नहीं रहा है। दावा नहीं करता, फिर भी कहे बिना नहीं रहा जाता कि मैंने टकराहट में टूटने की आवाज सुनी है। सरल, सहज स्वाभिमान की आवाज उदारता और विनम्रता उसमें आधार संरचना है। त्याग और ग्रहण का अदभुत विवेक ही हमारी जातीय मनीषा है। बहरहाल !
इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं ज्ञानपीठ का आभारी हूँ।
ईमान की बात कहूँ तो कोई एक पक्ष चुन लेना मेरे लिए सदैव दुष्कर रहा है। एक जिद या संकेत पर इधर या उधर पंक्ति में खड़ा हो जाना मुझे स्वीकार्य नहीं हुआ है। क्या यही स्वाधीन मन की गतिविधि है ? या स्वेच्छाचारी अराजक उपक्रम ?
समीक्षक स्वभाववश अन्य के अँधेरे में खास दिलचस्पी रखते हैं। जबकि मौका निकाल उन्हें चिराग तले अँघेरे की शिनाख्त करनी चाहिए। पीछे मुड़कर देखना हर बार कुछ मूल्यवान देखने या वहाँ से ले आने के लिए नहीं हुआ है। आदान-प्रदान में आस्था के बावजूद जब एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से टकराती है तो आलोचना की भाषा में एक खास तरह की चमक आ जाती है। भाषिक विशिष्टता अक्सर मानवीय समृद्धि का उदाहरण होती हैं।
ये समीक्षाएँ साक्षी हैं कि मैने आत्म-समर्पण नहीं किया है न तटस्थ के दबाव में निश्छल भावुकता का अनादर ही। व्यक्ति हो या संस्था-उससे टकराने मात्र के लिए टकराना मेरा इरादा नहीं रहा है। दावा नहीं करता, फिर भी कहे बिना नहीं रहा जाता कि मैंने टकराहट में टूटने की आवाज सुनी है। सरल, सहज स्वाभिमान की आवाज उदारता और विनम्रता उसमें आधार संरचना है। त्याग और ग्रहण का अदभुत विवेक ही हमारी जातीय मनीषा है। बहरहाल !
इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं ज्ञानपीठ का आभारी हूँ।
भक्ति-आन्दोलन सगुणोपासना
हिन्दी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन की क्रान्तिकारी भूमिका है। भारत के इतिहास में घटित अन्य सभी आन्दोलनों में से वह अधिक व्यापक और विशाल तो था ही, प्रभाव के स्तर पर दीर्घायु और संक्रमणशील भी साबित हुआ। इस आन्दोलन में एक साथ ही अनेक मतों,
सम्प्रदायों और जातियों की महान विभूतियों ने योगदान किया था। खासतौर से
पन्द्रहवीं और सोलहवीं-इन दो शताब्दियों में समूचा भारत वर्ष साधना और
प्रेमोल्लास के अभूतपूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इतना बड़ा आन्दोलन
क्यों और कैसे घटित हुआ ? इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं। इतिहासकारों
का एक बड़ा वर्ग इसे स्वाभाविक और स्वतःस्फूर्त मानता है जबकि दूसरा वर्ग
इसके कारणों की खोज हमारी जातीय पराधीनता में करता है। इतना निश्चित है कि
उस काल में भारत के हिन्दू राजे आपसी कलह और विद्वेष में लिप्त थे और
एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते-लड़ते इतने हतदर्प और निस्तेज हो चले थे कि
विदेशी आक्रान्ता निश्चित भाव से अपना साम्राज्य-विस्तार कर सके। भक्त
कवियों ने जातीय संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने नैतिक दायित्व
का विषम परिस्थितियो में भी पूरी क्षमता से निर्वाह किया और यह दृष्टांत
प्रस्तुत किया कि राजनीति जब किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाती है तब साहित्य ही
उसके और समाज के मार्ग-दर्शन का बीड़ा उठाता है।
प्रसंगवश, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में ‘पूर्व मध्यकाल’ की चर्चा के आरम्भ में ही लिखा है, ‘देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के ह्रदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही देवमन्दिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपने वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे, आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गये। इतने भारी राजनैतिक उलटफेर के पीछे हिन्दू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छायी रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ? ’ (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ.43)
भक्ति-आन्दोलन को जो लोग भारत में इस्लाम की प्रतिक्रिया मानते हैं, आचार्य शुक्ल उनकी भावधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ‘इसके पीछे हमारी जातीय पौरुष की हताशा है’- इस विचार का खण्डन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी के मत में ‘मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिन्ध में तब फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। ‘द्विवेदी जी जोर देकर कहते हैं कि ‘ इस देश में अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता है, जैसा आज है।’ उन्होंने ग्रियर्सन के इस विचार का भी खण्डन किया है कि ‘ भक्ति-आन्दोलन अचानक बिजली के समान फैल गया।’ उनकी मान्यता है कि इसके लिए ‘सैकड़ों वर्षों से मेघखण्ड एकत्र हो रहे थे।’ भक्ति-आन्दोलन के अविर्भाव के पीछे ‘ उस काल की लोक प्रवृत्ति का शास्त्र-सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना है।’ शास्त्र-सिद्ध आचार्य दक्षिण भारत के वैष्णव थे, जहाँ सातवीं शताब्दी के पहले ही वैष्णव भक्ति ने जोर पकड़ लिया था। अलवार भक्तों के प्रयास से भक्ति का विस्तार हुआ। ये आलवार भक्त बारह की संख्या में बताए गये हैं। इनमें से नौ के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर किसी को कोई सन्देह नहीं है। इन्हीं में एक कावियित्री अन्दाल भी थीं। अलवार भक्तों में कुछ अस्पृ्श्य जातियों में उत्पन्न हुए थे। इन्हीं की परम्परा में आचार्य रामानुज हुए, जिनके सुयोग्य शिष्य रामानन्द ने उपासना के क्षेत्र में लक्ष्मण और सीता के साथ राम-रूप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा की। अनुश्रुति है कि ‘भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लाए रामानन्द/परगट कियो कबीर ने, सात द्वीप नौ खण्ड।’ इससे रामानन्द और कबीर के सम्बन्ध उजागर होता है।
दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संस्थापक इतिहास-प्रसिद्ध चार आचार्य हुए-(1) रामानुज, (2) मध्वाचार्य, (3) विष्णू स्वामी और. (4) निम्बार्क । इनके प्रयासों से वैष्णव धर्म की जो प्रशस्त पावन धारा दक्षिण में प्रवाहित हुई, उसे उत्तर भारत में ले आने और अधिक वेग से प्रवाहमान बनाने का क्रान्तिकारी कार्य जिन महापुरुषों ने किया, उनमें रामानन्द, बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु प्रमुख हैं। इनमें रामानन्द सबसे क्रान्तिरारी माने गये है। उनकी शिष्य-परम्परा में जाति-भेद नहीं माना गया और आगे चलकर यह उक्ति प्रचलित हुई।
प्रसंगवश, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में ‘पूर्व मध्यकाल’ की चर्चा के आरम्भ में ही लिखा है, ‘देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू जनता के ह्रदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही देवमन्दिर गिराए जाते थे, देवमूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपने वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे, आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गये। इतने भारी राजनैतिक उलटफेर के पीछे हिन्दू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छायी रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था ? ’ (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ.43)
भक्ति-आन्दोलन को जो लोग भारत में इस्लाम की प्रतिक्रिया मानते हैं, आचार्य शुक्ल उनकी भावधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ‘इसके पीछे हमारी जातीय पौरुष की हताशा है’- इस विचार का खण्डन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। द्विवेदी जी के मत में ‘मुसलमानों के अत्याचार के कारण भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिन्ध में तब फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में। ‘द्विवेदी जी जोर देकर कहते हैं कि ‘ इस देश में अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता है, जैसा आज है।’ उन्होंने ग्रियर्सन के इस विचार का भी खण्डन किया है कि ‘ भक्ति-आन्दोलन अचानक बिजली के समान फैल गया।’ उनकी मान्यता है कि इसके लिए ‘सैकड़ों वर्षों से मेघखण्ड एकत्र हो रहे थे।’ भक्ति-आन्दोलन के अविर्भाव के पीछे ‘ उस काल की लोक प्रवृत्ति का शास्त्र-सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना है।’ शास्त्र-सिद्ध आचार्य दक्षिण भारत के वैष्णव थे, जहाँ सातवीं शताब्दी के पहले ही वैष्णव भक्ति ने जोर पकड़ लिया था। अलवार भक्तों के प्रयास से भक्ति का विस्तार हुआ। ये आलवार भक्त बारह की संख्या में बताए गये हैं। इनमें से नौ के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर किसी को कोई सन्देह नहीं है। इन्हीं में एक कावियित्री अन्दाल भी थीं। अलवार भक्तों में कुछ अस्पृ्श्य जातियों में उत्पन्न हुए थे। इन्हीं की परम्परा में आचार्य रामानुज हुए, जिनके सुयोग्य शिष्य रामानन्द ने उपासना के क्षेत्र में लक्ष्मण और सीता के साथ राम-रूप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा की। अनुश्रुति है कि ‘भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लाए रामानन्द/परगट कियो कबीर ने, सात द्वीप नौ खण्ड।’ इससे रामानन्द और कबीर के सम्बन्ध उजागर होता है।
दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संस्थापक इतिहास-प्रसिद्ध चार आचार्य हुए-(1) रामानुज, (2) मध्वाचार्य, (3) विष्णू स्वामी और. (4) निम्बार्क । इनके प्रयासों से वैष्णव धर्म की जो प्रशस्त पावन धारा दक्षिण में प्रवाहित हुई, उसे उत्तर भारत में ले आने और अधिक वेग से प्रवाहमान बनाने का क्रान्तिकारी कार्य जिन महापुरुषों ने किया, उनमें रामानन्द, बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु प्रमुख हैं। इनमें रामानन्द सबसे क्रान्तिरारी माने गये है। उनकी शिष्य-परम्परा में जाति-भेद नहीं माना गया और आगे चलकर यह उक्ति प्रचलित हुई।
जाति-पाँति पूछै नहिं कोई।
हरि को भजै सो हरि को होई।।
हरि को भजै सो हरि को होई।।
इस उक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण सन्त मत के कवि
हैं। सगुण भक्ति में कृष्णोपासक कवियों ने इस परम्परा को कायम रखा। सूफी
सम्प्रदाय के कवि इस परम्परा से अलग हैं। उनका सीधा सम्बन्ध रामानुज या
रामानन्द से नहीं था। फिर भी उनकी प्रेम-भावना ने सह्रदय हिन्दुओं और
मुसलमानों को ब्राह्माचार और पाखण्ड से मुक्ति के गम्भीर और रचनात्मक
आश्वासन दिए। जिस तरह कबीर, रैदास, दादू जैसे सन्तों ने नाथ-सिद्ध योगियों
के साधना-मार्ग के कील-काँटे निकाल कर उनकी क्रान्तिकारी भावनाओं को भक्ति
के रस से सींचा, उसे सर्वथा एक नया संस्कार दिया, उसी प्रकार मलिक मुहम्मद
जायसी, कुतुबन, मंझन सरीखे प्रेममार्गी कवियों ने सूफी मत को हिन्दुओं में
प्रचलित लोकगाथाओं से जोड़कर गहरे रचनात्मक अर्थ में भारतीय होने का एहसास
कराया। अतः भक्ति-आन्देलन का एक शानदार पहलू निर्गुण मत है तो दूसरा उससे
भी चमकदार पहलू उसका प्रेम-मार्ग है।
भक्ति-आन्दोलन की जो दो अन्य शाखाएँ हैं, वे क्रमश: कृष्ण और राम के आख्यान से सम्बद्ध है। आचार्य शुक्ल ने इन सगुणोपासक भक्ति-धाराओं को ही ध्यान में रखकर इस्लामी कट्टरता का जिक्र किया है। शुक्ल जी की अवधारणा के पीछे वल्लभाचार्यकृत ‘कृष्णाश्रय’ ये पंक्तियाँ हैं।
भक्ति-आन्दोलन की जो दो अन्य शाखाएँ हैं, वे क्रमश: कृष्ण और राम के आख्यान से सम्बद्ध है। आचार्य शुक्ल ने इन सगुणोपासक भक्ति-धाराओं को ही ध्यान में रखकर इस्लामी कट्टरता का जिक्र किया है। शुक्ल जी की अवधारणा के पीछे वल्लभाचार्यकृत ‘कृष्णाश्रय’ ये पंक्तियाँ हैं।
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च।
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरवावृतेष्विह।
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववृतयोगिषु।
तिरोहितार्थवेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु।
पांषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
गंगादितीर्थवर्येषु दुष्टैरवावृतेष्विह।
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववृतयोगिषु।
तिरोहितार्थवेदेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु।
पांषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम।।
अर्थात देश म्लेच्छाक्रान्त है। गंगादि तीर्थ
दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो
रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष
पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कष्णाश्रय ही
जीवन का कल्याण है। वल्लभाचार्य के समय तक देश में इस्लामी शासन सुदृढ़ हो
चला था। हिन्दुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण में
विजय नगर बचा था लेकिन बहमनी सुलतानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन
भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कृति का असर तेज हो चला था।
‘ इस परिस्थिति में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रचार
द्वारा ही लोगों के कल्याण-मार्ग की ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय
संस्कृति के बने रहने की सम्भावना वल्लभाचार्य जी को दिखाई
पड़ी।’ आगे चलकर महाप्राण निराला ने इस्लाम के चन्द्रोदय और
हिन्दुओं के संस्कृति-सूर्य के द्वारा ‘तुलसीदास’ के
आरम्भिक छन्दों में उस युग की प्रतिक्रिया और प्रभाव का सजीव चित्र खींचा
है।
भक्ति-आन्दोलन के सन्दर्भ में इस्लाम का सुदृढ़ शासन एक तथ्य है। उसका प्रभाव हो या उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया-सगुण मार्ग का निर्गुण मत से विरोध अलक्षित नहीं रहा। निर्गुण भक्ति के पीछे एकेश्वरवाद था और सगुण भक्ति के अन्तर्गत अवतारवाद की मान्यता थी। कृष्ण हो या राम दोनों ही अवतार माने गये। कृष्ण के लीला विहार का दृष्यपट द्वापर है और राम अपनी मर्यादा के लिए पुरुषार्थ-प्रदर्शन त्रेता के परिवेश में करते हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे गये और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण को लेकर जीवन के उपभोगपक्ष अर्थात आनन्द की सिद्धावस्था का काव्य प्रचुरता में लिखा गया तो राम को लेकर जीवन के कर्म-संघर्ष को अभिव्यक्ति दी गयी। अकारण नहीं है कि कृष्ण स्वरूप में मुसलमान कवियों ने भी गहरी रुचि ली। सगुण भक्ति के ये दोनों आलम्बन प्रयोजन का एकता से बँधे है। उनके अवतरित होने का प्रयोजन है दुष्टों का संहार जो धर्म-मार्ग की मुख्य बाधा है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा था।
भक्ति-आन्दोलन के सन्दर्भ में इस्लाम का सुदृढ़ शासन एक तथ्य है। उसका प्रभाव हो या उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया-सगुण मार्ग का निर्गुण मत से विरोध अलक्षित नहीं रहा। निर्गुण भक्ति के पीछे एकेश्वरवाद था और सगुण भक्ति के अन्तर्गत अवतारवाद की मान्यता थी। कृष्ण हो या राम दोनों ही अवतार माने गये। कृष्ण के लीला विहार का दृष्यपट द्वापर है और राम अपनी मर्यादा के लिए पुरुषार्थ-प्रदर्शन त्रेता के परिवेश में करते हैं। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे गये और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण को लेकर जीवन के उपभोगपक्ष अर्थात आनन्द की सिद्धावस्था का काव्य प्रचुरता में लिखा गया तो राम को लेकर जीवन के कर्म-संघर्ष को अभिव्यक्ति दी गयी। अकारण नहीं है कि कृष्ण स्वरूप में मुसलमान कवियों ने भी गहरी रुचि ली। सगुण भक्ति के ये दोनों आलम्बन प्रयोजन का एकता से बँधे है। उनके अवतरित होने का प्रयोजन है दुष्टों का संहार जो धर्म-मार्ग की मुख्य बाधा है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा था।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।7।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।8।।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।7।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।8।।
आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का
भाषान्तरण किया।
जब-जब होंहि धरम कै हानी।
बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।।
तब-तब धरि प्रभु मनुज शरीरा।
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीड़ा।।
बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।।
तब-तब धरि प्रभु मनुज शरीरा।
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीड़ा।।
राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं
और धरती पर इनका अवतार असुरों,
पापियों और अभिमानियों के विनाश के लिए होता है। वे धर्म के संस्थापक हैं
और सज्जन की पीड़ा दूर करते हैं। उनमें क्षात्र-धर्म का सौन्दर्य खास बात
है।
जहाँ तक विष्णु-रूप की कल्पना की बात है तो इससे सर्वप्रथम साक्षात्कार ऋग्वेद में विष्णु की कल्पना सूर्य के रूप में की गयी है। संरक्षण की अमित आभा के कारण विष्णु को ‘परम पद’ कहा गया है। कालान्तर में विष्णु-स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु के वामन रूप का चित्रण है, जहाँ वह राक्षसे के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। रामायण-काल में कदाचित् पहली बार विष्णु को ब्रह्म का स्थानापन्न माना गया जब कि महाभारत में उसका स्रस्टा रूप प्रदर्शित किया गया। ब्रह्मा उसके नाभि कमल से व्युत्पन्न हैं और रुद्र उसके मस्तक से। पुराणों में विष्णु के विकसनशील स्वरूप को सबसे ऊँची जगह मिली। माना जाता है कि पाँच सहस्त्राब्दियों से पहले भारत में वैष्णव धर्म प्रतिष्ठित हो चला था जिसे कालान्तर में भागवत धर्म भी कहा गया और नारायणी भावना से जोड़कर उसे व्यापक बनाया गया।
जैसा कि डॉक्टर रामचन्द्र तिवारी ने लिखा है, ‘ भागवत धर्म शुद्ध वैदिक धर्म नहीं था। उसे वेदसम्मत् प्रमाणित करना पड़ा। ‘शक्ति सम्पन्न आर्येत्रर जातियों को समाज की उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिए, उसके विश्वासों और आचार्यों के साथ उनका धार्मिक उन्नयन किया गया और इस प्रयास में भागवत धर्म प्रतिष्ठित हुआ होगा। इसका एक दूसरा पहलू इस्लाम की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इस्लाम की कट्टरता की प्रतिक्रिया के विपन्न दौर में हिन्दू और अधिक हिन्दू बनें हों, यह सम्भव है। लेकिन इससे भारतीय जन-जीवन के अन्तर्विरोधी की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इतिहास सम्मत तथ्य है कि आठवीं शताब्दी के आस-पास भारतीय समाज अनेक जातियों, उपजातियों में विभाजित होकर विकारग्रस्त हो चला था। सवर्ण जातियों के वर्चस्व को दोनों तरफ से चुनौती मिलने लगी थी। बाहर से शक, हूण, पल्लव, कुषाण जातियों का आक्रमण और भीतर से पिछड़ी जातियों का अभ्युदय सामाजिक ढाँचे में व्यापक परिवर्तन की भूमिका प्रस्तुत कर रहा था। आभीर जाति ने वैष्णव धर्म के भीतर कृष्ण भावना का समावेश कर उस महाप्रतापी आन्दोलन की भूमिका बनायी जिसे हम भक्ति-आन्दोलन के रूप में जानते हैं। यही वह समय है, जब शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सूत्रपात किया था। वह लंबे समय तक लोकप्रिय भी रहा। शांकर मत में सम्पूर्ण सृष्टि एक ही चिरन्तन सत्ता से प्रोदभासित मानी गयी है और जीव को उस चिरन्तन सर्वोपरि सत्ता से अभिन्न माना गया है। दक्षिण के आलवार भक्तों ने प्रेम-भावना से जोड़कर उसे एक मानवीय अर्थवत्ता प्रदान की और तब भक्ति-आदोलन भारतीय समाज में आन्तरिक एकता का संवाहक भी बन सका।
भक्ति-आन्दोलन के पीछे भारतवर्ष की आन्तरिक जीवनी शक्ति सक्रिय थी। वह एक विशाल या कहें अखिल भारतीय संस्कृति आन्दोलन था। ऐसे आन्दोलन को वेवर, ग्रियर्सन, भण्डारकर जैसे लोग यदि ईसाइयत की देन कहते हैं तो मानना पड़ेगा कि उनकी मान्यताएँ बेपर की उड़ान हैं। क्राइस्ट और कृष्ण के नाम-साम्य से किसी तरह की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले भारत में कृष्णाख्यान लोक में प्रचलित था। प्रसंगवश डॉक्टर रामचन्द्रतिवारी ने लिखा है-‘भक्ति-आन्दोलन में निहित प्रेम और समता की भावना का प्रेरक-स्त्रोत ईसाई धर्म को माना जाए तो घूम-फिरकर भारतवर्ष में ही लौट आना पड़ता है, क्योंकि ईसाई धर्म भी बौद्धधर्म से प्रभावित माना गया है। बौद्ध धर्मावलम्बियों और जैन व्यापारियों के अलेक्जेण्ड्रिया में बसने की बात बहुत पुरानी है। अशोक ने मेसी डोनिया में भी बौद्धभिक्षुओं को धर्म के प्रचारार्थ भेजा था। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक उदारता और सामाजिक सहिष्णुता ईसाई धर्म में पायी जाती है, वह वस्तुतः हमारे धर्मग्रन्थों में पहले ही प्रतिपादित हो चुकी थी। इस तथ्य की जानकारी के लिए एक ही पुस्तक दासगुप्ता की ‘द लिगेसी ऑफ इण्डिया’ का अध्ययन पर्याप्त है। अलवार भक्तों की प्रेम भावना को पुराणों में प्रतिपादित धर्मिक सहिष्णुता और सामाजिक उदभाव से जोड़कर लोकप्रिय रूप देने का श्रेय हिन्दी के सगुणोपासक कवियों को है। सूर, तुलसी जैसे महाकवियों की वाणी का जैसा असर जनमानस पर पड़ा, वैसा अन्य. कवियों का नहीं।’
सूर की काव्य-प्रतिभा से अभिभूत होकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ‘सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिकाव्य परम्परा का, चाहे वह मौखिक हो रही हो, पूर्ण-विकास-सा प्रतीत होता है।’ शुक्ल जी की इस स्थापना के आधार पर सूर से पहले के ब्रजभाषा काव्य की खोज की गयी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया कि ‘दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में भागवत परम्परा से भिन्न भी कोई लीला गान की शास्त्रीय परम्परा रही होगी। जयदेव का गीत ‘गीत-गोविन्द’ पूर्णरूप से भागवत परम्परा का ग्रन्थ नहीं है। उसमें प्रमुख गोपी राधा है, जो भागवत में अपरिचित हैं। इसके अतिरिक्त ‘गीत-गोविन्द’ का रास ‘वसन्त-रास’ है, जो भागवत का ‘शरद-रास’ नहीं। अतः ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत वर्ष में लीला-गान की परम्परा कब शुरू हुई ? लेकिन दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में मात्रिक छन्दों में गेय पद लिखने की प्रथा चल रही थी। उन दिनों उड़ीसा में उड़िया भाषा में कष्ण-लीला के पद रचे जाते थे और सम्भवतः उड़िया लीला गान से प्रभावित होकर ही जयदेव ने ‘गीत-गोविन्द’ की रचना की होगी। जयदेव के उपरान्त लोक भाषा में गेय पदों का कृष्ण लीला-परक काव्य मिथिला के विद्यापति और बंगाल के चण्डीदास ने ही लिखा। इस तरह संक्षेप में कहें तो बौद्ध-सिद्धों के गान, जयदेव का ‘गीत-गोविन्द’ और चण्डीदास विद्यापति के पद कृष्णलीला-गान की परम्परा का समृद्ध करते हैं। बौद्ध-सिद्धों के गान में कृष्ण और राधा के प्रसंग नहीं आते, नहीं आ सकते थे, अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह मत समीचीन है कि विद्यापति पर गीत-गोविन्द का स्पष्ट भाव होने के कारण कृष्ण काव्य का सूत्र पात जयदेव से ही मानना चाहिए।’
जयदेव का रचना काल विक्रम की तेरहवीं शताब्दी सर्वमान्य है। उन्हें बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के दरबार में ‘राजकवि का सम्मान प्राप्त था। कवि के रूप में उनकी विश्वप्रसिद्धि का एक ही कारण है-उनकी अमर रचना ‘गीत-गोविन्द’। इसमें उन्होंने लिखा है।
जहाँ तक विष्णु-रूप की कल्पना की बात है तो इससे सर्वप्रथम साक्षात्कार ऋग्वेद में विष्णु की कल्पना सूर्य के रूप में की गयी है। संरक्षण की अमित आभा के कारण विष्णु को ‘परम पद’ कहा गया है। कालान्तर में विष्णु-स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु के वामन रूप का चित्रण है, जहाँ वह राक्षसे के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। रामायण-काल में कदाचित् पहली बार विष्णु को ब्रह्म का स्थानापन्न माना गया जब कि महाभारत में उसका स्रस्टा रूप प्रदर्शित किया गया। ब्रह्मा उसके नाभि कमल से व्युत्पन्न हैं और रुद्र उसके मस्तक से। पुराणों में विष्णु के विकसनशील स्वरूप को सबसे ऊँची जगह मिली। माना जाता है कि पाँच सहस्त्राब्दियों से पहले भारत में वैष्णव धर्म प्रतिष्ठित हो चला था जिसे कालान्तर में भागवत धर्म भी कहा गया और नारायणी भावना से जोड़कर उसे व्यापक बनाया गया।
जैसा कि डॉक्टर रामचन्द्र तिवारी ने लिखा है, ‘ भागवत धर्म शुद्ध वैदिक धर्म नहीं था। उसे वेदसम्मत् प्रमाणित करना पड़ा। ‘शक्ति सम्पन्न आर्येत्रर जातियों को समाज की उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित करने के लिए, उसके विश्वासों और आचार्यों के साथ उनका धार्मिक उन्नयन किया गया और इस प्रयास में भागवत धर्म प्रतिष्ठित हुआ होगा। इसका एक दूसरा पहलू इस्लाम की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इस्लाम की कट्टरता की प्रतिक्रिया के विपन्न दौर में हिन्दू और अधिक हिन्दू बनें हों, यह सम्भव है। लेकिन इससे भारतीय जन-जीवन के अन्तर्विरोधी की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इतिहास सम्मत तथ्य है कि आठवीं शताब्दी के आस-पास भारतीय समाज अनेक जातियों, उपजातियों में विभाजित होकर विकारग्रस्त हो चला था। सवर्ण जातियों के वर्चस्व को दोनों तरफ से चुनौती मिलने लगी थी। बाहर से शक, हूण, पल्लव, कुषाण जातियों का आक्रमण और भीतर से पिछड़ी जातियों का अभ्युदय सामाजिक ढाँचे में व्यापक परिवर्तन की भूमिका प्रस्तुत कर रहा था। आभीर जाति ने वैष्णव धर्म के भीतर कृष्ण भावना का समावेश कर उस महाप्रतापी आन्दोलन की भूमिका बनायी जिसे हम भक्ति-आन्दोलन के रूप में जानते हैं। यही वह समय है, जब शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सूत्रपात किया था। वह लंबे समय तक लोकप्रिय भी रहा। शांकर मत में सम्पूर्ण सृष्टि एक ही चिरन्तन सत्ता से प्रोदभासित मानी गयी है और जीव को उस चिरन्तन सर्वोपरि सत्ता से अभिन्न माना गया है। दक्षिण के आलवार भक्तों ने प्रेम-भावना से जोड़कर उसे एक मानवीय अर्थवत्ता प्रदान की और तब भक्ति-आदोलन भारतीय समाज में आन्तरिक एकता का संवाहक भी बन सका।
भक्ति-आन्दोलन के पीछे भारतवर्ष की आन्तरिक जीवनी शक्ति सक्रिय थी। वह एक विशाल या कहें अखिल भारतीय संस्कृति आन्दोलन था। ऐसे आन्दोलन को वेवर, ग्रियर्सन, भण्डारकर जैसे लोग यदि ईसाइयत की देन कहते हैं तो मानना पड़ेगा कि उनकी मान्यताएँ बेपर की उड़ान हैं। क्राइस्ट और कृष्ण के नाम-साम्य से किसी तरह की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले भारत में कृष्णाख्यान लोक में प्रचलित था। प्रसंगवश डॉक्टर रामचन्द्रतिवारी ने लिखा है-‘भक्ति-आन्दोलन में निहित प्रेम और समता की भावना का प्रेरक-स्त्रोत ईसाई धर्म को माना जाए तो घूम-फिरकर भारतवर्ष में ही लौट आना पड़ता है, क्योंकि ईसाई धर्म भी बौद्धधर्म से प्रभावित माना गया है। बौद्ध धर्मावलम्बियों और जैन व्यापारियों के अलेक्जेण्ड्रिया में बसने की बात बहुत पुरानी है। अशोक ने मेसी डोनिया में भी बौद्धभिक्षुओं को धर्म के प्रचारार्थ भेजा था। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक उदारता और सामाजिक सहिष्णुता ईसाई धर्म में पायी जाती है, वह वस्तुतः हमारे धर्मग्रन्थों में पहले ही प्रतिपादित हो चुकी थी। इस तथ्य की जानकारी के लिए एक ही पुस्तक दासगुप्ता की ‘द लिगेसी ऑफ इण्डिया’ का अध्ययन पर्याप्त है। अलवार भक्तों की प्रेम भावना को पुराणों में प्रतिपादित धर्मिक सहिष्णुता और सामाजिक उदभाव से जोड़कर लोकप्रिय रूप देने का श्रेय हिन्दी के सगुणोपासक कवियों को है। सूर, तुलसी जैसे महाकवियों की वाणी का जैसा असर जनमानस पर पड़ा, वैसा अन्य. कवियों का नहीं।’
सूर की काव्य-प्रतिभा से अभिभूत होकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ‘सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिकाव्य परम्परा का, चाहे वह मौखिक हो रही हो, पूर्ण-विकास-सा प्रतीत होता है।’ शुक्ल जी की इस स्थापना के आधार पर सूर से पहले के ब्रजभाषा काव्य की खोज की गयी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया कि ‘दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में भागवत परम्परा से भिन्न भी कोई लीला गान की शास्त्रीय परम्परा रही होगी। जयदेव का गीत ‘गीत-गोविन्द’ पूर्णरूप से भागवत परम्परा का ग्रन्थ नहीं है। उसमें प्रमुख गोपी राधा है, जो भागवत में अपरिचित हैं। इसके अतिरिक्त ‘गीत-गोविन्द’ का रास ‘वसन्त-रास’ है, जो भागवत का ‘शरद-रास’ नहीं। अतः ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि भारत वर्ष में लीला-गान की परम्परा कब शुरू हुई ? लेकिन दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में मात्रिक छन्दों में गेय पद लिखने की प्रथा चल रही थी। उन दिनों उड़ीसा में उड़िया भाषा में कष्ण-लीला के पद रचे जाते थे और सम्भवतः उड़िया लीला गान से प्रभावित होकर ही जयदेव ने ‘गीत-गोविन्द’ की रचना की होगी। जयदेव के उपरान्त लोक भाषा में गेय पदों का कृष्ण लीला-परक काव्य मिथिला के विद्यापति और बंगाल के चण्डीदास ने ही लिखा। इस तरह संक्षेप में कहें तो बौद्ध-सिद्धों के गान, जयदेव का ‘गीत-गोविन्द’ और चण्डीदास विद्यापति के पद कृष्णलीला-गान की परम्परा का समृद्ध करते हैं। बौद्ध-सिद्धों के गान में कृष्ण और राधा के प्रसंग नहीं आते, नहीं आ सकते थे, अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह मत समीचीन है कि विद्यापति पर गीत-गोविन्द का स्पष्ट भाव होने के कारण कृष्ण काव्य का सूत्र पात जयदेव से ही मानना चाहिए।’
जयदेव का रचना काल विक्रम की तेरहवीं शताब्दी सर्वमान्य है। उन्हें बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के दरबार में ‘राजकवि का सम्मान प्राप्त था। कवि के रूप में उनकी विश्वप्रसिद्धि का एक ही कारण है-उनकी अमर रचना ‘गीत-गोविन्द’। इसमें उन्होंने लिखा है।
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि
विलासकलासुकुतुहलम्।
मधुर कोमल कान्त पदावली श्रृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्।।
मधुर कोमल कान्त पदावली श्रृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्।।
अर्थात् ‘यदि हरि-स्मरण में मन सरस
हो, यदि विलास कला में
कुतूहल हो तो जयदेव की मधुर कोमल-कान्त पदावली को सुनो।’
हरि-स्मरण और विलास-कला दोनों का आनन्द एक साथगीत-गोविन्द को पढ़ने से
मिलता है। इसमें जयदेव ने राधा-कृष्ण का मिलन, कृष्ण की मधुर लीलाएँ और
प्रेम की मादक अनुभूति सरस और मधुर शब्दावली में लिखी है। गीत-गोविन्द की
सारी पदावली कोमल कान्त है और उनमें कामदेव के बाणों की मीठी पीड़ा
है।’ ए.बी. कीथ ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि जयदेव की पदावली
इतनी मधुर है और भावों के अनुकूल है कि इसका अनुवाद अन्य किसी भाषा में
ठीक से हो ही नहीं सकता। इसमें अनुप्रासों के सहारे जिस सफलता से
संकेत-व्यंजना की गयी है, वह अप्रतिम है। यथा।
ललित-लवंगलता-परिशीलन कोमलमलय समीरे।
मधुकर-निकर-करम्बित कोकिल कूजति कुंज-कुटीरे।।
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते।
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते।।
उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधूजन जनित विलापे।
अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे।।
मृगमद सौरभरभसवशंवद नवदलमाल तमाले।
युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किंशुक जाले।।
मदन महीपति कनकदण्डरुचि केसरकुसुम विकासे।
मिलित शिलीमुख पाटलिपटल कृतस्मरतूण विलासे ।।
मधुकर-निकर-करम्बित कोकिल कूजति कुंज-कुटीरे।।
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते।
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते।।
उन्मद मदन मनोरथ पथिक वधूजन जनित विलापे।
अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल बकुल कलापे।।
मृगमद सौरभरभसवशंवद नवदलमाल तमाले।
युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि किंशुक जाले।।
मदन महीपति कनकदण्डरुचि केसरकुसुम विकासे।
मिलित शिलीमुख पाटलिपटल कृतस्मरतूण विलासे ।।
गीत-गोविन्द को पं. विद्यानिवास मिश्र ने ठीक
ही एक नाट्य प्रबन्ध कहा
है-‘एक ऐसा नाट्य प्रबन्ध जिसमें कुल बारह सर्ग हैं। एक सर्ग
में कम-से-कम एक और अधिक-अधिक से चार अष्टपादियाँ हैं। प्रत्येक अष्टपादी
के अन्त में कथा-योजना सूत्र के रूप में अथवा आशीर्वचन के रूप में श्लोक
में वर्णित है। अष्टपदी की योजना इस प्रकार है कि यह गायी जा सके और उसके
साथ-साथ अभिनय भी प्रस्तुत हो।’ (साक्षात्कार, जनवरी-मार्च,
1988) गेयता और अभिनेयता की पारस्परिक अन्तरंगता ने
‘गीत-गोविन्द’ की भाषा को तरल और पारदर्शी बना दिया
है। ग्रन्थ-रचना का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि एक नयी राधा रची जाय
और उसकी रचना स्वंय कृष्ण करें, कुछ इस तरह कि वह काव्य की, वैष्णव भक्ति
की, कला और संगीत की अधिष्ठात्री बन जाए। जयदेव की कला अद्वितीया है,
जिसका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं। काल के प्रवाह में बड़े कवियों ने
राधा-कृष्ण सम्बन्धी कविताएँ लिखीं किन्तु जयदेव की किसी से तुलना नहीं की
जा सकती। अकेले मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि
मिली।
जयदेव के बाद कृष्ण-काव्य परम्परा में विद्यापति और चण्डीदास के पदों को व्यापक लोकप्रीयता मिली। इन कवियों में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को सम्पूर्ण भारत वर्ष में फैलाने में बड़ी भूमिका निभायी। चण्डीदास के पदों में राधा के अत्यन्त कोमल और सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है। जबकि विद्यापति में राधा अधिक विलासवती और विदिग्धा है। सुकुमार सेन के शब्दों में चण्डीदास की कृति ‘श्रीकृष्ण कीर्तन की संरचना सामान्य आख्यान काव्यों में सर्वथा भिन्न है। उनके काव्य का स्वर सर्वथा लौकिक है, जो प्राय: फूहड़पन और अश्लीलता की सीमा का स्पर्श करने लगता है।’ (बांग्ला साहित्य का इतिहास, पृ.76) चण्डीदास के आख्यान प्रसिद्ध पुराणों में नहीं मिलते। उनका काव्य स्वर सर्वथा मान है, आध्यात्मिक नहीं। यह भिन्न बात है कि ‘ कथ्य का वर्णन करते हुए, परम्परागत श्रृंगारिक रूढ़ियों पर चण्डीदास ने भी उसी तरह बल दिया है, जिस तरह जयदेव ने गीत-गोविन्द में।’ चण्डीदास से सर्वथा अलग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक् हैं। उनकी पदावली में राधा और कृष्ण की जिस प्रेम-लीला का चित्रण हुआ है, वह अपूर्व है। विद्यापति के वर्णनों में शरीर पक्ष प्रधान अवश्य है किन्तु वह चित्त में विकार नहीं उत्पन्न करता, बल्कि भावों की सान्द्रता और अभिव्यक्ति की प्रेषण-क्षमता के कारण विद्यापति की पदावली अत्यधिक लोकप्रिय हुई। डॉक्टर मैंनेजर पाण्डेय लिखते हैं’-महाकवि विद्यापति मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जनसंस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। ‘विद्यापति अपभ्रंश काव्य-परम्परा के अन्तिम कवि हैं और लोकभाषा मैथली के प्रथम महाकवि। विद्यापति और चण्डीदास के पदों को चैतन्य महाप्रभु तन्मय और भाव-विभोर होकर गाते थे, यह एक तथ्य है जिसे सब जानते हैं।
चैतन्य के समानान्तर कृष्ण भक्ति काव्य के मूल स्त्रोत श्रीमद भागवत के भी अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए। यहाँ अनुवाद से अभिप्राय है-काव्यानुवाद। असमिया के कवि शंकरदेव (15 वीं सदी), उड़िया के जगन्नाथ, तेलगू के पोतनात्य, गुजराती के भालण आदि ने श्रीमदभागवत के जो काव्यानुवाद किये, वे उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गुजरात लंबे समय तक कृष्ण भक्ति का केन्द्र बना रहा। वहाँ के प्रसिद्ध कवि बिल्व मंगल (1250-1350) ने’ बाल-गोपाल स्तुति‘ और ‘कृष्ण कर्णामूत’ की रचना की और सम्पूर्ण गुजरात में कृष्ण-भक्ति की धारा प्रवाहित की। गुजरात के प्रसिद्ध कवि नरसी मेहता ने सम्पूर्ण कृष्ण-लीला को ही अपने काव्य का विषय बनाया। उन्होंने बाल-गोपाल के पद भी बनाए। ब्रजभाषा के जैन कवि साधार अग्रवाल का ‘प्रद्युम्नचरित’ एक प्राचीन रचना है। सूर-पूर्व कवियों ने विष्णुदास ने भी कृष्ण-लीला-विषयक गान की रचना की थी।
हिन्दी में कृष्ण भक्ति काव्य को सबसे अधिक निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य से ही मिली। इन महात्माओं ने राधा-कृष्ण की भक्ति को एक व्यवस्थित और सुसंगत दार्शनिक आधार दिया, जिससे भक्ति-आन्दोलन की जड़ें परिपुष्ट हुईं। निम्बार्क में ‘दशश्लोकी’ में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने कृष्ण को सर्वोपरि ब्रह्म कहा। वे अरविन्द नयन और व्यूह अवयवी हैं। वे कल्याण-राशि और सब प्रकार से दोष-मुक्त हैं। वृषभानुजा राधा निम्बार्क की दृष्टि में सौन्दर्य-ज्योति-पुंज हैं। श्रीकृष्ण उनके वामाग में विराजमान हैं। अपनी छवि-द्युति से वे आलोक-पुंद विकीर्ण करती हैं। सहस्त्रों सखियाँ उनकी सेवा में तत्पर हैं। राधा मनोवांछित वस्तु प्रदात्री हैं। उनके पादारविन्द की अर्चना-सेवा से ही मुक्ति सम्भव है और श्रीकृष्ण की आराधना ब्रम्हा और शिव भी करते हैं। इस तरह निम्बार्क दर्शन में राधा-कृष्ण को अनुभूति के साथ-साथ ज्ञान और भक्ति का विषय भी बनाया गया।
निम्बार्क के नाम से जो सम्प्रदाय चला, उसमें ब्रजभाषा के आदि कवि श्री भट्ट हुए। उन्होंने ‘युगल शतक’ की रचना की। चैतन्य महाप्रभु (1485-1533) तो भावुकता और आत्मिक उल्लास की प्रतिमूर्त्ति ही थे। चैतन्य का लिखा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। उनके केवल आठ श्लोक ही उपलब्ध हैं। परन्तु उनके विचारों को श्रीकृष्णदास रचित ‘चैतन्य-चरितामृत’ में पल्लवित किया गया है। कालान्तर में रूप जीव और सनातन गोस्वामियों ने अपने-अपने ग्रन्थों में चैतन्य-चरित-प्रकाश किया है। चैतन्य के विचारों का सार यह है कि श्रीकृष्ण देवाधिदेव हैं। वे मूर्तिमान सौन्दर्य हैं, प्रेमपरक है। उनकी तीन शक्तियाँ हैं-(1) परम ब्रह्म शक्ति, (2) माया शक्ति और (3) विलास शक्ति। विलास शक्तियाँ दो हैं-(क) प्राभव विलास-जिसके माध्यम से श्रीकृष्ण एक से अनेक होकर गोपियों से क्रीड़ा करते हैं। (ख) वैभव-विलास-जिसके द्वारा वे चतुर्व्यूह का रूप धारण करते है। चैतन्य मत के व्यूह-सिद्धान्त का आधार प्रेम और लीला है। श्रीकृष्ण लीला गोलोक में नित्य है। उनकी मूल शक्ति प्रेम है और वही आनन्द का कारण है। यही प्रेम भक्त के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। महाभाव ही राधा है। राधा ही कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम का आलम्बन हैं। वही उनके प्रेम की आदर्श प्रतिमा है। गोपी-कृष्ण-लीला प्रेम का प्रतिफल है।
चैतन्य निम्बार्क की तुलना में वल्लभाचार्य का मत अधिक व्यवस्थित है। उनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत और भक्ति-सिद्धान्त पुष्टि-मार्ग कहा गया है। वल्लभाचार्य के ग्रन्थों में प्रमुख हैं-(1) पूर्व मीमांसा-भाष्य, (2) उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य, (3) भागवत की सूक्ष्म और सुबोधिनी टीका और (4) तत्त्वदीप-निबन्ध। वल्लभमत में भी श्रीकृष्ण ही को सर्वोच्च ब्रह्म माना गया है। वे सच्चिदानन्द हैं, पुरुषोत्तम हैं। भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह आवश्यक है। महापुष्टि ईश्वर प्राप्ति की बाधाओं का परिहार करती हैं। ईश्वर के अनुग्रह से ही प्रेमाभक्ति की उपलब्धि होती है। प्रेमाभक्ति की तीन अवस्थाएँ हैं-(1) प्रेम, (2) आसक्ति और (3) व्यसन। राधा-कृष्ण की लीला में प्रवेश ही भक्ति का लक्ष्य है और यह भगवान के अनुग्रह से ही सम्भव है।
निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य ने कुल मिलाकर राधावल्लभ कृष्ण के जिस स्वरूप की दार्शनिक मीमांसा की, रूपगोस्वामी ने उसी की भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया ‘उज्ज्वल नीलमणि’ तथा ‘भक्ति रसामृतसिन्धु’ में। उन्होंने काव्य-रस और भक्ति-रस का सम्बन्ध भी स्पष्ट किया। काव्य-रस के भीतर कृष्ण नायक है और राधा नायिका। भागवत विषयक रति स्थायी भाव है और उसी से शान्ति, प्रीति, सख्य या प्रेयस, वात्सल्य या अनुकम्पा और कान्ता का मधुरा पाँच प्रकार के रस-निष्पन्न होते हैं। आनन्दमय मधुर रस या उज्ज्वल रस ही श्रेष्ठ है, वही भक्ति-रस है।
इस तरह निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति काव्य की वैचारिक-दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। महाकवि सूर ने उसी के आधार पर काव्योत्कर्ष का अप्रतिम प्रतिमान स्थापित किया। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बने। उम्र में अपने गुरु से वे कुल दस दिन छोटे थे। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पहले ही कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी थी। मथुरा, वृन्दावन के बीच गऊ घाट पर सूरदास भजन गाया करते थे। वैष्णव धर्म के दिग्विजय-अभियान में निकले वल्लभाचार्य जब गऊ घाट पर पहुँचे, तब उनका आदेश पाकर सूर ने स्वरचित पद सुनाया-‘प्रभु हौं सब पतिनन को टीको।’ इसे सुनकर वल्लभाचार्य जी ने कहा-‘सूर ह्वै कै ऐसो घिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करि।’ पूछने पर उन्होंने सूरदास जी को श्रीमद भागवत के दशम् स्कन्ध की अनुक्रमणिका बतायी और तब से महाकवि आजीवन श्रीकृष्णलीला के पद बनाते रहे। सूर के जन्मान्ध होने को लेकर विवाद है। उनका जीवन-वृत्त और रचनाएँ विवाद के घेरे में हैं। ‘साहित्य-लहरी’, सूर-सारावली’ आदि भी उन्हीं की कृतियाँ हैं, लेकिन सूरदास की वास्तविक प्रतिष्ठा का आधार उनकी एकमात्र कृति ‘सूरसागर’ ही है।
प्रसंगवश, शुक्ल जी ने लिखा है-‘जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयुष-धारा, जो काल की कठोरता में दब गयी थी, अवकाश पाते ही लोकभाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल-कण्ठ से प्रकट हुई और आगे चलकर व्रज के करील कुंजो के बीच मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर झंकार अन्धे कवि सूरदास की वीणा की थी।’ सूर की सीमा ही विशिष्टता है। उनका अनुभूति क्षेत्र सीमित है। वात्सल्य और श्रृंगार इन्हीं दोनों रसों में उनकी गति है। इन क्षेत्रो का वे कोना-कोना झाँक आए हैं। ‘बाल्य-काल और यौवन-काल कितने मनोहर होते हैं, उनके बीच की नाना मनोहर परिस्थितियों के विराट् चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उदघाटन सूर ने अपनी बन्द आँखों से किया है, उतना अन्य कवि ने नहीं।’ इन दोनों रसों के प्रवर्तक रतिभाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और पत्यक्षीकरण सूरदास जी कर सके उतनी का और कोई नहीं। शुक्ल जी की शब्दावली है-‘हिन्दी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व य
जयदेव के बाद कृष्ण-काव्य परम्परा में विद्यापति और चण्डीदास के पदों को व्यापक लोकप्रीयता मिली। इन कवियों में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन को सम्पूर्ण भारत वर्ष में फैलाने में बड़ी भूमिका निभायी। चण्डीदास के पदों में राधा के अत्यन्त कोमल और सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है। जबकि विद्यापति में राधा अधिक विलासवती और विदिग्धा है। सुकुमार सेन के शब्दों में चण्डीदास की कृति ‘श्रीकृष्ण कीर्तन की संरचना सामान्य आख्यान काव्यों में सर्वथा भिन्न है। उनके काव्य का स्वर सर्वथा लौकिक है, जो प्राय: फूहड़पन और अश्लीलता की सीमा का स्पर्श करने लगता है।’ (बांग्ला साहित्य का इतिहास, पृ.76) चण्डीदास के आख्यान प्रसिद्ध पुराणों में नहीं मिलते। उनका काव्य स्वर सर्वथा मान है, आध्यात्मिक नहीं। यह भिन्न बात है कि ‘ कथ्य का वर्णन करते हुए, परम्परागत श्रृंगारिक रूढ़ियों पर चण्डीदास ने भी उसी तरह बल दिया है, जिस तरह जयदेव ने गीत-गोविन्द में।’ चण्डीदास से सर्वथा अलग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक् हैं। उनकी पदावली में राधा और कृष्ण की जिस प्रेम-लीला का चित्रण हुआ है, वह अपूर्व है। विद्यापति के वर्णनों में शरीर पक्ष प्रधान अवश्य है किन्तु वह चित्त में विकार नहीं उत्पन्न करता, बल्कि भावों की सान्द्रता और अभिव्यक्ति की प्रेषण-क्षमता के कारण विद्यापति की पदावली अत्यधिक लोकप्रिय हुई। डॉक्टर मैंनेजर पाण्डेय लिखते हैं’-महाकवि विद्यापति मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जनसंस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। ‘विद्यापति अपभ्रंश काव्य-परम्परा के अन्तिम कवि हैं और लोकभाषा मैथली के प्रथम महाकवि। विद्यापति और चण्डीदास के पदों को चैतन्य महाप्रभु तन्मय और भाव-विभोर होकर गाते थे, यह एक तथ्य है जिसे सब जानते हैं।
चैतन्य के समानान्तर कृष्ण भक्ति काव्य के मूल स्त्रोत श्रीमद भागवत के भी अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए। यहाँ अनुवाद से अभिप्राय है-काव्यानुवाद। असमिया के कवि शंकरदेव (15 वीं सदी), उड़िया के जगन्नाथ, तेलगू के पोतनात्य, गुजराती के भालण आदि ने श्रीमदभागवत के जो काव्यानुवाद किये, वे उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गुजरात लंबे समय तक कृष्ण भक्ति का केन्द्र बना रहा। वहाँ के प्रसिद्ध कवि बिल्व मंगल (1250-1350) ने’ बाल-गोपाल स्तुति‘ और ‘कृष्ण कर्णामूत’ की रचना की और सम्पूर्ण गुजरात में कृष्ण-भक्ति की धारा प्रवाहित की। गुजरात के प्रसिद्ध कवि नरसी मेहता ने सम्पूर्ण कृष्ण-लीला को ही अपने काव्य का विषय बनाया। उन्होंने बाल-गोपाल के पद भी बनाए। ब्रजभाषा के जैन कवि साधार अग्रवाल का ‘प्रद्युम्नचरित’ एक प्राचीन रचना है। सूर-पूर्व कवियों ने विष्णुदास ने भी कृष्ण-लीला-विषयक गान की रचना की थी।
हिन्दी में कृष्ण भक्ति काव्य को सबसे अधिक निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य से ही मिली। इन महात्माओं ने राधा-कृष्ण की भक्ति को एक व्यवस्थित और सुसंगत दार्शनिक आधार दिया, जिससे भक्ति-आन्दोलन की जड़ें परिपुष्ट हुईं। निम्बार्क में ‘दशश्लोकी’ में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने कृष्ण को सर्वोपरि ब्रह्म कहा। वे अरविन्द नयन और व्यूह अवयवी हैं। वे कल्याण-राशि और सब प्रकार से दोष-मुक्त हैं। वृषभानुजा राधा निम्बार्क की दृष्टि में सौन्दर्य-ज्योति-पुंज हैं। श्रीकृष्ण उनके वामाग में विराजमान हैं। अपनी छवि-द्युति से वे आलोक-पुंद विकीर्ण करती हैं। सहस्त्रों सखियाँ उनकी सेवा में तत्पर हैं। राधा मनोवांछित वस्तु प्रदात्री हैं। उनके पादारविन्द की अर्चना-सेवा से ही मुक्ति सम्भव है और श्रीकृष्ण की आराधना ब्रम्हा और शिव भी करते हैं। इस तरह निम्बार्क दर्शन में राधा-कृष्ण को अनुभूति के साथ-साथ ज्ञान और भक्ति का विषय भी बनाया गया।
निम्बार्क के नाम से जो सम्प्रदाय चला, उसमें ब्रजभाषा के आदि कवि श्री भट्ट हुए। उन्होंने ‘युगल शतक’ की रचना की। चैतन्य महाप्रभु (1485-1533) तो भावुकता और आत्मिक उल्लास की प्रतिमूर्त्ति ही थे। चैतन्य का लिखा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। उनके केवल आठ श्लोक ही उपलब्ध हैं। परन्तु उनके विचारों को श्रीकृष्णदास रचित ‘चैतन्य-चरितामृत’ में पल्लवित किया गया है। कालान्तर में रूप जीव और सनातन गोस्वामियों ने अपने-अपने ग्रन्थों में चैतन्य-चरित-प्रकाश किया है। चैतन्य के विचारों का सार यह है कि श्रीकृष्ण देवाधिदेव हैं। वे मूर्तिमान सौन्दर्य हैं, प्रेमपरक है। उनकी तीन शक्तियाँ हैं-(1) परम ब्रह्म शक्ति, (2) माया शक्ति और (3) विलास शक्ति। विलास शक्तियाँ दो हैं-(क) प्राभव विलास-जिसके माध्यम से श्रीकृष्ण एक से अनेक होकर गोपियों से क्रीड़ा करते हैं। (ख) वैभव-विलास-जिसके द्वारा वे चतुर्व्यूह का रूप धारण करते है। चैतन्य मत के व्यूह-सिद्धान्त का आधार प्रेम और लीला है। श्रीकृष्ण लीला गोलोक में नित्य है। उनकी मूल शक्ति प्रेम है और वही आनन्द का कारण है। यही प्रेम भक्त के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। महाभाव ही राधा है। राधा ही कृष्ण के सर्वोच्च प्रेम का आलम्बन हैं। वही उनके प्रेम की आदर्श प्रतिमा है। गोपी-कृष्ण-लीला प्रेम का प्रतिफल है।
चैतन्य निम्बार्क की तुलना में वल्लभाचार्य का मत अधिक व्यवस्थित है। उनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैत और भक्ति-सिद्धान्त पुष्टि-मार्ग कहा गया है। वल्लभाचार्य के ग्रन्थों में प्रमुख हैं-(1) पूर्व मीमांसा-भाष्य, (2) उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य, (3) भागवत की सूक्ष्म और सुबोधिनी टीका और (4) तत्त्वदीप-निबन्ध। वल्लभमत में भी श्रीकृष्ण ही को सर्वोच्च ब्रह्म माना गया है। वे सच्चिदानन्द हैं, पुरुषोत्तम हैं। भक्ति के लिए भगवान का अनुग्रह आवश्यक है। महापुष्टि ईश्वर प्राप्ति की बाधाओं का परिहार करती हैं। ईश्वर के अनुग्रह से ही प्रेमाभक्ति की उपलब्धि होती है। प्रेमाभक्ति की तीन अवस्थाएँ हैं-(1) प्रेम, (2) आसक्ति और (3) व्यसन। राधा-कृष्ण की लीला में प्रवेश ही भक्ति का लक्ष्य है और यह भगवान के अनुग्रह से ही सम्भव है।
निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य ने कुल मिलाकर राधावल्लभ कृष्ण के जिस स्वरूप की दार्शनिक मीमांसा की, रूपगोस्वामी ने उसी की भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया ‘उज्ज्वल नीलमणि’ तथा ‘भक्ति रसामृतसिन्धु’ में। उन्होंने काव्य-रस और भक्ति-रस का सम्बन्ध भी स्पष्ट किया। काव्य-रस के भीतर कृष्ण नायक है और राधा नायिका। भागवत विषयक रति स्थायी भाव है और उसी से शान्ति, प्रीति, सख्य या प्रेयस, वात्सल्य या अनुकम्पा और कान्ता का मधुरा पाँच प्रकार के रस-निष्पन्न होते हैं। आनन्दमय मधुर रस या उज्ज्वल रस ही श्रेष्ठ है, वही भक्ति-रस है।
इस तरह निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति काव्य की वैचारिक-दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। महाकवि सूर ने उसी के आधार पर काव्योत्कर्ष का अप्रतिम प्रतिमान स्थापित किया। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बने। उम्र में अपने गुरु से वे कुल दस दिन छोटे थे। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के पहले ही कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी थी। मथुरा, वृन्दावन के बीच गऊ घाट पर सूरदास भजन गाया करते थे। वैष्णव धर्म के दिग्विजय-अभियान में निकले वल्लभाचार्य जब गऊ घाट पर पहुँचे, तब उनका आदेश पाकर सूर ने स्वरचित पद सुनाया-‘प्रभु हौं सब पतिनन को टीको।’ इसे सुनकर वल्लभाचार्य जी ने कहा-‘सूर ह्वै कै ऐसो घिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करि।’ पूछने पर उन्होंने सूरदास जी को श्रीमद भागवत के दशम् स्कन्ध की अनुक्रमणिका बतायी और तब से महाकवि आजीवन श्रीकृष्णलीला के पद बनाते रहे। सूर के जन्मान्ध होने को लेकर विवाद है। उनका जीवन-वृत्त और रचनाएँ विवाद के घेरे में हैं। ‘साहित्य-लहरी’, सूर-सारावली’ आदि भी उन्हीं की कृतियाँ हैं, लेकिन सूरदास की वास्तविक प्रतिष्ठा का आधार उनकी एकमात्र कृति ‘सूरसागर’ ही है।
प्रसंगवश, शुक्ल जी ने लिखा है-‘जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयुष-धारा, जो काल की कठोरता में दब गयी थी, अवकाश पाते ही लोकभाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल-कण्ठ से प्रकट हुई और आगे चलकर व्रज के करील कुंजो के बीच मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएँ श्रीकृष्ण की प्रेमलीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर झंकार अन्धे कवि सूरदास की वीणा की थी।’ सूर की सीमा ही विशिष्टता है। उनका अनुभूति क्षेत्र सीमित है। वात्सल्य और श्रृंगार इन्हीं दोनों रसों में उनकी गति है। इन क्षेत्रो का वे कोना-कोना झाँक आए हैं। ‘बाल्य-काल और यौवन-काल कितने मनोहर होते हैं, उनके बीच की नाना मनोहर परिस्थितियों के विराट् चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उदघाटन सूर ने अपनी बन्द आँखों से किया है, उतना अन्य कवि ने नहीं।’ इन दोनों रसों के प्रवर्तक रतिभाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और पत्यक्षीकरण सूरदास जी कर सके उतनी का और कोई नहीं। शुक्ल जी की शब्दावली है-‘हिन्दी साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व य
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book